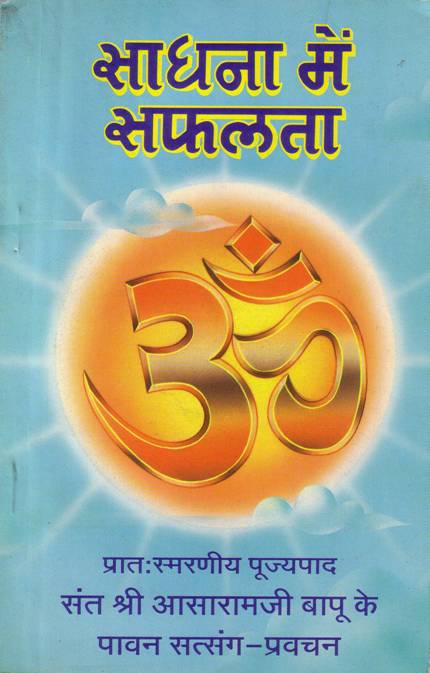
प्रातःस्मरणीय
पूज्यपाद संत
श्री आसारामजी
बापू के
सत्संग-प्रवचन
साधना
में सफलता
हम धनवान होंगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं इसमें शंका हो सकती है परंतु भैया ! हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है? विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है परंतु इस जीवन की गाड़ी छूटने का कोई निश्चित समय है?
आज तक आपने जगत में जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है.... आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे, प्यारे भैया ! वह सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जायेगा, जाना अनजाना हो जायेगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जायेगी।
अतः सावधान हो जाओ। अन्तर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, निजस्वरूप के अगाध आनन्द को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो।
जागो.... उठो.... अपने भीतर सोये हुए निश्चयबल को जगाओ। सर्वदेश, सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीन-हीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके।
सदा स्मरण रहे कि इधर-उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना-काल में आत्मचिन्तन में लगाओ और व्यवहार-काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शान्त वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवन्त एवं प्रसन्न रहो। जीवमात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो। दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठ में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग एवं सत्साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदान्त से पुष्ट एवं पुलकित करो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
निवेदन
इस पुस्तक में साधना में आरूढ़ साधक के लिए आवश्यक सूचनाएँ एवं मार्गदर्शन दिया गया है। गीता के श्लोकों पर पूज्यश्री की अनुभव-संपन्न सरल वाणी के सहज प्रवचन लिपिबद्ध किए गये हैं। हतोत्साह अथवा बिखरी हुई साधनावाला साधक भी मार्गदर्शन पाकर नया उत्साह, नयी प्रेरणा और सहज सुलभ साधन और चिन्तन-प्रणालिका पाकर अपने परमात्मदेव का अनुभव कर सकता है और जनसाधारण भी इस पुस्तक से अपनी आध्यात्मिक प्यास जगाकर परमात्म-प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ें ऐसी सरल भाषा में संतों के प्रवचन और मार्गदर्शन प्रस्तुत किये गये हैं।
विघ्नों और संघर्षों से भरा हुआ अल्प जीवन शीघ्र ही जीवनदाता को पा सके ऐसे मार्गदर्शनवाली पुस्तक जनता जनार्दन के करकमलों तक पहुँचाने के सेवा का सुअवसर पाकर समिति धन्यता महसूस करती है।
साधकों से और जनता-जनार्दन से विनंति है कि अनुभव-संपन्न इस पावन प्रसाद को अपने अन्य साधक बन्धुओं और मित्रों तक पहुँचाकर पुण्य के भागी बनें।
यह प्रकाशन पढ़कर सूक्ष्म मनन करने वाले साधक अपने सुझाव समिति को भेजने की कृपा कर सकते हैं।
श्री
योग वेदान्त
सेवा समिति
अमदावाद
आश्रम
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
घोर
क्लेश में भी
सत्पथ पर
अडिगता
गुरु
में
ईश्वर-बुद्धि
होने के उपाय
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
साधना
में सफलता
विषय सुख की लोलुपता आत्मसुख प्रकट नहीं होने देती। सुख की लालच और दुःख के भय ने अन्तःकरण को मलिन कर दिया। तीव्र विवेक-वैराग्य हो, अन्तःकरण के साथ का तादात्म्य तोड़ने का सामर्थ्य हो तो अपने नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, व्यापक चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाय। वास्तव में हम बोध स्वरूप हैं लेकिन शरीर और अन्तःकरण के साथ जुड़े हैं। उस भूल को मिटाने के लिए, सुख की लालच को मिटाने के लिए, दुःखियों के दुःख से हृदय हराभरा होना चाहिए। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसे निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करने पर फिर नितान्त एकान्त की आवश्यकता है।
आरुरुक्षार्मुनेर्योगं
कर्म कारणमुच्यते।
योगारूढस्य
तस्यैव शमः
कारणमुच्यते।।
'योग में आरूढ़ होने की इच्छावाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है।'
(भगवद्
गीताः 6.3)
एकान्त में शुभ-अशुभ सब संकल्पों का त्याग करके अपने सच्चिदानंद परमात्मस्वरूप में स्थिर होना चाहिए। घोड़े के रकाब में पैर डाल दिया तो दूसरा पैर भी जमीन से उठा लेना पड़ता है। ऐसे ही सुख की लालच मिटाने के लिए यथायोग्य निष्काम कर्म करने के बाद निष्काम कर्मों से भी समय बचाकर एकान्तवास, लघु भोजन, देखना, सुनना आदि इन्द्रियों के अल्प आहार करते हुए साधक को कठोर साधना में उत्साहपूर्वक संलग्न हो जाना चाहिए। कुछ महीने बंद कमरे में एकाकी रहने से धारणा तथा ध्यान की शक्ति बढ़ जाती है। आन्तर आराम, आन्तर सुख, आन्तरिक प्रकट होने लगता है। धारणा ध्यान में परिणत होती है।
जब तक परम पद की प्राप्ति न हो तब तक हे साधक ! खूब सावधान रहना। एक प्रकार से आपके माने हुए मित्र, भगत आपके गहरे शत्रु हैं। किसी न किसी प्रकार आपको संसार में, नाम-रूप की सत्यता में घसीट लाते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म वृत्ति उनके परिचय में आने से फिर स्थूल होने लगती है और तुम्हें ज्ञात भी नहीं होता।
सावधान ! ये मित्र और भगत भी गहरे शत्रु हैं। इन सांसारिक व्यक्तियों के मिलने जुलने के कारण आपके नये आध्यात्मिक संस्कार और ध्यान की एकाग्रता लुप्त हो जायेगी। कभी-कभी अपने मन की बेवकूफी साधन-भजन के समय में लापरवाही कराने लगेगी। संसारी लोगों से मिलना-जुलना साधनाकाल में बहुत ही अनर्थकारी है। दोनों कि विचारधाराएँ उत्तर दक्षिण हैं। संसारी व्यक्ति बातचीत करने का शौकीन होता है। नश्वर भोग-प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है। साधक का लक्ष्य शाश्वत परमात्मा होता है। संसारी व्यक्ति की बातचीत का फल किसी के प्रति राग या द्वेष होता है। संसारियों के साथ बातें करने से राग, द्वेष और जगत की सत्यता दृढ़ होने लगती है। संसारी व्यक्ति जिह्वा के अतिसार से पीड़ित होता है। गपशप, व्यर्थ की बातें, बे-सिरपैर की बातें, लम्बी बातें, बड़ी बातें ये सब उसे सुखद लगती हैं। जबकि साधक मितभाषी, आध्यात्मिक विषय पर ही प्रसंग के अनुसार बोलनेवाला होता है। उसे संसारी बातों में रूचि नहीं और साधना-काल में सांसारिक बातों में उसे पीड़ा भी होती है लेकिन नैतिक भावों से प्रभावित होकर अपनी आन्तर पुकार के विपरीत भी वह संसार की हाँ में हाँ करने लगे अथवा उनके संपर्क में आकर बलात् संसार में खिंच जाये तो उसकी महीनों की कठोर साधना के द्वारा प्राप्त योगारूढ़ता क्षीण होने लगती है। दोनों की चिन्तन-विधि भी परस्पर भिन्न होती है। संसारी व्यक्ति की चिन्तनधारा का विषय पत्नी, संतान, धन संचित करने का उपाय, मित्र और शत्रु, राग-द्वेष होता है। उसका लक्ष्य ऐन्द्रिक सुखों का साधन होता है। उसका चिन्तन बहुत ही तुच्छ होता है। साधक का चिन्तन दिव्य होता है। 'संकल्प-विकल्प मन में उठते हैं उससे परे उसके साक्षी ब्रह्मस्वरूप परमात्मा में स्थिति कैसे हो?' आदि का अर्थात् परमात्म-विश्रान्ति विषयक उसका चिन्तन होता है। संसारी व्यक्ति सदा स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कार्य करता है, अहंकार सजाने के लिए कार्य करता है जबकि साधक समग्र संसार को अपना स्वरूप समझकर निःस्वार्थ भाव से, अहंकार विसर्जित करते हुए कार्य करता है। संसारी व्यक्ति के पास जो भाग-सामग्री है उसे वह बढ़ाना चाहता है और भविष्य में भी ऐन्द्रिक सुखों की सुव्यवस्था रखता है। साधक सारे ऐन्द्रिक विषय व्यर्थ समझकर इन्द्रियातीत, देशातीत, कालातीत, गुणातीत, आत्मसुख, परमात्म-स्थिति चाहता है। संसारी व्यक्ति जटिलता, बहुलता, रोगों के घर देह और क्षणभंगुर भोग और सुख की तुच्छ लालच में मँडराता है जबकि साधक सरल व्यक्ति होता है। देह से और तुच्छ भोगों से पार आत्मसुख का अभिलाषी होता है। संसारी व्यक्ति संगति खोजता है, साधक सर्वथा एकान्त पसंद करता है।
हे साधक ! तथा कथित मित्रों से, सांसारिक व्यक्तियों से अपने को बचाकर सदा एकाकी रहना। यह तेरी साधना की परम माँग है।
स्वामी रामतीर्थ प्रार्थना किया करते थेः
"हे प्रभु ! मुझे सुखों से और मित्रों से बचाओ। दुःखों से और शत्रुओं से मैं निपट लूँगा। सुख और मित्र मेरा समय व शक्ति बरबाद कर देते हैं और आसक्ति पैदा करते हैं। दुःखों में और शत्रुओं में कभी आसक्ति नहीं होती।
जब-जब साधक गिरे हैं तो तुच्छ सुखों और मित्रों के द्वारा ही गिरे हैं।
भैया ! सावधान ! एकान्तवास नितान्त आवश्यक है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए एकान्तवास साधना की एक महान् माँग है, अनिवार्य आवश्यकता है। आप एक बार एकान्त का सुख भली प्रकार प्राप्त कर लें तो फिर आप उस पावन एकान्त के बिना नहीं रह सकते।
जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य नहीं जाना, जिनमें विषय वासना की प्रबलता होती है वे ही निरंकुश बन्दर की तरह एक डाल से दूसरी डाल, कभी काशी कभी मथुरा, कभी डाकोर तो कभी रामेश्वर, कभी गुप्तकाशी तो कभी गंगोत्री, इधर से उधर घूमते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बहिरंग दौड़-धूप में शक्ति और एकाग्रता क्षीण होती है।
उत्तरकाशी, वाराणसी, रामेश्वर और गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी के तट पर पवित्र स्थानों के इर्दगिर्द प्रकृति के सुरम्य वातावरण में, अरण्य में, नदी, सरोवर, सागरतट अथवा पहाड़ों में, जहाँ पूर्वकाल में ऋषि, मुनि या संत निवास कर चुके हैं ऐसे पवित्र स्थानों की महिमा का पता सूक्ष्म साधना करने वाले साधकों को ही चल सकता है। महापुरुषों के आध्यात्मिक स्पन्दनवाले स्थान साधक को बहुत सहाय करते हैं। हिमालय और गंगातट जैसे पावन स्थानों में कुछ महीने रहकर अथवा अपने अनूकूल किसी एकान्त कमरे में लोकसंपर्करहित होकर अपनी धारणा तथा ध्यानशक्ति बढ़ायें और बड़ी सावधानीपूर्वक उस एकाग्रता का संरक्षण करें। यदि आप अपनी रक्षा करनी नहीं जानते तो आपका मूल्यवाण प्राण, चुम्बकीय शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति और प्राणशक्ति आपसे मिलनेवाले लोगों के प्रति चली जायेगी। आपको एक शक्ति-कवच बना लेना चाहिए। जो उन्नत साधक हों, ज्ञान-वैराग्य-भक्ति से भरे दिलवाले हों, उनके साथ प्रतिदिन एक घण्टा मिलना-जुलना, विचार विमर्श करना हानिकारक नहीं है। आपके हृदय में पता चलेगा कि किन व्यक्तियों से मिलने जुलने में वैराग्य बढ़ता है, प्रसन्नता, शान्ति बढ़ती है और किन लोगों से मिलने में आपके आध्यात्मिक संस्कार व शान्ति क्षीण होती है। संसारी आकांक्षाओंवाले लोगों के बीच अगर आना ही पड़े तो मौन का अवलम्बन लेना, अपनी साधना का प्रभाव छुपाना और उनके बीच जब हो तो जिह्वा तालू में लगाये रखना। इससे तुम्हारी शक्ति क्षीण होने से बच जायेगी। उनकी बातें कम से कम सुनना, युक्तिपूर्वक उनसे अपने को बचा लेना।
कभी-कभी अपना मन भी मनोराज करके हवाई किले बाँधने लगता है। साधनाकाल में बड़े प्रचार-प्रसार का और प्रसिद्ध होने का, लोक-कल्याण करने आदि का तूफान मचाया करता है। यह नितान्त हानिकर्ता है। उस समय परमात्मा को सच्चे हृदय से प्यार करें, प्रार्थना करें किः "हे प्रभो ! अहंकार बढ़ाने की मिथ्या नाम रूप की प्रसिद्धि विषयक तुच्छ वासनाएँ मुझे तुमसे मिलने में बाधा कर रहीं हैं। हे नाथ ! हे सर्वनियन्ता ! हे जगदीश्वर ! हे अन्तर्यामी ! मेरी इस निम्न प्रकृति को तू अपने आपमें पावन कर दे। मैं तेरे साथ अभिन्न हो जाऊँ। कहीं ये तुच्छ संकल्प-विकल्प पूरे करने में नया प्रारब्ध न बन जाये, नयी मुसीबतें खड़ी न हो जाय।"
इस प्रकार शुद्ध भाव करके निःसंकल्प, निश्चिन्तमना होकर समाधिस्थ होइये। संकल्प का विस्तार नहीं, संकल्प की पूर्ति नहीं लेकिन संकल्प की निवृत्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वह दशा आने से वास्तव में सुधार-कार्य आपके द्वारा होने लगेंगे और आपको कोई हानि नहीं होगी।
निःसंकल्प ब्रह्म है। संकल्प के पीछे भागना तुच्छ जीव होना है। जो-जो भगीरथ कार्य हुए हैं वे निःसंकल्प अवस्था में पहुँचे हुए महापुरुषों के द्वारा ही हुए हैं। परमात्मा की इस विराट सृष्टि में हमारा मन अपनी कल्पना से सुधारना आदि करने का जाल बुनकर हमें फँसाता है। उस समय 'हरिः ॐ तत्सत् और सब गपशप...। आनन्दोऽहम्.... सर्वोऽहम्.... शिवरूपोऽहम्.... कल्याण-स्वरूपोऽहम्.... मायातीतो-गुणातीतो शान्तशिवस्वरूपोऽहम्....' इस प्रकार अपने शिवस्वरूप में, शान्त स्वरूप में मस्त हो जाना चाहिए।
हताशा, निराशा के विचारों को महत्त्व नहीं देना चाहिए। हजार बार मनोराज होने की, पीछे हटने की संभावना है लेकिन हर समय नया उत्साह, सर्वशक्तिदायी प्रणव का जाप, आत्मबल और परमात्म-प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए।
बन्द कमरे में शुद्ध भाव से अपने अन्तर्यामी प्रभु से, इष्ट से, गुरु से प्यार करके प्रेरणा पाते रहना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता सत्पुरुषों के जीवन-चरित्र और अनुभव-वचनवाले ग्रन्थों का बार-बार अवलोकन करना चाहिए। वास्तव मे देखा जाये तो परमात्म-प्राप्ति कठिन नहीं है लेकिन जब मन और मन की बुनी हुई जालों में फँसते हैं तो कठिन हो जाता है। मन-बुद्धि से परे अपने सूक्ष्म, शुद्ध, 'मैं' को देखो तो नितान्त सरल और सहज सदैव-प्राप्त परमात्मा मिलेगा। तुम्हीं तो वह परब्रह्म परमात्मा हो, जिससे सारा जाना जाता है।
हे ज्ञान स्वरूप देव ! तू अपनी महिमा में जाग। कब तक फिसलाहट की खेल-कूद मचा रखेगा? तू जहाँ है, जैसा है, अपने आपमें पूर्ण परम श्रेष्ठ है। अपने शुद्ध, शान्त, श्रेष्ठ स्वरूप में तन्मय रह। छोटे-मोटे व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, प्रतिकूलताओं से प्रभावित मत हो। बार-बार ॐकार का गुंजन कर और आत्मानंद को छलकने दे। ॐ....ॐ.....ॐ.....
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
साधना की
नींवः
श्रद्धा
संसार से वैराग्य होना दुर्लभ है। वैराग्य हुआ तो कर्मकाण्ड से मन उठना दुर्लभ है। कर्मकाण्ड से मन उठ गया तो उपासना में मन लगना दुर्लभ है। मन उपासना में लग गया तो तत्त्वज्ञानी गुरु मिलना दुर्लभ है। तत्त्वज्ञानी गुरु मिल भी गये तो उनमें श्रद्धा होना और सदा के लिए टिकना दुर्लभ है। गुरु में श्रद्धा हो गई तो भी तत्त्वज्ञान में प्रीति होना दुर्लभ है। तत्त्वज्ञान में प्रीति हो जाये लेकिन उसमें स्थिति करना दुर्लभ है। एक बार स्थिति हो गई तो जीवन में दुःखी होना और फिर से माता के गर्भ में उल्टा होकर लटकना और चौरासी के चक्कर में भटकना सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
तत्त्वज्ञान के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति बनाकर आवरण भंग करके जीवनमुक्त पद में पहुँचना ही परम पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ-भवन का प्रथम सोपान है श्रद्धा।
तामसी श्रद्धावाला साधक कदम-कदम पर फरियाद करता है। ऐसे साधक में समर्पण नहीं होता। हाँ, समर्पण की भ्रांति हो सकती है। वह विरोध करेगा। राजसी श्रद्धावाला साधक हिलता रहता है, भाग जाता है, किनारे लग जाता है। सात्विक श्रद्धावाला साधक निराला होता है। परमात्मा और गुरु की ओर से चाहे जैसे कसौटी हो, वह धन्यवाद से, अहोभाव से भरकर उनके हर विधान को मंगलमय समझकर हृदय से स्वीकृति देता है।
प्रायः राजसी और तामसी श्रद्धावाले लोग अधिक होते हैं। तामसी श्रद्धावाला कदम-कदम पर इन्कार करेगा, विरोध करेगा, अपना अहं नहीं छोड़ेगा। वह अपने श्रद्धेय के साथ, अपने इष्ट के साथ, सदगुरु के साथ विचारों से टकरायगा। राजसी श्रद्धावाला जरा-सी परीक्षा हुई, थोड़ी सी कुछ डाँट पड़ी तो वह किनारे हो जायगा, भाग जाएगा। सात्त्विक श्रद्धावाला किसी भी परिस्थिति में डिगेगा नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करेगा।
साधक में सात्त्विक श्रद्धा जग गई तो उसका मन तत्त्व-चिन्तन में, आत्म-विचार में लग जाता है। अन्यथा तो तत्त्वेत्ता सदगुरु मिलने के बाद भी तत्त्वज्ञान में मन लगना कठिन है। किसी को आत्म-साक्षात्कारी गुरु मिल जायें और उनमें श्रद्धा भी हो जाये तो यह जरूरी नहीं की सब लोग आत्मज्ञान के तरफ चल ही पड़ेंगे। राजसी-तामसी श्रद्धावाले लोग आत्मज्ञान के तरफ नहीं चल सकते। वे तो अपनी इच्छा के अनुसार तत्त्वज्ञानी सदगुरु से लाभ लेना चाहेंगे। इच्छा-निवृत्ति की ओर से प्रवृत्त नहीं हो सकते। जो वास्तविक लाभ तत्त्वज्ञानी सदगुरु उन्हें देना चाहते हैं उससे वे वंचित रह जाते हैं।
सात्त्विक श्रद्धावाले साधक को ही तत्त्वज्ञान का अधिकारी माना गया है और केवल यही तत्त्वज्ञान होने पर्यन्त सदगुरु में अचल श्रद्धा रख सकता है। वह प्रतिकूलता से भागता नहीं और प्रलोभनों में फँसता नहीं। संदीपक ने ऐसी श्रद्धा रखी थी। सदगुरु ने कड़ी कसौटियाँ की, उसे दूर करना चाहा लेकिन वह गुरुसेवा से विमुख नहीं हुआ। गुरु ने कोढ़ी का रूप धारण किया, सेवा के दौरान कई बार संदीपक को पीटते थे फिर भी कोई शिकायत नहीं। कोढ़ी शरीर से निकलने वाला गन्दा खून, पीव, मवाद, बदबू आदि के बावजूद भी गुरुदेव के शरीर की सेवा-सुश्रुषा से संदीपक कभी ऊबता नहीं था। भगवान विष्णु और भगवान शंकर आये, उसे वरदान देना चाहा लेकिन अनन्य निष्ठावाले संदीपक ने वरदान नहीं लिया।
विवेकानन्द होकर विश्वविख्यात बनने वाले नरेन्द्र को जब सात्विक श्रद्धा रहती तब रामकृष्णदेव के प्रति अहोभाव बना रहता है। जब राजसी श्रद्धा होती तब वे भी हिल जाते। उनके जीवन में छः बार ऐसे प्रसंग आये थे।
पहले तो आत्मज्ञानी सदगुरु मिलना अति दुर्लभ है। वे मिल भी जायें तो उनके प्रति हमारी सात्त्विक श्रद्धा निरन्तर बनी रहना कठिन है। हमारी श्रद्धा रजो-तमोगुण से प्रभावित होती रहती है। इसलिए साधक कभी हिल जाता है और कभी विरोध भी करने लगता है। अतः जीवन में सत्त्वगुण बढ़ाना चाहिए।
आहार की शुद्धि से, चिन्तन की शुद्धि से सत्त्वगुण की रक्षा की जाती है। अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचारे वाले व्यक्तियों के संग से बचना चाहिए।
अपने जीवन के प्रति लापरवाही रखने से श्रद्धा का घटना, बढ़ना, टूटना-फूटना होता रहता है। फलतः साधक को साध्य तक पहुँचने में वर्षों लग जाते हैं। जीवन पूरा हो जाता है फिर भी आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। साधक अगर पूरी सावधानी के साथ छः महीना ठीक प्रकार से साधना करे तो संसार और संसार की वस्तुएँ आकर्षित होने लगती हैं। सूक्ष्म जगत की कुंजियाँ हाथ लग जाती हैं। निरन्तर सात्विक श्रद्धायुक्त साधना से साधक बहुत ऊपर उठ जाता है। रजो-तमोगुण से बचकर, सत्त्वगुण के प्राधान्य से साधक तत्त्वज्ञानी सदगुरु के ज्ञान में प्रवेश पा लेता है। फिर तत्त्वज्ञान का अभ्यास करने में परिश्रम नहीं पड़ता। अभ्यास सत्त्वगुण बढ़ाने के लिए, श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा स्थिर हो गई तो तत्त्वविचार अपने आप उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को साधना में तत्पर रहना चाहिए, सात्त्विक श्रद्धा की सुरक्षा में सतर्क रहना चाहिए। इष्ट में, भगवान में, सदगुरु में सात्त्विक श्रद्धा बनी रहे।
तत्त्वज्ञान तो कइयों को मिल जाता है लेकिन वे तत्त्वज्ञान में स्थिति नहीं करते। स्थिति करना चाहते हैं तो ब्रह्माकारवृत्ति उत्पन्न करने की खबर नहीं रखते। बढ़िया उपासना किए बिना भी किसी को सदगुरु की कृपा से जल्दी तत्त्वज्ञान हो जाये तो भी विक्षेप रहेगा। मनोराज हो जाने की संभावना है। उच्च कोटि के साधक आत्म-साक्षात्कार के बाद भी ब्रह्माभ्यास में सावधानी से लगे रहते हैं। साक्षात्कार के बाद ब्रह्मानन्द में लगे रहना यह साक्षात्कार की शोभा है। जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वे भी ध्यान-भजन, शुद्धि-सात्त्विकता का ख्याल रखते हैं। हम लोग अगर लापरवाही कर दें तो अपने पुण्य और साधना के प्रभाव का नाश ही करते हैं।
जीवन में जितना उत्साह होगा, साधना में जितनी सतर्कता होगी, संयम में जितनी तत्परता होगी, जीवनदाता का मूल्य जितना अधिक समझेंगे उतनी हमारी आंतरयात्रा उच्च कोटि की होगी। ब्रह्माकारवृत्ति उत्पन्न होना भी ईश्वर की परम कृपा है। सात्त्विक श्रद्धा होगी, ईमानदारी से अपना अहं परमात्मा में समर्पित हो सकेगा तभी यह कार्य संपन्न हो सकता है। तुलसीदासजी कहते हैं-
ये
फल साधन ते न
होई......।
ब्रह्मज्ञानरूपी फल साधन से प्रकट न होगा। साधन करते-करते सात्त्विक श्रद्धा तैयार होती है। सात्त्विक श्रद्धा ही अपने इष्ट में, तत्त्व में अपने आपको अर्पित करने को तैयार हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि की प्रशंसा तो करे, अग्नि को नमस्कार तो करे लेकिन जब तक वह अग्नि में प्रवेश नहीं करता, अपने आपको अग्नि में समर्पित नहीं कर देता तब तक अग्निमय नहीं हो सकता। लोहा अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है तो स्वयं अग्नि बन जाता है। उसकी रग-रग में अग्नि व्याप्त हो जाती है। ऐसे ही साधक जब तक ब्रह्मस्वरूप में अपने आपको अर्पित नहीं करता तब तक भले ब्रह्म परमात्मा के गुणानुवाद करता रहे, ब्रह्मवेत्ता सदगुरु क गीत गाता रहे, इससे लाभ तो होगा, लेकिन ब्रह्मस्वरूप, गुरुमय, भगवदमय ईश्वर नहीं बन पाता। जब अपने आपको ईश्वर में, ब्रह्म में, सदगुरु में अर्पित कर देता है तो पूर्ण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।
'ईश्वर' और 'गुरु' ये शब्द ही हैं लेकिन तत्त्व एक ही है।
ईश्वरो
गुरुरात्मेति
मूर्ति भेदे
विभागिनोः।
आकृतियाँ दो दिखती हैं लेकिन वास्तव में तत्त्व एक ही है। गुरु के हृदय में जो चैतन्य प्रकट हुआ है वह ईश्वर में चमक रहा है। ईश्वर भी यदि भक्त का कल्याण करना चाहें तो सदगुरु के रूप में आकर परम तत्त्व का उपदेश देंगे। ईश्वर संसार का आशीर्वाद ऐसे ही देंगे लेकिन भक्त को परम कल्याण रूप आत्म-साक्षात्कार करना होगा तो ईश्वर को भी आचार्य की गद्दी पर आना पड़ेगा। जैसे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया श्रीरामजी ने हनुमानजी को उपेदेश दिया।
साधक ध्यान-भजन-साधना करते हैं। भजन की तीव्रता से भाव मजबूत हो जाता है। भाव के बल से भाव के अनुसार संसार में चमत्कार भी कर लेते हैं लेकिन भाव साधना की पराकाष्ठा नहीं है, क्योंकि भाव बदलते रहते हैं। साधना की पराकाष्ठा है ब्रह्माकारवृत्ति उत्पन्न करके आत्मसाक्षात्कार करना।
साधन-भजन-ध्यान में उत्साह, जगत में नश्वरबुद्धि और उच्चतम लक्ष्य की हमेशा स्मृति, ये तीन बातें साधक को महान् बना देती हैं। ऊँचे लक्ष्य का पता नहीं तो विकास कैसे होगा? ब्रह्माकारवृत्ति उत्पन्न करके आवरण भंग करना, आत्म-साक्षात्कार करके जीवनमुक्त होना, यह लक्ष्य यदि जीवन में नहीं होगा तो साधना की छोटी-मोटी पद्धतियों में, छोटे-मोटे साधना के चुटकुले में रुका रह जायेगा। कोल्हू के बैल की तरह वहीं घूमते-घूमते जीवन पूरा कर देगा।
अगर सावधानी से छः महीने तक ठीक ढंग से उपासना करे, तत्त्वज्ञानी सदगुरु के ज्ञान को विचारे तो उससे अदभुत लाभ होने लगता है। लाबयान ऊँचाई के सामर्थ्य का अनुभव करने लगता है। संसार का आकर्षण टूटने लगता है। उसके चित्त में विश्रान्ति आने लगती है। संसार के पदार्थ उससे आकर्षित होने लगते हैं। फिर उसे रोजी-रोटी के लिए, सगे-सम्बन्धी, परिवार-समाज को रिझाने के लिए नाक रगड़ना नहीं पड़ता। वे लोग ऐसे ही रीझने को तैयार रहेंगे। केवल छः महीने की सावधानी पूर्वक साधना..... सारी जिन्दगी की मजदूरी से जो नहीं पाया वह छः महीने में पा लेगा। लेकिन सच्चे साधक के लिए तो वह भी तुच्छ हो जाता है। उसका लक्ष्य है ऊँचे से ऊँचा साध्य पा लेना, आत्म-साक्षात्कार कर लेना।
प्रह्लाद के पिता ने प्रह्लाद को भजन करने से रोका था। लेकिन प्रह्लाद की प्रीति-भक्त भगवान में दृढ़ हो चुकी थी। प्रारम्भ से ही उसने सत्संग सुना था। जब वह माँ कयाधू के गर्भ में था तब कयाधू नारदजी के आश्रम में रही थी। माँ तो सत्संग सुनते झपकियाँ ले लेती थी लेकिन गर्भस्थ शिशु के मानस पर सत्संग के संस्कार ठीक से अंकित होते थे।
प्रह्लाद ग्यारह वर्ष का हुआ तो उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसको सिपाहियों के साथ गश्त करने के रखा। एक रात को प्रह्लाद ने देखा कि दूर कहीं आग की ज्वालाएँ निकल रही हैं, धुआँ उठ रहा है। नजदीक जाकर देखा तो कुम्हार के मटके पकाने के निभाड़े में आग लगाई थी। कुम्हार वहाँ खड़ा हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा थाः
"हे प्रभो ! अब मेरे हाथ की बात नहीं रही और तू चाहे तो तेरे लिए कुछ कठिन नहीं। हे भगवान ! तू दया कर। मैं तो नादान हूँ लेकिन तू उदार है। हे कृपासिन्धो ! तू मेरी भूल सुधार दे। मैं जैसा तैसा हूँ लेकिन तेरा हूँ। तू रहम कर। तेरी दया से सब कुछ हो सकता है। तू उन निर्दोष बच्चों को बचा ले नाथ !"
कुम्हार बार-बार प्रणाम कर रहा है। आँखों में आँसू सरक रहे हैं। वही प्रार्थना के शब्द दुहराये जा रहा है और निभाड़े की आग जोर पकड़ रही है। प्रह्लाद उसके पास गया और पूछाः
प्रश्नः क्या बाता है? क्या बोल रहा है?
कु. "कुमार ! हमने मटके बनाये और आग में पकाने के लिए जमाकर रखे थे। उन कच्चे मटकों में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे। हमने सोचा था कि आग लगाने के पहले उन्हें निकाल लेंगे। लेकिन भूल गये। निभाड़े के बीच में बच्चे रह गये और आग लग चुकी है। अब याद आया कि अरे ! नन्हें-मुन्ने मासूम बच्चे जल-भुनकर मर जायेंगे। अब हमारे हाथ की बात नहीं रही। चारों और आग लपटें ले रही है। प्रभु अगर चाहें तो हमारी गलती सुधार सकता है। बच्चों को बचा सकता है।"
प्रश्नः "यह क्या पागलपन की बात है? ऐसी आग के बीच बच्चे बच सकते हैं?"
कु.- "हाँ युवराज ! परमात्मा सब कुछ कर सकता है। वह कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं समर्थः है। वही तो छोटे-से बीज में से विशाल वृक्ष बना देता है। पानी की बूँद में से राजा-महाराजा खड़ा कर देता है। वही पानी की बूँद मनुष्य बनकर रोती है, अच्छा-बुरा, अपना-पराया बनाती है। जीवनभर मेरा-तेरा करती है और आखिर में मुट्ठीभर राख का ढेर छोड़कर भाग जाती है। यह क्या ईश्वर की लीला का परिचय नहीं है? समुद्र में बड़वानल जलती है वह पानी से बुझती नहीं और पेट में जठराग्नि रहती है वह शरीर को जलाती नहीं। गाय रूखा-सूखा घास खाती है और सफेद मीठा दूध पीता है तो जहर बनाता है। माँ रोटी खाती है तो दूध बनाती है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूध अपने आप बन्द हो जाता है। परमात्मा की लीला अपरंपार है। वह बिल्ली के बच्चों को भी बचा सकता है।"
प्र.- "बिल्ली के बच्चे कैसे बचते हैं यह मुझे देखना है। मटके पक जायें और तुम निभाड़ा जब खोलो तब मुझे बुलाना।"
कु.- "हाँ महाराज ! आप सुबह में आना। आप आयेंगे बाद में मैं निभाड़ा खोलूँगा।"
सुबह में प्रह्लाद पहुँच गया। कुम्हार ने थोड़ा सा अन्तर्मुख होकर भगवान का स्मरण करते हुए चारों ओर से गरम-गरम मटके हटाये तो बीच के चार मटके कच्चे रह गये थे। उनको हिलाया तो बिल्ली के बच्चे 'म्याऊँ म्याऊँ' करते छलांग मारकर बाहर निकल आये।
प्रह्लाद के चित्त में सत्संग के संस्कार सुषुप्त पड़े थे वे जग आये, भगवान की स्मृति हो आयी और लगा कि सार वही है। संसार से वैराग्य हो गया और भजन में मन लग गया।
प्रह्लाद भगवान के रास्ते चल पड़ा तो घोर विरोध हुआ। एक असुर बालक विष्णुजी की भक्ति करें, देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु यह कैसे सह सकता है? फिर भी प्रह्लाद दृढ़ता से भजन करता रहा। पिता ने उसे डाँटा, फटकारा, जल्लादों से डराया, पर्वतों से गिरवाया, सागर में डुबवाया लेकिन प्रह्लाद की श्रद्धा नहीं टूटी।
पहले तो ईश्वर में सच्ची श्रद्धा होना कठिन है। श्रद्धा को जाय लेकिन टिकना कठिन है। श्रद्धा टिक भी जाये फिर भी तत्त्वज्ञान होना कठिन है।
हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद को मारने के लिए कई प्रयास किये। प्रह्लाद ने सोचाः 'जिस हरि ने बिल्ली के बच्चों को बचाया तो क्या मैं उसका बच्चा नहीं हूँ? वह मुझे भी बचाएगा।' प्रह्लाद भगवान के शरण हो गया। पिता ने पर्वतों से गिरवाया तो मरा नहीं, सागर में फिंकवाया तो डूबा नहीं। आखिर लोहे के स्तंभ को तपवाकर पिता बोलाः
"तू कहता है कि मेरा भगवान सर्वत्र है, सर्व समर्थ है। अगर ऐसा है तो वह इस स्तंभ में भी है, तो तू उसका आलिंगन कर। वह सर्व समर्थ है तो यहाँ भी प्रकट हो सकता है।"
प्रह्लाद ने तीव्र भावना करके लोहे के तपे हुए स्तंभ को आलिंगन किया तो वहाँ भगवान का नृसिंहावतार प्रकट हुआ।
जब भोगों का बाहुल्य हो जाता है, जब दुष्टों के जोर जुल्म बढ़ जाते हैं तब भगवान के चाहे कहीं से किसी भी रूप में प्रकट होने को समर्थ हैं।
नृसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु का वध करके स्वधाम पहुँचाया, प्रह्लाद को राज्य दिया और भगवान अन्तर्ध्यान हो गये।
प्रह्लाद ने भगवान के दर्शन तो किए लेकिन भगवत्तत्व का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ। भगवान का तात्त्विक स्वरूप जानना कठिन है।
कुछ समय बीता। असुरों के आचार्य ने प्रह्लाद को भरमाया। बोलेः
"प्रह्लाद ! विष्णु ने तुम्हारे पिता को मार डाला। तुमने उनकी शरण माँगी थी, रक्षण की प्रार्थना की थी लेकिन ऐसा कहा था कि मेरे पिता को मार डालो?"
"नहीं, मैंने पिता को मारने को तो नहीं कहा था।"
"तुमने कहा नहीं फिर क्यों मारा? तुम पर विष्णु की प्रीति थी तो पिता की बुद्धि सुधार देते। उनकी हत्या क्यों की?"
विष्णु भगवान में प्रह्लाद की दृढ़ श्रद्धा तो थी लेकिन श्रद्धा को हिलानेवाले लोग मिल जाते हैं तो श्रद्धा 'छू....' हो जाती है। ऐसी श्रद्धा हिलाने वाले कई लोग साधक के जीवन में आते रहते हैं। ऐसी श्रद्धा हिलाने वाले कई लोग साधक के जीवन में आते रहते हैं। साधना में, गुरुमन्त्र में, ईश्वर में, सदगुरु में, सत्संग में श्रद्धा हिलानेवाला कोई न कोई तो मिल ही जायेगा। बाहर से कोई नहीं मिलेगा तो हमारा मन ही तर्क-वितर्क करके विरोध करेगा, श्रद्धा को हिलायेगा। इसीलिए श्रद्धा सदा टिकनी कठिन है।
असुरगुरु शुक्राचार्य ने प्रह्लाद की श्रद्धा को हिला दिया। शुक्राचार्य तत्त्वज्ञानी नहीं हैं, संजीवनी विद्या जानते हैं। असुरों पर उनका पूरा प्रभाव है। लेकिन ब्रह्मज्ञान के सिवाय का प्रभाव किस काम का? वह प्रभाव तो चौरासी लाख योनियों की यातनाओं के प्रति ही खींच ले जायगा।
शुक्राचार्य प्रह्लाद को कहते हैं- विष्णु ने तुम्हारे बाप को मार डाला फिर भी तुम उनको पूजते हो? कैसे मूर्ख हो ! इतनी अन्धश्रद्धा?
किसी श्रद्धालु को कोई बोले कि 'ऐसी तुम्हारी अन्धश्रद्धा !' तो वह बचाव तो करेगा कि मेरी अन्धश्रद्धा नहीं है, सच्ची श्रद्धा है लेकिन विरोधी का कथन उसकी श्रद्धा को झकझोर देगा। शब्द देर-सबेर चित्त पर असर करते ही हैं इसीलिए 'गुरुगीता' में भगवान शंकर ने रक्षा का कवच फरमाया किः
गुरुनिन्दाकरं
दृष्टवा
धावयेदथ
वासयेत्।
स्थानं
वा
तत्परित्याज्यं
जिह्वाच्छेदाक्षमो
यदि।।
'गुरु की निन्दा करने वाले देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए।'
शुक्राचार्य ने प्रह्लाद में भगवान विष्णु के प्रति वैरभाव के संस्कार भर दिये। प्रह्लाद आ गया उनके प्रभाव में। कहने लगाः "आप कहो तो विष्णु से बदला लूँ।"
भगवान विष्णु का विरोध करता हुआ प्रह्लाद सेना को सुसज्जा कर के आदि नारायण का आवाहन कर रहा हैः "आ जाओ। तुम्हारी खबर लेंगे।"
भगवान भक्त का अहंकार और पतन नहीं सह सकते। दयालु श्रीहरि ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में लकड़ी, झुकी कमर, कृश काय, श्वेत वस्त्रादि से युक्त ब्राह्मण के रूप में प्रह्ललाद के राजदरबार में जाने लगे। द्वार पर पहुँचे तो दरबान ने कहाः
"हे ब्राह्मण ! प्रह्लाद युद्ध की तैयारी में हैं। युद्ध के समय साधु-ब्राह्मण का दर्शन ठीक नहीं माना जाता।"
ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहाः "मैंने सुना है कि प्रह्लाद साधु ब्राह्मण का खूब आदर करते हैं और तू मुझे जाने से रोक रहा है?"
दरबान के कहाः "प्रह्लाद पहले जैसे नहीं हैं। अब सावधान हो गये हैं। शुक्राचार्य ने उनको समझा दिया है। अब तो भगवान विष्णु से बदला लेने की तैयारी में हैं। साधु-ब्राह्मण का आदर करने वाले प्रह्लाद वे नहीं रहे। हे ब्राह्मण ! तुम चले जाओ।"
"भाई ! कुछ भी हो, मैं अब प्रह्लाद से मिलकर ही जाऊँगा। तू नहीं जाने देगा तो मैं यहीं प्राण त्याग दूँगा। तुमको ब्रह्महत्या लगेगी।"
इस प्रकार द्वारपाल को समझा-बुझाकर भगवान प्रह्लाद के समक्ष पहुँचे। अभिवादन करते हुए ब्राह्मण वेशधारी प्रभु ने कहाः
"प्रह्लाद ! तेरा कल्याण हो। सुना है अपने पितृहन्ता विष्णु से तुम बदला लेना चाहते हो। तुम मेरा बदला भी लेना। मुझ बूढ़े ब्राह्मण का भी सर्वनाश हो गया।" ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने विष्णु विरोधी कुछ बातें कहीं। प्रह्लाद ने उनको नजदीक बिठाया। बातों का सिलसिला चला।
ब्राह्मण ने पूछाः "तुम विष्णु से बदला लेना चाहते हो? विष्णु कहाँ रहते हैं?"
प्र.- "वे तो सर्वत्र हैं। सर्व हृदयों में बैठे हैं।"
ब्रा.- "हे मूर्ख प्रह्लाद ! जो सर्वत्र है, सर्व हृदयों में है, उसका विनाश तू कैसे करेगा? मालूम होता है, जैसा मैं मूर्ख हूँ, वैसा ही तू मन्दमति है। शुक्र के बहकावे में आकर दुष्ट निश्चयी हुआ है। मैं यह छड़ी गाड़ता हूँ जमीन में, उसको तू निकालकर दिखा तो मानूँगा कि तू विष्णु से युद्ध कर सकता है।"
ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने जमीन में अपनी छड़ी गाड़ दी। प्रह्लाद उठा सिंहासन से। खींचा छड़ी को एक हाथ से, फिर दोनों हाथ से। पूरा बल लगाया। छड़ी खींचने में झुकना पड़ा। बल लगा। प्राणापान की गति सम हुई। राज्यमद कुछ कम हुआ। प्रह्लाद की बुद्धि में प्रकाश हुआ कि यह ब्राह्मण वेशधारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। भक्ति के पुराने संस्कार थे ही। ऊपर से कुसंस्कार जो पड़े थे वे हटते ही प्रह्लाद उस ब्राह्मण वेशधारी को नम्रतापूर्वक आदर भरे वचनों से कहने लगाः
"हे विप्रवर ! आप कौन हैं?"
भगवान बोलेः "जो अपने को नहीं जानता वह मेरे को भी ठीक से नहीं जानता। जो अपने को और मेरे को नहीं जानता वह माया के संस्कारों में सूखे तिनके की नाई हिलता-डुलता रहता है। हे प्रह्लाद ! तू सन्मति को त्याग कुमति के आधीन हुआ है। तबसे तू अशान्त और दुःखी हुआ है। कुनिश्चय करने वाला व्यक्ति हमेशा दुःख का भागी होता है।"
करूणानिधान के कृपापूर्ण वचन सुनकर प्रह्लाद समझ गया कि ये तो मेरे श्रीहरि हैं। चरणों पर गिर पड़ा। क्षमा माँगने लगा। तब भक्तवत्सल भगवान प्रह्लाद को कहने लगेः
"क्षमा तो तू कर। मेरे को मारने के लिए इतनी सेना तैयार की है ! तू क्षमा कर मेरे को!"
कहाँ तो पिता की इतनी शासना-पर्वत से गिराना, पानी में फेंकना आदि ! ये शासना करने पर भी प्रह्लाद विष्णु की भक्ति में लगे रहे। शुक्राचार्य ने अपना होकर धीरे-धीरे कुसंस्कार भर दिये तो वही प्रह्लाद विष्णुजी युद्ध करने को तत्पर हुआ।
जब तक सर्व व्यापक श्रीहरित्व का साक्षात्कार नहीं होता, अन्तःकरण से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता, परिच्छिन्नता नहीं मिटती तब तक जीव की श्रद्धा और स्थिति चढ़ती उतरती रहती है।
वैकुंठ में भगवान के पार्षद जय-विजय प्रतिदिन श्रीहरि का दर्शन करते हैं लेकिन हरितत्त्व का साक्षात्कार न होने क कारण उनको भी तीन जन्म लेने पड़े। प्रह्लाद को श्रीहरि के श्रीविग्रह का दर्शन हुआ, हरि सर्वत्र है ऐसा वृत्तिज्ञान तो था लेकिन वृत्तिज्ञान सुसंग कुसंग से बदल जाता है। पूर्ण बोध अबदल है।
प्रह्लाद जैसों की भी श्रद्धा कुसंग के कारण हिल सकती है तो हे साधक ! भैया ! तू ऐसे वातावरण से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे संस्कारों के बचना जो तुझे साधना के मार्ग से, ईश्वर के रास्ते से फिसलाते हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जैसी
भावना वैसी
सिद्धि
भगवान सर्वव्यापक और शाश्वत हैं। वे सबको मिल सकते हैं। आप जिस रूप में भगवान को पाना चाहते हैं उस रूप में आपको मिलते हैं। श्रीकृष्ण गीता में भी वचन देते हैं किः
ये
यथा मां
प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव
भजाम्यहम्।
'हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।'
(गीताः
4.11)
आप कुशलता से परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान पदार्थों के रूप में मिलेंगे। आलसी और प्रमादी रहते हैं तो भगवान रोग और तमोगुण के रूप में मिलेंगे। दुराचारी रहते हैं तो भगवान नरक में मिलेंगे। सदाचारी और संयमी रहते हैं तो भगवान स्वर्ग के रूप में मिलेंगे। सूर्योदय के पहले स्नानदि से शुद्ध होकर प्रणव का जाप करते हैं तो भगवान आनन्द के रूप में मिलते हैं। सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं तो भगवान आलस्य के रूप में मिलेंगे। भगवान की बनाई अनेक लीलाओं को, इष्टदेव को, आत्मवेत्ता सदगुरु को प्यार की निगाहों से देखते हैं, श्रद्धा-भाव से, अहोभाव से दिल को भरते हैं तो भगवान प्रेम के रूप में मिलेंगे। वेदान्त का विचार करते हैं, आत्म-चिन्तन करते हैं तो भगवान तत्त्व के रूप में मिलेंगे। घृणा और शिकायत के रूप में देखते हैं तो भगवान शत्रु के रूप में मिलेंगे। धन्यवाद की दृष्टि रखते हैं तो भगवान मित्र के रूप में मिलते है। अपने चित्त में सन्देह है, फरियाद है, चोर डाकू के विचार हैं तो भगवान उसी रूप में मिलते हैं। अपनी दृष्टि में सर्व ब्रह्म की भावना है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता है तो दूसरों की नजरों में जो क्रूर हैं, हत्यारे हैं, डाकू हैं, वे तुम्हारे लिए क्रूर हत्यारे नहीं रहेंगे।
आप निर्णय करो कि भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं। जब सब भगवान हैं, सर्वत्र भगवान हैं तो आपको जो मिलेगा वह भगवान ही है। समग्र रूप उसी के हैं। यह स्वीकार कर लो तो सब रूपों में भगवान मिल जायेंगे। आनन्द ही आनन्द चाहो, प्रेम ही प्रेम चाहो तो भगवान उसी रूप में मिलेंगे।
किसी को लगेगा कि जब सर्वत्र भगवान हैं तो पाप-पुण्य क्यों? फिर पाप करने में हर्ज क्या है?
हाँ, कोई हर्ज नहीं। डटकर पाप करो। फिर भगवान नरक के रूप में प्राप्त होंगे।
'सब ब्रह्म है तो जो आवे सो खाओ, जो आवे सो पियो, जो मिले सो भोगो, चाहे सो करो क्या हर्ज है?'
तो भगवान सर्वत्र हैं। वे रोग के रूप में प्रकट होंगे। संयम से रहोगे तो भगवान स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होंगे।
भगवान हमारे समक्ष अपने समग्र रूप में प्रकट हो जायें ऐसी इच्छा हो तो अपने 'मैं' को खोजो। 'मैं' खो जाएगा फिर लगेगा कि भगवान समग्र रूपों में हैं और भी भगवत्तत्व था।
महायोगी श्री अरविन्द गीता के महान् उपासक थे। वे गीता के सत्यों को अपने जीवनरूपी साँचे में ढालने को पूर्णरूपेण कृतसंकल्प थे। वेदों और उपनिषदों का सार गीता है जिसे पढ़कर उन्होंने तीन प्रतिज्ञाएँ की थीं। राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर भारत माता को अँग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना एवं आत्मसाक्षात्कार करना।
अलिपुर बम-कांड में उनकी धरपकड़ हुई और कारावास में डाल दिये गये। वहाँ पर भी उनकी योग साधना सतत चालू थी। रात-रात भर परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। श्री अरविन्द के बचाव पक्ष के बैरीस्टर श्री चित्तरंजनदास थे जिन्होंने फीस में एक पाई भी न ली थी (बाद में वे देशबन्धु दास के नाम से प्रसिद्ध हुए)। सरकार की ओर से सैंकड़ों प्रमाण और साक्षी खड़े किये गये थे जिनका खंडन करने के लिए उन्हें दिन रात श्रम करना पड़ता था। सालभर मुकद्दमा चला। एक दिन अंग्रेज न्यायाधीश के पास कड़े पुलिस बंदोबस्त तले श्री अरविंद को जेल में से अदालत लाया गया। देशभक्ति से चकचूर जनता ने न्यायालय को खचाखच भर दिया था। सरकारी वकीलों के समक्ष बेरीस्टर चित्तरंजनदास उपस्थित हुए। उस समय विद्युत-पंखे नहीं थे। विशाल चँवर से न्यायाधीश पर पवन डाला जा रहा था। चँवर डुलाने के लिए कैदियों का उपयोग किया जाता था।
सरकार कृतसंकल्प थी कि श्री अरविन्द को मुजरिम साबित कर फाँसी पर लटका दे और श्री अरविन्द शांतभाव से श्रीकृष्ण का चिन्तन किये जा रहे थे। उस समय उन्हें जो अनुभूति हुई वह अत्यंत रसीली एवं अदभुत थी। भगवान के समग्र स्वरूप का गीता वचन प्रत्यक्ष हुआ। श्री अरविन्दजी के ही शब्दों में इस प्रकार हैः
"मैंने न्यायाधीश की ओर देखा तो मुझे उनमें श्रीकृष्ण ही मुस्कराते दीखे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने वकीलों की ओर देखा तो मुझे वकील दिखाई ही नहीं दिये, सब श्रीकृष्ण का रूप दिखाई दिये। वहाँ उपस्थित कैदियों की ओर निहारा तो सब कृष्णरूप धारण कर बैठे हुए दिखे। जगह-जगह मुझे श्रीकृष्ण का हूबहू दर्शन हुआ। श्रीकृष्ण मेरे सामने देखकर बोलेः 'तू बराबर देख। मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर डर किस बात का?' उनके दिव्य दर्शन से, अभयदान प्रदान करती हुई उनकी वाणी से मैं संपूर्ण निर्भय हो गया। चिन्ता मात्र पलायन हो गई।" वर्षभर अदालत में मुकद्दमा चला। केस के अन्त में गोरे न्यायाधीश ने चुकादा दियाः 'निर्दोष'। लोगों के आनंद का पार न रहा। उन्होंने श्री अरविन्द को कन्धे पर बिठाकर आनंदोत्सव मनाते हुए प्रचण्ड जयघोष कियाः
"जय श्रीकृष्ण, जय श्री अरविन्द।"
समय की धारा में वह प्रसंग भी सरक गया, स्वप्न की नाई।
उमा
कहौं मैं
अनुभव अपना।
सत्य
हरिभजन, जगत
सब सपना।।
यह सपने जैसे संसार में सब समय की धारा में स्वप्नवत् हो जाता है। अतः जगत सब स्वप्न है। 'मैं आत्मरूप से सबका आधार सच्चिदानंद स्वरूप हूँ... सोऽहम्.... शिवोऽहम्.....' ऐसा चिन्तन करोगे तो भगवान ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाएँगे।
भोगी और विलासी को रोग होते हैं। विकारी जीवन में पश्चाताप, भय और चिन्ता होती है। भय, चिन्ता होवे तभी 'भगवान भय और चिन्ता के रूप में प्रकट हुए हैं' – ऐसा करके भय और चिन्ता से बाहर निकल जाओ। भगवदबुद्धि से भय को देखोगे तो भय दुःख नहीं देगा। भगवदबुद्धि से रोग और शत्रु को देखोगे तो रोग और शत्रु दुःख नहीं देंगे। भगवदबुद्धि से सुख और स्वर्ग को देखोगे तो वह सुख और स्वर्ग विषयासक्ति नहीं कराएँगे। कितने सुन्दर समाचार हैं!
आप भगवान को किसी रूप में प्रकट करना नहीं चाहते लेकिन भगवान जैसे हैं वैसा जमाना चाहते हैं, जैसे हैं वैसे ही देखना चाहते हैं।
जैसे हैं वैसे देखना चाहते हैं तो वे सब कुछ हैं। उनको सब कुछ जान लो, देख लो। नरक भी वे ही हैं, स्वर्ग भी वे ही हैं। रोग भी वे ही हैं और जो स्वास्थ्य भी वे ही हैं। धन्यवाद भी वे ही हैं, शिकायत भी वे ही हैं।
'हमको भगवान पूरे दिखने चाहिए।'
पूरा देखनेवाला कौन है, उसको पूरा खोजो। जो पूरा देखने वाले को पूरा खोज लेता है उसके अपने भीतर भगवान पूरे प्रकट हो जाते हैं।
खोजने में परिश्रम पड़े तो वे सब कुछ हैं ही ऐसा संतों का अनुभव मान लो न ! अपने को पूरा खोजोगे तो क्या होगा?
हेरत
हेरत गयो
कबीरो हेराई।
खोजते-खोजते खोजनेवाला खो जायेगा। 'मैं..... मैं....' करने वाला मिथ्या हो जायेगा। शेष ब्रह्म ही ब्रह्म रह जायेगा। नमक की पुतली गई समुद्र की थाह लेने। पुतली तो खो गई, हो गई सागर। ऐसे ही देह और अहंकार खो गया और रह गया केवल ब्रह्म। मिटी बूँद हो गई सागर। बूँद भी पानी है, सागर भी पानी है।
श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने करोड़ों ग्रन्थों का सार बताते हुए कहाः
श्लोकार्धेन
प्रवक्ष्यामि
यदुक्तं
ग्रन्थकोटिभिः।
ब्रह्म
सत्यं
जगन्मिथ्या
जीवो
ब्रह्मैव ना परः।।
अर्ध
श्लोक कर कहता
हूँ कोटि
ग्रन्थ को
सार।
ब्रह्म
सत्य है जगत
मिथ्या जीव
ब्रह्म निरधार।।
जिसको मूल हम जीवात्मा बोलते हैं वह ब्रह्म अलग से नहीं है। जिसे हम तरंग बोलते हैं वह सागर से अलग नहीं। जिसे घटाकाश बोलते हैं वह महाकाश से अलग नहीं। जिसको हम जेवर बोलते हैं वह सोने से अलग नहीं। जिसे हम दो गज जमीन बोलते हैं वह पूरी पृथ्वी से अलग नहीं। दीवाल बाँध कर सीमा खड़ी कर सकते हो लेकिन अलग नहीं कर सकते हो लेकिन जमीन अलग नहीं कर सकते। 'हमारी जमीन..... तुम्हारी जमीन' ये मन की रेखाएँ खड़ी कर सकते हो लेकिन जमीन अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही 'हमारा शरीर.... तुम्हारा शरीर....' अलग मान सकते हो लेकिन दोनों की जो वास्तविक 'मैं' है उसे अलग नहीं कर सकते। घड़ों का अलगाव हो सकता है लेकिन घड़ों के आकाश का अलगाव नहीं हो सकता। चित्त के अलगाव हो सकते हैं लेकिन चित्त जिसके आधार से फुरते हैं उल चिदाकाश का अलगाव नहीं हो सकता। 'वह चिदाकाश आत्मा मैं हूँ'.... ऐसा ज्ञान कराने का भगीरथ कार्य वेदान्त का है। 'वास्तव मे तुम आत्मा हो, विश्वात्मा हो, परब्रह्म परमात्मा हो। मरने और जन्मने वाले पुतले नहीं हो' – ऐसा वेदान्त दर्शन फरमाता है। ॐ.... ॐ.....ॐ....
ऐसा ज्ञान पचाने वाला सिद्ध पुरुष शूली पर चढ़ते हुए भी निर्भीक होता है, रोते हुए भी नहीं रोता, हँसते हुए भी नहीं हँसता।
सन्तुष्टोऽपि
न सन्तुष्टः
खिन्नोऽपि न च
खिद्यते।
तस्याश्चर्यदशां
तां तां
तादृशा एव
जानते।।
'ज्ञानी पुरुष लोक दृष्टि से संतोषवान होते हुए भी संतुष्ट नहीं है और खेद को पाये हुए भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। उसकी उस-उस आश्चर्य दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं।'
(अष्टावक्र
गीताः 56)
तन
सुकाय पिंजर
कियो धरे रैन
दिन ध्यान।
तुलसी
मिटै न वासना
बिना विचारे
ज्ञान।।
करोड़ों वर्ष की समाधि करो लेकिन आत्मज्ञान तो कुछ निराला ही है। ध्यान भजन करना चाहिए, समाधि करनी चाहिए लेकिन समाधिवालों को भी फिर इस आत्मज्ञान में आना चाहिए। सेवा अवश्य करना चाहिए और फिर वेदान्त में आना चाहिए। नहीं तो, सेवा का सूक्ष्म अहंकार आयेगा। कर्तृत्व की गाँठ बँध जाएगी तो स्वर्ग में घसीटे जाओगे। स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर पतन होगा।
वेदान्त का जिज्ञासु समझता है कि कर्मों का फल शाश्वत नहीं होता। पुण्य का फल भी शाश्वत नहीं और पाप का फल भी शाश्वत नहीं। पुण्य सुख देकर नष्ट हो जाएगा और पाप दुःख देकर नष्ट हो जाएगा। सुख और दुःख मन को मिलेगा। मन के सुख-दुःख को जो जानता है उसको पाकर पार हो जाओ। यही है वेदान्त। कितना सरल।
जिसको
अपना बिछुड़ा
हुआ प्यारा
स्वजन मिल जाये,
उसको कितना
आनन्द होता है
! मेले
में बिछुड़े
बच्चे को माँ
मिल जाये
पत्नी को
बिछुड़ा हुआ
पति मिल जाये,
मित्र को बिछुड़ा
हुआ मित्र मिल
जाये तो कितना
आनन्द होता है
!
जब अपना स्वजन कहीं मिल जाय तो इतना आनन्द होता है तो जिसको वेदान्त का ज्ञान हो जाता है उसको तो सर्वत्र अपना प्रिय प्रेमास्पद, अपना आपा मिलता है..... उसको कितना आनन्द मिलता होगा। ॐ....ॐ.....ॐ...
ॐ आनन्द ! ॐ आनन्द !! ॐ आनन्द !!!
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
कर्म और
ज्ञान
एक लंगड़ा आदमी बैठा था बद्रीनाथ के रास्ते पर। कहे जा रहा थाः "लोग बद्रीनाथ की यात्रा को जा रहे हैं। हमारे पास पैर होते तो हम भी भगवान के दर्शन करते।" पास में साथी बैठा था। वह सूरदास था। सुन रहा था उसकी बात। वह भी कहने लगाः "यार ! मैं भी चाहता था कि ईश्वर के दर्शन करूँ लेकिन मेरे पास आँखों की ज्योति नहीं है। कम से कम ईश्वर के धाम में तो जाने की रूचि है।"
एक महात्मा ने कहाः "एक की आँखें और दूसरे के पैर, दोनों का सहयोग हो जायेगा तो तुम लोग बद्रीनाथ पहुँच जाओगे।"
ऐसे ही जीवन के तत्त्व का जो ज्ञान है वह आँख है। वह ज्ञान अगर कर्म में नहीं आता तो वह लंगड़ा रह जाता है। कर्म करने की शक्ति जीवन में है लेकिन ज्ञान के बिना है तो ऐसी अन्धी शक्तियों का दुरुपयोग हो जाता है। जीवन बरबाद हो जाता है। यही कारण कि जिनके जीवन में जप-तप-ज्ञान-ध्यान और सदगुरुओं का सान्निध्य नहीं है ऐसे व्यक्तियों की क्रियाशक्ति राग, द्वेष और अभिमान को जन्म देकर हिंसा आदि का प्रादुर्भाव कर देती है। कर्म करने की शक्ति भ्रष्टाचार के तरफ, दूसरों का शोषण करने के तरफ, अहंकार को बढ़ाने के तरफ नष्ट हो जाती है।
क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। आज तक ऐसा कोई मनुष्य, प्राणी पैदा ही नहीं हुआ जो बिना क्रिया के, बिना कर्म के रह सके। कर्म करना ही है तो ज्ञान संयुक्त कर्म करें। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है कि ज्ञानी महापुरुष, जगत की नश्वरता जानने वाले महापुरुष भी सत्कर्म करते हैं। क्योंकि उनको देखकर दूसरे करेंगे। बिना कर्म के नहीं रह सकेंगे तो अच्छे कर्म करें। अगर कर्म करने की शक्ति है तो ज्ञान, भक्ति और योग के द्वारा उसे ऐसा सुसज्जित कर दें कि ज्ञान संयुक्त कर्म जीवनदाता तक पहुँचा दे।
कर्मों से कर्मों को काटा जाता है। उन कर्मों में ज्ञान की सुवास होगी तो कर्मों को काटेंगे और अहंकार की गन्ध होगी तो कर्म बन्धन की जाल बुनेंगे। इसीलिए कर्मों के जगत में ज्ञान का समन्वय होना चाहिए।
ज्ञान में सुख भी है और समझ भी। जैसे मेरे मुँह में रसगुल्ला रख दिया जाये और मैं प्रगाढ़ निद्रा में हूँ तो मिठास नहीं आयेगी। जब जागूँ तब वृत्ति जिह्वा से जुड़ेगी तो रसगुल्ले की मिठास का ज्ञान होते ही सुख आयेगा। बिना ज्ञान के सुख नहीं। ज्ञान में समझ भी है, सुख भी है। तमाम प्रकार के सुख, शक्ति एवं ज्ञान जहाँ से प्रकट होते हैं वह उदगम स्थान आत्मा है। उस आत्मदेव का साक्षात्कार करना ही आत्मज्ञान है। उस ज्ञान के बिना मनुष्य चाहे कितनी सारी क्रियाएँ कर ले लेकिन क्रियाओं का फल उसकी परेशानियों का कारण बन जाता है। वही क्रियाएँ अगर ज्ञान संयुक्त होती हैं तो उनका फल अकर्तृत्व पद की प्राप्ति कराता है। उपनिषदों का ज्ञान, वेदान्त का ज्ञान एक ऐसी कला है, कर्मों में ऐसी योग्यता ले आता है कि आदमी का जीवन नश्वर जगत में होते हुए भी शाश्वत के अनुभव संयुक्त हो जाता है। मरनेवाले देह में रहते हुए अमर आत्मा का दीदार होने लगता है। मिटने वाले सम्बन्धों में अमिट का सम्बन्ध हो जाता है। गुरुभाइयों का सम्बन्ध मिटनेवाला है, गुरु का सम्बन्ध भी मिटने वाला है लेकिन वह सम्बन्ध अमिट की प्राप्ति करा देता है, अगर ज्ञान है तो। ज्ञान नहीं है तो मिटने वाले सम्बन्धों में ऐसा मोह पैदा होता है कि चौरासी-चौरासी लाख जन्मों तक आदमी भटकता रहता है।
यस्य ज्ञानमयं तपः। ज्ञान के संयुक्त तप हो। ज्ञानसहित क्रिया हो। श्रीकृष्ण के जीवन में देखो तो कितनी सारी क्रियाएँ हैं लेकिन ज्ञान संयुक्त क्रियाएँ हैं। जनक के जीवन में क्रियाएँ हैं लेकिन ज्ञान संयुक्त हैं। राम जी के जीवन में कर्म हैं लेकिन ज्ञान संयुक्त हैं।
प्रातःकाल
उठ रघुनाथा।
मात
पिता गुरु
नावई माथा।।
यह ज्ञान की महिमा है।
गुरु
ते पहले जगपति
जागे.....
गुरु विश्वामित्र जागें उसके पहले रामजी जग जाते थे। ज्ञानदाता गुरुओं का आदर करते थे।
जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है।
यति गोरखनाथ पसार हो रहे थे तो किसी किसान ने कहाः "बाबाजी ! दोपहर हुई है। अभी-अभी घर से खाना आयेगा। आप भोजन पाना, थोड़ी देर विश्राम करना और शाम को जहाँ आपकी मौज हो, विचरण करना।"
किसान की आँखों ने तो एक साधु देखा लेकिन भीतर एक समझ थी कि थोड़ी सेवा कर लूँ। उसने गोरखनाथजी को रिझाकर रोक लिया। भोजन कराया। फिर गोरखनाथजी ने आराम किया। शाम को जब रमते भये तब किसान ने प्रणाम करते कहाः
"महाराज ! खेती करते-करते ढोरों जैसा जीवन बिता रहे हैं। कभी आप जैसे संत पधारते हैं। कुछ न कुछ मुझे थोड़ा-सा उपदेश दे जाइये।"
गोरखनाथ ने देखा कि है तो पात्र। पैर से शिखा तक निहारा। बोलेः
"और उपदेश क्या दूँ? जो मन में आवे वह मत करना।"
ये वचन गोरखनाथ को गुरु मच्छन्दरनाथ ने कहे थे। वे ही वचन गोरखनाथ ने किसान को कहे और जोगी रमते भये।
संध्या हुई। किसान ने हल कन्धे पर रखकर पाँव उठाये। घर की ओर चला। याद आया गुरुजी का वचनः 'मन में आये वह मत करना।' महाराज ! वह रुक गया ! ऐसा रुका कि उसका मन भी रुक गया ! जो भी मन में आता वह नहीं करता। मन से पार हो गया। चौरासी सिद्धों मं वह एक सिद्ध हो गया – हालीपाँव। मतलब, हल उठाया पाँव रखा और गुरुवचन में टिक गया। नाम पड़ गया हालीपाँव सिद्ध।
कहाँ तो साधारण किसान और कहाँ हालीपाँव सिद्ध !
शबरी ने गुरु के वचन सिर पर रखे और राम जी द्वार पर पधारे। किसान ने गोरखनाथ के वचन अडिगता से माने। मन हो गया अडिग। किसान में से हालीपाँव सिद्ध।
कर्म तो उसके पास थे लेकिन कर्मों को जब ज्ञान-निष्ठा का दीया मिल गया तो वह सिद्ध हो गया।
संत सुन्दरदास हो गये। अच्छे, उच्च कोटि के संत थे। उनसे किसी ने पूछाः
"स्वामीजी ! भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे?"
वे बोलेः "भगवान के दर्शन करने से भगवान में सन्देह हो सकता है लेकिन भगवान की कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है। भगवान की कथा की अपेक्षा भगवान के प्यारे भक्त हो गये हैं, संत हो गये है उनका जीवन-चरित्र पढ़ने सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। भगवान की कथा की अपेक्षा भगवान के प्यारों की कथा से भक्ति का प्राकट्य शीघ्र हो जाता है।"
नारेश्वर में रंग अवधूत जी महाराज हो गये। अच्छे संत थे। उनसे किसी ने पूछाः
"आप तो बाबाजी ! ज्ञातज्ञेय हो गये हैं। अभी आपको क्या रुचता है?"
वे बोलेः "संतो के जीवन चरित्र पढ़ने में मेरी अभी भी रुचि रहती है। नर्मदा के किनारे परिक्रमा करते कोई संत आ जायें तो भोजन पकाकर उन्हें खिलाऊँ ऐसे भाव आ जाते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है।"
संत का मतलब यह हि कि जिनके द्वारा अपने जन्मों का अंत करने का ज्ञान मिल जाय, क्रियाओं का अंत करने का ज्ञान मिल जाय।
अकेला ज्ञान लंगड़ा हो जायेगा, शुष्क हो जायेगा। अकेली क्रिया अन्धी हो जायेगी। हम लोग क्रियाएँ जीवनभर किए जा रहे हैं और अन्त में देखो तो परिणाम कुछ नहीं, हताशा..... निराशा।
प्रेम में से ज्ञान निकाल दो तो वह काम हो जायगा। ज्ञान में से प्रेम में निकाल दो तो वह शुष्क हो जायेगा। ज्ञान में से योग निकाल दो तो वह सामर्थ्यहीन हो जायेगा। योग में से ज्ञान और प्रेम निकाल दो तो वह जड़ हो जायगा।
इसलिए भाई मेरे ! प्रेम में योग और ज्ञान मिला दो तो प्रेम पूर्ण हो जायगा, पूर्ण पुरुषोत्तम का साक्षात्कार करा देगा। ज्ञान में प्रेम और योग मिला दे तो ज्ञान ईश्वर से अभिन्न कर देगा। योग में ज्ञान और प्रेम मिला दो तो सर्व समर्थ स्वरूप अपने आपा का अनुभव हो जायगा।
मतलब, प्रेमा भक्ति कर के अपने परिच्छिन्न अहं को मिटा दो, योग कर के अपनी दुर्बलता मिटा दो और ज्ञान पा कर अपना अज्ञान मिटा दो। ज्ञान ऐसा हो कि देहाध्यास गल जाय।
क्रिया के साथ ज्ञान हो और ज्ञान के साथ कर्म हो। दोनों का समन्वय हो। ज्ञान में सुख भी होता है और समझ भी होती है। ब्रह्मचर्य रखना अच्छा है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है और लम्बे समय तक चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है। यह समझ तो है लेकिन जब सुख की लोलुपता आ जाती है तो ब्रह्मचर्य से गिरकर आदमी विकारी सुख क्षणभर के लिए लेता है और फिर पछताता है। पापी आदमी को विकारी सुख में रुचि होती है। आपको ज्ञान के साथ सुख की भी जरुरत है।
माना है कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, किसी का अहित करना फायदे में नहीं है। सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य बोलते हैं लेकिन जब दुःख पड़ता है तब सत्य को छोड़कर असत्य बोले देते हैं। क्यो? सुख के लिए। झूठ किसलिए बोलते हैं? सुख के लिय। ब्रह्मचर्य खंडित क्यों करते हैं? तुच्छ सुख के लिए।
माँग तुम्हारी सुख की है।
गंगाजी गंगोत्री से चली। लहराती गुनगुनाती गंगा सागर को मिलने भाग रही है। गंगा जहाँ से प्रकट हुई है वहीं जा रही है। ऐसे ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने के लिए ही तुम्हारे जीवन की आकांक्षा है। तुम आनन्दकन्द, सच्चिदानन्द परमात्मा से प्रकट हुए हो, स्फुरित हुए हो। तुम जिसे 'मैं... मैं.... मैं.....' बोल रहे हो वह 'मैं' आनन्द-स्वरूप परमात्मा से स्फुरित हुई है। वह मैं आनन्द-स्वरूप परमात्मा तक पहुँचने के लिए ही सारी क्रियाएँ कर रही है। जैसे गंगाजी चली तो सागर तक पहुँचने के लिए ही सारी चेष्टा करती है। लेकिन हमने स्वार्थपरायण होकर उसके बहाव को रोककर तालाब बना दिया, उसको थाम दिया तो वह पानी गंगासागर तक नहीं पहुँचता। ऐसे ही सुख की प्राप्ति की इच्छा है और हमारी सुबह से शाम तक की दौड़ सुख तक पहुँचने की है लेकिन जहाँ बिना ज्ञान के, बिना समझ के, स्वार्थी, ऐन्द्रिक सुख की चेष्टा करते हैं तो गंगाजल को रास्ते में खड्डों में बाँध देते हैं। ऐसे ही हमारी चित्त की धारा को अज्ञानवश मान्यता में हम उंडेल देते हैं तो हमारा जीवन रास्ते में रुक जाता है। हालाँकि हमारा प्रयत्न तो सुख के लिए हैं लेकिन हमारा आत्मा सुख स्वरूप है, इस प्रकार का ज्ञान न होने के कारण हम बीच में भटक जाते हैं और जीवन पूरा हो जाता है। अर्थात् जीव अपना असली ब्रह्मस्वरूप नहीं समझ पाता।
हम जो-जो नियम शास्त्रों से सुनते है, स्वीकार करते हैं वे नियम तब खण्डित करतेहैं जब हमें भय हो जाता है अथवा सुख की लोलुपता हमें घेर लेती है। हम नीचे आ जाते हैं। तब क्या करना चाहिए?
सुख की लोलुपता और दुःख के भय को मिटाना हो तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। वह ज्ञान तत्त्वज्ञान हो अथवा तत्त्वज्ञान का सुख पाने की तरकीब रूप योगयुक्तियाँ हो। योगयुक्तियाँ और तत्त्वज्ञान से जब भीतर का सुख मिलने लगेगा तो निर्भयता आने लगेगी। फिर हमारी समझ के खिलाफ हम फिसलेंगे नहीं।
संत सुंदरदासजी महाराज उच्च कोटि के साक्षात्कारी पुरुष थे। नवाब ने उनके चरणों में सिर रखा किः "बाबाजी ! जिस आनन्द में आप आनन्दित होते हो, जिस परमात्मा को पाकर आप तृप्त हुए हो, जिस ईश्वर के साक्षात्कार से आप आत्मारामी हुए हो वह हमें भी उपलब्ध करा दो।"
सुना है कि जब सात जन्मों के पुण्य जोर करते हैं तब आत्म-साक्षात्कारी संत महापुरुष के दर्शन करने की इच्छा होती है। दूसरे सात जन्म के पुण्य जब सहयोग करते हैं तब उनके द्वार तक ही पहुँच पायेंगे। तीसरे सात जन्म के पुण्य उनमें नहीं मिलेंगे तो हम उनके द्वार से बिना दर्शन ही लौट जायेंगे। या तो बाबा जी कहीं बाहर चले गये होंगे फिर पहुँचेंगे अथवा बाबाजी आनेवाले होंगे उससे पहले रवाना हो जायेंगे, बाद में बाबाजी लौटेंगे। जब तक पूरे इक्कीस जन्मों के पुण्य जोर नहीं मारेंगे तब तक आत्म-साक्षात्कारी महापुरुषों के दर्शन नहीं होंगे, उनके वचनों में विश्वास नहीं होगा।
स्वल्पपुण्यवतां
सजन्
विश्वासो नैव
जायते।
अल्प पुण्यवालों को तो आत्मवेत्ता संत पुरुषों के दर्शन और वचन में विश्वास ही नहीं हो सकता है। तुलसीदासजी कहते हैं-
बिन
पुण्यपुंज
मिले नहीं
संता।
नवाब कहता हैः "महाराज ! मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है अब चाहता हूँ कि आप जिस आत्मरस से, जिस आत्मज्ञान से कृतकार्य हुए हैं वह आत्मा कैसा है उसका अनुभव मुझे कराइये।"
सुन्दरदासजी ने स्वच्छ जल से भरा हुआ काँसे का एक कटोरा मँगवाया। उसमें थोड़ी भस्म मिलाई। फिर कहाः
"नवाब ! इस जल में अपना मुख देखो।"
"भगवन् ! इसमें नहीं दिख पायगा। यह तो कीचड़ जैसा हो गया।"
"अच्छा।" फिर स्वच्छ जल का दूसरा कटोरा मँगवाया और उसको थोड़ा धक्का देकर पानी हिला दिया और कहाः
"अब इसमें अपना मुँह देखो।"
"स्वामीजी ! अब मुँह तो दिख रहा है लेकिन विचित्र-सा दिख रहा है, खण्ड-खण्ड होकर दिख रहा है। साफ नहीं दिखता।"
पानी को स्थिर होने दिया फिर कहाः "अब इसमें देखो।"
"महाराज ! अब ठीक दिख रहा है।" महाराजजी ने पानी डाल दिया और चुप होकर बैठे गये। नवाब ने फिर प्रार्थना की किः "महाराज ! हम लोग आत्मा का अनुभव कैसे करें? कैसे उस परमात्मा को पाएँ? कैसे हमें आनन्द-स्वरूप की अनुभूति हो? कृपा करके बताइये।"
सुन्दरदासजी
ने कहाः "मार्ग
मैंने 'प्रेक्टीकल
बता दिया।
केवल
सैद्धान्तिक
ही नहीं,
व्यावहारिक
सुझाव दे
दिया।"
"महाराज ! हम समझे नहीं। जरा विस्तार से कहिए नाथ।"
तब संतश्री ने कहाः "पहले राखवाले पानी में मुँह देखने को कहा, नहीं देख पाये क्योंकि पानी मैला था। ऐसे ही चित्त जब मैला होता है, विषय-वासनायुक्त चेष्टाएँ होती हैं, ज्ञान बिना की क्रियाएँ होती हैं उससे चित्त मलिन हो जाता है। मलिन चित्त में तुम्हारे आत्मा-परमात्मा का मुखड़ा नहीं दिख सकता। चित्त शुद्ध होने लगता है तो समझ बढ़ती है। आदमी में आध्यात्मिक योग्यता पनपने लगती है।"
कोई आदमी अच्छे पद पर है। वह चाहे तो लाखों-करोड़ों रुपये इकट्ठे कर सकता है लेकिन उसे भ्रष्टाचार अच्छा नहीं लगता। तो समझो, भगवान की उस पर कृपा है। लोग चाहे कुछ भी सोच लें, मूर्ख लोग चाहे कुछ भी कह दें कि साहब भोले भाले हैं, लेकिन वास्तव में साहब समझदार हैं।
भ्रष्टाचार करने का मौका है फिर भी नहीं किया, कपट करके धनवान होने का मौका है फिर भी कपट नहीं किया तो हमारे दिलरूपी कटोरे में जो राख है वह चली जायगी, मल चला जायगा। पानी स्वच्छ हो जायगा। अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा।
अन्तःकरण स्वच्छ तो हो जायगा लेकिन अब भी उसमें अपना मुखड़ा नहीं दिखेगा। आत्म-साक्षात्कार नहीं होगा। क्यो? क्योंकि चित्त शुद्ध तो हुआ है लेकिन आत्म-साक्षात्कार के लिए केवल चित्त शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। हम अच्छा व्यवहार करते हैं, सात्त्विक हैं, किसी का शोषण नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, बचपन से संतों के पास जाते हैं यह ईश्वर की बहुत कृपा है, धन्यवाद है, लेकिन साक्षात्कार के लिए एक कदम और आगे रखना होगा भैया !
चित्त शुद्ध है इसलिए बैठते ही भगवान की भक्ति स्मरण हो आती है, धन्यवाद है। लेकिन भगवत्तत्व का बोध तब तक नहीं होगा, आत्म-साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक चित्त की अविद्या निवृत्त न हो।
चित्त के तीन दोष हैं- चित्त का मैलापन, चित्त की चंचलता और चित्त को अपने चैतन्य का अभान। मल, विक्षेप और आवरण।
समझ से युक्त क्रियाएँ करने से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध व्यवहार से चित्त शुद्ध होता है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से भी चित्त शुद्ध होता है।
शुद्ध चित्त को ध्यान से एकाग्र किया जाता है। एकाग्र चित्त में अगर तत्त्वज्ञान के विचार ठीक ढंग से बैठ गये तो साक्षात्कार हो जाये।
महाराजा भर्तृहरि अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर जोगी बन गये। सहज स्वभाव विचरण करते-करते किसी गाँव से गुजरे तो दुकान पर हलवाई हलवा बना रहा था। हलवे की खुश्बू ने उनके चित्त को आकर्षित कर लिया। सम्राट होकर तो खूब भोग भोगे थे। पुराने संस्कार जग आये। हलवा खाने की इच्छा हो गई। हलवाई को कहाः
"भाई ! हलवा दे दे।"
"पैसे हैं तुम्हारे पास?" जोगी को घूरते हुए हलवाई बोला।
"पैसे तो नहीं है।"
"बिना पैसे हलवा कैसे मिलेगा? पैसे लाओ।"
"पैसे कहाँ मिलेंगे?" भर्तृहरि ने पूछा।
हलवाई बोलाः "गाँव की दक्षिण दिशा में दुष्काल राहत कार्य चल रहा है, तालाब खुद रहा है। वहाँ जाओ। मजदूरी करो। शाम को पैसे मिल जाएँगे।"
एक समय का सम्राट वहाँ गया। कुदाली-फावड़ा चलाया। मिट्टी के टोकरे उठाए। दिनभर मजदूरी की। शाम को पैसे मिले और आ गये हलवाई की दुकान पर। हलवा लिया और पूछते-पूछते गाँव की उत्तर दिशा में तालाब की ओर चले।
भर्तृहरि अपने मन को कहने लगेः "अरे मनीराम ! तूने राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, घरबार छोड़ा, सम्राट पद छोड़ा और हलवे में अटक गया? हलवा नहीं मिला इसलिए दिन भर गुलामी करवाई?
बदमाश ! जरा सी लूली के लाड़ लड़ाने के लिए इतना परेशान किया?"
मन को अगर थोड़ी सी छूट देंगे तो वह और ज्यादा छूट ले लेगा। पास में भैंस का गोबर पड़ा था। भर्तृहरि ने वह उठाया और तालाब के किनारे पहुँचे। एक हाथ से हलवे का कौर उठाकर मुँह तक लाते और फिर तालाब में डाल देते जो मछलियाँ खा जाती। दूसरे हाथ से गोबर का कौर उठाते और मुँह में ठूँसते, अपने आपको कहतेः 'ले, खा यह हलवा।' ऐसे करते-करते करीब पूरा हलवा पानी में चला गया। गोबर का काफी हिस्सा चला गया पेट में। हलवे का आखिरी ग्रास हाथ में बचा तब मन मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गया और बोलाः
"हे नाथ ! अब तो कृपा कीजिए। इतना तो जरा-सा खाने दीजिए !"
लेकिन निष्ठा इतनी परिपक्व थी, दृढ़ता थी कि वे अपने निश्चय में अचल थे। मन को कहाः
"तूने पूरे दिनभर मुझे धूप में नचाया, मजदूरी करवाई और अभी हलवा खाना है? सदियों से तूने मुझे गुलाम बनाया है और अब भी मैं तेरे कहने में चलूँ?"
भर्तृहरि ने वह आखिरी कौर भी तालाब में फेंक दिया। मन ने देखा कि मैं किसी वीर के हाथ लगा हूँ।
एक बार मन आपके आगे हार जाता है तो आपमें सौ गुनी ताकत आ जाती है। आप मन के आगे हार जाते हो तो मन को सौ गुनी ताकत आ जाती है आपक नचाने के लिए।
जितना ध्यान और ज्ञान का अभ्यास बढ़ेगा, उनका हम पर प्रभाव रहेगा उतना हम मन पर विजय पायेंगे। जितना ज्ञान और ध्यान से वंचित रहकर क्रियाएँ करेंगे उतना ही मन पर हम पर विजेता हो जायेगा।
एक सेठ को मुनीम ने कहाः "सेठजी ! सात सौ में मेरे परिवार का पूरा नहीं होता। मुझे महीने का पंद्रह सौ चाहिए।"
सेठ ने कहाः "जा चला जा.... गेट आउट।"
मुनीम ने कहाः "कोई हरकत नहीं। मैं तो गेट आउट हो जाऊँगा लेकिन आप सदा के लिए गेट आउट हो जायेंगे।"
"क्या बात है?"
"मुझे पता है। आपने मुझसे जो बहियाँ लिखवाई हैं और इन्कमटैक्स के फार्म भरवाये हैं... तुमने मुझसे जो गलत काम करवाये हैं, अलग हिसाब रखवाये हैं उसकी सब जानकारी मेरे पास है। अगर आप पन्द्रह सौ तनख्वाह नहीं देते तो कोई हरकत नहीं। मैं चला जाऊँगा इन्कमटैक्स ऑफिसरों के पाश"
सेठजी ने कहाः "तुम भले सौलह सौ ले लो लेकिन रहो यहाँ।"
मुनीम जानता था सेठ की कमजोरी। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर ज्ञान और ध्यान नहीं है तो मन हमारी कमजोरियाँ जानता है। हाँ, सेठ को अगर इन्कमटैक्स कमिश्नर के साथ सीधा व गहरा सम्बन्ध होता, तो वह सेठ मुनीम को लात मार देता। ऐसे ही सब मिनिस्टरों के भी मिनिस्टर परमात्मा के साथ सीधा सम्बन्ध हो जाय तो मनरूपी मुनीम का ज्यादा प्रभाव न रहे। जब तक परमात्मा के साथ सम्बन्ध न हुआ हो तब तक तो मन को रिझाते रहो।, उससे दबे-दबे रहो।
अपनी योग्यता को ऐसी विकसित कर लो कि मनरूपी मुनीम जब जैसा चाहे वैसा हमें न नचाए लेकिन हम जैसा चाहें वैसा मुनीम करने लगे।
हम अपने मनरूपी मुनीम के आगे सदा से हारते आए हैं। इसने हम पर ऐसा प्रभाव डाल दिया कि हमें जैसा कहता है वैसा हम करते हैं। क्योंकि प्रारम्भ में ज्ञान था नहीं।
ध्यान और ज्ञान का प्रभाव नहीं है तो हम दुर्बल हो जाते हैं, हमारा गुलाम मन-मुनीम बलवान हो जाता है। दिखते तो हैं बड़े-बड़े सेठ, बड़े-बड़े साहब, बड़े-बड़े अधिकारी लेकिन गहराई में गोता मार कर देखें तो हम गुलाम के सिवाय और कुछ नहीं हैं। क्योंकि मनरूपी गुलाम के कहने में चल रहे हैं।
मन की गुलामी जितने अंश में मौजूद है उतने अंश में दुःख मौजूद है, पराधीनता मौजूद है, परतन्त्रता मौजूद है। यह गुलामी कैसे दूर हो?
गुलामी दूर होती है समझ से और सामर्थ्य से। ज्ञान समझ देता है और ध्यान सामर्थ्य देता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
खोजो
अपने आपको
रमण महर्षि के पास कुछ भक्त पहुँचे। जिनकी दृष्टि मात्र से जीव आनन्द को प्राप्त होता है, जिसकी महिमा गाते शास्त्र थकते नहीं, युद्ध के मैदान में न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण जिस ज्ञान की श्रेष्ठता व पवित्रता बताते हैं उस ज्ञान को प्राप्त किये हुए आत्मवेत्ता जीवन्मुक्त महापुरुष के दर्शन करने की कई दिनों की इच्छा पूर्ण हुई। सुना था कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष श्री रमण महर्षि के सान्निध्य में बैठने मात्र से हृदय शान्ति व आनन्द का अनुभव करता है। आज वह सुअवसर प्राप्त हो गया।
भक्त-मण्डल महर्षि को प्रणाम करके बैठा। किसी ने श्रीकृष्ण की आराधना की थी तो किसी ने अम्बाजी की, किसी ने रामजी को रिझाने के प्रयास किये थे तो किसी ने सूर्यनारायण को अर्घ्य दिये थे किसी ने व्रत किये थे तो किसी ने फलाहार से वर्ष बिताए थे। किसी ने दो देव बदले थे तो किसी ने तीन, चार या पाँच देव बदले थे।
जब तक ज्ञानवान, आत्मारामी, प्रबुद्ध महापुरुष के चरणों में जाकर साधना का मार्ग सुनिश्चित नहीं होता तब तक मनमानी साधना जमती नहीं। हृदय की गहराई में आशंका बनी रहती है कि साधना पूर्ण होगी कि नहीं, फलदायी बनेगी कि नहीं। गहराई में यह संदेह विद्यमान हो तो ऊपर-ऊपर से कितने ही व्रत नियम करो, कितनी ही साधना करो, शरीर को कष्ट दो लेकिन पूर्णरूपेण लाभ नहीं होता। अचेतन मन में सन्देह बना ही रहता है। यही हम लोगों के लिए बड़े में बड़ा विघ्न है।
योगवाशिष्ठ महारामायण में आया है कि शमवान पुरुष के सर्व सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, उसके चित्त में शोक के प्रसंग में शोक नहीं होता, हर्ष के प्रसंग में हर्ष नहीं होता, भय के प्रसंग में भयभीत दिखता हुआ भी भयभीत नहीं होता, रूदन के प्रसंग में रोता हुआ दिखता है फिर भी नहीं रोता है, सुख के प्रसंग में सुखी दिखता है फिर भी सुखी नहीं होता।
जो सुखी होता है वह दुःखी भी होता है। जितना अधिक सुखी होता है उतना अधिक दुःख के आघात सहता है। मान के दो शब्दों से जितना अधिक खुश होता है उतना अधिक अपमान के प्रसंग में व्यग्र होता है। धन की प्राप्ति से जितना अधिक हर्ष होता है, धन चले जाने से उतना अधिक शोक होता है। चित्त जितना तुच्छ, हल्का और अज्ञान से आक्रान्त होता है उतना ही छोटी-छोटी बातों से क्षोभित होता है। चित्त जब बाधित हो जाता है तब क्षोभित होता हुआ दिखे उसको क्षोभ स्पर्श नहीं कर सकता। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को कहाः
धीरो
न द्वेष्टि ससारं
आत्मानं न
दिदृक्षति।
हर्षाभर्षविनिर्मुक्तो
न मृतो न च
जीवति।।
"हर्ष और द्वेष से रहित ज्ञानी संसार के प्रति न द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। वह न मरा हुआ है और न जीता है।"
(अष्टावक्र
गीताः 83)
जो धीर पुरुष हैं, शम को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध कर लिया, परमात्म-दर्शन कर लिया, ब्रह्मा-विष्णु-महेश समन्वित विश्व के तमाम देवों की मुलाकात कर ली, जो अपने स्वरूप में परिनिष्ठित हो गये वे ही कृतकृत्य हैं। शास्त्रों में उन्हीं को धीर कहा है।
जो क्षुधा-तृषा, सर्दी-गर्मी सहन करते हैं उनमें तो धैर्य तो है लेकिन वे तपस्वी हैं। वे व्यावहारिक धैर्यवान हैं। शास्त्र किनको धैर्यवान कहते हैं? अष्टावक्र मुनि कहते हैं- धीरो न द्वेष्टि संसारम्.... संसार की किसी भी परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होता, उसे द्वेष नहीं होता। आत्मानं न दिदृक्षति। आत्मा-परमात्मा का दर्शन करने की, उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। संसार की प्राप्ति तो नहीं चाहता, इतना ही नहीं प्रभु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रही। क्योंकि अपना आत्मा ही प्रभु के रूप में प्रत्यक्ष हो गया है। फिर प्राप्त करना कहाँ बाकी रहा? जैसे, मेरे को आसारामजी महाराज के दर्शन करने की इच्छा नहीं। अगर मैं इच्छा करूँ तो मेरी इच्छा फलेगी क्या? मैं जानता हूँ कि आसारामजी महाराज कौन हैं।
जिसने अपने-आत्मस्वरूप को जान लिया, परमात्म-स्वरूप को जान लिया उसको परमात्म-प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती।
हर्षाभर्षविनिर्मुक्तो
न मृतो न च
जीवति।
हर्ष और शोक, सुख और दुःख – इन द्वन्द्वों से ठीक प्रकार से मुक्त हो जाता है। वह जीता भी नहीं और मरता भी नहीं। साधारण मनुष्य हो जाता है। वह जीता भी नहीं और मरता भी नहीं। साधारण मनुष्य दिन में कई बार जीता मरता रहता है। धीर पुरुष किसी भी प्रसंग से जीता-मरता नहीं और देह के विसर्जन से भी मरता नहीं।
ऐसे धीर पुरुष के समक्ष बैठने से चित्त में उल्लास, शान्ति, आनन्द का प्राकट्य होता है। महादुराचारी, पापी आदमी पर भी महापुरुष की दृष्टि पड़े तो कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। जीवन में कुछ पुण्य किये हों, उपासना आराधना की हो, किसी के आँसू पोंछे हों, माता-पिता का दिल शीतल किया हो तो अधिक लाभ मिलता है।
उन भक्तों के जन्मों के पुण्य फलित हुए तो वे सत्पुरुष के सान्निध्य में पहुँच सके। उन्होंने रमण महर्षि से प्रश्न कियाः
"स्वामी जी ! हमें कैसी साधना करनी चाहिए? रामायण सुनते हैं तो भगवान श्रीराम सर्वेसर्वा लगते हैं। भागवत की कथा सुनते हैं तो 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव' यह मंत्र भाता है। शिवपुराण सुनते हैं तो 'नमः शिवाय' मंत्र प्यारा लगता है। कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। अब हम क्या करें?"
सब भक्तों ने इस प्रकार अपने-अपने प्रश्न महर्षि के समक्ष प्रस्तुत किये। ये प्रश्न केवल उन लोगों का ही नहीं था, हम सबका भी यही प्रश्न है। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक छोटी-छोटी बातों में चित्त उद्विग्न हो जाता है। उपासना करने से चित्त थोड़ा शुद्ध होता है, स्थिर होता है और आत्मबोध से चित्त बाधित होता है। शुद्ध बना हुआ चित्त फिर अशुद्ध हो सकता है लेकिन बाधित चित्त शुद्धि-अशुद्धि के पार पहुँच जाता है।
रमण महर्षि ऐसी बात बताते हैं जहाँ देव बदलने और चित्त के पतन व उत्थान को स्थान ही न मिले। महर्षि ने सबके प्रश्न सुने। क्षणभर निजानन्द में गोता लगाया। फिर बोलेः
"भाई ! तुम जिस देव की उपासना आराधना करते हो वह सब ठीक है। बार-बार अपने को प्रश्न करो कि उपासना आराधना करने वाला मैं कौन हूँ? सतत अपने आप से यह प्रश्न करो। तुम्हारा जो कोई देव होगा वह प्रसन्न मिलेगा। देवो भूत्वा दैवं यजेत्। देव होकर देव की पूजा करो।"
तुम कौन हो? तुम यदि हाड़-मांस के अनथाभाई, छनाभाई होकर पूजा करोगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। तुम अपने को खोजो तो पता चलेगा कि तुम कैसे दिव्य देह हो। तुम्हारी आत्मा कितनी महान है। 'मैं कौन हूँ' यह प्रश्न अपने को पूछो और अपने आपको खोजो तो तमाम प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिलते जायेंगे। भीतर से अपने आपकी सही पहचान हो गई तो तुम्हारे सब जप-तप फलित हो गये, सब दान-पुण्य सार्थक हो गये। फिर तो तुम्हारी मीठी निगाहें जिन पर पड़ेगी वे भी लाभान्वित होने लगेंगे।
बात छोटी-सी लगती है लेकिन पच्चीस-पचास साल से अलग-अलग उपासना करने से जो आध्यात्मिक विकास नहीं होता वह विकास 'मैं कौन हूँ' की खोज से हो सकता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
गीताज्ञान-सरिता
येषां
त्वन्तगतं
पापं जनानां
पुण्यकर्मणाम्।
ते
द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
भजन्ते मां
दृढ़व्रताः।।
'निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग-द्वेष जनित द्वन्द्वरूप मोह से मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं।'
(गीताः
7.28)
द्वन्द्व कई प्रकार के होते हैं- गृहस्थ जीवन के द्वन्द्व, ब्रह्मचारी जीवन के द्वन्द्व, वानप्रस्थ जीवन के द्वन्द्व, संन्यास जीवन के द्वन्द्व, स्वर्ग में जाओ तो भी द्वन्द्व और उपासना मार्ग में जाओ तो भी द्वन्द्व। कोई साधना करने लगेगा तो प्रश्न होगा कि ये देव बड़े कि वो देव बड़े? ये भगवान बड़े? यह साधना बड़ी कि वह साधना बड़ी? ये संत बड़े कि वे संत बड़े?
तमाम प्रकार के द्वन्द्व हमारे चित्त की शक्तियों को बिखेर देते हैं। लेकिन जिनके पापों का अन्त हो गया है ऐसे भक्त चित्त की तमाम शक्तियों को केन्द्रित करके भगवान के भजन में दृढ़तापूर्वक लग जाते हैं। दृढ़ता से भगवान का भजन करने वाला भगवन्मय हो जाता है।
भजन में जब तक दृढ़ता नहीं आती तब तक भजन का रस नहीं आता जब तक भजन का रस नहीं आता तब तक भव के रस का आकर्षण नहीं जाता।
मनुष्य की अपेक्षा जीव शाश्वत है। मनुष्य साठ, सत्तर, अस्सी साल तक जीता है जबकि जीव अनन्त शरीर बदलता हुआ जीता है। मनुष्य को संस्कार देने पड़ते हैं कि तू जीव नहीं है, शिवस्वरूप है। प्रारंभ में दीक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि अब तू ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्याश्रम के धर्मों का पालन कर। फिर दूसरे आश्रम में प्रवेश होता है तब अध्यारोप किया जाता है कि तू गृहस्थी है। फिर वानप्रस्थी है और आखिर में परम पद पाने के लिए संन्यास।
प्रारम्भ में व्यावहारिक दृष्टि से अध्यारोप हुआ कि 'मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ।' इन अध्यारोपों को हटाने के लिए संन्यस्त का अध्यारोप किया गया।
संन्यास माने क्या? सर्व संकल्पों का त्याग। पैर में काँटा चुभ जाय तो उसे निकालने के लिए दूसरा काँटा (सुई) जान-बूझकर चुभाया जाता है। पैर में रखने के लिए नहीं अपितु पहले काँटे को निकालने के लिए यह दूसरा चुभाया है। पहला निकल गया तो दूसरा भी निकाल दिया जाता है।
ऐसे ही जन्म-जन्मांतरों के संस्कार-कुसंस्कार धोने के लिए ब्रह्मचर्याश्रम के नियम-धर्म, गृहस्थ और वानप्रस्थ के नियम धर्म को स्वीकार कराया जाता है। 'मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन, साधना, विद्याभ्यास, वेदशास्त्रों का अभ्यास और गुरुसेवा करना मेरा पवित्र कर्त्तव्य है।' फिर, 'मैं गृहस्थी हूँ। धर्म के मुताबिक धनोपार्जन करना, पवित्रता से जीवन जीना और जीने देना, इतर तीन आश्रमों का यथाशक्ति पोषण करना मेरा कर्त्तव्य है।' फिर, 'मैं वानप्रस्थी हूँ। इन्द्रिय-संयम करके अब मुझे तपस्वी जीवन बिताना चाहिए।' लेकिन 'मैं कौन हूँ?' इसका ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले अध्यारोपित संस्कारों को निर्मूल करने के लिए संन्यास धर्म को स्वीकार किया जाता है।
संन्यास का अर्थ है तमाम इच्छाओं का त्याग। हृदय में जब मोक्ष की तीव्र इच्छा जगे तब दूसरी छोटी-मोटी तमाम इच्छाएँ उस मुमुक्षा की अग्नि में स्वाहा हो जाती है। दूसरी इच्छाओं से पल्ला छुड़ाने के लिए मोक्ष की इच्छा की जाती है। जब दूसरी इच्छाएँ भली प्रकार हट गई तो मोक्ष की इच्छा का भी बाध किया जाता है। तब 'मेरा मोक्ष हो, परमात्मा का दीदार हो' – ऐसी भावना भी आवश्यक नहीं रहती। मोक्षेच्छा मिटते ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है।
साधक को यह मार्ग समझ में आ जाये, किसी सच्चे सदगुरु का मार्गदर्शन मिल जाय तो कार्य सरल बन जाता है। अन्यथा तो बाहर के मंदिर-मस्जिदों में जाते-जाते, बाहर के देवी-देवताओं को पूजते-पूजते, संसार-व्यवहार चलाते-चलाते, इन्द्रियों के विषयों में भटकते-भटकते, विविध प्रकार के द्वन्द्वों में उलझते-उलझते एक ही आयुष्य नहीं बल्कि युग के युग बीत गये।
एक शाम को भोजू सोने की सुई से कपड़ा सीने की चेष्टा कर रहा था। नयी-नयी शादी हुई थी और सोने की सुई दहेज में मिली होगी। सुई की नोक हाथ में चुभी और झटका तो सुई गिर पड़ी ,खो गई। घर में अन्धेरा हो रहा था। भोजू भागा बाजार में नगरपालिका के फानूस की रोशनी में धूल के छोटे-छोटे ढेर बनाकर सुई खोजने लगा। रात के आठ बजे.... नौ... दस र ग्यारह बजे। भोजू अपने कार्य में बड़ा व्यस्त था। खाना-पीना भी याद नहीं। सोने की सुई जो खोई थी ! रात्री के बारह बजे नाटक देखकर लौटते हुए मित्रों ने देखा तो पूछाः
"अरे भाई भोजू ! यह सब क्या कर रहा है?"
"माफ करो। मैं बहुत काम में हूँ।" भोजू ने सिर ऊँचा किए बिना अपना काम चालू रखा।
"अरे दोस्त ! बता तो सही ! हम कुछ सहाय करें।" मित्र-मण्डल भोजू के इर्द-गिर्द जमा हो गया।
"सहाय करना हो तो करो लेकिन मेरे पास समय नहीं है बातें करने का। बहुत जरूरी काम में लगा हूँ।"
"कौन सा जरूरी काम?" मित्रों की उत्सुकता बढ़ी।
"सोने की सुई खो गई है।" आखिर भोजू ने बता ही दिया।
"कहाँ खोई?"
"खोई तो घर में है..."
"तो यहाँ क्यों खोज रहा है?" मित्रों को आश्चर्य हुआ।
"घर में अन्धेरा है। वहाँ दीया कौन जलाये? यहाँ जलता हुआ फानूस तैयार है।" भोजू ने अपना प्रगाढ़ (अ) ज्ञान प्रकाशित किया।
"अरे पगला ! इस प्रकार यहाँ खोजते-खोजते एक रात्री नहीं, पूरा आयुष्य बिता देगा तो भी सुई यहाँ नहीं मिलेगी। घर में जा, दीया जला और सुई जहाँ खोई है वहीं खोज।"
इस प्रकार जीव सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, मृत्यु के बाद नये जन्म में.... इस प्रकार युग-युगान्तर तक 'सुखों को पकड़े रखना और दुःखों को दूर करना' – इसी दौड़ में लगा है।
सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? दुःख को दूर हटाना और सुख को सम्भालना। हरेक प्राणी जीवन से मृत्यु पर्यंत यही प्रवृत्ति करता है। आखिर में उसे क्या हाथ लगता है? सभी भोजू के साथी....। सुख कहाँ है यह पता नहीं। सुख खोया है यह तो थोड़ा-थोड़ा पता लगता है लेकिन कहाँ खोजना चाहिए इसकी सूझ नहीं। खोया है घर में और खोजता है बाजार में।
कबीरजी कहते हैं-
भटक
मूंआ भेदू
बिना पावे कौन
उपाय।
खोजत
खोजत युग गये
पाव कोस घर
आय।।
सुख को खोजते-खोजते, शान्ति को खोजते-खोजते, अमरता को खोजते-खोजते युग बीत गये फिर भी जीव बेचारा अभागा ही रह गया। हरेक जन्म में बाप किये, माँ की, पति किये, पत्नी की, घरबार बनाये, परिवारों को निभाये, क्या-क्या नहीं किया बेचारे ने? लेकिन मृत्यु का एक ही झटका और सब किया कराया चौपट। फिर दूसरे गर्भ में उल्टा होकर लटकना, नारकीय यातनाओं के साथ जन्मना, दुःख भोगते-भोगते जीना। जैसा-जैसा वातावरण मिला वैसे संस्कार चित्त में जम गये। जीव सोचता है कि इतना कर लूँ तो आराम.... बाबाजी हो जाऊँ, फिर आराम....। यह कर लूँ फिर आराम.... वह कर लूँ फिर आराम...। ऐसा करते-करते जीवन पूरा हो गया। आखिर पूछो कि "पशा काका ! क्या हाल है?"
"अरे काका ! मरने में भी आराम नहीं है।"
बिलकुल सच बात है। मरने में भी आराम नहीं और करने में भी आराम नहीं। तो आराम कहाँ है?
येषां
त्वन्तगतं
पापं जनानां
पुण्यकर्मणाम्।
ते
द्वन्द्वमोहिनिर्मुक्ता
भजन्ते मां
दृढ़व्रता।।
जिनके पापों का अन्त हुआ हो, पुण्य कर्मों का उदय हुआ हो, मोह विनिर्मुक्त हुआ हो वह दृढ़ता से भगवान का भजन कर सकता है। ज्ञान के बिना भजन नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना पुण्य नहीं हो सकता, साक्षात् भगवान भी तुम्हारे कन्धे से टकराकर चले जायें तो ज्ञान के बिना पता नहीं चलता।
श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि वसुदेवजी ने यज्ञ किया। नारदजी पधारे तो वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगेः
"भगवान ! हमारे अहोभाग्य कि आप जैसे प्रभु पधारे। हे देवर्षि ! अब मुझ पर कृपा करो कि मुझे भगवान के दर्शन हो जायें। मेरा कल्याण हो जाय।"
यह सुनकर नारदजी सस्मित-वदन होकर कहने लगेः "अरे वसुदेवजी ! ये सब साधू-संत महात्मा लोग आपके यज्ञ के धूएँ चाटने आये हैं क्या? हम लोग यहाँ क्यों आये हैं?"
"महाराज ! आपने पधार कर हमें दर्शन दिये लेकिन..."
"अरे हम भी भगवान के दर्शन करने ही तो यहाँ आये हैं।"
"अच्छा ! कहाँ हैं भगवान?" वसुदेवजी विस्फुरित नेत्रों से देखने लगे।
"वहाँ देखो..... वह नटखट नागर संतो की जूठी पत्तल उठा रहे हैं।"
"अरे वह तो मेरा कन्हैया है। आप मुझे भगवान के दर्शन कराइये।"
भगवान जिनकी गोद में खेलते हैं ऐसे वसुदेवजी भी भगवत्तत्व का भान न होने से यज्ञ कराकर नारदजी से आशीर्वाद माँगते हैं और भगवान को खोजने की, पाने की तैयारियाँ कर रहे हैं।
एक बार मुंबई का कोई सज्जन अमदावाद के आश्रम में दर्शनार्थ आया। पुस्तकें पढ़ी होगी, लोगों से सुना होगा तो दर्शन करने की इच्छा जगी। हम कहीं बाहर गये थे। वह वापस लौट गया। दर्शन नहीं हो सके।
कुछ दिन बाद उसे व्यवसाय के निमित्त लुधियाना जाना हुआ। लौटते वक्त सोचा कि अमदावाद होकर फिर मुंबई जायँगे। वह दिल्ली में 'रिजर्वेशन कोच' में बैठा। संयोगवशात् हम भी उसी गाड़ी से अमदावाद लौट रहे थे। उसी कम्पार्टमैन्ट में प्रवेश किया। उसे पता नहीं था कि जिन महाराज के दर्शनार्थ अमदावाद आश्रम में गया था वे ही महाराज हैं। वह बोलाः
"बाबाजी ! आगे जाओ।"
"हमारी रिजर्वेशन टिकट का नंबर 19 है। आपका कौन-सा है?" हमने पूछा।
"अठारह।" वह बोला।
"आप अपनी जगह बैठो, हम हमारी जगह बैठते हैं। आपको कोई हरकत नहीं है न? " हमने थोड़ा विनोद किया।
"अच्छा, बैठो।" मुँह बिगाड़ते हुए वह बोला।
गाड़ी चली। छोटे-मोटे स्टेशन आये और गये। जयपुर आया। अब भी उस सज्जन को बाबाजी के दर्शन नहीं हुए। जिनके दर्शन करने मुंबई से अमदावाद गये थे वे ही उसी कम्पार्टमैन्ट में पास वाली सीट पर बैठे थे फिर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं कि यही वे संत हैं।
गाड़ी अजमेर पहुँची। वहाँ के भक्तों को हमारे प्रवास की खबर मिल चुकी थी। फल-फूल लेकर भक्तों का टोला अजमेर के प्लेटफार्म पर जमा हो गया था। गाड़ी ने स्टेशन में प्रवेश किया तो 'आसारामजी महाराज की जय..... आसारामजी महाराज की जय......' के नाद से स्टेशन गुँजा दिया।
ये सज्जन खिड़की से बाहर झाँकने लगे। 'जिनके दर्शन करने अमदावाद गया था कि वे ही आसारामजी महाराज अजमेर में पधारे हैं क्या? इतने में भक्तों का टोला फूलहारों के साथ खोजता-खोजता हमारे कोच के पास आ पहुँचा। दर्शन होते ही फिर से जय-जयकार हुआ। भीतर आकर लोग प्रणाम करने लगे, फूलहार चढ़ाने लगे, बाहरवाले दूर से ही पुष्पवृष्टि करने लगे। सभी के चेहरे आनन्द से महक रहे थे। प्लेटफार्म पर आनन्द-उत्सव होने लगा।
ये सज्जन यह दृश्य देखकर दंग रह गये। किसी भक्त से पूछाः
"क्या ये ही अमदावादवाले आसारामजी महाराज हैं?"
"हाँ हाँ.... ये ही मोटेरावाले साँईं है।" भक्त बड़े उत्साह से बोला।
सुनकर तुरन्त वह सज्जन चरणों में लिपट पड़ा। गदगद् कण्ठ से बोल उठाः
"बापू...! बापू....!! मैंने पहचाना नहीं। आपके दर्शन के लिए तो मैं आश्रम में गया था। आपके दर्शन नहीं हुए। दिल्ली से आप साथ में हैं लेकिन...."
उस सज्जन को मुलाकात तो दिल्ली में हो गई लेकिन दर्शन अजमेर में हुए।
यह तो कल्पित प्रसंग आपको समझाने के लिए कहा। सत्य बात यह है कि बापूओं के बापू परब्रह्म परमात्मा हमारी सीट के ऊपर ही बैठे हैं लेकिन आज तक हमारा अजमेर नहीं आया। युगों से उनसे हमारी मुलाकात है, कभी वियोग सम्भव ही नहीं फिर भी आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। क्या आश्चर्य है !
अभी पापों का अन्त नहीं हुआ। पूरे पुण्यों का उदय नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में हमारी दृढ़ता नहीं आयी।
येषां
त्वन्तगतं
पापं जनानां
पुण्यकर्मणाम्।
ते
द्वन्द्वमोहिनिर्मुक्ता
भजन्ते मां दृढ़व्रता।।
वृत्रासुर और इन्द्र का युद्ध हुआ। वृत्रासुर कहता हैः "हे इन्द्र ! अब देर न करो। मेरा शीघ्र हनन करो। क्योंकि जो आया है सो जायगा। अभी मेरा मन श्रीहरि के स्नेह में लगा है। इस समय मुझे मार दोगे तो मैं श्रीहरि को प्राप्त हो जाऊँगा। जब संसार के द्वन्द्वों में मेरा मन रहे और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाये तो अवगति होगी। अभी मेरे लिए यह सुअवसर है। मुझे श्रीहरि की दृढ़भक्ति प्राप्त हो जायेगी। मेरे इस नश्वर देह को गिरा दो।"
धन-वैभव, साधन-संपदा अज्ञान से सुखद लगते हैं लेकिन उनमें द्वन्द्व रहते हैं। राग-द्वेष, इच्छा-वासना के पीछे जीव का जीवन समाप्त हो जाता है। द्वन्द्वों से मुक्त हुए बिना भगवान की दृढ़ भक्ति प्राप्त नहीं होती।
निर्द्वन्द्व तो वह हो सकती है जो जगत को स्वप्न तुल्य समझता है। निर्द्वन्द्व तो वह हो सकता है जो ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के ज्ञान को पचा लेता है। निर्द्वन्द्व तो वह हो सकता है जिसको शिवजी का अनुभव अपना अनुभव बनाने की तीव्र लगन लगी है। शिवजी भगवती पार्वती से कहते हैं-
उमा
कहौं मैं
अनुभव अपना।
सत्य
हरिभजन जगत सब
सपना।।
वृत्रासुर और इन्द्र का युद्ध हुआ होगा तब कितना घमासान मचा होगा, ठोस सत्य भासता होगा। अब देखो तो सब स्वप्न। रामायणकाल और महाभारतकाल सब स्वप्न। मंथरा का कपट, कैकेयी का क्रूर निश्चय, दशरथ का विरह, अयोध्यावासियों की करुण स्थिति, सुमन्त्र के आँसू, रामजी का वनगमन, शूर्पनखा की कामवृत्ति, लक्ष्मण की अथक सेवा और आखिर में राम-रावण का भीषण युद्ध। यह सब जिस समय हुआ होगा तब कितना ठोस सत्य भासता होगा। अब देखो तो देख स्वप्न।
ऐसे-ऐसे अवतारों की चेष्टाएँ और लीलाएँ काल के अन्तराल में स्वप्न की तरह सरक गई तो तुम्हारी-हमारी चेष्टाओं का मूल्य ही क्या है? समय की धारा में सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। गंगा के जल में दो बार कोई नहा नहीं सकता।
'मैं दस बार नहा सकता हूँ।' कोई कहे।
नहीं भैया ! जिस पानी में आपने गोता लगाया वह पानी तो कहीं का कहीं बह गया। जब-जब नया गोता लगाओगे तब नया पानी आ जायेगा। इसी प्रकार समय की धारा है। वैसे का वैसा समय आ सकता है वही का वही समय वापस नहीं आता। दीपक की लौ जलती है। वही की वही दिखती है लेकिन वही है नहीं। वैसी की वैसी है किन्तु हर पल नयी नयी हो रही है।
ऐसे ही हम वही के वही लगते हैं वास्तव में वही के वही हैं नहीं। हमारे शरीर के कोष हरदम बदल रहे हैं। हमारे विचार बदल रहे हैं, बुद्धि बदल रही है। हाँ, हमारा वास्तविक तात्विक स्वरूप वही का वही अपरिवर्तनशील है।
तुम जिसको 'मैं' मानते हो उस देह के कोष बदल रहे हैं, मन की वृत्तियाँ बदल रही हैं, बुद्धि के निर्णय बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं किन्तु जिसको तुम 'मैं' नहीं मानते वह आत्मा ही सचमुच तुम हो। उस सच्ची 'मैं' को तुम वास्तव में जान लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाय। फिर तो जिस पर तुम्हारी करुणामय दृष्टि पड़े वह द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ता के मार्ग पर चल पड़े।
राग-द्वेष से प्रेरित होकर जो कार्य किये जाते हैं वे द्वन्द्व और मोह को बढ़ाते हैं। ईश्वर-प्रीत्यर्थे कार्य किये जायें तो द्वन्द्वमोह निर्मूल होने लगते हैं। तुम क्या बोलते हो, किसके साथ बोलते हो उसकी गहराई में तुम्हारा ही अन्तर्यामी आत्मदेव है इस भाव बोलो तो तुम्हारे द्वन्द्व-मोह कम हो जायेंगे। चालू व्यवहार में भक्ति हो जायेगी, चालू व्यवहार में योग और ज्ञान का अभ्यास हो जायेगा। अन्तःकरण पवित्र होने लगेगा। तुम्हारा प्रभाव बढ़ने लगेगा फिर भी उसका अहंकार नहीं आयेगा।
ज्ञान का मार्ग ऐसा है कि अहंकार को उत्पन्न ही नहीं होने दे। अहंकार दूसरे को देखकर होता है। भय दूसरे को देखकर होता है। घृणा दूसरे को देखकर होती है। आसक्ति दूसरे पर होती। जब सबमें आत्मस्वरूप श्रीहरि को निहारा तो भय किससे? आसक्ति किससे? अहंकार किससे? नरसिंह मेहता ने कितना सुंदर गाया हैः
अखिल
ब्रह्माण्डमां
एक तुं
श्रीहरि।
जूजवे
रूपे अनन्त
भासे।।
दो संन्यासी युवक यात्रा करते-करते किसी गाँव में पहुँचे। लोगों से पूछाः "हमें एक रात्रि यहाँ रहना है। किसी पवित्र परिवार का घर दिखाओ।" लोगों ने बताया किः "वह एक चाचा का घर है। साधू-महात्माओं का आदर-सत्कार करते हैं। अखिल ब्रह्माण्डमां एक तुं श्रीहरि पाठ उनका पक्का हो गया है। वहाँ आपको ठीक रहेगा।" उन्होंने उन सज्जन चाचा का पता बताया।
दोनों संन्यासी वहाँ गये। चाचा ने प्रेम से सत्कार किया, भोजन कराया और रात्रि-विश्राम के लिए बिछौना बिछा दिया। रात्रि को कथा-वार्ता के दौरान एक संन्यासी ने प्रश्न कियाः
"आपने कितने तीर्थों में स्नान किया है? कितनी तीर्थयात्रा की है? हमने तो चारों धाम की तीन-तीन बार यात्रा की है।"
चाचा ने कहाः "मैंने एक भी तीर्थ का दर्शन या स्नान नहीं किया है। यहीं रहकर भगवान का भजन करता हूँ और आप जैसे भगवद् स्वरूप अतिथि पधारते हैं तो सेवा करने का मौका लेता हूँ। अभी तक कहीं भी गया नहीं हूँ।"
दोनों संन्यासी आपस में सोचने लगेः 'ऐसे व्यक्ति का अन्न खाया ! अब यहाँ से चले जायें तो रात्रि कहाँ बिताएँ? यकायक चले जायें तो उसको दुःख होगा। चलो, कैसे भी करके इस विचित्र वृद्ध के यहाँ रात्रि बिता दें। जिसने एक भी तीर्थ नहीं किया उसका अन्न खा लिया ! हाय! ' आदि आदि। इस प्रकार विचारते सोने लगे लेकिन नींद कैसे आवे? करवटें बदलते-बदलते मध्यरात्रि हुई। इतने में द्वार से बाहर देखा तो गौ के गोबर से लीपे हुए बरामदे में एक काली गाय आयी.... फिर दूसरी आयी..... तीसरी.... चौथी.... पाँचवीं..... ऐसा करते-करते असंख्य गायें आईं। हरेक गाय वहाँ आती, बरामदे में लोटपोट होती और सफेद हो जाती तब अदृश्य हो जाती। ऐसी कितनी ही काली गायें आयी और सफेद होकर विदा हो गईं। दोनों संन्यासी फटी आँखों से देखते ही रहे। दंग रह गये कि यह क्या कौतुक हो रहा है !
आखिरी गाय जाने की तैयारी में थी तो उन्होंने उसे वन्दन करके पूछाः
"हे गौ माता! आप कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ आकर आप श्वेतवर्ण हो जाती हो इसमें क्या रहस्य है? कृपा करके अपना परिचय दें।"
गाय बोलने लगीः "हम गायों के रूप में सब तीर्थ हैं। लोग हममें 'गंगे हर.. यमुने हर... नर्मदे हर....' आदि बोलकर गोता लगाते हैं, हममें अपना पाप धोकर पुण्यात्मा होकर जाते हैं और हम उनके पापों की कालिमा मिटाने के लिए द्वन्द्वमोह से विनिर्मुक्त आत्मज्ञानी, आत्मा-परमात्मा में विश्रान्ति पाये हुए ऐसे सत्पुरुष के आँगन में आकर पवित्र हो जाते हैं। हमारा काला बदन पुनः श्वेत हो जाता है। तुम लोग जिनको अशिक्षित गँवार बूढ़ा समझते हो वे बुजुर्ग तो जहाँ से तमाम विद्याएँ निकलती हैं उस आत्मदेव में विश्रान्ति पाये हुए आत्मवेत्ता संत हैं।"
पढ़ना अच्छा है लेकिन पढ़ाई का अहं अच्छा नहीं। संन्यासी होना अच्छा लेकिन संन्यास का अहं अच्छा नहीं। सेठ होना ठीक है लेकिन सेठ का अहं ठीक नहीं। अमलदार होना ठीक है लेकिन अमलदारी का अहं ठीक नहीं।
कुछ भी बनो लेकिन सदा याद रखो कि आखिर तब तक? यह स्मरण रहे तो द्वन्द्व और मोह पिघल जायगा। फिर आत्मरस प्रकट होने में सुगमता रहेगी। छोटे बालक को देखा? लेटा हुआ आकाश के साथ कुश्ती करता है। तोतले शब्द भी मधुर लगते हैं। क्योंकि उसके भीतर के द्वन्द्व, उसके अहंकार अभी ठोस नहीं बने। उसके चित्त में अभी 'मैं' और 'मेरा' का द्वन्द्व पनपा नहीं। वह बड़ा होगा, उसके चित्त में जब द्वन्द्व जगेंगे तब उसकी निर्दोषता दूर हो जायेगी, दोष आ जायेंगे, अहंकार पुष्ट होगा। ऋषि कहते हैं-
वीतरागभयक्रोधः
मुनि
मोक्षपरायणः।
'जिसका राग, भय और क्रोध व्यतीत हो गया है वह मुनि मोक्षपरायण है।'
बाल्यावस्था में राग, भय और क्रोध सुषुप्त रहते हैं। उम्र बढ़ती है तो राग-भय-क्रोध भी पुष्ट हो जाते हैं। ध्यान, भजन, साधना के द्वारा जब विवेक जगाया जाता है तब विकार व्यतीत हो जाते हैं। तब मनुष्य मुनि बन जाता है, मननशील बन जाता है। मन्त्रदृष्टा को ऋषि कहा जाता है और आत्मज्ञान का मनन करके स्वरूप में विश्रांति पाते हैं उनको मुनि कहा जाता है। नारदजी ऋषि भी थे और मुनि भी थे। वशिष्ठजी महाराज ऋषियों में भी गिने जाते हैं और मुनियों में भी गिने जाते हैं। शुकदेवजी महाराज मुनि कहे जाते हैं।
जब तक जीव अपने आत्मा-परमात्मा में जगता नहीं तब तक उसका दुर्भाग्य चालू ही रहता है। चालू दुर्भाग्य में जीव अपने को भाग्यवान मान लेता है कि 'आहा ! मुझे नौकरी मिल गई। बड़ा भाग्यवान हूँ।' अरे भैया ! तुझे अपने आत्मा का ज्ञान मिला है?"
"नहीं।"
तो पूरा भाग्यवान नहीं।
"मुझे अच्छा परिवार मिला। मैं भाग्यवान.....। मुझे अच्छा धन्धा मिला, अच्छे मित्र मिले, अच्छा माहौल मिला.... मैं बहुत भाग्यवान हूँ....।"
वास्तव में ये सब अत्यंत तुच्छ चीजें हैं। साथ रहने वाली नहीं है। अपितु गुमराह करने वाली संसार की विपादायें हैं। ऐसा तो हर जन्म में कुछ न कुछ मिलता है फिर भी जीव अभागे के अभागे ही रहते हैं।
वास्तव में भाग्यवान तो तब जब 'मैं कौन हूँ' इसका भान हो जाये। फिर उस पर नजर डाल दे वह चमकने लग जाय।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सच्ची
कृपा
एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण के मन में धन पाने की तीव्र कामना हुई। वह सकाम यज्ञों की विधि जानता था किन्तु धन ही नहीं तो यज्ञ कैसे हो? वह धन की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ समय एक देवता की पूजा करता, परन्तु उससे कुछ लाभ नहीं पड़ता तो दूसरे देवता की पूजा करने लगता और पहले को छोड़ देता। इस प्रकार उसे बहुत दिन बीत गये। अन्त में उसने सोचाः "जिस देवता की आराधना मनुष्य ने कभी न की हो, मैं अब उसी की उपासना करूँगा। वह देवता अवश्य मुझ पर शीघ्र प्रसन्न होगा।"
ब्राह्मण यह सोच ही रहा था कि उसे आकाश में कुण्डधार नामक मेघ के देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। ब्राह्मण ने समझ लिया कि, 'मनुष्य ने कभी इनकी पूजा न की होगी। ये बृहदाकार मेघदेवता देवलोक के समीप रहते हैं। वे मुझे अवश्य धन देंगे।' बस बड़ी श्रद्धा-भक्ति से ब्राह्मण ने उस कुण्डधार मेघ की पूजा प्रारम्भ कर दी।
ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर कुण्डधार देवताओं की स्तुति की, क्योंकि वह स्वयं तो जल के अतिरिक्त किसी को कुछ दे नहीं सकता था। देवताओं की प्रेरणा से यक्ष-श्रेष्ठ मणिभद्र उसके पास आकर बोलेः "कुण्डधार तुम क्या चाहते हो?"
कुण्डधारः "यक्षराज ! देवता यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उपासक इस ब्राह्मण को वे सुखी करें।"
मणिभद्रः "तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण यदि धन चाहता है तो इसकी इच्छा पूर्ण कर दो। यह जितना धन माँगेगा वह मैं इसे दे दूँगा।"
कुण्डधारः "यक्षराज ! मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्रार्थना नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि देवताओं की कृपा से यह धर्मपरायण हो जाये। इसकी बुद्धि धर्म में लगे।"
मणिभद्रः "अच्छी बात ! अब ब्राह्मण की बुद्धि धर्म में ही स्थित रहेगी।"
उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके चारों ओर कफन पड़ा हुआ है। यह देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगाः "मैंने इतने देवताओं की और अन्त में कुण्डधार मेघ की भी धन के लिए आराधना की, किन्तु इनमें कोई उदार नहीं दिखता। इस प्रकार धन की आशा में ही लगे हुए जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ? अब मुझे परलोक की चिन्ता करनी चाहिए।"
ब्राह्मण वहाँ से वन में चला गया। उसने अब तपस्या करना प्रारम्भ किया। दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करने के कारण उसे अदभुत सिद्धि प्राप्त हुई। वह स्वयं आश्चर्य करने लगाः 'कहाँ तो मैं धन के लिए देवताओं की पूजा करता था और उसका कोई परिणाम नहीं होता था और अब मैं स्वयं ऐसा हो गया कि किसी को धनी होने का आशीर्वाद दे दूँ तो वह निःसन्देह धनी हो जायेगा !'
ब्राह्मण का उत्साह बढ़ गया। तपस्या में उसकी श्रद्धा बढ़ गयी। वह तत्परतापूर्वक तपस्या में लगा रहा। एक दिन उसके पास वही कुण्डधार मेघ आया। उसने कहाः
"ब्राह्मण ! तपस्या के प्रभाव से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब आप धनी पुरुषों तथा राजाओं की गति को देख सकते हैं।"
ब्राह्मण ने देखा कि धन के कारण गर्व में आकर लोग नाना प्रकार के पाप करते हैं और घोर नर्क में गिरते हैं।
कुण्डधार बोलाः "भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके आप यदि धन पाते और अन्त में नर्क की यातना भोगते तो मुझसे आपको क्या लाभ होता? जीव का लाभ तो कामनाओं का त्याग करके धर्माचरण करने में ही है। उन्हें धर्म में लगाने वाला ही उनका सच्चा हितैषी है।"
ब्राह्मण ने मेघ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कामनाओं का त्याग करके वह मुक्त हो गया।
जो आपकी कामना बढ़ावे वह आपका मित्र व हितैषी नहीं। अन्त में नर्क में सड़ता गलता जीवन बिताना पड़े, तुच्छ योनियों में छटपटाना पड़े ऐसे कामनापूर्ति के मार्ग में आपको लगानेवाला मित्र आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। कुण्डधार की तरह ज्ञान, वैराग्य, तपस्या बढ़ाकर परम पद में स्थित करना चाहते हैं वे ही आपके सच्चे हितैषी हैं। अतः ऐसे हितैषी ऋषियों की, शास्त्रों की बात को आदर से अपने जीवन में उतारकर धन्य हो जाओ।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
घोर
क्लेश में भी
सत्पथ पर
अडिगता
महाभारत की कथा सुनी मैंनेः
जब भगवान विष्णु ने वामनरूप से बलि से पृथ्वी तथा स्वर्ग का राज्य छीनकर इन्द्र को दे दिया तब कुछ ही दिनों में राज्यलक्ष्मी के स्वाभाविक दुर्गुण गर्व से इन्द्र पुनः उन्मत्त हो उठे। एक दिन वे ब्रह्माजी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोलेः
"पितामह ! अब अपार दानी राजा बलि का कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं सर्वत्र खोजता हूँ, पर उनका पता नहीं मिलता। आप कृपाकर मुझे उनका पता बताइये।"
ब्रह्माजी ने कहाः "तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं। तथापि किसी के पूछने पर झूठा उत्तर नहीं देना चाहिए, अतएव मैं तुम्हें बलि का पता बतला देता हूँ। राजा बलि इस समय ऊँट, बैल, गधा या घोड़ा बनकर किसी शून्य, उजाड़ जगह में रहते हैं।"
इन्द्र ने इस पर पूछाः "यदि मैं किसी स्थान पर बलि को पाऊँ तो उन्हें अपने वज्र से मार डालूँ या नहीं?"
ब्रह्माजी ने कहाः "राजा बलि ! अरे... वे कदापि मारने योग्य नहीं हैं। तुम्हें उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।"
तदनन्तर इन्द्र बलि की खोज में निकल पड़े। अन्त में एक खाली घर में उन्होंने एक गधा देखा और कई लक्षणों से उन्होंने अनुमान किया कि ये राजा बलि हैं। इन्द्र ने कहाः
"दानवराज ! इस समय तुमने बड़ा विचित्र वेश बना रक्खा है। क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशा पर कोई दुःख नहीं होता? इस समय, तुम्हारे छत्र, चामर और वैजयन्ती माला कहाँ गई? कहाँ गया वह तुम्हारा अप्रतिहत दान का महाव्रत और कहाँ गया तुम्हारा सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि और जल का रूप?"
बलि ने कहाः "देवेन्द्र ! इस समय तुम छत्र, चामर, सिंहासनादि उपकरणों को नहीं देख सकोगे। पर फिर कभी मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम उन्हें देख सकोगे। तुम जो इस समय अपने ऐश्वर्य के मद में आकर मेरा उपहास कर रहे हो, यह केवल तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का ही परिचायक है। मालूम होता है, तुम अपने पूर्व के दिनों को सर्वथा ही भूल गये। पर सुरेश ! तुम्हें समझ लेना चाहिए, तुम्हारे वे दिन पुनः लौटेंगे।
देवराज ! इस विश्व में कोई वस्तु सुनिश्चित और सुस्थिर नहीं है। काल सबको नष्ट कर डालता है। इस काल के अदभुत रहस्य को जानकर मैं किसी के लिए भी शोक नहीं करता। यह काल धनी-निर्धन, बली-निर्बल, पण्डित-मूर्ख, रूपवान-कुरूप, भाग्यवान-भाग्यहीन, बालक-युवा-वृद्ध, योगी तपस्वी धर्मात्मा, शूर और बड़े से बड़े अहंकारियों में से किसी को भी नहीं छोड़ता। सभी को एक समान ग्रस्त कर लेता है। सबका कलेवा कर जाता है।
ऐसी दशा में महेन्द्र ! मैं क्यों सोचूँ? काल के ही कारण मनुष्य को लाभ-हानि और सुख-दुःख की प्राप्ति होती है। काल ही सबको देता है और पुनः छीन भी लेता है। काल के ही प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए वासव ! तुम्हारा अहंकार, मद तथा पुरुषार्थ का गर्व केवल मोह मात्र है। ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा विनाश किसी मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य की कभी उन्नति होती है और कभी अवनति। यह संसार का नियम है। इसमें हर्ष-विषाद नहीं करना चाहिए। न तो सदा-सदा किसी की उन्नति ही होती है और न सदा अवनति या पतन ही। समय से ही ऊँचा पद मिलता है और समय ही गिरा देता है। इसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक दिन देवता, पितृ, गन्धर्व, मनुष्य, नाग, राक्षस सब मेरे अधीन थे। अधिक क्या, "नमस्तस्यै दिशेऽप्यस्तु यस्यां वैरोचनिर्बलिः।" – जिस दिशा में राजा बलि हो उस दिशा को भी नमस्कार ! यों कहकर, मैं जिस दिशा में रहता था उस दिशा को भी लोग नमस्कार करते थे। पर जब मुझ पर भी काल का आक्रमण हुआ, मेरा भी दिन पलटा खा गया और मैं इस दशा में पहुँच गया तब किस गरजते और तपते हुए पर काल का चक्र न फिरेगा?
मैं अकेला बारह सूर्यों का तेज रखता था। मैं ही पानी का आकर्षण करता और बरसाता था। मैं ही तीनों लोकों को प्रकाशित करता और तपाता था। सब लोकों का पालन, संहार, दान, ग्रहण, बन्धन और मोचन मैं ही करता था। मैं तीनों लोकों का स्वामी था, किन्तु काल के फेर से इस समय मेरा वह प्रभुत्व समाप्त हो गया। विद्वानों ने काल को दुरतिक्रम और परमेश्वर कहा है। बड़े वेग से दौड़ने पर भी कोई मनुष्य काल को लाँघ नहीं सकता। उसी काल के आधीन हम, तुम, सब कोई है।
इन्द्र ! तुम्हारी बुद्धि सचमुच बालकों जैसी है। शायद तुम्हें पता नहीं कि अब तक तुम्हारे जैसे हजारों इन्द्र हुए और नष्ट हो चुके। यह राज्य, लक्ष्मी, सौभाग्यश्री, जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हारी बपौती या खरीदी हुई दासी नहीं है। वह तो तुम जैसे हजारों इन्द्रों के पास रह चुकी है। वह इसके पूर्व मेरे पास थी। अब मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आयी है और शीघ्र ही तुमको भी छोड़कर दूसरे के पास चली जायेगी। मैं इस रहस्य को जानकर रत्तीभर भी दुःखी नहीं होता। बहुत-से-कुलीन धर्मात्मा गुणवान राजा अपने योग्य मन्त्रियों के साथ भी घोर क्लेश पाते हुए देखे जाते हैं। साथ ही इसके विपरीत मैं नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख मनुष्यों को बिना किसी की सहायता से राजा बनते देखता हूँ। अच्छे लक्षणोंवाली परम सुन्दरी तो अभागिनी और दुःखसागर में डूबती दीख पड़ती है और कुलक्षणा, कुरूपा भाग्यवती देखी जाती है। मैं पूछता हूँ, इन्द्र ! इसमें भवितव्यता-काल यदि कारण नहीं है तो और क्या है?
काल के द्वारा होने वाले अनर्थ बुद्धि या बल से हटाये नहीं जा सकते। विद्या, तपस्या, दान और बन्धु-बान्धव कोई भी कालगत मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता।
आज तुम मेरे सामने वज्र उठाये खड़े हो। अभी चाहूँ तो एक घूँसा मारकर वज्र समेत तुमको गिरा दूँ। चाहूँ तो इसी समय अनेक भयंकर रूप धारण कर लूँ, जिनको देखते ही तुम डरकर भाग खड़े हो जाओ। परन्तु करूँ क्या? यह समय सह लेने का है, पराक्रम दिखलाने का नहीं। इसलिए यथेच्छ गधे का ही रूप बना कर मैं अध्यात्म-निरत हो रहा हूँ। शोक करने से दुःख मिटता नहीं, वह तो और बढ़ता है। इसी से बेखटके हूँ, बहुत निश्चिन्त, इस दुरवस्था में भी।"
बलि के विशाल धैर्य को देखकर इन्द्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहाः
"निःसंदेह तुम बड़े धैर्यवान हो जो इस अवस्था में भी मुझ वज्रधारी को देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते। निश्चय ही तुम राग-द्वेष से शून्य और जितेन्द्रिय हो। तुम्हारी शांतचित्तता, सर्वभूतसुहृदता तथा निर्वैरता देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम महापुरुष हो। अब मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं रहा। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरी ओर से बेखटके रहो, निश्चिन्त और निरोग होकर समय की प्रतीक्षा करो।
यों कहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर चले गये और बलि पुनः अपने स्वरूप-चिन्तन में स्थिर हो गये।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
करुणासिन्धु
की करुणा
ईश्वर के मार्ग पर एक बार कदम रख ही दिये हैं तो चल ही पड़ना। पीछे न मुड़ना। जिज्ञासु के हृदय की पुकार होती है, पक्के मर्दों के दिल की आवाज होती है कि जो करना है सो करना है, पाना है सो पाना है। कण्ठगत प्राण आ जाय तो भी वापस नहीं मुड़ना है।
ईश्वर के मार्ग पर कदम रखनेवाले वे ही लोग पहुँचते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं। परमात्मा के मार्ग पर वे ही वीर चल पाते हैं जिनके अन्दर अथाह उत्साह, महान् सहनशक्ति, विचित्र विचारबल होता है। वे ही इस मार्ग के पथिक हो पाते हैं।
भोंय
सूवाडुं भूखे
मारुं उपरथी
मारुं मार।
एटलूँ
करतां जो हरि
भजे तो करी
नाखुं
निहाल।।
ऐसे निहाल कर देने वाले सदगुरु का सहारा जिन जिज्ञासु साधकों को मिल जाता है वे सचमुच धन्य हैं। सदगुरु की महिमा अपार है। योगीश्वर देवाधिदेव भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं-
अज्ञानमूलहरणं
जन्मकर्मनिवारकम्।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं
गुरुपादोदकं
पिबेत्।।
'अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारनेवाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए।'
(श्रीगुरुगीता)
देह में अहंता-ममता अज्ञान का मूल है। जगत में सत्यबुद्धि करना अज्ञान का मूल है। वृत्तियों की सत्यता मानना अज्ञान का मूल है। सुख और दुःख में सत्यबुद्धि करना अज्ञान का मूल है। जीवन और मौत में सत्यबुद्धि करना अज्ञान का मूल है। पद और प्रतिष्ठा में रस आना अज्ञान का मूल है। जगत की किसी भी परिस्थिति में सुख से बँध जाना यह अज्ञान की ही महिमा है।
जन्म-जन्मान्तर तक भटकाने वाले जो कर्म हैं, बाहर सुख दिखाने वाले जो कर्म हैं, बाहर सत्यता दिखानेवाली जो बुद्धि है उस बुद्धि को बदलकर ऋतंभरा प्रज्ञा पैदा कर दे, रागवाली बुद्धि को हटाकर आत्मरतिवाली बुद्धि पैदा कर दे, सरकते हुए संसार से चित्त हटाकर शाश्वत परमात्मा के तरफ ले चले ऐसे कोई सदगुरु मिल जाय तो वे अज्ञान को हरण कर के, जन्म-मरण के बन्धनों को काटकर तुम्हें स्वरूप में स्थापित कर देते हैं।
अज्ञान का मूल क्या है? अज्ञान का मूल वासना है। जैसे नाविक नाव को ले जाता है और नाव नाविक को ले जाती है ऐसे अज्ञान से वासना पैदा होती है और वासना से अज्ञान बढ़ता है। नश्वर में प्रीति बढ़ती रहती है यह अज्ञान का लक्षण है। ज्ञान की केवल बातों से काम न चलेगा, यंत्रवत माला घुमाने से काम न चलेगा, सेठों को राजी रखने से काम न चलेगा। तुम चाहे कितने ही मंत्र करते रहो लेकिन बेवकूफी कम हुई या बढ़ी उस पर निगाह रखनी पड़ेगी। अज्ञान घटता है या नहीं यह देखना पड़ेगा। यदि तुम अज्ञान में ही मंत्र करते जाओगे तो मंत्र का फल तुम्हारी वासनापूर्ति होगा और वासनापूर्ति हुई तो तुम भोग भोगोगे। भोग से भोग की इच्छा नयी हो जायगी।
तप करने से क्या फर्क पड़ता है? जप करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब कोई सदगुरु मिल जाय। फर्क तो तब पड़ता है जब सदगुरु की सीख दिल में उतर जाय... जन्म-मरण के चक्र में डालनेवाले जो कर्म हैं उन कर्मों का निवारण करनेवाला कोई सदगुरु मिल जाय... सत्य के झलकें देनेवाला, सत्य के गीत सुनानेवाला सदगुरु मिल जाय.... जिनके सान्निध्य से तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य निखर आये, जिनके उपदेश से तुम्हारी बुद्धि की मलिनता दूर होकर विवेक-वैराग्य जग जाय !
काश ! वे दिन कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे कि जब भर्तृहरि पूरा राज्य छोड़कर चले गये। गोरखनाथ के चरणों में जा पड़े। गोरखनाथ के चरणों में गिरते समय राजा भर्तृहरि को संकोच नहीं हुआ, लज्जा नहीं आयी, कोई पद और प्रतिष्ठा याद नहीं आये। वे समझते थेः अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं.... जन्म-जन्मांतर के जो कर्म हैं उनका निवारण करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो सदगुरु की करुणाकृपा में है। जन्म-जन्मांतर की बेवकूफी को दूर करने की यदि कुंजियाँ हैं तो संतों के द्वार पर हैं।
रहुगण राजा राज्य से उपराम होकर शांति पाने के लिए जा रहा है। होगी बुद्धि कुछ पवित्र। कई राजा तो मरते दम तक आसक्ति नहीं छोड़ते। रहुगण ऐसा हतभागी नहीं था। वह भीतर की शान्ति खोजने जा रहा है पालकी में बैठकर। पालकी उठानेवालों में से रास्ते में एक आदमी बीमार पड़ा तो जड़भरतजी उसकी जगह पर पालकी ढोने में लगा दिये गये। सबमें अपने आपको निहारनेवाले जड़भरतजी चींटी-चींटा आदि देखते तब उनको बचाने के लिए थोड़ा सा कूद पड़ते। राजा का सिर पालकी में टकराता। इससे राजा उनको डाँटता-फटकारता।
ब्रह्मनिष्ठ जड़भरतजी को उस अज्ञानी राजा पर करुणा हुई। बुद्ध पुरुष करुणा के भंडार होते हैं। सच्ची करुणा और सच्ची उदारता, सच्ची समझ और सच्चा ज्ञान तो जड़भरतजी जैसों के पास ही हुआ करता है। मूर्खों की नजर में वे जड़ जैसे थे लेकिन वास्तव में वे ही चैतन्य पुरुष होते हैं। संसारियों ने उनका नाम जड़ रख दिया था, लेकिन वे ऐसे ही जड़ थे कि हजारों जड़ लोगों की जड़ता का नाश करने की कुंजियाँ उनके पास थीं। क्या दुर्भाग्य रहा होगा लोगों का कि ऐसे भरतजी का सान्निध्य-लाभ न पा सके। उन व्यास मुनि को हृदयपूर्वक नमस्कार हो कि उन्होंने जड़भरतजी के जीवन पर थोड़ा-सा प्रकाश डाल दिया। वह प्रकाश आज भी काम आ रहा है।
अज्ञान के मूल को हरने वाले, जन्मों के कर्मों को हटानेवाले जड़भरत राजा रहुगण को कहते हैं-
"हे राजन् ! जब तक तू आत्मज्ञानियों के चरणों में अपने अहं को न्योछावर न करेगा, जब तक ज्ञानवानों की चरणरज में स्नान करके सौभाग्यशाली न बनेगा तब तक तेरे दुःख न मिटेंगे, तेरा शोक न मिटेगा।
दुःख
को हरते सुख
को भरते करते
ज्ञान की बात
जी।
जग
की सेवा लाला
नारायण करते
दिन रात जी।।
सच्ची सेवा तो संत पुरुष ही करते हैं। सच्चे माता-पिता तो वे संत महात्मा गुरु लोग ही होते हैं। हाड़-मांस के माता-पिता तो तुमको कई बार मिले हैं। तुमने लाखों-लाखों बाप बदले होंगे, लाखों-लाखों माँए बदली होंगी। लाखों-लाखों कण्ठी बाँधनेवाले गुरु बदले होंगे, लेकिन जब कोई सदगुरु मिलते हैं तो तुम्हें ही बदल देते हैं।
अज्ञान के मूल को हटानेवाले, जन्म-मरण के कारणों को और पातकों को भस्मीभूत करने वाले, ज्ञान और वैराग्य के अमृत को तुम्हारे दिल में भरने वाले सत्पुरुषों का सत्संग और सान्निध्य मिल जाय तो कितना अहोभाग्य ! ऐसे पुरुषों की डाँट भी मिल जाय तो कितनी सुहावनी होगी ! वे डण्डा लेकर पिटाई करने लग जाएँ तो कितने मधुर होंगे वे डण्डे ! वे तमाचा मार दें तो भी उसमें कितनी करुणा होगी !
मेरे गुरुदेव ने एक बार मुझे ऐसी जोरों की डाँट चढ़ायी कि सुननेवाले भयभीत हो गये। मैंने अपने आपको धन्यवाद दिया कि जिन हाथों से हजार-हजार मीठे फल मिले हैं उन्हीं हाथों से यह खट्टा-मीठा फल कितना सुंदर है ! कितनी उदारता के साथ वे डाँटते हैं ! उस दिन की बात याद आती है तो भाव से तन-मन रोमांचित हो जाते हैं। उस डाँट में कितनी करुणा छुपी थी ! कितना अपनत्व छुपा था !
किसी संन्यासी जी ने मुझे कहा था किः "ऐ युवक ! तू मेरे पास से रिद्धि-सिद्धि सीख ले। मैं तुझे अनुष्ठान बताता हूँ। इससे तुझे जो चाहिए वे चीजें मिलने लगेगी।" इस प्रकार के प्रलोभन देकर वह अपना कुछ कचरा मुझे दे रहा था। गुरुदेव को पता चला। मुझे बुलवाया। चरणों में बिठाया और पूछाः
"क्या बात सुन रहा था?"
मैंने जो कुछ सुना था वह श्रीचरणों में सुना दिया। सदगुरु के आगे यदि ईमानदारी से दिल खोलकर बात न करोगे तो हृदय मलिन होगा। भीतर ही भीतर बोझा बढ़ाना पड़ेगा, जाओगे कहाँ? मैंने पूरा दिल खोलकर सदगुरु के कदमों में रख दिया। संन्यासी के साथ जो बातचीत हुई थी वह ज्यों की त्यों दुहरा दी। फिर मैं क्षणभर मौन हो गया, जाँचा कि कोई शब्द रह तो नहीं गया। गुरु के साथ विश्वासघात करने का पाप तो नहीं लग रहा? गुरु से बात छुपाने का दुर्भाग्य तो नहीं मिल रहा? मैंने ठीक से जाँचा। जो कुछ स्मरण आया वह सब कह दिया। ईमानदारी से सारी की सारी बात कह देने के बाद भी ऐसी जोरों की डाँट पड़ी कि मेरा हार्टफेल न हुआ, बाकी उत्साह, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और सच्चाई सब फेल हो रहा था। सदगुरु ने ऐसी डाँट चढ़ाने के बाद स्नेहपूर्ण स्वर से कहाः
"बेटा ! देख।"
आहा !
डाँट भी इतनी
तेज और 'बेटा' कहने
में प्यार भी
इतना पूर्ण। क्योंकि
पूर्ण पुरुष
जो भी करते
हैं वह पूर्ण ही
होता है।
श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब फेल होने का पूरा मौका था लेकिन जिन्होंने माया की जंजीरों को फेल कर दिया है, जिन्होंने अज्ञान को फेल कर दिया है उनके चरणों में यदि अपना अहंकार फेल हो जाय तो घाटा भी क्या है? अपनी अक्ल और चतुराई उनके चरणों में फेल हो जाय तो घाटा क्या पड़ा? मेरी सारी बुद्धिमत्ता, सारी व्यापारी विद्या, सारी साधना की अकड़ फेल हो गई। सिर नीचे हो गया, आँखें झुक गईं। उन्होंने कहाः
"बेटा ! सुन। साधक-जिज्ञासु बाज पक्षी है। जैसे बाज पक्षी आकाश को उड़ान लेता है और शिकारी तीर चढ़ाकर ताकता रहता है उसे गिराने के लिए। ऐसे ही साधक ईश्वर के तरफ चलता है तो भेदवादी लोग, अज्ञानी लोग ताकते रहते हैं तुम्हें गिराने के लिए। परिस्थितियाँ ताकती रहती हैं फिर तुम्हें संसार में खींचने के लिए। कानों में ऐसी बातें भर देते हैं कि साधक का पतन हो जाये। अज्ञानियों की बातों को महत्व न दो।
बेटा ! मैं तुझे डाँटता हूँ लेकिन भीतर तेरे लिए प्रेम के सिवा और कुछ नहीं। मैंने तेरे को कंपित कर दिया लेकिन तेरे लिए करुणा के सिवा और कुछ नहीं।"
जन्मों की धारणा और मान्यताओं को तोड़नेवाले, अज्ञान के मूल स्वरूप इच्छाओं को हटाने वाले, बेवकूफी को छीनने वाले, ज्ञान और वैराग्य को हृदय में भरने वाले, विवेक और शांति की छाया में रखने वाले उन गुरुजनों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम !
इस जीव की हालत तो ऐसी है जैसे बाढ़ में बहता हुआ कोई कीड़ा एक भँवर से दूसरे भँवर में भटकता जा रहा है। दयालु पुरुष की नजर पड़े और उसको उठाकर वृक्ष की छाया में रख दे। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ताओं का काम होता है। सदियों से भटकते हुए जीव संसार की सरिता में बहे जा रहे हैं, उनको वे प्रेम का प्रसाद देकर, पुचकार का सहारा देकर, साधना का इशारा देकर उन्हें संसार-सरिता के किनारे लगा देते हैं। जन्म-मरण के भँवर से बाहर निकालने के लिए सहारा दे देते हैं। ये कृपासिन्धु गुरु लोग इस पृथ्वी पर न होते तो लोग संसार में बिना आग जलते। यदि वे महापुरुष इस वसुन्धरा पर न होते तो लोग बिना पानी के डूबे रहते चिन्ता में। यदि वे दयालु ज्ञानीजन न होते तो मानव मानव का भक्षण किये बिना न रहता। यदि ज्ञानवानों की अनुकम्पा बार-बार इस पृथ्वी पर न बरसती तो मनुष्य पशु से ज्यादा भयंकर कृत्य करता।
ये सब उन्हीं सत्पुरुषों की देन है कि आज हजारों-हजारों दिल प्रभु के प्रेम में पिघल सकते हैं। हजारों दिल पाप-ताप का निवारण करके परमात्मा के प्यार में बह सकते हैं। प्यारे के दीदार में वे बिक सकते हैं। उनक मुलाकात में वे बिखर सकते हैं। चाहे वे ज्ञानवान समाज में प्रसिद्ध हुए हों चाहे अप्रसिद्ध रहे हों, लोगों के बीच रहे हों चाहे न रहे हों, लेकिन उन सदगुरुओं की बड़ी भारी कृपा है जो सत् में विचरण करते-कराते हैं, और सदा-सदा कराते ही रहेंगे। उन सत्पुरुषों की तो कृपा है हम लोगों पर। वे ही लोग हम पर अनुकम्पा करते हैं। बाकी के लोग तो भगवान के नाम पर दुकानदारी चलाते हैं, मत-पंथ-वाड़े बनाते हैं। सत्पुरुष ही ऐसे होते हैं, सच्चे संत महात्मा ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में भगवान के नाम का रस पिला सकते हैं। वे वास्तविक में अज्ञान को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। बाकी तो पंथ-वाड़े कब्रिस्तान हो जाते हैं। जीवन जीवन नहीं रहता। जीवन मौत के तरफ सरकता जाता है। ज्ञानवान पुरुषों की कृपा होती है तब जीवन जीवनदाता के रास्ते पर चलना शुरु करता है।
जिन्होंने ज्ञानवान पुरुषों की बात का सेवन किया है, जिन्होंने ज्ञानी के कदमों में अपने अहंकार को बिखेर दिया है, जिन्होंने ज्ञानी की बातों में अपने अहं को, मान्यताओं को कुर्बान कर दिया है उनको इहलोक और परलोक में दुःख नहीं रहता। वे सचमुच धनभागी हैं। धनवान धनी नहीं है, सत्तावान धनी नहीं हैं, इच्छावान धनी नहीं है, जो संत और परमात्मा का प्यारा होता है वही सच्चा धनी है।
निर्धनीया
सब जग धनवन्ता
नहीं कोई।
धनवन्ता
ता को जानिये
जाको रामनाम
धन होई।।
मौत के समय तुम्हारे रुपये-पैसे क्या रक्षा करेंगे? मौत के समय तुम्हारे बेटे और बहुएँ क्या रक्षा करेंगी भैया? मौत के समय तुम्हारे बड़े महल क्या साथ चलेंगे? मौत के समय भी सदगुरु की दी हुई प्रसादी तुम्हारा साथ करेगी, मौत के समय भी गुरु का ज्ञान तुम्हारे दिल में भरेगा तो तुम मौत की भी मौत करके मोक्ष के तरफ चल पड़ोगे। ये संस्कार व्यर्थ नहीं जाते। सत्संग के ये वचन मौके पर काम कर जाते हैं। दीया जलता है, औरों के लिए प्रकाश कर जाता है। नदियाँ बहती हैं, औरों के लिए पानी दे जाती हैं। मेघ बरसता है, औरों के लिए। इसी प्रकार महापुरुष दुनियाँ में बरस जाते हैं चार दिनों के लिए, उनकी याद रह जाती है, उनके गीत रह जाते हैं, उनका ज्ञान रहा जाता है। उनका शरीर तो चला जाता है लेकिन उनकी स्मृति नहीं जाती, उनके लिए आदर-प्रेम नहीं जाता। उनके लिए श्रद्धा के फूल बरसते ही रहते हैं।
वे आँखे धन्य हैं कि उनकी याद में बरस पड़े। वे होंठ धन्य हैं कि उनकी याद में कुछ गुनगुनाये। वह जिह्वा धन्य है कि उनकी याद में कुछ कह पाये। वह शरीर धन्य है कि उनकी याद में रोमांचित हो पाये। वे निगाहें धन्य हैं कि उनकी तस्वीरों के तरफ निहार पायें।
ऐसे पुरुषों को हम क्या दे सकते हैं जिनको सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य तुच्छ लगा है, जिनकी सारी इच्छाएँ और कामनाएँ नष्ट हो गई हैं? उन महापुरुषों को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास उनको देने के लिए है ही क्या? शरीर रोगी और मरने वाला, मन कपटी, चीजें बिखरने वाली। हम दे भी क्या सकते हैं? हमारे तो उनके कदमों में हजार-हजार प्रणाम हों ! लाखों-लाखों प्रणाम हों ! करोड़ों-करोड़ों प्रणाम हों ! जिन्होंने हमारे पीछे अपना सर्वस्व लुटा दिया, जिन्होंने हमारे पीछे अपनी समाधि का त्याग कर दिया, जिन्होंने हमारे पीछे अपने एकान्त को न्योछावर कर दिया, उन पुरुषों को हम दे भी क्या सकते हैं?
हम व्यावहारिक बुद्धि के आदमी ! हम स्वार्थी पुतले ! हम इन्द्रियों के गुलाम ! हम विषय-लम्पटता की जाल में घूमने वाले मकड़े ! हम उनको क्या दे सकते हैं?
हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं.... हम उनको आँखों के पुष्प दे सकते हैं.... दो आँसू दे सकते हैं- लो गुरुदेव ! ले लो.... ये आँसू ले लो... हमारी पुकार ले लो.... हमें चुप कराने की जिम्मेदारी भी तुम ही सम्भालो ! हे सदगुरु....
कुपुत्रो
जायेत
क्वचिदपि
कुमाता न
भवति।
पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कब कुमाता हुई? पिता कब कुपिता हुए? जब बेवफाई की तो बेटे ने की है, माँ ने कब ही है?
वे प्यारे शूली को सेज बनाकर गये, वे प्यारे जहर को अमृत बनाकर गये, वे प्यारे विरोध को गहने बनाकर गये, वे प्यारे जहर को अमृत बनाकर गये, वे प्यारे विरोध को गहने बनाकर गये, वे प्यारे अपमान को सिंगार बनाकर गये, केवल, जिज्ञासुओं की इन्तजार में कि कोई साधक मिल जाय, हमें लूटनेवाला कोई शिष्य मिल जाय। वे बेवकूफों के आगे भी अपने आपको लुटाते रहे, कहीं एक प्यारा मिल जाय, कहीं एक जिज्ञासु मिल जाय, हमें झेलनेवाला कहीं एक मुमुक्षु मिल जाय। इसी आशा आशा में हजारों पर बरसते रहे, लाखों-लाखों पर बरसते रहे। कितने धीर पुरुष रहे होंगे वे सत्पुरुष !
हमारे सदगुरु हों या और किसी के सदगुरु हों, वे तो सारे विश्व के सदगुरु हैं। लोग उन्हें नहीं जानते तो लोग अन्धे हैं। लोग उन्हें नहीं मानते तो लोग पागल हैं। वे महापुरुष तो सारे ब्रह्माण्ड के होते हैं। ऐसे सदगुरुओं के कदमों में अवतारों के भी सिर झुक जाते हैं, तुम्हारे हमारे झुक जायें तो क्या बड़ी बात है? ॐ.....ॐ....ॐ....
गुरु
दीवो गुरु
देवता....
गुरु एक दीया है। दीया जल जाता है औरों के लिए, गुरु भी जीवन को खपा लेते हैं औरों के लिए।
गुरु
दीवो गुरु
देवता गुरु
विण घोर
अन्धार।
जे
गुरु वाणी
वेगळा
रड़वड़िया
संसार।।
जो गुरु वाणी से दूर हैं वे खाक धनवान हैं? जो गुरु के वचनों से दूर हैं वे खाक सत्तावान हैं? जो गुरु की सेवा से विमुख हैं वे खाक देवता हैं? वे तो भोगों के गुलाम हैं। जो गुरु के वचनों से दूर हैं वे क्या खाक अमृत पीते हैं? उनको तो पद-पद पर राग-द्वेष का जहर पीना पड़ता है।
जे
गुरुवाणी
वेगळा
रड़वड़िया
संसार.....
अज्ञान के मूल को हरण करने वाले, जन्म कर्म को निवारने वाले, सदियों के पापों को भस्म करने वाले, अनन्त पकड़ों और मान्यताओं को तोड़कर परमात्मा से जोड़ने वाले सदगुरुओं के लिए वेदव्यास कहते हैं-
अज्ञानमूलहरणं
जन्मकर्मनिवारकम्।
ज्ञानवैराग्य
सिद्ध्यर्थं
गुरुपादोकं
पिबेत्।।
गुरु के चरणों का जल, चरणामृत पियें। उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालें। उनकी चाह में अपनी चाह मिला दें। उनकी निष्ठा में अपनी निष्ठा मिला दें। उनकी मस्ती में अपनी हस्ती मिटा दें, कल्याण हो जायगा।
तू क्या हस्ती रखता है भैया? जिनका बड़ा राजवैभव लहलहा रहा था वे महाराजा भर्तृहरि गोरखनाथ के चरणों में जा पड़ेः "हे नाथ !"
गुरु के कदमों में सम्राट आज अश्रुपात करके, सिर में खाक डालते हुए, रूखे-सूखे टुकड़े चबाकर भी रहना पसंद करता है, जबकि आज का कहलाने वाला बुद्धिमान, अहंकारी 'रॉक एण्ड रोल' में नाचना पसंद करता है, क्लबों में जाना पसंद करता है, सिनेमा में धक्के खाना पसंद करता है लेकिन गुरुओं का द्वार उसे भाता नहीं।
हे समझदारों के वेश में नासमझ नादानों ! दुनियाँ की चीजें तुम्हें क्या सुख देंगी? सिनेमा की पट्टियाँ तुम्हारा बल और बुद्धि, तुम्हारा तेज और ओज नष्ट कर देगी। यदि जीवन में बल और बुद्धि, तेज और ओज बढ़ाना है तो ऋषि कहते हैं-
गुरुदेव की कृपा का जल तुम पीते रहो। उसी से नहाते रहो। उसी की समझ में तुम डूबे रहो। उनके सत्संग में ही तुम खोये रहो। उन्हीं के गीतों में तुम गुलतान रहो।
जगत में तुस सदा से खोते आये हो, सदियों से तुम नश्वर चीजों के लिए मिटते आये हो। अब उस परमात्मा के लिए अपने अहं को मिटाकर देखो। यदि मिट भी गये और कुछ नहीं मिला, ठगे भी गये तो घाटा ही क्या है? वैसे भी तुम ठगाते आये हो। कोई पत्नी से ठगा गया, कोई पति से ठगा गया, कोई बहू से ठगा गया, कोई बेटे से ठगा गया, कोई सत्ता से ठगा गया, कोई चोरों से ठगा गया। आखिर में तो सब मौत से ठगे जानेवाले हैं।
मौत ठगे ले उसके पहले तू गुरु से ठगा जा घाटा भी क्या पड़ेगा? अब ठगवाने को तुम्हारे पास बचा भी क्या है? युगों से तुम ठगाते आये हो, युगों से तुम हारते आये हो। एक बार और हार सही। एक बार और दाँव सही।
चाहे
तैरा दो चाहे
डुबा दो,
मर
भी गये तो
देंगे
दुवाएँ।
'अज्ञानमूल
हरणं.....
ऋषि का सन्देश कितना सुन्दर रहा होगा ! कितनी उदार और करुणापूर्ण वाणी प्रकट हुई होगी ! श्लोक किसी पामर व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। ये किसी अहंकारी के वचन नहीं हैं। ये तो हैं किसी पूरे अनुभवी के वचन। पूरा सत्शिष्य ही सदगुरु का अमृत पी सकता है। यह शेरनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ही रह सकता है। छोटे-मोटे पात्र को तो वह चीरकर चला जाता है। ये गुरु के वचन अभागे को शोभा नहीं देते।
योगवाशिष्ठ महारामायण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं-
"हे रामजी ! जैसे खीर सुवर्ण के पात्र में शोभा पाती है और श्वान की खाल में पवित्र खीर भी अपवित्र हो जाती है ऐसे ही मतलबी और स्वार्थी शिष्यों के आगे ब्रह्मज्ञान शोभा नहीं पाता लेकिन अहंकार रहित सत्पात्र शिष्यों के हृदय में गुरु के वचन शोभा देते हैं, पवित्र शिष्यों के दिल में ये वचन उगते हैं। उगे हुए वचनों को जब सींचा जाता है तब उनमें मोक्षरूपी फल लगता है। उससे वह स्वयं भी तृप्त होता है और दूसरों को भी तृप्ति देता है।"
गुरु के उपदेश का जो सेवन करते हैं, गुरु के कृपाकटाक्ष को जो दिल की प्यालियों से पीते हैं उनको यहाँ भी दुःख स्पर्श नहीं करता और वहाँ भी स्पर्श नहीं करता। वे यहाँ भी सुख की घड़ियाँ जी लेते हैं। उन सौभाग्यशाली शिष्यों को दुःख से सुख बनाना आता है, सुख में सुविधा बनाना आता है और सुविधा से सत्य के दीदार पाना आता है। ऐसे सत्शिष्य बोलते है कि एक बार कदम रख ही लिया तो फिर क्या रुकना? ईश्वर के रास्ते चल दिया तो मुड़कर क्या आना?
तूफान
और आँधी हमको
न रोक पाये।
वे
और थे मुसाफिर
जो पथ से लौट
आये।।
जो सत्शिष्य हैं, जो सदगुरु के कदमों बिखर गया है, जिसने अपने दिल की प्याली सीधी रखी है और सदगुरु के अमृत को पी लिया है वह साधना के मार्ग से, भगवान के मार्ग से लौटकर नहीं आता। संसारी तूफानों से वह डरता नहीं। ऐसा कौन सा साधक सिद्ध बना है जिसने तूफान और आँधी का मुकाबला न किया हो? ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्हें कुचलने के लिए लोगों ने प्रयास न किये हों? ऐसे कौन-से संत पुरुष हैं जिन्होंने लोगों की बातों को कुचलकर, पैर तले दबाकर परमात्म-प्राप्ति की यात्रा न कर दिखायी हो?
वे ही पहुँचे हैं जो रुके नहीं। अनूकूलता में फँसे नहीं और प्रतिकूलता से डरे नहीं वे ही तो पहुँचे हैं। बगभगत तो रह गये, थोड़ी-सी उलझन में उलझ गये लेकिन सत्पात्र साधक तो मंजिल तय करके ही रहता है।
और कोई मुसाफिर होते हैं तो पथ से लौटते रहते हैं लेकिन सदगुरु के रास्ते चला और पथ से लौटा तो सत्शिष्य किस बात का? अगर लौट भी गया तो जो हजारों यज्ञ करने से भी मिलना कठिन है वह स्वर्ग और ब्रह्मलोक का सुख उसे अनायास मिलता है।
शुक्र अपने ब्रह्मवेत्ता पिता भृगु ऋषि की सेवा में रहकर साधना कर रहे थे। सेवा से निवृत्त होते तो योगाभ्यास में लग जाते, ध्यान करते। साधना करते-करते उनकी वृत्ति सूक्ष्म हुई तो सूक्ष्म जगत में गति होने लगी। अभी परमपद पाया न था। न अज्ञानी थे न ज्ञानी थे। बीच में झूले खा रहे थे। एक दिन आकाश मार्ग से जाती हुई विश्वाची नामक अप्सरा देखी तो मोहित हो गये। अन्तवाहक शरीर से उसके पीछे स्वर्ग में गये।
इन्द्र ने उन्हें देखा तो सिंहासन छोड़कर सामने आये। स्वागत किया और अपने आसन पर बिठाकर पूजा करने लगे।
"आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि महर्षि भृगु के पुत्र और सेवक तुम स्वर्ग में आये हो।"
हालाँकि वे गये तो थे विश्वाची अप्सरा के मोह में फिर भी उनकी की हुई साधना व्यर्थ नहीं गई। इन्द्र भी अर्घ्यपाद्य से उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मज्ञान की इतनी महिमा है कि ब्रह्मज्ञानी योगभ्रष्ट सेवक भी सुरपति से पूजा जा रहा है।
आप लोग तीन-चार दिन की ध्यान योग शिविरों में जो आध्यात्मिक धन कमा लेते हो इतना मूल्यवान खजाना आपने पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा। इससे हमारे पूर्वजों का भी कल्याण होता है। तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे या न करे, तुम्हें अभी वह पुण्य-संचय दिखे या न दिखे लेकिन बात सौ प्रतिशत सत्य है। साधक यदि सब चिन्ताओं से मुक्त होकर परमात्मा के ज्ञान में लग जाये तो वह स्वयं अनपढ़ होते हुए भी पढ़े हुए लोगों को ज्ञान दे सकता है, निर्धन होते हुए भी धनवानों को दान दे सकता है, अनजान होते हुए भी जानकारों को नयी जानकारी दे सकता है। उसके पास सारे ज्ञान का खजाना प्रकट होने लगते हैं। बिना पढ़े हुए शास्त्रों के रहस्य उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। बिना देखी हुई चीजें उनके द्वारा प्रकाशित होने लगती हैं। विभिन्न विद्या, शाखाएँ और विज्ञान की जानकारियाँ उसके आगे छोटी रह जाती हैं। जब गुरुभक्त के हृदय का द्वार खुल जाता है तो उसके आगे सारा जहाँ छोटा हो जाता है। स्वर्ग और फरिश्ते भी छोटे हो जाते हैं।
शादी के बाद छः महीने में ही एक महिला का पति चला बसा। महिला पागल-सी हो गई। भाग्यवशात् उसे सच्चे संत का सत्संग मिल गया। सत्संग में जाने लगी और संत गुरु-परमात्मा के आदेशानुसार घर में साधन-भजन करने लगी।
उसने गुरुकृपा पाकर ध्यानयोग में प्रगति की। सूक्ष्म जगत के परदे हटने लगे। रहस्यमय लोक में उसकी वृत्ति गति करने लगी। ध्यान में कई देवी-देवताओं के दर्शन होने लगे। एक बार इन्द्रदेव विमान लेकर प्रकट हुए और स्वर्ग में चलने के लिए आमंत्रण दिया। गुरुदेव ने महिला से कह रखा था कि किसी प्रलोभन में मत फँसना। उसने गुरुजी का स्मरण करते हुए इन्द्र को इन्कार कर दिया।
इन्द्र ने कहाः "गुरु की बात गुरु के पास रही। तुझे मौका मिला है तो स्वर्ग की सैर करके तो देख !"
दस-पन्द्रह मिनट वार्तालाप चला होगा। वह महिला गुरु की आज्ञा में दृढ़ रही।
ये सारे देव-देवियाँ हैं। उनको देखने के लिए तुम्हारे पास आँखें चाहिए। जैसे, वातावरण में रेडियो और टी.वी. के 'वेव्ज़' हैं फिर भी तुम्हें वे दिखते नहीं, सुनाई नहीं पड़ते क्योंकि तुम्हारे पास उसको प्रकट करने का साधन नहीं है। इसी प्रकार देवी और देवता, किन्नर और गन्धर्व ये सब हैं। उनके साथ तुम्हारा संवाद हो सकता है ऐसे तुम भी हो। लेकिन इसके लिए एक सूक्ष्म, भावप्रधान, एकाग्रवृत्ति चाहिए, कुछ ऊँची यात्रा चाहिए। वह यात्रा अगर हो जाय तो तुम यक्ष-गन्धर्व-किन्नर और देवी देवता के दर्शन कर सकते हो, उनसे वार्तालाप कर सकते हो, उनसे सहाय ले सकते हो, भविष्य की जानकारी पा सकते हो।
लेकिन सदगुरु का सत्शिष्य इन चीजों में उलझाता नहीं, इनकी इच्छा भी नहीं करता। उनका रास्ता तो और निराला होता है।
अमदावाद से दिल्ली जाने के लिए लोकल ट्रेन में बैठो तो छोटे-मोटे कई स्टेशनों के दर्शन होंगे। बिना स्टेशन के भी गाड़ी कहीं-कहीं रुक जायेगी क्योंकि लोकल जो है ! कई जंगल, नदी, नाले के दृश्य देखने को मिलेंगे। मेल से जायें तो छोटे-छोटे स्टेशन देख न पाओगे। गाड़ी धड़ाधड़ आगे बढ़ती जायगी। अगर तुम हवाई जहाज में बैठो तो बीच के रास्ते के स्टेशनों का अस्तित्व ही तुम्हारे लिए नहीं है।
चौथा रास्ता है नादानों का, जिन्होंने यात्रा की ही नहीं। वे लोग चिल्लायेंगे किः "पालनपुर नहीं है, आबूरोड नहीं है, अजमेर जयपुर नहीं है, दिल्ली भी नहीं है। अगर होते तो मुझे दिखते।"
अरे नादान ! न तू लोकल में लटका, न मेल में बैठा, न हवाई जहाज की यात्रा की। तू तो देह में और नश्वर भोगों में उलझा है। मोह माया में फँसा है। तेरे को बोलने का हक नहीं। व्यर्थ प्रलाप करके पाप बढ़ा लेता है।
इस पृथ्वी पर कई नास्तिक हुए, कई फकीर हुए, कई संत महापुरुष हुए। फकीरों ने तो संशय की फाकी कर दी लेकिन नास्तिकों ने साधना की ही फाकी कर दी। न ध्यान के गाँव में गये न कीर्तन के गाँव में गये, न सत्पुरुषों के चरणों में मिट पाये और अपना जजमैन्ट देते गये कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है.... कुछ नहीं है।
ऐसे लोगों को महापुरुष आवाहन देते हैं, अनुभवनिष्ठ संतपुरुष नास्तिकों को ललकारते हैं किः "तुम बोलते हो 'कुछ नहीं है।' कुछ नहीं है। यह कहने वाला कौन है यह तो बताओ ! 'नहीं' बोलता है तो किसकी सत्ता से, किसकी शक्ति से बोलता है रे? "कुछ नहीं है का प्रमाण तेरे पास क्या है?"
'मुझे दिखता नहीं इसलिए कहता हूँ कि कुछ नहीं है। मैं अपनी आँखों से देखूँ तब मानूँ।"
तात्त्विक अनुभव आँखों से देखे नहीं जाते, कानों से सुने नहीं जाते, नाक से सूँघे नहीं जाते, जिह्वा से चखे नहीं जाते, हाथ से छुए नहीं जाते। फिर भी हैं।
नास्तिक कहता हैः
जब
लग न देखूँ
मोरे नैन तब
लग न मानूँ
तोरे बैन।
फकीर कहते हैं- "ऐसे ही तेरे को वह तत्त्व बता दूँ? मेरे प्रभु को देखने के लिए तेरे पास नम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, समय नहीं है तो मेरे पास भी ईश्वरीय मस्ती छोड़कर तेरे जैसे भूत के पीछे लगने का समय नहीं है। बार-बार जन्मो और मरो, संसार के भँवरों मे भटको।"
ऐसा मानव-जन्म, ऐसी देह, ऐसी बुद्धि.... और इसे पत्थर परखने के लिए गँवा रहे हो?
वशिष्ठजी कहते हैं- 'हे रामचन्द्रजी ! संसारी लोगों को देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है कि नाहक वे अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय गँवा रहे हैं, नश्वर चीजों के पीछे, नश्वर भोगों के पीछे। जिसका नाश हो जायेगा उसके पीछे जीवन दे रहे हैं और जिसका कभी नाश नहीं होगा ऐसे शाश्वत आत्मदेव से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। कितने अभागे हैं ! हे रामजी ! ऐसे लोगों को धिक्कार है। लौकिक विद्याएँ तो वे जानते हैं लेकिन आत्मविद्या से वे वंचित हैं। गन्धर्व लोग गीतनृत्य तो जानते हैं लेकिन आत्म-मस्ती में नाचने से वंचित हैं। उन देवताओं को भी धिक्कार है कि वे स्वर्ग का अमृत पीकर अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। संतों का अमृत पीकर अपने पापों का नाश करते तो क्या घाटा था?'
पाँच ही तो इन्द्रियाँ है तुम्हारे पास। इससे पाँच विषय ही जान पाते होः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। इसके अलावा जानने का तुम्हारे पास कोई साधन नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे पास छठी इन्द्रिय होती तो जगत के छठे विषय का भी ज्ञान हो जाता। नाक खराब है तो तुम्हारे लिए सुगन्ध नहीं है। जन्म से आँख नहीं है तो रूप गायब हो गया। कान खराब है तो शब्द गायब है। जगत में कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी चार इन्द्रियाँ होती है, तीन इन्द्रियाँ होती हैं। उनके लिए जगत भी चार हिस्से का, तीन हिस्से का रह जाता है। तुम्हारे लिए जगत पाँच हिस्से का है। योगी जब छठी इन्द्रिय जाग्रत कर लेते हैं तो उनके लिए जगत छः हिस्से में। इससे भी आगे चलकर कोई अपनी वृत्ति ब्रह्माकार कर लेता है तो उसके लिए जगत अनन्त-अनन्त हिस्सों में होते हुए भी सब एक से निकलते हैं और एक ही एक को देखता, एक ही एक को सुनता है, एक ही एक को चखता है, आदि आदि। ऐसे कोई अनुभवनिष्ठ महापुरुष, संत, फकीर मिल जायें। नास्तिक भी यदि उनके पास पहुँच जाय तो उसको आस्तिक बनाने की कुंजियाँ वे रखते हैं। हाँ... यदि उनको रहमत आ जाय...!
उस नास्तिक को संत ने कहाः "ऐ मरने वाले ! भगवान के अस्तित्व पर तुम्हें विश्वास नहीं? तो हमें भी तेरी बात पर विश्वास नहीं।"
"महाराज ! मेरी बात तो सुनो।''
"तेरी बात सुनने का समय नहीं है। मैं तो उन शिष्यों की बात सुनता हूँ जो सिर झुकाकर नम्र बनकर कुछ समझना चाहते हैं। तूने सिर तो झुकाया नहीं, प्रणाम तो किये नहीं। ठूँठ होकर आ गया और बड़ी बातें बनाने लग गया।"
"महाराज ! यदि प्रणाम करने से कुछ हो सकता है तो लो, मैं दण्डवत् प्रणाम करता हूँ।"
उसने किया दण्डवत्। बाबाजी ने कसकर जोर से एक घूँसा मार दिया।
"बाप रे... मर गया... मर गया...."
"क्या हुआ... क्या हुआ?"
"बहुत दर्द होता है।"
"कहाँ है दर्द? देखूँ जरा।"
"बाबाजी ! आँखों से दिखता नहीं।"
"जरा चख लूँ।"
"बाबाजी ! तुम अजीब आदमी हो ! जीभ से दर्द चखा न जायेगा।"
"अच्छा ! मैं कान लगाकर सुन लूँ।"
"महाराज ! यह दर्द आँखों से दिखता नहीं, कान से सुना नहीं जाता, जीभ से चखा नहीं जाता, नाक से सूँघा नहीं जाता।"
"तो स्पर्श करके जान लूँ, कितना दर्द है।"
"बाबाजी ! घायल की गति घायल जाने। यह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है। यह तो महसूस होता है।"
"अरे भैया ! ऐसे ही बाबा की गति बाबा जाने, अहंकारी क्या पहचाने?"
संत की गति तो परमात्मा जानते हैं, थोड़ी-थोड़ी संत के साधक जानते होंगे। जिसके चश्मे अपने ढंग के होते हैं वे संतों की परीक्षा तो भले करें लेकिन संतों के अनुभव को नहीं समझ पाते। वे कहेंगेः 'उन संत को देखा, सुना। उनका लेक्चर अच्छा था' – आदि आदि।
संत कभी लेक्चर नहीं करते। लेक्चर तो लेक्चरर करते हैं। संत तो ईश्वर के साथ एक होकर बेत हैंष संत की वाणी सत्संग होती है।संत की वाणी सुनने से जितने पाप कटते हैं उतने तो चान्द्रायण व्रत से भी नहीं कटते। गंगास्नान से जितना फल होता है उससे कई गुना फल तो संत के दर्शन से होता है। ऐसे कोई संत मिल जाय !
जड़भरत राजा रहुगण को कह रहे हैं- "हे राजन् ! तुमको शांति तब मिलेगी जब ज्ञानवानों की चरणरज में स्नान करोगे।" गोरखनाथ कह रहे हैं राजा भर्तृहरि को, अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक को, वशिष्ठजी कह रहे हैं श्रीराम को। ऋषि कह रहे हैं हम लोगों को।
नहीं
मैं नहीं तू
नहीं अन्य रहा,
गुरु
शाश्वत आप
अनन्य रहा।
गुरु
सेवत ते नर
धन्य यहाँ,
तिनको
नहीं दुःख
यहाँ न वहाँ।।
जिन्होंने गुरुओं से ज्ञान की कुंजी पा ली वे समझते हैं कि संसार सारा स्वप्न है। वे संसार के दुःख को भी देखते रहते हैं और सुख को भी देखते रहते हैं, स्वर्ग और नर्क को भी देखते रहते हैं। वे दृष्टा, साक्षी होकर आत्मा में मस्त रहते हैं फिर 'मैं' और 'तू' की कल्पना वहाँ जोर नहीं मारती। अहंता और ममता वहाँ परेशानी पैदा नहीं करती। वे निर्मल पद में जीते हैं। बाजार से गुजरते हैं लेकिन खरीददार नहीं होते। सुख-दुःख के बाजार से निकल तो जाते हैं लेकिन वे कोई निराली मस्ती में होते हैं। ज्ञानी भी तुम्हें बाजार में मिल सकता है, युद्ध में मिल सकता है, राज्य में मिल सकता है, लेकिन वह बाजार में है नहीं, युद्ध में है नहीं, राज्य में है नहीं। ज्ञानी तुम्हें घर में मिल सकता है। लेकिन वह घर में है नहीं। तुम्हारी सभा के बीच मिल सकता है लेकिन वह केवल सभा में ही नहीं, अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डों में फैला हुआ चैतन्य है।
ज्ञानी की चेतना का बयान, ज्ञानी की गरिमा का बयान तो वेद भी नहीं कर सकते। 'नेति.... नेति.... नेति....।' पृथ्वी, जल, तेज इन तीन भूतों जितनी व्यापकता? नहीं। वायु और आकाश जितनी व्यापकता? नहीं, उससे भी परे। उससे भी परे जो चैतन्य होता है वही तो ज्ञानी का अपना आपा होता है।
'हे रामजी ! जब ज्ञानवान होता है तब सुख से जीता है, सुख से लेता है, सुख से देता है, सुख से खाता है, सुख से पीता है। सब चेष्टा करता हुआ दिख पड़ता है लेकिन हृदय से कुछ नहीं करता। जब वह शरीर का त्याग कर देता तो ब्रह्मा होकर सृष्टि करता है, विष्णु होकर पालन करता है, रूद्र होकर संहार करता है, सूर्य होकर तपता है और चाँद होकर औषधि पुष्ट करता है। ऐसा ज्ञानी का वपु होता है। सच पूछो तो अज्ञानी का भी वही वपु है लेकिन अज्ञानी अपने को देह मानकर सुख-दुःख के पीछे भटकता है। ज्ञानी अपने को स्वरूप में डूबा हुआ रखकर कर्म करते हुए भी सुख-दुःख से निराला रहता है। अखा भगत कहते हैं-
साथी
शीतलता अखा
सदगुरु केरे
संग।
सच्ची जो शीतलता है, सच्ची जो शान्ति है, सदगुरुओं के संग में है। अखा भगत मस्त आत्मज्ञानी संत हो गये। वे भी निकले थे सत्य को पाने के लिए, मार्ग में आँधी और तूफान बहुत आये फिर भी वे कहीं रुके नहीं। सुना है कि वे कई मठ-मंदिरों में गये, महंत-मंडलेश्वरों के पास गये। घूमते-घामते जगन्नाथपुरी में पहुँचे। जगन्नाथजी के दर्शन किये। वहाँ किसी मठ में गये तो महंत ने आँख उठाकर देखा तक नहीं। बड़े-बड़े सेठों से ही बात करते रहे।
दूसरे दिन अखा भगत किराये पर कोट, पगड़ी, मोजड़ी, छड़ी, आदि धारण करके शरीर को सजाकर महंत के पास गये और प्रणाम करके जेब से सुवर्ण-मुद्रा निकालकर रख दी। महंत ने चेले को आवाज लगायी। चेले ने आज्ञानुसार मेवा-मिठाई, फलादि लाकर रख दिये।
अखा नये कपड़े लाये थे किराये पर, उन कोट, पगड़ी, आदि को कहने लगेः 'खा...खा... खा...।' छड़ी को लड्डू में ठूँसकर बोल रहे हैं- 'ले... खा... खा...।' मठाधीश कहने लगाः "सेठजी ! यह क्या कर रहे हो?"
"महाराजजी ! मैं ठीक कर रहा हूँ। जिसको तुमने दिया उसको खिला रहा हूँ।"
"तुम पागल तो नहीं हुए हो?"
"पागल तो मैं हुआ हूँ लेकिन परमात्मा के लिए, रुपयों के लिए नहीं, मठ-मंदिरों के लिए नहीं। मैं पागल हुआ हूँ तो अपने प्यारे के लिए हुआ हूँ।"
साधना-काल में हम भी घूमते-घामते, भटकते-टकराते हुए कई बार घर लौटे आये। फिर गये। जब लीलाशाह बापू मिल गये तब बिक गये उनके चरणों में। ऐसे पुरुष होते हैं अज्ञान को हरण करने वाले। अन्य लोग तो अज्ञान को बढ़ानेवाले होते हैं। अखा भगत कह रहे हैं-
सच्ची
शीतलता अखा
सदगुरु केरे
संग।
और
गुरु संसार के
पोषत हैं
भवरंग।।
और लोग हैं वे संसार का रंग देते हैं, सांसारिक रंग में हमें गहरा डालते हैं। वैसे ही हम अन्धे हैं और वे हमें कूप में डालते हैं। 'इतना करो तो तुम्हें यह मिलेगा... वह मिलेगा। तुम्हारा यश होगा, कुल की प्रतिष्ठा होगी.... स्वर्ग मिलेगा।' पहले से ही हमारा मन चंचल बन्दर, फिर शराब पिला दी, ऊपर से काटे बिच्छू, फिर कहना ही क्या? अर्जुन गीता में कहते हैं-
चञ्चलं
हि मनः कृष्ण
प्रमाथि
बलवददृढम्।
तत्याहं
निग्रहं
मन्ये
वायोरिव
सुदुष्करम्।।
'हे श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ।'
(गीताः
6.34)
किसी की धन-दौलत, सुख-वैभव आदि सांसारिक प्रलोभन, नष्ट हो जाने वाले पदार्थ देखकर उनकी ओर लालायित नहीं होना चाहिए। अविनाशी आत्मा को पाने के लिए इच्छाएँ मिटानी चाहिए, न कि भोगों को पाने की इच्छाएँ करनी चाहिए। 'ऐसे दिन कब आयेंगे कि अकृत्रिम आनन्द को पाऊँगा?... नश्वर भोगों की लालसा मिटाकर शाश्वत आत्मा में स्थिर होऊँगा?.. देह होते हुए भी विदेही तत्त्व में प्रतिष्ठित हो जाऊँगा?' इस प्रकार की परमात्म-प्राप्ति की इच्छा जोर पकड़ेगी तो तुच्छ इच्छाएँ, नश्वर चीजों की इच्छाएँ, मिटनेवाले संयोगों की इच्छाएँ हटकर अमर आत्मा में स्थिति होने लगेगी। ॐ....ॐ....ॐ.....
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सच्ची
लगन जगाओ
वीरसिंह नामक एक बड़ा तेजस्वी राजा हो गया। वह प्रजापालक, न्यायनिष्ठ, दीन-दुःखियों की सहाय करने वाला और निरभिमानी था। उसको संसार के और सब सुख थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान-प्राप्ति के लिए इष्ट-उपासनादि कई उपाय किये मगर आशा पूरी नहीं हुई।
एक बार स्वप्न में उसने सुना कि महात्मा मधुसूदन सरस्वती नामक संत की सेवा करेगा तो पुत्र-प्राप्ति होगी। ठीक ही कहा हैः
जे
को जनम मरण ते
डरे।
साध
जनां की शरणी
पड़े।।
जे
को अपना दुःख
मिटावे।
साध
जनां की सेवा
पावे।।
जिसको जन्म-मृत्यु के भय से पल्ला छुड़ाना हो उसे संतों के शरण में जाना चाहिए। जो सचमुच अपने दुःखों को मिटाना चाहे उसे संतों की सेवा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
राजा वीरसिंह अपने राज्य-कारबार की व्यवस्था करके राजमहल और राजधानी छोड़कर कुछ सेवकों-अनुचरों के साथ सरिता के तीर पर तम्बू लगाकर रहने लगा। स्वप्न के आदेशानुसार महात्मा मधुसूदनदासजी की खोज करने के लिए चारों ओर लोग दौड़ाये। कई दिनों के परिश्रम के बाद एक मंत्री खुशखबरी लाया किः
"महाराज ! बधाई हो। हमारा कार्य सफल हो गया। जिन महापुरुष को खोजने के लिए आपने अरण्यवास किया और खोज करवाई उन महात्मा श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का पता लग गया है।"
राजा के आनन्द का ठिकाना न रहा। मंत्री, सैनिकों आदि के साथ संत श्री के दर्शनार्थ निकल पड़े। उन दिनों में मधुसूदनजी महाराज एक झोपड़ी बनाकर मौन धारण करके, बन्द आँख से, आसनस्थ होकर तपस्या कर रहे थे। अपने श्वासों को निहारते हुए आत्म-चैतन्य का अनुसंधान कर रहे थे। अपने ब्रह्मस्वरूप में विश्रान्ति पाने के लिए कृतनिश्चय थे। चौदह साल तक अर्धोन्मिलित नयन और मौन।
राजा झोंपड़ी पर पहुँचा। साष्टाँग दंडवत् प्रणाम करके बोलाः
"स्वामीजी ! मेरे अहोभाग्य कि आपके पावन दर्शन हुए। अब मुझे सेवा करने का मौका दीजिए।" राजा ने अपने स्वप्न की पूरी बात बता दी।
मधुसूदन जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आँख उठाकर देखा तक नहीं। क्योंकि साधना चालू थी। कैसे निष्पाप होंगे वे !
ते
द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
भजन्ते मां
दृढ़व्रताः।
भजन में कितनी दृढ़ता है !
राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि, "बाबाजी की कुटिया के इर्दगिर्द एक बहुत बड़ा भव्य, दिव्य आलीशान मंदिर खड़ा कर दो। बाबाजी को अपने आसन पर तपश्चर्या में कोई दिक्कत न होने पावे।"
आदेश देकर राजा चला गया। कुछ ही समय में वहाँ संगमरमर का भव्य मंदिर खड़ा हो गया। भगवान के विग्रह की प्राणप्रतिष्ठा की गईष सेवा-पूजा, आरती-उपासना के लिए पुजारी रखा गया। अन्य तमाम प्रकार की आवश्यक सामग्रियाँ लायी गयीं। तीन वर्ष और बीत गये। सत्रह वर्ष के बाद मधुसूदन जी ने आँख खोली तो सामने भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए। आसपास देखा तो भव्य मंदिर ! पास में पुजारी हाथ जोड़कर खड़ा है ! पुरानी झोंपड़ी का कोई पता नहीं। पुजारी से पूछाः
"भाई ! यह सब क्या है? मेरी झोंपड़ी कहाँ गई?"
"महाराज ! आज से तीन वर्ष पूर्व राजा साहब आये थे। आपके दर्शन किये और उनके आदेश के अनुसार यह मंदिर बनवाया है।"
"तीन साल पहले....?" स्वामी जी को आश्चर्य हुआ।
"हाँ महाराज!"
थोड़ी देर मधुसूदनजी शांत हो गये। आँख बन्द करके मौन में डूब गये। फिर खड़े होकर चुपचाप वहाँ से चल दिये कभी वापस न लौटे।
आयी
मौज फकीर की
दिया झोपड़ा
फूँक।
ऐसे महापुरुष अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, अपने एक-एक श्वास की कीमत जानते हैं। भव्य मंदिर मिल जाये तो क्या और भव्य महल मिल जाये तो क्या? भव्य गाड़ी मिल जाय तो क्या और सुंदर लाड़ी मिल जाय तो क्या? आखिर क्या? क्षण-भंगुर भोग और रोगों का घर तन। उनके संयोग से मिलकर क्या मिलेगा? घाटा ही घाटा है, अपने साथ धोखा है।
विश्वामित्र को मेनका मिली तो क्या हुआ?
लेकिन जिनके पुण्यकर्म जोर नहीं मारते ऐसे हम लोगों के मन छोटी-छोटी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि पहले इतना कर लें फिर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे। ऐसा करते-करते जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन काम पूरे नहीं होते।
अतः अपना मूल्यवान समय तुच्छ वस्तु अथवा मित्राचारी के नैतिक भावों से प्रभावित होकर नष्ट न होने पाय। परमात्मा को पाये बिना जीवन कहीं नष्ट न हो जाय इसमें सावधान रहना।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
आत्म-प्रशंसा
से पुण्यनाश
महाराज ययाति ने दीर्घकाल तक राज्य किया था। अन्त में सांसारिक भोगों से विरक्त होकर अपने छोटे पुत्र को उन्होंने राज्य दे दिया और वे स्वयं वन में चले गये। वन में कन्दमूल खाकर, क्रोध को जीत कर, वानप्रस्थाश्रम की विधि का पालन करते हुए पितरों एवं देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए तपस्या करने लगे। वे नित्य विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे। जो अतिथि अभ्यागत आते उनका आदरपूर्वक कन्दमूल फल से सत्कार करते और स्वयं कटे हुए खेत में गिरे हुए अन्न के दाने चुनकर तथा स्वतः वृक्ष से गिरे फल लाकर जीवन-निर्वाह करते थे। इस प्रकार पूरे एक सहस्र वर्ष तप करने के बाद महाराज ययाति ने केवल जल पीकर तीस वर्ष व्यतीत कर दिये। फिर एक वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे। उसके पश्चात एक वर्ष तक वे पञ्चाग्नि तापते रहे। अन्त के छः महीने तो वायु के आहार पर रहकर एक पैर से खड़े होकर वे तपस्या करते रहे।
इस कठोर तपस्या के फल से राजा ययाति स्वर्ग पहुँचे। वहाँ देवताओं ने उनका बड़ा आदर किया। वे कभी देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते और कभी ब्रह्मलोक चले जाते थे। उनका यह महत्त्व देवताओं की ईर्ष्या का कारण हो गया। ययाति जब कभी देवराज के भवन में पहुँचते, तब इन्द्र क साथ उनके सिंहासन पर बैठते थे। देवराज इन्द्र उन परम पुण्यात्मा को अपने से नीचा आसन नहीं दे सकते थे। परन्तु इन्द्र को बुरा लगता था। इसमें वे अपना अपमान अनुभव करते थे। देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययाति को स्वर्ग-भ्रष्ट कर दिया जाय। इन्द्र को भी देवताओं का भाव भी ज्ञात हो गया।
एक दिन ययाति इन्द्र-भवन में देवराज इन्द्र के साथ एक सिंहासन पर बैठे थे। नाना प्रकार की बड़ाई करते हुए इन्द्र ने कहाः
आप तो महान पुण्यात्मा हैं। आपकी समानता भला, कौन कर सकता है? मेरी यह जानने की बहुत इच्छा है कि आपने कौन-सा ऐसा तप किया है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ इच्छानुसार रह लेते हैं?"
ययाति बड़ाई सुनकर फूल गये और वे इन्द्र की मीठी वाणी के जाल में आ गये। वे अपनी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अन्त में उन्होंने कहाः "इन्द्र ! देवता, मनुष्य, गन्धर्व और ऋषि आदि में कोई भी तपस्या में मुझे अपने समान दिखाई नहीं पड़ता।"
बात समाप्त होते ही देवराज का भाव बदल गया। कठोर स्वर में वे बोलेः "ययाति ! मेरे आसन से उठ जाओ। तुमने अपने मुख से अपनी प्रशंसा की है, इससे तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गये, जिनकी तुमने चर्चा की है। देवता, मनुष्य, गन्धर्व, ऋषि आदि में किसने कितना तप किया है, यह बिना जाने ही तुमने उनक तिरस्कार किया है, इससे अब तुम स्वर्ग से गिरोगे।"
आत्म-प्रशंसा ने ययाति के तीव्र तप के फल को नष्ट कर दिया। वे स्वर्ग से गिर गये। उनकी प्रार्थना पर देवराज ने कृपा करके यह सुविधा उन्हें दे दी थी कि वे सत्पुरुषों की मण्डली में ही गिरें। अतः वे अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिबि नामक चार ऋषियों के बीच गिरे।
राजा ययाति ने उन महापुरुषों से प्रार्थना कीः "मुझे पुनः ऐसे नश्वर स्वर्गादि का सुख नहीं भोगना है कि जहाँ से अपने पुण्यों का वर्णन करने से ही गिरा दिया जाय। अब मुझे शाश्वत आत्मपद की प्राप्ति करनी है जहाँ पहुँचने के बाद गिरने की सम्भावना नहीं। अनन्त ब्रह्माण्डों में अपना स्वरूप व्याप रहा है उस अन्तर्यामी परमात्मा का मुझे साक्षात्कार हो जाय। हे कृपालु ! मुझे ऐसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें, जिसको पाकर फिर कभी पतन नहीं होता, ऐसे अपरिवर्तनशील आत्मदेव का, सत्य श्रीहरि का बोध हो जाय।"
वे आत्मवेत्ता संत प्रसन्न हुए और ययाति को भी अच्यु के ज्ञान का लाभ कराया जो कि हर प्राणी का अपना आपा है और सदा साथ में है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
मस्तक-विक्रय
कोसल के राजा का नाम दिग-दिगन्त में फैल रहा था। वे दीनों के रक्षक और निराधार के आधार थे। जब काशीपति ने उनकी कीर्ति सुनी, तब वे जल-भुन गये। उन्होंने बड़ी सेना ली और कोसल पर चढ़ आये। युद्ध में कोसलनरेश हार गये और वन में भाग गये। नगर में किसी ने काशीराज का स्वागत नहीं किया।
कोसलनरेश की पराजय से वहाँ की प्रजा रात-दिन रोने लगी। काशीराज ने देखा कि प्रजा उनका सहयोग कर कहीं पुनः विद्रोह न कर बैठे, इसलिए शत्रु के निःशेष करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दीः
"जो कोसलपति को ढूँढ लायगा उसे 100 मोहरें दी जायेंगी।"
जिसने भी यह घोषणा सुनी, आँख-कान बन्द कर जीभ दबा ली।
इधर कोसलनरेश फटे चीथड़ों में जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन एक पथिक उनके सामने आया और पूछने लगाः
"वनवासी ! इस वन का कहाँ जाकर अन्त होता है और कोसलपुर का मार्ग कौन सा है?"
राजा ने पूछाः "तुम्हारे वहाँ जाने का कारण क्या है?"
"मैं व्यापारी हूँ। मेरी नौका डूब गई है। अब द्वार-द्वार कहाँ भीख माँगता फिरूँ? सुना था कि कोसल के राजा बड़े उदार हैं अतएव उन्हीं के दरवाजे जा रहा हूँ।" पथिक बोला।
थोड़ी देर तक कुछ सोचकर राजा ने कहाः "चलो, तुम्हें वहाँ तक पहुँचा ही आऊँ। तुम बहुत दूर से हैरान होकर आये हो।"
काशीराज की सभा में एक जटाधारी व्यक्ति आया। काशीनरेश ने पूछाः "कहिये, किसलिए पधारे?"
जटाधारी ने कहाः "मैं कोसलराज हूँ। तुमने मुझे पकड़कर लाने वाले को सौ सुवर्णमुद्राएँ देने की घोषणा करायी है। बस, मेरे इस साथी को वह धन दे दो। इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्थित किया है।"
सारी सभा सन्न रह गयी। प्रहरी की आँखों में भी आँसू आ गये। काशीपति सारी बातें जान-सुनकर स्तब्ध रह गये।
त्याग, धैर्य और परहित में परायण कोसलनरेश जगत को, भोगपदार्थों को तुच्छ समझते थे। बाह्य के राज्य की अपेक्षा भीतर के राज्य की उनको ज्यादा कद्र थी। बाह्य शरीर सजाने की अपेक्षा उन्होंने हृदय को त्याग से, प्रेम से, निर्भयता से सजा रखा था। उस सुहावने हृदय में परमात्मा अपने पूरे प्रभाव से आसीन थे।
ऐसे पवित्र हृदयवाले कोसलनरेश का काशीनरेश पर अदभुत प्रभाव पड़ा। कुटिलता और बाह्य बल की अपेक्षा आन्तरिक बल बहुत पवित्र, दिव्य होता है। उस दिव्य आध्यात्मिक प्रभाव से काशीनरेश का हृदय पिघल गया। भरे कण्ठ कहाः
"अब मैं बाह्य राज्य नहीं जीतूँगा। महाराज ! जो अहंकार का विस्तार कराने में हिंसा, युद्ध, छीना-झपटी कराके, दूसरों को नीचा दिखाकर अपने को चक्रवर्ती राजा बनाने की दुर्वासना थी उस दुर्वासना ने मेरे से अन्याय करवाया। अब मैं दुर्वासना को जीतने के लिए एकान्त अरण्य की शरण लूँगा। आप मुझे क्षमा करें। अहंकार और ईर्ष्यावश जो कुछ मेरे से अनुचित हो गया उसमें वह वासना ही तो कारण है महाराज ! यह वासना निवृत्त करना ही तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, यह तुम्हारे प्रभाव से अब समझ रहा हूँ। निर्वासनिक पुरुष को प्रारब्ध वेग से सब भोग आकर प्राप्त होते हैं फिर भी वह निर्लेप रहता है। ऐसा जीवन पाने की मैं चेष्टा करूँगा।"
कोसलनरेश का हृदय प्यार से, उदारता से, अहोभाव से छलक आया। दोनों की आँखों से प्रेमाश्रु की सरिताएँ बह चलीं। मानो, दोनों दिलों में एक ही अलख पुरुष की, एक ही परमेश्वर की परम रसमयी धारा उमड़ी। धन्य घड़ियाँ... धन्य क्षणें हो गईं।
काशीनरेश ने कोसलनरेश का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बिठा दिया और उनके मस्तक पर मुकुट पहना दिया। सारी सभा धन्य-धन्य बोल उठी।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
शरणागतियोग
दैवी
ह्येषा
गुणमयी मम
माया
दुरत्यया।
मामेव
ये
प्रपद्यन्ते
मायामेतां
तरन्ति ते।।
'यह अलौकिक, अति अदभुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात् संसार से तर जाते हैं।'
न
मां
दुष्कृतिनो
मूढाः
प्रपद्यन्ते
नराधमाः।
माययापहृ
तज्ञाना आसुरं
भावमाश्रिताः।।
'माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर-स्वभाव को धारण किये हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।'
(भगवद्
गीताः 7.14.15)
ये दोनों श्लोक साधक के जीवन में स्पष्टता, सहज स्वाभाविक, सुगम और शाश्वत मार्ग का निर्देश करते हैं।
तीन गुणवाली माया दैवी है। इस माया का तरना पड़ा दुस्तर है। इस माया कि सरिता में कोई अपने पुरुषार्थ का तुम्बा बाँधकर पार होना चाहे और साथ में पत्थर भी बाँध ले तो पार नहीं हो सकता। फेन सागर का नाप लेना चाहे तो वह संभव नहीं। वह तरंगो की झपटों में छिन्न-भिन्न हो जाता है। उसको अपना ही पता नहीं रहता। ऐसे ही अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डों में फैले हुए परब्रह्म परमात्मा के आगे मनुष्य का बाहुबल, मनुष्य की अक्ल, मनुष्य का पुरुषार्थ, मनुष्य का उपार्जन, मनुष्य को जो कुछ सर्जन आयोजन है वह शून्यवत है। जैसे फेन और बुदबुदे का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व न होते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व मानकर वे कुछ बनना चाहे, कुछ पाना चाहे, सागर को नापना चाहे तो असम्भव है। लेकिन वे फेन और बुदबुदे अगर मिट जाये, अपने आधार, अपने अधिष्ठान उस सागर को जाने ले, समर्पित हो जाय तो उनके लिए सागर को पाना सरल भी है। सागर के सहारे वे ही नाच रहे हैं। सागर से ही वे उत्पन्न हुए, सागर में ही जी रहे हैं और सागर में ही मिल जायेंगे। लेकिन उस सागर से अपनी अलग सत्ता मानकर कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता, कुछ जानना चाहता और अपनी अक्ल-होशियारी पर अपनी बुद्धि पर, अपने बाहूबल पर वह बुलबुला अगर सागर को पाना चाहे, मापना चाहे तो असम्भव है। हाँ, बुलबुला माप नहीं सकता, सागर को पा नहीं सकता लेकिन सागर में मिट सकता है, मिटकर सागर हो सकता है। सच पूछो तो उसे मिटने की भी आवश्यकता नहीं, वह अभी भी मिटा हुआ है। क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं, सागर की सत्ता ही उसकी सत्ता है, सागर का होना ही उसका होना है। पानी का होना ही बुदबुदे का होना है। ऐसा जो समझ लेता है कि मेरे अन्तःकरण रूपी बुदबुदे का होना है। ऐसा जो समझ लेता है कि मेरे अन्तःकरणरूपी बुदबुदे में तमाम विचार उठते हैं, जिस समय जैसे-जैसे गुण आते हैं वैसे-वैसे संकल्प-विकल्प होते हैं लेकिन अन्तःकरण को सत्ता-स्फूर्ति देने वाला मेरा परमात्मा है। मैं उसी की शरण हूँ। मेरा वही आधार है। इस प्रकार जो अन्तर्यामी परमात्मा की शरण स्वीकार कर लेता है, अनन्त की स्मृति कर लेता है उसके लिए संसार-सागर तरना इतना आसान है जितना गोपद लाँघ जाना आसान होता है। मगर जो अपनी मान्यता, अपने मन-बुद्धि-अन्तःकरण के बल से संसार-सागर तरना चाहे तो उसके लिए संसार-सागर अति विकट हो जाता है। चोर को अगर तीनों काल का ज्ञान हो सकता हो, हिरन यदि शिकारी की गरदन मरोड़ सकता हो, अपराधी व पापी आदमी यदि सत्य-संकल्प बन सकता हो, मछली अगर बँसी को निगल सकती हो तो ऐसा आदमी संसार-सागर तर सकता है। अर्थात् ऐसे आदमी के लिए संसार-सागर तरना दुस्तर है।
कई लोग आसुरी भाव के आश्रित होकर भगवान का स्मरण नहीं करते। कई लोग स्मरण करते हैं लेकिन उनमें वासनाएँ भरी हैं। कई लोग स्मरण-ध्यान-भजन करते हैं तो अपने को कर्त्ता मानकर कुछ विशेष बनने की आकांक्षा में लगे हैं। ये सब करने वाले भी परमात्मा को नहीं पा सकते और न करनेवाले भी नहीं पा सकते। क्योंकि माया का ऐसा जाल है कि करने वाले किसकी सत्ता से किया जा रहा है उसको नहीं समझ रहा है। जो सारभूत है, जो सबको सत्ता-स्फूर्ति देकर नाच नचा रहा है उसको नहीं जानता और अपनी वजूदी, अपनी हस्ती बीच में अड़ा देता है।
वास्तव में देखा जाये तो पुण्य करने वाले हम कौन होते हैं? परमात्मा पुण्य करवा रहा है। दान करने वाले हम कौन होते हैं? वह करवा रहा है। हम सेवा, जप करने वाले कौन होते हैं? हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं।
एक लड़के ने माँ को कहाः "माँ ! तेरा ऋण चुकाने के लिए तन-मन-धन से सेवा करूँ। मेरे हृदय में तो आता है कि माँ, मेरी चमड़ी से तेरे चरणों की मोजड़ी बनवा दूँ।"
सुनकर माँ हँस पड़ीः "बेटा ! ठीक है। तेरी भावना है, मेरी सेवा हो गई। बस मैं संतुष्ट हूँ।"
"माँ तू हँसी क्यों?"
"बेटा ! तू कहता है कि मेरी चमड़ी से तेरी मोजड़ी बनवा दूँ। लेकिन यह चमड़ा तू कहाँ से लाया? यह चमड़ा भी तो माँ का दिया हुआ है।"
ऐसे ही यदि हम कहें किः 'हे प्रभु ! तेरे लिए मैं प्राणों का त्याग कर सकता हूँ, तेरे लिए घर-बार छोड़ सकता हूँ, तेरे लिए पत्नी-परिवार छोड़ सकता हूँ, तेरे लिए संसार छोड़ सकता हूँ....।' लेकिन घर-बार, संसार-परिवार लाये कहाँ से? उसी प्रभु का ही तो था। तुमने छोड़ा क्या? तुमने केवल उसको आदर देते हुए अपना अन्तःकरण पवित्र किया, वरना तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं। जैसे बेटे का अपना चमड़ा है ही नहीं, माँ का दिया हुआ है वैसे ही जीव का अपना कुछ है ही नहीं। सब कुछ ईश्वर का ही है। लेकिन जीव मान लेता है कि, 'यह मेरा है... भगवान ! तुझे देता हूँ। मैंने इतना किया, उतना किया... अब तू कृपा कर।'
कुछ न करने वालों की अपेक्षा ऐसे भक्त भी ठीक हैं लेकिन श्रीकृष्ण कहते हैं कि वे भी माया में ही हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह गुणों वाली माया बड़ी दुस्तर है। इसको तरना कठिन है।
'माया दुस्तर है, कठिन है...' ऐसा कहने से कोई साधक उत्साहहीन न हो जाये इसलिए भगवान ने आगे तुरन्त रास्ता भी बता दिया किः मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण आता है वह माया को तर जाता है।' भगवान के शरणागत भक्त के लिए माया तर जाना आसान भी है।
भगवान के शरण होने का मतलब क्या है? क्या हम 'कृष्ण.... कृष्ण करें? क्लीं कृष्णाय नमः... क्लीं कृष्णाय नमः....' करें? नहीं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। वे कहते हैं कि 'मेरे शरण।' कई लोग 'कृष्ण... कृष्ण....' जप करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वे श्रीकृष्ण के शरण हैं ही। कई लोग शिवजी का जप करते हैं किन्तु जरूरी नहीं कि वे शिवजी के शरण हैं ही।
भगवान का जप करते हैं लेकिन फल क्या पाना चाहते हैं? संसार। तो वे संसार के शरण हैं। माला घुमा रहे हैं नौकरी के लिए, जप कर रहे हैं शादी के लिए, ध्यान-भजन-स्मरण कर रहे हैं नश्वर चीजों के लिए, नश्वर कीर्ति के लिए। तो हम भगवान के शरण नहीं हैं, नश्वर के शरण हैं। अगर हमारा जप-ध्यान-अनुष्ठान पद-प्रतिष्ठा पाने के लिए है, व्यक्तित्व के शृंगार के लिए है तो हम भगवान के शरण नहीं हैं, शरीर के शरण हैं। 'हमें कोई महंत कह दे, हम ऐसा जियें कि हमारे महंतपद का प्रभाव पड़े, हम संत होकर जियें, साँई होकर जियें, लोगों पर प्रभाव छोड़ जायें, हम सेठ होकर जियें, साहूकार होकर जियें' – इस प्रकार की वासना भीतर है और हम भगवान की सेवा-पूजा-उपासना-आराधना करते हैं तो हम भगवान के शरण नहीं हैं। भगवान को अपनी इच्छापूर्ति का साधन बना दिया। हम शरण हैं माया के।
हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो जाँचो कि किसलिए कर रहे हैं? तन्दरुस्ती के लिए कर रहे हैं? यश के लिए कर रहे हैं? स्वर्ग-प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? अथवा ईश्वर-प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? अगर हमारे कर्मों में ईश्वर-प्राप्ति मुख्य है तो हम परमात्मा के शरण हैं। लक्ष्य अगर ईश्वर-प्राप्ति नहीं है तो हम मंदिर में होते हुए भी रुपयों के शरण हैं, पत्नी के शरण हैं, बच्चों के शरण है, सत्ता के शरण है, सुख के शरण हैं।
भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण आ जाता है वह माया को तर जाता है। भगवान के शरण जाने वाला व्यक्ति इतना महान् हो जाता है, ऐसा शाश्वत आनन्द प्राप्त कर लेता है कि फिर उसको नश्वर पदार्थों की आसक्तियों के शरण होने का दुर्भाग्य नहीं मिलता है।
ईश्वर के शरण होने से ईश्वर हमें पराधीन नहीं बना रहे हैं। ईश्वर हमें ईश्वर बना रहे हैं। ईश्वर हमें अपनी महिमा में जगा रहे हैं।
ईश्वर का स्मरण बड़ा हितावह है। स्मृति एक ऐसी चीज है, स्मरण एक ऐसा अदभुत खजाना है कि वह परम कल्याण के द्वार खोल देता है। नदी बह रही है सागर की ओर। उसमें से नहर निकालो तो उसके द्वारा नदी का पानी जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। ऐसे ही अन्तःकरण से अनन्त-अनन्त वृत्तियाँ उठ रही हैं। इन वृत्तियोंरूपी सरिताओं में बहकर हम संसाररूपी सागर में गिर रहे हैं। ईश्वर का स्मरण करने का मतलब यह है कि हमने ईश्वर की ओर वृत्तिरूपी जल को ले जाने के लिए एक नहर खोल ली। एक आयोजन कर लिया कि नदी का पानी खारे सागर में न जाय बल्कि खेतों में जाय। ऐसे ही वृत्तियाँ जन्म-मरण के संसार-सागर में नष्ट न हो, जीवन बरबाद न हो और आत्मज्ञान के उद्यान में उसका ठीक उपयोग हो। ईश्वर-स्मरण का मतलब है कि हमारा मन इधर-उधर की कल्पनाओं में न जाय, संसार की वासनाओं में न जाय, अनेक प्रकार के ख्यालों में हमारा मन न बिखरे, भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में न उलझे। लेकिन हमारा मन जहाँ से प्रकट हुआ है उसी परमात्मा में पहुँचे।
जो ईश्वर का स्मरण नहीं करते हैं वे क्या बिना स्मरण बैठे हैं? काष्ठ मौन में या समाधि में टिक हैं? नहीं। उनको संसार का स्मरण आता है। जो हरि का स्मरण नहीं करते, परमात्मा का स्मरण नहीं करते वे संसार सागर में बुरी तरह डूबते-उतरते रहते हैं, बड़ी-बड़ी तरंगों की थप्पड़ें खाते रहते हैं।
परमात्मा का बढ़िया स्मरण वह है कि जिस चीज पर मन जाय, जिस कर्म में हम हो, जिस बात में लगे हों, जिस देश में हों, जिस रंग में हों, जिस रूप में हों, जिस जात में हों, जिस नात में हों, जिस व्यवहार में हो, उस समय उन सबका जो आधार है उस परमात्मा की स्मृति बनी रहे। नजर फूल पर गई तोः 'आहा ! कितना सुहावना सुगन्धित गुलाब का फूल है ! उसका प्रागट्य स्थान परमात्मा है। फूलों में सत्ता परमात्मा की है।' नजर पड़ी किसी मित्र पर, मित्र की नजर मुझ पर पड़ी तोः 'दोनों मित्रों की आँखों में बैठकर एक ही मेरा प्रभु झाँक रहा है। वही सब मित्रों का मित्र है। वाह वाह प्रभु !'
नज़र पड़ी किसी मोटरगाड़ी परः 'हाय ! मुझे ऐसी गाड़ी मिल जाय !' ना, ना। स्मृति आ जाय किः 'वाह प्रभु ! क्या तेरी लीला है ! गाड़ी बनाने वालों में तेरी सत्ता, गाड़ी घुमाने वालों में तेरी सत्ता, गाड़ी देखने में इस अन्तःकरण को भी तेरी ही सत्ता चला रही है। वाह प्रभु !'
यह परमात्मा का स्मरण अदभुत होगा। कभी माला नहीं घुमायी और ऐसे ही स्मरण हो जाय किः 'तू सर्व हैं..... सबमें है.... मुझमें भी तू ही है। शिवोऽहम्.... सच्चिदानन्दोऽहम्... अजरोऽहम्.... साधकोऽहम्.... शिष्योऽहम्... धनी अहं... निधर्नोऽहम्.. मूर्खोऽहम्... विद्वानोऽहम्....।'
'जो कोई दिखे वह मैं ही अथवा उसमें मेरा ही परमात्मा बैठा है। मूर्खता और विद्वता उसके अन्तःकरण के भाव हैं, अन्तःकरण की योग्यता अयोग्यता है लेकिन सत्ता तो मेरे परमात्मा की है।' ऐसा जो स्मरण है वह अनन्य स्मरण है। जिसको ऐसा अनन्य स्मरण आ जाय उसके लिए संसार तरना बायें हाथ का खेल है। अगर अनन्य स्मरण नहीं आता तो किसी मंत्र का स्मरण ठीक है। मंत्र का स्मरण करते-करते देखे कि हमारी वृत्तियों की गहराई में लक्ष्य परमात्मा है कि संसार है। जितना-जितना स्मृति में संसार पड़ा है उतना उसको निकालते जायें। अगर नहीं निकल पाता है तो प्रार्थना करें किः 'हे प्रभु ! सब तेरी माया है। मैं सत्त्वगुण में न उलझ जाऊँ, रजोगुण-तमोगुण में न उलझ जाऊँ मेरे नाथ ! मैं कमाने और खाने में अपना जीवन नष्ट न कर दूँ। रुपयों की राशि बढ़ाने में अपना जीवन नष्ट न कर दूँ। मेरी स्मृति सरिता आपकी ओर निरन्तर बहती रहे।'
कई लोग भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन रुपये कमाने के लिए। रूपये कमाते हैं वह तो ठीक है लेकिन संग्रह करने में लगे हैं, संग्रह की राशि बढ़ाने में लगे हैं। यह परमात्मा का स्मरण नहीं है, रूपयों का स्मरण है। ऐसे लोग माया में मोहित हो गये हैं, संसार में भटकते हैं, जन्मते और मरते हैं।
कई लोग भगवान का भजन करते हैं शारीरिक सुविधा-अनुकूलता पाने के लिए।
एक घुड़सवार जा रहा था। रहा होगा वेदान्ती, रहा होगा सदगुरु का शिष्य। रास्ते हाथ से चाबुकर गिर पड़ा। कई यात्री पैदल चल रहे थे। किसी को न बोलकर स्वयं रुका, घोड़े से नीचे उतरा। गिरा हुआ चाबुक उठाया। किसी सज्जन ने पूछाः "भाई ! तुमने परिश्रम किया। हमको किसी को बोलते तो कोई न कोई चाबुक उठा देता। थोड़ी सेवा कर लेता।"
सवार कहता है किः "जगत में आकर मनुष्य को किसी की सेवा करनी चाहिए। सेवा लेनी नहीं चाहिए। दूसरों की सेवा ले तब जब बदले में अधिक सेवा करने की क्षमता हो।"
सेवा लेने की रूचि भक्तिमार्ग से गिरा देती है, साधना से गिरा देती है। छोटी-छोटी सेवा लेते-लेते बड़ी सेवा लेने की आदत बन जाती है। मेरे बदले कोई नौकर भगवान की सेवा-पूजा कर ले, मेरे बदले कोई पण्डित-ब्राह्मण जपानुष्ठान कर ले ऐसी वृत्ति बन जाती है। जीवन में आलस्य आ जाता है।
घुड़सवार कहता हैः "भैया ! मैं तुम्हारी सेवा अभी तो ले लूँ लेकिन फिर कौन जाने मिलें न मिलें। आपका प्रत्युपकार करने का मौका मिले न मिले। फिर कब ऋण चुका सकूँ? जन्म हुआ है सेवा करने के लिए, शरीर का सदुपयोग करने के लिए। जैसे दीया तेल और बाती जलाकर दूसरों के लिए रोशनी करता है ऐसे ही आदमी को चाहिए कि वह अपनी शक्ति और समय का सदुपयोग करके विश्व में उजाला करे। ऐसा नहीं कि दूसरे के दीये पर ताकता रहे। आप मेरी सेवा तो कर लेते लेकिन मेरे को आपकी सेवा का मौका कब मिलता? मेरे पर आपका ऋण क्या?"
"इतनी जरा-सी सेवा में ऋण क्या?"
"जरा-जरा से आदमी बड़ी सेवा पर आ जाता है। छोटी-छोटी गलतियों से आदमी बड़ी गलती पर चला जाता है।"
गाफिल साधक मन ही मन समाधान कर लेता है कि किसी व्यक्ति से थोड़ी बातचीत कर ली तो क्या हुआ? थोड़ी सी गपशप लगा ली तो क्या हुआ? ऐसे करते-करते वह पूरा जीवन बरबाद कर देता है। माया में ही उलझा रह जाता है। माया बड़ी दुस्तर है।
माया को तर जाना अगर आदमी के हाथ की बात होती तो शास्त्र आज्ञा नहीं देते कि संतों का संग करो। सच्चे संत और गुरुजनों का स्वभाव होता है कि कैसे भी करके साधकों को माया से पार होने में सहाय करना। इसलिए तो आवश्यकता आने पर क्रोध भी दिखा देते हैं, डाँटते-फटकारते भी हैं। वे किसी के दुश्मन थोड़े ही हैं? वे जब डाँटते हैं तो तुम तर्क करके अपना बचाव मत करो। अपनी गलती खोजो, अपनी बेवकूफी को ढूँढो। साधक-साधिका बन जाना कठिन नहीं है लेकिन अपनी निम्न आदतें बदल देना, बन्धनों को काटकर मुक्त हो जाना, त्रिगुणमयी माया को तर जाना बड़े पुरुषार्थ का काम है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि हम सम्पूर्णतया परमात्मा के शरण हो जायें। उनकी स्मृति इतनी बनी रहे कि संसार की आसक्ति छूट जाय। संसार का मोह न रहे, आकर्षण न रहे।
जब
खुली बाजार
सौदा न किया।
अब
रही हड़ताल
गाफिल से
दिया।।
कहीं ऐसा न हो जाय इसलिए सावधान रहना। जीवन का अन्तिम श्वास आ जाय, जीवन की हड़ताल होने लगे तब कहीं पश्चाताप हाथ न लगे। इसलिए अभी से ही मोक्ष का सौदा कर लो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
दीक्षाः
जीवन का
आवश्यक अंग
जैसे डॉक्टरी पास करने के बाद भी बड़े डॉक्टर के साथ रहना, देखना, सीखना जरूरी होता है, वकालत पास करने पर भी वकील के पास रहना-सीखना जरूरी होता है, वैसे ही ईश्वर से मिलने के लिए, अनजाने रास्ते पर चलने के लिए किसी जानकार की सहायता लेना आवश्यक है।
ईश्वर एक ऐसी वस्तु है, सत्य एक ऐसी वस्तु है जिसको आप आँख से देख भी सकते हैं, नाक से सूँघ भी सकते हैं और जिसे जीभ से चखकर भी जान सकते हैं। परंतु जो इन्द्रियों का विषय भी नहीं है, जो आपकी सभी इन्द्रियों को संचालित करने वाला है, वह अन्तर्यामी आपका आत्मा ही है। किसी भी इन्द्रिय की ऐसी गति नहीं है कि वह उल्टा होकर आपको देखे। उसके लिए प्रमाण होता है वाक्य। गुरु जो हैं वे-
चरणदास
गुरु कृपा
कीन्हीं।
उलट
गयी मोरी नैन
पुतरिया।।
गुरु हमारी छठी इन्द्री का दरवाजा खोल देते हैं, हमें बाहर की चीजों को देखने वाली आँख की जगह भीतर देखने वाली आँख, आत्मा-परमात्मा को देखने वाली शक्ति का दान करते हैं। माने, गुरु ईश्वर का दान करते हैं और शिष्य उसको ग्रहण करता है, पचा लेता है। ईश्वर का दान करने को 'दी' बोलते हैं और पचाने की शक्ति को 'क्षा' बोलते हैं। इस तरह बनता है 'दीक्षा'। दीक्षा माने, देना और पचाना। गुरु का देना और शिष्य का पचाना।
जिसका कोई गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। क्या आप ऐसे हैं कि आपका लोक-परलोक में, स्वार्थ-परमार्थ में कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है? फिर तो आप बहुत असहाय हैं। क्या आप इतने बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धि का आपको इतना अभिमान हैं कि आप आपने से बड़ा ज्ञानी किसी को समझते ही नही? यह तो अभिमान की पराकाष्ठा है भाई !
दीक्षा कई तरह से होती हैः आँख से देखकर, संकल्प से, हाथ से छूकर और मंत्र-दान करके। अब, जैसी शिष्य की योग्यता होगी, उसके अनुसार ही दीक्षा होगी। योग्यता क्या है? शिष्य की योग्यता है श्रद्धा और गुरु की योग्यता है अनुग्रह। जैसे वर-वधु का समागम होने से पुत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही श्रद्धा और अनुग्रह का समागम होने से जीवन में एक विशेष प्रकार के आत्मबल का उदय होता है और शिष्य के लिए इष्ट का, मंत्र का और साधना का निश्चय होता है ताकि आप उसको बदल न दें। नहीं तो कभी किसी से कुछ सुनेंगे, कभी किसी से कुछ, और जो जिसकी तारीफ करने में कुशल होगा, अपने इष्ट व मंत्र की खूबखूब महिमा सुनायेगा वही करने का मन हो जायगा। फिर कभी 'योगा' करेंगे तो कभी विपश्यना' करेंगे, कभी वेदान्त पढ़ने लगेंगे तो कभी राम-कृष्ण की उपासना करने लगेंगे, कभी निराकार तो कभी साकार।
आपके सामने जो सुन्दर लड़का या लड़की आवेगी उसी से ब्याह करने का अर्थ होता है कि एक ही पुरुष या एक ही स्त्री हमारे जीवन में रहे, वैसे ही, मंत्र लेने का अर्थ होता है कि एक ही निष्ठा हमारे जीवन में हो जाय, एक ही हमारा मंत्र रहे और एक ही हमारा इष्ट रहे।
एक बात आप और ध्यान में रखें। निष्ठा ही आत्मबल देती है। यही भक्त बनाती है। यही स्थितप्रज्ञ बनाती है। परमात्मा एक अचल वस्तु है। उसके लिए जब हमारा मन अचल हो जाता है तब अचल और अचल दोनों मिलकर एक हो जाते हैं।
इसलिए, गुरु हमको अपने इष्ट में, अपने ध्यान में, अपनी पूजा में, अपने मंत्र में अचलता, निष्ठा देते हैं और आप जो चाहते हैं सो आपको देते हैं। देने में और दिलाने में वे समर्थ होते हैं। हम तो कहते हैं कि वे लोग दुनिया में बड़े अभागे हैं, जिनको गुरु नहीं है।
देखो, यह बात भी तो है कि यदि कोई वेश्या के घर में भी जाना चाहे तो उस मार्गदर्शक चाहिए, जुआ खेलना चाहें तो भी कोई बताने वाला चाहिए, किसी की हत्या करना चाहे तो भी कोई बतानेवाला चाहिए, फिर यह जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, भक्ति हैं, साधना है उसको आप किसी बतानेवाले के बिना, गुरु के बिना कैसे तय कर लेते हैं, यह एक आश्चर्य की बात है।
गुरु आपको मंत्र भी देते हैं, साधना भी बताते हैं, इष्ट का निश्चय भी कराते हैं और गलती होने पर उसको सुधार भी देते हैं। आप बुरा न मानें, एक बात मैं आपको कहता हूँ। ईश्वर सब है, इसलिए उसकी प्राप्ति का साधन भी सब है।
सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्ति में, सब क्रिया में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। केवल आपको अभी तक पहचान करानेवाला मिला नहीं है इसी से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पात हैं। अतः दीक्षा तो साधना का, साधना का ही नहीं जीवन का आवश्यक अंग है। दीक्षा के बिना तो जीवन पशु-जीवन है।
(स्वामी
अखण्डानन्द
सरस्वती)
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सब रोगों
की औषधिः
गुरुभक्ति
हम लोगों के जीवन में दो तरह के रोग होते हैं- बहिरंग और अन्तरंग। बहिरंग रोगों की चिकित्सा तो डॉक्टर लोग करते हैं और वे इतने दुःखदायी भी नहीं होते हैं जितने कि अन्तरोग होते हैं।
हमारे अन्तरंग रोग हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह.
भागवत में इस एक-एक रोग की निवृत्ति के लिए एक-एक औषधि बतायी है। जैसे काम के लिए असंकल्प, क्रोध के लिए निष्कामता, लोभ के लिए अर्थानर्थ का दर्शन, भय के लिए तत्त्वादर्शन आदि।
औषति
दोषान् धत्ते
गुणान् इति
औषधिः।
जो दोष को
जला दे और
गुणों का आधान
कर दे उसका
नाम है औषधि।
फिर, अलग-अलग
रोग की
अलग-अलग औषधि
न बताकर एक
औषधि बतायी और
वह है अपने
गुरु के प्रति
भक्ति। एतद्
सर्व
गुरोर्भक्तया।
यदि अपने गुरु के प्रति भक्ति हो तो वे बतायेंगे कि, बेटा ! तुम गलत रास्तें से जा रहे हो। इस रास्ते से मत जाओ। उसको ज्यादा मत देखो, उससे ज्यादा बात मत करो, उसके पास ज्यादा मत बैठो, उससे मत चिपको, अपनी 'कम्पनी' अच्छी रखो, आदि।
जब गुरु के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जायगा तब दूसरों से प्रेम नहीं होगा। भक्ति में ईमानदारी चहिए, बेईमानी नहीं। बेईमानी सम्पूर्ण दोषों की व दुःखों की जड़ है। सुगमता से दोषों और दुःखों पर विजय प्राप्त करने का उपाय है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ और हित के साथ गुरु की सेवा करना।
श्रद्धा और पूर्ण नहीं होगी और यदि तुम कहीं भोग करने लगोगे या कहीं यश में, पूजा में, प्रतिष्ठा में फँसने लगोगे और गुरुजी तुम्हें मना करेंगे तो बोलोगे कि, गुरुजी हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारी उन्नति उनसे देखी नहीं जाती, इनसे देखा नहीं जाता है कि लोग हमसे प्रेम करें। गुरुजी के मन अब ईर्ष्या आ गयी और ये अब हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं।
साक्षात् भगवान तुम्हारे कल्याण के लिए गुरु के रूप में पधारे हुए हैं और ज्ञान की मशाल जलाकर तुमको दिखा रहे हैं, दिखा ही नहीं रहे हैं, तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। तुम देखते हुए चले जाओ आगे.... आगे... आगे...। परंतु उनको कोई साधारण मनुष्य समझ लेता है, किसी के मन में ऐसी असद् बुद्धि, ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है तो उसकी सारी पवित्रता गजस्नान के समान हो जाती है। जैसे हाथी सरोवर में स्नान करके बाहर निकले और फिर सूँड से धूल उठा-उठा कर अपने ऊपर डालने लगे तो उसकी स्थिति वापस पहले जैसी ही हो जाती है। वैसे ही गुरु को साधारण मनुष्य समझने वाले की स्थिति भी पहले जैसी ही हो जाती है।
ईश्वर सृष्टि बनाता है अच्छी-बुरी दोनों, सुख-दुःख दोनों, चर अचर दोनों, मृत्यु-अमरता दोनों। परंतु संत महात्मा, सदगुरु मृत्यु नहीं बनाते हैं, केवल अमरता बनाते हैं। वे जड़ता नहीं बनाते हैं, केवल चेतनता बनाते हैं। वे दुःख नहीं बनाते, केवल सुख बनाते हैं। तो संत महात्मा माने केवल अच्छी-अच्छी सृष्टि बनाने वाले, लोगों के जीवन में साधन डालने वाले, उनको सिद्ध बनाने वाले, उनको परमात्मा से एक कराने वाले।
लोग कहते
हैं कि
परमात्मा
भक्तों पर
कृपा करते
हैं, तो करते
होंगे, पर महात्मा
न हो तो कोई
भक्त ही नहीं
होगा और
भक्त ही जब
नहीं होगा तो
परमात्मा
किसी पर कृपा
भी कैसे
करेंगे? इसलिए
परमात्मा
सिद्ध पदार्थ
है और महात्मा
प्रत्यक्ष
है। परमात्मा
या तो परोक्ष
हैं, - सृष्टिकर्ता
कारण के रूप
में और या तो
अपरोक्ष हैं –
आत्मा के रूप
में। परोक्ष
हैं तो उन पर
विश्वास करो
और अपरोक्ष
हैं तो 'निर्गुणं,
निष्क्रयं,
शान्तं' हैं।
महात्मा का
यदि कोई
प्रत्यक्ष
स्वरूप है तो
वह साक्षात्
महात्मा ही
है। महात्मा
ही आपको ज्ञान
देते हैं। आचार्यात्, विदधति, आचार्यवान
पुरुषो वेदा।
जो लोग आसमान में ढेला फेंककर निशाना लगाना चाहते हैं उनकी बात दूसरी है। पर, असल बात यह है कि बिना महात्मा के न परमात्मा के स्वरूप का पता चल सकता है न उसके मार्ग का पता चल सकता है। हम परमात्मा की ओर चल सकते हैं कि नहीं इसका पता भी महात्मा के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए, भागवत के प्रथम स्कंध में ही भगवान के गुणों से भी अधिक गुण महात्मा में बताये गये हैं, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। ग्यारहवें स्कंध में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया है किः
मद्भक्तापूजाभ्यधिका।
'मेरी पूजा से बड़ी है महात्मा की पूजा'।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
गुरु में
ईश्वर-बुद्धि
होने के उपाय
जानने और चाहने पर भी गुरु में पूर्ण ईश्वर बुद्धि क्यों नहीं होती है? वह कैसे हो सकती है? गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अपने मन को ले जाकर कैसे बैठायें?
जब तुम गुरु के बारे में विचार करोगे कि इनका शरीर दिव्य है, चिन्मय है तो उनकी दिव्यता व चिन्मयता का चिन्तन करते-करते तुम्हारा मन भी दिव्य और चिन्मय हो जायगा और तुम भी अपने शरीर को भूल जाओगे और तुम्हारी 'ध्येयाकार समापत्ति' हो जायगी।
तब तुम देखोगे कि गुरु तो साक्षात् परमात्मा के स्वरूप में बैठे हैं और उसी समय तुम्हें अपने परमात्मा, अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का उतना-उतना ज्ञान हो जायगा, जितना-जितना ज्ञान तुम्हें अपने सूक्ष्म स्वरूप का होगा। जब तक तुम अपने को हड्ड़ी-मांस-चाम समझ रहे हो तब तक गुरु में भी हड्डी-मांस-चाम की बुद्धि होना सम्भव है। परंतु भाव से जैसे आप जयपुर की बनी राम, कृष्ण, शिव की मूर्ति को साक्षात् भगवान मानते हो और गण्डकी शिला को शालग्राम मानते हो, वैसे ही अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से मनुष्य के रूप में दिखते हुए गुरु को भी आप पहले दिव्य रूप में देखो और उनकी जो क्रिया है, उनको कर्म के रूप में नहीं, लीला के रूप में देखो। इस तरह जितनी-जितनी सूक्ष्मता आपके आत्मा में बढ़ेगी, उतना-ही-उतना गुरु का सूक्ष्म रूप आपको दिखायी पड़ेगा।
झण्डा
गाड़ो जायके
हद-बेहद के
पार,
हद-बेहद
के पार दूर
जहाँ अनहद
बाजे,
हद-बेहद
के पार है
हमारी चौकी।
'जो हद बेहद के पार है, हमारे बैठने की जगह वह है।'
उपासना के ग्रन्थों में इस तरह का वर्णन आता है कि प्रसाद को भोजन समझना अपराध है, मूर्ति को जड़ समझना अपारध है, गुरु को मनुष्य समझना अपराध है।
जैसे-जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, आपकी स्थिति ऊँची होती जायेगी, वैसे-ही-वैसे आप अपने सदगुरु के आसन के पास पहुँचते जायेंगे और वह आपकी उपासना हो जायगी।
(स्वामी
अखण्डानन्द
सरस्वती)
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
आज्ञापालन
की महिमा
गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की अपेक्षा उनकी आज्ञाओं का पालन करना श्रेष्ठतर है। आज्ञाकारिता एक मूल्यवान सदगुण है, क्योंकि यदि आप आज्ञाकारिता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे तो आत्म-साक्षात्कार के पथ के कट्टर शत्रु अहं का धीरे-धीरे उन्मूलन हो जायगा।
जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है केवल वही अपनी निम्न आत्मा पर आधिपत्य रख सकता है। आज्ञाकारिता अत्यन्त व्यावहारिक, अनन्य तथा सक्रिय अध्वयवसायी होनी चाहिए। गुरु की आज्ञाकारिता न तो टाल मटोल करती है और न सन्देह ही प्रकट करती है। दम्भी शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन भयवश करता है। सच्चा शिष्य अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन प्रेम के लिए, प्रेम के कारण करता है।
आज्ञा-पालन की विधि सीखिए। उस स्थिति में ही आप आदेश दे सकते हैं। शिष्य बनना सीखिये, तभी आप गुरु बन सकेंगे।
इस भ्रामक धारणा को त्याग दीजिए कि गुरु की अधीनता स्वीकार करना, उनका आज्ञानुवर्ती होना तथा उनकी शिक्षाओं को कार्यान्वित करना दासता की मनोवृत्ति है। अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि 'किसी अन्य व्यक्ति की अधीनता स्वीकार करना अपनी गरिमा एवं स्वाधीनता के विपरीत है। यह एक गम्भीर और भारी भूल है। यदि आप ध्यानपूर्वक चिन्तन करें तो आप देखेंगे कि आपकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता वास्तव में आपके अपने ही अहं तथा मिथ्याभिमान की नितान्त घृणित दासता है, यह विषयी मन की तरंग है। जो अपने अहं तथा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही स्वतन्त्र व्यक्ति है। वह शूरवीर है। इस विजय को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति गुरु के उच्चतर अध्यात्मीकृत व्यक्तित्व की अधीनता स्वीकार करता है। वह इस अधीनता-स्वीकरण द्वारा अपने निम्न अहं को पराजित करता था असीम चेतना के आनन्द को प्राप्त करता है।
आध्यात्मिक पथ कला की स्नातकोत्तर उपाधि के लिए शोध-प्रबन्ध लिखने जैसा नहीं है। यह सर्वथा भिन्न प्रणाली है। इसमें गुरु की सहायता की आवश्यकता प्रतिक्षण रहती है। इन दिनों साधक आत्मनिर्भर, उद्धत तथा स्वाग्रही बन गये हैं। वे गुरु की आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की चिन्ता नहीं करते । वे गुरु बनाना नहीं चाहते। वे प्रारम्भ से ही स्वतंत्रता चाहते हैं। वे समझते हैं कि वे तुरीय अवस्था में हैं जबकि उन्हें आध्यात्मिक अथवा सत् का प्रारम्भिक ज्ञान भी नहीं होता है। वे स्वेच्छाचारिता अथवा अपनी बात मनवाने और स्वेच्छानुसार चलने को स्वतन्त्रता समझने की भूल करते हैं। यह गम्भीर शोचनीय भूल है। यही कारण है कि उनकी उन्नति नहीं होती। वे साधना की क्षमता तथा ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास खो बैठते हैं। ऐसे निगुरे लोग आत्मशान्ति से, आत्म-सामर्थ्य से, आत्म-प्रेम से वंचित रह जाते हैं। अतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा हैः
गुरुबिन
भवनिधि तरहीं
न कोई।
चाहे
बिरंचि शंकर
सम होई।।
(शिवानन्दजी)
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
शिवाजी
महाराज की
गुरुभक्ति
छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास स्वामी के एकनिष्ठ भक्त थे। समर्थ भी सभी शिष्यों से अधिक उन्हें प्यार करते। शिष्यों को भावना हुई की शिवाजी के राजा होने के कारण समर्थ जी उनसे अधिक प्रेम रखते हैं। समर्थ जी ने तत्काल उनका सन्देह दूर करने का सोचा। वे शिष्यमण्डली के साथ जंगल में गये। सभी रास्ता भूल गये और समर्थजी एक गुफा में जाकर उदर-शूल का बहाना करके लेट गये। शिष्य आये। देखा, पीड़ित हो रहे हैं गुरुजी। शूल-निवारण का उपाय समर्थजी से पूछा और एक-दूसरे के मुँह ताकने लगे। दुर्बल मन के लोग और तक भगत की जैसी हिलचाल होती है वैसा वातावरण बन गया।
इधर शिवाजी महाराज समर्थ के दर्शनार्थ निकले। उन्हें पता चला कि वे इस जंगल में कहीं हैं। खोजते-खोजते एक गुफा के पास आये। गुफा में पीड़ा से विह्वल शब्द सुनाई पड़ा। भीतर जाकर देखा तो साक्षात् गुरुदेव ही विकलता से करवटें बदल रहे हैं। शिवाजी ने हाथ जोड़कर उनकी वेदना का कारण पूछा।
समर्थ जी ने कहाः "शिवा ! भीषण उदर-पीड़ा से विकल हूँ।"
"महाराज ! इसकी दवा?"
"शिवा ! इसकी कोई दवा नहीं। रोग असाध्य है। हाँ, एक ही दवा काम कर सकती है, पर जाने दो..."
"नहीं गुरुदेव ! निःसंकोच बताएँ। शिवा गुरुदेव को स्वस्थ किये बिना चैन नहीं ले सकता।"
"सिंहिनी का दूध और वह भी ताजा निकला हुआ, पर शिवा ! वह सर्वथा दुष्प्राप्य है।"
पास में पड़ा गुरुदेव का तुम्बा उठाया और समर्थ जी को प्रणाम करके शिवाजी तत्काल सिंहिनी की खोज में निकल पड़े।
कुछ दूर जाने पर एक जगह दो सिंह-शावक दिखाई पड़े। शिवाजी ने सोचाः 'निश्चय ही यहाँ इनकी माता आयगी।' संयोग से वह आ भी गई। अपने बच्चों के पास अनजाने मनुष्य को देख वह शिवा पर टूट पड़ी और अपने जबड़े में उनकी गरदन पकड़ ली।
शिवा कितने ही शूरवीर हों, पर यहाँ तो उन्हें सिंहनि का दूध जो निकालना था ! उन्होंने धीरज धारण किया और हाथ जोड़कर सिंहिनी से विनय करने लगे।
"माँ ! मैं यहाँ तुम्हें मारने या तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाने को नहीं आया। गुरुदेव को स्वस्थ करने के लिए तुम्हारा दूध चाहिए, उसे निकाल लेने दो। गुरुदेव को दे आऊँ, फिर भले ही तुम मुझे खा जाना।" शिवाजी ने ममता भरे हाथ से उसकी पीठ सहलाई। मूक प्राणी भी ममता से अधीन हो जाते हैं। सिंहिनी का क्रोध शान्त हो गया। उसने शिवाजी का गला छोड़ा और बिल्ली की तरह उन्हें चाटने लगी।
मौका देख शिवाजी ने उसी कोख में हाथ डाल दूध निचोड़कर तुम्बा भर लिया और उसे नमस्कार कर बड़े आनन्द के साथ निकल पड़े।
गुफा में पहुँच कर गुरुदेव के समक्ष दूध से भरा हुआ तुम्बा रखते हुए शिवाजी ने गुरुदेव को प्रणाम किया।
"आखिर तुम सिंहिनी का दूध भी ले आये ! धन्य हो शिवा ! तुम्हारे जैसे एकनिष्ठ शिष्य के रहते गुरु को पीड़ा ही क्या रह सकती है !" समर्थजी ने शिवा के सिर पर हाथ रखते हुए अन्य शिष्यों की ओर दृष्टि की।
अब शिष्यों को पता चला कि ब्रह्मवेत्ता गुरु अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसकी अपनी विशेष योग्यताएँ होती हैं, विशेष कृपा का वह अधिकारी होता। ऐसे विशेष कृपा के अधिकारी गुरुभाइयों को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपनी दुर्बलताएँ, अयोग्यताएँ दूर करने में लगना चाहिए। ईर्ष्या करने से अपनी दुर्बलताएँ और अयोग्यताएँ बढ़ती हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
धर्म में
दृढ़ता कैसे
हो ?
श्रीराममिश्रजी महात्मा पुण्डरीकाक्षजी की सेवा में गये। बोलेः "भगवन् ! मेरे मन में स्थिरता नहीं है। इसका कारण मैंने यह निश्चय किया है कि मेरी निज धर्म में दृढ़ता नहीं है। इसलिए आप कृपापूर्वक यह बताएँ कि धर्म में दृढ़ता किस प्रकार होती है।"
संत श्री ने कहाः "जिस उपाय से दृढ़ता होती है, उसे आप नहीं कर सकते, इसलिए उसका बताना व्यर्थ है।"
मिश्रजी ने फिर कहाः "आप उसे बताएँ, मैं अवश्य करूँगा। जिस किसी ने जो उपाय मुझे बताया है उसे मैंने अवश्य किया है। आप संकोच न करें। इसके लिए मैं सर्वस्व त्याग करने को भी तैयार हूँ।"
श्रीपुण्डरीकाक्षः "आपने अभी तक अन्धों से ही यह बात पूछी है, आँखों वालों से नहीं। अन्धों की लकड़ी पकड़कर भला, आज तक कोई गन्तव्य स्थान पर पहुँचा है?"
मिश्रजीः "हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने ठोकर खाकर इसका अनुभव किया है। तभी तो आँखवालों के पास आया हूँ।"
श्रीपुण्डरीकाक्षः "आपके उस अनुभव में एक बात की कसर रह गई है। आपमें आँखवालों की पहचान नहीं है, नहीं तो मेरे पास क्यों आते?
मिश्रजी ने बहुत अनुनय-विनय करने पर आचार्य पुण्डरीकाक्ष ने उन्हें महीने पीछे बताने को कहा। जब अवधि बीतने पर मिश्रजी फिर आये तब संत श्री ने कहाः
"दूसरों का पाप छिपाने और अपना पाप कहने से धर्म में दृढ़ता प्राप्त होती है।"
इस सुन्दर उपदेश को सुनकर मिश्रजी ने गदगद स्वर से कहाः "भगवन् ! कृपा के लिए धन्यवाद ! मुझे अपने सदाचारीपन को बड़ा गर्व था और दूसरों की बुराइयाँ सुनकर उन्हें मुँह पर फटकारना और भरी सभा में उन्हें बदनाम करना अपना कर्त्तव्य समझता। उसी अन्धे की लकड़ी को पकड़कर मैं भवसागर को पार करना चाहता था। कैसी उलटी समझ थी !"
अपनी भूल समझकर पश्चाताप करने से जीवन की घटनाओं पर विचार करने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब मनुष्य अपनी अल्पज्ञता से सधे हुए दृष्टि कोण को छोड़कर भगवदीय दृष्टिकोण से देखने और विचार करने लगता है।
अपना गुण प्रकट करना और दूसरों का दोष प्रकट करना, इससे आदमी धर्म से च्युत हो जाता है। जो दूसरों का दोष छुपाता है और अपना दोष प्रकट करता है उसको धर्म में दृढ़ता होती है। जिसको धर्म में दृढ़ता होती है वह इहलोक और परलोक में सुख-शान्ति का भागी होता है।
दूसरों को टोटे चबाने की अपेक्षा उन्हें खीर खांड खिलाने का सोचो तो धर्म में दृढ़ता होती है, शांति और प्रेम बढ़ने लगता है। हृदय की उदारता हो, कायरता नहीं। वीरों को उदारता और क्षमा शोभा देती है, कायरों को नहीं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
आत्म-पूजन
देवाधिदेव महादेव जी ने श्री वशिष्ठजी से कहाः 'हे मुनीश्वर ! इस जगत में ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र जो बड़े देवता हैं वे सब सर्वसत्ता रूप एक ही आत्मदेव से प्रकट हुए हैं। सबका मूल बीज वही देव है। जैसे अग्नि से चिनगारी और समुद्र से तरंगे उपजते हैं वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त सभी उसी आत्मदेव से उपजते हैं और पुनः उसी में लीन होते हैं। सब प्रकाशों का प्रकाश और तत्त्ववेत्ताओं का पूज्य वही है।
हे मुनिशार्दूल ! जरा, मृत्यु, शोक और भय को मिटाने वाला आत्मदेव ही सबका सार और सबका आश्रय रूप है। उसका जो विराट रूप है वह कहता हूँ, सुनो। वह अनन्त है। परमाकाश उसकी ग्रीवा है। अनेक पाताल उसके चरण हैं। अनेक दिशाएँ उसकी भुजा हैं। सब प्रकाश उसके शास्त्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रूद्रादि देवता और जीव उसकी रोमावली है। जगज्जाल उसका विवृत है। काल उसका द्वारपाल है। अनन्त ब्रह्माण्ड उसकी देह के किसी कोण में स्थिति है। वही आत्मदेव शिवरूप सर्वदा और सबका कर्त्ता है, सब संकल्पों के अर्थ का फलदाता है। आत्मा सबके हृदय में स्थित है।
हे ऋषिवर्य ! अब मैं वह आत्म-पूजन कहता हूँ जो सर्वत्र पवित्र करने वाले को भी पवित्र करता है और सब तम और अज्ञान का नाश करता है। आत्मपूजन सब प्रकार से सर्वदा होता है और व्यवधान कभी नहीं पड़ता। उस सर्वात्मा शान्तरूप आत्मदेव का पूजन ध्यान है और ध्यान ही पूजन है। जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करो। सबका प्रकाशक आत्मा ही है। उसका पूजन दीपक से नहीं होता, न धूप, पुष्प, चन्दनलेप और केसर से होता है। अर्घ्य पाद्यादिक पूजा की सामग्रियों से भी उस देव का पूजन नहीं होता।
हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! एक अमृतरूपी जो बोध है, उससे उस देव का सजातीय प्रत्यय ध्यान करना ही उसका परम पूजन है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मदेव अनुभव रूप है। सर्वदा और सब प्रकार उसका पूजन करो अर्थात् देखना, स्पर्श करना सूँघना, सुनना, बोलना, देना, लेना, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ क्रियाएँ हैं, सब चैतन्य साक्षी में अर्पण करो और उसी के परायण बनो। आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप-दीप और पूजन की सामग्री है। ध्यान ही उस परमदेव को प्रसन्न करता है और उससे परमानन्द प्राप्त होता है। अन्य किसी प्रकार स वह देव प्राप्त नहीं होता।
हे मुनीश्वर ! मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत-दान के फल को पाता है। सत्रह निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे ते अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पर्यन्त पूजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल को पाता है और जो दिनभर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे महर्षे ! यह परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है।
यथा प्राप्ति के समभाव में स्नान करके शुद्ध होकर ज्ञान स्वरूप आत्मदेव का पूजन करो। जो कुछ प्राप्त हो उसमें राग-द्वेष से रहित होना और सर्वदा साक्षी का रूप अनुभव में स्थित रहना ही उसका पूजन हो। जो नित्य, शुद्ध, बोधरूप और अद्वैत है उसको देखना और किसी में वृत्ति न लगाना ही उस देव का पूजन है। प्राण अपानरूपी रथ पर आरूढ़ जो हृदय में स्थित है उसका ज्ञान ही पूजन है।
आत्मदेव सब देहों में स्थित है तो भी आकाश-सा निर्लिप्त निर्मल है। सर्वदा सब पदार्थों का प्रकाशक, प्रत्यक् चैतन्य जो आत्मतत्त्व अपने हृदय स्थित है वही अपने फुरने से शीघ्र ही द्वैत की तरह हो जाता है। जो कुछ साकाररूप जगत देख पड़ता है, सो सब विराट आत्मा है। इससे अपने में इस प्रकार विराट की भावना करो कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेरी देह है, हाथ, पाँव, नख, केश है। मैं ही प्रकाश रूप एक देव हूँ। नीति इच्छादिक मेरी शक्ति है। सब मेरी ही उपासना करते हैं। जैसे स्त्री श्रेष्ठ भर्ता की सेवा करती है, वैसे ही शक्ति मेरी उपासना करती है। मन मेरा द्वारपाल है जो त्रिलोकी का निवेदन करने वाला है। चिन्तन मेरा आने-जाने वाला प्रतिहारी है। नाना प्रकार के ज्ञान मेरे अंग के भूषण हैं। कर्मेन्द्रियाँ मेरे दास, ज्ञानेन्द्रियाँ मेरे गण हैं ऐसा मैं एक अनन्त आत्मा, अखण्डरूप, भेद से रहित अपने आप में स्थित परिपूर्ण हूँ।
इसी भावना से जो पूजा करता है वह परमात्मदेव को प्राप्त होता है। दीनता आदि उसके सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक नहीं उपजता। न तोष होता है न कोप होता है। वह विषय की प्राप्ति से तृप्ति नहीं मानता और न इसके वियोग से खेद मानता है। न अप्राप्त की वाञ्छा करता है न प्राप्त के त्याग की इच्छा करता है। सब पदार्थों मे उसका समभाव रहता है।
हे मुनीश्वर ! भीतर से आकाश-सा असंग रहना और बाहर से प्रकृति-आचार में रहना, किसी के संग का हृदय में स्पर्श न होने देना और सदा समभाव विज्ञान से पूर्ण रहना ही उस देव की उपासना है। जिसके हृदयरूपी आकाश से अज्ञानरूपी मेघ नष्ट हो गया है उसको स्वप्न में भी विकार नहीं होता।
हे महर्षे ! यह परम
योग है। यही
परम क्रिया है
और यही परम प्रयोजन
है। जो परम
पूजा करता है
वह परम पद को पाता
है। उसको सब
देव नमस्कार
करते हैं और
वह पुरुष सबका
पूजनीय होता
है।"
(श्री
योगवाशिष्ठ
महारामायण)
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
चिन्ता व
ईर्ष्या से
बचो
चिन्ता, ईर्ष्या और जलन आदमी को आत्मानन्द से दूर कर देती है, सहजता-सरलता-स्वाभाकिता से दूर कर देती है। आत्मानन्द से तो दूर कर ही देती है, तन मन का स्वास्थ्य भी खराब कर देती है। चिन्ता और ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि आँखों से जो दिखता है उसको दूसरा मानते हैं और देह को 'मैं' मानते हैं।
'वह आदमी मौज कर रहा है....'
'अरे उसमें भी मैं हूँ' – यह ज्ञान नहीं है इसलिए ईर्ष्या होती है। अपने जीवन की चिन्ता होती है। अपने अचिन्तय पद का ख्याल नहीं है। इसलिए संसार की छोटी-छोटी बातों में चिन्ता होती है, दूसरों के सुख की ईर्ष्या होती है। चिन्ता और ईर्ष्या आत्मानन्द लेने में रूकावट है। परमात्मा की दिव्य सुधा निशदिन बरस रही है, आत्म-अमृत बरस रहा है लेकिन चित्त की मलिनता के कारण उसका अनुभव नहीं होता। संसार की चिन्ता मस्तिष्क में रखते हैं इससे परमात्मा का सुख जो बिलकुल नजदीक है, स्वाभाविक है फिर भी दिखता नहीं। चित्त में चित्र-विचित्र इच्छाएँ-आकांक्षाएँ मँडरा रही हैं। मुनिशार्दूल वशिष्ठजी कहते हैं - "हे रामजी ! इच्छावानों से वृक्ष भी भय पाते हैं।"
बढ़िया सत्संग होता है, तत्त्वज्ञान को ऊँची बात होती है, चित्त आत्म-विश्रान्ति की गहराइयों को छूकर तृप्त होता है, बड़ा आनन्द आता है लेकिन सांसारिक बातें खड़ी करके सब बिखेर देते हैं। बढ़िया तत्त्वज्ञान की बात होती है, श्रवण मनन चलता है लेकिन ईर्ष्या तत्त्वज्ञान को अन्तःकरण में बैठने नहीं देती। मेहमान घर में आये उसको आदर नहीं दो, उसको बैठाओ नहीं तो वह क्या बात करेगा? तत्त्वज्ञान का अवकार नहीं, आदर नहीं इसलिए वह अन्तःकरण में ठहरता नहीं। तत्त्वज्ञान ठहर जाय तो बेड़ा पार हो जाय। दुनियाँ के राजे-महाराजे वह सुख नहीं भोगते जो आत्मज्ञानी आत्मसुख भोगते हैं। बुढ़ापा और मौत सबको पकड़ते हैं लेकिन आत्मज्ञानी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बुढ़ापा तो आयेगा, मौत तो होगी लेकिन ज्ञानी शरीर के बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा नहीं समझते, शरीर की मौत को अपनी मौत नहीं समझते।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
शीलवान
नारी
सब धर्मों का मूल कारण शील है। शील आने से अन्य सब गुण आ मिलते हैं। पतिव्रता स्त्री के जो धर्म हैं वे सब धर्म शील में आ जाते हैं और जितने दोष कर्कशा नारी के हैं वे सब अशील कहलाते हैं। शीलरहित नारियों का आचार इस प्रकार होता हैः
एक घर से दूसरे घर बिना कारण भटकना, निश्चिन्तता से घर में न बैठना, पर पुरुष के साथ बातचीत करने में आनन्द समझना, काम कहीं करना और मन कहीं रखना, स्वयं दुर्गुणों का भण्डार होने पर भी दूसरों के दुर्गुण कथन करने में बृहस्पति के समान वक्ता बन बैठना, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठने में बड़ों के आदर-मान का ख्याल न रखना, दूसरों की पंचायत करना, बातें करते दुष्ट शब्दों का उच्चारण करना, असत्य बोलना, झूठी सौगंध खाना, पति को नौकर के समान समझ कर हुकुम चलाना, वहम की बातें करना, बहम में लगे रहना, मंत्र-तंत्र जादू-टूणों-फूणों को अत्यन्त वहम के साथ मानना, मोहन वशीकरण, पुत्र-रक्षा आदि के निमित्त धूर्तों के पास जाना, यदि पति इन बातों को झूठी कहे तो क्रुष्ट (शापित) कहना, मलिन रहना, घर को मलिन रखना, रसोई किस प्रकार होती है यह ठीक न जानना, रसोई में बार-बार कंकड़, बाल या कोयले आते रहना, बालकों को कैसे सुधारना-कैसे उनकी रक्षा करना यह न जानना, जानती हो तो भी लापरवाही से वैसा न करना, कुल की प्रतिष्ठा बिगड़ने की परवाह न होना, आसपास के पड़ौसियों से टंटा करना, पति से लड़ना, झूठ बोलना, उसको डाँटना, ताना देना, लड़कों को बिना कारण मारना, चिल्लाना आदि। ये सब शील रहित नारी के लक्षण हैं। उसमें छल, प्रपंच, परमैत्री, दुस्साहस, अपवित्रता, कटुता, निर्लज्जता, निठुरपना आदि अवगुण होते हैं। ऐसी नारी दूसरों को दुःख देती है और आप भी अनेक योनियों में पड़कर दुःख भोगती है।
अपना इहलोक-परलोक का कल्याण चाहने वाली महिलाओं को ऐसी नारियों की संगत से बचकर जो शीलवान है, पवित्र है, सहनशील है, त्यागशील है, शुद्ध प्रेम से युक्त है अर्थात् जिसमें पतिव्रता स्त्री के सदगुण हैं ऐसी गुणवान नारी का आदर का करना चाहिए और कुलटा नारी से नौ गज दूर रहना चाहिए।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
पिटारे
में बिलार
एक किसान पिटारे में घी, गुड़, मिठाई, रोटियाँ आदि रखकर खेत में जा रहा था। बच्चों को कहता गया किः "तुम्हारी माँ बाहरगाँव गई है। स्कूल से आ जाओ तो पिटारे से भोजन लेकर खा लेना। मैं शाम को घर लौटूँगा।"
किसान खेत में चला गया। बच्चे भी स्कूल में पढ़ने गये। इधर एक बिलार पिटारे में घुस गया। मजे से घी, गुड़, मिठाई, रोटियों का भण्डारा करके आराम से वहीं बैठ गया। दोपहर को स्कूल से भूखे-प्यासे बच्चे आये। भोजन लेने के लिए ज्योंहि पिटारे में हाथ डाला तो बिलार गुर्रायाः 'हूँऽऽऽ....!'
बच्चे बेचारे डर गये। अब क्या करें? बिना खाये ही मन मसोस कर रह गये। खेल में जी लगायें परंतु भूखे पेट.....। कब तक खेलें ? फिर पिटारे की तरफ निहारें, साहस बटोरकर पास जायें और हाथ लम्बा करें तो वह बिलार गुर्रायेः 'हूँऽऽऽ....! हूँऽऽऽ...!' बच्चे डर कर फिर वापस।
दिन बीत गया। सन्ध्या हुई। किसान खेत से लौटा। देखा तो बच्चों के मुख म्लान हैं। भूख और प्यास के मारे लोथपोथ हो रहे हैं। पूछने पर बच्चों ने बतायाः
"पिताजी ! पिटारे में बिलार घुस गया है। पूरा कब्जा जमा लिया है। हम कैसे खायें?"
किसान भी पिटारे के पास गया, देखा तो बिलार गुर्राने लगाः 'हूँऽऽऽ....! हूँऽऽऽ...!' किसान ने उठाया खरपिया। किसान के खरपिया उठाते ही बिलार छू हो गया।
ऐसे ही यह जीव मोह-ममता रूपी घी, गुड़ खाकर, अहंता रूपी मिठाइयाँ खाकर, 'तेरा-मेरा' रूपी रोटियाँ चबाकर इस देह रूपी पिटारे में बैठ जाता है। 'हूँऽऽऽ....! हूँऽऽऽ....!' गुर्राता है। 'मैं सेठ.... मैं साहब.... मैं अमथाभाई..... मैं छनाभाई.... मैं पिता..... मैं पति.....' ऐसे में मैं-मैं करता है।
गुरुदेवरूपी किसान आता है। साधकरूपी बच्चों से पूछता हैः "दुःखी क्यों हो भैया ?" साधकरूपी बच्चे बताते हैं- "आत्मानन्द की भूख लगी है। संसार की थकान ने मथ डाला है, थका दिया है। क्या करें ?"
गुरुदेव उठाते हैं ब्रह्मज्ञान का डण्डा और आत्मदृष्टि की चोट मारते हैं तब देहरूपी पिटारे से 'हूँऽऽऽ...! हूँऽऽऽ....!' करने वाला अहंरूपी बिलार कूदकर भाग जाता है। तब साधक आत्मानन्द का रसपान करके तृप्ति का अनुभव करते हैं। इसी अवस्था के लिए शंकराचार्यजी कहते हैं-
गलिते
देह-अध्यासे
विज्ञाते
परमात्मनि।
यत्र
यत्र मनो याति
तत्र तत्र
समाधयः।।
जब देहाध्यास गल जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ चित्त में समाधि का ही एहसास होता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
.......तो
दिल्ली दूर
नहीं
एक आदमी भागा-भागा जा रहा था। उसे जाना था दिल्ली लेकिन दिल्ली का पता नहीं था। एक बूढ़ा बैठा था उससे पूछाः "अरे जनाब ! दिल्ली कितनी दूर है ?"
"क्या मतलब ?" बूढ़े आश्चर्य व्यक्त किया।
"मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है?"
बुजुर्ग जमाने का खाया हुआ था, बुद्धिमान था। वह बोलाः "दिल्ली कितनी दूर है यह मैं बता सकता हूँ लेकिन मेरे दो शर्ते हैं।"
"दिल्ली कितनी दूर है यह बताने में दो शर्तों की क्या आवश्यकता है ?"
"हाँ, दो शर्तों पर ही बताऊँगा।" बूढ़ा दृढ़ रहा। आसपास में कोई था नहीं इसलिए इस आदमी को मानना पड़ा। उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दी।
बूढ़े ने कहाः "मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दो तब बताऊँगा कि दिल्ली कितनी दूर है।"
"पूछिये।"
"मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप दिल्ली में जाना कहाँ चाहते हो ? क्योंकि आठ मील पीछे दिल्ली को छोड़कर आर रहे हो। दूसरा प्रश्न यह है कि कितनी गति से जाना चाहते हो ? तुम एक घण्टे में भी पहुँच सकते हो और चार कदम चलकर पचास कदम चल सको उतनी देर बैठ जाओ तो पाँच-दस घण्टे लग जायेंगे। चलकर वापस ही आते रहो तो कभी नहीं पहुँचोगे। पहले चलकर, दौड़कर अपनी गति दिखा दो और जहाँ जाना चाहते हो उस स्थान का नाम बता दो तो कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए दिल्ली का रास्ता कितने घण्टे का है।"
शुक्रिया अदा करते हुए वह आदमी बोलाः "हाँ, आपकी शर्त बिलकुल ठीक है। अब तक मैं समझ रहा था कि आप बात को व्यर्थ में मचल रहे हो।"
"तुम दिल्ली को पीठ दिये खाड़ी हो। आगे ही आगे चलकर दिल्ली जाना चाहते हो तो नाक की सीध में चलते ही जाओ... चलते ही जाओ। जरा भी टेढ़े मेढ़े न होना। पूरी पृथ्वी का चक्कर काटकर दिल्ली पहुँच जाओगे। ऐसे भी दिल्ली जा सकते हो और वापस लौटना स्वीकार है तो मैं वह रास्ता भी बता दूँ। वापस लौट जाओगे तो दिल्ली जल्दी पहुँच जाओगे।"
ऐसे ही हमारी चेतना सुख के लिए कौन सी दिल्ली जाना चाहती है ? किस प्रकार जाना चाहती है ? कौन-सा सुख लेना चाहती है ? शाश्वत या नश्वर ? नश्वर सुख में यह जीवन हजारों जन्म नष्ट करता आया है। पदार्थों की आकांक्षा का कोई अन्त नहीं। पृथ्वी की तो सीमा है लेकिन पदार्थों की तृष्णा की कोई सीमा नहीं। पदार्थ यहाँ भी हैं, परलोक में भी हैं। पृथ्वी लोक के अलावा अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, भुर, भुवः, स्वः, जन, तप, महर्, स्वर्ग आदि अनेक लोक हैं। कितने लोकों के पदार्थों की आकांक्षा करोगे सुख के लिए ?
अगर तुम पीछे लौटना स्वीकार करते हो तो दिल्ली नजदीक हो जाती है। आगे ही बढ़ते जाओगे तो पृथ्वी का चक्कर काटकर वहाँ आओगे। विषय-वासना-विकारों में आगे बढ़ते हो तो चौरासी लाख योनियों का चक्कर काटकर फिर मनुष्य देह में आओगे। अगर वापस मुड़कर अभी 'दिले तस्वीरे है यार....' करके भीतर गोता लगाना चाहते हो तो दिल्ली दूर नहीं है, आत्मसुख पाना कठिन नहीं है। ॐ...ॐ....ॐ.....
ॐ शान्ति ! ॐ शान्ति !! ॐ शान्ति !!!
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
ध्यान
के क्षणों
में......
हमारा सूक्ष्म विकास हो रहा है। हमारा चित्त ॐकार की ध्वनि से परम शान्ति में, परमात्मा के आह्लादक स्वरूप में शान्त हो रहा है। हम महसूस कर रहे हैं कि हम शान्त आत्मा हैं। संकल्प-विकल्प मिट रहे हैं। चित्त की चंचलता शिथिल हो रही है। भ्रम दूर हो रहे हैं। सन्देह निवृत्त हो रहे हैं।
हमें पता भी नहीं चलता इस प्रकार गुरुदेव हमारी सूक्ष्मातिसूक्ष्म यात्रा करा रहे हैं... हमें पता भी नहीं चलता। अन्तवाहक शरीर पर चढ़े हुए कई जन्मों के संस्कार निवृत्त होते जा रहे हैं। वाणी के उपदेश से भी मौन उपदेश, मौन रहकर संकल्प से गुरुदेव की कृपा हमारे भीतर काम करती है। हमें पता भी नहीं होता कि मौन से कितना लाभ हो रहा है ! सदगुरु की कृपा कैसे कार्य करती है इसका पता हमें प्रारम्भ में नहीं चलता। गुरुकृपा हमारी नजदीक होकर भी काम करती है और हजारों मील दूर होकर भी काम करती है। गुरुदेव के बोलने पर तो उनकी कृपा काम करती ही है लेकिन मौन होने पर विशेष रूप से काम करती है। मौन के संकल्प की अपेक्षा बोलने का संकल्प कम सामर्थ्यवाला होता है। मौन में आत्म-विश्रान्ति की अपेक्षा बाहर के क्रिया-कलाप छोटे हो जाते हैं। सूक्ष्म पर्तें उतारने के लिए सूक्ष्म साधनों की जरूरत पड़ती है। यह घटना मौन में, शान्ति में घटती है। शिष्य जब आगे बढ़ता है तब ख्याल आता है कि जीवन में कितना सारा परिवर्तन हुआ।
शास्त्रों में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारणाख्य गुरु, परम गुरु (सदगुरु) आदि अनेक प्रकार के गुरु बताये गये हैं। इन सबमें परम गुरु अथवा सदगुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर 'श्री गुरुगीता' में कहते हैं-
जलानां
सागरो राजा यथा
भवति
पार्वति।
गुरुणां
तत्र
सर्वेषां
राजायं परमो
गुरुः।।
'हे पार्वती ! जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा है।'
जिन्हें सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, स्व-स्वरूप में जगे हैं, परहितपरायण हैं ऐसे सदगुरुओं की प्राप्ति अति कठिन है। ऐसे सदगुरु मिलते हैं तो हमारा आमूल परिवर्तन हो जाता है। देहाध्यास गलने लगता है। चित्त सत्पद में विश्रान्ति पाने लगता है।
जैसे माँ बालक को कभी पुचकारती है, कभी डाँटती है, कभी दुलार करती है। कभी किसी ढंग से कभी किसी ढंग से बच्चे का लालन-पालन करती है। वह माँ की अपनी प्रकृति है। गुरु, जो सदा जागृत स्वरूप में सजाग हैं ऐसे परम गुरु कभी किसी ढंग से कभी किसी ढंग से हमारा भीतरी आध्यात्मिक लालन-पालन करते हैं। उनका पूर्व आयोजित कोई कार्यक्रम नहीं होता साधक के लालन-पालन का कि यह करना है, वह करना है। जिस समय जिस प्रकार से, जिस कारण, क्रिया-कलाप से हमारा उत्थान होता होगा उस समय उस प्रकार का व्यवहार करेंगे और उस ढंग से हम पर बरसते हैं।
जैसे चतुर वैद्य अपने मरीज को अपनी निगाहों में रखता है और किस समय कौन-सी औषधि की आवश्यकता है यह ठीक से समझकर उसका इलाज करता है, ऐसे ही हमारे आन्तरिक स्वास्थ्य के लिए सदियों पुरानी लड़खड़ाती तंदरुस्ती के लिए, युगों पुरानी रूग्णता का निवारण करने के लिए परम गुरु भिन्न-भिन्न प्रकार की औषधि, उपचार, संयम-नियम का उपयोग करते हैं।
साधक की जिस समय जैसी प्रकृति होती है उस समय उसे गुरु उसी प्रकार के भासते हैं। हरेक साधक के अपने संस्कार होते हैं, योग्यता-अयोग्यता होती है, अपनी मान्यताएँ और पकड़े होती हैं। सबकी अपनी-अपनी देखने-सोचने की दृष्टि है। प्रारम्भ में हर साधक को अपने सदगुरु के प्रति अपने ढंग का आदर, मूल्य अथवा लड़खड़ाती श्रद्धा आदि होते हैं।
साधक जब प्रारम्भ में सदगुरु के श्रीचरणों में आता है उस समय उनको अपने ढंग से देखता है. उनकी योग्यता मापता है वह दृष्टि छोटी-सी होती है। साधक ज्यों-ज्यों संतत्व के नजदीक जाता है, ज्यों-ज्यों उस पर ब्रह्मवेत्ता सदगुरु की कृपा बरसती है, सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं साधक की बुद्धि शुद्ध होती है, साधक का अन्तःकरण शान्त होता है, तन और मन के विकार क्षीण होते हैं त्यों-त्यों वह साधक सदगुरु का महत्व समझता जाता है। जब साधक में रजोतमोगुण आ जाता है तो उसके जीवन में सदगुरु के सान्निध्य का और उपदेश का प्रभाव थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। जब सत्त्वगुण पुनः बढ़ता है तब उसके चित्त में सदगुरु तत्त्व का शुद्ध-विशुद्ध संचार निखरने लगता है।
चतुर साधक रजो-तमोगुण बढ़े नहीं उसकी सावधानी रखता है। अगर रजो-तमोगुण आ जाता है तो गुरु-निर्दिष्ट मार्ग से उस रजो-तमोगुण को दबाता है, क्षीण करता है।
गुरुकृपा अनिवार्य है साथ-साथ में साधक का पुरुषार्थ भी अनिवार्य है। सूर्यनारायण की कृपा अनिवार्य है खेती के लिए उतनी ही किसान की सजगता भी अनिवार्य है। किसान का परिश्रम और सावधानी अनिवार्य है, तभी खेती फलती है। ऐसे ही गुरु की कृपा आवश्यक है और साधक का साधन-भजन में उत्साह भी आवश्यक है, परिश्रम भी आवश्यक है तथा किया हुआ साधन-भजन, किया हुआ पुरुषार्थ, लायी हुई सात्त्विकता, की हुई आध्यात्मिक यात्रा कहीं बिखर न जाय इसकी सजगता भी साधक के लिए अनिवार्य है। सावधानी नहीं होगी तो गाय, बकरे आदि पशु उसे कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे। अथवा, साधक सिंचाई नहीं करेगा, खाद नहीं डालेगा तो खेत का लहलहाना मुश्किल हो जायेगा।
ऐ साधक ! तू अपने दिल के खेत में ब्रह्मविद्या की सिंचाई करते रहना जिससे आत्मज्ञान का फल लगे। यह सिंचाई तब तक करते रहना, सावधानी से बाड़ बनाते रहना, निगरानी करते रहना जब तक तुझे अमृतपद की प्राप्ति न हो जाय।
यह संसार कटीला मार्ग है। जैसे खेत हरा-भरा होते ही पशु आ जाते हैं, छोटे-मोटे जीवाणु भी लग जाते हैं तो किसान उसका इलाज करता है, बाड़ मजबूत करता है वैसे साधना के खेत को बिगाड़ने वाले प्रसंग भी आते हैं।
चार पैसे का अनाज प्राप्त करने के लिए किसान सब प्रकार की सावधानी रखता है तो हे साधक ! विश्वनियन्ता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना भैया ! तू भी अपनी संयम की बाड़ करना। साधना के भिन्न-भिन्न प्रकारों की सिंचाई करते रहना। साथ में देखना कि कहीं मान बड़ाई, सुख-दुःख के थपेड़े आकर तेरे साधनारूपी खेत को तो उजाड़ नहीं रहे हैं ! जब मौका मिले तब तू एकान्त में जाना। एकान्तवास करना, अल्प देखना, अल्प बोलना, अल्प सुनना। बाकी का समय अपनी साधनारूपी खेती की सिंचाई करना।
किसान घर छोड़कर खेत में ही खाट डाल देता है। ज्यों-ज्यों खेत उभरता है, दाने लगते हैं त्यों-त्यों किसान अपनी जिम्मेदारी अधिक महसूस करता है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक भले ही जिम्मेदारी अधिक महसूस करता है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक भले ही जिम्मेदारी महसूस न करे, साध्य को पाने के लिए सुरक्षा की बाड़ न करे मगर जो साधक कुछ चार कदम चल पड़े हैं, जिन्हें आत्मज्ञान का लगा हुआ फल महसूस हो रहा, जिन्हें शांति, प्रेम और आनन्द का एहसास हो रहा है, जिनका सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म साधना में प्रवेश हो रहा है, जो केवल बाहर के उपदेशों से ही नहीं लेकिन आन्तर मन से, आन्तर यात्रा से पवित्र हुए हैं ऐसे साधक घर से खटिया हटाकर खेत में खटिया डाल देते हैं। बाहर के लोकाचाररूपी घर से खटिया हटाकर ब्रह्मचिन्तनरूपी खेत में अपनी खटिया रख देना। आत्म-चिन्तन के खेत में, आत्म-प्रीति के खेत में खटिया धर देना। उठना भी खेत में, बैठना भी खेत में, चलना भी खेत में हो जाता है। खेत ज्यों लहलहाता है, फसल देने को तत्पर होता है त्यों किसान घर पर जाने का समय कम कर देता है। भोजन भी खेत में ही मँगा लेता है।
ऐसे ही हे साधक ! तू भी अपना खान-पान, रहन-सहन साधनामय बना दे। किसान चार पैसे के धान्य के लिए इतनी कुरबानी करता है तो ऐ मेरे प्यारे वत्स ! तू भी अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डनायक रूपी आत्मज्ञान के फल को पाने के लिए सजग रहना। क्योंकि ते री संपत्ति किसान की संपत्ति से बहुत ऊँची है। तेरा लक्ष्य किसान के लक्ष्य से अनन्त गुना ऊँचा है। इसलिए तू सावधान रहना। तू हजारों मील गुरु से दूर होगा तभी भी याद रखना, तेरे गुरु की कृपा तेरी सहाय रहेगी।
साधक का दिल पुकार उठाः
"हे गुरुदेव ! जब जब मैं निराश हुआ हूँ, थका हूँ, हताश हुआ हूँ तब-तब क्षणभर के लिए ही आपकी स्मृति लाकर थोड़ा सा ही भीतर से आपकी ओर आया हूँ तो तुरन्त मुझे आश्वनासन मिला है, मार्ग मिला है, प्रेम मिला है, पुचकार मिली है। गुरुदेव ! जब मैं फिसला हूँ, मनमानी की है, तब-तब तुम्हारी डाँट मिली है, तुम्हारी कड़ी नज़र दिखी है। जब-जब मैं तुम्हारी करुणा कृपा के अनुकूल चला हूँ तब वही कड़ी नज़र मीठी नज़र हुई है।
आपकी कड़ी नज़र भी हमारी गढ़ाई के लिए है और आपकी मीठी निगाहें भी हमारी गढ़ाई के लिए है। आपका बोलना भी हमारे कल्याण के लिए है और मौन होकर सूक्ष्म सहाय करना भी हमारे कल्याण के लिए है। अब इस प्रकार की अनुभूतियाँ हो रही हैं।
हे ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव ! हे आत्मारामी मेरे गुरुदेव ! आप न जाने किस-किस प्रकार से हमारा लालन-पालन करते हैं। आपका कोई पूर्व आयोजन नहीं लेकिन आपकी हर अदा, हर चेष्टा, हर अँगड़ाई, हर हिलचाल, चाहे फिर हाथ की चेष्टा हो चाहे नयनों की छटाएँ हो, चाहे बोलना हो, चाहे चुप होना हो, हम लोगों को न जाने किस-किस रूप में वह रहस्यमयी अँगड़ाईयाँ मिलती हैं ! नृत्य करता ब्रह्म हमारे जीवन में ब्रह्मभाव, अपनी ब्राह्मी अनुभूति का सिंचन करता है। उन ब्रह्मवेत्ताओं को एक क्षण बाद का भी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता है। सहज रूप से हमारी गढ़ाई करते हैं क्योंकि वे सहज स्वरूप में स्थित होते हैं। जिसने उनकी करीबी का एहसास किया है, जिसने अपने आपको उस परमात्मा में प्रतिष्ठित कर दिया है, अपने आपको उनमें मिला दिया है ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं की हर चेष्टा बड़ी रहस्यमयी होती है, प्रारम्भ में हम समझें चाहे न समझें, हम पा सकें, हजम कर सकें चाहे न कर सकें लेकिन उनकी हर चेष्टा बड़ी रहस्यमयी होती है। उनके चलने, फिरने, खाने, पीने, बोलने, बैठने के ढंग की छोटी से छोटी चेष्टा भी हमारे लिए नितान्त कल्याणकारी होती है। ऐसे जो परम गुरुलोग हैं, ब्रह्मवेत्ता सत्पुरुष हैं उनका बयान करने की ताकत हमारी जिह्वा में नहीं है।"
शिल्पी तो पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाता है लेकिन ब्रह्मगुरु सदगुरु तो विरोध करने वाले, प्रतिक्रिया करनेवाले मन्द बुद्धि के मनुष्य को ब्रह्म बनाते हैं। पत्थर में से मूर्ति बनाना आसान है क्योंकि पत्थर शंका नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, घर नहीं भागेगा। परंतु साधक तो घर भी भागेगा, दुकान की तरफ भी भागेगा। थोड़ा सुकर्म में चलेगा तो कुकर्म में भी भागेगा, चिन्ता में भी गिरेगा, अहंकार की ओर भी दौड़ेगा। कभी-कभी अपने गुरु के विषय में उसके चित्त में कैसे-कैसे विचार उठेंगे। न जाने कैसे-कैसे खिसकने के तरीके खोजेगा, कैसे-कैसे बचाव के तरीके खोजेगा। पत्थर की मूर्ति बनाना आसान है लेकिन इस कलियुग के चलते पुर्जे, चंचल चित्त रखने वाले मानव को महेश्वर के अनुभव में प्रतिष्ठित करना कितना कठिन है ! वह अति कठिन कार्य सहज में, स्वाभाविक, स्वनिर्मित मनोरंजन के भाव से परम गुरुओं के द्वारा संपन्न होता है।
ऐसे गुरुओं को समझने के लिए हे मेरे साधक! हे मेरे मन ! तू अथाह विश्वास, अथाह साधन-सामग्री, अथाह पुरुषार्थ, अथाह प्रेम से अथाह ईश्वर को पाने का दृढ़ निश्चय रखेगा तभी तू अथाह अनुभव के दाताओं को पहचान पायेगा, उनको समझ पायगा। जितना तू परमात्मा के लिए लालायित रहेगा उतना ही परमात्मा के प्यारों को पहचान पायगा, उनके निकट हो पायगा।
हे वत्स ! जो विकारों के प्यारे हैं, परिवर्तित पदार्थों के प्यारे हैं उनके प्रभाव से तू बचना। जो परमात्मा के प्यारे हैं और तुझे परमात्मा में प्रतिष्ठित बनाकर ही चैन की नींद लेना चाहते हैं, तुझे परमात्म-पद में विश्राम कराने के लिए तत्पर है उनको तू सहयोग करना। आनाकानी मत करना, इन्कार मत करना, शिकायत मत करना, छटकने के उपाय मत करना। तू फिसलने की अपनी पुरानी आदत को मत पकड़ना।
हे मेरे साधक ! हे भैया ! तेरा जीवन कितना कीमती है यह वे ब्रह्मवेत्ता जानते हैं और तू कितना तुच्छ चीजों में गिर रहा है यह भी वे जानते हैं। नन्हा-मुन्ना बालक अपनी विष्टा में खेलता है और सुख मानता है, अंगारों को पकड़ने के लिए लालायित होता है, बिच्छु और साँप से खेलने को लालायित होता है। उस अबोध बच्चे को पता ही नहीं कि अभी उनके विषैले डंक तुझे त्राहिमाम करा देंगे। हे साधक ! विषय-विकाररूपी जिस मल-मूत्र-विष्टा में खेलने को तत्पर है वे तुझे बीमार कर देंगे ! तेरी तन्दुरुस्ती को बिगाड़ देंगे। तू अंगारों से खेलने को जा रहा है ! तू तो मक्खन-मिश्री खाने को आया है लाला ! मिट्टी में, गोबर में खेलने को नहीं आया। चौरासी-चौरासी लाख जन्मों में तू इन गोबरों में, कंकड़-पत्थरों में खेला है, पति पत्नी के तुच्छ विकारी सम्बन्धों में तू खेला है, तू बकरा बना है, कई बार तुच्छ बकरियों के पीछे घूमा है। तूने न जाने कितने-कितने जन्मों में तुच्छ खेल खेले हैं। अब तू लाला के साथ खेल, राम के साथ खेल, अब तो तू शिवजी की नाईं समाधि लगाकर स्व के साथ खेल।
हे प्यारे साधक ! अगर तू अपने सदगुरु को खुश करना चाहता है तो उनकी आज्ञा मान और उनकी आज्ञा यही है कि वे जहाँ खेलते हैं उस परमात्मा में तू भी खेल। गुरु जहाँ गोता मारते हैं उसी में तू गोता मार भैया ! गुरुओं की जो समझ है वहाँ अपनी वृत्ति को पहुँचाने का प्रयास कर। इन नश्वर खिलौनों को पकड़कर कब तक सुख मनायगा ? कब तक अंगारों की ओर तू भागेगा ? करुणामयी माँ बच्चे को समझाती है, बच्चा रुक जाता है। माँ इधर-उधर जाती है बच्चा फिर अंगारों की ओर जाता है, चमकते अंगारों को खिलौना समझकर तू छू लेता है और चिल्ला उठता है। तब उसकी माँ को कितना दुःख होता है ! उस समय बालक को माँ की करुण स्थिति का पता नहीं। माँ उसे थप्पड़ मार देती है उस थप्पड़ में भी वात्सल्य भरा होता है, करुणा होती है। बच्चे का कान पकड़ना भी करुणा से भरा है। बच्चे का हाथ-पैर बाँधकर सजा देना भी प्यार और करुणा से प्रेरित होता है।
ऐ साधक ! तू जब गलत रास्ते जाता है, कंटकों और अंगारों में कदम रखता है तो सदगुरुरूपी माता-पिता कड़ी आँख दिखाते हैं, तू उसे महसूस भी करता होगा। 'गुरु रूठ गये हैं.... नाराज हो गये हैं.... पहले जैसे नहीं हैं....' ऐसा तुझे लगेगा लेकिन गौर से जाँच करेगा तो पता चलेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अंगारों की ओर गया, तू बिच्छू की ओर गया, तू सर्पों की ओर गया इसलिए वे पहले जैसे नहीं भासते। तू शंका-कुशंका में गया, अपनी अल्प मति से ब्रह्मवेत्ता गुरुओं को तौलने का दुस्साहस करने को गया इसलिये उन्होंने कड़ी आँख दिखायी है। वह भी तेरे कल्याण के लिए है। कड़ी आँख भी करुणा से भरी है, कृपा से भरी है, प्रेम से भरी है। कड़ी आँख भी पुकार से भरी है कि तू चल... चल....। तू रुक मत। आगे चल। गिर मत। सावधान हो। फिसल मत। साहस कर। गद्दार मत बन, सतर्क हो। कृतघ्न मत बन, कृतज्ञ हो।
इस प्रकार की उन आँखों से झलकती हुई ज्योति को तू समझा कर। 'गुरु नाराज हैं' ऐसा करके तू शिकायत मत कर, दुःखी होकर तू संसार के कचरे में अधिक मत कूदना। गुरु नाराज हैं तो उन्हें रिझाने का एक ही तरीका है कि तू फिर जहाँ भी हो, घर में हो, मन्दिर में हो, अरण्य में हो, तू फिर ध्यान करना शुरु कर दे, फिर से परमात्मा को प्यार करना शुरु कर दे। तू फिर गुरुओं के अनुभव में डूबना शुरु कर दे। गुरु की कड़ी आँख, गरम आँख उसी समय तुझे शीतल मिलेगी। गुरु उसी क्षण तुझ पर प्रसन्न दिखेंगे। दूसरे क्षण में तुझ पर बरसते हुए दिखेंगे। तू उनके अनुभव में मिटता जा। तू भी अपनी खटिया खेत में रखता जा। तू भी अपना समय साधनारूपी खेत में बिताता जा। तेरे खेत में गुरु की बुआई हुई है, सिंचाई हुई है। उन्हें तेरा खेत लहलहाता दिखता है।
किसान का बेटा खेत की रखवाली न करे, खेत में गधे घुस जाएँ तो बाप नाराज होता है। ऐसे ही हे साधक ! तेरे साधनरूपी खेत में तू अहंकार और वासनारूपी गधे-गधियों को मत घुसने देना। जड़ भोगवादी भैंसों को मत घुसने देना। मीठी-मीठी बात बोलकर तेरे अपने होकर तेरा समय खराब करने वाले मित्र-सम्बन्धी रूपी गायों को भी मत घुसने देना। उन टोलों को दूर से आते देखता है तो चतुर किसान पहले से ही डंडा उठाता है, टार्च उठाता है, आवाज लगाता है। ऐसे ही जब तेरे खेत में कोई प्रवेश करने लगे तो ॐ की गर्जना करना। 'नारायण.... नारायण...' रूपी टार्च का प्रकाश कर देना। गुरुमंत्र की छड़ी खटका देना। वे ढोर दूर से ही भाग जायें, पक्षी उड़ान ले लें। तेरा खेत चुगने आयें उससे पहले ही तू तैयारी रखना।... तो तेरा खेत बच जायगा।
किसान चार पैसे के धान्य की इतनी रखवाली करते हैं। उन किसानों को भी तू गुरु मान लिया कर इस समय।
ऐ वत्स ! तुझे पता नहीं लेकिन तेरे गुरु को पता है कि तू क्या हो सकता है। तुझमें कितना सारा भरा वह तेरे परम हितैषी जानते हैं। तेरे दोस्त तो तेरी तिजोरियाँ जाँचेंगे, तेरे रिश्ते-नाते तेरी तन्दुरुस्ती और रूप लावण्य निहारेंगे। लेकिन गुरुदेव जो तू है उसको निहारेंगे। जो तू है वह उन्हें दिखता है। उन्हें तुझमें जैसा दिखता है वैसा तू एक दिन अपने में खोज ले, वे खुश हो जायेंगे। वे तुम्हें पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तू पहुँचने का साहस कर। तू कहीं थकेगा तो वे तुझे सहाय करेंगे।यह सहाय वे दिखायेंगे भी नहीं, अन्यथा तू लाचार हो जायेगा। फिर हर कदम में उनकी सहाय चाहेगा। चलता रह। तू जहाँ थकेगा वहाँ सूक्ष्म रूप से सहयोग करते रहेंगे। तुझे पता तक नहीं चलने देंगे, वे इतने उदार हैं।
बस, ट्रेन या हवाई-जहाजवाले तो टिकट लेकर फिर तेरी मुसाफिरी कराते हैं। चालू गाड़ी में भी टिकट वसूल करते हैं लेकिन गुरुदेव तो पहुँचने के बाद भी टिकट नहीं माँगेगे।
भगवान सदाशिव कहते हैं कि ऐसे ब्रह्मवेत्ता सदगुरु सब गुरुओं में राजा हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
चिन्तन-कणिका
जब तक चित्त चंचल है और विषयों में सुखबुद्धिया रमणीयता बुद्धि बनी हुई है तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। मल और विक्षेप की निवृत्ति हुए बिना तथा चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान का अधिकार नहीं होता।
सबसे पहले वैराग्य होता है, फिर जिज्ञासा होती है। उसके पश्चात ज्ञान और प्रेम होता है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसे ज्ञान कहते हैं और आत्माकार वृत्ति का स्थिर रहना ही प्रेम है।
चिन्तन-स्मरण से सब कुछ हो जायेगा। चिन्तन का अभ्यास जितना बढ़ेगा, उतनी ही संसार से विरक्ति और भगवत्प्रेम की प्राप्ति होगी।
'मैं
सम्पूर्ण
प्रपंच से
भिन्न हूँ'-ऐसी
भावना करने से
चित्त की
साम्यावस्था
हो जाती है।
यही चित्त की
निर्विशेष
स्थिति है। इसका
काल अधिक
बढ़ने पर
चित्त विलीन
हो जाता है।
आसन और वृत्ति इन दोनों को ही स्थिर रखकर अभ्यास करना चाहिए। स्थिरसुखमासनम् – इस सूत्र के अनुसार स्थिर आसन रखकर ध्यान करना चाहिए। चेतनत्व की भावनापूर्वक इष्ट का ध्यान दस मिनट प्रतिदिन करने से फल प्रतीत होगा। तीस मिनट के अभ्यास से विशेष अवस्था प्रतीत होगी और एक घण्टा पैंतीस मिनट के अटूट ध्यान से देहानुसन्धान की निवृत्ति यानि समाधि हो जायेगी।
संकल्प-त्याग करने का अभ्यास करने से निश्चय ही भगवान मिल जाते हैं – इसका मैं ठेका लेता हूँ।
सुषुप्ति में जीवात्मा प्रकृति के अधीन रहता है और समाधि में जीवात्मा के अधीन प्रकृति रहती है। जब अफसर फौज के अधीन रहता है तो फौज उसे मार डालती है और जब अफसर के अधीन फौज रहती है तो अफसर चाहे जो कर सकता है।
इच्छा, क्रिया और ज्ञान इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध है। क्रिया रोक देने से आसन और प्राणायाम हो जाते हैं। इच्छा की निवृत्ति होने पर धारणा और ध्यान हो जाते हैं तथा इच्छापूर्वक क्रिया न करने पर क्रिया की शान्ति अर्थात् समाधि हो जाती है।
ज्ञान तो मानो एक अफसर है, जो सबका साक्षीमात्र है। करने धरने वाली इच्छा है और उसका व्यापार है।
ध्यान से ज्ञान होता है। ध्यान के बिना ज्ञान रह ही नहीं सकता।
ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर निद्रा कम हो जाती है, ध्यानाभ्यासी पुरुष एक डेढ़ घण्टा सोकर भी रह सकता है। इसी से ध्यान स्वाभाविक हो जाता है तो फिर आराम की इच्छा नहीं रहती। जब चित्त से विक्षेप निकल जाये तभी ध्यान पूरा हुआ समझो।
कुछ भी हो, बिना संयम के कुछ भी नहीं हो सकता। संयम के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संयमरहित जीवन व्यर्थ है। दृढ़ अभ्यास की निरन्तर आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से कुछ नहीं होता। सावधान चित्त से निरन्तर अभ्यास में लगे रहे। यह पुस्तकी विद्या नहीं, अनुभव का पथ है।
दृष्टि से सृष्टि बनाना वेदान्त है और सृष्टि से दृष्टि हटाना योग या उपासना है।
तत्त्वज्ञान के लिए कुछ बनाना-बिगाड़ना नहीं होता। द्वैत ज्यों का त्यों बना रहता है और अद्वैत का बोध हो जाता है। जैसे सोने के आभूषण बने रहते हैं और उनमें सोने की अखण्डैकरसता का बोध हो जाता है। इसके लिए सोने को तोड़ना-फोड़ना नहीं पड़ता।
तुम्हारा चित्त जितना भगवान में लगेगा उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। संसार-चिन्तन से तुम जितने ही उपराम होंगे, संसार तुमसे उतना ही अधिक प्रेम करेगा। जब भगवान से पूर्ण प्रेम होगा तो संसार तुम्हारे अधीन होगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ