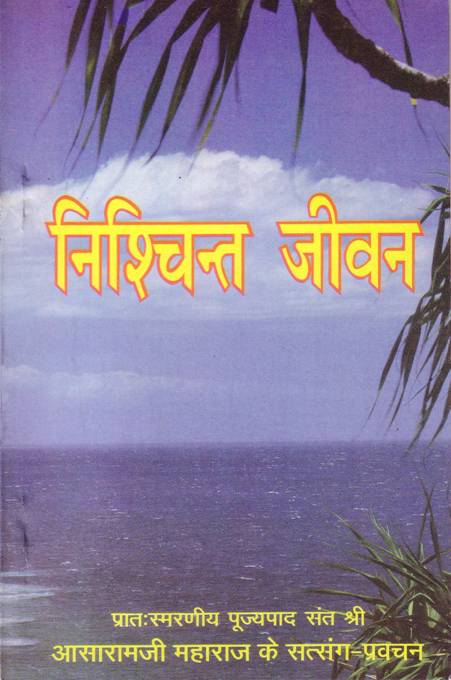
प्रातःस्मरणीय
पूज्यपाद संत
श्री
आसारामजी
बापू के
सत्संग-प्रवचन
निश्चिन्त
जीवन
पूज्य बापू का पावन सन्देश
हम धनवान होगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं इसमें शंका हो सकती है परंतु भैया ! हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है? विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है परंतु इस जीवन की गाड़ी छूटने का कोई निश्चित समय है?
आज तक आपने जगत में जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है.... आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे, प्यारे भैया ! वह सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जायेगा, जाना अनजाना हो जायेगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जायेगी।
अतः सावधान हो जाओ। अन्तर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, निजस्वरूप के अगाध आनन्द को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो।
जागो.... उठो.... अपने भीतर सोये हुए निश्चयबल को जगाओ। सर्वदेश, सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीन-हीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके।
सदा स्मरण रहे कि इधर-उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना-काल में आत्मचिन्तन में लगाओ और व्यवहार-काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शान्त वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवन्त एवं प्रसन्न रहो। जीवमात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो। दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग एवं सत्साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदान्त से पुष्ट एवं पुलकित करो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
निवेदन
आत्मवेत्ता, जीवन्मुक्त, प्राणीमात्र के परम सुहृद संतों के दिव्य अनुभूतों एवं गीता, रामायण, उपनिषद व पुराणों के पावन प्रसंगों की लेती हुई.... भक्तों-साधकों को अपने प्रसाद में सराबोर करने वाली...... 'मधुर-मधुर नाम हरि ॐ' के संकीर्तन नाद से हर दिल में ईश्वरीय मस्ती जगाने वाली सत्संग-सरिता को लिपिबद्ध करके आपके करकमलों में रखने का सौभाग्य समिति को प्राप्त कर रहा है।
इसमें विवेक-वैराग्य को बढ़ाकर आत्मा परमात्मा के अभिमुख कराने वाले भिन्न-भिन्न प्रवचन और प्रसंग हैं। कहीं कहीं अत्यंत सूक्ष्म तत्त्वज्ञान है तो कहीं कहीं सारगर्भित, सहज समझ में आ जाय ऐसे इशारे हैं।
इस वेदवाणी को, अनुभववाणी को एक बार ही पढ़कर रख नहीं देना है अपितु बार-बार इसका पठन करके नये नये भाव और वेदान्त की सूक्ष्मता समझकर संसार में जीवन्मुक्तावस्था पाने की सामग्री और प्रेरणा लेना है।
कृपया इस पुस्तक का बार-बार पठन-मनन आप भी करें और दूसरों को भी इसमें सहभागी बनाकर पुण्य प्राप्त करें।
अस्तु.....।
विनीत,
श्रीयोग
वेदान्त सेवा
समिति।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सर्व बन्धनों
से मुक्ति का उपाय
धर्मानुष्ठान
और शरीर-स्वास्थ्य
कुकर्म
के फल से कोई बच
नहीं सकता
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
चिन्ता से निश्चिन्तता की ओर
अन्तःकरण की दो धाराएँ होती हैं- एक होती है चिन्ता की धारा और दूसरी होती है चिन्तन की धारा, विचार की धारा।
जिसके जीवन में दिव्य विचार नहीं है, दिव्य चिन्तन नहीं है वह चिन्ता की खाई में गिरता है। चिन्ता से बुद्धि संकीर्ण होती है। चिन्ता से बुद्धि का विनाश होता है। चिन्ता से बुद्धि कुण्ठित होती है। चिन्ता से विकार पैदा होते हैं।
जो निश्चिन्त हैं वे दारू नहीं पीते। जो विचारवान हैं वे फिल्म की पट्टियों में अपना समय बरबाद नहीं करते। सौ वेश्याओं के पास जाना इतना बुरा नहीं जितना फिल्म में जाना बुरा है ऐसा स्वामी माधवतीर्थजी ने लालजी महाराज को कहा। लालजी महाराज पूर्व जीवन में नाटक के रसिया थे। नाटक देखने के लिए दो पाँच दस मील चलना पड़े तो भी चलकर नाटक देख लेते। जब कमाने लगे तब अपने पैसों से दूसरों को भी नाटक दिखाने की वृत्ति बनी रहती। लेकिन संत के दो वचन लग गये, सदविचार उत्पन्न हो गया तो जीवन परिवर्तन हो गया। अभी आपके सामने ऊँचे आसन पर आदर योग्य हो रहे हैं। यह विचार का ही तो प्रभाव है।
स्वामी माधवतीर्थ ने कहा कि सौ वेश्याओं के पास जाना उतना हानिकारक नहीं जितना फिल्म में जाना हानिकारक है। वेश्या दिखेगा कि हानि है लेकिन फिल्म के गहरे संस्कार में पता ही नहीं चलता कि हानि हो रही है। फिल्म में जो दिखता है वह वास्तव में सच्चा नहीं है फिर भी हृदय में जगत की सत्यता और आकर्षण पैदा कर देता है। फिर हृदय में अभाव खटकता रहेगा। अभाव खटकता रहेगा तो चिन्ता के शिकार बन जाएँगे। चलचित्र विचार करने नहीं देंगे, इच्छा बढ़ा देंगे। हल्की सांसारिक इच्छाओं से आदमी का विनाश होता है।
विचारवान पुरूष अपनी विचारशक्ति से विवेक-वैराग्य उत्पन्न करके वास्तव में जिसकी आवश्यकता है उसे पा लेगा। मूर्ख आदमी जिसकी आवश्यकता है उसे समझ नहीं पायेगा और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको आवश्यकता मानकर अपना जीवन खो देगा। उसे चिन्ता होती है कि रूपये नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, गाड़ी नहीं होगी तो कैसे चलेगा, अमुक वस्तु नहीं होगी तो कैसे चलेगा। उसे लगता है कि अपने रूपये हैं, अपनी गाड़ी है, अपना साधन है, हम स्वतन्त्र हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है तो परतन्त्र हो गये..... रूपये पैसे नहीं हैं तो परतनत्र हो गये।
उन बेचारे मन्द बुद्धिवाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि रूपये पैसे से स्वतन्त्रता नहीं आती। रूपये पैसे हैं तो आप स्वतन्त्र हो गये तो क्या रूपये-पैसों की परतंत्रता नहीं हुई ? गाड़ी की, बंगले की, फ्लेट की, सुविधाओं की परतंत्रता हुई। इन चीजों की परतंत्रता पाकर कोई अपने को स्वतंत्र माने तो यह नादानी के सिवाय और क्या है ? वास्तव में रूपये-पैसे, गाड़ी, मकान आदि सब तुम्हारे शरीर रूपी साधन के लिए चाहिए। साधन के लिए साधन चाहिए। तुम्हारे लिये इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम वास्तविक स्वरूप में परम स्वतंत्र हो। तुमको अपने ज्ञान की आवश्यकता है। अपना ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तुम अपने साधन (शरीर) की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता मान लेते हो। साधन की आवश्यकता भी उतनी नहीं जितनी तुम मानते हो। आवश्यकताएँ मन के नखरे हैं। शरीर साधन है। साधन की जो नितान्त आवश्यकता है वह आसानी से पूरी होती है। जो बहुत जरूरी आवश्यकता है वह बहुत आसानी से पूरी होती है।
जैसे, पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता है। उसमें ज्यादा परिश्रम नहीं है कमाने में और रोटी बनाने में। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने में और पचाने में परिश्रम है।
अन्न से ज्यादा जरूरत है जल की। जल प्राप्त करने में उतना भी परिश्रम नहीं है जितना अन्न प्राप्त करने में होता है। जल से भी ज्यादा आवश्यकता है हवा की। जीने के लिए हवा के बिना नहीं रह सकते। ऐसी मूल्यवान हवा प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम करते हो ? कुछ नहीं। हवा तो सदा सर्वत्र मुफ्त में उपलब्ध है।
तुम्हारे शरीररूपी साधन को जो आवश्यकता है वह पूरी करने की व्यवस्था शरीर देने वाले दाता, सृष्टिकर्त्ता ईश्वर ने की है।
तुलसीदास जी कहते हैं-
पहले
रच्यो
प्रारब्ध
पीछे दियो
शरीर।
तुलसी
चिन्ता क्यों
करे प्रेम से
भजो रघुवीर।।
पहले इस देह का प्रारब्ध बना है, बाद में देह बनी है। तुम्हारे इस साधन की जो आवश्यकता है उसकी पहले व्यवस्था हुई है, बाद में देह बनी है। अगर ऐसा न होता तो जन्मते ही तैयार दूध नहीं मिलता। उस दूध के लिए तुमने-हमने कोई परिश्रम नहीं किया था। माँ के शरीर में तत्काल दूध बन गया और बिल्कुल बच्चे के अनुकूल। ऐसे ही हवाएँ हमने नहीं बनाईं, सूर्य के किरण हमने नहीं बनाये, प्राणवायु हमने नहीं बनाया लेकिन हमारे इस साधन को यह सब चाहिए तो सृष्टिकर्त्ता ने पहले बनाया। अतः इस शरीररूपी साधन की जो नितान्त आवश्यकता है उसके लिए चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सृष्टिकर्त्ता की सृष्टि में आवश्यकता पूरी करने की व्यवस्था है। अज्ञानजनित इच्छा-वासनाओं का तो कोई अन्त ही नहीं है। वे ही भटकाती हैं सबको।
इच्छाएँ हमारी बेवकूफी से पैदा होती हैं और आवश्यकताँ सृष्टिकर्त्ता के संकल्प से पैदा होती हैं। शरीर बना कि उसकी आवश्यकताएँ खड़ी हुईं। सृष्टिकर्त्ता का संकल्प है कि तुम मनुष्य जन्म पाकर मुक्त हो जाओ। अगर तुम अपने को सृष्टिकर्त्ता के संकल्प से जोड़ दो तो तुम्हारी मुक्ति आसानी से हो जाएगी। तुम अपनी नई इच्छाएँ बनाकर चिन्ता करके अपने को कोसते हो तो तुम कर्म के भागी बन जाते हो।
जैसे, किसी ने गुनाह किया और जेल में है। चार साल की सजा हुई है। अब जेल का जैसा नियम है ऐसा वह चलता रहे तो चार साल कट जाएँगे, वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह जेल में गड़बड़ी करे, तूफान करे, अपराध करे तो और सजा बढ़ जाएगी। ऐसे ही जीव इस संसाररूपी कारावास में आये हैं, कोई मनुष्य होकर आया है कोई पशु होकर आया है कोई पक्षी होकर। जो लोग समझते हैं कि हम संसार में चार दिन सुख भोगने के लिए आये हैं उन हतभागियों को पता ही नहीं कि संसार सुख लेने की जगह नहीं है। सुख लेगा कौन ? यह जरा खोजो। अपने शरीररूपी साधन को तुम सुखी करना चाहते हो ? साधन जड़ है। उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम्हें अपना पता नहीं। तुम्हारी कल्पना ही है कि हम सुखी हो जाएँ। यही कारण है कि एक वस्तु पर किसी की कल्पना बन जाएः 'यह मिल जाए तो मैं सुखी....' तो उस कल्पनावाले को वह वस्तु सुखद भासती है। वही वस्तु दूसरे को सुखद नहीं भासती। शराबी, कबाबी, मांसाहारी को ये तुच्छ चीजें सुख देती हैं जबकि सदाचारी को ये सुख नहीं देती। तो मानना पड़ेगा कि वस्तुओं में सुख नहीं है, हमने कल्पना का सुख बनाया है।
कल्पना का सुख और कल्पना का दुःख बना बनाकर आदमी चिन्ता के घटीयंत्र में घूमता रहता है। इस प्रकार अपना सारा आयुष्य पूरा कर देता है।
चिन्ता उन्हीं की होती है जिनके पास ठीक चिन्तन नहीं है। शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए पुरूषार्थ करना हाथ-पैर चलाना, काम करना, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन इसके पीछे अन्धी दौड़ लगाकर अपनी चिन्तनशक्ति नष्ट कर देना यह बहुत हानिकारक है।
निश्चिन्त जीवन कैसे हो ?
निश्चिन्त जीवन तब होता है जब तुम ठीक उद्यम करते हो। चिन्तित जीवन तब होता है जब तुम गलत उद्यम करते हो। लोगों के पास है वह तुमको मिले इसमें तुम स्वतन्त्र नहीं हो। तुम्हारा यह शरीर अकेला जी नहीं सकता। वह कइयों पर आधारित रहता है। तुम्हारे पास जो है वह दूसरों तक पहुँचाने में स्वतन्त्र हो। तुम दूसरे का ले लेने में स्वतंत्र नहीं हो लेकिन दूसरों को अपना बाँट देने में स्वतंत्र हो। मजे की बात यह है कि जो अपना बाँटता है वह दूसरों का बहुत सारा ले सकता है। जो अपना नहीं देता और दूसरों का लेना चाहता है उसको ज्यादा चिन्ता रहती है।
लोग शिकायत करते हैं किः 'हमको कोई पूछता ही नहीं... हमको कोई प्रेम नहीं देता..... हमारा कोई मूल्य नहीं है...... हमारे पास कुछ नहीं है.....।'
तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम शरीर तो है। तुम्हारे पास मन तो है। रूपये-पैसे नहीं हैं चलो, मान लिया। लेकिन तुम्हारे पास शरीर, मन और चिन्तन है। तुम औरों की भलाई का चिन्तन करो तो और लोग तुम्हारी भलाई का चिन्तन किए बिना नहीं रहेंगे। तुम्हारे पास जो तनबल है, मनबल है, बुद्धिबल है उनको परहित में खर्च डालो। औरों का लेने में तुम स्वतन्त्र नहीं हो लेकिन अपना औरों तक पहुँचाने में स्वतन्त्र हो। अपना औरों तक पहुँचाना शुरू किया तो औरों का तुम्हारे तक अपने आप आने लग जाएगा।
होता क्या है ? अपना कुछ देना नहीं, औरों का ले लेना है। काम करना नहीं और वेतन लेना है। मजदूर को काम कम करना है और मजदूरी ज्यादा लेना है। सेठ को माल कम देना है और मुनाफा ज्यादा करना है। नेता को सेवा कम करना है और कुर्सी पर ज्यादा बैठना है। सब भिखमंगे बन गये हैं। देने वाला दाता कोई बनता नहीं, सब भिखारी बन गये। इसलिए झगड़े, कलह, विरोध, अशान्ति बढ़ रही है।
परिवार में भी ऐसा होता है। सब सुख लेने वाले हो जाते हैं। सुख देने वाला कोई होता नहीं। मान लेने वाले हो जाते हैं, मान देने वाला कोई नहीं होता। खुद जो दे सकते हैं वह नहीं देना चाहते हैं और लेने के लालायित रहते हैं। सब भिखमंगों के ठीकरे टकराते हैं।
वास्तव में मान लेने की चीज नहीं, सुख लेने की चीज नहीं, देने की चीज है। जो तुम दे सकते हो वह अगर ईमानदारी से देने लग जाओ तो जो तुम पा सकते हो वह अपने आप आ जाएगा।
तुम प्रेम पा सकते हो, अमरता की अनुभूति पा सकते हो, शाश्वत जीवन पा सकते हो। तुम्हारे पास जो नश्वर है वह तुम दे सकते हो। नश्वर देने की आदत पड़ते ही नश्वर की आसक्ति मिट जाती है। नश्वर की आसक्ति मिटते ही शाश्वत की प्रीति जगती है। शाश्वत कोई पराई चीज नहीं है। तुम सब कुछ दे डालो फिर भी तुम इतने महान् हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। तुम बाहर की दुनियाँ से सब कुछ ले लो लेकिन तुम्हारा शरीर इतना तुच्छ है कि आखिर कुछ उसके पास रह नहीं सकता। यह बिल्कुल सनातन सत्य है।
अगर तुम भक्त हो तो भावना ऐसी करो कि सब भगवान का है। सबसे भगवान के नाते व्यवहार करो। अगर तुम ज्ञानमार्ग में हो तो विचार करो कि सब प्रकृति का है, सब परिवर्तनशील है। संसार और शरीर दोनों एक है। शरीर को संसार की सेवा में लगा दो।
शरीर संसार के लिए है। एकान्त अपने लिए है और प्रेम भगवान के लिए है। यह बात अगर समझ में आ जाय तो प्रेम से दिव्यता पैदा होगी, एकान्त से सामर्थ्य आयेगा और निष्कामता से बाह्य सफलताएँ तुम्हारे चरणों में रहेंगी।
शमा जलती है परवानों को आमंत्रण नहीं देती। परवाने अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जीवन अगर परहित के लिए खर्च होता है तो तुम्हारे शरीर रूपी साधन के लिए आवश्यकताएँ, सुविधाएँ अपने आप आ जाती हैं। लोग नहीं देंगे तो लोकेश्वर उनको प्रेरित करके तुम्हारी आवश्यकताएँ हाजिर कर देंगे।
जिसने
बाँटा उसने
पाया। जिसने
सँभाला उसने गँवाया।
तालाब और नदी के बीच बात चली। तालाब कहता हैः
"पगली ! कलकल छलछल करती, गाती गुनगुनाती भागी जा रही है सागर के पास। तुझे वह क्या देगा ? तेरा सारा मीठा जल ले लेगा और खारा बना डालेगा। जरा सोच, समझ। अपना जल अपने पास रख। काम आयगा।"
नदी कहती हैः "मैं कल की चिन्ता नहीं करती। जीवन है बहती धारा। बहती धारा को बहने ही दो।"
तालाब ने खूब समझाया लेकिन सरिता ने माना नहीं। तालाब ने तो अपना पानी संग्रह करके रखा। ऐसे ऐसे मच्छों को, मगरों को रख दिये अपने भीतर कि कोई भीतर आ ही न सके, स्नान भी न कर सके, डर के मारे पानी पीने भी न आ सके।
कुछ समय के बाद तालाब का बँधियार पानी गंदा हुआ, उसमें सेवार हो गई, मच्छर बढ़ गये, गाँव में मलेरिया फैल गया। गाँव के लोगों ने और नगर पंचायत ने मिलकर तालाब को भर दिया।
उधर सरिता तो बहती रही। सागर में अपना नाम-रूप मिटाकर मिल गई। अपने को मैं सागर हूँ ऐसा एहसास करने लगी। उसी सागर से जल उठा, वाष्प बना, वर्षा हुई और नदी ताजी की ताजी बहती रही। 'गंगे हर.... यमुने हर.... नर्मदे हर...' जय घोष होता रहा।
गंगा ने कभी सोचा नहीं किः साधु पुरूष आयें तो उन्हें शीतल जल दूँ और सिंह आये तो उसे जहर डालकर दूँ। वह तो बहती जा रही है। सिंह आये तो भी शीतल जल पी जाए और साधु आये तो भी शीतल जल में नहा ले, जल पी ले।
जीवन भी एक ऐसी अमृतधारा हो कि कोई दुष्ट से दुष्ट हो, चाण्डाल से चाण्डाल हो और सज्जन से सज्जन हो, तुम्हारे द्वारा उन दोनों की कुछ न कुछ सेवा हो जाती है तो तुमने कर्जा चुका दिया। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सेवा का बदला वे लोग ही दें। क्या ईश्वर के हजार-हजार हाथ नहीं हैं देने के लिए ? लाखों-लाखों दिल उस परमात्मा के नहीं हैं क्या ?
त्याग से, प्रसन्नता से एकान्त से अदभुत विकास होता है। साधना काल में एकांतवास अत्यन्त आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने छः साल तक उरणावलि अरण्य में एकान्तवास किया था। जिसस भारत में आकर सत्रह साल तक एकान्तवास में रहे थे। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने नर्मदा तट पर सदगुरू के सान्निध्य में एकान्तवास में रहकर ध्यानयोग, ज्ञानयोग इत्यादि के उत्तुंग शिखर सर किये थे। उनके दादागुरू एवं सदगुरू गौड़पादाचार्य ने एवं गोविन्दपादाचार्य ने एकान्त-सेवन किया था। अपनी वृत्तियों को इन्द्रियों से हटाकर अन्तर्मुख की थी।
कभी कभी अपने को बन्द कमरे में कुछ दिन तक रखो। प्रारंभ में तुम्हें अकेले रहने में सुविधा न होगी। पहले दो चार घण्टे ही रहो। आत्म-विचार को बढ़ाओ। आत्म-विचार को बढ़ाने वाले पुस्तक पढ़ो। जप करो। प्राणायाम करो। योगासन करो। मौन रखो। मौन से शक्तियों का विकास होता है। साधक ऊपर उठता है। उसकी तपश्चर्या से, मौन से, एकान्त-सेवन से, बन्द कमरे में अज्ञात रहने से सुषुप्त शक्तियाँ विकसित होती हैं। विरोध करने वाले भी उस साधक का आदर करने लग जाते है। अन्न जल, आजीविका की तकलीफ होती थी वह आसानी से दूर हो जाएगी। पुण्य बढ़ेगा।
आध्यात्मिक मार्ग में देखा जाए तो तुम्हारे शत्रु वास्तव में तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। बाहर से मित्र दिखते हुए मित्र तुम्हारे गहरे शत्रु हैं। वे तुम्हारा समय खा जाते हैं और तुम्हारी आध्यात्मिक पूँजी चूस लेते हैं, तुमको भी पता नहीं चलता। उनको भी पता नहीं होता कि हम अपने मित्र की आध्यात्मिक पूँजी बरबाद कर रहे है। वे कुछ न कुछ व्यावहारिक काम, सामाजिक काम ले आते हैं, बातें ले आते हैं और तुम्हें बलात् उनके साथ सहमत होना पड़ता है। इन कार्यों में, प्रवृत्ति में तुम्हें संसारी लोगों का संपर्क होता है।
संसारी लोग की और साधक की दिशा बहुत अलग होती है। संसारी के पास जो जो संसार के पद-पदार्थ होते हैं उन्हें बढ़ाने की एवं भविष्य के हवाई किले बाँधने की इच्छा होती है। साधक अपने पास जो है उसको सत्कार्य में लगाने के लिए सोचता है और भविष्य में हरिमय हो जाने की इच्छा करता है।
साधक का लक्ष्य परमात्मा है और संसारी का लक्ष्य तुच्छ भोग है। संसारी की धारा चिन्ता के तरफ जा रही है और साधक की धारा चिन्तन के तरफ जा रही है।
छोटे विचारवाले तुम्हारे मित्र, जिनको संसार प्रिय है, जिनको संसार सच्चा लगता है, जो देह को मैं मान कर देह को सुखी करने में लगे हैं, जो सोचते हैं कि इतना किया है और इतना करके दिखाना है, इतना पाया है और इतना पाकर दिखाना है, इतना देखा है, इतना और देखना है ऐसे संसारी आकर्षणवाले लोगों के संपर्क में जब तुम आ जाओगे तब तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी विचार-शक्ति, तुम्हारी आध्यात्मिक पूँजी, महीनों की साधना की कमाई अथवा अगले जन्मों की पुण्याई तुम बिखेर डालोगे।
जब आध्यात्मिक पूँजी बिखर जाती है तब साधक बेहाल हो जाता है। जिसस जब भारत के योगियों से योग के रहस्य सीखकर, आध्यात्मिक पूँजी वाले बनकर अपने देश में गये तब लोगों ने उनको माना, पूजा और जब जिसस लोक-सम्पर्क में अधिक आये, आत्म-विचार, एकान्त-सेवन और आत्म-मस्ती छूट गई फिर पूजा करने वाले उन्हीं लोगं ने जिसस को क्रॉस पर चढ़ाया। तब जिसस के उदगार निकलेः
“O my God ! I lost my energy.” ( हे मेरे प्रभु ! मैंने अपनी शक्ति खो दी।)
कहा जाता है कि जिसस का पुनरूत्थान हुआ। वे एकान्त में चले गये। अंतिम समय में एकान्त अज्ञातवास में रहे इसलिए आज पूजे जा रहे हैं।
वे ही महापुरूष बड़ा काम कर गये हैं, उन्होंने ही जगत का कल्याण किया है जिन्होंने एकान्त-सेवन किया है, जिन्होंने आत्म-विश्लेषण किया है, जिन्होंने तुच्छ वस्तुओं का आकर्षण छोड़कर, तुच्छ वस्तुओं की चिन्ता छोड़कर सत्य वस्तु का अनुसंधान किया है। उन्होंने ही जगत की सच्ची सेवा की है। उन्हीं की सिद्धान्त आज तक हम पर राज्य कर रहे हैं। उन महापुरूषों के संकल्प, उन महापुरुषों के आदर्श, उन महापुरूषों के चित्र हमारे दिल पर आज भी राज्य कर रहे हैं।
जिन्होंने 'तू-तू..... मैं-मैं....' करके डण्डे के बल से अपना अहंकार पोसने के लिए राज्य किया है उनकी सत्ता हमारे दिल पर राज्य नहीं कर सकती। जिन महापुरूषों की मधुर स्मृति हमारे हृदय सिंहासन पर आरूढ़ है वे चाहे वेदव्यास हों चाहे वशिष्ठजी महाराज हों, वल्लभाचार्य हों चाहे रामानुजाचार्य हों, एकनाथ जी हों चाहे नामदेव हों, संत ज्ञानेश्वर हों चाहे तुकारामजी हों, शुकदेवजी हों चाहे अष्टावक्र मुनि हों, उनका चित्र दिखे या कथा-प्रसंग सुनने में आये या सिद्धान्त की बात मिले, हमारे दिल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को चिन्तन के द्वारा महान् बनाया था।
विचार अपने विषय में होता है और चिन्ता दूसरे के विषय में होती है। अपने विषय में कभी चिन्ता नहीं होती। यह बिल्कुल नई बात लगेगी। अपने विषय में कभी चिन्ता नहीं होगी, अपने विषय में कभी संदेह नहीं होगा, अपने विषय में कभी भय नहीं होगा, अपने विषय में कभी शोक नहीं होगा। जब भय होता है, शोक होता है, चिन्ता होती है तो पर के विषय में होती है।
तुम अपने आप हो आत्मा, दूसरा है शरीर। स्व है आत्मा और पर है शरीर। शरीर के लिए सन्देह रहेगा कि यह शरीर कैसा रहेगा ? बुढ़ापा अच्छा जाएगा कि नहीं ? मृत्यु कैसी होगी ? लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा कोई सन्देह, चिन्ता या भय नहीं होगा। आत्म-स्वरूप से अगर मैं की स्मृति हो जाए तो फिर बुढ़ापा जैसे जाता हो, जाय.... जवानी जैसे जाती हो, जाय.... बचपन जैसे जाता हो, जाय..... मेरा कुछ नहीं बिगड़ता।
दुनियाँ के सब लोग मिलकर तुम्हारे शरीर की सेवा में लग जाएँ फिर भी तुम्हारे स्व में कुछ बढ़ौती नहीं होगी। तुम्हारा विरोध में सारा विश्व उल्टा होकर टँग जाय फिर भी तुम्हारे स्व में कोई कटौती नहीं होगी, कोई घाटा नहीं होगा। ऐसा विलक्ष्ण तुम्हारा स्व है। इतने तुम स्वतन्त्र हो। संसार के सारे देशों के प्रेसिडेन्ट, प्रमुख, राष्ट्रपति, सरमुखत्यार, सुल्तान, प्राईम मिनिस्टर सब मिलकर एक आदमी की सेवा में लग जाएँ उसको सुखी करने में लग जाएँ फिर भी जब तक वह आदमी स्व का चिन्तन नहीं करता, स्व का विचार नहीं करता, आत्म विचार नहीं करता तब उसका दुर्भाग्य चालू रहता है। उपर्युक्त सब लोग मिलकर एक आदमी को सताने लग जाए और वह आदमी अगर आत्म-स्वरूप में सुप्रतिष्ठित है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। उसके शरीर को चाहे काट दें या जला दें फिर भी वह आत्मवेत्ता अपने को कटा हुआ या जला हुआ मानकर दुःखी नहीं होगा। वह तो उस अनुभव पर खड़ा है जहाँ.....
नैनं
छिदन्ति
शस्त्राणि
नैनं दहति
पावकः।
न
चैनं
क्लेदयन्त्याप
न शोषयति
मारूतः।।
'आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती।'
(भगवद् गीताः 2.23)
शुकदेवजी और जड़भरत जी जैसे महापुरूषों को कई लोगों ने सताया लेकिन उनका तिनका तक बिगड़ा नहीं क्योंकि वे चिन्तन के बल से स्व में.... आत्मा में प्रतिष्ठित थे।
अभी विनाशकारी अणुबम इतनी मात्रा में बने हैं कि पूरी मानव जात उनसे सात बार मर सकती है। इस पृथ्वी पर मानो साढ़े तीन अरब आदमी हैं तो पच्चीस अरब आदमी मर सकें, उतने अणुबम बनाये गये हैं। आदमियों की शारीरिक आकृतियाँ मरेंगी, मिटेंगी लेकिन आदमियों का चैतन्य जो स्व है, आत्मा है उसको तो ये सब अणुबम मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। सब के सब अणुबम एक आदमी पर खर्च कर दिये जाएँ फिर भी उस आदमी की आत्मा को तनिक भी हानि नहीं हो सकती।
आपका 'स्व' इतना स्वतन्त्र है और शरीर 'पर' है। बेवकूफी से क्या हो गया है कि 'स्व' का पता नहीं और 'पर' को 'स्व' मान लिया..... शरीर को 'मैं' मान लिया।
व्यवहार में कहते हैं, 'मेरा हाथ....' तो तुम हाथ नहीं हो, हाथ से अलग हो। 'मेरा पैर....' तो तुम पैर नहीं हो, पैर से अलग हो। 'मेरा पेट...' तो तुम पेट नहीं हो, पेट से अलग हो। 'मेरा शरीर....' तो तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो। 'मेरा मन.....' तो तुम मन नहीं हो, मन से अलग हो। 'मेरी बुद्धि....' तो तुम बुद्धि नहीं हो, बुद्धि से अलग हो।
तुम्हारे 'स्व' पर, आत्मा पर माया के दो आवरण हैं। माया की यह शक्ति है। जैसे विद्युत के तार में विद्युत दिखती नहीं लेकिन बल्बों के द्वारा, पंखों के द्वारा विद्युत की उपस्थिति का पता चलता है। ऐसे ही माया कोई आकृति धारण करके नहीं बैठी है लेकिन माया का विस्तार यह जगत दिख रहा है उससे माया के अस्तित्व का पता चलता है।
इस माया की दो शक्तियाँ हैः आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण बुद्धि पर पड़ता है और विक्षेप मन पर पड़ता है। सत्कार्य करके, जप तप करके, निष्काम कर्म करके विक्षेप हटाया जाता है। विचार करके आवरण हटाया जाता है।
पचास वर्ष तपस्या की, एकान्त का सेवन किया, मौन रहे, समाधि की, बहुत प्रसन्न रहे, सुखी रहे लेकिन भीड़ भड़ाके में आते ही गड़बड़ होगी। भीड़ में वाहवाही होगी तो मजा आयेगा लेकिन लोग तुम्हारे विचार के विरोधी होंगे तो तुम्हारा विक्षेप बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी बुद्धि पर से आवरण गया नहीं। अगर आवरण चला गया तो तुम्हें शूली पर भी चढ़ा दिया जाय, कंकड़-पत्थर मारे जाएँ, अपमान किया जाय फिर भी आत्मनिष्ठ के कारण तुम दुःखी जैसे दिखोगे लेकिन तुम पर दुःख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपमान में तुम अपमानित जैसे दिखोगे लेकिन तुम पर अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मृत्यु के समय लोगों को तुम्हारी मृत्यु होती हुई दिखेगी परन्तु तुम पर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम खाते-पीते, आते-जाते, लेते-देते हुए दिखोगे फिर भी तुम इन सबसे परे होगे। तुम आत्म-स्वरूप से कितने स्वतंन्त्र हो !
वासना से परतन्त्रता का जन्म होता है और आत्म विचार से स्वतन्त्रता का।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जीवन्मुक्तों की महिमा
लभन्ते
ब्रह्मनिर्वाणमृषयः
क्षीणकल्मषाः।
छिन्नद्वैधा
यतात्मानः
सर्वभूतहिते
रताः।।
'जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा नियुक्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्मवेत्ता पुरूष शान्त ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।'
(गीताः 5.25)
सब पाप नष्ट हुए बिना ब्रह्मनिष्ठा होती नहीं। जिनके सब पाप नष्ट हुए हैं उनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियों के अर्थात् देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य पशु पक्षी जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनके हित में रत होते हैं। जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्मवेत्ता पुरूष शान्त ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
सब पाप मिट जाने का सौभाग्य जिनका होता है उनके सब संशय मिट जाते हैं।
माण्डूक्य उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण में आता है कि ज्ञानी ब्रह्मसाक्षात्कार करके कैसा रहता है।
जड़वत्
लोकमाचरेत्।
वह ज्ञानी लोगों में जड़ जैसा होकर रहता है, अज्ञानियों की तरह रहता है।
चार आदमियों ने भाँग पी ली। चारों भाँग के नशे में चूर हो गये। एक आदमी नशे में ऊटपटांग बोलने लगा। दूसरा गाना गाने लगा। तीसरा नाचने लगा। चौथा आदमी प्रगाढ़ नींद सो गया। सब नशा तो एक जैसा था लेकिन अपने अपने चित्त के संस्कार के मुताबिक चेष्टा करने लगे। ऐसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार करने वाले ज्ञानियों का ज्ञान तो एक समान होता है पर लौकिक जीवन उनका अपना निराला ही होता है।
जिनके सब पाप अलविदा हो गये हैं वे अपने आत्म-परमात्म-स्वभाव में निसंशय हो जाते हैं।
लौकिक व्यवहार, खान-पान, रहन सहन से ज्ञानी को नापा नहीं जाता। वेश-भूषा से ज्ञान का पता नहीं चलता। आप अपने आपको नाप सकते हैं अपनी मति के अनुसार परन्तु जिनकी मति मतिदाता से अभिन्न हुई है, मति-गति से पार परमात्म-स्वरूप में जो स्थित हैं ऐसे ज्ञानियों को नापना असम्भव है। आपकी मति जितनी ऊँची होगी उतना आपका उनके बारे में ऊँचा अनुमान और आदर होगा। मति जब नीची होगी तब उनके बारे में नीचा अनुमान और नीचा निर्णय होगा। जब तक मनुष्य को पूर्ण आत्म-साक्षात्कार नहीं होता तब तक पूर्ण पुरूषों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, मति, गति में चढ़ाव-उतार होता ही रहता है। अतः जल्दी पूर्णता को पाओ.... पूर्ण पुरूष को पहचानो और पूर्ण हो जाओ।
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरूष शान्त ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
स्कंद पुराण में एक कथा आती हैः
एक जीवन्मुक्त महात्मा भिक्षा हेतु बस्ती में गये। एक कुम्हारिन रो रही थी। महात्मा ने पूछाः
"क्यों रोती हो बहन ?"
"महाराज ! मेरे पति देव हो गये।"
"न कोई मरता है न जीता है। जीना-मरना सब भ्रांति मात्र है। 'यह मेरा पति' ऐसा तूने सुन-सुनकर मान लिया था। सब पाँच भूत हैं और पाँच भूत माया मात्र हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब भ्रांति ही भ्रांति हैं। उनसे बने हुए पुतले भी भ्रांति मात्र हैं। कौन किसका पति... कौन किसकी पत्नी ? फिर क्यों रोती है ?"
जीवन्मुक्त महात्मा का तो अनुभव अपने ढंग का था लेकिन कुम्हारिन तो बेचारी अपनी दृष्टि से जी रही थी। वह बोलीः
"महाराज ! यह ज्ञान तो आप ही जानो। मैं तो इसीलिए रोती हूँ कि अब मिट्टी कौन लाएगा ? रौंदेगा कौन ? घड़े कौन बनाएगा ?
न कोई पति के लिए रोता है न पत्नी के लिए रोता है। सब रोते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने मतलब के लिए।
कुम्हारिन बोलती हैः "महाराज ! ये सब काम अब कौन करेगा ? मैं इसलिए रोती हूँ।"
महात्मा बोलेः "इतना काम तो हम ही कर देंगे बेटी, तू चिन्ता मत कर।"
वे महात्मा वहाँ कुम्हार का काम करने लग गये। हैं तो महात्मा ज्ञानी लेकिन जड़वत् लोकमाचरेत्। अज्ञानी जैसा आचरण भी कर लेते हैं। उनको ऐसा नहीं होता कि 'मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ। मुझसे यह काम कैसे होगा !" उनको कोई पकड़ नहीं होती। ज्ञानी तो अपने सहित सारे विश्व को अपना आत्मा मानते हैं। ज्ञानी के भीतर भेद नहीं होता इसलिए उन्हें भीतर शांति होती है। हम लोगों के भीतर भेद होता है इसलिए हमारे मन-इन्द्रियों से अच्छा व्यवहार होता है तो हमें हर्ष होता है और मन-इन्द्रियों से कुछ ऐसा वैसा व्यवहार हो जाता है तो हमें शोक होता है। हमारे तन-मन का कोई आदर करता है तो हम खुश होते हैं, कोई उंगली उठाता है, अनादर करता है तो हम नाराज हो जाते हैं।
हम अपने को देह मानते हैं और दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। मेरे साथ पत्नी इस प्रकार चले, पुत्र इस प्रकार चले, परिवार इस प्रकार चले। हम अपनी मान्यताओं की गठरी सिर पर लेकर घूमते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुकूल जो व्यवहार करता है उसके साथ राग होता है। जो प्रतिकूल चलता है उसके साथ द्वेष हो जाता है, भय हो जाता है, क्रोध हो जाता है।
ये राग और द्वेष, भय और क्रोध हमारे चित्त को मलिन करते हैं। अनुकूलता आती है तो चित्त में राग की रेखा गहरी होती है, प्रतिकूलता आती है तो द्वेष या भय की रेखा गहरी होती है। चित्त में रेखाएँ पड़ जाती हैं तो चित्त क्षत-विक्षत हो जाता है। फिर वह शांत, स्वस्थ नहीं रहता। ....और
अशान्तस्य
कुतः सुखम्।
अशान्त चित्त को सुख कहाँ ? संशयवाले को सुख कहाँ ? उद्विग्न को सुख कहाँ ?
किसी जीवन्मुक्त महात्मा के चरणों में एक अदभुत स्वभाव वाला आदमी पहुँचा। बोलाः
"महाराज ! मैं चंबल की घाटी का हूँ। डाकू हूँ। अपनी शरण में रखोगे ?"
"हाँ, ठीक है।" महात्मा ने स्वीकृति दी।
"महाराज ! मैं दारू पीता हूँ।"
"कोई बात नहीं।"
"महाराज ! मैं जुआ खेलता हूँ।"
"कोई बात नहीं।"
"महाराज ! मैं दुराचार भी करता हूँ।"
"कोई बात नहीं।"
"महाराज ! मुझमें दुनियाँभर के दोष हैं।"
"कोई बात नहीं।"
"महाराज ! आप यह सब स्वीकार कर रहे हैं ?"
"भैया ! जब सृष्टिकर्त्ता तुझे अपनी सृष्टि से नहीं निकालता तो मैं तुझे अपनी दृष्टि से क्यों निकालूँ ?"
जो जीवन्मुक्त महापुरूष हैं वे ऐसा नहीं समझते कि मेरा आचरण सही है और दूसरे का आचरण गलत है। मेरा शरीर-तंत्र ठीक है, शुद्ध है, दूसरे का अशुद्ध है। ''मैं ठीक और दूसरा गलत..." ऐसा नहीं। दूसरों को भी मेरा अनुभव समझ में आ जाय, दुःखों और क्लेशों से छूट जाएँ ऐसी उन सर्वभूतहितेरताः महापुरूषों की चेष्टा होती है।
हम लोगों का हित इसी में है कि हम अपने आपको समझें। हम अपने आपको नहीं समझेंगे तो कैसी भी परिस्थिति होगी, चित्त का राग और द्वेष जाएगा नहीं।
वस्तुओं से प्राप्त जो सुख है अथवा हमारी मान्यताओं के अनुसार जो सुख है वह वास्तविक में राग का सुख है, आत्मा का सुख नहीं है। हमारी इच्छा के खिलाफ जो हो रहा है उससे जो दुःख होता है वह वास्तविक में बाहर दुःख नहीं है। हमारी मान्यताएँ हमको दुःख देती हैं।
को
काहू को नहीं
सुख दुःख करी
दाता।
निज
कृत कर्म हि
भोगत
भ्राता।।
हम लोग अपने ही विचार, अपनी ही मान्यताओं की गठरियाँ, अपने ही संस्कार पैदा करके दुःख की रेखाएँ खींचकर अपने को जंजीर में बाँधते हैं और सुख की रेखाएँ खींचकर अपने आप आसक्त होकर बँध मरते हैं।
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने संकल्प किया कि प्रभुजी युगल सरकार जिस रास्ते से यात्रा को गये उसी रास्ते में मैं यात्रा को जाऊँ। यात्रा करते-करते दण्डकारण्य आया। रास्ता सँकरा था। सँकरी पगदण्डी के किनारे झाड़ी में कोई भोगी आदमी वेश्या के साथ विलास कर रहा था। तुलसीदासजी रास्ते में आधे तक आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि अगर वापस लौटूँगा तो भी उन लोगों को सन्देह होगा कि बाबाजी ने देख लिया। आगे जाऊँगा तो भी शरमिन्दे होंगे।
उन संत-प्रवर ने अन्धा होने का अभिनय किया। हाथ में लाठी थी। आँखें बन्द कर लीं। लाठी आगे ठोकते-ठोकते चलते हुए पुकारने लगेः
"ऐ भाई ! भगवान के नाम पर कोई रास्ता दिखा दो....।"
भोगी आदमी ने सोचा कि चलो, अच्छा हुआ। यह बाबा आ तो रहा था लेकिन अन्धा है। वह बोलाः
"महाराज ! सीधे सीधे चले जाओ चुपचाप.... जल्दी से। यही रास्ता है। निकल जाओ जल्दी।"
महाराज लकड़ी टेकते-टेकते घाटी की झाड़ी से बाहर निकले। आँखें खोली तो सामने सियाराम मुस्कुराते हुए मिले।
"प्रभु ! आप यहाँ कैसे ?"
"तुलसीदास ! सज्जन में भगवान देखना आसान है लेकिन सबमें भगवान देखने वाले, दुर्जन में भी भगवान देखने वाले तुम्हारे जैसे संत-प्रवर दुर्लभ हैं। ऐसे संतों को देखने के लिए मैं आ जाता हूँ।
यह जरूरी नहीं कि हम जैसा चाहते हैं ऐसा जगत बन जाएगा। यह सम्भव नहीं है। हम चाहेंगे ऐसी पत्नी होगी यह सम्भव नहीं है। पति ऐसा ही होगा यह सम्भव नहीं है। शिष्य ऐसा ही होगा यह सम्भव नहीं है। हम जैसा चाहें ऐसे गुरू बनें यह सम्भव नहीं है। यह सम्भव नहीं है ऐसा समझते हुए भी जितना भी उनका कल्याण हो सके ऐसी उनको यात्रा कराना यह अपने हृदय को भी खुश रखना है और उनका भी कल्याण करना है। हृदय को भी खुश रखना है और उनका भी कल्याण करना है।
अगर हम किसी प्रकार की पकड़ बाँध रखें तो हमें दुःख होगा। यदुवंशी लोग भगवान श्रीकृष्ण के कुल में पैदा हुए हैं। श्रीकृष्ण के होते हुए वे लोग बोतल पीकर एक दूसरे से युद्ध करके खत्म हो गये। सबके अपने-अपने संस्कार होते हैं। जीव अपने संस्कार, मान्यताओं के पाश में बँधा है। यह पाश तब खत्म होता है जब हमारे पुण्य और आत्मविचार बलवान होते हैं। हमारे पुण्य जोर नहीं करेंगे तो हम निःसंशय नहीं हो सकेंगे। जितने अंश में हमारे पुण्य और आत्मविचार की कमजोरी है। हमारी मान्यताओं का जोर ज्यादा है, पुण्यों का जोर कम है। पुण्य तो हैं लेकिन मान्यताओं का इतना जोर है कि पुण्य कमजोर हो रहे हैं।
बुद्धेः
फलं
अनाग्रहः।
बुद्धि का फर क्या है ? अनाग्रह। हम जगत को ठीक कर सकें यह हमारे हाथ की बात नहीं है। हम सबको अन्न-वस्त्र दे दें यह हमारे हाथ की बात नहीं है। सबको मकान दे दें यह हमारे हाथ की बात नहीं है। सबको हमारी शुभ इच्छा के अनुसार चलायें यह हमारे हाथ की बात नहीं है लेकिन सबमें बैठा हुआ परमात्मा निर्लेप नारायण है, असंग है, बाकी सब प्रकृति की लीला है ऐसा समझकर यथाशक्ति सबका हित करना और सुखद विचारों से सुखी रहना हमार हाथ की बात है।
इसका मतलब यह नहीं कि हम आलसी हो जाएँ, प्रमादी हो जाएँ, कोई भूखा है तो भले भूखा मरे, कोई नंगा है तो भले नंगा रहे, हमारे पास ज्यादा वस्त्र हों तो छुपाकर रखें..... नहीं। उनमें अपना आत्मा देखकर उनके हित के लिए यथायोग्य करें लेकिन ऐसा नहीं सोचें कि मैं उनका हित नहीं करता तो इनका क्या होता.... मैं इनके बच्चों को अन्न वस्त्र नहीं देता, उनको नहीं पढ़ाता तो इनका क्या होता। नहीं....
आप और वे पृथक नहीं हैं। जैसे आप अपने शरीर के अंगों को पोसते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज मैंने अपने पैरों को मजबूत करने के लिए भोजन किया, पैरों के ऊपर उपकार किया। अपने अंगों की पुष्टि आप सहज भाव से करते हैं। आप भोजन करते हैं तो आँखों का हित हो जाता है, कानों का हित हो जाता है, हाथ पैर का हित हो जाता है, पेट और पीठ का हित हो जाता है। सारे शरीररूपी नगर का हित हो जाता है। आपको ऐसा अहंकार नहीं आता कि मैं भोजन करके सारे अंगों को पुष्ट करता हूँ। आप सहज स्वाभाविक शरीर के तमाम अंगों को पुष्ट करते हैं। आप अपने शरीर के हित में रत हैं। फिर भी शरीर के लिए आप जो कुछ सुविधाएँ चाहते हो वे सब सदैव सर्वत्र प्राप्त नहीं कर सकते। जितना हित कर सकते हैं उतना करते हैं।
जैसे आप अपने एक शरीर के साथ हित का व्यवहार करते हैं और जितना हित कर सकते हैं उतना करते हैं। उसका आपको अहंकार नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानवान सर्व भूतों का उनके अधिकार के अनुसार जितना हित होता है उतना कर देते हैं और हित करने का अहंकार उनमें नहीं होता। वे जानते हैं कि एक ही अन्तःकरण या शरीर मेरा नहीं अपितु सब अन्तःकरण और शरीर मेरे हैं। मैं अन्तःकरण या शरीर नहीं अपितु अनन्त अनन्त अन्तःकरण जिसमें कल्पित हैं वह चिदाकाश मैं हूँ। ऐसा उनका अनुभव होता है इसलिए उनको गहराई में हर्ष, शोक, राग, द्वेष, भय या अभिनिवेश नहीं होता। यह बहुत ऊँची स्थिति है। यह बिना स्मृति के आयेगी नहीं। स्मृति का अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म को याद किया करो। विजातीय चिन्तन और व्यवहार से आदमी बहिर्मुख हो जाता है। वृत्ति स्थूल हो जाती है, मोटी हो जाती है। आदमी तुच्छ हो जाता है। ब्रह्म का चिन्तन करने से विजातीय चिन्तन छूट जाता है। ब्रह्म का स्मरण हकीकत में होता नहीं, दूसरे का स्मरण छोड़ने के लिए ब्रह्म के स्मरण का एक अवलम्बन मात्र लेना पड़ता है। ब्रह्म तो अपना स्वभाव है। अपने इस ब्रह्म-स्वभाव को जान लेने वाला आदमी निःसंशय हो जाता है।
अगर आप अपने शरीर को 'मैं' मानेंगे और संसार को सच्चा मानेंगे तो आपके पास कुछ भी हो उससे आप सुखी नहीं रहेंगे। शरीर को 'मैं' माना और संसार को सच्चा माना तो मुसीबतें आयी ही समझो। दुःख, भय, शोक, चिन्ता आदि आयेंगे ही। सब तो आपके चित्त के अनुसार होगा नहीं और सब सदा के लिए एक जैसा रहेगा नहीं।
हम जो चाहते हैं वह सब अपना होता नहीं। जो अपना होता है वह सब भाता नहीं। जो भाता है वह सदा के लिए टिकता नहीं। हमारा अन्तःकरण है ऐसे ही दूसरों के भी अपने-अपने अन्तःकरण हैं। हम दुःखी क्यों होते हैं ? क्योंकि हमारा आग्रह होता है कि दूसरों को ऐसा-ऐसा करना चाहिए।
हम अज्ञानवश परचिन्तन में चले जाते हैं। परचिन्तन होते ही 'स्व' की शक्ति क्षीण होने लगती है। परचिन्तन छोड़ते ही स्व की शक्ति जागृत होती है, आकर्षण होता है और प्रीति प्रकट होती है। स्व की प्रीति प्रकट हो गई, अपने आप में तृप्ति मिल गई फिर बाहर कुछ भी हो, कोई परवाह नहीं। अगर आप अपने आप में तृप्त हो तो बाहर आपकी बात किसी ने मानी तो क्या और नहीं मानी तो क्या ? आपको कोई दुःख नहीं होगा। इसीलिए श्रीकृष्ण कहते हैं-
सन्तुष्टः
सततं योगी
यतात्मा
दृढनिश्चयः।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्योमद्भक्तः
स मे प्रियः।।
'जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन इन्द्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए हैं और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है।'
(भगवद् गीताः 12.14)
बाहर की परिस्थितियों से जो सन्तुष्ट होना चाहते हैं वे भोगी हैं। अपनी समझ या स्मृति का सदुपयोग करके जो सन्तुष्ट रहते हैं वे योगी हैं। वे अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में अर्पित कर देते हैं।
हम लोग क्या करते हैं ? हम अपने मन और बुद्धि को हमारी मान्यताओं में अर्पित कर देते हैं, दूसरों की मान्यताओं में अर्पित कर देते हैं। लोगों की नजरों में हम भले दिखें ऐसी चेष्टाएँ करते कर देते हैं। लोगों की नजरों में हम भले दिखें ऐसी चेष्टाएँ करते हैं। हजार-हजार प्रकार की बुद्धि वाले, हजार-हजार विचारवाले हजारमुखी संसार में आप सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकते।
आप कैसा भी शरीर बनायें, कैसा भी आचरण करें, कैसा भी व्यवहार चलायें लेकिन सब आपसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते। क्योंकि सब अपने-अपने ढंग की मान्यताओं से जीते हैं। उनकी जिस समय जैसी मान्यताएँ होती हैं ऐसा आपके प्रति भाव, अभाव, श्रद्धा-अश्रद्धा, अपना परायापन आदि का भाव आ जाता है।
कोई आदमी आप पर श्रद्धा करता है इसलिए आप बड़े हो जाते हैं तो आप गलती करते हैं। कोई आपसे नफरत करता है और आप छोटे हो जाते हैं तो आप गलती करते हैं। पाँच पच्चीस, सौ-दो सौ आदमी वाहवाही करें तो आप बड़े हो जाएँ या पच्चीस-पचास आदमी आपकी निन्दा करें तो आप छोटे हो जायें तो आप अपने आपमें नहीं आये। आप निःसंशय नहीं हुए। आप जितात्मा नहीं हुए। आप प्रशान्तात्मा नहीं हुए। आप ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित नहीं हुए।
ब्रह्मचारी एकाकी रहता है, अकेले में रहता है। एकाकी और अकेले में रहने से ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा होती है। अधिक संपर्क में ब्रह्मचर्य का नाश होता है। ब्रह्मचर्य माने सब इन्द्रियों का संयम और मन का ब्रह्म में विचरण।
ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने वाला योगी संतुष्ट होता है। वह निष्पाप हो जाता है। एक बार परमात्मा को जान लिया और निःसंशय हो गया तो वह सिद्ध बना हुआ योगी व्यवहार में आने पर भी विचलित नहीं होता। व्यवहार में तो विक्षिप्त कर दें ऐसे प्रसंग तो आते ही हैं फिर भी ज्ञानी को अपने ब्रह्म-स्वभाव की स्मृति यथावत् बनी रहती है। व्यवहार में ज्ञानी भीतर से अपने को कुछ विशेष मानकर नहीं रहता। ज्ञानी का और अज्ञानी का खान-पान, रहन-सहन, उठ-बैठ, बोल-चाल आदि सब लोकव्यवहार एक समान दिखेगा लेकिन दोनों की भीतरी समझ में बहुत बड़ा फासला होता है। अज्ञानी ज्ञानी को मानेगा कि ये ज्ञानी हैं, महान् हैं..... लेकिन ज्ञानी अपने को यह नहीं मानेगा कि मैं इतना महान् हूँ या तुच्छ हूँ।
हम लोगों में परचर्चा करने की आदत होती है। पर की चर्चा में स्व की प्रीति खत्म हो जाती है। जब परचर्चा में प्रवृत्त होने लगो तब सजग होकर अपने आपको पूछो कि हमारा जन्म दूसरों के दोष देखने के लिए हुआ है कि अपने को प्रभु में मिलाने के लिए हुआ है ? दूसरों के दोष देखने की अपेक्षा गुण देखने चाहिए। गुण देखने की अपेक्षा उनमें परमात्मा देखना चाहिए।
सांख्य के द्वारा तत्त्वज्ञान होने में अड़चन यह आती है कि हमारी देह में प्रीति होती है। प्राणीमात्र को अपने देह में प्रीति होती है। इसीलिए तत्त्वज्ञान जल्दी से नहीं होता। तत्त्वज्ञान हुए बिना सब संशय दूर नहीं होते। दृष्टा-दृश्य का विवेक, साक्षित्व का विवेक तो बिना वेदान्त के भी आदमी कर सकता है। तत्त्वज्ञान पाने के लिए दृश्य-दृष्टा के विवेके से भी आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए वेदान्त चाहिए। वेदान्त-सिद्धान्त का ज्ञान चाहिए। वेदान्तनिष्ठ महापुरूष का कृपा-प्रसाद चाहिए।
अकेले रहकर कितनी भी समाधि करो, जितेन्द्रिय हो जाओ, ब्रह्मचर्य-व्रत में स्थित हो जाओ फिर भी एक अन्तःकरण में अहंप्रत्यय रहेगा। 'मैं इसको छोड़ूँ.... उसको छोड़ूँ...... एकान्त में जाऊँ.... तपस्या करूँ... ध्यान करूँ.... आनन्द में रहूँ.....' ये संकल्प बने रहेंगे। साधक नर्मदा किनारे एकान्त में जाएगा, ध्यान-साधना करेगा, आनन्द में रहेगा लेकिन वहाँ भी मछुआ आ जाएगा तो उसे देखकर खिन्न होगा कि इस बला का कहाँ दर्शन हो गया ! ऐसे-वैसे किसी भी प्रसंग से दुःख हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी समझ नहीं है न ! जब तक तत्त्वज्ञान नहीं हुआ तब तक दुनियाँ के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने को कैसी भी अवस्था में ढाल दो लेकिन देह की परिच्छिन्नता तो बनी ही रहेगी। चाहे कितना भी धन रख लो, कितनी भी सत्ता हस्तगत कर लो, कितना भी परिचय बढ़ा लो, कितने भी पदार्थ पा लो, कितनी भी एकाग्रता कर लो, तपस्या कर लो लेकिन जब तक एक देह में 'मैं' पना है तब तक द्वैत बना रहेगा। जब तक द्वैत रहेगा तब तक मुसीबतों का अन्त नहीं आयेगा।
द्वितीयाद्
वै भयं भवति।
दूसरे से भय बना रहता है।
जब तक दूसरा दिखता रहेगा तब तक भय बना रहेगा। एकाग्र होने वाले को विक्षेप का भय, सदाचारी को दुराचारी का भय, सत्ताधीश को सत्ताभ्रष्ट हो जाने का भय, धनवान को धन चला जाने का भय। इन सब भयों से बचने के लिए, भय को दबाने के लिए लोग फिर उसी प्रकार का सामान इकट्ठा करते हैं जो भय को और बढ़ाते हैं। अपने साथियों का झुण्ड बनने से आदमी निर्भय नहीं होता अपितु और खोखला हो जाता है।
आप जितना ज्ञान की शरण जाते हैं, आत्मविश्वास की शरण जाते हैं, अद्वैतभाव की शरण जाते हैं उतना आप निर्भय बनते हैं। आप जितना अद्वैतनिष्ठा में स्थित होते हैं उतना आप सर्वभूतहिते रताः बनते हैं।
हम लोगों की आदत है शरीर से सुख लेने की। कई जन्मों के संस्कार पड़ गये हैं, कई युगों का ऐसा अभ्यास हो गया है। जिस शरीर में आते हैं उसको 'मैं' मान लेते हैं। उसी को खिलाने-पिलाने में, उसकी लालन-पालन में, उसी की वाहवाही में, उसी के यश में उसी को अमर करने में हमारी रूचि होती है। यह पुराना रोग है।
..........तो अब क्या करें ? देह की आसक्ति कैसे मिटायें ?
दूसरों के सुख का चिन्तन करने से अपने देह को सुखी करने का चिन्तन छूट जाएगा। अपने देह को सुखी रखने का चिन्तन छूटते ही आत्मा में प्रीति होने लगेगी।
देह को सुखी रखने का चिन्तन न करें तो ? देह दुःखी होगा ?
ना.... ना.... फिर देह से जो होगा वह औषध की तरह आचरण हो जाएगा। अपने आपको देह से पृथक जान लिया तो आपके देह के द्वारा जो कुछ भी होगा वह दूसरों के हित के लिए होगा। देह के द्वारा अगर सुख लेने की वासना है तो, सुख भोगने की वासना है तो देह में आसक्ति हो जाएगी। देहाध्यास मजबूत हो जाएगा। राग मजबूत हो जाएगा। राग मजबूत होते ही चित्त मलिन हो जाएगी।
एक राजा था। रनवास में बहुत सुविधाएँ रखी थीं। ऐसी ऐसी रानियाँ थीं कि राजा को रनवास से बाहर ही न आने देतीं थीं। इत्र आदि चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी को रजस् और तमस् में बाँधे रखती हैं, नीचे के केन्द्रों में ही ले जाती हैं।
राजा महल में ही रहने लगा।
राजा का वजीर विश्वासपात्र था। वह सब राजकाज सँभाल लेता था। प्रजा को तथा अमलदार वर्ग को पता चला कि राजा साहब आजकल सप्ताह-सप्ताह तक, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक, महीने-महीने तक रनवास में ही रहते हैं। सब अमलदार मनमाना करने लगे।
दीवान ने देखा कि राजा साहब आते नहीं और मेरे नियंत्रण में अमलदार रहते नहीं। राज्य में अन्धाधुन्धी हो रही है। प्रजा का बुरी तरह शोषण हो रहा है। बदमाश लोग प्रजा का खून चूस रहे हैं।
वजीर ने जाकर महल का दरवाजा खटखटाया। रानियों ने सोचा कि मूँआ दीवान आया है, राजा साहब को कोई सूचना देगा, राजा साहब हमको छोड़कर दरबार में चले जाएँगे। रानियों ने दीवान को आँखें दिखायी।
दीवान बोलाः "अच्छा ! राजा साहब से मिलने नहीं देती तो कोई बात नहीं लेकिन यह चिट्ठी तो उन्हें पहुँचा देना।"
रानियों ने कहाः "तू चला जा। अगर दुबारा आया तो दासियों से पिटाई करवा देंगे।"
आठ-दस, बारह-पन्द्रह दिन हो गये लेकिन राजा बाहर नहीं आया। वजीर ने सोचा की अभी राजा साहब को चिट्ठी मिली नहीं। अरे राम ! राज्य लुटा जा रहा है। गुन्डों ने प्रजा को घेर लिया है। महीनों भर अपने महल से राजा साहब बाहर ही नहीं आते। दीवान को मुलाकात ही नहीं देते !
वजीर को वैराग्य हो आया। 'मेरे होते होते राज्य जल रहा है.... मुझसे देखा नहीं जाता। क्या करूँ ?' वजीर चुपचाप बैठ गया...... शान्त.....। भीतर से आवाज आयी किः 'एक दिन जलना है। उसको देखकर क्या जलता है ? जो बुझाना है उसको बुझा। अपनी पकड़ और आग्रह है उसको बुझा।'
वजीर चला गया जंगल में। महल के पीछे के इलाके में जाकर बैठ गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। सूबेदारों ने राजा के महल के द्वार खटखटाये। राजा ने द्वार खोला तो सूबेदारों ने कहाः
"महाराज ! दीवान चले गये, कई दिन हो गये। अब तो बिल्कुल अन्धाधुधी हो गई है।"
"दीवान चला गया ? वह तो मेरा विश्वासपात्र था ! उसके भरोसे तो मैं निश्चिन्त था। वह चला गया ?"
"हाँ महाराज ! वे चिट्ठी लेकर महल में आये थे। दो-दो दिन, पाँच-पाँच दिन खड़े रहे लेकिन उनको आपकी मुलाकात नहीं हुई। आखिर थककर वे चले गये।"
"कहाँ गया ?"
"जंगल में। झोंपड़ी बाँधकर बैठ गये हैं ध्यानस्थ।"
राजा पहुँचा वजीर के पास और बोलाः
राजा पहुँचा वजीर के पास और बोलाः
"तू मेरा विश्वासपात्र दीवान है। सब छोड़कर जंगल में बैठा है। क्या फायदा हुआ ?"
"महाराज ! फायदा यह हुआ कि मैं कई दिनों तक कई बार आपके महल के द्वार पर खड़ा रहा। रानी साहेबाओं ने बुरी तरह डाँटा। आपकी मुलाकात नहीं हुई। अब सब कुछ छोड़कर झोंपड़े में परमात्मा-चिन्तन में रह रहा हूँ तो आप खुद चल कर मेरे पास आये। मुझे लाभ हुआ कि नहीं हुआ ?"
पर के चिन्तन से हमारी शक्ति क्षीण होती है। स्व (आत्म-परमात्मा) के चिन्तन से शक्ति जागृत होती है, बढ़ती है।
स्व क्य है ? पर क्या है ? हम निष्पाप कैसे हों ? हमारे कल्मष दूर कैसे हों ? जब तक कल्मष हैं तब तक ज्ञान नहीं होता। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब कल्मष नहीं जाते। जैसे नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले भागती है ऐसे ही ये भी एक दूसरे के पोषक हैं। कल्मष जाएँगे तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो कल्मष जाएँगे।
कल्मष होते क्या हैं ? कल्मष होते हैं पर का चिन्तन अधिक बढ़ जाने से। स्व का अज्ञान.... स्व की विस्मृति हो जाती है। चित्त मलिन होता है।
चित्त को शुद्ध करने का उत्तम से उत्तम एक तरीका है। वह आसान भी है। सब अवस्थाओं में कर सकते है। सब जगह समाधि नही कर सकते। सब जगह कीर्तन नहीं कर सकते। बस में बैठे कीर्तन करेंगे तो लोग भगतड़ा कहकर उपहास करेंगे। आप पर का चिन्तन छोड़कर स्व की स्मृति कहीं भी कर सकते हैं। बस में भी कर सकते हैं और बाजार में भी।
स्व की स्मृति करने के लिए प्रारंभ में थोड़ा एकान्त चाहिए लेकिन अभ्यास हो जाने पर वह कहीं भी कर सकते हैं।
स्व क्या है, पर क्या है यह समझ लें।
जिसको रखने से न रहे उसको बोलते हैं पर। जिसको छोड़ने से भी न छूटे उसको बोलते हैं स्व। जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते वह है स्व। जिसको आप सदा रख नहीं सकते वह है पर। मकान, दुकान, घर, गाड़ी यह जो कुछ भी है वह पर है। अपना शरीर भी पर है, स्व नही है। अगर शरीर स्व होता तो वह कहने में चलता। तुम नहीं चाहते कि बाल सफेद हों, तुम नहीं चाहते हो कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़े, तुम नहीं चाहते कि शरीर में कोई भी रोग हो। शरीर पर है।
उपनिषद में आता है कि जो स्वाभाविक होता है वह मिटता नहीं। जो आस्वाभाविक होता है उसको रखने की इच्छा नहीं होती। बर्फ की ठण्डक मिटाने के लिए आपकी इच्छा नहीं होगी। अग्नि की गर्मी मिटाने के लिए आपकी इच्छा नहीं होगी। ठण्डा होना बर्फ का स्वभाव है। गर्म होना अग्नि का स्वभाव है। मुँह में दाँत होना स्वाभाविक है लेकिन दाँत में तिनका होना अस्वाभाविक है इसलिए तिनका निकालकर ही चैन लेते हैं। आँखों के पोपचों में बाल स्वाभाविक हैं लेकिन बाल आँख में घुस जाता है तो वह खटकता है। उसे निकालना पड़ता है। खटकता वह है जो अस्वाभाविक है। जो स्वाभाविक होता है वह सुख देता है।
शान्ति पाना स्वाभाविक है। आपकी वह माँग है। घर-बार, पुत्र-परिवार छोड़कर शहर से बाहर आश्रम में सत्संग सुनने आ जाते है तो शान्ति पाना स्वाभाविक है। सत्संग के वातावरण में आकर कोई लफंगा फिल्मी गीत गाने लग जाए तो यह आपको अस्वाभाविक लगेगा। उसे आप तुरन्त चुप कर देंगे।
सदा रहना आपका स्वभाव है। आप नहीं चाहते कि मैं मर जाऊँ। जानना आपका स्वभाव है। आप अज्ञानी, मूर्ख नहीं रहना चाहते है। कोई आपको अज्ञानी कहकर पुकारे तो आपको खटकेगा। आप अज्ञान नहीं चाहते। आप मौत नहीं चाहते। आप दुःख नहीं चाहते। आप सदा रहना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं और आनन्द चाहते हैं।
आप सत् हैं इसलिए सदा रहना चाहते हैं। आप चित् हैं इसलिए ज्ञान चाहते हैं। आप आनन्द स्वरूप हैं इसलिए आनन्द चाहते है। असत्, जड़ और दुःखरूप हो जाना यह अस्वाभाविकता है। आप यह अस्वाभाविकता त्यागकर अपनी असली स्वाभाविकता पाना चाहते हैं। सच्चिदानन्द आपका स्वभाव है। आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, अज्ञान और दुःख मिटाना चाहते हैं। अज्ञान आपको अखरता है क्योंकि आप ज्ञानस्वरूप हैं, दुःख आपको अखरता है क्योंकि आप आनन्दस्वरूप हैं, दुःख आता है तो आप बेचैन होते हैं। सुख में वर्ष के वर्ष बीत जाते हैं तो कोई पता नहीं चलता लेकिन आपकी किसी मान्यता को ठेस पहुँची तो आप दुःखी हो गये। दुःख आता है तो आप दुःख मिटाने की कोशिश करते हैं। सुख आता है तो सुख मिटाने की कभी कोशिश की ? ऐसा कोई माई का लाल देखा जिसको आनन्द ही आनन्द मिला और उसे मिटाने की कोशिश की हो ? सुख और आनन्द मिटाने की कोशिश कोई नहीं करता फिर भी वह मिट तो जाता ही है। दुःख वापस आ ही जाता है। क्यों ? क्या कारण है ? सुख और आता रहे... आनन्द और आता रहे.... आता रहे... ऐसी चाह करते-करते पर का चिन्तन हुआ और आनन्द भाग गया।
स्व का माने हमारा स्वभाव है सत्, चित् और आनन्द। पर का स्वभाव है असत्, जड़ और दुःख।
असत् पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। जड़ को तो पता ही नहीं कि मैं हूँ। देह जड़ है, पाँच भूतों का पुतला है। सुबह से रात तक, जीवन से मौत तक इसको खिलाओ-पिलाओ, नहलाओ, घुमाओ लेकिन देखो तो कभी न कभी कोई न कोई शिकायत जरूर होगी।
तन
धरिया कोई न
सुखिया देखा।
जो
देखा सो
दुखिया रे।।
'डॉक्टर साब ! दवा कर दो, बहुत पीड़ा हो रही है....' लेकिन डाक्टर सा'ब को पूछो कि अपना क्या हाल है ? अपनी पत्नी का क्या हाल है ? सुबह इन्जेक्शन लेकर अस्पताल में जाता हूँ बाबाजी !'
मैं ऐसे डाक्टरों को जानता हूँ जिन्होंने अपने इलाके में नाम कमाया है। उनके बाप उनको मेरे पास ले आये और प्रार्थना करने लगे किः
"स्वामी जी ! आप इसको समझाइये। इसने नाम कमाया है, मरीजों को तो ठीक करता है लेकिन खुद इतना बेठीक है कि रोज नशे के इन्जेक्शन लेता है। M.B.B.S. की डिग्री भी है, कमाता भी है, प्रैक्टीस भी अच्छी चलती है लेकिन कभी नशे-नशे में किसी मरीज का बेड़ा गर्क कर देता है। यह हिन्दुस्तान है बाबा जी ! सब चल रहा है। परदेश में प्रैक्टीस करता तो वहाँ के लोग और सरकार इसको दिन के तारे दिखा देती। आप आशीर्वाद करो।"
स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर में, किसी में भी, 'मैं' पना है तो अभी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान हुआ नहीं तो असत्, जड़ और दुःख का सम्बन्ध छूटा नहीं। जब तक असत्, जड़ और दुःख का सम्बन्ध नहीं छूटा तब तक सत्, चित्, और आनन्द स्वरूप में प्रीति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सत्-चित्-आनन्द-स्वरूप आयेगा, मिलेगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। सत्-चित्-आनन्द यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा आपका स्व है। देह पर है। पर का स्वभाव है असत्-जड़-दुःख।
आत्मा और देह का परस्पर अध्यास हो गया। एक का स्वभाव दूसरे में दिखने लगा। आत्मा का अध्यास देह में होने लगा इसलिए आप देह से सदा रहना चाहते हैं। देह से सब जानना चाहते हैं। देह से सदा सुखी रहना चाहते हैं। ऐसे पर के चिन्तन की आदत पड़ गई। यह आदत पुरानी है इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है।
तत्त्वज्ञान समझने में जो असमर्थ हैं उनके लिए योग सुगम उपाय है। प्राण-अपान की गति को सम करके भ्रूमध्य में प्रणव की धारणा करें। इससे पर का स्वभाव छूटेगा। स्व का आनन्द प्रकट होगा। सत् चित् आनन्द स्वभाव बढ़ेगा।
एकान्त में जाकर बैठो। चाँद सितारों को निहारो। निहारते निहारते सोचो कि वे दूर दिख रहे हैं, बाहर से दूर दिख रहे हैं। भीतर से देखा जाए कि मैं वहाँ तक व्यापक न होता तो वे मुझे नहीं दिखते। मेरी ही टिमटिमाहट उनमें चमक रही है। मैं ही चाँद में चमक रहा हूँ... सितारों में टिमटिमा रहा हूँ।
कीड़ी
में तू नानो
लागे हाथी में
तूँ मोटो
क्यूँ।
बन
महावत ने माथे
बेठो
होंकणवाळो
तूँ को तूँ।
ऐसो
खेल रच्यो
मेरे दाता
जहाँ देखूँ
वहाँ तूँ को
तूँ।।
इस प्रकार स्व का चिनत्न करने से सामने दिखेगा पर लेकिन पर में छुपे हुए स्व की स्मृति आ जाए तो आपको खुली आँख समाधि लग सकती है और योग की कला आ जाए तो बन्द आँख भी समाधि लग सकती है।
सतत खुली आँख रखना भी संभव नहीं और सतत आँख बन्द करना भी संभव नही। जब आँख बन्द करने का मौका हो तब बन्द आँख के द्वारा यात्रा कर लें और आँख खोलने का मौका हो तो खुली आँख से यात्रा कर लें। यात्रा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जाना है। पर के चिन्तन से बचना है, बस। यह प्रयोग लगता तो इतना सा है लेकिन इससे बहुत लाभ होता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सर्व बन्धनों से मुक्ति का उपाय
ये
हि वृत्तिं
विजानन्ति
ज्ञात्वापि
वर्धयन्ति
ये।
ते
वै सत्पुरूषाः
धन्याः
वन्द्यास्ते
भुवनत्रये।।
'जो इस ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं और जानकर इसे बढ़ाते हैं वे सत्पुरूष धन्य हैं। वे ही तीनों लोकों में वन्दनीय हैं।'
(अपरोक्षानुभूतिः 131)
जो ब्रह्माकार वृत्ति को नहीं जानते हैं वे घटाकार वृत्ति से, मठाकार वृत्ति से, पटाकार वृत्ति से, सुखाकार वृत्ति से, दुःखाकार वृत्ति से चिपक चिपककर अपने को सताते रहते हैं।
वृत्ति उत्पन्न होती है। घड़ा देखा घटाकारवृत्ति, मठ देखा तो मठाकार वृत्ति, मित्र देखा तो मित्राकार वृत्ति, शत्रु देखा तो शत्रुआकार वृत्ति, पुस्तक देखी तो पुस्तकाकार वृत्ति.... ये वृत्तियाँ तो उठती रहती हैं। जिसने सत्संग सुनकर ब्रह्माकार वृत्ति को जान लिया वह पुरूष धन्य है।
जीव के सारे दुःखों का मूल कारण है अपने उदगम स्थान ब्रह्म-परमात्मा को नहीं जानना। उस अपने मूल स्रोत ब्रह्म-परमात्मा को जान लेने मात्र से जीव के सारे दुःख दूर हो जाते हैं।
ज्ञात्वा
देवं मुच्यते
सर्व
पाशेभ्यः।
उस देव को जानकर आदमी सारे बन्धनों से मुक्त हो जाता है।
अपने में से दोष निकालना अच्छा है। दोष निकालने के लिए गुण भरना अच्छा है। गुण प्रकृति में होते हैं। दोषी होने की अपेक्षा गुणवान होना ठीक है। सिर में केरोसीन लगाने की अपेक्षा सुगंधित तेल लगाना ठीक है लेकिन उसे भी साबुन लगाकर आखिर उतारना ही पड़ता है अन्यथा वह सिर में मैल जमाकर देता है। यज्ञ करते समय भी हाथ जलते हैं। एक आदमी दुष्कृत्य करता है और लोहे की जंजीर से बंधता है। दूसरा आदमी सुकृत करता है तो सोने की जंजीर से बंधता है। बन्धन तो दोनों को है।
ब्रह्माकार वृत्ति सुकृत दुष्कृत दोनों से पार कराके जीव को कृत अकृत से पार अपने स्वरूप में जगाती है। सुकृत दुष्कृत की अपेक्षा अच्छा है। लेकिन जीव सुकृत दुष्कृत दोनों से परे नहीं पहुँचा, सुकृत-दुष्कृत से आच्छादित होता रहा तो पूर्ण नहीं हो पाता। पाप बुरा फल देकर खत्म हो जाता है। पुण्य अच्छा फल देकर खत्म हो जाता है। पाप न करें, पुण्य करें। लेकिन इससे भी आगे जाकर विचार करें कि पुण्य का कर्त्ता कौन है ?
हमारे देश के तत्त्ववेत्ता मनीषियों की यह प्रसिद्ध विलक्षणता है कि कोई भी विषय का विचार करेंगे तो उसके परिणाम पर नजर दौड़ायेंगे। 'इसका आखिरी परिणाम क्या होगा, अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा ?' यह सोच विचार करके ही कोई भी कर्माकर्म का निर्णय करेंगे। यह उनकी विलक्षण योग्यता है और उनकी यह विलक्ष्णता सारे विश्व में प्रसिद्ध है।
जिसका आखिरी परिणाम मोक्ष नहीं है, जिसका आखिरी परिणाम जीवन्मुक्ति नहीं है, जिसका आखिरी परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है वे सारे के सारे कृत्य बालकों की चेष्टा के समान हैं। सारी उपासनाएँ, सारे दर्शनशास्त्र, सारा योग, सारा ध्यान, ज्ञान, भक्ति, भजन, भाव का आखिरी प्रयोजन है कि जीव बन्धन से मुक्त हो जाये।
ज्ञात्वा
देवं मुच्यते
सर्वपाशेभ्यः।
जिसको जानने से सर्व पाशों से मुक्त हो जाए उस देव को जानने का अगर हेतु है तुम्हारे क्रिया-कलाप का तो वह सार्थक है। उस देव को कब जाना जाता है ? जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तब। घटाकार वृत्ति पैदा हो रही है, मठाकार वृत्ति पैदा हो रही है, सुखाकार वृत्ति पैदा हो रही है लेकिन सुखाकार वृत्ति जितनी देर टिकी उतनी देर सुख, फिर वृत्ति बदली तो सुख गायब हो गया। ब्रह्माकार वृत्ति एक बार अगर उत्पन्न हो जाय, केवल तीन क्षण के लिए ही सही, तो जीव का आवरण भंग हो जाता है। फिर सुख-दुःख में सत्य-बुद्धि नहीं रहती, मान-अपमान में सत्य-बुद्धि नहीं रहती, पुण्य-पाप में सत्य-बुद्धि नहीं रहती, विक्षेप और समाधि में सत्य-बुद्धि नहीं रहती। बहुत ऊँची बात है। यह ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट हाथ में काँसा लिए, सिर में खाक डालकर संतों के शरण में जाते थे।
उस ब्रह्माकार वृत्ति को जानो। ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करने की कला को जानो। जानकर उसे बढ़ाओ।
अब ऐहिक विज्ञान ने भी प्राचीन ऋषियों के सत्य की ओर कुछ यात्रा की है। वे भी पदार्थ का विश्लेषण करते-करते वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सबका जोड़ एक ही में आता है। वैज्ञानिक खोज जहाँ से शुरू करते हैं, वापस वहीं आखिर में आ जाते हैं। सब एक ही तत्त्व से जुड़े हैं। तिनका हो चाहे वटवृक्ष हो, दोनों सूर्य से जुड़े हैं। आदमी बड़ा हो चाहे छोटा हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, गोरा हो चाहे काला हो, लाभकर्त्ता हो चाहे हानिकर्त्ता हो, लेकिन उसका शरीर सूर्य से जुड़ा है।
सूर्य जिससे जुड़ा है, चंद्र जिससे जुड़ा है, आकाश जिससे जुड़ा है उस चैतन्य से तुम जुड़े हो। राजा के महल में जलने वाला बल्ब और गरीब के झोंपड़े में जलने वाला बल्ब दोनों पावर हाउस के वायर से जुड़े हैं अतः पावर हाउस से ही जुड़े हैं।
ऐसे ही प्राणीमात्र ब्रह्म-परमात्मा से जुड़ा है।
सागर का हर बिन्दु सागर से जुड़ा है। कोई छोटी तरंग होती है कोई बड़ी होती है। नदी में कहीं-कहीं भँवर बनता है। लगता है कि भँवर में पानी वही का वही है लेकिन नहीं। वह पानी चला जाता है और दूसरा आता है, भँवर के आकार में घूमता है और चला जाता है।
ऐसे ही लगता है कि यह शरीररूपी भँवर वही का वही है लेकिन उसमें सूक्ष्म सत्ताएँ सूर्य की, जल की, वायु की, पृथ्वी की, आकाश की हैं। वे सत्ताएँ निरन्तर बदलती ही जाती है। हम हर श्वास में बदल रहे हैं. यह बदलाहट जिसकी सत्ता से मिलती है उस चैतन्य को, अबदल आत्मा को पहचान लो। ब्रह्मज्ञान का श्रवण-मनन करके आनन्द-स्वरूप ब्रह्म-परमात्मामय वृत्ति बनाना ही ब्रह्माकार वृत्ति है।
भगवदाकार वृत्ति बनती है, इष्टाकार वृत्ति बनती है, स्मरणाकार वृत्ति बनती है। स्मरण होता है तब लगता है कि हमारा स्मरण चालू है। स्मरण चालू नहीं था तब, स्मरण चालू है तब, स्मरण छूट जाएगा तब....तीनों को जो जानता है वह कौन है ?
खोजनहार
नू खोज ले।
ढूँढनहार
नू ढूँढ ले।।
आहा.... ! बेड़ा पार.......। वे लोग धन्य हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं, जानकर जो बढ़ाते हैं।
मारवाह में कोई सज्जन रहते थे। वे कमाने के लिए कलकत्ता गये। घर से जब निकले उन दिनों में उनकी पत्नी गर्भवती थी। वे सज्जन पंद्रह-सत्रह साल कलकत्ते में ही रह गये। पुराना जमाना था। संदेश व्यवहार एवं यातायात की सुविधाएँ नहींवत् थीं। डाक-तार एवं रेलगाड़ियाँ नहीं थीं।
इधर पत्नी को लड़का हुआ। समय पाकर बड़ा होते-होते वह पंद्रह-सत्रह साल का हो गया। बेटे ने बाप को नहीं देखा था और बाप ने बेटे को नहीं देखा था। माँ ने बेटे से कहा कि तलाश करो, तुम्हारे पिता कलकत्ते कमाने गये हुए हैं। हम इधर दुःख में दिन गुजार रहे हैं। उनके कोई समाचार नहीं मिल रहे हैं। जरा जाँच करो।
बेटा तो गरीबी में दिन काट रहा था। जो कुछ फटा-टूटा पहना था, मैली फटी चदरिया थी वह लेकर निकल पड़ा कलकत्ता जाने के लिए। उधर कलकत्ता में पिता को भी हुआ कि बहुत साल हो गये हैं, अब अपने घर जाऊँ। काम-धन्धा ठीक हो गया है, कमाई भी अच्छी हुई है। अब अपने देश में जाऊँ। ऐसा सोचकर वह कलकत्ता से मारवाड़ आने के लिए चला।
बच्चा घूमता-घामता, थका माँदा यात्रा करते-करते एक रात्रि को किसी धर्मशाला में जा ठहरा। उसी धर्मशाला में कलकत्ता से चला हुआ पिता भी ठहरा था। लड़के की हालत देखकर उसे छोटी सी खोली दे दी गई। लड़का मारे ठण्ड के ठिठुर रहा था, सर्दी जुकाम के कारण खाँस भी रहा था। पास में ही उस कलकत्ता वाले सेठ को दिया हुआ बढिया कमरा था। सेठ ने धर्मशाला के व्यवस्थापक से शिकायत कीः
"ऐसी सुन्दर धर्मशाला में कैसे अवारा छोरों को ठहरने देते हो ? वह छोरा खाँस रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है। हटाओ इसको। निकालो यहाँ से। चाहिए तो हमसे दो रूपये चार्ज ज्यादा ले लो। मेरी नींद खराब हो रही है। कल मुझे और आगे यात्रा करनी है।"
लड़के को खोली से बाहर निकाल दिया गया। फुटपाथ पर ठण्ड में ठिठुरते हुए सारी रात बितायी। सुबह में सेठ अपने कमरे से बाहर निकले। धर्मशाला से बाहर आये। फुटपाथ पर देखा तो वही रातवाला लड़का।
"अरे ! कैसे बदतमीज नालायक लोग हैं ! इस धर्मशाला में ठहरने की औकात ! कहाँ से आया है रे छोरा ?"
"सेठ जी ! राजस्थान से आ रहा हूँ।"
"राजस्थान से ? कौन से इलाके से ?"
"सिरोही जिले में फलानी.... जगह से।"
"वहाँ तो मेरा भी गाँव है। किस जाति का है।"
"मारवाड़ी हूँ।"
"कौन-सा कुल ?"
"फलाना.....।"
"तेरे पिता का नाम क्या है ?"
लड़के की आँखों से आँसू बहने लगेः
"मेरे पिता का नाम अमुक है। मैं माँ के पेट में था तब मेरे पिता कलकत्ता गये हैं। आज पन्द्रह-सत्रह साल हो गये....।"
अब तो महाराज ! लड़के की खाँसी चली गई, जुकाम भाग गया। पिता ने पुत्र को गले लगा लिया... मधुर लग गया अपना लाडला।
क्यों ?
उस बच्चे में 'मेरापन' आ गया। जान लिया कि यह 'मेरा' है। 'मेरा' है तो उसके सारे दोष गायब।
लड़का भी अब फरियाद नहीं करेगा कि 'सेठ का सत्यानाश हो..... मुझे बाहर निकलवा दिया.... आधी रात को ठण्ड में धकेल दिया।' ना.... ना......। अब यह रोष नहीं रहेगा। अब तो मेरे पिता....!'
अज्ञान दशा में दोनों एक दूसरे को दुत्कार रहे थे, बेटा मन ही मन दुत्कार रहा था, बाप वाणी से भी दुत्कार रहा था। लेकिन जब दोनों ने जान लिया कि हम दोनों में एक ही रक्त है तो गले लग गया।
क्रोध कब होता है ? जब सामने दूसरा होता है। भय कब होता है ? जब दूसरा होता है। काम कब होता है ? जब दूसरा दिखता है। तुम कितने भी सुन्दर हो लेकिन तुमको अपने आप पर काम-विकार नहीं होगा। स्त्री हो चाहे पुरूष हो, काम हमेशा दूसरे पर ही होता है। यह कामाकार वृत्ति है। जिस पर काम होता है उसमें भी अपने चैतन्य को देख लो तो काम राम में बदल जाएगा, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अद्वैत में निष्ठा होते ही भय प्रेम में बदल जाएगा, घृणा स्नेह में बदल जाएगी। बाहर से आप यथोचित लेना देना, हँसना-रोना करेंगे लेकिन भीतर से आपको लगेगा कि सब मुझमें है और मैं सबमें हूँ। जैसे शरीर को देखो तो हाथ अलग हैं, मूछ के बाल अलग हैं लेकिन ये सब मिलाकर एक आप ही हैं न ! इस देह के पुर्जे भिन्न होते हुए भी सब एक अभिन्न सत्ता से संचालित होते हैं, अभिन्न सत्ता के लिए ही सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे ब्रह्माण्ड में जो भिन्न भिन्न क्रिया-कलाप हैं वे अभिन्न चैतन्य से संचालित हैं और उसी से मिलने के लिए ही सब यात्रा कर रहे है। देर सबेर सब वही जाएंगे। पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, हजारों जन्मों के बाद पहुँचे या आज ही पहुँच जाय लेकिन जायगा वहीं।
हमें देर सबेर उसी चैतन्य परमात्मा में अभिन्न रूप से पहुँचना पड़ेगा तो क्यों न आज ही उसके साथ के शाश्वत सम्बन्ध की स्वीकृति देकर अभिन्नता महसूस करें ? वह महा यात्रा आज ही क्यों न कर लें ?
इस जीव को देर सबेर ब्रह्माकार वृत्ति के जगत में पहुँचना ही पड़ेगा।
बैलगाड़ी में यात्रा करते-करते तुम अमेरिका जाने की चेष्टा करो तो पहुँचने की संभावना नहीं। पहिये घुमाते-घुमाते, बैल बदलते-बदलते, दिन रात, मास और वर्ष बिताते-बिताते, एक दो, दस जन्म बदलते-बदलते फिर पता चले कि हवाई जहाज के सिवाय अमेरिका नहीं पहुँच सकते..... फिर हवाई जहाज में बैठो। इसके बदले अभी समझ लो कि बैलगाड़ी में अमेरिका नहीं पहुँच सकते अतः अभी से हवाई जहाज में बैठ जाओ.... मर्जी तुम्हारी है।
ऐसे ही जगदाकार वृत्तियों से तुम जगदीश्वर के पास नहीं जा सकते हो। ब्रह्माकार वृत्तिरूपी हवाई जहाज में बैठो तो तुम जगदीश्वर से भिन्न नहीं हो।
वृत्तियाँ तो आप बनाते ही हैं। बम्बई आकार वृत्ति, मद्रासाकार वृत्ति, अहमदाबादाकार वृत्ति, जगदाकार वृत्ति। ऐसी वृत्तियाँ तो आप बहुत बनाते हैं। ये वृत्तियाँ तो सब बैलगाड़ी के चाक घुमाने जैसी हैं। इन वृत्तियों से तो आप देह में ही रहते हैं। देह से पार अपने आप में नहीं आते।
सत्त्वगुण से दयालु वृत्ति बनती है, रजोगुण से अहंकारी वृत्ति बनती है और तमोगुण से द्वेषाकार वृत्ति बनती है। मन में द्वेष आया तो समझो तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण हो गया। वृत्ति में दया आयी, प्रेम आया, शान्ति आयी, आनन्द आया तो समझो सत्त्वगुण है। सत्त्वगुण की वृत्ति भी टिकती नहीं, रजोगुण की वृत्ति भी टिकती नहीं और तमोगुण की वृत्ति भी टिकती नहीं। वृत्तियाँ सदैव बदलती रहती हैं। बदलने वाले को बदलनेवाला समझकर अबदल का साक्षात्कार कर ले उसका नाम है ब्रह्माकार वृत्ति।
न
चलति
भगवतपदारविन्दात्
लव
निमिषार्धमपि।
ब्रह्माकार वृत्तिवाला भगवद् पद से, भगवत् तत्त्व से एक क्षण भी वह चलित नहीं होता। सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियों से काम लेता होगा लेकिन अपनी ऊँचाई पर टिका रहता है। सनकादिक ऋषि पाँच वर्ष के बालक.... क्रीड़ा करते हैं, यात्रा करते हैं लेकिन एक क्षण भी ब्रह्माकार वृत्ति से, भगवदानुभव से दूर नहीं जाते। वशिष्ठजी महाराज उपदेश करते हैं, आश्रम चलाते हैं लेकिन एक क्षण भी ब्रह्माकार वृत्ति से दूर नहीं होते। शुकदेवजी महाराज जंगल छोड़कर बस्ती में आते हैं, रास्ते से गुजरते हैं, लोग कंकड़-पत्थर मारते हैं, अपमान करते हैं लेकिन शुकदेव जी महाराज के लिए सब ब्रह्म है। उन्हें कोई क्षोभ नहीं होता। राजा परीक्षित के दरबार में सोने के सिंहासन पर बैठते हैं तो कोई हर्ष नहीं होता। हर्षाकार, शोकाकार, दुःखाकार वृत्ति का कोई महत्त्व ही नहीं है उनके लिए। ये सारी वृत्तियाँ बाधित हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ठण्ड नहीं लगती, ज्ञानी को सज्जन सज्जन नहीं दिखेगा, दुर्जन दुर्जन नहीं दिखेगा। दिखेगा तो सही लेकिन उसमें सत्य बुद्धि नहीं होगी। उसकी शाश्वतता नहीं दिखेगी।
रस्सी में साँप दिखा। टॉर्च जलाकर देख लिया कि साँप नहीं है, रस्सी है। फिर टॉर्च बंद करके दूर जाकर बैठे तो वहाँ से दिखेगा कि साँप जैसा ही लेकिन साँप की सत्यता गायब हो गई।
ठूँठे में चोर दिखा। टॉर्च जलाकर देख लिया कि चोर नहीं है, ठूँठा है ! फिर दूर से चोर जैसा ही दिखेगा लेकिन वास्तविकता जान ली है।
मरूभूमि में पानी दिखा। वहाँ गये। मरूभूमि को मरूभूमि जान लिया। वापस आ गये। तुम्हारे दोस्त आकर बोलते हैं- 'चलो, उस पानी में नहाकर आयें।' तुम समझाते हो कि वहाँ पानी नहीं है, मैं देखकर आया हूँ। मित्र आग्रह करते हैं तो तुम भी चल पड़ते हो। दस आदमी वे हैं, ग्यारहवें तुम भी तौलिया लेकर साथ में हो लिये। वे लोग जा रहे हैं सत्य बुद्धि से, तुम जा रहे हो, विनोद-बुद्धि से। वे सब जानते हैं कि पानी नहीं है, मरूभूमि है तब वे दुःखी होते हैं जबकि तुम्हें तो विनोद होगा और कहोगे किः मैं तो पहले से ही जानता था।
ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद तुम जगत के साथ यथायोग्य व्यवहार करोगे लेकिन जगत के लोग जगत से सुख पाने की कोशिश करते हैं जबकि तुम्हें पता है कि जगत से सुख नहीं मिल सकता। जैसे मरूभूमि से पानी नहीं मिल सकता ऐसे ही संसार से कोई वास्तविक शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। यह तुम्हें पता है इसलिए संसार का कोई आकर्षण नहीं होगा।
तुम वही होते हो जैसी तुम्हारी वृत्ति होती है। दुकान की वृत्ति करते हो तो तुम दुकान पर हो, घर की वृत्ति करते हो तो तुम घर पर हो, बाजार की वृत्ति करते हो तो बाजार में हो, देह की वृत्ति करते हो तो तुम देह में हो, जाति की वृत्ति की गाँठ बाँधते हो तो जाति वाले हो, सम्प्रदाय की वृत्ति की गाँठ बाँधते हो तो सम्प्रदाय वाले बन जाते हो, भगवदाकार वृत्ति बनाते हो तो भगवान में आ जाते हो, दुःखाकार वृत्ति करते हो तो दुःखी होते हो, सुखाकार वृत्ति बनाते हो तो सुखी होते हो।
ऐसे ही तुम ब्रह्माकार वृत्ति बनाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा।
जो इस ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं, जानकर उसे बढ़ाते हैं वे सत्पुरूष धन्य हैं। वे तीनों लोकों में वन्दनीय हैं।
वे सत्पुरूष क्यों हैं ? कुदरत जिसकी सत्ता से चलती है उस सत्य में वे टिके हैं इसलिए सत्पुरूष हैं। हम लोग साधारण क्यों हैं ? हम लोग परिवर्तनशील, नश्वर, साधारण चीजों में उलझे हुए हैं इसलिए साधारण हैं।
मूलस्वरूप में तुम शान्त ब्रह्म हो। अज्ञानवश देह में आ गये और अनुकूलता मिली तो वृत्ति एक प्रकार की होगी, प्रतिकूलता मिली तो वृत्ति दूसरे प्रकार की होगी, साधन-भजन मिला, सेवा मिली तो वृत्ति थोड़ी सूक्ष्म बन जाएगी। जब अपने को ब्रह्मस्वरूप में जान लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर हाँ हाँ सबकी करेंगे लेकिन गली अपनी नहीं भूलेंगे।
तुम जब अपने-अपने घर जाओगे, अपने-अपने व्यवहार में जाओगे तब अपनी गली याद रखना कि यह तुम्हारा घर नहीं है शरीर का घर है... तुम्हारा व्यवहार नहीं है, शरीर का व्यवहार है।
तुम्हारा घर तो... जो प्रभु का घर है वही तुम्हारा घर है।
वास्तव में तो जिस ईंट, चूने, लोहे, लक्कड़ के घर को तुम 'मेरा' घर मान रहे हो वह घर भी प्रभु का है। जिन चीजों से घर बना है वे चीजें प्रकृति की हैं। प्रकृति परमात्मा की है। कुम्हार ने ईंटें बनाईं मिट्टी, अग्नि, पानी से। मिट्टी, अग्नि, पानी किसी व्यक्ति के नहीं हैं, ये ईश्वर की चीजें हैं। ईश्वर की चीजों से चूना बना, ईश्वर की चीजों से लक्कड़ बना। ईश्वर की ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़ के मिश्रण से घर बना तो यह घर किसका हुआ ? ईश्वर का हुआ।
"बरसात तुम बनाते हो ?"
"नहीं, ईश्वर बनाता है।"
"जमीन तुमने बनाई ?"
"नहीं, ईश्वर ने बनाई।"
"अन्न किसका हुआ ?"
"ईश्वर का हुआ।"
ईश्वर का अन्न खाकर बच्चे पैदा किये। इस बच्चों में ममता हो गई कि ये मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चों में से ममता हटाकर उन्हें ईश्वर के बच्चे समझकर उनका लालन-पालन करो तो अन्तःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ? ये मेरे बच्चे हैं... उन्हें अच्छा बनाऊँ... उन्हें अच्छा पढ़ाऊँ... दूसरे किसी के बेटे अनपढ़ रह जाएँ तो कोई हर्ज नहीं लेकिन मेरे बेटे बढ़िया हों...... यह ममता है। यह देहाकार वृत्ति का परिणाम है। 'दूसरों के बेटे जिस तत्त्व के हैं उसी तत्त्व के ये मेरे बेटे हैं।' इस प्रकार की वृत्ति बनाओगे तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होने में सहाय मिलेगी।
जो पराये हैं उन्हें अपना मानो और जो अपने हैं उन्हें ठाकुर जी के मानो, तुम्हारा व्यवहार, धन्धा, घर-गृहस्थी सब बन्दगी हो जाएगी।
उधार लेकर, करप्शन करके, झूठ बोलकर, काला बाजार करके लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, परिवार को सुखी करने का प्रयास करते हैं लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने घर में, अपने परिवार में हर महीने दो हजार, पाँच हजार आदि का दान करता हूँ। क्योंकि वे यह खर्च ममतावश होकर कर रहे हैं इसलिए दान का फल नहीं मिलता। पाँच रूपये भी अगर किसी अजनबी की सेवा में लगा देते हैं तो अन्तःकरण प्रसन्न हो जाता है कि आज अच्छा काम किया। क्योंकि वहाँ ममता नहीं है।
एक पौराणिक कथा हैः
एक आदमी का जीवन दुर्व्यसन एवं दुश्चरित्र में अस्तव्यस्त हो गया था। वह शराबी भी था, जुआरी भी था और वेश्यागामी भी था। एक बार अपने जन्मदिन पर वह शराबी चाँदी की थाली में स्वस्तिकाकार में मेवा-मिठाई, पान-बीड़ा आदि सजाकर अपनी प्रेयसी गणिका के पास जा रहा था। शराब की प्याली व्याली लगा ली थी। नशे में झूमता जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। चोट लगी तो कुछ देर पड़ा रहा। नशे में तो था ही।
वह ऐसी जगह थी कि जहाँ पुराने शिवालय के अवशेष नजर आ रहे थे। पूर्वकाल में कोई संत पुरूष वहाँ शिवलिंग की स्थापना करके ध्यानस्थ हुआ करते थे। जैसे शिवलिंग में शिव हैं वैसे ही सचराचर सृष्टि में भी शिव ही ओतप्रोत हैं.... ऐसा करके उस ब्रह्मवेत्ता संत पुरूष ने अपनी वृत्ति ब्रह्माकार बनाई थी। समय पाकर वे संत ब्रह्मलीन हो गये। शिवालय भी जीर्ण-शीर्ण हो गया। कालांतर में अवशेष मात्र रह गया।
उसी जगह पर वह शराबी गिर पड़ा। उस भूमि में मिट्टी के कणों का प्रभाव कहो चाहे वहाँ के वायब्रेशनों का प्रभाव कहो, उस शराबी के पूर्व संचित पुण्यों का उदय हुआ।
जो आदमी जहाँ बैठता है और जो विचार करता है, उस आदमी के चले जाने के बाद भी वहाँ उसके विचारों का, वायब्रेशनों का प्रभाव रहता है। कोई आदमी अच्छे विचार करके गया और दूसरा आदमी वहाँ आयेगा तो उसको अच्छे विचार आने लगेंगे। इसी कारण से तीर्थों का महत्त्व है। ध्यान, भजन, साधना, तपस्या करने वाले साधकों का एवं भगवन्नमय रहने वाले संतों का प्रभाव नये आने वाले श्रद्धावान यात्री लोगों को भी लाभान्वित करता है। तीर्थ में जाने से लोगों के विचार पवित्र होने लगते हैं। सिनेमा के थीएटर में जाने से उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में पनपेंगे। सिनेमा के रसियों को आश्रम में ले आओगे तो वे भी 'हरि ॐ' बोलने लग जाएँगे। स्थान का भी प्रभाव होता है।
गाँधी जी किसी गुफा में गये थे। शान्ति से बैठे तो प्रणव की ध्वनि सुनाई पड़ी। गुफा में साधना करने वाले तो चल बसे थे लेकिन प्रणव के जाप का प्रभाव मौजूद था। गाँधी जी लिखते हैं-
"सात्त्विक वृत्ति वाले व्यक्तियों का प्रभाव लम्बे समय तक रहता है यह मेरा अनुभव है।"
वह शराबी गिर पड़ा तो पड़ा रहा सुन्न होकर। अनजाने में वह अहंशून्य हो गया थोड़ी देर के लिए। उसके श्वास में वहाँ का प्राणवायु गया जहाँ के वातावरण में ब्रह्माकार वृत्तिवाले संत पुरूष के वायब्रेशनों का प्रभाव था। शराबी का अन्तःकरण अनजाने में ही थोड़ा निर्मल हो गया। उसको जब होश आया और उठा तो सोचने लगाः
"धिक्कार है मुझे ! एक तो धन कमाने में पाप, फिर शराब पीने का पाप..... और वह भी अपने जन्मदिन पर ! इतना ही नही, मैं उस गणिका के पास जा रहा हूँ जिसने मेरा जीवन और यौवन नोच डाला है ! ऐसी डाइन को पान-बीड़ा देने जा रहा हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन को ! इन पापों का फल मैं कहाँ भोगूँगा ? हाय...."
पश्चाताप से उसके पाप धुलने लगे। चाँदी की थाली में सजाये हुए मेवा-मिठाई, पान-बीड़े आदि सब पदार्थ निर्दोष बच्चों को बाँट दिये।
कथा कहती है कि समय पाकर उसकी मृत्यु हुई और यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने कहाः
"तुम्हारे खाते में पुण्य की दो घड़ियाँ हैं। ब्रह्माकार वृत्तिवाले संत जहाँ रहते थे वहाँ तुमने दो घड़ियाँ बिताई हैं और जिस चीज में ममत्व था उस चीज पर से ममत्व हटाकर अन्य लोगों को बाँटा था। अतः इन दो घड़ी के पुण्य के बदले तुम्हें दो घड़ी स्वर्ग का राज्य दिया जायेगा। तुम्हारे अन्य तमाम पापों के लिए तुम्हें दीर्घ काल तक नर्क की यातनाएँ भुगतनी पड़ेंगी। नर्क की यातनाएँ पहले भोगो या बाद में भोगो, मर्जी तुम्हारी।"
शराबी ने सोचाः नर्क की यातनाएँ तो भोगनी ही पड़ेंगी परन्तु पहले देख लूँ, स्वर्ग का राज्य कैसा है।
उसे स्वर्ग ले जाया गया, सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया गया। उसको विचार आयाः मैं दो घड़ी अच्छी जगह में रहा और थोड़ा सा दान किया तो दो घड़ी तक राज्य मिल रहा है ! अब दो घड़ी में तो स्वर्ग छोड़ना है। जितना हो सके सत्कर्म कर लूँ !
उसने वशिष्ठजी महाराज का आवाहन किया और स्वर्ग की कामधेनु गाय दान में दे दी। विश्वामित्र का आवाहन किया और उच्चैश्रवा घोड़ा उनको दे दिया। कौण्डिन्य ऋषि का आवाहन करके ऐरावत हाथी दे दिया। स्वर्ग की जो-जो मूल्यवान विभूतियाँ थीं वे सब फटाफट ब्रह्मवेत्ता महापुरूषों को दे डाली।
दो घड़ी पूरी हुई। चित्रगुप्त भागता भागता आया और कहाः
"अब आपको यातना भोगने लायक शरीरों में नहीं जाना पड़ेगा। आपके पुण्य बहुत बढ़ गये हैं। आप सम्राट बनेंगे।"
"मैं सम्राट कैसे बनूँगा ?"
"आप ब्रह्माकार वृत्तिवाले संत के स्थान में गये थे और सत्कर्म किया था। यहाँ स्वर्ग में आकर भी आपने भोग नहीं भोगे, भोग का पर हित में खर्च कर दिया। अतः आपको सम्राट बलि का अवतार मिलेगा।"
वही शराबी दूसरे जन्म में परम भागवत प्रह्लाद का पौत्र, विरोचन का पुत्र राजा बलि बना। जिसके पास भगवान को वामन बनकर जाना पड़ा।
......तो ऐसी महिमा है ब्रह्माकार वृत्तिवाले सत्पुरूषों की।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
धर्मानुष्ठान और शरीर-स्वास्थ्य
धर्म से संकल्प मर्यादित होता है, उपासना से संकल्प बलवान होता है, योग से संकल्प के बन्धन कटते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरूषार्थों को सिद्ध करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना नितान्त आवश्यक है। चित्त जितना संयत होता है, स्वास्थ्य के नियम जानने वाला होता है, भोग में नियंत्रण और ज्ञान रखने वाला होता है उतना ही शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है और बुद्धि सत्य-स्वरूप परमात्मा में विश्रान्ति पाकर अपने जन्म-मरण के बन्धन काटने में सफल होती है।
लक्ष्य जितना ऊँचा होता है उतने ही संकल्प शुद्ध होते हैं। ऊँचा लक्ष्य है मोक्ष, ऊँचा लक्ष्य है परमात्मा-प्राप्ति, ऊँचा लक्ष्य है, अनन्त ब्रह्माण्डनायक ईश्वर से मिलना। ऊँचा लक्ष्य तुच्छ संकल्पों को दूर कर देता है। ऊँचा संकल्प जितना दृढ़ होगा उतना ही तुच्छ संकल्पों को हटाने में सफलता मिलेगी। जितना तुच्छ संकल्पों को काट दिया जाएगा, भाग दिया जायगा उतना ही ऊँचा जीवन, ऊँची समझ, ऊँचा स्वास्थ्य, ऊँचा सुख, ऊँची शांति और ऊँचे में ऊँचे परमात्मा की प्राप्ति सुलभ होगी। साधक जब ऊँचे में ऊँचे पद को पाने में सफल हो जाता है तब वह साधक बन जाता है।
पहलवानों की तरह कसरत करना एक बात है और योगियों की तरह सारे शरीर को स्वास्थ्य मिले, कोई हानि न हो, तन-मन की दोष निवृत्त हों इस ढंग से आसन, प्राणायाम, कीर्तन, नृत्य आदि करना निराली ही बात है। यह जरूरी नहीं है कि बलवान पहलवान के जीवन में स्वास्थ्य हो। पहलवान लोग खूब दण्ड बैठक लगाते हैं। इससे मांसपेशियाँ तो स्थूल हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं लेकिन हृदय पर बोझ पड़ता है। नस नाड़ियों के तन्त्र को भी परिश्रम पड़ता है। प्रायः पहलवान लोग बुढ़ापे में रोग के शिकार बन जाते है। उनको जवानी में भी रोग होते रहते हैं।
ऋषियों ने योगासन खोजे हैं।
आसनेन
रजो हन्ति।
आसन से रजोगुण का हनन होता है। रजोगुण में इच्छाएँ-वासनाएँ रहती हैं, बेवकूफी रहती है। आसन करने से रजोगुण क्षीण होता है। सत्त्वगुण बढ़ता है।
सत्वात्
संजायते
ज्ञानम्।
सत्त्वगुण से बुद्धि में सब प्रकार के ज्ञान का प्रकाश पाने की योग्यता बढ़ती है। ऋषि दीर्घ काल तक जीते थे, दीर्घजीवी होते थे लेकिन पहलवान दीर्घायु नहीं सुने गये।
आसन करने से, प्राणायाम करने से नाड़ी तंत्र को, स्वास्थ्य तंत्र को, जठराग्नि को, मस्तिष्क को ठीक से व्यायाम मिलता है। उनमें ठीक से क्षमताएँ विकसित होती हैं। ऋषि पद्धति से जो लोग आसन, प्राणायाम करते हैं उनको डॉक्टरों के इन्जैक्शन एवं केप्सूलों के कारण दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। जो लोग स्वास्थ्य के नियम तथा आसन-प्राणायाम जानते हैं उनको बार-बार हकीमों, डॉक्टरों को परेशान करने का समय नहीं आता है। वे सहज ही स्वस्थ रहते हैं।
मन में जितनी हल्की इच्छाएँ ज्यादा होती हैं उतना चित्त में विक्षेप ज्यादा होता है। मन ज्यादा विक्षिप्त रहता है तो तन बार-बार बीमार पड़ता है। मन में इच्छाएँ, वासनाएँ जोर मारती हैं तो मन विक्षिप्त रहता है, इसको आधि कहते हैं। जिसके मन में आधि आती है उसका तन व्याधियों से घिर जाता है। शरीर व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है तब एलौपैथी दवाइयों से उन व्याधियों को थोड़ा दबाया जा सकता है। लेकिन मन में अगर आधि है तो व्याधियाँ फिर से पनप उठती हैं। एलौपैथी की दवाइयों से रिएक्शन होने की संभावना रहती है। एक व्याधि जाती है तो दूसरी व्याधि आने की संभावना बहुत रहती है। आयुर्वैदिक ढंग से व्याधियों को दूर हटाते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन व्याधियाँ मिटती हैं और बदले में दूसरी व्याधि नहीं आती, अगर आयुर्वेदिक नियम जानने वाला सही वैद्य हो और परहेज पालने वाला मरीज हो तो।
रोग उत्पन्न कैस होते हैं और कुदरती ढंग से निर्मूल कैसे किये जा सकते हैं यह जानना चाहिए। बहुत सारे रोग तो हमारी बेवकूफी की देन हैं। न चिन्तन करने जैसा मन में चिन्तन करते हैं, भय न जगाने जैसा भय जगाते हैं, अनावश्यक उद्वेग जगाते हैं इससे भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानो, हमारा कोई मित्र चला गया या किसी ने हमें कुछ किया तो बार-बार उसका दुःखद चिन्तन करने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है कभी भी दुःखद चिन्तन को महत्त्व नहीं देना चाहिए। मानो हमारे पिता चल बसे। मोह के कारण हम रोयेंगे लेकिन बुद्धि भी है तो उनकी उत्तर क्रिया करके उनकी जीवात्मा को प्रेरणा देंगे कि आपका शरीर नश्वर था। हे पिता ! आपकी आत्मा तो शाश्वत है। आप कभी मरते नहीं। इस जन्म में आपका और मेरा बाप-बेटे का सम्बन्ध था परन्तु ऐसे तो तुम्हारे कई बेटे और हमारे कई बेटे और हमारे कई पिता भी हो गये। आप कौन-कौन से बेटे को याद करेंगे और हम कौन कौन से पिता को याद करेंगे ? इसलिए आप अमरता की ओर चलिये और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए की मैं इस शरीर को मरने वाला समझूँ और स्वयं आत्मा को अमर जानकर मुक्तता का प्रसाद पाऊँ और आप भी अमर हो जाओ। अन्य किसी गर्भ में मत जाओ।
मानो, मेरा इकलौता बेटा मर गया। अखबारों में खबर छप गई कि आसाराम जी महाराज के पुत्र का निधन हो गया। लोग मिलने को आयें और मैं रोता रहूँ तो वह मेरी बेवकूफी है। मैं आपसे कहूँ- "मेरा बेटा मर गया, व्यावहारिक जगत में यह कहना ठीक होगा शायद, लेकिन वास्तव में मेरा बेटा कभी पैदा ही नहीं हुआ था। पैदा हुआ था पंचभौतिक शरीर और पंचभौतिक शरीर पाँच भूतों में लीन हो गया। बाकी आत्मा-परमात्मा तो अद्वितीय स्वरूप है। उसमें कौन जन्मा और कौन मरा ? सामाजिक मान्यताओं के कारण हम एक दूसरों को आश्वासन देते हैं क्योंकि हम बहुत नीचे जगत में जीते हैं। बुद्ध पुरूषों के, ज्ञानवानों के अथवा सत्शास्त्रों के विचारों में हम नहीं जीते इसलिए हमें परेशानी होती है। आपकी शुभ भावना से मुझे ऐसी परेशानी नहीं है। आप लोग बैठिये, सत्संग सुनिये, प्रसाद पाइये, आनन्द में रहिए।"
आने वालों को मैंने सान्तवना दे दी क्योंकि मेरे अन्तःकरण में बेवकूफी के बदले गुरू की कृपा का प्रसाद है।
धन से बेवकूफी नहीं मिटती है, सत्ता से बेवकूफी नहीं मिटती है, तपस्या से बेवकूफी नहीं मिटती है, व्रत रखने से बेवकूफी नहीं मिटती है। बेवकूफी मिटती है ब्रह्मज्ञानी महापुरूषों के कृपा-प्रसाद से और सत्संग से, सत्शास्त्रों की रहमत से।
दुनियाँ में जो भी दुःख हैं उनके मूल में बेवकूफी काम करती है। जितनी बेवकूफी प्रगाढ़ होगी उतना दुःख प्रगाढ़ होगा। जितनी बेवकूफी शिथिल होगी उतना दुःख शिथिल होगा। बेवकूफी चली गई तो तुम आनन्दस्वरूप बन जाते हो। हमारी और ईश्वर की जात एक होते हुए भी हम बेवकूफी के कारण अपने को दीन, हीन, दुःखी, जन्मने-मरनेवाला बनाकर परेशान हो रहे हैं।
स्वास्थ्य के नियम न जानने से आदमी बार-बार बिमारियों का शिकार होता रहता है। जो बार-बार बीमार होता है वह कुदरत के नियमों से टक्कर लेता है, अर्थात् वह कुदरत का अपराधी है। जो कुदरत का अपराधी है वह बिमारीरूपी सजा बार-बार भोगता है।
परदेश में धर्म का नियंत्रण नहीं है इसलिए वासनाओं का विस्तार खूब है। वासनाओं के विस्तार के कारण लोग बार-बार बिमार होते हैं। इसलिए हमारे बच्चे जैसे मूँगफली, चना खाते हैं वैसे परदेशी लोग सुबह से शाम तक टेबलेटस खाते रहते हैं। सुबह की अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, रात की अलग..... न जाने कितनी ही किस्म की गोलियाँ जेब में रखते हैं। इतना दयनीय और पराधीन जीवन है उनका।
वहाँ के मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर कहते हैं- अगर पचास वर्ष में किसी को हार्ट एटैक या हाई बी.पी. नहीं हुआ तो वह अमेरिका में जिया ही नहीं, वह धनवान होकर जिया ही नहीं, बड़ा आदमी होकर जिया ही नहीं। बड़े आदमी की निशानी ही यही है कि उसे हाई बी.पी. या हार्ट एटैक हो। वास्तव में वह बड़ा आदमी नहीं है। वह बिलकुल छोटा आदमी है। छोटी-छोटी इच्छाओं के पीछे अपने को खपाया है। बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उस परमात्मा को पाये हुए महापुरूषों की शरण उसने नहीं ली इसलिए वह बड़ा आदमी दिखते हुए बेवकूफी आदमियों की लाइन में आ जाता है।
जो अपने तन की तन्दुरूस्ती की सुरक्षा न कर सके, अपने मन को दुःख से न बचा सके उसके बड़प्पन को हम क्या करेंगे ?
संसार है..... कोई जन्मेगा कोई मरेगा, कोई आयेगा कोई जाएगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी.... इसी का नाम तो दुनियाँ हैं। साईकिल पर जाते हैं, कार में जाते हैं तो कभी चढ़ाव आते हैं कभी उतार आते हैं। उतार आया तो मजे से गाड़ी जा रही है, तो क्या वही बैठे रहोगे ? चढ़ाव को देखकर घबरा जाओगे क्या ? चढ़ाव को भी लाँघते जाओ, उतार को भी लाँघते जाओ, अपना मार्ग काटते जाओ। ऐसे ही अनुकूलता को भी लाँघते जाओ प्रतिकूलता को भी लाँघते जाओ।
प्रमोशन मिल गया, अनुकूल पद मिल गया तो साधन-भजन की रूचि खत्म हो गई। वह बेवकूफ आदमी माना जाता है। ऐसा सत्य कहने का अधिकार सदगुरू को होता है और सदगुरू जैसा हितैषी दुनियाँ में कोई नहीं हो सकता।
सत्गुरू
मेरा शूरमा
करे शब्द की
चोट।
मारे
गोला प्रेम का
हरे भरम की
कोट।।
मन में आधि पैदा करना यह भरम है। यह नहीं हुआ.... वह नहीं हुआ... ऐसा नहीं मिला... वैसा नहीं मिला.... ऐसा क्यों हुआ... वैसा क्यों हुआ... इससे मन में आधि जमा होती है। आधि जमा होने से शरीर में व्याधि आ जाती है। आदमी सुयोग्य होते हुए उसकी सारी योग्यताएँ दब जाती हैं। अच्छा होते हुए, नम्र होते हुए, दानी होते हुए, भक्त होते हुए भी छोटी सी गलती उसकी सारी भक्ति को, सारी नम्रता को, सारी योग्यताओं को दबा देती है।
जैसे, खीर बनाई है। उसमें सारे मसाले हैं, शक्कर है, बदाम है, पिस्ता है लेकिन बेवकूफी से दहीवाला चम्मच उस खीर में घुमाने लग गया। हो गया काम पूरा।
चम्मच जरा दहीवाला था.... मुझे पाता नहीं था..... मैंने जानबूझकर तो नहीं डाला। जरा सा चम्मच डाल दिया तो क्या हुआ ?
अरे मूर्खानन्द ! सब खत्म हो गया।
ऐसे ही हम अपने जीवन में आधि का चम्मच ले आते हैं तो किया कराया सब चौपट हो जाता है। खीर खाकर तृप्ति होने वाली थी, उसके बदले हम भूखे रह जाते हैं। दान, पुण्य, सत्कर्म करके आत्म-तृप्ति का अनुभव होना चाहिए उस अनुभव को पाने का अधिकार हम खो बैठते हैं।
तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा हैः
गुरू
बिन भवनिधि
तरहिं न कोई।
चाहे
बिरंचि शंकर
सम होई।।
संसाररूपी सागर को कोई अपने आप तर नहीं सकता। चाहे ब्रह्माजी जैसे सृष्टिकर्त्ता हों, शिवजी जैसे संहारकर्त्ता हों फिर भी अपने मन की चाल से, अपनी मान्यताओं के इन जंगल से निकालने के लिए पगडण्डी दिखाने वाले सदगुरू अवश्य चाहिए।
सत्संग में आप लोगों के साथ ये उद्योगपति बैठे है। पहले वे समझते थे किः "हम करोड़ों कमाते हैं, लाखों का दान करते हैं, लोग बोलते हैं गुरू करो..... गुरू करो। अब हमें गुरू करने की क्या जरूरत है ? हमारे पास किस बात की कमी है ? हजारों लोगों को हम प्रभावित करते हैं, बड़े-बड़े उदघाटन करते हैं, बड़ी-बड़ी संस्थाओं में हम ट्रस्टी हैं।
जब सदगुरू के द्वार पर आये, सत्संग सुना तब पता चला कि उस समय की हमारी मान्ताएँ बेवकूफीवाली थी, अब कुछ महसूस होता है कि ठीक रास्ते पर आये हैं।"
भगवान के राम के गुरू थे और भगवान श्रीकृष्ण के भी गुरू थे। राजा जनक के भी गुरू थे। ऐसे गुरू नहीं जो तुम्हारी खुशामद करते रहें। वे पण्डा हो सकते हैं या दुकानदार हो सकते हैं जो शिष्यों की, भक्तों की खुशामद करते हैं। तुम्हारी उन्नति के लिए अनुशासन करने में तुम्हारा लिहाज न रखें, तुमको डाँट सकें, तुम्हारा कान पकड़ सकें, तुम्हारी कल्पित मान्यताओं के गढ़ को गिरा सकें वे सदगुरू होते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बाहर से ठोकता है लेकिन भीतर हाथ रखकर उसे सुरक्षित भी रखता है ऐसे ही तुम्हारे जीवन को सदगुरू आत्मिक प्रेम की वर्षा से सुरक्षित भी बनाते हैं और दोष निकालने के लिए कठोर अनुशासन भी करते है। कुम्हार के घड़े में तो पानी भरा जाएगा लेकिन सदगुरू के द्वारा परिशुद्ध किये गये तुम्हारे जीवनरूपी घड़े में परमात्मा प्रकट होता है। कुम्हार मिट्टी में से घड़ा बनाता है जबकि सदगुरू जीव में से ब्रह्म बनाते हैं, जीव को अपने शिवस्वरूप में जगाते हैं।
इसलिए तुम भूलकर भी ऐसे महापुरूषों का दामन मत छोड़ना। उनके द्वारा तुम्हारी पिटाई-घुटाई को अपनी बेइज्जती मानकर भाग मत जाना, धन्यवाद से भर जाना कि कितना ध्यान रखते हैं ! वे अपना समझते है तभी अनुशासन करते हैं। पराये बच्चे पर थोड़ा ही अनुशासन चलाया जाता है ! पराये बच्चे को चॉकलेट दी जाती है। माँ अपने बच्चे को ही तमाचा मार सकती है। सदगुरू ने हमको अपना समझा है इस बात से तुम धन्यवाद से भर जाना। उनके प्रति फरियाद दिल में कभी भी नहीं लानी चाहिए।
तेरे
फूलों से भी
प्यार तेरे
काँटों से भी
प्यार......।
माँ मिठाई देती है तो उसमें उसका प्यार ही है, पर जब थप्पड़ मारती है तब वह भी प्यार का ही एक रूपान्तर है।
ऐसे सदगुरूओं के चरणों में जब हम पहुँचते हैं तब हमारी आधियाँ क्षीण होने लगती हैं। मन की आधियाँ कम होने से तन की व्याधियाँ भी कम हो जाती हैं।
व्याधि प्राकृतिक वातावरण के परिवर्तन से भी होती है, तरतीव्र प्रारब्धवेग से भी होती है, पाँच-दस प्रतिशत। बाकी 80-90 प्रतिशत व्याधियाँ अपनी बेवकूफी के कारण होती हैं।
उसके पास यह है, मेरे पास नहीं.... मेरा यह मर गया... मेरा वह चला गया... मेरी नौकरी चली गई.... ऐसी चिन्ताओं से पाचनतंत्र एवं ज्ञानतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चिन्तन करना ठीक है लेकिन चिन्ता करना हानिकारक है।
मेरे
चिन्तयो होत
नहीं हरि को
चिन्तयो होय।
हरि
को चिन्तयो
हरि करे मैं
रहूँ
निश्चिन्त।।
हम अपने आपको ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारी कब किस ढंग से उन्नति करना यह बहुत ठीक ढंग से वह जानता है। उसके आगे हमारी मति क्या है ? दुनियाँ की सारी मतियाँ मिलकर भी खोज-खोजकर थक जाती हैं, मतियों का अन्त होता है तब वेदान्त का श्रीगणेष होता है।
हम अपनी मति से परिस्थितियों को, भगवान को, सदगुरू को तोलते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। शास्त्र की मति से, सदगुरू की मति से अथवा ईश्वरार्पण मति से जब सोचते हैं तब मन की आधियाँ कम हो जाती हैं और तन की व्याधियाँ भी क्षीण होने लगती हैं।
शरीर की व्याधियाँ कुछ तो औषध से दूर होती हैं कुछ प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होती हैं। बहुत सारी व्याधियाँ उपवास से भी दूर होती हैं और जप से, दान से, पुण्य से भी आधि-व्याधि क्षीण होती है।
रोक फेलर व्याधिग्रस्त हो गया। मन में खूब आधि थीः 'और पैसा कमाऊँ... और पैसा कमाऊँ.....।' आधि ने ऐसी व्याधि ला दी कि डॉक्टरों ने कहा छः महीनों से ज्यादा नहीं जी सकते।
किन्ही समझदारों ने बताया कि हाय पैसा.... हाय पैसा.... करके जगत का चिन्तन कर रहे हो उसके बदले में पैसे का सदुपयोग करो। दूसरों के कल्याण में पैसे खर्च कैसे करें ऐसी योजना बनाओ।
रोकफेलर ने लोककल्याण के लिए पैसे खर्च करना चालू कर दिया। डॉक्टरों ने कहा था कि छः महीनों में मर जाओगे लेकिन रोक फेलर उसके बाद 32 साल तक जिया।
दान से, सत्कर्म से मन की आधियाँ नष्ट होती हैं क्योंकि ध्यान, भजन, सत्संग से मन के दूषित संकल्प क्षीण होते हैं और शुभ संकल्प फलते हैं। शुभ संकल्प फलते हैं तो आदमी का शुभ होने लगता है।
यश, धन और भोग ये तीन प्रकार से प्राप्त होते हैं। किसी आदमी को कब धन मिल जाए वह नहीं जानता, कब यश मिल जाय वह नहीं जानता, यश कब अपयश में बदल जाए वह नहीं जानता।
यश, धन और भोग एक तो मिलते हैं पूर्व संचित सुकृत के बल से, पहले किये हुए पुण्यों के बल से। परिश्रम तो सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि निर्धन परिश्रम नहीं करता। कुछ धनवान ऐसे हैं जो थोड़ा-सा परिश्रम करते हैं और बहुत सारा धन कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवनभर परिश्रम करते हैं और मुश्किल से आजीविका चला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवनभर परिश्रम करते हुए भी गरीबी की रेखा से नीचे ही रहते हैं। हालाँकि उनको किसी दाता के द्वारा या सरकार की ओर से कुछ भी सुविधा मिल जाय फिर भी उनको दूषित इच्छाएँ, हल्की इच्छाएँ उनको बरबाद कर देती हैं। शराब, कबाब में या सत्ते-पंजे में अपनी पूँजी नष्ट कर देते हैं। फिर वहीं के वहीं।
कई झोंपड़ी वालों को पक्के मकान मिले। वे लोग दो-दो हजार में मकान बेचकर फिर झोंपड़े में बैठ गये। उन मकानों की अभी साठ-साठ हजार गुडविल चलती है। अपनी बेवकूफी के कारण कई लोग वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। पुण्य के अभाव के कारण भी ऐसी बेवकूफी आ जाती है। ज्ञान के अभाव के कारण भी बेवकूफी आ जाती है। कुल मिलाकर कहा जाय तो बेवकूफी का फल ही दुःख है।
जिसको हम चतुराई समझते हैं वह चतुराई अगर शास्त्र, सदगुरू और भगवान से सम्मत नहीं है तो वह चतुराई भी बेवकूफी है। वकालत में चतुर हो गये, इधर का उधर, उधर का इधर... दो वकील पार्टनर बन गये। एक मुवक्किल इसका एक मुवक्किल उसका। जो मुवक्किल ज्यादा पैसा दे उसके पक्ष में केस करा दिया। न्यायाधीश को अपने पक्ष में ला दिया। बड़ी चतुराई दिखती है। लेकिन ऐसी चतुराई से कमाया हराम का पैसा बेटी और बेटे की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बेटा-बेटी अनैतिक मार्ग पर चले जाते हैं।
पूर्वसंचित सुकृत से यश, धन और भोग मिलते हैं। दूसरा, वर्त्तमान के उद्योग से, पुरूषार्थ से यश, धन और भोग मिलते हैं। वर्त्तमान में एक होता है मनमाना पुरूषार्थ। इससे अल्पकालीन यश, धन और भोग मिलता है। दूसरा होता है धर्ममर्यादा को ख्याल में रखते हुए किया गया उद्योग। इससे लम्बे समय तक रहने वाला यश, धन और भोग मिलते हैं। तीसरा, किसी की कृपा से, अनुग्रह से यश, धन और भोग मिलते हैं। धनवानों का, धर्मात्माओं का, देवताओं का और भगवान का अनुग्रह यश, धन और भोग की प्राप्ति कराता है। अनुग्रह होने पर विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता।
आदमी जब ईमानदारी का सहारा लेता है, सच्चाई का सहारा लेता है तो धन, यश और भोग लम्बे समय तक टिकते हैं, सुखद बनते हैं। बेईमानी से पाया हुआ धन, यश और भोग अल्पकालीन होगा और उतना सुखद नहीं बनेगा। हृदय में शान्ति नहीं होगी। बुद्धि अच्छे मार्ग में नहीं जाने देगी।
अगर थोड़ी बहुत भक्ति की जाय सेवा की जाय, ईमानदारी से धन, यश, भोग प्राप्त किय जायें तो वे भगवान के मार्ग पर ले जाएँगे।
धनवान बहुत लोग होते है। जिनका धन पाप और शोषण से इकट्ठा हुआ है उनको भगवान और संत में श्रद्धा नहीं होगी। जिनको थोड़ा-बहुत सत्कर्म करते हुए धन मिला है उनको भगवान और संत में श्रद्धा होगी। भगवान और संत में श्रद्धा होने से वे धनवान स्थायी धन, स्थायी यश और स्थायी भोग के अधिकारी बनने लगते है। धीरे-धीरे वे आत्म-प्रसाद भी पा लेते हैं। कितना बड़ा अधिकार है। भगवान, संत और शास्त्रों में श्रद्धा नहीं हो रही तो ऐसे धनवान की मति जैसे-तैसे भोग में अपने को खत्म कर देती है।
पैसा है लेकिन भीतर में खुशी नहीं है तो वह धनवान नहीं है, निर्धन है। तन्दुरूस्ती नहीं है तो वह निर्धन है। पति-पत्नी के बीच, पुत्र परिवार के बीच स्नेह नहीं है तो वह धन किस काम का ?
धर्म से वासनाएँ नियंत्रित होती हैं। वासनाएँ नियंत्रित होने से अंतःकरण में बल आता है और मन की आधियाँ क्षीण होती हैं। मन की आधियाँ क्षीण होने से तन की व्याधियाँ कम हो जाती हैं।
अधर्म की वासनाएँ भड़कती हैं, मन में आधियाँ बढ़ती हैं और शरीर की व्याधियाँ भी बढ़ती हैं।
विद्यार्थी बच्चों का धर्म है ब्रह्मचर्य पालना, नासाग्र दृष्टि रखना। पहले के जमाने में बालक पाँच साल का होते ही गुरूकुल में भेज दिया जाता था। पच्चीस साल का होने तक वहीं रहता था, ब्रह्मचर्य पालता था, विद्याध्ययन एवं योगाभ्यास करता था। गुरूकुल से वापस आता तब देखो तो शरीर सुडौल, मजबूत। कमर में मुँज की रस्सी बँधी हुई और उस रस्सी से लंगोट खींची हुई होती थी। वे जवान बड़े वीर, बड़े तन्दुरूस्त, बड़े स्वस्थ होते थे। उस समय समरांगण में योद्धा के बल की तुलना हाथियों के बल से की जाती थी। कोई योद्धा दो हजार हाथियों का बल रखता था, कोई पाँच हजार और कोई दस हजार। अभी का आदमी तो उसे गप्प ही समझता है। उसकी बुद्धि ऐसी छोटी हो गई है। उस काल में तो बड़े-बड़े अदभुत वीर हो गये हैं।
वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स और राजा रघु की कथा है।
कौत्स विद्याध्ययन करके गुरूकुल से विदा ले रहा था। वह गुरू जी से बोलाः
"गुरूजी ! मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, गुरूदक्षिणा देना चाहता हूँ। आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूँ ?"
गुरूजी बोलेः "बेटा ! तू गरीब ब्राह्मण है। क्या सेवा करेगा तू ? आश्रम में इतने साल तक तुमने शरीर से सेवा की। अब दक्षिणा से सेवा नहीं करोगे तो भी चलेगा बेटा ! कोई जरूरत नहीं है। जाओ, आनन्द करो। धर्म का प्रचार-प्रसार करो, दूसरों को एवं अपने को उन्नत करो।"
गुरूजी ! बिना दक्षिणा के विद्या स्थिर नहीं रहती। इसलिए कृपा करो, आज्ञा दो, आप जो माँगेंगे वह दक्षिणा ला दूँगा।"
गुरू ने देखा कि है तो कंगाल और फिर भी कहता है जो माँगोगे वह दूँगा ! वे बोलेः
"अच्छा बेटा ! तू आश्रम में चौदह साल रहा है तो चौदह सहस्र सुवर्ण मुद्राएँ ले आ। हालाँकि मैंने जो दिया है उसका पूरा बदला नहीं है फिर भी इतने से चल जाएगा।"
उस जमाने में जो आदमी बोल देता था उसका मूल्य रखता था। बोला हुआ वचन पालता था। कौत्स प्रणाम करके विदा हुआ। सोचने लगाः चौदह सहस्र सुवर्ण मुद्राएँ मुझ ब्राह्मण को कौन दे सकता है ? और कोई नहीं, केवल दाता शिरोमणि राजा रघु ही दे सकते हैं। कौत्स घूमता-घामता राजा रघु के राज्य में गया। उन्ही राजा रघु के कुल में भगवान श्रीराम अवतरित हुए। धर्मात्मा लोग होते हैं वहीं भगवान और संत अवतरित होते हैं। उन्हीं लोगों को स्थायी यश मिलता है। राम जी के साथ राजा रघु का नाम जुड़ गया।
रघुकुल
रीत सदा चली
आई।
प्राण
जाय पर बचन न
जाई।।
रामचन्द्रजी आदर से सिर झुकाते हैं, मैं रघुकुल का हूँ ऐसा कहकर रघुकुल का गौरव व्यक्त करते हैं।
ऐसे राजा रघु के राज्य में कौत्स पहुँचा। लेकिन राजा रघु तो अपना पूरा राज्य अपने शत्रु को दे बैठे थे। स्वयं जंगल में जाकर झोंपड़ी में रहते थे, मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे।
हुआ ऐसा था कि राजा रघु के राज्य का वैभव देखकर उनके शत्रु ने राज्य पर चढ़ाई कर दी। मंत्रियों ने राजा रघु से कहा किः
"पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है। वे हमसे युद्ध करना चाहते हैं।"
"वे युद्ध क्यों करना चाहते हैं ?"
"उनको यह राज्य चाहिए ?"
"अच्छा ! उनको राज्य करने की वासना है। ठीक है। अब बताओ, वे प्रजा का पालन कैसा करते हैं ? वात्सल्य भाव से करते है कि शोषण भाव से ?"
"अपनी प्रजा का पालन तो खूब वात्सल्य भाव से करते हैं।"
राजा रघु बोलेः
"प्रजा का अच्छी तरह पालन ही करना है तो इस शरीर से हो या उस शरीर से हो, क्या फर्क पड़ता है ? नाहक लोगों की मार-काट हो स्त्रियाँ विधवा बनें, माताएँ पुत्रहीन बनें, बहनें अपने दुलारे भाई को खो बैठें, मासूम बच्चे पिता की छत्रछाया खोकर अनाथ बन जाएँ यह तो अच्छा नहीं है। युद्ध करने से तो यह सब होगा।
मंत्रीगण ! जाओ, उनको बुलाओ। उनसे कहो कि राजा रघु तुम्हें ऐसे ही राज्य दे देना चाहते हैं।"
शत्रु राजा आये। उनके हृदय में पूरा यकीन था कि राजा रघु वास्तव में धर्मात्मा हैं और जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। उनके आते ही राजा रघु ने राजतिलक कर दिया। अपना सारा राज्य सौंप दिया।
राजा रघु ने तो स्वेच्छा से अपना राज्य दे दिया लेकिन प्रजा का हृदय तो रघु से जुड़ा था। शत्रु राजा ने घोषणा करवाई कि राजा रघु को जो कोई स्थान देगा, सहारा देगा, उसे मृत्युदण्ड दिया जाएगा। मृत्युदण्ड के भय से लोग खामोश रह गये। राजा रघु के लिए हृदय पिघल रहा था फिर भी कुछ नहीं कर पाये।
राजा रघु जंगल में चले गये। ठीकरे में भिक्षा माँगकर खा लेते, कंदमूल से गुजारा कर लेते, एक झोंपड़ी में रह लेते। आत्मा-परमात्मा की साधना के मार्ग में लग गये।
राज्य छोड़ना उनके तरतीव्र प्रारब्ध में होगा। उन्होंने राज्य छोड़ा तो धर्मानुकूल रहकर राज्य छोड़ा, अपनी खुशी से, स्वेच्छा से छोड़ा। राज्य से चिपके रहते, मरते-मरते छोड़ते तो इतिहास में ऐसे चमकते नहीं।
वह ब्राह्मण कुमार कौत्स राजा रघु के राज्य में आया। उसे पता चला कि उनके स्थान पर तो दूसरा राजा है। राजा रघु कहीं जंगल में वनवासी भिक्षुक होकर रहते हैं। कौत्स को राजा रघु की महिमा का पता था, उन पर श्रद्धा थी कि राजा न होने पर भी वे सहायरूप बनेंगे ही। वे सदा श्रीसम्पन्न राजवी हैं।
घूमते-घामते आखिर कौत्स राजा रघु की पर्णकुटि खोज ही ली।
सुबह का समय था। पूर्वाकाश में प्रातः के सुनहरे सूर्य का उदय हो रहा था। राजा रघु सूर्य के सामने प्रातः सन्ध्या करने बैठे थे। कौत्स ने देखा कि राजा रघु के सन्ध्या वन्दन करने के पात्र सुवर्ण के तो नहीं हैं, अन्य धातु के भी नहीं हैं। मिट्टी के पात्र से सन्ध्या कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं।
कौत्स निराश हो गया। जिनके पास बर्तन भी मिट्टी के बचे हैं ऐसे राजा रघु से चौदह सहस्र सुवर्ण मुद्राएँ क्या माँगना ? वह बिना कुछ कहे वापस लौट पड़ा।
राजा रघु का ध्यान उधर गया। एक ब्राह्मण कुमार कुछ कहे बिना वापस जा रहा है, क्या बात है ? उन्होंने कौत्स को बुलाया। उनके आग्रह करने पर कौत्स ने अपनी बात बताई, वहाँ आने का प्रयोजन बताया और आखिर कहाः
"महाराज ! विधाता ने क्या कर दिया ?"
"क्यों निराश होता है विप्र ! प्रारब्ध में जो होना होता है, होता है। रो-रोकर भोगें या हँसकर भोगें, हमारी मर्जी की बात है। विपत्ति आने से हमको क्या फर्क पड़ता है ?"
"महाराज ! आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम जैसे याचकों का तो सब कुछ चला गया। आप जैसे दाता भिखारी हो गये तो हमको मुँह माँगा दान कौन देगा ? हे विधाता ! तूने क्या कर दिया ?"
"अरे ब्राह्मण ! तू अपने को कोस मत, विधाता को दोष मत दे। बोल तेरा अभीष्ट क्या है ?"
"अब आप क्या देंगे ? आपके पास मिट्टी के बर्तनों के अलावा बचा ही क्या है ? अब मुझे गुरूदक्षिणा देने के लिए चौदह सहस्र सुवर्ण मुद्राएँ कौन देगा ?"
राजा रघु ने कहाः "पागल ! निराश मत हो। ठहर में अभी सुवर्ण मुद्राएँ दे देता हूँ।"
राजा रघु ने गहरी साँस ली। प्राणायाम किया।
प्राणशक्ति जितनी सूक्ष्म होती है उतना संकल्प बलवान होता है। इस विषय में आप लोग नहीं जानते। मैं भी पूरा नहीं जानता। थोड़ा बहुत जानता हूँ उससे बहुत लाभ मिलता है।
तुम जो श्वास लेते हो वह स्थूल प्राण है। तुम नियम से प्राणायाम और योगासन का विधिपूर्वक अभ्यास करो तो तुम्हारा प्राण सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म प्राण होने पर संकल्प शक्ति का विकास होता है। उसके द्वारा बहुत बड़े कार्य हो सकते हैं। योगी पुरूषों का तो यहाँ तक कहना है कि तुम्हारे प्राण सूक्ष्मतम हो जाएँ तो तुम आकाश में स्थित सूर्य और चन्द्र को गोलों की तरह अपने संकल्प से चला सकते हो और ठहरा सकते हो। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र ये सब प्राणशक्ति से संचालित होते हैं। प्राण जितना सूक्ष्म होता है उतना आदमी का बल बढ़ता है।
जैसे, अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ। मैं आसन करके आया हूँ। मेरे प्राणों का तालमेल सही है। मैं बोलूँगा तो लोग मेरे प्रवचन से ज्यादा तत्पर हो जाएँगे। अगर मेरे प्राणों की रिधम (ताल) ठीक नहीं है, मेरे प्राण सूक्ष्म नहीं बने हैं, मेरे मन में पवित्रता नहीं है तो इससे भी बढ़िया बढ़िया कथाएँ या बातें रटकर सुना दूँ तो तुम्हें ऐसा आनन्द नहीं आयेगा। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर ऐसे लेक्चर करने वाले लोग बहुत होते हैं। उनको सुनने के लिए दो लोग बैठते हैं तो दो लोग उठते हैं, आते जाते रहते हैं। उनमें और संतों में यही फर्क है कि संतों का जीवन धर्मानुकूल है। मन में विकारों को क्षीण करने की शक्ति आयी है। जैसे हीरे से हीरा कटता है ऐसे मन से ही मन के विकार काटे जाते हैं।
शुभ संकल्प, प्राण की रिधम को, गुरू के मार्गदर्शन को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, संकल्प उन्नत किया है इसलिए उनके प्राण की गति ऊँची हो गई, सूक्ष्म हो गई। तभी उनकी वाणी का प्रभाव पड़ता है।
जिस दिन मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ, मेरे प्राण की रिधम सही होती है उस दिन सत्संग प्रवचन में जो भी विषय हो, जो भी मैं बोलूँगा तो आनन्द ही आनन्द आयेगा। जिस दिन मेरे प्राणी की स्थिति ठीक नहीं होती, प्राण किसी रोग निवृत्त करने में लगे हैं उस दिन मेरे बोलने का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। यह मेरा अनुभव है।
इन्द्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। धर्म का अनुष्ठान करने से मन और प्राण को नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है।
धर्मात्मा राजा रघु ने कौत्स से कहाः
"पागल ! निराश क्यों होता है ? ठहर। मैं क्षत्रिय हूँ। तुम ब्राह्मण हो। माँगना तुम्हारा अधिकार है और देना मेरा कर्त्तव्य है। देने के लिए मेरे पास द्रव्य नहीं है तो मैं युद्ध करके भी ला सकता हूँ। इस धरती के लोगों से क्या युद्ध करना ! वह युद्ध कब निपटे ? मैं तो अपने बाण का निशाना बनाता हूँ कुबेर भण्डारी को।"
राजा रघु ने उठाया धनुष। सरसंधान किया। कुबेर को ललकारा किः "या तो चौदह सहस्र सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।"
देवताओं के खजानची के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य धर्मात्माओं में होता है। दुरात्मा बेचारे क्या कर सकते हैं !
जिनके संकल्प हल्के हैं वे बच्चे बच्चों को जन्म देने लग गये। अभी वे मर्द हुए ही नहीं और बच्चे पैदा करने लग गये। ऐसे लोगों के मन और प्राण दुर्बल होते हैं। वे लोग यह बात समझने के भी काबिल नहीं होते। सत्शास्त्र की बात मति माने तो भी सत्य होती है और मति न माने तो भी सत्य होती है।
वैशम्पायन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को कथा सुना रहे थे। जन्मेजय बात में सन्देह कर कहने लगाः
"गुरूजी ! आप कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीम ने हाथियों को ऐसे जोर से घुमाकर आकाश में फेंका कि वे अभी तक आकाश में घूम रहे हैं। यह कैसे हो सकता है ? इतनी गप्प ! गुरूजी ! कुछ तो मर्यादा रखो। मैं जन्मेजय हूँ। सारा राज्य सँभालता हूँ। मेरे आगे आप ऐसी बात कर रहे हैं ?"
वैशम्पायन ने कहाः "हे मूर्ख ! तेरी मति समझने के काबिल नहीं है तो शास्त्र और संत की बात में अविश्वास करता है ?"
वैशम्पायन जी ने सूक्ष्म प्राण का उपयोग किया, संकल्प शक्ति का उपयोग किया, हाथ ऊँचा किया और झटका मारा तो आकाश से एक हाथी आकर वहाँ गिरा। वैशम्पायन ने कहाः
"भीम ने जो हाथी फेंके थे और अभी आकाश में गुरूत्वाकर्षण से बाहर जाकर घूम रहे हैं उनमें से यह एक हाथी है, देख ले मूर्ख ! अब तो विश्वास करेगा ?"
हमारे देश में ऐसे योगी हो गये हैं। ऐसी क्षमता सबके अंतःकरण में बीज रूप में पड़ी है। लेकिन हम धर्म का महत्त्व नहीं जानते, संयम का महत्त्व नहीं जानते इसलिए वे शक्तियाँ विकसित नहीं होती। इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, विकारी केन्द्रों में चले जाते हैं। इससे कितना पुण्यनाश होता है, बाद में कितनी बेइज्जती होती है, कितना दुःख उठाना पड़ता है इसका गणित हम नहीं जानते। छोटे-छोटे आकर्षणों में अपना सर्वनाश कर देते हैं।
सती अनसूया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को बालक बना दिया। सती शांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया। हम यह शास्त्रों में पढ़ते हैं लेकिन इन सबको कल्पनाएँ समझ लेते हैं।
कथा कहती है कि राजा रघु ने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुबेर को पता चला कि अरे ! ये तो राजा रघु हैं ! राजा रघु से युद्ध ! ना.... ना.... ना.... असम्भव। कुबेर भण्डारी ने सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। राजा रघु ने कौत्स से कहा कि ले ले ये सुवर्ण मुद्राएँ। कौत्स ने गिनकर चौदह सहस्र सुवर्ण मुद्राएँ ले ली। फिर भी काफी बच गई। राजा रघु ने कहाः
"मैंने तेरे लिए ही ये सुवर्ण मुद्राएँ मँगवाई हैं, मेरे लिए नहीं। अतः हे विप्र कुमार ! ये सारी सुवर्ण मुद्राएँ तू ही ले जा।"
कौत्स कहता हैः "मुझे गुरूदक्षिणा में चौदह सहस्र देनी हैं, उतनी मैंने ले ली। इससे एक भी ज्यादा मुझे नहीं चाहिए।"
राजा रघु बोलेः "ये मुद्राएँ तेरे निमित्त आयी हैं। उन्हें लेना मेरा हक नहीं है।"
कितना धर्म का अनुशासन स्वीकार किया है ! अपने मन पर कितना संयम है ! लोग घोड़े पर जीन रखकर, रकाब बाँधकर उसमें पैर रखकर सवारी करते हैं। ऐसे ही मन पर यदि धर्म और संयम का जीन और रकाब रखकर सवारी की जाय तो.... घोड़ा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है परन्तु मनरूपी घोड़ा जीवात्मा को परमात्मामय बना देता है।
कौत्स बोलता हैः "राजन् ! मुझे जितनी आवश्यक हैं उतनी ही मुद्राएँ लूँगा। ज्यादा लेकर मैं परिग्रह क्यों करूँ ? अपना हृदय क्यों खराब करूँ ?"
दाता तो देकर छूट जाता है। आजकल लेने वाला इतना कंगाल है कि उसका पेट नहीं भरता। देने वाला इतना दरिद्र है कि उसके दिल से छूटता नहीं। उदार आत्मा तो कोई कोई होते हैं।
लेने वाले को थोड़े से तृप्ति हो जानी चाहिए। वह आवश्यकताएँ बढ़ाए नहीं। दान के माल से ऐश न करें, मौज न उड़ाये, पर व्यवहार चलाये।
धर्म का अनुष्ठान करने से अंतःकरण निर्भार होता है ,हृदय में खुशी होती है और अधर्माचरण करने से हृदय बोझीला होता है, दिल की खुशी मारी जाती है।
हमें जो धन, यश और भोग मिलता है वह जितना प्रारब्ध में होता है उतना ही मिलता है। अथवा यहाँ जैसा उद्योग होता है उसी प्रकार का मिलता है। उद्योग अगर अधर्म से करें तो दुःख, चिन्ता और मुसीबत आती है। धर्म के अनुकूल उद्योग करें तो सुख, शान्ति और स्थिरता आती है।
अनुग्रह से भी धन, यश और भोग मिल सकता है। लेकिन देखना यह है कि अनुग्रह किसका है। सज्जन सेठ का, धर्मात्मा साहूकार का अनुग्रह है कि दुरात्मा का है ? साधु का अनुग्रह है कि असाधु का ?
सज्जनों का अनुग्रह, देवताओं का अनुग्रह, सदगुरू और भगवान का अनुग्रह तो वांछनीय है, अच्छा है, स्वीकार्य है। लेकिन दुर्जन का अनुग्रह ठीक नहीं होता। जैसे पक्षियों को फँसाने के लिए शिकारी दाने डालता है। पक्षी दाने चुगने उतर आते हैं और जाल में फँस जाते हैं। फिर छटपटाने लगते हैं। स्वार्थी आदमी कोई अनुग्रह करे तो खतरा है। कोई बदचलन स्त्री, कोई नटी बहुत प्यारे करने लगे, नखरे करने लगे तो खतरा है। वह आदमी की जेब भी खाली कर देगी और नसों की शक्ति भी खाली कर देगी। घड़ीभर का सुख देगी लेकिन जिन्दगी भर फिर रोते रहो, तुच्छ विकारी आकर्षणों में मरते रहो।
तुमको जो धन, यश, भोग और सुख देने वाले हैं वे कैसे हैं यह देखो। वे सज्जन हैं, संत हैं, देव हैं, भगवान हैं कि विकारी आदमी हैं ? विकारी और दुर्जन लोगों के द्वारा मिला हुआ धन, सुख, भोग, भोक्ता को बरबाद कर देता है।
आजकल दोस्त भी ऐसे मिलते हैं। कहते हैं- "चल यार ! सिनेमा देखने चलते हैं। मैं खर्च करता हूँ... चल ब्ल्यू रूम में... ब्ल्यू फिल्म देखते हैं...।"
दस-बारह साल के लड़के ब्ल्यू फिल्म देखने लग जाते हैं। उनकी मानसिक अवदशा ऐसी हो जाती है, वे ऐसी कुचेष्टाओं में ग्रस्त हो जाते हैं कि हम व्यासपीठ पर बोल नहीं सकते। वे बच्चे बेचारे अपना इतना सर्वनाश कर देते हैं कि बाप धन भी दे जाता है, मकान भी दे जाता है, धन्धा भी दे जाता है फिर भी वह बच्चा चारित्र्यभ्रष्ट होने के कारण न धन सँभाल पाता है, न मकान सँभाल पाता है, न धन्धा चला सकता है, न स्वास्थ्य सँभाल पाता है, न माता की सेवा कर पाता है, न माता का आदर कर पाता है, न पिता का श्राद्ध कर्म ठीक से कर पाता है, न माता का भविष्य सोच पाता है न पिता का कल्याण सोच पाता है। वह लड़का अपने ही विकारी सुख में इतना खप जाता है कि उसके जीवन में कुछ सत्त्व नहीं बचता। जरा-सा बोलो तो नाराज हो जाता है, जरा सा समझाओ तो चिढ़ जाता है, घर छोड़कर भाग जाता है। उसको जरा-सा डाँटो तो आत्महत्या के विचार आयेंगे।
आत्महत्या के विचार आते हैं तो मन की दुर्बलता की पराकाष्ठा है। बचपन में वीर्यनाश खूब होता है तो बार-बार आत्महत्या के विचार आते हैं। वीर्यवान पुरूष को आत्महत्या के विचार नहीं आते। संयमी पुरूष को आत्महत्या के विचार नहीं आते। आत्महत्या के विचार वे ही लोग करते हैं जिनका सेक्स्युअल केन्द्र मजबूत होने से पहले ही द्रवित हो गई, क्षीण हो गई। यही कारण है कि हमारे देश की अपेक्षा परदेश में आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। हमारे देश में भी पहले की अपेक्षा आजकल आत्महत्याएँ ज्यादा होने लगी हैं क्योंकि फिल्मों के कुप्रभाव से बच्चे सेक्स्युअल केन्द्र के शिकार हो गये हैं।
आखिर निष्कर्ष क्या निकालना है ?
निष्कर्ष यह निकालना है कि हमें धन, यश और भोग आवश्यक हैं लेकिन इतने नहीं जितने हम मानते हैं। भोग अगर नियंत्रित होगा, वासना अगर नियंत्रित होगी तो मन के संकल्प-विकल्प कम होंगे, मन बलवान होगा।
अपना उद्देश्य ऊँचा बनाओ। आत्म-धन पाने का, आत्म-सुख जगाने का उद्देश्य बनाओ। आत्म-धन और आत्म-सुख शाश्वत है। वह धन पाओगे तो यहाँ का धन दास की तरह सेवा में रहेगा। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को धनंजय कहते है। लोग बोलते हैं कि मैं धनवान हूँ लेकिन उन बेचारों को पता नहीं कि वे धन के मात्र चौकीदार हैं। धन सँभालते सँभालते चले जाते हैं। धन का सदुपयोग नहीं कर पाते तो वे धन के स्वामी कैसे हुए ? स्वामी तो उसको कहा जाता है जो स्वतन्त्र हो। धनवान तो धन से बँधे हुए हैं, धन के दास हैं, गुलाम हैं, धन के चौकीदार हैं। बैंक के द्वार पर चौकीदार बंदूक लेकर खड़ा रहता है। वह धन का चौकीदार है, स्वामी थोड़े ही है !
कई लोग तन के, मन के, धन के दास होते हैं। तन से बीमार रहते हैं, मन से उद्विग्न रहते हैं और धन को सँभालते सँभालते सारा जीवन खपा देते हैं।
कुछ लोग तन के, मन के, धन के स्वामी होते हैं। तन को यथायोग्य आहार-विहार से तन्दुरूस्त रखते हैं, मन को विकारी आकर्षणों से हटाकर आत्म-सुख में डुबाते हैं और धन का बहुजन हिताय सदुपयोग करते हैं।
तन, मन, धन का स्वामी बनना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है।
तन का स्वामी कैसे बनें ? स्वास्थ्य के नियम जानकर तन को क्या खिलाना, कितना खिलाना, क्या न खिलाना, कितना समय सोना, कितना समय जागना, कहाँ जाना, कहाँ न जाना इनका विवेक करो। इन नियमों को चुस्तता से आचरण में लाओ तो तन के स्वामी हो जाओगे। साथ-ही-साथ मन के भी स्वामी हो जाओगे।
मन के स्वामी बनोगो तो तन के भी स्वामी बन जाओगे। तन का स्वामी बनने का संकल्प करोगे तो मन का स्वामी बनने में सहाय मिलेगी. दास बनकर जिये तो क्या जिये ?
मत पुजारी बन तू खुद भगवान होकर जी.....।
चार दिन जी लेकिन शरीर का भगवान होकर जी। दास और गुलाम मत बन। तू शहनशाह होकर जी।
धर्म से इच्छाएँ मर्यादित होती हैं। उपासना से इच्छाएँ शुद्ध होती हैं। ध्यान से इच्छाएँ खत्म होती हैं। इच्छाएँ खत्म होने से सामर्थ्य बढ़ता है। इच्छाएँ नियंत्रित होने से सामर्थ्य पनपता है। इच्छाएँ शुद्ध होने से कर्म की शुद्धि और लक्ष्य की शुद्धि होती है। योग से इच्छाएँ निवृत्त होती हैं और तत्त्वज्ञान से सारी इच्छाएँ भुनी जाती हैं।
अब मर्जी तुम्हारी है। हमने तो शास्त्र, संतों के वचन और अपने अनुभव को आपके समक्ष रख दिया है। तुम्हें जो अच्छा लगे, आत्मसात् कर लो।
नारायण.... नारायण.... नारायण..... नारायण..... नारायण.....
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
कुकर्म के फल से कोई बच नहीं सकता
पाकिस्तान के सख्खर में साधुबेला आश्रम था। रमेशचन्द्र नाम के आदमी को उस समय के संत महात्मा ने अपनी जीवन कथा सुनाई थी और कहा था कि मेरी यह कथा सब लोगों को सुनाना। मैं कैसे साधु-संत बना यह समाज में जाहिर करना। वह रमेशचन्द्र बाद में पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में आ गया था। उस संत ने अपनी कहानी उसे बताते हुए कहा थाः
"मैं जब गृहस्थ था तब मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूँजी लगाकर रूई का धन्धा किया और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया। रूई खरीदकर संग्रह करते और मुंबई में बेच देते। धन्धे में अच्छा मुनाफा होने लगा।
एक बार हम दोनों मित्रों को वहाँ के व्यापारी ने मुनाफे के एक लाख रूपये लेने के लिए बुलाया। हम रूपये लेकर वापस लौटे। एक सराय में रात्रि गुजारने रूके। आज से साठ-सत्तर वर्ष पहले की बात है। उस समय क एक लाख जिस समय सोना साठ-सत्तर रूपये तोला था। मैंने सोचाः एक लाख में से पचास हजार मेरा मित्र ले जाएगा। हालाँकि धन्धे में सारी पूँजी उसी ने लगाई थी फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था। फिर भी मेरी नीयत बिगड़ी। मैंने उसे दूध में जहर पिला दिया। लाश को ठिकाने लगाकर अपने गाँव चला गया। मित्र के कुटुम्बी मेरे पास आये तब मैंने नाटक किया, आँसू बहाय और उनको दस हजार रूपये देते हुए कहा कि मेरा प्यारा मित्र रास्ते में बीमार हो गया, एकाएक पेट दुखने लगा, काफी इलाज किये लेकिन... हम सबको छोड़कर विदा हो गये। दस हजार रूपये देखकर उन्हें लगा कि, 'यह बड़ा ईमानदार है। बीस हजार मुनाफा हुआ होगा उसमें से दस हजार दे रहा है।' उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया।
बाद में तो मेरे घर में धन-वैभव हो गया। नब्बे हजार मेरे हिस्से में आ गये थे। मैं जलसा करने लगा। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। मेरे आनन्द का ठिकाना न रहा। बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी अगम्य रोग से ग्रस्त हो गया। रोग ऐसा था कि भारत के किसी डॉक्टर का बस न चला उसे स्वस्थ करने में। मैं अपने लाडले को स्वीटजरलैंड ले गया। काफी इलाज करवाये, पानी की तरह पैसे खर्च किये, बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब करीब सब धन नष्ट हो गया। दूसरा धन कमाया वह भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर बच्चे को भारत में वापस ले आया। मेरा इकलौता बेटा ! अब कोई उपाय नहीं बचा था। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के इलाज चालू रखे। रात्रि को मुझे नींद नहीं आती और बेटा दर्द से चिल्लाता रहता।
एक दिन बेटे को देखते देखते मैं बहुत व्याकुल हो गया। विह्वल होकर उसे कहने लगाः
"बेटा ! तू क्यों दिनो दिन क्षीण होता चला जा रहा है ? अब तेरे लिए मैं क्या करूँ ? मेरे लाडले लाल ! तेरा यह बाप आँसू बहाता है। अब तो अच्छा हो जा, पुत्र !
बेटा गंभीर बीमारी में मूर्छित सा पड़ा था। मैंने नाभि से आवाज उठाकर बेटे को पुकारा था तो बेटा हँसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ। अभी तो बेहोश था फिर कैसे हँसी आई ? मैंने बेटे से पूछाः
"बेटा ! एकाएक कैसे हंस रहा है ?"
"जाने दो....।"
"नहीं नहीं.... बता क्यों हँस रहा है ?"
आग्रह करने पर आखिर बेटा कहने लगाः
"अभी लेना बाकी है, अभी बीमारी चालू रहेगी, इसलिए मैं हँस रहा हूँ। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर दिया था। मुंबई की धर्मशाला में मुझे खत्म कर दिया था और मेरा सारा धन हड़प लिया था। मेरा वह धन और उसका सूद मैं वसूल करने आया हूँ। काफी कुछ हिसाब पूरा हो गया है। अब केवल पाँच सौ रूपये बाकी हैं। अब मैं आपको छुट्टी देता हूँ। आप भी मुझे इजाजत दो। ये बाकी के पाँच सौ रूपये मेरी उत्तर क्रिया में खर्च डालना, हिसाब पूरा हो जाएगा। मैं जाता हूँ... राम राम...." और मेरे बेटे ने आँख मूँद ली, उसी क्षण वह चल बसा।
मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुकी थी। सारा धन नष्ट हो गया और बेटा भी चला गया। मुझे किये हुए पाप की याद आयी तो कलेजा छटपटाने लगा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता है तब देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ेगी तो भी ऊपरवाली सरकार तो है ही। उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता।
मैंने बेटे की उत्तर क्रिया करवाई। अपनी बची-खुची संपत्ति अच्छी-अच्छी जगहों में लगा दी और मैं साधु बन गया हूँ। आप कृपा करके मेरी यह बात लोगों को कहना। मैंने भूल की ऐसी भूल वे न करें, क्योंकि यह पृथ्वी कर्मभूमि है।"
कर्मप्रधान
विश्व करी
राखा।
जो
उस करे तैसा
फल चाखा।।
कर्म का सिद्धान्त अकाट्य है। जैसे काँटे से काँटा निकलता है ऐसे ही अच्छे कमों से बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। सबसे अच्छा कर्म है जीवनदाता परब्रह्म परमात्मा को सर्वथा समर्पित हो जाना। पूर्व काल में कैसे भी बुरे कर्म हो गये हों उन कर्मों का प्रायश्चित करके फिर से ऐसी गलती न हो जाए ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जिसके प्रति बुरे कर्म हो गये हों उनसे क्षमायाचना करके, अपना अन्तःकरण उज्जवल करके मौत से पहले जीवनदाता से मुलाकात कर लेनी चाहिए।
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-
अपि
चेत्सुदराचारो
भजते
मामनन्यभाक्।
साधुरेव
स मन्तव्यः
सम्यग्व्यवसितो
हि सः।।
'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात् उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है।'
(भगवद् गीताः 9.30)
तथा-
अपि
चेदासि
पापेभ्यः
सर्वेभ्यः
पापकृत्तमः।
सर्वं
ज्ञानप्लवेनैव
वृजिनं
संतरिष्यसि।।
'यदि तू अन्य सर्व पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्र से भली-भाँति तर जाएगा।'
(भगवद् गीताः 4.36)
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
विवेक की धार तेज बनाओ
जीवन को शीघ्र ऊर्ध्वगामी बनने के लिए बुद्धि में सदैव दृढ़ संकल्प मौजूद रहे किः
'मैं उनकी बात कभी नहीं मानूँगा जो मुझे मौत से नहीं छुड़ा सकते। मैं उन चीजों को जानने की कोशिश कभी नहीं करूँगा जो मुझे गर्भवास में धकेल दे। मौत के बाद मुझे मालिक से मिलने में जो कर्म रूकावट कर देता है वह कर्म के लिए विष है।'
एक पौराणिक कथा हैः
शुकदेव जी का जन्म हुआ तब वे सोलह वर्ष के थे। जन्मते ही वे घर छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे। पिता वेदव्यासजी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, पुकार रहे हैं-
"पुत्र ! पुत्र !! सुनो। कहाँ जाते हो ? रूको... रूको.... मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरी बात सुनो।"
पुत्र ने सोचा कि, 'आखिर पिता भी जैसे तैसे नहीं हैं। वन में जाना है तो उनकी आशिष लेकर ही जाना उचित है। उनको प्रार्थना कर देता हूँ।"
शुकदेवजी ने पिता से कहाः "मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। फिर मुझे वापस बुलाना उचित समझें तो बुलाइये। पिताजी ! सुनिये।
किसी गाँव के बाहर नदी किनारे एक ब्रह्मचारी युवक प्रातःकाल उठकर हररोज सन्ध्या-वन्दन, उपासना, योगाभ्यास आदि करता था। जप-ध्यानादि के बाद जब उसे भूख लगती तो वह एक समय भिक्षापात्र लेकर नगर में मधुकरी करता था। उस ब्रह्मचारी का संयम, साधना, ओज, तेज बढ़ता चला गया।
उसी गाँव में एक कुलटा स्त्री नववधु होकर आयी थी। दो मंजिल वाला उसका मकान था। ब्रह्मचारी जब भिक्षा लेने नगर में निकलता तो वह कुलटा खिड़की से उसे निहारती।
एक दिन उस युवती का पति बाहर जाने को निकल गया तब युवती ने ब्रह्मचारी को खिड़की से झाँककर बुलाया और कहाः
"इधर आओ। मैं तुम्हें भिक्षा देती हूँ।"
वह निर्दोष ब्रह्मचारी युवक सहज स्वभाव से भिक्षा लेने ऊपर पहुँच गया। युवक के अंदर आते ही उस कुलटा ने दरवाजा बन्द कर दिया। युवक से अनधिकार चेष्टा करने की कोशिश की। ब्रह्मचारी घबराया। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीः
"हे प्रभु ! मेरी साधना अधूरी न रह जाय। हे मेरे मालिक ! तू ही मेरा रक्षक है। काम तो वैसे ही तीर लिये खड़ा होता है। फिर यह कामिनी अपना प्रयास कर रही है। हे राम ! तू कृपा कर। मैं मारा जा रहा हूँ। तू कृपा करेगा तो ही बच पाऊँगा। हे प्रभु कृपा कर...... कृपा कर.....।"
उस ब्रह्मचारी की भीतरी प्रार्थना अन्तर्यामी परमात्मा ने सुन ली। उस युवती का पति बाहर जाने को घर से निकला था। संयोगवश उसे पेट में गड़बड़ी महसूस हुई और संडास जाने के लिए घर वापस लौट आया। घर का दरवाजा खटखटाया और पत्नी को पुकारा। पत्नी ने पति की आवाज पहचानी और वह घबराई। अब इस युवक साधु का क्या किया जाय ? उसने तुरन्त निर्णय कर लिया और युवक को संडास की मोरी में दबा दिया। पत्नी ने दरवाजा खोला। पति को संडास जाना था तो वह संडास गया। मल-मूत्र-विष्टा का त्याग किया। फिर नहाधोकर अपनी पत्नी को भी साथ लेकर बाहर चला गया।
वह नवयुवक ब्रह्मचारी बेचारा उस संडास की मोरी में सरकता सरकता एक दिन के बाद नीचे आया। उस कुलटा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बेचारे को मोरी में उलटा धकेल दिया था। सिर नीचे और पाँव ऊपर, जैसे माता के गर्भ में बच्चा उल्टा होकर पड़ा रहता है। इस प्रकार वह धीरे धीरे सरकते हुए एक दिन के बाद जब नीचे उतरा तब भंगी को उसके सिर के बाल दिखाई दिये। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने युवक को बाहर खींच लिया। युवक तो बेहोश हो गया था। भंगी को संतान नहीं थी। वह उसे अपने घर में ले गया। मूर्छित ब्रह्मचारी का इलाज किया। काफी कोशिशों के बाद युवक होश में आया। होश में आया तो वह भागकर अपनी झोंपड़ी में आया। नदी में अच्छी तरह स्नान किया। फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, जपादि करके स्वस्थ हुआ।
पिता जी ! उस युवक को फिर से भूख लगी। दो चार दिन के बाद भिक्षा हेतु उसे नगर में आना ही पड़ा। तब तक वह कुलटा स्त्री भी अपने घर वापस लौट आयी थी।
पिताजी ! वह युवक उस मोहल्ले में से अब गुजरेगा ही नहीं लेकिन अगर वह अनजाने में उस मोहल्ले से गुजरे और वह कुलटा स्त्री उसे पूरी पकवान खिलाने को बुलाय तो वह वहाँ जायगा क्या ? वह स्त्री उसे बार-बार अनुनय विनय करे, अच्छे अच्छे कपड़े देने का, सुन्दर वस्त्राभूषण देने का प्रलोभन दे तो वह जायेगा क्या ? नहीं, वह युवक ब्रह्मचारी उस कुलटा के पास कदापि नहीं जाएगा। क्योंकि उसे एक बार संडास की मोरी का अनुभव याद है, नाली से गुजरने की पीड़ा की स्मृति है।
पिताजी ! उस ब्रह्मचारी की तो एक ही बार मोरी से गुजरने का अनुभव याद है इससे हजारों हजारों प्रलोभनों के बावजूद भी वह कुलटा के पास नहीं जाता जबकि मैं तो हजारों हजारों नालियों से, माताओं के गर्भों में घूमता घूमता आया हूँ। पिताजी ! मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, संसार के कीचड़ से मुझे बचने दीजिए। मुझे कई जन्मों से स्मरण है कि माता की गर्भरूपी मोरी कैसी गन्दी होती है।
उस कुलटा स्त्री के संडास की मोरी तो एक दिन की थी लेकिन यहाँ माता के गर्भरूपी मोरी में तो नौ महीने और तेरह दिन तक उल्टा होकर लटकना पड़ता है। वहाँ मल-मूत्र-विष्टा सतत बनी रहती है। माँ तीखा पदार्थ खाती है तो बच्चे की कोमल चमड़ी पर जलन होती है। उसकी पीड़ा तो बच्चा ही जानता है। माँ की गन्दी योनि के मार्ग से बाहर निकलते समय बच्चे को जो पीड़ा होती है उसका क्या बयान किया जाय ? माँ की अपेक्षा दस गुना अधिक पीड़ा बच्चे की होती है। बच्चा बेचारा बेहोश का हो जाता है।
हे पिता जी ! ऐसी पीड़ाओं से मैं केवल एक ही बार नहीं गुजरा हूँ लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बार गुजरा हूँ। अब आप मुझे क्षमा करो। मुझे उस गन्दी नालियों में ले जाने वाले संसार की ओर न घसीटो।"
संसार और चित्तवृत्तियों का बहुत पसारा मत करो। बहुत पसारा करने से फिर गंदी मोरियों से पसार होना पड़ेगा, नालियों से पसार होना पड़ेगा। कभी दो पैरवाली माँ की नाली से पसार होंगे कभी चार पैरवाली माँ की नाली से पसार होंगे, कभी आठ पैरवाली माँ की नाली से, कभी सौ पैरवाली माँ की नाली से। आज तक ऐसी कई प्रकार की माँ की नालियों से पसार होते आये हैं युगों से। अब कब तक उन नालियों से गुजरते रहोगे ? अब उन नालियों से उपराम हो जाओ। अब तो उस परमात्मा से मिलो, फिर कभी किसी नाली से गुजरना न पड़े।
अपने विवेक और वैराग्य को निरन्तर जागृत रखना। विवेक जरा-सा भी कम हुआ कि नाली तैयार हो जाती है। विवेक जरा-सा भी कम हुआ कि नाली तैयार हो जाती है। ब्रह्मचारी को जरा-सी विस्मृति हो जाएगी तो वह कुलटा उसे फिर से बुलाने में उत्सुक है। तुम सदा याद रखना कि आखिर क्या ? इतना खा लिया फिर क्या ? इतना भोग लिया फिर क्या ? अखबारों में इतनी फोटो छपवा ली फिर क्या ?
इसलिए खूब सतर्क रहो।
संत एकनाथ जी के पास एक बूढ़ा पहुँचा। बोलाः
"आप भी गृहस्थी मैं भी गृहस्थी। आप भी बच्चों वाले मैं भी बच्चों वाला। आप भी सफेद कपड़ों वाले मैं भी सफेद कपड़े वाला। लेकिन आपको लोग पूजते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आप इतने खुश रह सकते हो, आप इतने निश्चिन्त जी सकते हो और मैं इतना परेशान क्यों ? आप इतने महान् और मैं इतना तुच्छ क्यों ?"
एकनाथ जी ने सोचा कि इसको सैद्धान्तिक उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, उसको समझ में नहीं आयेगा। कुछ किया जाय... एकनाथ जी ने उसे कहाः
"चल रे सात दिन में मरने वाले ! तू मुझसे क्या पूछता है ? अब क्या फर्क पड़ेगा ? सात दिन में तो तेरी मौत है।"
वह आदमी सुनकर सन्न रह गया। एकनाथ जी कह रहे हैं सात दिन में मौत है तो बात पूरी हो गई। वह आदमी अपनी दुकान पर आया लेकिन उसके दिमाग में एकनाथ जी के शब्द घूम रहे हैं- "सात दिन में मौत है। उसको धन कमाने का जो लोभ था, हाय हाय थी वह शान्त हुई। अपने प्रारब्ध का जो होगा वह मिलेगा। ग्राहकों से लड़ पड़ता था तो अब प्रेम से व्यवहार करने लगा। शाम होती थी तब दारू के घूँट पी लेता था वह दारू अब फीका हो गया। एक दिन बीता.... दूसरा बीता.... तीसरा बीता....। उसे भोजन में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वाद के व्यंजन, आचार, चटनी आदि चाहिए था, जरा सी कमी पड़ने पर आगबबूला हो जाता था। अब उसे याद आने लग गया कि तीन दिन बीत गये, अब चार दिन ही बचे। कितना खाया-पिया ! आखिर क्या ? चौथा दिन बीता.... पाँचवाँ दिन आया...। बहू पर क्रोध आ जाता था, बेटे नालायक दिखते थे, अब तीन दिन के बाद मौत दिखने लगी। सब परिवारजानों के अवगुण भूल गया, गद्दारी भूल गया। समाधान पा लिया कि संसार में ऐसा ही होता है। यह मेरा सौभाग्य है कि वे मुझसे गद्दारी और नालायकी करते हैं तो उनका आसक्तिपूर्ण चिन्तन मेरे दिल में नहीं होता है। यदि आसक्तिपूर्ण चिन्तन होगा तो फिर क्या पता इस घर में चूहा होकर आना पड़े या साँप होकर आना पड़े या चिड़ियाँ होकर आना पड़े, कोई पता नहीं है। पुत्र और बहुएँ गद्दार हुई हैं तो अच्छा ही है क्योंकि तीन दिन में अब जाना ही है। इतने समय में मैं विट्ठल को याद कर लूँ- विट्ठला... विट्ठला.... विट्ठला...
भगवान का स्मरण चालू हो गया। जीवन भर जो मंदिर में नहीं गया था, संतों को नहीं मानता था उस बूढ़े का निरन्तर जाप चालू हो गया। संसार की तू-तू, मैं-मैं, तेरा-मेरा सब भूल गया।
छट्ठा दिन बीतने लगा। ज्यों-ज्यों समय जाने लगा त्यों-त्यों बूढ़े का भक्तिभाव, नामस्मरण, सहज-जीवन, सहनशक्ति, उदारता, प्रेम, विवेक, आदि सब गुण विकसित होने लगे। कुटुम्बी दंग रह गये कि इस बूढ़े का जीवन इतना परिवर्तित कैसे हो गया ! हम रोज मनौतियाँ मनाते थे कि यह बूढ़ा कब मरे, हमारी जान छूटे।
लोग देवी-देवता की पूजा-प्रार्थना करते हैं, मनौतियाँ मानते हैं, संतों से आशीर्वाद माँगते हैं, "हे देवी देवता ! इस बूढ़े का स्वर्गवास हो जाये, हम भंडारा करेंगे... हे महाराज ! आशीर्वाद दो, मेरा ससुर बहुत दुःखी है।"
"क्या है उसे ?"
"वह बीमार है, आँखों से दिखता नहीं, बुढ़ापा है। खाना हजम नहीं होता। नींद नहीं आती। सारी रात 'खों... खों....' करके हमारी नींद खराब करता है। आप आशिष करो। या तो वह नवजवान हो जाय या तो आप दया करो......।"
"क्या दया करूँ?"
"बाबा ! आप समझ जाओ, हमसे मत कहलवाओ।"
जिन
लाय तो सूर
सठा आहेन।
से
कांधी कीं न
थींदा।।
जिन बच्चों को तुम जन्म देते हो, पालते-पोसते हो, अपने पेट पर पट्टियाँ बाँधकर उनको पढ़ाते हो उनको बड़ा होने दो। उनको बहू मिलने दो। तुम्हारा बुढ़ापा आने दो। फिर देखो तुम्हारा हाल क्या होता है।
बहुत
पसारा मत करो
कर थोड़े की
आश।
बहुत
पसारा जिन
किया वे भी
गये निराश।।
चार चार पुत्र होने पर भी बूढ़ा परेशान है क्योंकि बूढ़े ने पुत्र पर आधार रखा है, परमात्मा का आधार छोड़ दिया है। तुमने परमात्मा का आधार छोड़कर पुत्र पर, पैसे पर, कुटुम्ब पर, राज्य पर, सत्ता पर आधार रखा तो अन्त में रोना पड़ेगा। सारे विश्व की सुविधाएँ जिसको उपलब्ध हो सकती हैं ऐसी भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा को भी विवश होकर अपने पुत्र की मौत देखनी पड़ी। खुद को गोलियों का शिकार होना पड़ा। दूसरे बेटे को आतंकवादियों ने उड़ा दिया। मौत कब आती है, कैसे आती है, कहाँ आती है कोई पता नहीं है। हम यहाँ से जाएँ लेकिन घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे क्या पता ? घर से दुकान पर जाते समय रास्ते में क्या पता कुछ हो जाय ! कोई पता नहीं इस नश्वर शरीर का।
उस बूढ़े का छट्ठा दिन बीत रहा है। उसकी प्रार्थना में उत्कण्ठा आ गई है कि हे भगवान ! मैं क्या करूँ ? मेरे कर्म कैसे कटेंगे ? विठोबा... विठोबा... माजा विट्ठला.... माजा विट्ठला.... जाप चालू है। रात्रि में नींद नहीं आयी। रविदास की बात उसको शायद याद आ गई होगी। अनजाने में उसके जीवन में रविदास चमका होगा।
रविदास
रात न सोइये
दिवस न लीजिए
स्वाद।
निशदिन
हरि को सुमरीए
छोड़ सकल
प्रतिवाद।।
बूढ़े की रात अब सोने में नहीं गुजरती, विठोबा के स्मरण में गुजर रही है।
सातवें दिन प्रभात हुई। बूढ़े ने कुटुम्बियों को जगायाः
"बोला चाला माफा करना... किया कराया माफ करना... मैं अब जा रहा हूँ।"
कुटुम्बी रोने लगे किः "अब तुम बहुत अच्छे हो गये हो, अब न जाते तो अच्छा होता।"
जो भगवान का प्यारा बन जाता है वह कुटुम्ब का भी प्यारा होता है, समाज का भी प्यारा होता है। जो भगवान को छोड़कर अपने कुटुम्बियों के लिए सब कुछ करता है उसको कुटुम्बी भी आखिर दुत्कारते हैं।
बूढ़ा कहता हैः "गोबर से लीपकर चौका लगाओ। मेरे मुँह में तुलसी का पत्ता दो। गले में तुलसी का मनका बाँधो। आप लोग रोना मत। मुझे विठोबा के चिन्तन में मरने देना।"
कुटुम्बी सब परेशान हैं। इतने में एकनाथ जी वहाँ से गुजरे। कुटुम्बी भागे। एकनाथजी के पैर पकड़े। आप घर में पधारो।
एकनाथ जी ने घर आकर बूढ़े से पूछाः
"क्यों, क्या बात है ? क्यों सोये हो ?"
"महाराज जी ! आप ही ने तो कहा था कि सात दिन में तुम्हारी मौत है। छः दिन बीत गये। यह आखिरी दिन है। संत का वचन मिथ्या नहीं होता। वह सत्य ही होता है।"
मैं भी तुम्हें कह देता हूँ कि आप लोग भी एक सप्ताह में, सात दिन में ही मरोगे। आप रविवार को मरोगे या सोमवार को मरोगे या मंगलवार को या बुधवार को या गुरूवार को या शुक्रवार को। इन छः दिनों में नहीं मरोगे तो शनिवार को तो जरूर मरोगे ही। आप जब कभी मरोगे तब इन सात दिनों में से कोई न कोई एक दिन तो होगा ही। आठवाँ दिन तो है ही नहीं।
एकनाथजी की बात भी सच्ची थी। संत क्यों झूठ बोलें ? हम समझते नहीं हैं संत की बात को तो कह देते हैं संत की बात गलत है।
शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार शायद बच भी सकता है। लेकिन सच्चे सदगुरू के हृदय में जिसका स्थान बन जाता है वह कैसे फेल हो सकता है ?
एकनाथ जी का वचन उस बूढ़े ने सत्य माना तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया।
एकनाथ जी उस बूढ़े से कहने लगेः
"तुमने मुझसे कहा था कि आप में और क्या फर्क है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी सात दिन में मौत होगी। तुमने अपनी मौत को सात दिन दूर देखा। अब बताओ, तुमने सात दिन में आनेवाली मौत को देखकर कितनी बार दारू पिया ?"
"एक बार भी नहीं।"
"कितनी बार क्रोध किया ?"
"एक बार भी नहीं।"
"कितने लोगों से झगड़ा किया ?"
"किसी से भी नहीं।"
"तुमको सात दिन, छः दिन, पाँच दिन, चार दिन दूर मौत दिखी। जितनी-जितनी मौत नजदीक आती गई उतना उतना तुम ईश्वरमय होते गये। संसार फीका होता गया। यह तुम्हारा अनुभव है कि नहीं ?"
"हाँ महाराज ! मेरा अनुभव है।"
"सात दिन मौत दूर है तो संसार में कहीं रस नहीं दिखा, भगवान में प्रीति बढ़ी, जीवन भक्तिमय बन गया। मेरे गुरू ने तो मुझे सामने ही मौत दिखा दी है। मैं हररोज मौत को अपने सामने ही देखता हूँ। इसलिए मुझे संसार में आसक्ति नहीं है और प्रभु में प्रीति है। जिसकी प्रभु में प्रीति है उसके साथ दुनियाँवाले प्रीति करते हैं। इसलिए मैं बड़ा दिखता हूँ और तुम छोटे दिखते हो। वरना हम और तुम दोनों एक ही तो हैं।"
अनात्म वस्तुओं में मन को लगाया, अनात्म पदार्थों में मन को लगाया तो हम अपने आपके शत्रु हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। अनात्म वस्तुओं से मन को हटाकर आत्मा में लगाते हैं तो हम श्रेष्ठ हो जाते हैं और अपने आपके मित्र हो जाते हैं, महान् हो जाते हैं।
नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, महावीर तुमसे बड़े नहीं थे, बुद्ध तुमसे बड़े नहीं थे, क्राइस्ट तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण भी तुमसे बड़े नहीं थे, तुम्हारा ही रूप थे, लेकिन वे सब बड़े हो गये क्योंकि उन्होंने अपने आप में, आत्मस्वरूप में स्थिति की, परमात्मा में स्थिति की और हम लोग पराये में स्थिति करते हैं, अनात्मा में स्थिति करते हैं, संसार स्थिति कते हैं इसलिए हम मारे जाते हैं।
अब तब जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई। अब बात समझ में आ गई। आगे सावधान रहना है। सदा याद रखना है कि हम सब सात दिन में मरने वाले हैं। आखिर कब तक ?
हम योजना बनाते हैं कि कल रविवार है, छुट्टी मनायेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे। लेकिन वह रविवार ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अर्थी पर आरूढ़ हो जाएँ। सोमवार के दिन हम श्मशान में ही पहुँच जाएँ। मंगलवार के दिन सगे-सम्बन्धी के वहाँ जाने का सोचते हैं लेकिन हो सकता है कि हम मरघट से ही मिलने चल पड़ें। बुधवार को हम विदेश जाने की तैयारी करते हैं लेकिन हो सकता है कि बुधवार के दिन यह शरीर बुद्धू की तरह मुर्दा होकर पड़ा हो। गुरूवार के दिन गुरू के द्वार जाने का संकल्प किया हो लेकिन हो सकता है कि गुरूवार के दिन गुरू के द्वार के बजाय यम के द्वार ही पहुँच जाएँ। शुक्रवार के दिन शुकदेवजी जैसे ज्ञान को पाने में लगते हैं कि शूकर-कूकर की योनियों की ओर जाते हैं, कोई पता नहीं। शनिवार के दिन किसी की शादी में आइसक्रीम खाने जाते हैं कि मृत्युशैय्या पर सोते हैं कोई पता नहीं।
सुबह उठो तब सबसे पहले परमात्मा को और मौत को याद कर लो। क्या पता कौन से दिन इस जहाँ से चले जायें। आज सोमवार है ? क्या पता कौन से सोमवार को हम चले जायें। आज मंगलवार है ? क्या पता कौन से मंगलवार को हम विदा हो जायें। मैं सच बोलता हूँ, इन सात दिनों में से कोई न कोई दिन होगा मौत का। भगवान की कसम...।
मौत को और परमात्मा को हररोज अपने सामने रखोगे तो महान होने में देरी नहीं है। मौत को और परमात्मा को सामने रखोगे तो अपने गाँव का साइन बोर्ड देखने का उत्साह होगा। अपने गाँव का स्टेशन आ जाय तो तुम चले जाने, पूछते मत रहना कि मेरा गाँव है कि तेरा गाँव है ? तुम चले जाना अपने गाँव। फलाना गया कि नहीं गया इसका इन्तजार मत करना।
कई लोग आश्चर्यजनक बातें करते हैं। वे लोग सत्संग में बैठते हैं। आध्यात्मिक वातावरण में चित्त शान्त हो जाता है। चित्त शान्त होता है तो खुली आँख भी आनन्द आने लगता है। चित्त शान्त नहीं है तो बन्द आँख से भी कुछ नहीं होता।
जब जब आनन्द आने लग जाये तो समझना कि अनजाने में चित्त शान्त हो गया है। बिना परिश्रम के, वातावरण के प्रभाव से, भगवान की कृपा से, संतों की करूणा से तुम्हारा चित्त अनजाने में ही धारणा में लग गया है, ध्यानस्थ हो गया है, तभी तुम्हें आनन्द आता है।
लोग मेरे पास आकर बोलते हैं-
"साँई मेरे पर दया करो।"
"क्या बात है ?"
"मेरा ध्यान नहीं लगता है। दया करो, मेरा ध्यान लग जाय।"
उसका चेहरा खबर दे रहा है कि उसने ध्यान का अमृत पिया है, एकाध घूँट झेल लिया है।
"तेरा ध्यान नहीं लगता है ?"
"नहीं साँईं ! ध्यान नहीं लगता है।"
"ध्यान के समय क्या होता है ? आनन्द आता है ?"
"साँईं ! आनन्द तो बहुत आता है।"
आनन्द बहुत आता है और ध्यान नहीं लगता है ! अरे बड़े मियाँ ! ध्यान का फल क्या है ? आनन्द है कि दुःख ? ईश्वरप्राप्ति का फल क्या है ?
मम
दर्शन फल परम
अनूपा।
जीव
पावहिं निज
सहज
स्वरूपा।।
भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है। जीव अपना स्वरूप पा ले, अपना सहज सुख आने लगे। उसे अपने सुखस्वरूप निजात्मा की अनुभूति होने लगे।
यह जरूरी नहीं कि हम गुरूदीक्षा लेंगे, गुरूजी कान में फूँक मारेंगे, सिर पर हाथ रखेंगे, हम नारियल देंगे, वस्त्र देंगे, पैसे देंगे बाद में गुरूजी करूणा-कृपा बरसायेंगे, ब्रह्मज्ञान देंगे।
ये कोई पण्डित गुरू नहीं हैं। सदगुरू तो बिना लिये ही दे देते हैं, खोजते रहते हैं कि लेने वाला कोई मिल जाय। पहले विधि विधान बनें, हम शिष्य बनें तभी वे कुछ देंगे ऐसी बात नहीं है। वे तो पहले से ही थोक में दे देते हैं, बाद में हमारी श्रद्धा होती है तो उन्हें गुरू मानते हैं। वरना वे अपने को गुरू मनवाने की भी इच्छा नहीं रखते। ये तो विश्वात्मा हैं। वे पाँच-पच्चीस हजार के, पच्चीस-पचास लाख के गुरू थोड़े ही हैं। ब्रह्मवेत्ता, आत्म-साक्षात्कारी पुरूष तो सारे ब्रह्माण्ड के गुरू हैं।
कृष्णं
वन्दे जगद्
गुरूम्।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
गुरू प्रसाद
अपने आत्मा परमात्मा में शान्त होते जाओ। चैतन्य स्वरूप परमात्मा में तल्लीन होते जाओ। चिन्तन करो कि 'मैं सम्पूर्ण स्वस्थ हूँ.... मैं सम्पूर्ण निर्दोष हूँ.... मैं सम्पूर्णतया परमात्मा का हूँ... मैं सम्पूर्ण आनन्दस्वरूप हूँ... हरि ॐ... ॐ...ॐ.... मधुर आनन्द... अनुपम शान्ति.... चिदानन्दस्वरूप परमेश्वरीय शान्ति.... ईश्वरीय आनन्द... आत्मानन्द.... निजानन्द... विकारों का सुखाभास नहीं अपितु निजस्वरूप का आनन्द....
निज सुख बिन मन होवईं कि थिरा ?
निज के सुख को जगाओ... मन स्थिर होने लगेगा। निज सुख नारायण का प्रसाद माना जाता है।
अपने आत्मसुख में तल्लीन होते जाएँगे। हृदयकमल को विकसित होने देंगे। आनन्दस्वरूप ब्रह्म के माधुर्य में अपने चित्त को डुबाते जाएँगे।
हे मेरे गुरूदेव ! हे मेरे इष्टदेव ! हे मेरे आत्मदेव ! हे मेरे परमात्मदेव ! आपकी जय हो.....!
यह ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला है। इस अमृतवेला में हम अमृतपान कर रहे हैं। अमृतवेला में आत्मारामी संत, अपने आत्मा-परमात्मा में, सोहं स्वभाव में रमण करते हैं। इस अमृतवेला में उनके ही आन्दोलन, वे ही तन्मात्राएँ बिखरती रहती हैं और साधकों को मिलती रहती हैं। प्रभात काल में साधारण आदमी सोये रहते हैं लेकिन योगीजन ब्रह्ममुहूर्त में जगाकर अपने आत्म-अमृत का पान करते हैं।
यह आत्म-ध्यान, यह आत्म-अमृत त्रिलोकी को पावन करने वाला है। यह परमात्म-प्रसाद चित्त के दोषों को धो डालता है और साधक को स्वतन्त्र सुख के द्वारा पर पहुँचा देता है। साधक ज्यों-ज्यों अन्तर्मुख होता जाता है त्यों-त्यों यह चिदघन चैतन्य स्वभाव का अमृत पाता जाता है।
दृढ़ निश्चय करो कि मैं सदैव स्वस्थ हूँ। मुझे कभी रोग लग नहीं सकता। मुझे कभी मौत मार नहीं सकती। मुझे विकार कभी सता नहीं सकते। मैं विकारों से, रोगों से और मौत से सदैव परे था और रहूँगा ऐसा मैं आनन्दस्वरूप आत्मा हूँ।
हरि ॐ.....ॐ......ॐ......
हम अपने आत्म-प्रसाद का स्मरण करते-करते आत्ममय होते जाएँगे।
जन्म
मृत्यु मेरे
धर्म नहीं
हैं।
पाप
पुण्य कुछ कर्म
नहीं हैं।
मैं
अज निर्लेपी
रूप।।
कोई
कोई जाने रे.....
हम विकारों को दूर भगायेंगे। अपने अहंकार को परमात्म स्वभाव में पिघला देंगे। रोग और बीमारी तो शरीर तो आती-जाती रहती है। हम शरीर से पृथक हैं। इस ज्ञान को दृढ़ करते जायेंगे। फिर आनन्द ही आनन्द है... मंगल ही मंगल है.... कल्याण ही कल्याण है।
सदैवे उच्च विचार.... उच्च विचारों से भी पार, उच्च विचारों के भी साक्षी... नीच विचारों को निर्मूल करने में सदैव सतर्क।
हमारा स्वरूप सनातन सत्य है। हमारा आत्मा सदैव शुद्ध, बुद्ध है। हम अपने शुद्ध, बुद्ध परमेश्वरीय स्वभाव में, अपने निर्भीक स्वभाव में, निर्विकारी स्वभाव में, अपने आनन्द स्वभाव में, अपने अकर्त्ता स्वभाव में, अपने अभोक्ता स्वरूप में, अपने भगवद् स्वभाव में सदैव टिककर निर्लेप भाव से इस शरीर का जीवन यापन करते जीवन की शाम होने से पहले जीवनदाता के स्वरूप में टिक जाएँगे। हरि ॐ.... हरि ॐ.... हरि ॐ.....
निर्विकार नारायण स्वरूप में स्थित होकर विश्रान्ति बढ़ाते जाओ। जितना जितना जगत का आकर्षण कम उतना ही उतना आत्म विश्रान्ति अधिक....। जितनी जितनी आत्म-विश्रान्ति अधिक उतनी ही परमात्मा में बुद्धि की प्रतिष्ठा अधिक। परमात्मिक शक्तियाँ बुद्धि में विलक्ष्ण सामर्थ्य भरती जाती हैं।
इन्द्रियों के आकर्षण को, जागतिक विकारी आकर्षण को मिटाने के लिए निर्विकारी नारायण स्वरूप का ध्यान, चिन्तन, आत्म-स्वरूप का सुख, आत्म-प्रसाद पाने का अभ्यास और उस अभ्यास में प्रोत्साहन मिले ऐसा सत्संग जीवन का सर्वांगी विकास कर देता है।
अन्तरतम चेतना में डूबते जाओ... परमात्म प्रसाद को हृदय में भरते जाओ।
मैं शान्त आत्मा हूँ..... मैं परमात्मा का सनातन अंश हूँ... मैं सत् चित् आनन्द आत्मा हूँ। ये शरीर के बन्धन माने हुए है। वास्तव में मुझ चैतन्य को कोई बन्धन नहीं था न हो सकता है। बन्धन भोग की वासना से पैदा होते हैं। बन्धन देह को 'मैं' मानने से प्रतीत होते हैं। बन्धन संसार को सच्चा समझने से लगते हैं। अपने आत्म-स्वभाव को पहचानने से, अपने आत्म-परमात्म स्वभाव को पहचानने से, अपने आत्म-परमात्म तत्त्व का साक्षात्कार करने से सब बन्धन कल्पित मालूम होते हैं, सारा संसार कल्पित मालूम होता है। तू-तू.... मैं-मैं..... यह अन्तः करण की छोटी अवस्था में सत्य प्रतीत होता है। अद्वैत की अनुभूति में, परमेश्वरीय अनुभूति में ये सारे छोटे-छोटे विचार, मान्यताएँ गायब हो जाती हैं। जो सुख देखा वह स्वप्न हो गया और जो दुःख देखा वह भी स्वप्न हो गया। बचपन आया वह भी स्वप्न हो गया, जवानी थी वह भी स्वप्न हो गयी, मौत भी आयेगी तो स्वप्न हो जाएगी।
हे चैतन्य जीव ! तेरी कई मौतें हुईं लेकिन तू नहीं मरा। तेरे शरीर की मौतें हुईं। तेरे शरीरों को बचपन, जवानी और वृद्धत्व आया, मौतें हुईं फिर भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जिसका कुछ नहीं बिगड़ा वह तू है। तू अपने उसी आत्म-स्वभाव को जगा। छोड़ संसार की वासना... छोड़ दुनियाँ का लालच... एक आत्मदृष्टि रखकर इस समय पार होने का संकल्प कर।
हरि ॐ... हरि ॐ.... हरि ॐ....
आज उत्तरायण का दिन है। गंगापुत्र भीष्म इसी दिन की राह देख रहे थे। आज देवताओं का प्रभात है। देवता लोग जागे हैं। छः महीने बीतते हैं तो देवताओं की रात होती है और छः महीन बीतते हैं तो उनका दिन होता है। तैंतीस करोड़ देवताओं को खूब-खूब धन्यवाद है, उसको प्रणाम है। देव लोग अब जागे हैं। पृथ्वी पर देवत्व का प्रसाद बरसे, सात्त्विक स्वभाव बरसे, हृदय प्रसन्न रहे और देवता भी प्रसन्न रहें, जीवन में आते हुए संसारी आकर्षण, भय, शोक आदि को वे हर लें।
सूर्यनारायण आज उत्तर की ओर अपने रथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हे सूर्यनारायण ! आज के दिन आपका विशेष स्वागत है। हम भी अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी विचारों में, ऊर्ध्वगामी सुख में, ऊर्ध्वगामी स्वरूप की ओर ले जाने के लिए आज हम प्रभात कालीन ध्यान में प्रवेश पा रहे हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सत्संग-सरिता
जहाँ भगवान का स्मरण चिन्तन होता है वह स्थान पवित्र माना जाता है। वहाँ के कण-कण में उस परमात्म-तत्त्व के परमाणु फैले रहते हैं। जो आदमी क्रोधी होता है उसके आसपास सात फीट के दायरे में क्रोध के परमाणु फैले रहते हैं। हर इन्सान एक पावर हाउस है। उसमें से कुछ न कुछ संस्कारों की सूक्ष्म तन्मात्राएँ निकलती रहती हैं। जहाँ भगवान की भक्ति करनेवाले लोग रहते हैं वह स्थान भी अपना कुछ दिव्य महत्त्व रखता है।
महाराष्ट्र में महात्मा गाँधी किसी गुफा में गये थे। गुफा में रहने वाले योगी को देव हुए कोई सात-आठ दिन ही हुए थे। खाली गुफा में गाँधी जी थोड़ी ही देर बैठे तो उन्हें ॐ की सूक्ष्म ध्वनि महसूस हुई।
जिस स्थान में भगवान का चिन्तन मनन होता है वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है तो आदमी भगवान का चिन्तन मनन करता है वह कितना पवित्र हो जाता होगा ! इसीलिये भगवान के मार्ग में चलने वाले महापुरूषों का आदर करने वाला उन्नत होता है। रूपये देकर लेक्चर सुनने वाली पाश्चात्य परंपरा से केवल सूचनाएँ मिलती हैं, अमृत नहीं मिलता। गुरू और शिष्य के बीच वह सम्बन्ध होता है जो भगवान और भक्त के बीच होता है।
तुच्छ वस्तुओं के लिए गुरूपद नहीं है। गुरूपद इसलिए है कि जीव जन्म-जन्मांतरें की भटकान से बचकर अपने गुरूतत्त्व को जान ले, अपने महान् पद को जान ले ताकि बार-बार दुःख-योनियों में न जाना पड़े। सूकर, कूकर आदि दुःख-योनियों हैं।
श्रद्धा में एक ऐसी शक्ति है कि आप ईश्वर के किसी भी रूप को मानकर चलें तो समय पाकर गुरूओं का गुरू अन्तर्यामी परमात्मा भीतर से आपका प्रेरक बन जाता है। फिर ऐसे महापुरूष के पास आप पहुँच जाते हैं कि जिनकी पवित्र निगाह से, पवित्र आभा से आपका चित्त ईश्वर की ओर चलने लगता है। जिनकी निगाहों से, जिनके शरीर के परमाणुओं से, जिनके चित्त से ईश्वरीय आकर्षण, ईश्वरीय प्रेम तथा ईश्वरीय यात्रा के लिए जन-समाज को सहाय मिलती रहती है वे मनुष्य जाति के परम हितैषी रहते हैं। उन्हें आचार्य कहा जाता है।
आचार्यवान
पुरूषो वेद।।
वे अभक्त को भक्ति दे सकते हैं, योग दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं और ईश्वराभिमुख बना सकते हैं।
पढ़ लिखकर पदवी पाना एक बात है लेकिन रामकृष्ण की तरह, शंकराचार्य की तरह समाज के मन को ईश्वराभिमुख करना सबसे ऊँची बात है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
वे ही महापुरूष
बड़ा काम कर गये हैं,
उन्होंने जगत की सच्ची सेवा
की है जिन्होंने एकान्त सेवन किया
है, जिन्होंने आत्म विश्लेषण किया है, जिन्होंने
तुच्छ वस्तुओं का आकर्षण छोड़कर, तुच्छ वस्तुओं की चिन्ता
छोड़कर सत्य वस्तु का अनुसंधान किया है और निश्चिन्त नारायन
स्वरूप में विश्रान्ति पायी है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ