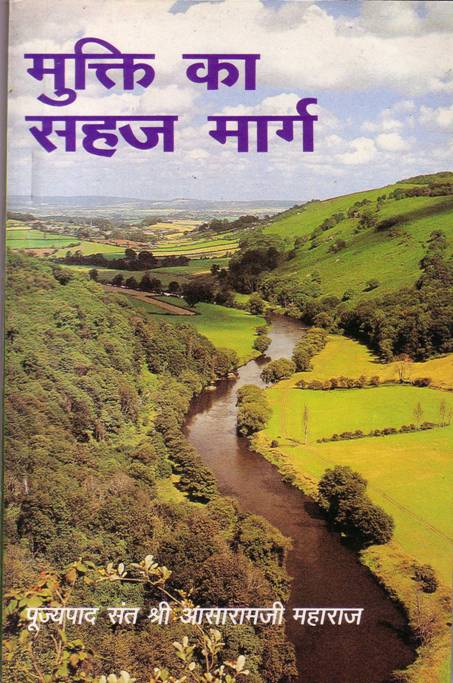
प्रातः
स्मरणीय
पूज्यपाद संत
श्री आसाराम जी
बापू के पावन
सत्संग-प्रवचन
मुक्ति का
सहज मार्ग
पूज्य
बापू का पावन
संदेश
हम धनवान होंगे या नहीं, यशस्वी होंगे या नहीं, चुनाव जीते या इसमें शंका हो सकती है परन्तु भैया ! हम मरेंगे या नहीं इसमें कोई शंका है ? विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है परन्तु इस जीवन की गाड़ी के छूटने का कोई निश्चित समय है ?
आज तक आपने जगत का जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है.... आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे, प्यारे भैया ! वह सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाएगा, जाना अनजाना हो जायेगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जायेगी।
अतः सावधान हो जाओ। अन्तर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, निजस्वरूप के अगाध आनन्द को, शाश्वत शान्ति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो।
जागो.... उठो.... अपने भीतर सोये हुए निश्चयबल को जगाओ सर्वदेश, सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा मे अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीन-हीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके।
सदा स्मरण रहे कि इधर-उधर भटकती वृत्तियों को बहकाओ नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना-काल में आत्मचिन्तन मे लगाओ और व्यवहार –काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शान्त वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवन्त एवं प्रसन्न रहो। जीवमात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो। दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरूषों के सत्संग एवं सत्साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदान्त से पुष्ट एवं पुलकित करो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
निवेदन
तत्त्वज्ञान को लोकभोग्य बनाकर रखना हो तो स्वाभाविक है कई बार आये, कई ढंग से आये और श्रवण के साथ आम जनता का मनन भी होने लगे।
इस पुस्तक में पूज्यपाद संत श्री आसारामजी महाराज के सत्संग प्रवचन ज्यों के त्यों दिये गये हैं। इसमें पुनरावृत्ति स्वाभाविक है। अतः साधक गुणग्राही दृष्टि से लाभ उठाने की कृपा करेंगे।
श्री
योग वेदान्त
सेवा समिति
अमदावाद
आश्रम
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
मुक्ति
का सहज मार्ग
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र
लोकोऽयं
कर्मबन्धनः।
तदर्थ
कर्म कौन्तेय
मुक्तसंगः
समाचर।।
'यज्ञ के निमित्त किये जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य-समुदाय कर्मों से बँधता है। इसलिए हे अर्जुन ! तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भाँति कर्त्तव्य कर्म कर।'
(भगवद्
गीताः 3.9)
सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माजी ने जीवों के दुःख की निवृत्ति का उपाय खोजा। जीव कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म यज्ञ के निमित्त नहीं हैं तो जीव दुःख को पाते हैं, जन्म-जन्मांतर को पाते हैं, अशांति को पाते हैं। अतः ब्रह्माजी ने यज्ञ करने की सलाह भी दी और यज्ञ करने की सामग्री भी दी।
यज्ञ वह है जो सृष्टिकर्त्ता के स्वरूप में विश्रान्ति दिला दे। जो कोई कर्म है उसमें यज्ञबुद्धि कर दे तो वह कर्म कर्त्ता को बन्धनों से छुड़ाता है। कर्म में भोगबुद्धि कर दी तो वह कर्म कर्त्ता को बाँधता है। कर्म में फलासक्ति, कर्म में संग-आसक्ति, कर्म में अहंपुष्टि अगर मिलती है तो वह कर्म कर्त्ता को बाँधता है।
कर्म में अगर यज्ञबुद्धि आ जाय, कर्म में अगर उदारता आ जाय, स्नेह आ जाय तो वह कर्म कर्त्ता को अपने स्वरूप का मान करा देता है।
कुछ लोग आलस्य, निद्रा के वश होकर कर्म का त्याग करते हैं वह तामसी त्याग है। तामस त्यागवाला मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। वृक्ष, पाषाण आदि मूढ़ योनियाँ हैं। कुछ लोग कर्म को दुःखरूप समझकर कर्म का त्याग करते हैं। यह राजस त्याग कहा जाता है। ये लोग दुःखयोनि को प्राप्त होते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म के रहस्यों को समझकर सात्त्विक त्याग करते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान से रवाना हो जाना चाहता है तो भगवान श्रीकृष्ण ने राजसी त्याग की अपेक्षा सात्त्विक त्याग का महत्त्व बताया है।
यज्ञार्थात् कर्म यानी यज्ञ के निमित्त किये जाने वाले कर्म। ऐसे कर्म सात्त्विक कर्म हैं। प्रकृति के मूल में देखा जाय, सृष्टि के मूल में देखा जाये तो यज्ञ हो रहा है। भगवान भास्कर प्रकट होते हैं, अनन्त-अनन्त जीवों को प्राणशक्ति देते हैं। पक्षी किल्लोल करते हैं, पेड़ पौधे लहलहाते हैं। यहाँ तक कि रोगी मनुष्य भी प्रभात काल में कुछ आश्वासन पा लेते हैं। सूर्यनारायण सतत यज्ञकर्म कर रहे हैं। चन्द्रमा यज्ञ कर्म कर रहे हैं। दरिया उछल कूद करके भी यज्ञ ही कर रहा है। पृथ्वी माता भी यज्ञ कर रही है प्रकृति के साथ तादात्म्य करें तो प्रकृति की गहराई में स्नेह है, उदारता है। प्रकृति का स्नेह और उदारता अपने परमात्म-स्वभाव से आया है। जीव का भी पारमार्थिक स्वभाव स्नेह और उदारता है लेकिन स्वार्थपूर्ण कर्म करता है तो स्नेह और उदारता संकीर्णता और शुष्कता में बदल जाती है। आदमी जब भीतर से संकीर्ण और शुष्क होता है तो उसके कर्म बाँधने वाले होते हैं। भीतर से जब स्नेह और उदारता से भर जाता है तो उसके कर्म परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। स्नेह और उदारता से किये जाने वाले यज्ञ-कर्म हैं। संकीर्णता से किये जाने वाले कर्म बन्धनकारक कर्म हैं।
व्यक्तित्व की संकीर्णता कुटुम्ब से अन्याय करवा देगी। कौटुम्बिक संकीर्णता पड़ोस से अन्याय करवा देगी। पड़ोस की संकीर्णता गाँव से अन्याय करवा देगी। गाँव की संकीर्णता प्रान्त से अन्याय करवा देगी। प्रान्त की संकीर्णता राज्य से अन्याय करवा देगी। राज्य की संकीर्णता राष्ट्र से अन्याय करवा देगी। राष्ट्र की संकीर्णता विश्व से अन्याय करवा देगी। यह नाम-रूप की आसक्ति और संकीर्णता ही नाम-रूप के आधार स्वरूप सच्चिदानन्द परमात्मा से मिलने में बाधा बन जाती है।
यज्ञ कर्म ये हैं जो तुम्हारी संकीर्णता छुड़ा दे और उदारता भर दे। ....तो जो कोई कर्म किये जायें वे यज्ञार्थ किये जायें, सेवा निमित्त किये जायें। आँखों को बुरी जगह जाने नहीं देना यह आँखों की सेवा है। वाणी को व्यर्थ नहीं खर्चना यह वाणी की सेवा है। मन को व्यर्थ चिन्तन से बचाना यह मन की सेवा है। बुद्धि को राग-द्वेष से बचाना यह बुद्धि की सेवा है। अपने को स्वार्थ से बचाना यह अपनी सेवा है और दूसरों की ईर्ष्या या वासना का शिकार न बनाना यह दूसरों की सेवा है। इस प्रकार का यज्ञार्थ कर्म कर्त्ता को परमात्मा से मिला देता है।
वास्तव में कर्त्ता का स्वभाव परमात्मा से मिलता-जुलता स्वभाव है। कर्त्ता ने बचपन देखा, कर्त्ता ने विफलता देखी। देखने वाला कर्त्ता तो वही का वही रहा... साक्षी। ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, रूपान्तर हुआ फिर भी सृष्टिकर्त्ता वही का वही। तो जीव-कर्त्ता और सृष्टिसर्जन-कर्त्ता दोनों का स्वभाव एक है। ईश्वर की आत्मा और अपनी आत्मा वास्तव में एक है। लेकिन अभागी वासनाओं ने, अभागे स्वार्थ ने हमको उस परम औदार्य स्वरूप और स्नेह की मधुरता से वंचित कर दिया।
जीवन में ऐसे कर्म किये जायें कि एक यज्ञ बन जाय। दिन में ऐसे कर्म करो कि रात को आराम से नींद आये। आठ मास में ऐसे कर्म करो कि वर्षा के चार मास निश्चिन्तता से जी सकें। जीवन में ऐसे कर्म करो कि जीवन की शाम होने से पहले जीवनदाता से मुलाकात हो जाय। ये सब कर्म यज्ञार्थ कर्म कहे जाते हैं।
तामस त्याग अधम योनि में ले जाता है। राजस त्याग दुःख देता है। सात्विक त्याग कर्त्ता को यज्ञार्थ कर्म कराता है। संयमी जीवन जीते हुए बच्चे को पेट में रखती है, सँभालती है यह भी यज्ञ है। अपनी सुख-सुविधा छोड़कर बच्चे को पालती-पोसती है यह भी यज्ञ है। संकीर्णता छोड़ते हुए, व्यक्तिगत विषय-वासना की लालच छोड़ते हुए जो कर्त्तव्य कर्म किये जाते हैं वह यज्ञ है।
यज्ञ केवल वेदी में ही, केवल यज्ञकुण्ड में ही नहीं होता, यज्ञ बाजार में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, कोर्ट में भी हो सकता है, स्मशान में भी हो सकता है। यज्ञ एकान्त में भी हो सकता है, भीड़ में भी हो सकता है। यज्ञार्थ कर्म कर्त्ता को अपने प्रियतम स्वभाव से मिला देता है।
क्रिया में बन्धन नहीं होता, क्रिया के भाव में बन्धन और मुक्ति निर्भर है। कर्म में बन्धन और मुक्ति नहीं, कर्त्ता के भाव में बन्धन और मुक्ति है। कर्त्ता किस भाव से कर्म कर रहा है ? राग से प्रेरित होकर कर रहा है ? द्वेष से प्रेरित होकर कर रहा है ? वासना से प्रेरित होकर कर रहा है ? .....कि परमात्मा-स्नेह से कर रहा है ?
वासना-तृप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्त्ता को बाँधता है। वासना-निवृत्ति के लिए जो यज्ञार्थ कर्म किये जाते हैं वे कर्त्ता को मुक्त स्वभाव में जगा देते हैं। कर्म किये बिना कोई रह नहीं सकता। अत्यंत आलस्य और प्रमाद में पड़े रहने से तो सकाम कर्म करना भी अच्छा है। आज का मनुष्य जहाँ स्वार्थ दिखता है वहाँ तो बड़ी छटपटाहट के साथ कार्य करता है। जहाँ देखता है कि अपना कोई बाह्य स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो वहाँ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। आज के कर्त्ता को पता नहीं कि स्वार्थ से प्रेरित होकर जो कर्म करता है वही कर्म उस बेचारे को बाँध देता है, अशान्त कर देता है, परमात्म-प्राप्ति की योग्यताएँ क्षीण कर देता है।
'स्वामी जी ! हम यज्ञार्थ कर्म करें, निष्काम भाव से कर्म करें, सेवाभाव से कर्म करें तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा ? सब लोग सेवा भाव से कर्म करने लग जायें तो गुजारा कैसे होगा ?' प्रश्न हो सकता है।
प्रकृति की गहराई में सब कार्य सेवाभाव से ही हो रहे हैं। सूर्यनारायण सेवाभाव से प्रकाश दे रहे हैं, चन्द्रमा सेवाभाव से शीतलता बरसा रहे हैं, वनस्पति को, औषधियों को पुष्ट कर रहे हैं, हवाएँ सेवाभाव से बह रही हैं, सागर सेवाभाव से लहरा रहा है। तुम्हारी इन्द्रियाँ भी तो सेवाभाव से तुम्हारे लिए कार्य कर रही है, तभी तो शरीर टिका है। आँख पदार्थ को देखती है लेकिन जिद्द नहीं करती कि पदार्थ मैंने देखा इसलिए मेरा हो गया, वह मुझमें भर दो। अगर पदार्थ को आँख में भर दिया तो आँख की सलामती नहीं रहेगी।
आँख पदार्थ को देखती है, हाथ उसे उठाता है। अब हाथ अगर आग्रह करे कि मैंने उठाया, मेरा हो गया, वह मुझमें भर दो तो यह सम्भव नहीं। अगर सम्भव भी कर दो तो हाथ निकम्मे हो जायेंगे। आँख ने देखा, यज्ञ कर। हाथ ने उठाया, मुँह को दे दिया, यज्ञ हो गया। मुँह चबाता है और गले को दे देता है। गला वह पदार्थ पेट को पहुँचा देता है। पेट उसमें से रस बनाकर शरीर में सब जगह भेज देता है। बाकी बचा हुआ त्याज्य कचरा अंतड़ियों से गुजरकर बाहर निकाल दिया जाता है। पेट अगर त्यागने योग्य चीज को पकड़ रखे तो बीमार हो जाय। शरीर के तमाम अंगों को देने योग्य रस का संग्रह कर बैठे तो अजीर्ण हो जायेगा, बीमारी से पीड़ित हो जायेगा। शरीर का पूरा तंत्र यज्ञस्वरूप चल रहा है।
प्रकृति की गहराई में यज्ञ हो रहा है। इसके साथ तादात्म्य कर दो तो प्रकृति के मूल स्वरूप परमात्मा को पा लोगे। जो भी मनुष्य यज्ञार्थ कर्म करते हैं वे मुक्ति को पाते हैं और यज्ञ से विरूद्ध कर्म करते हैं वे कर्म में बँध जाते हैं, दुःखों में घसीटे जाते हैं।
सुनी है कहानी। नगर के राजमार्ग से राजा की सवारी जा रही थी। एक बुढ़िया का लड़का कहने लगाः "माँ ! मुझे राजा से मिलना है।"
माँ बोलीः "बेटे ! हम गरीब लोग.... तेरे पिता कई वर्ष पूर्व चल बसे..... अपनी कोई पहुँच नहीं है। राजा से मिलना कोई साधारण बात नहीं है।"
"कुछ भी हो, माँ ! मुझे राजा से मिलना ही है।" बेटे ने हठ कर ली। माँ ने युक्ति बताते हुए कहाः
"बेटा ! एक उपाय है। राजा का महल बन रहा है वहाँ जाकर काम में लग जा। सप्ताह के बाद तनख्वाह मिलेगी तो लेना मत। बस उत्साह से काम में लगे रहना।"
लड़का काम में लग गया। बड़ी तत्परता और चाव से लगा रहा। एक हफ्ता बीता, दूसरी बीता, तीसरा भी गुजर गया। लड़का तनख्वाह लेने का इन्कार करता और काम बड़े उत्साह के साथ करता। वजीर ने देखाः अजीब लड़का है ! बढ़िया काम करता है और अपनी मजदूरी के पैसे नहीं लेता ! वजीर के दिल पर लड़के के लिए अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जाकर राजा को बताया तो राजा ने उस बच्चे को बुलाया। उत्साह और तत्परता एवं अहोभाव से काम करने वाले बच्चे की वाणी में माधुर्य था, दिल में उदारता थी। राजा को मिलने में जो स्नेह था वह उमड़ आया। राजा के दिल पर बच्चे का जादू-सा प्रभाव पड़ा। राजा बोलाः
"आज से यह लड़का महल बनाने के काम में नहीं अपितु मेरी अंगत सेवा के कार्य में लगा दिया जाय।"
वजीर बोलाः "जो आज्ञा राजन् !"
बच्चा राजा के महल में सेवा कार्य करने लगा। महल का खान-पान और निवास तो मिलना ही था। राजमहल के भोजन और निवास की इच्छा रखकर कोई कार्य करे तो उसको ऐसा भोजन और निवास मुश्किल से मिलता है। सेवा के लिए सेवा करने वाले बच्चे को भी भोजन और निवास मिल ही गये। मानो बच्चे का काम करना काम न रहा, यज्ञ हो गया।
'सेवा के लिए शरीर को टिकाना है' यह भाव आ जाय तो जीवन यज्ञ बन जाय। भोग के लिए शरीर को टिकाया तो बन्धन हो गया। परहित के कार्य करने के लिए शरीर को तन्दुरूस्त रखना यह यज्ञ हो गया। अपने को कुछ विशेष बनाने के लिए शरीर का लालन-पालन किया तो बन्धन हो गया।
जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वे बड़े आनन्द से जीते हैं, बड़ी मौज से जीते हैं। जितना-जितना निःस्वार्थ भाव होता है उतना-उतना भीतर का रस छलकता है। मन बुद्धि विलक्षण शक्ति से सम्पन्न हो जाते हैं।
विधवा माई के बच्चे को राजा की सेवा मिल गई, राजा का संग मिल गया उसकी बुद्धि ने कुछ विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। रानी का हृदय भी उसने जीत लिया।
व्यक्ति जितना निःस्वार्थ होता है उतनी उसकी सुषुप्त जीवनशक्ति विकसित होती है। आदमी जितना स्वार्थी होता है उतनी उसकी योग्यताएँ कुण्ठित हो जाती हैं। अपने अहं को पोसने के लिए आदमी जितना काम करता है उतना ही वह अपनी क्षमताएँ क्षीण करता है। श्रीहरि को प्रसन्न करने हेतु जितना कार्य करता है उतनी उसकी क्षमताएँ विकसित होती हैं।
उस बच्चे की क्षमताएँ विकसित हो गईं। उसने अपने सुन्दर कार्यों से राजा-रानी का हृदय जीत लिया। दोनों के दिल-दिमाग में बच्चे की निर्दोषता एवं कार्य की तत्परता का प्रभाव छा गया। एक दिन राजा ने रानी से कहाः
"हमें कोई सन्तान नहीं है। इस बालक को गोद ले लें और अपना राजकुमार घोषित कर दें तो ?"
रानी हर्ष से बोल उठीः "हाँ हाँ..... मैं भी तो यही चाहती थी लेकिन आपसे बात करने में जरा संकोच होता था। आज आपने मेरे दिल की ही बात कह दी अब विलम्ब क्यों ? शुभस्य शीघ्रम्। राजपुरोहित को बुलाइये और....।"
दोनों ने निर्णय ले लिया और बच्चे को अपना पुत्र घोषित करके राजतिलक कर दिया। महल में और सारे नगर में आनन्दोत्सव मनाया गया। राजमार्ग पर दोनों की शोभायात्रा निकली। राजा और राजकुमार का अभिवादन करने के लिए सड़कों पर प्रजा की भीड़ हो गई। कुमार ने अपनी बुढ़िया माँ को देखा। उसके नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। अपनी वात्सल्यमयी माँ से मिलने के लिए वह लालायति हो उठा। वह राजा से बोलाः
"महाराज श्री ! वहाँ देखो, मेरी माँ खड़ी है जिसने मुझे आपसे मिलने का रास्ता दिखाया था। मैं उसके चरण-स्पर्श करने को जाऊँ ?"
"तू अकेला ही नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ।"
दोनों रथ से नीचे उतरे और जाकर बुढ़िया को प्रणाम किया। बुढ़िया के पास कैसी अदभुत कुंजी थी सत्संग की ! उसने बेटे को सिखाया था कि तू निष्काम भाव से कर्म कर। अन्यथा, लड़के के पास कोई हथियार नहीं था कि राजा को वश कर ले। उस बुढ़िया के पास भी कोई हथियार नहीं था कि राजा आकर उसके पैर छुए।
निष्कामता एक ऐसा अनुपम हथियार है कि जीव को ईश्वर के पास नहीं जाना पड़ता है, ईश्वर ही जीव के पास आ जाता है। बुढ़िया को राजमहल के द्वार नहीं खटखटाने पड़े, राजा स्वयं उसके घर आ गया। निष्कामता से उस बच्चे का चित्त इतना विकसित हुआ, इतना उन्नत हुआ कि वह स्वयं राजा बन गया। राजाओं का भी जो राजा है परमात्मा, उसको भी प्रसन्न करना चाहें तो यज्ञार्थ कर्म किये जायें। यज्ञार्थ कर्म करने से हृदय में तृप्ति होती है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। मनु महाराज कहते हैं-
"जो कार्य करने से तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है, जो महापुरूषों के द्वारा अनुमोदित है और शास्त्र-सम्मत है वह कार्य सत्कार्य है !"
यहाँ कोई आपत्ति उठा सकता है कि शराबी का हृदय तो शराब पीने से प्रसन्न होता है, जुआरी का हृदय जुआ खेलने से खुश होता है, भोगी का हृदय भोग भोगने से खुश होता है तो ये पुण्यकार्य हैं ? सत्कार्य हैं ?
नहीं। ये कार्य सत्कार्य नहीं। सत्कार्य की व्याख्या में हृदय की प्रसन्नता के अलावा दो शर्तें और भी हैं- कार्य महापुरूषों के द्वारा अनुमोदित हो और शास्त्र-सम्मत हो।
महापुरूषों के द्वारा वही बात अनुमोदित होगी जो शास्त्र-सम्मत हो, सदाचारयुक्त हो, कल्याणकारी हो।
जाति सम्प्रदाय, समाज, वर्ण आदि कुछ हद तक तो उचित हैं, अच्छे हैं। ये सब आदमी के कुलधर्म आदमी की वासनाओं को नियन्त्रित करने में उपयोगी है। जातीयता और सामाजिकता व्यक्ति के कार्यों को व्यक्तिगत न रखकर समाज तक पहुँचाने में सहायभूत होते हैं। लेकिन जातीयता का भेदभाव करके मनुष्य मनुष्य से जब नफरत करने लगता है तो वही जातीयता खतरा पैदा करती है। ऐसे ही सम्प्रदाय कुछ नीति-नियम बनाकर हमारी वासनाओं को नियन्त्रण करके हमें ऊपर उठाता है तब तक तो ठीक है लेकिन एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय से, एक पार्टी दूसरी पार्टी से दलबन्दी करके हमारे चित्त में संकीर्णता के संस्कार आबद्ध करते हैं तो गड़बड़ है। सम्प्रदाय या पार्टीबाजी हमें अपने ही चक्र में बाँधकर रखना चाहते हैं तो वे हानिकारक हो जाते हैं।
सब चीजें आदमी की योग्यता पर निर्भर करती हैं। कोई चीज एक आदमी के लिए हितकर है और दूसरे के लिए अहितकर भी हो जाती हैं। जैसे, "नारायण हरि" करके भिक्षा माँगकर खाना संन्यासी के लिए हितकर है लेकिन गृहस्थी आदमी अगर भिक्षा का अन्न खाय तो उसके लिए हितकर नहीं है। विरक्त महापुरूष शिखा-सूत्र-यज्ञोपवित का त्याग कर के संन्यास ले लें तो उनके लिए हितकर है लेकिन भोगी आदमी शिखा-सूत्र-यज्ञोपवित का त्याग कर दे, नीति नियम छोड़कर संन्यासी का वेश धारण कर ले तो यह अहितकर है।
कुछ नीति-नियम, रीत-रिवाज समाज को ऊपर उठाने के लिए हैं लेकिन उन्हीं रीति-रिवाजों को पकड़े रखकर ऊपर उठने के बजाय आदमी जब संकीर्ण दायरा बना लेता है, जटिल हो जाता है तो वे बन्धन कारक हो जाते हैं।
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- "जो कर्म करते हो, यज्ञार्थ कर्म करो।"
लोग फल तो खाना चाहते हैं लेकिन फलदायी वृक्ष को काट देते हैं। उन्नत होने चाहते हैं, यश-सुख-आनन्द चाहते हैं लेकिन यशस्वी होने के, आनन्दित होने के, सुखी होने के निष्काम कार्य में सकामता का कुल्हाड़ा मार देते हैं।
जितना-जितना यज्ञबुद्धि से कर्म होता है उतना-उतना कर्त्ता अपने आत्म-स्वभाव में जगता जाता है। जितना स्वार्थबुद्धि से कर्म करता है उतना-उतना कर्त्ता पर स्वभाव में प्रविष्ट होता जाता है।
स्वधर्मे
निधनं श्रेयः परधर्मो
भयावहः।
स्वधर्म, स्वकर्म, अपने हिस्से आये हुए सत्कृत्य, अपनी जवाबदारी के कर्त्तव्यकर्म करते-करते मर जाना अच्छा है लेकिन परधर्म भयावह है। माता-पिता का स्वधर्म है बच्चों का पालन-पोषण करना। माँ बच्चे का लालन-पालन करती है, यह यज्ञकर्म है। लेकिन माँ अगर बाद में सोचने लगे कि बच्चा अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, कमाने लगा, अब मुझे सुख दे, तो यह गड़बड़ हो गई। अब माँ को सुख देना बच्चे का कर्त्तव्यकर्म है लेकिन माँ की अपेक्षा बनी रही उससे सुख पानी की तो, यह यज्ञकर्म में विघ्नरूप बन जाएगा। अपने हिस्से का कर्त्तव्यकर्म करते जाओ। दूसरा इसका बदला क्या देगा उधर ध्यान दिया तो यज्ञार्थ कर्म नहीं रहा।
सेवा करने वाला सामने वाले के गुणदोष देखेगा तो सेवा नहीं कर पायेगा। यज्ञार्थ कर्म करते जाओ। अपना कर्त्तव्य निभाते जाओ।
कोई सुखी आदमी बाजार से गुजर रहा था। रास्ते में एक बीमार आदमी अकेला पड़ा था, खाँस रहा था, निःसहाय होकर रोग से पीड़ित हो रहा था। बड़ा लाचार दिखता था। सुखी आदमी ने पूछाः
"सेवा करने वाला, दवाई इलाज करने वाला कोई नहीं है ?"
"बाबू जी ! मैं अकेला हूँ। दुनियाँ में मेरा कोई नहीं है.....!"
उस आदमी को दया आ गई। उठवाकर रोगी को अपने घर ले आया। डॉक्टर को बुलवाकर इलाज करवाया। बिस्तर पर सुलाया। यह है यज्ञार्थ कर्म। अभी तक कर्त्ता का सात्त्विक भाव है।
रोगी का इलाज होता रहा। वह खाँसता रहा। कुछ आराम भी महसूस करता रहा। कर्त्ता के मन में उसे देखकर विचार आयाः "यह पड़ा था फुटपाथ पर। मैं दया कर के इसे यहाँ ले आया हूँ। ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता।"
वह आदमी अब सात्त्विकता में से राजस में आ गया। अपने आपको बड़ा सेवाभावी समझने लगा।
कुछ समय और बीता। खाँसने वाले रोगी ने खाँसते-खाँसते दीवार पर थूक दिया, गन्दगी कर दी। अब कर्त्ता को आ गया गुस्सा। वह बोल उठाः "तुम लोग तो फुटपाथ के ही अधिकारी हो। चल, निकल जा बाहर'। निःसहाय रोगी को घर से बाहर निकाल दिया। कर्त्ता तमस् से आक्रान्त हो गया।
प्रारम्भ में यज्ञार्थ कर्म तो हुआ। कर्त्ता सावधान नहीं रहा तो रजस् आ गया। रजस् के पीछे तमस् भी आ गया।
रजस् तमस् जब आने लगे तब कर्त्ता को सावधान होकर समझना चाहिए, सोचना चाहिये किः 'मैं लाया क्या था ? ले क्या जाना है ? जगन्नियन्ता ने जो कुछ दिया है वह उसी की सेवा में लग जाये, यही जीवन की कृतत्यता है।' ऐसा समझकर कर्त्ता अगर यथायोग्य कार्य करता है तो वह कार्य यज्ञरूप बन जायेगा, अपने आनन्द-स्वरूप, सुख-स्वरूप, मुक्त-स्वरूप आत्मदेव में जगने के लिए काबिल होता जायेगा। सब कर्म यज्ञार्थ करे और यथायोग्य करे। ऐसा नहीं कि यज्ञार्थ कर्म में कुत्ते को खाने के लिए घास डाल दे और गाय को रोटी खिला दे। यह कोई यथायोग्य कार्य नहीं है।
कर्त्ता यथायोग्य कर्म तो करे लेकिन अपने पुण्य कार्य का, यज्ञार्थ कार्य का, सत्कर्म का अहंकार न करे। पानी का ग्लास कह दे कि मैं लोगों की प्यास बुझाता हूँ तो वह पागल है। बल्ब कह दे कि मैं अन्धकार मिटाता हूँ तो वह पागल है। बल्ब को जहाँ से अन्धकार मिटाने की शक्ति मिलती है उसको भूलकर वह स्वतन्त्र रीति से अन्धकार नहीं मिटा सकता। प्यास बुझाने का अहंकार करने वाला ग्लास अपने मूल स्रोत पानी के बिना कैसे मिटा सकता है ?
ऐसे ही यह कर्त्ता अनन्त चैतन्य सत्ता से जुड़ा है, विश्वेश्वर से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। उस परमात्मा से अपने को अलग करके अगर कोई सत्कर्म करने का अहंकार करता है तो कर्त्ता बँध जाता है।
आपके पास जो कुछ है वह यज्ञार्थ कर्म में लगा दो तो आपको और ज्यादा मिलता जायेगा। आपके पास जो कुछ है उसको स्वार्थ में संकीर्ण कर दो तो मिलना कम हो जायेगा और जो है वह परेशानी पैदा कर देगा।
एक छोटी-सी कहानी है। एक बार नदी और तालाब के बीच 'तू-तू.... मैं-मैं' हो गई। तालाब ने नदी से कहाः "पगली ! रूक जा। भागी जा रही है नादान ! कल-कल.... छल-छल गुनगुनाती, भागती, कितनी टक्करें सहती हुई दौड़ी जा रही हैं ! वहाँ खारा समुद्र है। अपना बिलौरी काँच जैसा निर्मल जल बहाती वहाँ जायेगी तो मिट जायेगी, नष्ट हो जायेगी। जरा रूक जा, थाम ले अपने आपको। वह खारा दरिया तुझे देगा क्या ? वह तो कृतघ्न है। कई नदियाँ उसमें समा गई। तेरा अस्तित्व भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा।"
नदी ने कहाः "भैया ! रूकना, थमना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं आलसी नहीं हूँ, प्रमादी नहीं हूँ। मुझे तो बहने दें.. चलने दें। मेरा जीवन तो पक्षपात रहित परोपकार के लिए ही है 'सर्वजनसुखाय..... सर्वजनहिताय' मेरा जीवन है। ऐसा नहीं कि गाय आयी तो मीठा जल दूँ और शेर आये तो जहर डाल दूँ, सज्जन नहाये तो शीतलता दूँ और दुर्जन नहाये तो पानी गर्म कर दूँ। ना.... ना..... । मेरा तो स्वभाव है सबके लिए निरन्तर बहते रहना। लोग 'गंगे हर... यमुने हर.... नर्मदे हर...' करें चाहे न करें लेकिन यज्ञार्थ जीवन जीना हमारा स्वभाव है।"
तालाब ने किसी को देना सीखा नहीं। संग्रह करना उसका स्वभाव है। समय पाकर उसका पानी गन्दा हो गया, बदबू आने लगी, मच्छर हो गये इर्दगिर्द। वहाँ से रोग के कीटाणु फैलने लगे। लोगों ने देखा कि तालाब गन्दगी फैलाता है, रोग फैलाता है तो नगरपालिका ने उसमें नगर का सारा कूड़ा-कचरा डालकर तालाब को भर दिया। जो संग्रह करना चाहता था वह गंदगी से भर गया। उसका अस्तित्व मिट गया। बहने वाली सरिता सदा बहती रही। बादलों ने उसको समृद्ध बनाया। पहाड़ों पर जमे हुए बर्फ ने गर्मी के मौसम में पिघलकर उसे वैभववान बनाया। सरिता सदा गुनगुनाती रही और तालाब का अस्तित्व मिट गया।
जिसके जीवन में यज्ञार्थ कर्म होते हैं उसकी योग्यताएँ निखरती रहती हैं। नया-नया परमात्मा-रस उसके द्वारा फैलता रहता है। जो लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बाहर का सुख पाने के लिए, बाहर की वाहवाही और यश पाने के लिए, धन के लिए, मान के लिए, अहं पोसने के लिए, राग-द्वेष और मोह-मदिरा से उन्मत्त होकर कर्म करते हैं वे अपने को बाँध देते हैं। जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वे परमात्मा को पा लेते हैं।
प्रकृति के मूल में देखा जाए तो उदारता और स्नेह भरा है। ऐसा कौन-सा हमारा पुरूषार्थ है कि हम परमात्म-साक्षात्कार कर सकें ? यह परमात्मा की उदारता है हमें मनुष्य जन्म मिला है। यह परमात्मा की उदारता है ऐसी बढ़िया बुद्धि मिली है। .....और यह भी उदारता है परमात्मा की कि श्रद्धा के साथ विवेक है। यह भी उसी की उदारता है कि हम सत्संग में जा सकते हैं। यह भी उदारता है कि सत्संग सुनकर हम मनन कर सकते हैं, मनन करते-करते यज्ञार्थ कर्म में आगे बढ़ सकते हैं। .....और यह भी उसी की उदारता है कि एक दिन वह वह नहीं रहेगा... हम हम नहीं रहेंगे... सब एकाकार.... हम न तुम... दफ्तर गुम।
ऐसी महान् पदवी पर पहुँच सकने वाला जीव अगर स्वार्थप्रेरित, हल्के, निकम्मे कृत्य करता है, वासनाएँ पूरी करने के लिए कर्म करता है तो जन्मान्तर में निम्न योनियों में चला जाता है, वृक्ष बन जाता है, पशृ-पक्षी कीट पतंग बन जाता है। आलसी, प्रमादी जीवन जीने वाला जीव मूढ़ योनियों को पाता है, कँटीला पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है। कभी पानी मिला न मिला। ऐसे ही दुःख भोगता है और समय पाकर पानी के बिना सूख जाता है। जब वह मनुष्य था तब किसी को कुछ दिया नहीं, किसी की सेवा की नहीं। ऐसे जीव बारिश के समय पैदा तो हो जाते हैं लेकिन बाद में बारिश के बिना तड़प-तड़प कर मर जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरों के काम आने वाले पेड़-पौधे भी अच्छी तरह जीते हैं। गाय-भैंस भी अच्छी होती है, उपयोगी होती है तो चारा मिलता है। उपयोगिता कम होते ही चारा पानी का हिसाब बदल जाता है।
ऐसे ही तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, तुम्हारी बुद्धि आदि ' बहुजनसुखाय ...... बहुजनहिताय ' प्रवृत्ति करके अगर सर्वेश्वर के कार्य में काम आते हैं तो सर्वेश्वर की सत्ता-स्फूर्ति-बल-बुद्धि-ओज-तन्दुरूस्ती आदि सब मिलता रहता है, समझ बढ़ती रहती है। अगर स्वार्थ में आ गये तो बुद्धि संकीर्ण बन जाती है।
यज्ञार्थ कर्म का अर्थ हैः कर्त्ता को पहले भीतर से उत्साह होना चाहिए कि यह सेवाकार्य मुझे करना चाहिए। जबरन सेवाकार्य नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि 'मैं सेवा कर रहा हूँ.... तुम सहयोग दो..... सहयोग दो.....।' सेवा के नाम से पैसे इकट्ठे करके महल बाँधकर रहने लगे यह यज्ञार्थ कर्म नहीं है। यज्ञार्थ कर्म अपने से शुरू होता है। दान का प्रारम्भ अपने घर से, सेवा का प्रारम्भ अपने शरीर से। जो लोग अपने आलीशान बंगले बना लेते हैं, महल खड़े कर देते हैं, विदेशी बैंकों में धन राशि जमा कर लेते हैं और चिल्लाते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो यह धोखा है।
सचमुच में अगर सेवा है तो आत्म-साक्षात्कार हो जाय। सचमुच में अगर सेवा है तो रात्रि को बढ़िया नींद आयेगी। सचमुच में अगर सेवा है तो चित्त में परमात्मा का ध्यान करने की रूचि जग जाएगी।
कर्त्ता को कर्म ऐसा करना चाहिए कि कर्म करते-करते वासना निवृत्त हो जाय। कर्त्ता को जीवन ऐसा बना लेना चाहिए कि वह जन्म-मरण से पार हो जाय।
जो लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, प्रजा पर कर (टेक्स) बढ़ाते रहते हैं, अपने महल बनाते रहते हैं और झंडा उठाये देश की सेवा का, राष्ट्र की सेवा का तो यह उनका यज्ञकर्म नहीं है, अहंकर्म है। अहंकर्म आदमी को बेचैन कर देता है और यज्ञकर्म आदमी को यज्ञपुरूष के साथ, परमात्मा के साथ मिला देता है।
यज्ञार्थत्कर्मणोऽन्यत्र
लोकोऽयं
कर्मबन्धनः।
तदर्थं
कर्म कौन्तेय
मुक्तसंगः
समाचर।।
''यज्ञ के निमित्त किये जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य-समुदाय कर्मों से बँधता है। इसलिए हे अर्जुन ! तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त ही भलीभाँति कर्त्तव्य कर।"
स्वार्थपूर्वक कर्म करने से तो अल्प चीज मिलती है जबकि निःस्वार्थ होकर कर्म करने से अनन्त परमात्मा मिलता है।
यज्ञो
दानं तपश्चैव
पावनानि
मनीषिणाम्।
'यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरूषों को पवित्र करने वाले हैं।'
(भगवद् गीताः 18.5)
वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्यागकर केवल प्रभु-प्रीत्यर्थ कर्म करता है। यज्ञ, दान और तप से बुद्धि पावन होती है। संसार के जो भी दुःख हैं वे सब प्रज्ञा के दोष से हैं, बुद्धि की मन्दता से हैं। स्वार्थ से कर्म करने से बुद्धि मन्द हो जाती है और निःस्वार्थ कर्म करने से बुद्धि खिल उठती है।
लोग भगवान की आराधना-उपासना करते हैं, अर्चना-सेवा-पूजा करते हैं उसमें भी फलस्वरूप कुछ मिल जाये, अपना ऐहिक कार्य सिद्ध हो जाय ऐसी आकांक्षा रखते हैं। ऐसी सेवा-पूजा में भीतर का रस नहीं खुलता। सहज भाव से सेवा-पूजा होती है, हम भगवान के हैं.... भगवान हमारे हैं, ऐसे आत्मिक भाव से स्नेहपूर्वक सेवा पूजा होती है तो वह जल्दी फल जाती है, भीतर आनन्द का स्रोत खोल देती है। इससे प्रज्ञा पावन होने लगती है।
मंदिर में कुछ स्वार्थ-भाव का संकल्प लेकर दर्शन करने जाते हैं तो यह कहने भर का दर्शन है और निःस्वार्थ भाव से जाते हैं तो दर्शन का मजा कुछ निराला ही है। जितना-जितना हृदय में निःस्वार्थता भरते जायेंगे उतना-उतना हृदय आन्तरिक सुख से छलकता जायेगा, अन्तर ज्योत से अलोकित होता जायेगा। हृदय जितना स्वार्थ से भरा होगा उतना आदमी पराधीन होता जाएगा। यह काम करूँ तो मुझे यह फायदा हो जायेगा...... वह काम करूँ तो मुझे वह फायदा हो जाएगा..... ऐसा सोचविचार करके स्वार्थपूर्ण कर्मों में उलझे रहने वाले लोगों का दिल-दिमाग संकीर्ण रह जाता है।
उड़ियाबाबा, हरिबाबा, आनन्दमयी माँ और हाथीबाबा ये आपस में मित्र संत थे। एक बार उनके पास कोई आदमी आये और पूछाः
"बाबाजी ! भगवान का नाम लेने से क्या फायदा ?" हाथीबाबा ने उड़ियाबाबा से कहाः "यह कोई बनिया है, वैश्य है। बड़ा स्वार्थी आदमी। भगवान का नाम लेने में भी फायदा ही फायदा ढूँढता है।" फिर उस आदमी से बोलेः
"अरे भाई ! भगवान का नाम स्नेह से लिया जाता है। उसमें क्या फायदा, कितना फायदा, इसका बयान करने वाला कोई वक्ता ही पैदा नहीं हुआ। भगवन्नाम-स्मरण से क्या लाभ होता है इसका बयान कोई नहीं कर सकता। नाम का बयान करते-करते सब नाममय हो गये लेकिन नाम का बयान पूरा नहीं हुआ। भगवान के नाम की महिमा का संपूर्ण बयान हो ही नहीं सकता।"
राम
न सकहिं नाम
गुण गाई।
भगवान खुद ही नाम की महिमा गा नहीं सकते तो दूसरों की क्या बात ?
मंत्रजाप
मम दृढ़
विश्वासा।
पंचम
भक्ति यह वेद
प्रकाशा।।
"मंत्रजाप और दृढ़ विश्वास यह भक्ति का पाँचवा सोपान है।" ऐसा तो कह दिया लेकिन नाम की महिमा का पूरा बयान नहीं हो सका।
कबीर और कमाल की कथा है। रामनाम से एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया तो कमाल समझता है कि मैं रामनाम की महिमा जानता हूँ। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने एक तुलसीपत्र पर राम शब्द लिखकर वह तुलसीपत्र पानी के घड़े में घोंट दिया। फिर उस पानी से पाँचसौ कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कमाल ने माना कि रामनाम से एक ही कोढ़ी नहीं बल्कि पाँच सौ कोढ़ी एक साथ ठीक हो सकते हैं। ऐसी राम नाम की महिमा है। इससे भी कबीर जी सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कमाल को भेजा सूरदास के पास। सूरदासजी ने गंगा में बहते मुर्दे को निकलवाया। उसके कान में राम शब्द का केवल र बोलने मात्र से मुर्दा जिन्दा हो गया। कमाल समझा कि रामनाम के 'र' कार मात्र से मुर्दा जिन्दा हो सकता है इतनी भारी महिमा है रामनाम की। कबीर जी ने कहाः "नहीं नहीं..... इतनी सी नहीं है मेरे राम जी की महिमा। रामनाम की महिमा का बयान करना हमारे बस की बात नहीं है।"
भृकुटी
विलास सृष्टि
लय होवहिं।
जिसने भृकुटी विलास मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है, प्रलय हो सकता है, उनके नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या कर सकोगे ?
अजब
राज है इस
मुहब्बत के
फसाने का।
जिसको
जितना आता है
उतना ही गाये
चला जाता है।।
भगवन्नाम की महिमा का पूरा बयान कोई नहीं कर सकता। बयान जितना करते हैं थोड़ा ही पड़ता है। सत्संग से कितना लाभ हो सकता है उसका बयान आज तक कोई नहीं कर सका। भील वालिया लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन गया नारदजी के सत्संग से। नारद जी स्वयं एक साधारण दासीपुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन। उनकी माँ किसी के वहाँ चाकरी करती थी। वहाँ संत-महात्मा पधारते। दासी अपने पुत्र को भी साथ ले जाती और उन संतों के सत्संग से पुत्र आगे चलकर देवर्षि नारद बन गया। मैत्रेय ऋषि पूर्व जन्मों में कीड़ा थे। वेदव्यास जी के संग से जन्मों जन्म उन्नति करके आखिर में ऋषि बन गये। सत्संग की महिमा लाबयान है।
सनकादि ऋषि ईश्वर कोटि के थे फिर भी सत्संग करते। चार में से एक वक्ता बन जाते, तीन श्रोता। शिवजी भी सत्संग करते और पार्वती जी सुनती। वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जावे सत्संग सुनने के लिए।
सत्संग पापी को पुण्यात्मा बना देता है, पुण्यात्मा को धर्मात्मा बना देता है, धर्मात्मा को महात्मा बना देता है, महात्मा को परमात्मा बना देता है और परमात्मा को....? अब आगे वाणी नहीं जा सकती।
मैं
संतन के पीछे
जाऊँ जहाँ
जहाँ संत
सिधारे......
क्या कंस को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है ? वह तो "हार्ट अटैक" से भी मर सकता था। रावण को मारने के लिए अवतार लिया होगा रामचन्द्रजी ने ? राक्षस तो अन्दर अन्दर ही लड़कर मर सकते थे, अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उस बहाने सत्संग का प्रचार प्रसार होगा, ऋषियों का सान्निध्य मिलेगा, सत्संग बँटेगा, सत्संग का प्रसाद भक्त समाज तक पहुँचेगा इस हेतु से रामजी आये।
परब्रह्म परमात्मा का बयान पूरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बयान किया जाता है बुद्धि से और बुद्धि है प्रकृति में। परमात्मा है प्रकृति से परे। ब्रह्म-परमात्मा के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति में ये तमाम तमाम जीव हैं और जीवों में जरा सी बुद्धि। वह छोटी-सी बुद्धि परमात्मा का क्या बयान करेगी ? बुद्धि से सच्चिदानंदघन परमात्मा का पूरा बयान नहीं किया जा सकता।
वेद कहते हैं- "नेति.... नेति....नेति....।" यानि, न इति... न इति.... न इति....। पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, वायु नहीं, आकाश नहीं। इससे भी परे, जो है वह है परमात्मा।
जो कुछ हम बने हैं शरीर रूप में, वह पंचभूतों को ही समूह है। पंचभूतों के ही हम फूल हैं, और क्या हैं ? मनुष्य, प्राणी, वनस्पति आदि सब कुछ इन पंच तत्त्वों से ही आता है। परमात्मा इन सबसे परे है, उसका बयान कैसे होगा ? बुद्धि जब उसका बयान सचमुच करने लगती है तो जितना-जितना बयान होता है उतनी-उतनी वह परमात्मामय होती जाती है। परमात्मा का बयान अगर पूरा किया तो फिर वह बुद्धि प्रकृति की बुद्धि नहीं बचती, वह परमात्म-स्वरूप हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि में प्रविष्ट हो जाय तो गर्म होकर अग्निमय बन जाता है।
परमात्मा का बयान भी भोगबुद्धि से नहीं, यज्ञार्थबुद्धि से होगा तभी बुद्धि परमात्ममय बनने लगेगी। बयान करने वाला यज्ञार्थ कर्म करे तभी यह सम्भव हो सकेगा। 'चलो, परमात्मा की चर्चा कर ली, कथा कर ली, दक्षिणा मिल गयी, रूपये-पैसे, फल-फूल, भेंट-सौगात मिल गई, अपना काम बन गया...' यह यज्ञार्थ कर्म नहीं हुआ। सत्संग करें यज्ञार्थ, जप करें यज्ञार्थ, सेवा करें यज्ञार्थ।
किसी को पानी पिलाना भी यज्ञ है, भोजन कराना भी यज्ञ है, दुःखी को आश्वासन देना भी यज्ञ है, बहिर्मुख को अन्तर्मुख करना भी यज्ञ है, दुश्चरित्रवाले को सच्चरित्र में लगाना भी यज्ञ है, निगुरे को सगुरा बनाना भी यज्ञ है, नास्तिक को आस्तिकता की ओर मोड़ना भी यज्ञ है।
ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं किः "मैं साधक बनकर सुखी हुआ हूँ तो और दस लोगों को साधक बनाना मेरा कर्त्तव्य है।'' ऐसे लोग भी हो गये जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि प्रतिदिन पाँच साधक बनाऊँगा, बाद में भोजन लूँगा। प्रतिदिन पाँच साधक नहीं बना पायें तो एक ही बनायें। प्रतिदिन एक नहीं तो सप्ताह में एक, महीने में एक साधक बनायें। यह भी यज्ञार्थ कर्म है।
भगवन्नाम का निःस्वार्थ भाव से स्नेहपूर्वक जप करना भी यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं-
यज्ञानां
जपयज्ञोऽस्मि।
यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ।
जप करके अपना शारीरिक, ऐहिक सुख सुविधा बढ़ाने की आकांक्षा है, अहं सजाने-बढ़ाने की इच्छा है तो यह यज्ञकर्म नहीं रहा, गड़बड़ी हो गयी। स्नेहपूर्वक जप, नाम-स्मरण करना अपना स्वभाव बन जाय, दान करना हमारा स्वभाव बन जाय, परहित करना हमारा स्वभाव बन जाय, यह हो गया यज्ञार्थ कर्म।
जो दूसरों को सुख देता है वह स्वयं दुःखी कैसे रह सकता है ? जो दूसरों को मान देता है उसको मान की क्या परवाह रहेगी ?
आजकल घर घर में, कुटुम्ब में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में इतना कलह क्यों ? क्योंकि यज्ञार्थ कर्म को भूल रहे हैं, अहंकारार्थ कर्म हो रहे हैं। राग और द्वेष से प्रेरित होकर, अहंकारपूर्वक जो कर्म होते हैं वे मनुष्य जाति को खतरे में डालते हैं। ये जो मानव-संहार के लिए बम बनाये जाते हैं वह क्या यज्ञार्थ कर्म हैं ? मनुष्य जाति का ही शोषण करके करोड़ों अरबों रूपये एकत्रित किये जाते हैं और वे ही रूपये मानव-संहार के लिए लगाये जाते हैं।
ब्रह्माजी ने कहा थाः "हे अमृतपुत्रों ! तुम्हें अगर सुखी जीवन जीना है तो यज्ञार्थ जीवन जियो।" इस प्रकार ब्रह्माजी ने यज्ञ करने के लिए उपदेश एवं सामग्री दी।
संसार में जो कुछ सामग्रियाँ हैं उसका उपयोग यज्ञबुद्धि से करो। वातावरण में प्रदूषण कम हो इस विषय में विचारना और कुछ न कुछ सहयोग देना यह भी यज्ञ है। हमारे इर्दगिर्द कम से कम गन्दगी हो, हमारी ओर से पड़ोसी को कोई तकलीफ न हो इसका ख्याल रखना भी यज्ञ है।
ऐसा नहीं कि किसी का दिल न दुःखे इसके लिए धर्म विरूद्ध कर्म भी करने लग जाना। नहीं। कोई धर्म विरूद्ध बात कहे तो युक्ति से उसे सन्मार्ग पर लाना चाहिए, उसके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए।
रामजी बड़ी कुशलता से व्यवहार करते थे। कोई उनके समक्ष किसी विषय में बात करे तो वे तब क सुनते जब तक वह धर्म विरूद्ध नहीं होती, किसी की हानि विषयक नहीं होती। अगर उसकी बात अयोग्य होती, अनिष्टकारक होती, धर्म से विरूद्ध होती तो रामजी उसको आधे में टोककर, अपमानित करके नहीं रोकते थे वरन् कुछ नया विषय छेड़कर, इतिहास या धर्म की बात बताकर उसकी वृत्ति को मोड़ देते थे। उसे अच्छी बात, सही बात, नीति और धर्मयुक्त बात बताते ताकि वह अपनी गलती अपने आप समझ लेता और सुधार लेता।
आँख को बुरी जगह न देना यह भी यज्ञ है। ईश्वर-कार्य करने के लिए अपने शरीर को तन्दुरूस्त रखना यह भी यज्ञ है। तन, मन, बुद्धि को निर्विकारी जीवन के मार्ग में लगाना यह भी यज्ञ है। जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं वैसे यज्ञबुद्धि से अपने बाल-बच्चों की, कुटुम्बियों की, सम्बन्धियों की, पड़ोसियों की रक्षा करना भी यज्ञ है।
हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता ही है, हमारे सम्पर्क में आने वाले लोगों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष परिणाम आता ही है। गन्दगी करता है, बुरे विचार करते हैं तो वातावरण कलुषित होता है, गन्दे परमाणु फैलते हैं। अगर धूप करते हैं, प्राणायाम करते और ध्यान करते हैं तो वातावरण में शुद्धि और पवित्रता फैलती है।
आचार्य विनोबा के पास एक आदमी आया और बोलाः "बाबाजी ! मैंने शौक से घोड़ा लिया, बड़ा महँगा है। लेकिन मैं उसके करीब जाता हूँ तो वह उछल कूद करता है। मुझे अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। मेरा नौकर उस पर सवार होकर मजे से घूमता है, घोड़ा कोई हरकत नहीं करता। मैं उसके पास जाता हूँ तो भड़कता है। ऐसा क्यों ?"
विनोबाजी बोलेः "तुमने घोड़े को कभी खिलाया पिलाया ?"
"नहीं। वह तो मेरा नौकर ही करता है।"
"नौकर खिलाता-पिलाता है तो नौकर को बैठने देगा। तुम खिलाओ-पिलाओ तो तुमको बैठने देगा। अब आठ दिन तक तुम उसे दाना-पानी दो, प्यार करो, उसकी पीठ सहलाओ। फिर देखो, क्या होता है।"
आठ दिन तो क्या, चार ही दिन में वह अपने घोड़े पर बैठकर बाबाजी के दर्शन करने पहुँच गया।
प्रकृति की गहराई में स्नेह और उदारता है। तुम अगर संकीर्णता और अहंकार रखते हो तो घोड़ा भी पास नहीं आने देगा। स्नेह और उदारता से उसकी सेवा करो तो वह भी स्नेह से अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हारी सेवा करता है। गाय-भैंस को डण्डे के बल से दुहते हैं और अच्छी तरह चारा पानी खिला-पिला कर स्नेह से सहलाते हुए दुहते हैं तो दूध की गुणवत्ता और प्रमाण में फर्क पड़ेगा।
सहज
मिले सो दूध
बराबर माँग
लिया सो पानी।
नोंच
लिया सो रक्त
बराबर बोले
कबीरा बानी।।
जो आदमी यज्ञार्थ कर्म नहीं करता वह जन्मान्तर में वृक्ष आदि बन जाता है। उससे प्रकृति जबरन यज्ञकर्म करवाती है। वृक्ष के फल, फूल पत्ते, टहनियाँ, जड़-मूल सब कुछ दूसरों के लिए काम में आता है। वृक्ष स्वयं धूप सहता है, बारिश आँधी तूफान सहता है और आखिर में ठनठनपाल रह जाता है। उसे जब मनुष्य जन्म मिला था तब स्वार्थ से जिया था। अब प्रकृति जबरन उससे सेवा करवाती है, कठोरता से काम लेती है।
मनुष्य योनि में प्रकृति अपना कठोरतापन हटा लेती है, मनुष्य को संकल्प-स्वातन्त्र्य प्रदान करती है। तीन से पाँच वर्ष की उम्र तक बालक होता है तब तक उस पर प्रकृति का पूरा प्रभाव होता है। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है त्यों-त्यों प्रकृति अपना प्रभाव हटाती जाती है, कर्त्ता को संकल्प-स्वातन्त्र्य मिलता जाता है। इसीलिए कर्त्ता पर कर्म का फल लागू हो जाता है।
सिंह अगर गाय को मार देता है, खा जाता है तो उसको पाप नहीं लगता। बिल्ली चूहे को पकड़कर नोच डालती है तो उसे पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य अगर अण्डा खाता है, बकरी काटकर खाता है तो पाप लगता है। पशु-पक्षी तो प्रकृति से प्रेरित होकर पुराने कर्म करते हैं। मनुष्य संकल्प स्वातन्त्र्य का उपयोग करके नये कर्म बनाता है। संकल्प करने में वह स्वतन्त्र है लेकिन इस स्वातन्त्र्य का उपयोग करके कर्म करता है फिर उस कर्म का फल भोगने में वह स्वतंत्र नहीं है, उसे अपना कर्मफल मजबूर होकर भोगना ही पड़ता है।
मनुष्य जो कर्म करता है उसके प्रेरक-बल के रूप में उसकी इच्छाएँ, वासनाएँ होती हैं। उसके रक्त में माता-पिता के, दादा-दादी के, नाना-नानी के संस्कारों का प्रभाव होता है। मनुष्य जन्म में उसे अगर सीख मिल जाय, कर्म-बन्धन काटने का मार्ग मिल जाय, अपने पुराने संस्कार हटाता जाय, हल्के स्वभाव को छोड़ता जाय, उचित स्वभाव बनाता जाय, यज्ञार्थ कर्म करता जाये, सेवा से अन्तःकरण पावन बनाता जाय तो उसके कर्म निष्कर्म-सिद्धि में पहुँच जायेंगे। निष्कर्म सिद्धि होते ही वह अपने शुद्ध स्वरूप में, आत्म-स्वरूप में टिकने लग जाएगा। अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप में टिक जाना ही जीवन का आखिरी लक्ष्य है।
व्यापारी दुकान पर जाता है। सुबह दुकान का दरवाजा खोलने से लेकर रात को बन्द करने तक वह कभी हँसता है, कभी नौकर को डाँटता है, कभी ग्राहकों की खुशामद करता है, कभी बाजार के चढ़ाव-उतार का सावधानी से चिन्तन करता है। ये सारी चेष्टाएँ उसकी पैसा कमाने की हैं। रात होते ही उसकी नज़र गल्ले पर जाती है कि कितना धन्धा हुआ, कितना पैसा आया। बिक्री का हिसाब लगाता है।
जैसे लोभी का मन काम करने के बाद अपने मुनाफे पर जाता है ऐसे ही सच्चे साधक का मन यज्ञार्थ कर्म करने के बाद भीतर गोता मारता है, जाँच करता है कि भीतर निर्मलता बढ़ी कि नहीं, आनन्द या कि नहीं, शांति मिली कि नहीं, अन्तर्यामी सन्तुष्ट हुए कि नहीं। जो भी यज्ञार्थ कर्म होंगे वे आन्तरिक सुख, आन्तरिक शांति, आन्तरिक ओज और विश्रान्ति प्रदान करेंगे।
लोग ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं क्योंकि जीवन में यज्ञार्थ कर्म नहीं है। ध्यान करने बैठते हैं तो एक वासना इधर खींचती है, दूसरी वासना उधर खींचती है अथवा मनोराज चलता है, क्योंकि कर्त्ता ने जगत में सत्यबुद्धि कर दी है और परमसत्यस्वरूप परमात्मा से दूर हो गया है। स्वार्थ ने कर्त्ता की परिच्छिन्नता को इतना मजबूत कर दिया कि अपने असीम स्वभाव का पता नहीं चलता। कर्त्ता स्वार्थ बुद्धि से अन्तःकरण में, इन्द्रियों में, कर्म में उतरता है तो परिच्छिन्न हो जाता है। निःस्वार्थ भावना से आता है तो अपने मूल शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लगता है।
यज्ञार्थ कर्म करने से कर्त्ता के चित्त में शांति आती है, कर्त्ता के चित्त में योग्यताएँ पनप उठती हैं, कर्त्ता के चित्त में अपने मूल स्वभाव को जानने की क्षमता आती है। इस लाभ के आगे ऐहिक लाभ कुछ नहीं है।
लोग बोलते हैं- "बाबाजी ! निःस्वार्थ भावना से कर्म करेंगे तो ये वस्तुएँ, ये पदार्थ, ये व्यक्ति मिलेंगे नहीं। वस्तु-पदार्थ-व्यक्तियों के बिना जियेंगे कैसे ? मर जायेंगे...."
....तो क्या इन सबके होने से आप सदा के लिए जीते रहेंगे ? इनके होते हुए भी आप मर जाएंगे। वास्तव में देखा जाये तो वस्तुओं के बिना आप जी नहीं सकते ऐसा नहीं है अपितु अपने मूल स्वभाव में, आत्म-स्वरूप में गये बिना जी नहीं सकते। लोग समझते हैं कि संसार को रखे बिना हम जी नहीं सकते। वास्तव में संसार को भूले बिना संसार की चीजों को त्यागे बिना हम जी नहीं सकते।
'हे रूपया ! तेरे बिना नहीं चलेगा।'
अरे भाई ! रात को तिजोरी छोड़े बिना नींद नहीं आयेगी। नींद में सब पदार्थों से मुख मोड़कर अपने मूल शान्त स्वरूप में, आत्म-स्वरूप में जाने या अनजाने आना ही पड़ता है। अगर नहीं आ सकते तो जीना दुष्कर हो जाता है। आने के लिए नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, कई प्रकार के इलाज करवाने पड़ते हैं।
शरीर थककर बिस्तर पर लेटा है। आप बाहर के सब स्वार्थों से, आकर्षणों से मुक्त होकर नींद में चले जाते हो तो आपके तन की थकान दूर जो जाती है। स्वार्थ छोड़कर अगर यज्ञार्थ कर्म किया तो आप परमात्मा में चले जाओगे, आपका जन्म-मरण का दारूण चक्र मिट जायेगा। बाह्य आकर्षण छोड़कर शान्त स्वरूप में जग जाएँगे।
हमारे तीन शरीर होते हैं- पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। ये शरीर हम नहीं हैं। शरीर हमारे साधन हैं। वस्तुओं में और साधनों में जितना अहं और मम होता है उतना ही कर्त्ता बेचारा डरता रहता है और जन्म मरण का भागी होता है।
कर्त्ता तीन चीजों से बँधता हैः वस्तु, व्यक्ति और साधन। 'मेरा मकान..... मेरी गाड़ी.....' यह वस्तु है। मेरी पत्नी.... मेरा पति.... मेरा बेटा..... यह व्यक्ति है। स्थूल-सूक्ष्म कारण शरीर- ये साधन हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से साधनों का सदुपयोग होगा और साध्य में पहुँचायेगा। यज्ञार्थ कर्म न करने से, साधनों को मैं मानने से आपत्ति बढ़ती रहेगी।
परमात्मा के स्वभाव में स्नेह और उदारता है। अपना स्वभाव भी वैसा बनाते जाएँगे तो परमात्मा में मिलते जाएँगे। यही जीवन की इतिकर्त्तव्यता है। मनुष्य जन्म मिला है और वह भी भारत में ! देवता लोग भी भारत में जन्म लेने को तरसते हैं, भारत-भूमि की प्रशंसा करते हैं। देवता लोग अपने संकल्प के मुताबिक गमनागमन कर सकते हैं क्योंकि वे पुण्य योनि में हैं। स्वर्ग में प्रचुर मात्रा के भोग हैं। वहाँ भोग में कोई विघ्न नहीं आता और फलतः भोगों में उपरामता भी नहीं आती जल्दी से। भोग का आकर्षण नहीं मिटने के कारण समय उनका खराब हो जाता है।
मनुष्य जन्म में भोग इतने मिलते नहीं, कुछ कुछ मिलते हैं तो उसमें विघ्न भी आते हैं। भोगों से उपरामता और वैराग्य आने का मौका है। यज्ञार्थ कर्म करने की यहाँ सुविधा है। इसलिए मनुष्य अगर चाहे तो वह परमात्म-प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। चाहे वह पापी में पापी हो, दुराचारी में दुराचारी हो वह भी अपना कल्याण कर सकता है।
अपि
चेदसि पापेभ्यः
सर्वेभ्यः
पापकृत्तमः।
सर्व
ज्ञानप्लवेनैव
वृजिनं
संतरिष्यसि।।
'यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्र से भली भाँति तर जायेगा।'
(भगवद् गीताः 4.36)
जीव ज्ञान की नाव में बैठ जाये तो आसानी से वह पार हो सकता है। हाँ तत्परता अपनी हो। जो भी कर्म करे उसके मूल में देखे, निगरानी रखे सूक्ष्मता से।
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं- "जो यज्ञार्थ कर्म करता है वह इधर-उधर भटकना पसन्द नहीं करता । वह बाहर के तीर्थों में दूर-दूर जाकर, श्रम उठाकर अपने को त्रस्त नहीं करता। कठिन तप करके अपने शरीर को तपाता नहीं, सुखाता नहीं। शरीर को भी यज्ञार्थ संभालता है। नंगे पैर यात्रा नहीं करता और प्रमादी होकर विलास भी नहीं करता। अति आहार और अति भूखापन से बचता है। अति भोग और अति त्याग से बचकर मध्यम मार्ग से चलकर यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्त रहता है।
अत्यंत बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए जो विधान है वह साधक के लिए नहीं है। जो साधक के लिए विधान है वह सिद्ध के लिए नहीं है। जो कर्म इस समय उचित है वह आगे चलकर दसरे संदर्भ में अनुचित भी बन सकता है। 10वीं कक्षा वाला विद्यार्थी चौथी कक्षा की किताब का अभ्यास करे तो यह उसके लिए अनुचित है।
ऐसे ही मनुष्य जन्म पाकर विषयों में ही उलझे रहना अनुचित है। मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति पाने के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं-
यह
तन कर फल विषय
न भाई।
मानव तन पाकर विषय भोगना उचित नहीं है। विषय भोग भोगना है तो पशुयोनि में खूब मजे से भोगा जा सकता है। पशुओं को कोई बाधा नहीं। हम असंयमी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर दें तो हम पशुता की ओर गये। अतः जीवन-सरिता को संयम के दो किनारों के बीच में बहाते हुए यज्ञार्थ कर्म करने चाहिए। भोजन करें तो भी यज्ञार्थ, पानी पियें तो भी यज्ञार्थ। हमारे पेट में जठराग्नि यानि भगवान अग्निदेव विराजमान हैं उनको आहुति देना है।
'मैं खा रहा हूँ... मजा ले रहा हूँ...'
नहीं....। मैं वैश्वानर को भोजन करा रहा हूँ। अपने बच्चे को भोजन कराते समय बच्चे में स्थित आदि नारायण को भोजन कराने की भावना करो। इससे भोजन कराना भी यज्ञ हो जाएगा।
बंगाल में एक स्त्री की शादी होते ही उसी वर्ष में उसका पति मर गया। एकाएक पति की मृत्यु होने से वह विधवा महिला विह्वल हो गई, बावरी सी बन गई। किसी सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि पति की याद में कहीं पागल न हो जाय यह लड़की ! उसके घरवालों को समझाया कि, 'फलानी जगह पर संत-महात्मा रहते हैं उनके पास ले जाओ इस बच्ची को। उनके दर्शन कराओ, सत्संग में बैठाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।'
वह विधवा युवती, सोलह वर्ष की बच्ची संत-दर्शन को गई। पति के वियोग में विह्वल। सौभाग्य-चिह्न बिन्दी विहीन ललाट, चूड़ियाँ विहीन हाथ, तन पर विधवा के धवल वस्त्र। आँखों में आँसू बहाती संत श्री के चरणों में पहुँची। बाबाजी ने आत्मिक प्यार भरे स्वर में पूछाः
"बेटा ! कैसे आयी ?"
वह रो पड़ी। सिसकते हुए बोलीः "दुनिया में मेरा कोई नहीं..... मैं क्या करूँ ?"
बाबाजी ने कहाः "अरे बेटी ! तू आज जितना झूठ बोल रही है उतना कभी नहीं बोली। तुझे इतना पता नहीं कि संत महात्मा के आगे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ?"
वह युवती चौंक उठी एकदम। बाबाजी को यकीन दिलाते हुए कहने लगीः "बाबाजी ! मैं सच बोलती हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मेरी बुढ़िया माँ थी उसने कन्यादान कर दिया और कुछ महीनों में वह प्रभु धाम में चली गई। फिर उसका जमाई भी चल बसा। मैं अकेली रह गई। मेरा कोई न रहा।"
"तू झूठ बोल रही है। तेरा कोई नहीं ? अरे ! तेरे हृदय में परमात्मा बैठा है वह तेरा है। हृदय की धड़कनें चला रहा है, तेरे तन में रक्त बहा रहा है, श्वास चला रहा है, आँखों को देखने की शक्ति दे रहा है, कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है वह सर्वान्तर्यामी परमात्मा तेरा है, तेरे साथ है, तेरे भीतर है और तू बोलती है मेरा कोई नहीं ? पगली ! वह तेरे और सबके हृदय में बैठा हुआ सृष्टिकर्त्ता कभी मरता नहीं। शरीर मरता है तब भी सूक्ष्म शरीर में अन्तर्यामी रहता है, प्रेरणा देता है, आगे की यात्रा करवाता है। सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है तब वह सर्वव्यापक ब्रह्म हो जाता है, विश्व चैतन्य हो जाता है।
ऐसे परब्रह्म परमात्मा जैसे सबके हैं वैसे तेरे भी हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके तो वे पूरे के पूरे हैं। ....और तू रोती है। धैर्य रख बेटी ! करूणामूर्ति महात्मा ने बच्ची को आश्वासन दिया।
लौकिक दृष्टि से कोई अनाथ सोचे कि दुनियाँ में मेरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा ही मेरा है, तो उसकी सारी की सारी वृत्तियाँ एक ही जगह पर लग जाती हैं, केन्द्रित हो जाती हैं। उसका मन परमात्मा में लगने लगता है।
कोई मशीन चलानी हो तो उसके छोटे-मोटे सब पुर्जे एकत्रित होने चाहिए, मशीन से संलग्न होने चाहिए। तभी मशीन चल सकती है।
अपनी जीवनरूपी मशीन तो ऐसी है कि उसकी वृत्तियाँरूपी पुर्जे जगह-जगह पर बिखरे पड़े हैं। ऐसी दशा में ईश्वर के मार्ग पर अपनी जीवन-गाड़ी दौड़ेगी कैसे ? अपना एक पुर्जा ऑफिस में पड़ा है, एक पुर्जा बाजार में भटक रहा है, एक पुर्जा परिवार की ममता में उलझा है, एक पुर्जा किसी ने अपमान कर दिया उसके पीछे लगा है, एक पुर्जा किसी ने मान दिया उसको भोगने में लगा है, एक पुर्जा मतमतांतर में गोते खा रहा है, एक पुर्जा भविष्य के सुख की तलाश में गया है। अपनी हृदयरूपी मशीन ऐसी बिखरी हुई पड़ी है। जो महसूस करता है कि, 'मेरा कोई नहीं है' –तो उसका बिखराव हट गया। अब वह लगेगा तो पूरा लगेगा। पूरा लगेगा तो परमात्मा भी पूरे के पूरे उसी के ही हैं।
बाबाजी ने उस बच्ची से कहाः "जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान होता है। और तेरा तो वह पूरे का पूरा है। उस भगवान को तू पिता मान, पति मान, पुत्र मान, भाई मान, जो तेरी भावना हो, मान। वह सब कुछ होने को तैयार है।"
बाबाजी ने युवती को लाला कन्हैया का विग्रह स्वरूप दे दिया, एक प्यारी मूर्ति दे दी। लड़की खुश हो गयी। "मैं कन्हैया को पुत्र मानकर उसकी सेवा करूँगी। वह कन्हैया को ले गयी अपने घर। रोज सुबह जल्दी उठे, कन्हैया को स्नेह से उठाये। स्वयं स्नान करके अपने लाला को नहलाये। फिर भोजन की थाली परोसकर उसके सामने रख दे। आँख बन्द करके भावना करे कि मेरा लाला खा रहा है, भोजन कर रहा है। फिर उसके हाथ-मुँह धुलाये। इस प्रकार मानसपूजा से समन्वित वह युवती अपने लाला का लालन पालन करने लगी।
ऐसा करते करते तीस साल बीत गये। सत्रह साल की बच्ची अब सैंतालीस की प्रौढ़ा हो गयी। उस समय रामकृष्ण परमहंस की ख्याती लोगों तक पहुँचने लगी थी। इस महिला के मन में हुआ कि, चलो, बाबाजी के दर्शन करने जाऊँ।......लेकिन मेरे लाला का क्या होगा ? उसको भूख लगेगी तो ? मेरे लाला के लिये क्या करूँ ?
उसने दाल-चावल की पोटली बाँधकर साथ में ले ली और लाला के साथ चल पड़ी रामकृष्णदेव के दर्शन करने। दक्षिणेश्वर में तो कई लोग बाबाजी के दर्शनार्थ आते थे, बैठते थे। बड़े-बड़े लोगों के बीच बाबाजी की बातचीत होती थी। वह बेचारी अनपढ़ माई बैठी थी एक कोने में।
आखिर दोपहर हुई। वह थकी। सोचने लगीः
"मेरे लाला को भूख लगी होगी। यहाँ तो खिचड़ी पकाने की सुविधा नजर नहीं आती है। मेरा लाला कैसे खायेगा ? घर जाऊँ और वहीं लाला को भोग लगाऊँ।"
वह उठकर चुपके से जाने लगी तो रामकृष्ण भी अचानक उठे और उसके पीछे भागे। बोलेः "माँ....माँ.... मुझे भूख लगी है। खाना खिलाओ।" महिला को समझाकर वापस बुला लाये। अपने चौके में रसोई पकाने की सुविधा कर दी। बुढिया ने खिचड़ी बनाई, पत्तल में परोसी। उसे संकोच हो रहा था कि बाबाजी को खिचड़ी कैसे खिलाऊँ ! इतने बड़े महात्मा पुरूष ! मेरी खिचड़ी खाएँगे !
इतने में ही रामकृष्ण स्वयं आये और खाने बैठ गये। माई का हृदय भाव से भर आया। स्नेहपूर्ण दिल से पत्तल परोस दी। रामकृष्ण मजे से खा रहे हैं। वह बुढ़िया समझ रही है कि मेरे लाला को भूख लगी है और वह नटखट नागर अठखेलियाँ करता हुआ खिचड़ी खा रहा है। ऐसी भावना करके वह रामकृष्णदेव को निहारती तो उसमें उसको लाला के दर्शन होने लगे। साक्षात श्री कृष्ण का बाल स्वरूप देखने लगी। भाव विभोर होकर अपने प्यारे लाला को छूने लगी तो लाला गायब ! सामने रामकृष्ण भोजन कर रहे हैं।
उस दिन से वह बुढ़िया कुछ अलौकिक भाव में ही रहने लगी। आनन्द से गुनगुनाती रहती, लाला से बात किया करती। कभी लाला को डाँटतीः "नटखट ! किसी का मक्खन चुरा के लाया है..... इत्र की बोतल उठा लाया है....
लोग उसे पागल समझते। कुछ भाग्यशाली लोग समझते कि इसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। वह जब लाला से बात करती तो लोग पूछतेः "कहाँ है लाला ?"
"यहीं तो खड़ा है, देखते नहीं ?"
"नहीं माता जी ! लाला सिर्फ तुम्हें ही दर्शन दे रहे हैं। उनसे प्रार्थना करो न कि हमको भी दर्शन देवे।"
माई ने लाला को कहा तो लाला ने मना कर दिया। लोगों ने अनुनय विनय किया तो बुढ़िया लाला से आग्रह करने लगी। लाला ने दर्शन तो न दिये लेकिन इत्र की एक बोतल दी। बुढ़िया ने अपने प्यारे लाला को डाँटाः
"तू कहाँ से रोज-रोज इत्र चुरा लाता है ? कौन देता है तेरे को ?"
लाला ने अन्य लोगों को दर्शन देने से तो इन्कार कर दिया लेकिन बुढ़िया कोई निराली दुनियाँ में पहुँच चुकी है इस समाचार से उन्हें वाकिफ करने के लिए इत्र की शीशी फोड़ दी। फर्श पर आवाज आयी। काँच के टुकड़े भी लोगों ने देखे। इत्र की सुगन्ध सर्वत्र फैल गयी। तबसे लोग जानने लगे कि यह पागल-सी दिखती महिला वास्तव में पागल नहीं है। इसने तो गल को पा लिया है। अपनी वृत्तियाँ प्रभु में एकाकार कर ली हैं।
मनुष्य के मन में अदभुत शक्ति है। आपका मन चाहे लाला में लगा दो चाहे योगाभ्यास में लगा दो चाहे यज्ञार्थ कर्म में लगा दो चाहे निज आत्मस्वरूप के अनुसन्धान में लगा दो। मन एकाग्र होते ही शुद्ध होने लगेगा, दिव्य होने लगेगा, शान्त होने लगेगा, आत्मविश्रान्ति पाने लगेगा।
आप जो भी कार्य करो यज्ञार्थ भावना से करो, ईश्वर से नाता जोड़ने के लिए करो, दूसरों का कल्याण करने की भावना से करो, अपनी वासनाएँ निवृत्त करके जीवन को निर्मल बनाने के हेतु से करो। जो कर्म भोगबुद्धि से, स्वार्थबुद्धि से, राग-द्वेष से प्रेरित होकर, ईर्ष्या के कारण से, दूसरों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किये जाते हैं वे कर्म कर्त्ता को बाँधने वाले हैं। दूसरों को सताकर ऐश-आराम पाने के लिए जो कर्म किये जाते हैं वे जीव को निम्न गति में ले जाते हैं। 'सबमें मेरा ही नारायण स्वरूप विलास कर रहा है'- ऐसी मंगल भावना से व्यवहार होता है वह परम मांगल्य के द्वार खोल देता है।
परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान की महिमा का कोई पार नहीं।
भगवन्नाम स्मरण करें, जप करें, तो भगवान को प्यार करने के लिए करें, भक्ति का दिखावा करने के लिए नहीं। जीव का अहंकार मिटाने के लिए जपयज्ञ करना है, व्यक्तित्व का सर्जन करने के लिये नहीं।
भक्त समझता है कि अपने जीवन में जो सत्कर्म है वह भगवान का कृपा-प्रसाद है और जो दोष हैं वे अपने हैं। जिनका योग में प्रेम होता है उसका अहंकार परमात्मा में विलय होता है। जिसका योग में प्रेम में नहीं होता उसका संस्कारों में प्रेम होता है। जो संस्कारों के अनुरूप कर्म करता है वह कर्मों में बँध जाता है। यज्ञ के अनुरूप जो कर्म करता है वह मुक्ततता का अनुभव करता है। कुछ माँ-बाप के संस्कार, कुछ दादा-दादी के संस्कार, कुछ नाना-नानी के संस्कार और कुछ अपने पूर्व जन्म के संस्कार के मुताबिक जीव अपनी वासनापूर्ति के लिए कर्म करता रहता है तो अपना कर्म-बन्धन बढ़ाता रहता है। यदि वह सजग होकर यज्ञार्थ कर्म करता जाय, अपने तन-मन बुद्धि पर लदी हुई संस्कारों की जाल को काटता जाय तो फिर वे घड़ियाँ दूर नहीं कि वह दिल में आराम पाकर दिलबर का साक्षात्कार कर ले।
यज्ञार्थ कर्म करने वाला महा धनवान होता है, अलौकिक आध्यात्मिक धन से वह धनी होता। उसके चित्त की धारा अवर्णनीय शान्ति को, निर्विषय निर्मल आनन्द को पाती है। यज्ञार्थ जीवन जीने वाला जीवनदाता को पा लेता है।
साधक वही है जो निरन्तर सावधान रहे। वह अपने जीवन पर निगरानी रखता है कि, 'मेरा कर्म कामार्थ तो नहीं हो रहा है ? अहंकारार्थ तो नहीं हो रहा है ?' ऐसी सावधानी रखनेवाला व्यक्ति ही साधक कहा जाता है। ऐसा साधक अपने साध्य को पा लेता है।
जो कर्म का कर्त्ता है वही कर्मफल को भोक्ता है। जो यज्ञार्थ कर्म करता है वह धीरे-धीरे कर्त्ताभाव से पार हो जाता है। कर्त्तापन-भोक्तापन से पार होने वाला परमात्म-पद में स्थित होने लगता है। पाप-पुण्य कर्त्ता को लगते हैं। सुख-दुःख भोक्ता को लगते हैं। कर्त्ता अपने को व्यक्ति मानता है तो पाप-पुण्य लगता है। कर्त्ता अपने को व्यक्ति माने, जहाँ से कर्त्ता को सत्ता मिल रही है उस अपने मूल स्रोत का ख्याल रखे, अपने आत्म-स्वरूप में गोता लगाता रहे तो पाप-पुण्य से रहित हो जाता है। जो पाप, पुण्य से रहित है वह सुख-दुःख के भोग से भी रहित हो जाता है। वह परम पद में स्थित हो जाता है।
निकम्मा आदमी तो मुर्दा है। अशुद्ध कर्म करने वाला आदमी पापी है। वासना-पूर्ति के लिए कर्म करने वाला भोगी है। परमात्मा को स्नेह करते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाले योगी है।
कर्त्ता में अगर ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे आत्मबोध होगा। कर्त्ता में अगर भक्ति के संस्कार है भगवदभाव, भगवत्प्रेम प्रकट होगा। वह भगवान के संतोष के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा और भगवान की कृपा-प्रसाद पा लेगा। कर्त्ता में वेदान्त के संस्कार होंगे तो कर्मबन्धन काटकर अपने निज स्वरूप में जग जाता है।
पाप कर्म छुपकर करें तो भी वह फल देता ही है तो प्रभु-प्रीत्यर्थ निष्काम कर्म करें तो वह क्यों फल नहीं देगा ? वह कर्म ऐसा फल देगा कि वह फल की गिनती में नहीं आता। ऐसा परम फल देगा वह कर्म।
जितना-जितना निष्काम कर्म होता है उतना परमात्म-आनन्द प्रकट होता है, स्नेह का स्वभाव छलकता है। परमात्मा का स्वभाव है स्नेह और उदारता। जो यज्ञार्थ कर्म करता है वह अपने इस परमात्म-स्वभाव को जगा लेता है।
ध्यान करने बैठो तो प्रारम्भ में थोड़े प्राणायाम कर लो। श्वास छोड़ते समय भावना करो कि, "मैं श्वास के साथ काम-क्रोध और राग-द्वेष को अलविदा दे रहा हूँ।" श्वास भीतर भरते समय भावना करो कि "अब मैं यज्ञार्थ कर्मों से जीवन को निर्मल बना रहा हूँ।"
प्रकृति में जो कार्य हो रहा है, यज्ञार्थ हो रहा है। ज्ञानवालों के जीवन में जो कार्य हो रहा है वह यज्ञार्थ हो रहा है। अपने में भी यज्ञार्थ जीवन जीने की क्षमताएँ बढ़ाते जाओ।
जो कर्म महान् दृष्टि से अनुशासित होते हैं वे कर्त्ता को बन्धन-मुक्त करते हैं। यह अनुशासन सदगुरू का हो सकता है, आत्मवेत्ता संतों का होता है या पवित्र शास्त्रों का होता है। साधक को अपने कर्मों पर निगरानी रखनी चाहिए कि वे गुरू या शास्त्रों को अनुशासन में हो रहे हैं कि अपनी वासना से प्रेरित होकर ही रहे हैं। क्षुद्र दृष्टि से किये जाने वाले कर्म कर्त्ता को बाँधते हैं। कर्म में जितनी उदार दृष्टि होती है उतना ही वे कर्म कर्त्ता को कृर्त्तृत्व अभिमान से हटाकर परब्रह्म परमात्मा में टिकने का अधिकारी बनाते हैं।
जाँच करोः आपके कर्मों में सच्चे अनुशासक की दृष्टि है ? .....कि कच्चे मन की मान्यताएँ हैं ? अगर कच्चे मन की मान्यताओं के मुताबिक कर्म हो रहे हैं तो वे कर्म आगे चलकर बन्धन रूप बनेंगे और अशान्ति पैदा करेंगे। अगर उदार शास्त्रदृष्टि के अनुसार कर्म हो रहे हैं तो वे कर्म बन्धन की बेड़ियाँ काटकर तुम्हें निर्दोष नारायण के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगे।
एक होती है शाश्वत दृष्टि और दूसरी होती है क्षुद्र दृष्टि यानी संकीर्ण दृष्टि, तुच्छ भोग की दृष्टि। शाश्वत दृष्टि यानी शाश्वत परमात्मा में टिकने वाली दृष्टि। असीम श्रीहरि को साक्षी रखकर जो कर्म होते हैं वे महान दृष्टि के अनुशासन में कर्म होते हैं। वे कर्म हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं।
आपका श्वासोच्छ्वास उस पूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ा है। आप जिस धरती पर खड़े हैं उस व्यापक धरती से जुड़े हैं, व्यापक आकाश से जुड़े हैं। ऐसे ही आप जो कर्म करें वह व्यापक विश्वात्मा के अनुशासन के मुताबिक यज्ञार्थ करें तो आप कर्त्तापन और भोक्तापन के भाव से पार होकर निर्दोष नारायण स्वभाव में जुड़ जायेंगे, ब्रह्म स्वभाव में जग जायेंगे।
अपने नारायण स्वभाव को प्यार करते जाओ... उसे प्रार्थना करते जाओ, रिझाते जाओः "हे देव ! अब हमारा देखना यज्ञार्थ हो जाये, हमारा भोजन करना, सोना यज्ञार्थ हो जाये। हे प्रभु हम तेरी विरह में रोयें.... तेरे प्यार में हँसें। तुझे पाने के लिए अपने तन को तन्दुरूस्त रखें। भोग भोगने के लिए नहीं, बड़ा कहलाने के लिए नहीं लेकिन बड़पप्न मिटाकर वास्तव में जो बड़ा है उस उदार स्वभाव को जगाने के लिए जियें। हे विश्वेश्वर ! हे देवेश्वर ! हे सर्वेश्वर ! हम जो भी करें, तुझे रिझाने के लिए करें।
जब-जब कार्य करो, उत्साह से करो, यज्ञार्थ करो। उन कार्यों से बहुजन हिताय.... बहुजन सुखाय भावना की सुगन्ध आये। बहुजनों में बैठा हुआ वह एक, बहुरूपों में बैठा हुआ वह अरूपी सन्तुष्ट हो और तुम्हारे दिल में प्रकट हो जाय, बस इसीलिए कर्म करो।
तुम इसे प्यार करो जो सचमुच प्यारा है। वह प्यारा तुम्हारे हृदय में प्रकट होने का इन्तजार कर रहा है। अगर वह इन्तजार न करता तो तुम्हें सत्संग में जाने के लिए प्रेरित भी नहीं करता... सत्साहित्य पढ़ने के लिए उत्सुक भी नहीं करता।
अभागा आदमी सत्संग में नहीं जा सकता।
आपका अन्तःकरण जिस देव के आधार पर है वह देव ब्राह्माण्डों में व्याप्त है। उस देवेश्वर को पाने के लिए, उस सर्वेश्वर को रिझाने के लिए, अपनी अखण्डता और व्यापकता जगाने के लिए, परिच्छिन्न आत्मदेव को रिझाने के लिए ही जीवन के सब क्रिया कलाप हों।
भगवान में जिसकी प्रीति है वह अहंकार को नहीं पोसता। ज्ञान में जिसकी प्रीति है वह प्रकृति के आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता।
हम उसे ही प्यार करेंगे जो सचमुच में प्यारा है। हम उसी में शान्ति पायेंगे जिससे योगेश्वरों को सत्ता मिलती है। उस सर्व सत्ताधीश को हम स्नेह करेंगे।
क्षुद्र दृष्टि को छोड़कर हम उदारत्मा गुरुदेव की अनुशासित दृष्टि से कर्म करेंगे। आलस्य और प्रमाद छोड़कर उत्साह से कार्य करेंगे।
जप करते समय, कीर्तन करते समय, ध्यान करते समय अपने दिल और दिमाग को दिव्य भावना से भर दो.... हृदय-मंदिर को इस आलोक से आलोकित कर दो कि हम अपने प्रियतम परमात्मा में पहुंच रहे हैं। .....हम अपने परिच्छिन्न अहंकार को मिटाये जा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं यज्ञार्थ ही कर रहे हैं....। हमारा रोम-रोम..... हमारी रग-रग पावन हो रही है परमात्म प्रेम से।
सत्संग की महिमा लाबयान है.... परमात्मा की महिमा लाबयान है। ऐसी लाबयान चीजों की सहज में प्राप्ति हो रही है। सत्संग में भगवन्नाम का स्मरण हो रहा है, जप हो रहा है, कीर्तन और ध्यान हो रहा है, हरिचर्चा हो रही है, आत्म-परमात्मदेव का अनुसन्धान हो रहा है, जन्म जन्मान्तर की थकान मिट रही है।
यज्ञार्थ कर्म कर्त्ता को परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। सत्संग में जिसकी प्रीति है, योग में जिसकी प्रीति है, ध्यान में जिसकी प्रीति है वह भोग के खड्डों से बच जाता है। जिसकी सत्संग में प्रीति नहीं, योग में प्रीति नहीं, ध्यान में प्रीति नहीं वह कुसंस्कारों का शिकार हो जाता है।
जीव का स्वभाव है नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, आनन्दस्वरूप सच्चिदानन्दघन। वह दिव्य स्वभाव अपना भूल गया है.... क्यों ? क्या विघ्न बीच में आ गया है ?
चाह
चमारी चूहड़ी
अति नीचन की
नीच।
तू
तो पूरन
ब्रह्म था जो
चाह न होती
बीच।।
सुख की चाह करके जीव क्षुद्र वस्तुओं के लिए, क्षुद्र भोगों के लिए प्रवृत्ति करता है। वह क्षुद्र अनुशासन के प्रेरित होकर कर्म करता है। विराट के अनुशासन में अपना जीवन ढाले तो विराट अनुशासन उसको अपने स्वभाव में जगाकर मुक्त कर देता है। अतः अपने जीवन को विराट परमात्मा से एक हो जाने की भावना से तरबतर बनाकर यज्ञार्थ कर्मों में बिताना चाहिए।
प्रवृत्ति तो करनी ही चाहिए। प्रवृत्ति के बिना कोई जीव रह ही नहीं सकता।
न हि
कश्चित्
क्षणमपि जातु
तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते
ह्यवशः कर्म
सर्वः
प्रकृतिजैर्गुणैः।।
'निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य-समुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।'
(भगवद गीताः 3.5)
शरीर से प्रवृत्ति कोई रोक दे तो भीतर ही भीतर मन मनोराज खड़ा कर देगा, विचारों की जंजीरें बनाना शुरू कर देगा। आलसी-प्रमादी होकर पड़ा रहना कोई निवृत्ति नहीं है। ऐसा मुर्दा जीवन भी कोई जीवन है ?
आलसी, प्रमादी, मुर्दा जीवन जीने से तो सकाम कर्म करना ठीक है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म उत्तम है। निष्काम कर्म करते-करते नैष्कर्म्यसिद्धि हो जाती है, कर्मों कि पूर्णाहुति हो जाती है, कर्त्ता अपने आत्म-स्वभाव में जग जाता है।
कोई चीज मिल जाना बड़े भाग्य की बात नहीं है। कोई चीज खो जाना दुर्भाग्य की बात नहीं है। चीज को खो जाने के कारण दुःखी हो जाना दुर्भाग्य की बात है। चीज मिल जाये उसमें आसक्त हो जाना दुर्भाग्य की बात है। चीज मिल जाय तब और खो जाय तब सम रहना यह बड़े भाग्य की बात है।
चीज मिल जाय उसका ठीक उपयोग करना, चीज खो जाय उसको खोजना लेकिन समता नहीं खोना। समता के सिंहासन पर डटे रहना यह परम सौभाग्य है।
समता उतनी मजबूत होती जाएगी जितना यज्ञार्थ कर्म में कर्त्ता आगे बढ़ता जायेगा। स्वार्थ-त्याग से जीवन जियेगा उतना ही जीवन उन्नत होता जायेगा। स्वार्थी आदमी भी खाता-पीता है चिन्ता के साथ। निःस्वार्थी अपने शरीर के सुख-चैन की परवाह नहीं करता। उसके लिए प्रकृति के विराट आयोजन में यथायोग्य व्यवस्था होती रहती है।
अपने देह की ममता छोड़ने के बराबर और कोई ऊँची अवस्था नहीं। देह में से 'अहं' और 'मम' उठ गया तो फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, स्थूल-सूक्ष्म-कारण ये तीनों शरीर विराट के साधन बन जायेंगे। तुम्हारे द्वारा विश्वनियन्ता काम करने लगेगा।
जैसे लावारिस माल सरकार का होता है। तुम्हारा स्वार्थ चला गया, देह में से अहंता-ममता चली गई तो अन्तःकरण हो गया परमात्मा का।
निःस्वार्थ कर्म करने से स्वार्थ विलीन हो जाता है। अन्तःकरण स्वच्छ हो जाता है, फिर परमात्मा उसके द्वारा काम करता है। परमात्मा की निगाह मात्र से हजारों आदमी आनन्दित होते हैं।
भूत और भविष्य की चिन्ता मत करो। बीत गया उसका शोक न करो। 'है' उसको हँसकर बिताओ। आयेगा उससे विमोहित मत हो।
माया में अदभुत शक्ति है। स्वार्थ ने तुमको संकीर्ण कर दिया। कामनाओं ने तुम्हें लूट लिया। चिंतित हो रहे हो कि मेरा क्या होगा ? अरे, माता के गर्भ में थे तब अपने रक्षण और पोषण की चिन्ता की थी ? उस विराट परमात्मा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की थी। बाहर आकर उस निर्दोष अवस्था में रहे नहीं स्वार्थ से प्रेरित होकर संकीर्ण हो गये। अब तुम फिर से यज्ञार्थ कर्म करते जाओ, निर्दोष निर्मल आत्म-स्वभाव में जगते जाओ। विराट अनुशासन तुम्हारे शरीर की सँभाल लेने के लिए प्रकृति को प्रेरित करता जायेगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
भगवन्नाम
की महिमा
रामायणकार कहते हैं-
नाम
अखिल अघ पुंज
नसावन.....।
भगवन्नाम का बड़ा भारी प्रभाव है। सारे पापों के समूह को नाश करने वाला है भगवान का नाम। भगवान का वाचिक नाम लेते-लेते मानसिक नाम में डूबते जायें तो सौ गुना अधिक लाभ करता है। नाम-जप के समय शरीर की रग-रग भगवान के प्यार में तल्लीन होती जाये, रोम-रोम में स्नेह से पुलकित होता जाय।
कहाँ
लगी कहुँ नाम
बड़ाई राम न
सके नाम गुण
गाई।
भगवान स्वयं भी नाम का पूरा बयान नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा का वर्णन, संत समागम का वर्णन और नाम-महिमा का वर्णन लाबयान है। जितना जिनको लाभ हुआ है उतना गाया है। पूरा बयान तो कोई नहीं कर पाये।
यह
राज समझ में
तो आता है
लेकिन समझाया
नहीं जाता।
वेदान्त श्रवण के लिए एकाग्रता करनी चाहिए। ध्यान से एकाग्रता आती है। नाम-जप से हृदय में निर्मलता आती है। मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और बुद्धि की मोक्षदायी तीव्र जिज्ञासा, आकांक्षा और ज्ञान के अनुकूल मनन को ही अभीष्ट माना गया है आध्यात्मिक साधना में।
आत्मज्ञान का श्रवण महापुण्यदायी है। आत्मज्ञान का श्रवण सब साधनों से उत्तम माना गया है। उस श्रवण के लिए मन की एकाग्रता, हृदय की पवित्रता और बुद्धि की जिज्ञासा, ये तीन साधन जब जुड़ते हैं तब थोड़े ही समय में साधक का परम कल्याण हो जाता है।
लेबोरेटरी में पदार्थों का विश्लेषण करना एक बात है, दुनियादारी का व्यवहार करना यह दूसरी बात है, रीत-रिवाज के मुताबिक धार्मिक क्रियाएँ करना यह तीसरी बात है और अपने दिल में ही दिलबर को निहार कर मोक्ष पा लेना, मुक्ति पा लेना सबसे अदभुत बात है।
देश की सेवा अच्छी है, समाज की सेवा अच्छी है लेकिन भगवद् –भक्ति तो कुछ निराली ही चीज है। जो भगवद्-भक्ति करता है उसके द्वारा वातावरण इतना मधुर और पवित्र हो जाता है कि लोगों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ऐसे पुरूष का नाम सुनकर भी लोगों के हृदय में सत्प्रेरणा और सदभाव पैदा हो लगता है। उनके सान्निध्य, दर्शन वाणी से तो प्रेरणा और सेवा होती ही रहती है। चाहे स्थूल दृष्टि से ऐसे महापुरूष कुछ भी करते हुए न दिखें फिर भी उनका अस्तित्व देश के लिए बड़ा हितावह होता है, मानव जात के लिए बड़ा कल्याणकारी होता है।
रामानंद स्वामी हरिनाम-स्मरण में तल्लीन रहते थे, रामरस में मस्त रहते थे। एकबार कोई सज्जन अपने बेटे को लेकर उनके दर्शनार्थ गये। देखा तो बाबाजी नहीं थे। जानकर बड़ा उदास हो गया। उसका लड़का बहुत बीमार था। काफी इलाज किये, लाभ नहीं हो रहा था। अब गुरू महाराज का ही सहारा था। शिष्य से पूछाः
"गुरू महाराज कहाँ पधारे हैं ?"
"महाराज किसी महापुरूष से मिलने गये हैं।"
"मेरे बच्चे की स्थिति बड़ी गम्भीर है। गुरू महाराज के आशीर्वाद लेने आया था। उनके सिवा मेरा और कोई नहीं। अब क्या किया जाय ?" वह गृहस्थ उदास हो गया। फिर शिष्य से विनती कीः
"अब आप ही कोई उपाय बताइये। आप गुरू महाराज की सेवा कर रहे हैं, सदा उनके पावन सान्निध्य का सेवन कर रहे हैं, निरन्तर दर्शन कर रहे हैं, ध्यान-भजन कर रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता सदगुरू की सेवा करने वाला भी पुण्यात्मा होता है। जो रामजी के परम भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, उन भक्त के भी जो भक्त हैं, दासों के भी जो दास हैं वे भी हमारे लिये वन्दनीय हैं, पूजनीय हैं। आप गुरू महाराज के नित्य चरणसेवी हैं। अब आप ही कोई उपाय बता दीजिये इस बच्चे के लिए। आप जो बोलेंगे वह आशीर्वाद हो जायेगा।"
शिष्य ने गुरू महाराज का स्मरण करके जो मन में आया वह बता दियाः "एक कागज पर तीन बार रामनाम लिखो और वह कागज पानी में घोंटकर बच्चे को पिला दो। रामजी की कृपा से ठीक हो जायेगा।"
सेठजी ने घर जाकर ऐसा ही किया। बेटा ठीक हो गया। दूसरे दिन बड़े उत्साह के साथ मेवे-मिठाइयाँ, फूल-फल, दान-दक्षिणा लेकर आश्रम में पहुँचा। उस शिष्य को साष्टाँग प्रणाम किया। गुरूजी भी पधार चुके थे, उनको चरणों में भावविभोर होकर लिपट गया। आँखों से प्रेमाश्रू बह रहे हैं। हृदय कृतज्ञता से गदगद हो रहा है।
गुरूजी ने सारी बात जानी। भीतर तो खुश हुए लेकिन शिष्य को रामनाम की और गरिमा समझाने के लिए बनावटी क्रोध का दिखावा किया। शिष्य को बुरी तरह डाँटाः
"तूने तीन रामनाम का खर्च कर दिया ! मेरे रामजी की महिमा का अनादर किया। मूर्ख ! तू मेरे आश्रय में रहने लायक नहीं है। भृकुटी विलास सृष्टि लय होवई। जिसके भृकुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है, नयी सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, जिनके संकल्प मात्र से पालना हो सकती है, ऐसे मेरे प्रभु के नाम को एक तुच्छ रोग दूर करने में खर्च कर दिया। तू मेरे आश्रम में रहने के काबिल नही है।"
शिष्य गिड़गिड़ाने लगा। सेठ ने शिष्य की ओर से गुरू महाराज से क्षमा की याचना की। गुरू महाराज पहुँचे हुए संत थे। वैखरी वाणी से रामनाम जपते-जपते मानसिक जप में जाते, फिर मध्यमा में और पश्यन्ती वाणी में पहुँचते। फिर पश्यन्ति को भी पार करके परावाणी में डूब जाते थे। जहाँ से सारी सृष्टि का आविर्भाव होता है और जहाँ आखिर में सृष्टि लीन हो जाती है। उस विश्व-चैतन्य में विश्रान्ति पाये हुए सत्पुरूष थे। शिष्य का कल्याण करने के लिए ही यह सब लीला हो रही थी।
रामजी की कृपा से कहो, अपने योगबल से कहो, गुरूजी ने एक चमकता हुआ पत्थर अपनी गद्दी के नीचे से निकाला। शिष्य को देते हुए कहाः 'बाजार में इसका मूल्यांकन करा के आ इसको बेचना नहीं है, केवल जाँच कराके आ कि इसका कितना दाम मिल सकता है।"
शिष्य पत्थर लेकर बाजार में पहुँचा। सब्जी वाली को दिखाया। पूछाः
"यह चमकता पत्थर लोगी ?"
माई ने देखा कि बड़ा शानदार है ! बोलीः "हाँ। वैसे तो बाट के स्थान पर रख सकती हूँ लेकिन बच्चों को खेलने दूँगी तो बच्चे खुश हो जाएँगे। इसके बदले में सेर भर सब्जी दे सकती है। चार मूली ले जाओ। टमाटर चाहिए तो सेरभर टमाटर ले जाओ।"
"नहीं बेचना है।" शिष्य पत्थर लेकर आगे गया। किरानेवाले को बताया तो बोलाः "अच्छा चमकीला पत्थर है। दो-पाँच रूपये दे सकता हूँ, छोड़कर जाओ।"
शिष्य आगे बढ़ा। पहुँचा किसी समझदार बनिये के पास। माल दिखाया। बनिये को लगाः "यह कुछ गहने जैसा लग रहा है, बड़ा सुन्दर है। पच्चीस-पचास रूपये में मिल जाये तो रख लूँ।" बनिये ने शिष्य को मूल्य बताया। शिष्य और आगे बढ़ा। पहुँचा सुनार के पास और पत्थर दिखाया। सुनार ने देखा कि यह तो हीरा है। इसको अगर तोड़कर छोटे-छोटे पुखराज बनाये जाएं तो इससे हजारों रूपये कमा सकता हूँ। उसने मन ही मन दाम का अंदाज लगाया। होगा पाँच-सात हजार का। वह शिष्य से बोलाः "दो तीन हजार दे सकता हूँ।"
शिष्य का आश्चर्य बढ़ रहा था। एक सेर सब्जी के मूल्य से तीन हजार के मूल्य तक पहुँचा था। उसकी हिम्मत बढ़ गई। समझ गया कि यह साधारण पत्थर नहीं है। 'नहीं बेचना है' कहकर आगे बढ़ा। किसी जौहरी को दिखाया। उसने पत्थर हाथ में लिया, इधर-उधर पलटकर देखा। बड़ा मूल्यवान हीरा है यह तो ! कुछ हिसाब लगाकर शिष्य से बोलाः "महाराज इसका मैं 25000 रूपये दे सकता हूँ।"
शिष्य तो दंग रह गया रकम सुनकर। गुरू महाराज अगर बेचने को कहते तो पाँच-दस रूपये में बेचकर आ जाता, क्योंकि उसके असली मूल्य का पता नहीं है। अच्छा हुआ गुरू महाराज ने बेचने का मना किया है। सिर्फ मूल्य का पता लगाना है। 'नहीं बेचना है।' कहकर शिष्य आगे बढ़ गया। पहुँचा एक बड़े जौहरी की प्रतिष्ठित दुकान पर। वहाँ कई निष्णात हीरापारखू काम करते थे। उन्होंने देखा कि यह तो बहुत मूल्यवान हीरा है। इसकी कीमत आँकना हमारे बस की बात नहीं है। ईमानदार लोग थे। बोलेः
"इसका दाम तो लाखों रूपया हो सकता है। हम इतनी रकम तो दे नहीं सकते।" हीरा वापस कर दिया।
आखिर शिष्य पहुँच गया राजा के पास। उसका हौंसला अब बढ़ गया था। अमूल्य चीज उसके पास जो था। राजदरबार में जाकर बोलाः
"राजाजी ! मैं एक मूल्यवान हीरा लाया हूँ। आप उसके कितने रूपये दे सकते हैं ?"
राजा ने पूछाः "यह हीरा कहाँ से लाये हो ?"
शिष्य ने अपने गुरूदेव स्वामी रामानंदजी का परिचय देते हुए कहाः "इस हीरे का मूल्य करवाना है।"
राजा स्वामी ने रामानंदजी को जानते थे, बड़ा आदर था उनके प्रति। दरबार के और लोग भी इन संत पुरूष को जानते थे, मानते थे। राजा ने अपने राज-जौहरियों को बुलाया, हीरा दिखाया। उन्होंने सूक्ष्मता से हीरे की जाँच की। आखिर में बतायाः
"महाराज ! यह चमकीला हीरा दिखता है लेकिन केवल हीरा ही नहीं है। यह तो पारस है पारस ! इससे तो सैंकड़ों हजारों मन सोना बना सकते हैं। इसका मूल्य हम क्या बतायें ? पूरा राज्य देकर भी यह पारस मिल जाय तो भी सस्ता है।"
राजा ने शिष्य से कहाः "स्वामी जी को विनती करना कि अगर बेचना है तो मैं यह तख्त दे सकता हूँ, पूरा राज्य दे सकता हूँ।"
"गुरू महाराज ने बेचने को मना किया है। केवल इसका मूल्यांकन करवाने भेजा है।"
"मूल्यांकन तो हम नहीं कर सकते, तख्त दे सकते हैं, राज्य दे सकते हैं इसके बदले में।"
शिष्य हीरा लेकर गुरू महाराज के चरणों में लौट आया।
गुरूजी ने पूछाः "बेटे ! क्या मूल्य हुआ इस सुहावने पत्थर का ?"
शिष्य तो आश्चर्य से मुग्ध हो गया था। बोलाः "गुरू महाराज ! इसके बदले में सारा राज्य मिल रहा है। हमें राज्य ले लेना चाहिए।"
अरे पगले ! अभी तूने इसका प्रभाव नहीं देखा। यह पारस है पारस ! रामानंदजी ने लोहे के टुकड़े मंगाये और पारस का स्पर्श कराकर सोना बना दिया।
"गुरू महाराज ! यह तो अदभुत चीज है !"
"यह तो जड़ हीरा है। मेरा रामनाम का हीरा तो ऐसा है कि उसके आगे यह राज्य तो क्या इन्द्र का राज्य भी फीका हो जाता है। ब्रह्मलोक का सुख भी उसके आगे कोई मूल्य नहीं रखता। ऐसा है आत्महीरा।"
जब
पाया आतम हीरा
जग हो गया सवा
कसीरा।
जिसको आत्महीरा मिल जाता है उसके लिए ब्रह्माण्ड भर के भोग तुच्छ हो जाते हैं।
वैखरी वाणी से रामनाम जपते-जपते, हरिनाम जपते-जपते, भगवन्नाम का स्मरण करते-करते जो साधक मानसिक जप में चले जाते, मध्यमा में पहुँच जाते हैं उनके सारे अघ, सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। उनका पाप का पुंज दग्ध हो जाता है। ऐसे निर्मल बने हुए साधक प्रभु-नाम स्मरण से जो रस पाते हैं वह रस राज्य सुख में नहीं है। राम तत्त्व में, परमात्म-तत्त्व में विश्रान्ति पाने से जो सुख मिलता है, जो आराम मिलता है, जो निर्द्वन्द्व और निःशंक शान्ति मिलती है वह शान्ति, वह सुख, वह आराम स्वर्ग के भोगों में नहीं है, ब्रह्मलोक के सुख में नहीं है।
परमात्म-तत्त्व को सुनने के लिए मन की एकाग्रता, हृदय की पवित्रता और बुद्धि की जिज्ञासा चाहिए।
भागवत में आता है कि सृष्टि के आदि में महाकाश रूप चिदघन चैतन्य था। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान की नाभि क्या है ? भगवान का शरीर क्या है ? भगवान का शरीर है चिदाकाश स्वरूप। उस चिदाकाश स्वरूप से ब्रह्माजी प्रकट हुए। चहुँ और निहारा। कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर आँखें बन्द करके चिन्तन करने लगे। तब रहस्य प्रकट हुआ और आदि सत्य-स्वरूप भगवान नारायण की कृपा से चतुःश्लोकी भागवत स्फुरित हुई। इन चार श्लोकों में चार बात बताई गईः सत्य का स्वरूप, माया का स्वरूप, जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप।
जो सृष्टि के आदि में था, सृष्टि के मध्य में है, सृष्टि के लय के बाद भी रहेगा, जो जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति में रहता है, जो बाल्यवस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में रहता है और मृत्यु के बाद भी रहता है, शरीर बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता, बुद्धि बदलने के बाद भी नहीं बदलता, सृष्टियाँ बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता वह है सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म। वही है सच्चिदानंदघन परमात्मा और वही है सनातन सत्य। इस सनातन सत्य का साक्षात्कार करानेवाला धर्म है सनातन धर्म।
जगत का रहस्य क्या है ? यह जगत जो दिखता है वह कोई और धातु से नहीं बना। उस सनातन सत्य का, परम तत्त्व का विवर्त ही यह जगत है। जैसे सागर का जल शान्त है, निस्तरंग। उसमें लहर आयी, तरंग उठा, भँवर बना, हलचल मच गई। कुछ का कुछ बनने लगा, बिगड़ने लगा। नया कुछ नहीं है। वही जल ही जल है। जल ही तरंग होकर दिख रहा है, भँवर बन रहा है, फेन और बुदबुदे पैदा कर रहा है। वैसे ही है तो केवल ब्रह्म। उसमें विवर्त से विश्व भास रहा होता है।
सत्य-स्वरूप परमात्मा की सत्ता से पंच भौतिक सृष्टि भास रही है। माया का विलास दिख रहा है। प्रकृति का परिवर्तन नजर आ रहा है। शरीर जन्मता है, बड़ा होता है, क्षीण होता है और मर जाता है। यह सब परिवर्तन जिसकी सत्ता से दिखता है, जिसकी सत्ता से परिवर्तन का ज्ञान होता है वह सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म है। सब जीवों का वही वास्तविक स्वरूप है। तुम्हारा भी असली स्वरूप वही है। हजार-हजार प्रलय होने के बाद भी तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होती ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। हजार-हजार लाभ होने पर भी तुम्हारे में कुछ बढ़ता नहीं, हजार-हजार लाभ होने पर भी तुम्हारे में कुछ घटता नहीं, हे मित्र ! हे साधक ! जिज्ञासु ! ऐसा तेरा स्वरूप है। प्रलय की आग भी उसे जला नहीं सकती। ऐसे अपने आत्मदेव को केवल तीन मिनट के लिए भी जान ले तो तेरा परम कल्याण हो जायगा।
चतुःश्लोकी भागवत में बताई गई इन बातों का यथार्थ श्रवण, मनन और निदिध्यासन किया जाय तो हृदय में मुक्ति का अनुभव हो जाय। वेदान्त का जिज्ञासु साधक बाहर की वस्तुओं का उतना मूल्यांकन नहीं करता जितना वृत्तियों का मूल्याकंन करता है। वह जाँच करता है कि बाहर की वस्तुओं और परिस्थितयों का प्रभाव मेरी वृत्तियों पर कैसा पड़ता है ? बाह्य परिस्थिति का प्रभाव जितना कम पड़ता है उतना साधक उन्नत होता है।
सुख का प्रभाव भी अपने अन्तःकरण की हल्की स्थिति होती है तब पड़ता है। दुःख का प्रभाव भी तब पड़ता है। अन्तःकरण की ऊँची स्थिति में सुख-दुःख का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, सुख-दुःख जिसकी सत्ता से भासता है उस मन के प्रभाव में भी वह साधक नहीं आता। वह अपने आत्मा के प्रभाव में इतना तल्लीन रहता है कि उसके चित्त पर सुख-दुःख का, मान-हानि का, अपने-पराये का और यहाँ तक कि जीवन-मरण का भी प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर बाह्य चीजों का प्रभाव अपने ऊपर पड़ रहा है तो समझ लेना, अभी जिज्ञासा नहीं जगी। राम में आराम पाने की आकांक्षा नहीं हुई। राम में आराम पाने के लिए श्रीकृष्ण बताते हैं-
तेषां
सततंयुक्तानां
भजतां
प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि
बुद्धियोगं
तं येन
मामुपयान्ति
ते।।
'उन निरन्तर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजने वालों भक्तों को मैं वह तत्त्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'
(भगवद् गीताः 10.10)
भगवान को प्रीतिपूर्वक अगर ध्याया जाय तो बुद्धियोग मिलता है। बुद्धि तो सबके पास है छोटी-मोटी। बुद्धि में योग मिल जाय, मन में एकाग्रता आ जाय तो भगवत्प्राप्ति में देर नहीं लगती।
चित्त की एकाग्रता वेदान्त में भी अभीष्ट है, योग में भी अभीष्ट है, भक्ति में भी अभीष्ट है और व्यवहार में भी अभीष्ट है।
निष्काम कर्म करने से भौतिक उन्नति होती है। हृदय की रसप्रद धारा शुरू होती है। शरीर को भौतिक बनाने से भगवान पदार्थों के रूप में प्राप्त होते हैं। अन्तःकरण को आस्तिक बनाने से भगवान प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। बुद्धि को आध्यात्मिक बनाने से भगवान समग्र स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, आत्म-साक्षात्कार हो जाता है।
गीता के सातवे अध्याय में भगवान कहते हैं-
मय्यासक्तमनाः
पार्थ योगं
युञ्जन्मदाश्रयः।
असंशयं
समग्रं मां
यथा
ज्ञास्यसि
तच्छ्रणु।।
'हे पार्थ ! अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन।'
(गीताः 7.1)
भगवान के समग्र स्वरूप का बोध हो जाय तो तुम्हारा धर्म केवल मंदिर में ही नहीं रहेगा, केवल मस्जिद में ही नहीं रहेगा, केवल यज्ञकुण्ड में ही नहीं रहेगा, केवल मस्जिद में ही नहीं रहेगा, केवल यज्ञकुण्ड में ही नहीं रहेगाष रसोई के चौके तक नहीं, छूत-छात नहीं रूकेगा अपितु जीवन के हर क्षेत्र में, हर चेष्टाओं में प्रकट हो जायेगा। चलते-फिरते, खाते-पीते, हँसते-रोते, लेते देते तुम्हारा धर्मानुष्ठान होता रहेगा। भगवान के समग्र स्वरूप का अगर ज्ञान हो जाय तो हरेक चेष्टा में उनकी कृपा महसूस होगी।
भगवान के समग्र स्वरूप का बोध हो जाय तो आपको पता चलेगा कि पदार्थों के रूप में भी वह प्यारा ही मिल रहा है। जीवन के रूप में भी वह प्यारा ही मिल रहा है और मृत्यु के रूप में भी वह प्यारा ही मिल रहा है। शांति के रूप में भी वह प्यारा मिल रहा है और विक्षेप के रूप में भी वह प्यारा मिल रहा है। ऐसी कोई चेष्टा उस प्यारे की नहीं है जो हमारे उत्थान और उन्नति विरूद्ध हो। जब आँधी और तूफान चलता है उसमें भी उस प्यारे की कृपा है। रोग, भूखमरी, महामारी और भयंकर युद्ध होते हैं उसमें भी हम लोगों की कुछ न कुछ घड़ाई होती है। बोधवान जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ उसे वही प्यारा नजर आता है।
जिधर
देखता हूँ
खुदा ही खुदा
है।
खुदा
से न कोई चीज
जुदा है।।
जब
अव्वल और आखिर
खुदा ही खुदा
है।
तो
अब भी वही है
क्या इसके
सिवा है ?
बुद्धि अगर आध्यात्मिक हो जाय तो भगवान समग्र स्वरूप में प्रकट हो जाएँगे।
योग तो बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग योग करके सिद्धियाँ पाना चाहते हैं। कुछ लोग योग करके सूक्ष्म जगत को देखना चाहते हैं। कई लोग योगाभ्यास करके ऐहिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग योग करके तन-मन को पवित्र करना चाहते हैं लेकिन कोई विरले हैं जो योग करके भगवान को पाना चाहते हैं। वे लोग भगवान की प्रीति के लिए योग करते हैं। जैसे लखनलाला योग करते थे, सेवा करते थे भगवान की प्रीति के लिए। रामजी ब्रह्मलीन हो गये तो लखनलाला सरयू के तीर पर अपने प्राणों की गति को सम करके अपनी देह को अदृश्य कर दिया। राम जी से प्रीति करने वाले जो नगरवासी योगयुक्ति जानते थे वे भी रामजी के पीछे उसी ढंग से गये।
उद्धव भगवान के प्रीतिपात्र थे। भगवान ने उनको तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर एकान्तवास में आत्मानुसन्धान के अभ्यास के लिए भेज दिया था। विदुरजी को ज्ञान में प्रीति थी, निष्ठा थी। उनको जब लगा कि दुर्योधन भगवान श्रीकृष्ण का अनादर कर रहा है तब उन्होंने उसका त्याग किया। चले गये गंगा किनारे। वहाँ उद्धवजी की मुलाकात हुई। दोनों मैत्रेय ऋषि के चरणों में पहुँचे।
विदुरजी ज्ञान निपुण थे। अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी अगर मिल जाते हैं, अपने से श्रेष्ठ भक्त अगर मिल जाते हैं, भगवान में रमण करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति मिल जाते हैं तो सुज्ञ पुरूष उनका संग करने में, उनका सत्संग सुनने में रूचि रखते हैं। मैत्रेय ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर जिज्ञासा करके वेदान्त-श्रवण करने को बैठ गये। विदुर जैसे ज्ञानी भी वेदान्त श्रवण करते हैं क्योंकि भगवान में, परमात्मा में उनकी प्रीति है।
हनुमानप्रसाद पोद्दार को भगवान के साकार श्रीविग्रह के दर्शन हुए। दर्शन के बारह साल बाद में भी एकान्तवास करने के लिए अपने मित्रों से, साथियों से विनती करके, जान छुड़ाके चले गये। कहते गयेः "मुझे थोड़े दिन परमात्मा में रहने दो.... उसके रस में डूबने दो।"
आदमी जितना-जितना परमात्मा-रस का अनुभव करता है उतना-उतना निर्मल होता है, बलवान होता है। संसार का ऐसा कोई भोग नहीं जो भोगने के बाद आदमी थके नहीं, भोगने के बाद आदमी मलिनता का अनुभव करे नहीं। भोजन में भी अगर मलिनता न होती तो भोजन के बाद हाथ-मुँह क्यों धोते ? ऐसा कोई भोग नहीं जिसमें मलिनता का मिश्रण न हो। योग ऐसा कि सारी मलिनताओं को हटा देता है।
हरिबाबा हो गये वृन्दावन में। वे प्रतिदिन तीन लाख भगवन्नाम जप करते थे। मंत्र जप पूरे होते, बाद में भिक्षा लेने जाते। कभी दोपहर के तीन बजे जाते, कभी चार बजे जाते, साढ़े चार बजे जाते। भिक्षा में जो कुछ बचा हुआ रूखा-सूखा मिल जाता, ठाकुर जी को भोग लगाकर पा लेते।
एक दिन उनको लगा कि ठाकुर जी कह रहे हैं-
"तुम एकदम रूखा-सूखा बेस्वाद भोग लगाते हो। कम से कम सबरस (नमक) तो उसमें डाला करो।"
बाबाजी ठाकुरजी पर नाराज हो गये कि आज आपको नमक खाने की इच्छा हुई ? तुम्हारे लिए नमक माँगू ? फिर कल बोलोगे कि सब्जी चाहिए.... परसों बोलोगे खीर चाहिए। ऐसे ठाकुरजी मुझे नहीं रखने हैं।
उठाया ठाकुरजी को और दूसरे किसी बाबाजी के वहाँ दे आये। फिर आये अपनी कुटिया में। भजन करने बैठे।
संयोगवशात् सामने बहती हुई यमुना नदी में एक नाव जा रही थी नमक भरके। अभी तो नहरें निकाली हैं इसलिए यमुना दुबली-पतली हो गयी है। उस वक्त बहुत पानी रहता था। नावें चलतीं थी उसमें।
किसी कारणवशात् नाव डूबने लगी। नाववालों ने मनौती मानी की अगर हम लोग बच जायें, नाव डूबे नहीं, किनारे सुरक्षित पहुँच जायें तो नाव का माल-सामान दान कर देंगे। दैवयोग से नाव बच गई। उन्होंने सारे नमक का ढेर लगा दिया हरिबाबाजी की कुटिया के पास। बाबाजी बाहर निकले तो देखा सब तमाशा। ठाकुर जी को उलाहना देने लगे कि नमक खाने की इतनी इच्छा हुई कि किसी को प्रेरणा करके नमक का ढेर लगवा दिया ? ऐसे सबरस के प्यासे भगवान का भजन हम नहीं करते। अपनी झोंपड़ी छोड़कर बाबाजी चले गये एकान्त में गहरी साधना करने के लिए।
भगवान के सच्चे भक्तों को संसार का सुख लेने की तनिक भ्राँति भी बाँध नहीं सकती। मन ही ठाकुरजी का बहाना बनाकर बोलता है कि नमक लाओ, आज बाल-भोग लगाओ, आज मोहनथाल लाओ। वास्तव में ठाकुरजी मोहनथाल खाना नहीं चाहते, अपना मन ही ठाकुर जी के नाम से धोखा करता है।
पुजारी बोलता है कि आज ठाकुरजी को खीर-पूरी अर्पण करना है, आज ठाकुरजी को घड़ी पहनना है, ठाकुरजी को पान-बीड़ा खाना है। सचमुच ठाकुरजी की भोग की इच्छा नहीं। हमारा अनियंत्रित मन युक्ति करके ठाकुर जी के नाम से भोग चाहता है। ऐसे ही भोग की इच्छा तृप्त करे इसके बजाय ठाकुरजी को भोग लगाकर करे यह भी चलो ठीक है। पान-बीड़ा खाना है तो ठाकुरजी को भोग लगाकर खाओ।
भगवान वेदव्यास ने तामसी और आसुरी स्वभाव के लोगों के लिए भी शास्त्रों की रचना की है। जिन लोगों को मांस-मदिरा के बिना नहीं चलता था ऐसे लोगों को थोड़ी छूट-छाट दी। अगर मांस खाना है तो पहले यज्ञ करो, देवी को बलि चढ़ाओ, बाद में खाओ। एकदम जो काट-काटकर खाते थे उसके बदले यज्ञ करेंगे, बलि देंगे फिर बाँटकर खाएँगे। उस खाने में विलम्ब होगा। जहाँ दस बकरे स्वाहा हो सकते थे उतने समय में एक ही बकरे तक पहुँचेंगे, नौ की हिंसा कम होगी।
जैसे बच्चा पाँच घण्टे बेकार भटकता है उसे बाप कहता हैः "बेटा देख ! तू हर रोज एक घण्टा सुबह और दो घण्टे शाम को घूमा कर। हर रोज तीन घण्टे। जो हर रोज पच्चीस रूपये बिगाड़ता है उसको कहाः "दो रूपये सुबह, तीन रूपये शाम को खर्च कर। हर रोज पाँच रूपये तेरी खर्ची बाँध देता हूँ।"
बाप ऐसे बच्चे को भटकने के लिए प्रेरित नहीं करता है लेकिन उसकी भटकान को नियंत्रित करने से लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही शास्त्रों में जो आदेश दिया है वह हमारे अनियंत्रित बेलगाम मन को युक्ति से नियंत्रण में लाने के लिए दिया है।
शास्त्रों ने बताया कि शादी-विवाह करना चाहिए। जीव में जन्मों-जन्मों से कामरस का आकर्षण है। इसी आकर्षण में ही जीवन बरबाद न हो जाय इसलिए काम को नियंत्रित करने के लिए एक ही व्यक्ति से शादी का आदेश दिया। जब तक शादी हो जाय तब तक चुप रहो। फिर एक पत्नी व्रत। पत्नी मायके चली जाय तब संयम से रहे। पत्नी का पैर भारी हो जाय तब संयम से रहे। पत्नी का स्वभाव गड़बड़ रहे तब तक संयम से रहे। इस प्रकार इन्द्रिय भोग से बचने के लिए शास्त्रों ने शादी-विवाह का आयोजन किया।
'भगवानों ने भी शादी की थी..... श्रीकृष्ण को भी राधा थी। शिवजी को भी पार्वती थी..... चलो हम भी अपनी पार्वती लायें। ऐसा तर्क देकर भोगी 'पार्वती' लाते हैं और पिक्चर में धक्का खाते हैं।
भोग में डूबने के लिए शास्त्रों ने आज्ञा नहीं दी लेकिन भोग में डूबने की आदतवालों को भोग से थोड़ा-थोड़ा बचाकर योग के तरफ मोड़ने का प्रयास किया है।
इसी सिद्धान्त पर वेदव्यासजी ने आसुरी, तामसी लोगों के लिए बनाये गये शास्त्रों में मांस-मदिरा आदि की थोड़ी छूट-छाट दी। नीति नियम बनाये। नारदजी पहुँचे वेदव्यास के पास और बोलेः
"भगवन् ! आपने शास्त्रों की रचना तो की, यज्ञ-होम-हवन के साथ अन्य चीजों की छूट-छाट तो दी लेकिन आपका संयम का हिस्सा वे लोग नहीं पढ़ेंगे, छूट-छाटवाला हिस्सा जल्दी से ले लेंगे। अपने मन के अनुकूल जो होगा वह झट से अमल में लायेंगे। शास्त्रों में कहा है कि बलि चढ़ाकर मांस खाओ।' खाने लगेंगे। शराब पीने लगेंगे।"
लोगों ने शिवजी को भाँग पीने वाले बना दिये हैं। 'शिवरात्री आयी। पियो भाँग। शिवजी की बूटी है।' अरे ! शिवजी के लिए तो कहा गया हैः
भुवन
भंग व्यसनम्।
यानी 'भगवान शिव को भुवनों का भंग करने का व्यसन है।' लोगों ने अर्थ लगाया कि शिवजी को भाँग पीने का व्यसन है। 'शिवजी की बूटी' कहकर लोग भाँग पीने लग गये।
नारद जी ने वेदव्यास जी से कहाः "महाराज ! आपने अति तामस प्रकृति के लोगों को मोड़ने के लिए थोड़ी छूट-छाट दी है। वे मुड़ेंगे तब मुड़ेंगे लेकिन और लोग इसका गैर फायदा उठाकर गिर सकते हैं। इसलिए आप भागवत जैसे ग्रन्थ की रचना करो, जिसमें भीतर का रस मिलता जाय। उसमें भगवान की कथा-वार्ता-चर्चा हो, भगवन्नाम की महिमा हो, भगवान के गुणगान हों। इससे भगवान में प्रीति जगेगी। भगवान में प्रीति जगेगी तब विषयों की प्रीति हटेगी।"
कायदे-कानून में विषयों की प्रीति नहीं हटती। कायदे से अगर आदमी ईमानदार बन जाता तो आज नेताओं के नौकर और स्वयं नेता भी ईमानदार हो जाते। कायदे तो ठीक हैं, उद्दण्ड और उच्छ्रंखल लोगों के लिए कायदों की आवश्यकता है लेकिन आदमी भीतर से ही अच्छा हो तो ईमानदार बन सकता है कायदे से नहीं।
किसी आदमी पर चार चौकीदार रख दो निगरानी रखने के लिए कि वह अच्छी तरह व्यवहार करे, अच्छा जिये। फिर भी वह आदमी अच्छा ही है इस बात में सन्देह होगा। क्योंकि वे चार लोग कैसी निगरानी रखते हैं यह भी देखना पड़ेगा। उनके ऊपर भी और कोई रखना पड़ेगा।
वस्तुओं का शोधन, परिमार्जन, परिवर्धन करना यह विज्ञान है। अन्तःकरण का शोधन, परिमार्जन और परिवर्धन करना यह धर्म हैं। धर्म से वासनाएँ निवृत्त होती हैं। योग से मन एकाग्र होता है। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और भगवान अपनी कृपा से प्राप्त की प्राप्ति का अनुभव करा देते हैं।
जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजते हैं, भगवन्नाम का जप करते-करते ध्यानस्थ होते हैं उनकी बुद्धि में भगवान योग मिला देते हैं जिससे वह भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है।
ददामी
बुद्धियोगं
तं येन
मामुपयान्ति
ते।
भगवान जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं कि वह मुझे खोजता है। दया करके उसको बुद्धियोग दे देते हैं, जीव भगवान को पहचान लेता है।
विषयों की खोज मिटाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। फिर, विषयों के सुख के आकर्षण को मिटाने के लिए भक्तिरस की, योगरस की आवश्यकता है। भक्ति करेंगे, योग करेंगे तो भीतर का रस आयगा। भक्ति और योग छूट गये तो मन इधर-उधर चला जायेगा। इसलिये भगवान कहते हैं-
तेषां
सततंयुक्तानां
भजतां
प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि
बुद्धियोगं
तं येन
मामुपयान्ति
ते।।
'जो सतत प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको मैं बुद्धियोग देता हूँ....'
आप सतत राम.... राम..... राम... राम... राम.... राम... राम करते रहे यह भी संभव नहीं, सतत समाधि में ही बैठे रहें यह भी संभव नहीं, सतत सत्संग में बैठे रहे यह भी संभव नहीं, सतत मंदिर रहकर पूजा-अर्चना-आरती करते रहें यह भी संभव नहीं। भगवान सततयुक्तानां क्यों कहते हैं ? हम भगवान में सतत निरन्तर कैसे लगें ?
जैसे पंखा, बिजली का गोला, टयूबलाईट, एम्पलीफायर आदि विद्युत से चलने वाले साधन अलग-अलग दिखते हैं लेकिन उन सबके कार्य का आधार एक ही विद्युत है, ऐसा जिसको ज्ञान है वह गोला देखता है तब भी विद्युत का साक्षात्कार हो रहा है, पंखे को देखता है तब भी विद्युत का साक्षात्कार हो रहा है और टयूबलाईट या एम्पलीफायर को देखता है तब भी विद्युत का साक्षात्कार हो रहा है।
ऐसे ही बुद्धि में जब योग मिल जाता है तो भिन्न-भिन्न व्यवहार करते समय, भिन्न-भिन्न क्रिया-कलाप करते समय व्यवहार के आधार अभिन्न आत्मा की स्मृति बनी रहती है।
भगवान का भजन जो प्रीतिपूर्वक करते हैं उनकी बुद्धि में योग मिल जाता है। बुद्धि में योग मिलने से जीव ज्ञातज्ञेय हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। वे इस जीव की परेशानी जानते हैं कि पहले वह संसार की चीजों को पकड़ता था, अब साधना के साधनों को पकड़ेगा, माला और मनके को पकड़ेगा, टीले और टपके को पकड़ेगा। भगवान जब अति प्रसन्न होते हैं तो उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्राप्त की प्राप्ति का एहसास करा देते हैं। 'मैं तुझसे दूर नहीं.... तू मुझसे दूर नहीं.....' ऐसा बोध करा देते हैं। बुद्धि में जब आत्म-प्रकाश की प्राप्ति होती है तब जीव का बोलना-चालना, लेना देना, खाना-पीना, रोना-धोना, लड़ना-खेलना सब भजन हो जाता है। कबीर जी कहते हैं-
साधो
भाई ! सहज
समाधि भली।
गुरू
कृपा भई जा
दिन ते दिन
दिन अधिक
चली।।
खाऊँ
पीऊँ सो करूँ
पूजा हरूँ
फरूँ सो करूँ
परिक्रमा।
सोऊँ
तब करूँ
दण्डवत् भाव न
राखूँ दूजा।।
साधो
भाई....
उसकी सहज समाधि हो जाती है। सहज समाधि वास्तव में सदा लगी हुई है, सबकी लगी हुई है लेकिन हम लोग नहीं जानते। इन्द्रियों के आकर्षण में, शरीर के आकर्षण में, बाहर के आकर्षण में उलझ गये इसलिए सहज समाधि का अनुभव नहीं होता।
आत्मा की समाधि कभी टूटी नहीं और अनात्मा की सच्ची समाधि कभी लगी नहीं। हर जीव परमात्मा में उत्पन्न होता है, परमात्मा में रहता है और परमात्मा में विलीन होता है जैसे हर तरंग सागर में उत्पन्न होती है, सागर में नाचती है और सागर में ही लीन होती है। ऐसे ही हम लोग सब ईश्वर में उत्पन्न होते हैं, ईश्वर में जी रहे हैं, ईश्वर में खेल रहे हैं, ईश्वर में लीन होंगे और फिर ईश्वर में ही उत्पन्न होंगे। फिर भी हमारी व्यक्तिगत मान्यताएँ, आकांक्षाएँ और वासनाएँ हमें ईश्वर से दूर होने का एहसास कराती हैं, परम सुख से दूर कर देती हैं। इसीलिए सुख के लिए हम भागते-फिरते हैं। जीव जितना-जितना बाह्य सुख के लिए भागता रहता है उतना-उतना दुःखी होता है।
ब्रह्मचिन्तन करते-करते प्रज्ञानन्द नाम के संत ब्रह्मलोक की गति तक पहुँच गये। अभी ब्रह्म साक्षात्कार तो नहीं हुआ था फिर भी जो सुख-वैभव ब्रह्माजी को मिलता है वह ब्रह्मचिन्तन करने वाले साधक को मिलता है। आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाय तो जीव ब्रह्म में लीन हो जाय। आत्म-साक्षात्कार नहीं हुआ तो वह ब्रह्मलोक के सुखों को भोगता है।
ब्रह्मलोक में इन्द्रियों के विकारी सुख नहीं है। वहाँ सहज में सुख के साधन मिलते हैं। वहाँ बुढ़ापा नहीं आता। वहाँ शरीर जीर्ण-शीर्ण नहीं होता, रोग नहीं आता। पानी पीने के लिए हाथ लम्बा नहीं करना पड़ता। ऐसे ही संकल्प मात्र से जलरस प्रकट हो जाता है, जीव तृप्त हो जाता है।
ऐसे दिव्य भोग भोगते-भोगते प्रज्ञानन्द को हजारों वर्ष बीत गये। प्रज्ञानन्द की इच्छा हुई किः "मैं जिस मृत्युलोक से ब्रह्मलोक में आया हूँ उस मृत्युलोक का क्या हाल-चाल है, जरा जान लूँ, देख लूँ।' उनकी बुद्धि तो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत थी। देखते हैं कि अरे, मृत्युलोक के मानव नाहक दुःखी हो रहे हैं। जहाँ दुःख नहीं है वहाँ दुःख पैदा कर रहे हैं। जहाँ भय नहीं वहाँ भय की कल्पना कर रहे हैं। जहाँ अशान्ति की गुंजाईश नहीं वहाँ अशान्ति बना रहे हैं। इन बेचारे जीवों को पता नहीं कि जो सुख आते हैं वे दुःख दे जाते हैं और चले जाने वाले में ये उलझ रहे हैं ? ऐसे आदमी हैं ? प्रज्ञानन्द को आश्चर्य हो रहा था। ब्रह्मलोक के लोगों ने बताया कि, "बाबाजी ! जब आप वहाँ थे तब आप भी ऐसा ही करते थे।'
आदमी जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण से प्रभावित हो जाता है। इसलिए छोटी-छोटी बातों में बह जाता है। जब उस वातावरण से ऊपर उठ जाता है, उन्नत बन जाता है तब पीछे रहने वाले लोगों के लिए सोचता है कि ये बेचारे क्या कर रहे हैं ! जैसे नन्हा-मुन्ना बच्चा चार पैसे का खिलौना मिलने से राजी हो जाता है और दो पैसे का खिलौना टूट जाने से दुःखी हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि हम खिलौनों के बिना भी जी सकते थे। उस समय यह पता नहीं था। उस समय तो वह सर्वस्व था। चार पैसे का सक्करपारा जीवन बन जाता था, दो पैसे की लॉलीपॉप जीवन बन जाती थी, कोई जरा सी आँख दिखा देता तो मृत्यु का भय हो जाता था, कोई जरा सा पुचकार देता तो पानी-पानी हो जाते थे। अब पता चला कि यह तो बचकानी बुद्धि थी।
जैसे बचपन की बुद्धि आपको अब छोटी लगती है ऐसे ही जब भगवान बुद्धियोग देंगे तब आज की बुद्धि भी आपको बचकानी लगेगी। दो पाँच लाख मिल गये, राजी हो गये। दो-पाँच लाख चले गये, दुःखी हो गये। जब बुद्धियोग मिलेगा तब पता चलेगा कि यह भी एक बाल्यावस्था है।
न
खुशी अच्छी है
न मलाल अच्छा
है।
यार
जिसमें रख दे
वह हाल अच्छा
है।।
हमारी
न आरजू है न
जुस्तजू है।
हम
राजी हैं
उसमें जिसमें
तेरी रजा है।।
ऐसी समता की ऊँचाई पर आदमी पहुँच जाता है।
मगध के राजा के सौ पुत्र थे। परम्परा ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा कुमार होता उसको राजगद्दी मिलती। उस परम्परा को मगधनरेश तोड़ना चाहते थे। सौ पुत्रों में सबसे बड़े को नहीं बल्कि जो सबमें विशेष योग्यतावाला हो उसे राज्य देना चाहते थे। जैसे, भगवान जिसकी विशेष योग्यता समझते हैं ऐसे प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले के आगे भगवान अपना रहस्य खोल देते है। प्रीतिपूर्वक भजने वाले को भगवान सत्संग में भेज देते हैं। प्रीति पूर्वक भगवान की आकांक्षा करने वाले को भगवान ब्रह्मवेत्ता गुरू की मुलाकात करा देते हैं ऐसे ही मगध नरेश ने सोचा कि 'सबसे उत्तम अधिकारी बेटे को ही राज्य देना चाहिए। सबसे बड़े बेटे को राज्य देना अनिवार्य नहीं है। जिसकी योग्यता हो वह राज्य का अधिकारी हो। अब परीक्षा करें।'
सौ बेटों को आदेश दिया कि कल भोजन शाला में सब लोग भोजन करने को एक साथ बैठोगे। भोजने के व्यंजन तैयार हुए। मंत्रियों को जो कुछ करना था सब समझा दिया गया। सौ के सौ राजकुमार भोजन करने बैठे। विशाल खण्ड में सुहावने आसन पर पंगत लग गई। भोजन के थाल परोसे गये। घण्ट बजा। 'नमः पार्वती हर हर महादेव....' नारे के साथ ज्यों ही भोजन शुरू हुआ तो भोजनालय में शिकारी कुत्ते छोड़ दिये गये। खुँखार कुत्ते आये तो सब राजकुमार मारे भय के भाग खड़े हुए। थाल छोड़-छोड़कर छू.... हो गये। सब भाग गये लेकिन श्रेणिक नाम का सबसे छोटा राजकुमार बैठा रहा। बराबर भोजन करके तृप्त होकर बाहर निकला। राजा ने छिपकर यह सब देखा।
दूसरे दिन राजा ने सभा भरी। राजकुमारों से कहाः "मैं राज्याभिषेक करना चाहता हूँ अधिकारी कुमार का। कल मैंने परीक्षा कर ली। मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जो परीक्षा में पास हुआ है। तुम लोगों ने कल अच्छी तरह से भोजन किया ?"
सब राजकुमार कहने लगेः "भोजन कैसे करें महाराज ! व्यवस्थापकों में अपना कार्य करने की कुशलता ही नहीं है। वे अपना फर्ज नहीं निभाते, अपनी डयूटी नहीं सँभालते। हम ज्यों भोजन करने लगे। त्यों एकाएक खूँखार शिकारी कुत्ते आ गये। दरवाजा खुला रह गया, क्या हुआ, सब गड़बड़ी हो गई।"
"अच्छा ! तो किसी ने भोजन नहीं किया ?"
श्रेणिक खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर बोलाः "पिता जी ! मैंने भोजन किया।"
"तूने भोजन किया ? बड़ा मूर्ख है। ये कितने चतुर लड़के हैं ! हिंसक कुत्तों से बच निकले। तू बैठा रहा ? कुत्ते काट लेते तो क्या करता ? पागल कहीं का !" अनजान होते हुए पिता ने कहा।
तब श्रेणिक कहता हैः "पिता जी ! मुझे कुत्ते नहीं काट सकते। मैंने भर पेट भोजन कर लिया।"
सब राजकुमार सोच रहे थे कि यह छोटा कैसा नासमझ है। खाने के लिए बैठा रहा नादान। पिता जी हमें ही पसन्द करेंगे। हरेक कुमार मान रहा है कि मेरे सिर पर ही पिता जी मुकुट पहनाएँगे। मेरे हिस्से मे ही राज्य आयेगा। मैं ही सबसे चतुर हूँ।
मगध नरेश ने चतुराई देख ली थी श्रेणिक की। बोलेः "बेटे ! खड़े हो जाओ। सबको बताओ कि तुमने कैसे भोजन कर लिया ? कुत्तों से क्यों नहीं डरा ?"
"महाराज ! भूखा कुत्ता ज्यों ही मेरे नजदीक आता था उसे मैं टुकड़ा फैंक देता था, वह शान्त हो जाता और खाने लगता। जो दूसरों को खिलाता है वह भूखा कैसे रह सकता है ?"
राजा ने श्रेणिक को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
समाज में हम लोग दुःखी क्यों होते हैं ? हम चाहते हैं कि मान मिले तो मुझे मिले, दूसरे का जो होना हो वह हो..... सुख मिले तो मुझे मिले, दूसरे का जो होना वह हो। इसी में हम उलझे रहते हैं। अरे ! दूसरों में भी अपना आपा ही छुपा है। मान मिले तो सबको दो, खाना मिले तो बाँटकर खाओ। वास्तव में मान लेने की चीज नही है, मान तो देने की चीज है।
श्रेणिक सफल हो गया इसमें वेदान्त छुपा है। जो अनजाने में भी वेदान्तिक जीवन जीते हैं उतने अंश में समाज में सफल हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हं। श्रेणिक भयभीत हो जाता तो वेदान्त से च्युत हो जाता। 'कुत्ते ऐसे हैं..... वैसे हैं...' ऐसा द्वेष करता तो भी भाग जाता। कुत्तों को खिलाया और साथ ही साथ खुद ने भी खा लिया। अर्थात् व्यवहार में समता आ गई। 'कुत्तों में भी मैं ही हूँ' ऐसा समझे चाहे न समझे लेकिन वैसा आचरण हो गया।
जो-जो आदमी जितना-जितना उन्नत है उसके पीछे उतना-उतना वेदान्त काम कर रहा है। आदमी जितना-जितना भीतर से सरल और साहसी होता है उतना-उतना ही परमात्मा-सामर्थ्य उसमें निखरता है।
केवल सरलता के बल से सब काम नहीं हो जाते। मूर्खों के आगे, पामर आदमियों के आगे अति सरल बन जाओ तो वे तुम्हारी सरलता का दुरूपयोग करने लग जाएँगे।
कहाँ सरल बनना और कहाँ कठोर बनना, कहाँ दान करना और कहाँ संग्रह करना, किससे विनम्र होकर काम करवाना और किसको आँख दिखाकर उसकी उन्नति करना यह वेदान्त के रहस्य को जानने वाले लोग ठीक से जानते हैं। वेदान्त का रहस्य जानने वाले लोग वे ही होते हैं जिनको भगवान बुद्धियोग देते हैं।
श्रीरामचन्द्रजी जानते थे कि टेक्स (कर) कितना और कैसे लेना चाहिए, संग्रह कब करना चाहिए। किसको कड़ा दण्ड देना चाहिए और किसको केवल लाल आँख दिखानी चाहिए, किसके आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए और किसके केवल मुस्कान से काम चलाना चाहिए। रामचन्द्रजी जानते थे, श्रीकृष्ण जानते थे, जनक जानते थे और जो भी ब्रह्मवेत्ता संत हैं वे जानते हैं। इसीलिए उनके द्वारा हम लोग उन्नत होते हैं। जिनको बुद्धियोग मिला है उनके संपर्क में आने से भी हमें बुद्धियोग का कुछ प्रसाद मिल जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
साधना
में सत्संग की
आवश्यकता
जप, तप, व्रत, उपवास, ध्यान, भजन, योग आदि साधन अगर सत्संग के बिना किये जायें तो उनमें रस नहीं आता। वे तो साधन मात्र हैं। सत्संग के बिना वे व्यक्तित्व का सिंगार बन जाते हैं।
जब तक ब्रह्मवेत्ता महापुरूष का जीवंत सान्निध्य इन साधनों का सुहावना नहीं बनाता तब तक ये साधन श्रम मात्र रह जाते हैं। ये साधन सब अच्छे हैं फिर भी सत्संग के बिना रसमय नहीं बनते। सत्संग इनमें रस लाता है।
रसौ
वै सः।
रस स्वरूप परमात्मा का बोध ब्रह्मवेत्ता अनुभवनिष्ठ महापुरूष की वाणी का शरण लिए बिना नहीं हो सकता। अकेले साधन-भजन करने से थोड़ी-बहुत सात्त्विकता आ जाती है, सच्चाई आ जाती है, साथ ही साथ सात्त्विकता और सच्चाई का अहं भी उतना ही आ जाता है। साधना का अहं खड़ा हो जाता है। अहं के अनुरूप घटना घटती है तो सुख होता है। अहं के प्रतिकूल घटना घटती है तो सुख होता है। अहं के प्रतिकूल घटना घटती है तो दुःख होता है। सुखी और दुःखी होने वाले हम मौजूद रहे।
सत्संग से क्या लाभ होता है ? हमारा माना हुआ जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व है, जीव का अहं है उसका पोल खुल जाता है। जैसे प्याज की पर्तें उतारते जाओ तो भीतर से कुछ ठोस प्याज जैसा निकलेगा नहीं। केवल पर्तें ही पर्तें है। ऐसे ही जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक 'मैं' का ठोसपना दिखता है। सत्संग मिलते ही 'मैं' की पर्तें हटती हैं और अपने चिदाकाश स्वरूप का दीदार हो जाता है। जीव मुक्ति का अनुभव कर लेता है।
एक साधु ने 'कलिदोषनिवारक' ग्रन्थ में पढ़ा कि साढ़े तीन करोड़ नाम जपने से सद्योमुक्ति होती है। उसने अनुष्ठान शुरू किया। साढ़े तीन करोड़ राम नाम का जप कर लिया। कुछ हुआ नहीं। दूसरी बार अनुष्ठान किया। फिर भी सद्योमुक्ति जैसा कुछ नहीं हुआ। जिन सत्पुरूष के द्वारा उस ग्रन्थ की बात सुनी थी उनको जाकर कहाः
"महाराज ! मैंने साढ़े तीन करोड़ जप दो बार किये। कुछ हुआ नहीं।"
तीसरी बार कर। संत ने सूचन किया।
तीसरी बार करने पर भी सद्योमुक्ति का कोई अनुभव नहीं हुआ। उनकी श्रद्धा टूट गई। फिर किसी ब्रह्मवेत्ता के पास गया और अपना हाल बताते हुए कहाः
"स्वामी जी ! सुना था कि साढ़े तीन करोड़ मंत्रजप करने से सद्योमुक्ति होती है। मैंने एक बार नहीं, तीन बार किया। मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ।"
"सद्योमुक्ति का मतलब क्या है ?" संत श्री ने पूछा।
"शीघ्र मुक्ति। सद्यो मोक्षप्रदायकः। तुरन्त मुक्ति हो जाती है।"
"वत्स ! तू मनमाना होकर साधना करता था इसलिए अटूट दृष्टि नहीं रही। तू अभी मुक्त है, इसी समय तू मुक्त है। तुझे बाँध सके ऐसी कोई भी परिस्थिति तीनों लोकों में भी नहीं है। तू अभी मुक्त है। तूने जप तो किया लेकिन सत्संग का रंग नहीं लगा। अब सत्संग में बैठकर देख। दीये में तेल तो भर दिया, बाती भी रख दी लेकिन जले हुए दीये के नजदीक नहीं गया। अब सत्संग में बैठ। शान्ति से ध्यानपूर्वक सुन। श्रद्धा के साथ विचार कर। तेरी सद्योमुक्ति है ही। 'मेरी सद्योमुक्ति अब होगी' – ऐसा मत मान। अभी इसी समय, यहीं तेरी सद्योमुक्ति है। हम लोग बड़े में बड़ी गलती यह करते हैं कि साधनों के बल से भगवान को पाना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं। साधन करने वाले का व्यक्तित्व बना रहेगा। केवल भगवान की कृपा से भगवान को पाना चाहते हैं तो आलस्य आ जायेगा। अतः तुम्हारा पुरूषार्थ और भगवान की कृपा का समन्वय कर। 'भगवान ऐसे हैं.... वैसे हैं' ऐसी मान्यता मत पकड़। वे जैसे हैं उसी रूप में अपने आप प्रकट हों।"
तुम्हारी धारणा के मुताबिक भगवान प्रकट हों ऐसा चाहोगे तो तुम्हारी धारणा कभी कैसी होगी कभी कैसी होगी। मुसलमान खुदा को चाहेगा तो अपनी धारणा का, वाघरी भगवान को चाहेगा तो अपनी धारणा का, रामानुजाचार्य के भक्त भगवान को चाहेंगे तो अपनी धारणा का, देवी का भक्त अपनी धारणा का चाहेगा, पटेल अपनी धारणा का भगवान चाहेगा, सिंधी अपनी धारणा का झूलेलाल चाहेगा।
तुम्हारी धारणा के भगवान तो तुम्हारी अन्तःकरण की वृत्ति तदनुकूल होगी तो वही होकर दिखेंगे। तुम्हारी वृत्ति माता के आकार की होगी तो भगवान माता के स्वरूप में दिखेंगे, तुम्हारी वृत्ति श्रीरामचन्द्रजी के आकार की होगी तो भगवान रामचन्द्र जी के रूप मे दिखेंगे। तुम्हारी वृत्ति झुलेलाल के आकार की होगी तो भगवान झुलेलाल के स्वरूप में दिखेंगे। ऐसे भगवान दिखेंगे और फिर अन्तर्ध्यान हो जायेंगे।
उन महापुरूष ने साधू को कहाः "तू सत्संग में आ तब तुझे भगवत-रस की प्राप्ति होगी, इसके बिना नहीं होगी।"
यही घटना बिल्ख के सम्राट इब्राहीम के साथ हुई। वह राजपाट छोड़कर भारत में आया और संन्यास ले लिया। मजदूरी करके, लकड़ियाँ बेचकर दो पैसे कमा लेता। एक पैसे से गुजारा करता, एक पैसा बच जाता। जब ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते तब साधुओं को भोजन करा देता। कहाँ तो बिल्ख का सम्राट और कहाँ लकड़हारा होकर परिश्रम करने वाला फकीर !
इब्राहीम के मन में आया कि, "मैं दान का नहीं खाता। इतना बड़ा राज्य छोड़ा, संन्यासी बना, फिर भी किसी के दान का नहीं खाता हूँ, अपना कमाकर खाता हूँष ऊपर से दान भी करता हूँ। फिर भी मालिक नहीं मिल रहा है, क्या बात है ?" वह प्रार्थना करने लगताः
"हे मेरे मालिक ! हे मेरे प्रभु ! हे भगवान ! हे खुदा ! हे ईश्वर ! मुझे कब मिलोगे ? मैं नहीं जानता कि आप कैसे हो। आप जैसे भी हो, मुझे सन्मार्ग दिखाओ।"
ऐसी प्रार्थना करते-करते ध्यानस्थ होने लगा। अंतर में प्रेरणा मिली कि, "जा ऋषिकेश के आगे। वहाँ अमुक संत हैं उनके पास जा।" बिल्खनरेश वहाँ पहुँच गया और बोलाः
"बाबाजी मैं बिल्ख का सम्राट था। राजपाट छोड़कर फकीर बना हूँ। अभी मेरा अहं नहीं छूटता। मैंने सुना है कि अहं मिटते ही मालिक मिलता है। पहले मैं राजा था ऐसा अहं था। फिर फकीर का अहं घुसा। अहं निकालने के लिए परीश्रम करके खाता हूँ, संग्रह न करके त्याग करता हूँ, बचा हुआ वित्त भंडारे में खर्च कर देता हूँ। पसीना बहाकर अपना अन्न खाता हूँ फिर भी मालिक क्यों नहीं मिलता ?"
बाबाजी ने कहाः "यह अपना खाने वाला" और "पराया खाने वाला" ही अड़चन है। मेरा और तेरा, अपना और पराया जो बनाता है वह अहं ही मालिक के दीदार में अड़चन है।"
सम्राट ने कहाः "महाराज ! मेरा वह अहं आप निकाल दीजिये। इतनी कृपा कीजिये।"
बाबाजी ने कहाः "हाँ, ठीक तू समझा है। अहं है तेरे पास ?"
"हाँ अहं है। वही दुष्ट परेशान कर रहा है।"
"तो देखो, कल प्रभात में चार बजे आ जाना। मैं तेरा अहं ले लूँगा।"
"जी महाराज !"
अनुभव-संपन्न ब्रह्मवेत्ता महापुरूष थे। सिद्धि के ऊँचे शिखर सर किये थे।
इब्राहीम जाने लगा। बाबाजी ने पीछे से कहाः "देख, अहं लाना, पूरा। कहीं आधा छोड़कर नहीं आना।"
इब्राहीम चकित रह गयाः "अहं छोड़कर कहाँ आऊँगा ? वह तो पूरे का पूरा साथ में रहता है।"
दूसरे दिन प्रभात में चार बजे इब्राहीम पहुँच गया बाबाजी के गुफा पर। बाबाजी डण्डा लेकर आये। बड़ी-बड़ी आँखे दिखाते हुए बोलेः "अहं लाया है ?"
"हाँ महाराज ! अहं है ।"
"कहीं छोड़कर तो नहीं आया ?"
"ना महाराज !"
"कहाँ है ?"
"हृदय में रहता है।"
"बैठ। निकाल उसको, मेरे को दिखा, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। जब तक अहं को निकालकर मेरे सामने नहीं रखा तब तक उठने नहीं दूँगा। इस डण्डे से सिर फोड़ दूँगा। तू सम्राट था तो उधर था। इधर अभी तेरा कोई नहीं। यहाँ बाबाओं के राज्य की सीमा में आ गया है। सिर फोड़ दूँगा अहं दिये बिना गया तो। देना है न अहं ? तो खोज, कहाँ है अहं ?"
"कैसे खोजूँ अहं को ? वह कहाँ होता है ?"
"अहं कहाँ होता है – ऐसा करके भी खोज। जहाँ होता है वहाँ से निकाल। आज तेरे को नहीं छोड़ूँगा।"
ज्यों
केले के पात
में पात पात
में पात।
त्यों
संतन की बात
में बात बात
में बात।।
कभी साधक का ताड़न करने से काम बन जाता है कभी पुचकार से काम हो जाता है। कभी किसी साधन से कभी किसी साधन से....। ये तो महापुरूष जानते हैं कि कौन से साधक की उन्नति किस प्रकार करनी चाहिए।
युक्ति से मुक्ति होती है, मजदूरी से मुक्ति नहीं होती।
इब्राहीम अहं को खोजते-खोजते अन्तर्मुख होता गया। प्रभात का समय। वातावरण शुद्ध था। बाबाजी की कृपा बरसती रही। मन की भाग दौड़ क्षीण होती गई। एक टक निहारते निहारते आँखें बन्द हुई। चेहरे पर अनुपम शांति छाने लगी। ललाट पर तेज उभरने लगा। डण्डे वाला बाबाजी तो गुफा के भीतर चले गये थे। डण्डा मारना तो था नहीं। जो कुछ भीतर से करना था वह कर दिया। इब्राहीम की सुरता की गति अन्तर्मुखी बना दी।
इब्राहीम को अहं खोजते-खोजते साढ़े चार बजे, पाँच बजे, छः बज गये। बैठा है ध्यानस्थ। बाहर का कोई पता नहीं। श्वासोच्छ्वास की गति मंद होती चली जा रही है।
सूर्योदय हुआ। सूर्य का प्रकाश पहाड़ियों पर फैल रहा है। अपने आत्मा का प्रकाश इब्राहीम के चेहरे पर दिव्य तेज ले आया है। बाबाजी देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि साधक ठीक जा रहा है।
घण्टों के बाद बाबाजी इब्राहीम के पास गयेः
"उठो उठो अब।"
इब्राहीम ने आँख खोली और चरणों में गिर पड़ा।
"अहं दे दो।"
"गुरू महाराज !....."
इब्राहीम के हृदय में भाव उमड़ रहा है लेकिन वाणी उठती नहीं। आँखों से भावविभोर होकर गुरू महाराज को निहार रहा है। विचार स्फुरता नहीं। आखिर बाबाजी ने उसकी बहिर्गति कराई। फिर बोलेः
"लाओ, कहाँ है अहं ?"
"महाराज ! अहं जैसी कोई चीज है ही नहीं। बस वही वह है। वाणी वहाँ जाती नहीं। यह तो आरोप करके बोल रहा हूँ।"
बाबाजी ने इब्राहीम को गले लगा लिया। "इब्राहीम ! तू गैर नहीं। तू इब्राहीम नहीं। तू मैं है, मैं तू हूँ।"
जब तक अहं को नहीं खोजा था तब तक परेशान कर रहा था। खोजो तो उसका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रहता। आँख देखती है, हम जुड़ जाते हैं- "मैंने देखा।"
मनःवृत्ति शरीर के तरफ बहती है तो अहं बना देती है और अपने मूल के तरफ जाती है तो मन रहता ही नहीं। जैसे तरंग उछलती है तो अलग बनी रहती है और पानी को खोजती है तो शान्त होकर पानी बनकर रह जाती है, अलग अस्तित्व मिट जाता है। ऐसे ही 'मैं.... मैं..... मैं.... मैं....' परेशान करता है। वह 'मैं' अगर अपने मूल को खोजता है तो उसका परिच्छिन्न अहं मिलता ही नहीं।
तीन प्रकार का अहं होता हैः स्थूल अहं, सदगुरू की शरण से विलीन होता है। सूक्ष्म अहं वेदान्त के प्रतिपादित साधन की तरकीब से बाधित होता है। तीसरा है वास्तविक अहं, वह ब्रह्म है, परम सुख-स्वरूप है। उसी में अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड फुरफुरा के लीन हो रहे हैं।
वास्तविक हमारा जो 'मैं' है उसमें अनन्त अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, स्थित रहती हैं और लय हो जाती हैं। फिर भी हमारा बाल भी बाँका नहीं होता। हमारा वास्तविक अहं वह है। अपनी वास्तविकता का बोध नहीं है तो वहाँ की एक तरंग, एक धारा, एक वृत्ति को 'मैं' मानकर उलझ रहे हैं। उलझते-उलझते सदियाँ बीत गईं लेकिन विश्रांति नहीं मिली।
बिना सत्संग के साधन-भजन भीतर व्यक्तित्व को सजाये रखता है। 'पहले मैं संन्यासी था, अब मैं साधक हूँ। पहले मैं भोगी था, अब मैं त्यागी हूँ। पहले बहुत बोलनेवाला था, अब मौनी हूँ। पहले स्त्री-पुत्र-परिवार के चक्कर में था, अब अकेला शांत हूँ। कमरा बन्द कर देता हूँ बस, मौज है। न किसी से लेना न किसी को देना।'
खतरा पैदा करोगे। जो अकेले कमरे में नहीं बैठते, एकान्त में नहीं रहते उनकी अपेक्षा आप ठीक हो। लेकिन जब कमरा न होगा, एकान्त न होगा तब परेशानी चालू हो जायेगी। ....और मौत तुम्हें कमरे से भी तो पकड़कर ले जायेगी।
जीते जी मौत के सिर पर पैर रखने की कला आ जाना-इसी का नाम आत्म-साक्षात्कार है। साक्षात्कार होने से राग-द्वेष और अभिनिवेश का अत्यंत अभाव हो जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से लगाव नहीं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से लगाव नहीं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से घृणा नहीं, द्वेष नहीं। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, जीने की आस्था। आत्म-साक्षात्कार हो जाता है तो जीने की आकांक्षा हट जाती है। जिसको अपने आपका बोध हो जाता है वह जान लेता है कि मेरी मौत तो कभी होती नहीं। एक शरीर तो क्या, हजारों शरीर लीन हो जायें, पैदा हो जायें, ब्रह्माण्डों की उथल-पुथल हो जाय फिर भी मुझ चिदाकाश स्वरूप को कोई आँच नहीं आती, ऐसा अपनी असली 'मैं' का साक्षात्कार हो जाता है।
देह
छतां जेनी दशा
वर्ते
देहातीत।
ते
ज्ञानीना
चरणमां हो
वन्दन
अगणित।।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
राजा
से मुलाकात
इच्छापुर नगर में रामू नाम का एक सज्जन रहता था। यह शास्त्री जी महाराज से संस्कृत पढ़ा, शास्त्रों का ज्ञान सीखा, स्कूली विद्या भी पढ़ी। साथ ही साथ उसने अपने अन्दर नम्रता, सरलता, सहजता और भगवान की भक्ति के गुण भी विकसित किये थे। उसकी बुद्धि में विशेष प्रकाश हुआ था।
रामू का एक मित्र था, कन्हैया। इच्छापुर नरेश के दीवान के पेशकार के वहाँ कन्हैया बर्तन माँजता था। एक सुबह रामू नहा-धोकर कन्हैया के घर पहुँचा। कन्हैया सोया हुआ था। रामू ने जाकर कन्हैया के पैर पकड़े और कहाः
"कन्हैया ! तू धन्य है.... धन्य है.....!"
कन्हैया चौंक उठा। बोलाः "मित्र ! यह क्या कर रहे हो ? तुम तो प्रातः जल्दी नहा धोकर यहाँ पहुँच गये और मैं तो अभी सो रहा था। मुझे तुम धन्य-धन्य मान रहे हो ? मेरी मजाक उड़ा रहे हो दोस्त !"
"नहीं कन्हैया ! मैं मजाक नहीं करता। तुम कैसे धन्य हो, सुनो। इच्छापुर नगर के राजा साहब योगी है, ज्ञानी हैं, परम भक्त है, परोपकारी हैं, वास्तव में सत्पुरूष हैं। जीवन्मुक्त महात्मा ही राजा बनकर राज्य चला रहे हैं। दीवान उनके सान्निध्य में कारोबार सँभाल रहे हैं। ऐसे महाभाग्यवान दीवान साहब के साथ पेशकार साहब को काम करने का मौका मिला है। ऐसे पेशकार साहब की सेवा में तुम हो। तो तुम भाग्यवान हुए कि नहीं ? इसीलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। दासों का भी जो दास है, उसका भी जो दास है वह भी मेरे लिए वन्दनीय है, पूजनीय है।"
"भैया रामू ! इसमें मेरा क्या बड़प्पन है ? राजा साहब तो सचमुच नारायण के स्वरूप हैं और उनके साथ उठने-बैठने वाले दीवान साहब भी भाग्यवान हैं, धन्य हैं। ऐसे दीवान साहब के संपर्क में रहने वाले पेशकार साहब भी वन्दनीय हैं लेकिन मैं तो रहा उनका बर्तन माँजने वाला। मैं धन्य कैसे ?"
"भाई ! कैसे भी हो, तुम उनके नजदीक तो जा सकते हो न ? तुम भी मेरे लिये धन्य हो।
भैया ! अब मैं संसार की नौकरी से थका हूँ। घर का गुजारा तो चल जाता है। पत्नी भी परिश्रम करती है, तीन बीघा जमीन है, तीन गायें हैं, दो भैंसे हैं। परिवार का लम्बा विस्तार नहीं है। अब मुझे अपने आपकी आवश्यकताएँ पूरी करनी हैं। इसलिए तुम मुझे अपनी सेवा दे दो।"
"अरे अरे ! मैं तो बर्तन माँजने वाला ! मेरी सेवा ?"
"हाँ हाँ तुम्हारी सेवा। मुझे तनख्वाह आदि कुछ नहीं चाहिए। केवल सेवा ही चाहिए। लाओ मैं तुम्हारे बर्तन माँज दूँ। तुम्हारे बर्तन न दो तो पेशकार साहब के वहाँ तुम्हारी सहाय करने दो। वहाँ पेशकार साहब के दर्शन होंगे जो राजा साहब के बिल्कुल निकट रहने वाले दीवान साहब के दर्शन करते हैं। दर्शन करने वालों के दर्शन करके मैं धन्य बनूँगा।"
"अरे दोस्त ! पेशकार साहब के दर्शन करने हों तो आज ही चलो। इसमें मेरे बर्तन माँजने की क्या जरूरत है ? चलो.... चलो.....।"
कन्हैया रामू को ले गया पेशकार के वहाँ। पेशकार ने पूछाः "यह कौन है ?"
"मेरा मित्र है रामू। आपके दर्शन करने आया है। सेवा में मुझे सहाय करेगा।"
रामू ने झट से बर्तन उठाये, माँज दिये। बुहारी लगा दी। कुर्सी टेबल आदि सब साफ-सुथरा कर दिया। पेशकार उसकी स्फूर्ति और उत्साह देखता ही रह गया। दोपहर होते-होते उसका चित्त रामू से प्रभावित हो गया। वह रामू से बोलाः "रामू ! तुम अगर यहाँ रहना चाहो तो रहो।"
"आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी दया है पेशकार साहब ! मैं तो चाहता था कि मुझे कन्हैया की सेवा मिल जाय तो भी काफी है। उसके बहाने आपके दर्शन कर सकूँगा। मुझे अब सीधी आपकी सेवा मिल रही है यह आपकी उदारता है।"
रामू ने पन्द्रह दिन, महीना काम किया। पेशकार ने तनख्वाह देना चाहा तो रामू ने इन्कार कर दियाः
"साहब ! मैं तनख्वाह के लिए नहीं आया। आप रोज दीवान साहब के दर्शन करते हैं। आप पवित्रात्मा है। मैं तो आपके दर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूँ और कभी न कभी आपकी कृपा से मुझे दीवान साहब के दर्शन भी हो जायेंगे। मुझे पैसे-वैसे नहीं चाहिए।"
"अरे ! दीवान साहब के दर्शन करने हैं तो आज ही चलो। बाद की क्या बात है ? ऐसा करो, मैं जाता हूँ। दीवान साहब आते हैं ग्यारह बजे। मैं जाता हूँ दस बजे और सब तैयारियाँ करता हूँ। मेरा दोपहर का भोजन तुम ले आना। दीवान साहब की ऑफिस में दीवान साहब के दर्शन हो जायेंगे।"
रामू दोपहर का भोजन ले गया, पेशकार साहब के सामने रख दिया और दीवान साहब के तरफ एकटक नजर से देखने लगा। निगाहों में प्यार उमड़ रहा है, हृदय में खुशी हो रही है कि "जीवन्मुक्त महापुरूष राजा साहब के प्रत्यक्ष सान्निध्य में जाने वाले दीवान साहब को मैं देख रहा हूँ ! धन्य... धन्य...... !! मैं कृत्कृत्य हो रहा हूँ। वाह.... वाह....!!!"
चित्त में अहोभाव भरने से, हृदय में प्रीति भरने से सामने वाले व्यक्ति का भी प्रेम मिलने लगता है। दीवान की नजर गई कि यह कैसा लड़का है ? बार-बार स्नेहपूर्वक निहारता है, खुश हो रहा है ! पूछाः
"कौन है यह युवक ?"
"यह कन्हैया का मित्र है।"
"बेटा ! इधर आ जा।"
रामू तो 'बेटा' शब्द सुनकर गदगद हो गया कि, "महाराज ! आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इस दीदार के लिए मैं वाञ्छा करता था, कन्हैया के पैर पकड़ता था और पेशकार साहब कृपा करके मुझे यहाँ ले आये और आप...."
रामू का हृदय भाव से भर आया। वाणी रूक गई।
दीवान ने पेशकार को कहाः "रामू अगर मेरी सेवा में रहे तो तुम्हें कोई हरकत नहीं ?"
"नहीं नहीं साहब ! कोई हरकत नहीं। आप ही रख लीजिए। रामू ! रहेगा न ?"
"अरे महाराज ! मेरे भाग्य में चार चाँद लग गये।"
रामू दीवान साहब के वहाँ काम करने लगा। दीवान उठे उसके पहले रामू उठ जाता। बड़े चाव से सेवा करता। दीवान ने एक दिन कहाः "तुम्हारे घर पैसे-वैसे चाहिए तो भेज दूँ। तेरी आय का कुछ साधन बना दूँ।"
"महाराज ! घर पर आय के साधन हैं, गुजारा चलता है बस। इस नश्वर देह को जो खाना चाहिए वह मिल जाता है। जैसा जीना चाहिए ऐसा जी लेता है। अधिक आसक्तियाँ बढ़ाकर भगवान से च्युत होने में कोई सार नहीं। जीवन्मुक्त सत्पुरूष राजा साहब के निकट सान्निध्य में जाने वाले आप जैसों का सान्निध्य मिल रहा है, यही मेरे लिए सच्चा धन है।"
"फिर भी तू अपने गाँव का पता बता दे दे। मैं कुछ न कुछ वहाँ भेज दूँगा।" दीवान साहब की प्रसन्नता बढ़ रही थी।
"नहीं महाराज ! वह मेरा गाँव नहीं, वह तो शरीर का गाँव है। मेरा गाँव तो.... जहाँ राजा जी का गाँव है वही मेरा गाँव है। काश, मुझे उस अपने गाँव का पता चल जाय। इच्छापुर नरेश के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, आप कितने पवित्र हैं। कितने महान हैं ! मेरा भी कोई दिन आयेगा कि मैं भी उन महापुरूष के दर्शन कर सकूँगा।"
"राजा साहब के दर्शन करने हैं तो आज ही दर्शन करा दूँ बेटे ! चिन्ता की क्या बात है ? देख, मैं जाता हूँ राजा साहब के वहाँ। वे दोपहर को एक बजे पधारते हैं। आज एकादशी है। तू दो बजे मेरा फलाहार वहाँ ले आना। राजा साहब के दर्शन हो जाएँगे।"
रामू पहुँच गया वहाँ। राजा की दृष्टि पड़ी। पूछाः
"यह कौन है नया सेवक ?"
"महाराज जी ! आप का ही सेवक है, रामू।"
रामू पलकें गिराये बिना राजा साहब को एकटक निहार रहा है। रामू की प्रीति इतनी बरस रही है कि राजा महत्त्वपूर्ण कागजात पर दस्तखत करते-करते भी रामू की चेष्टाएँ निहार लेते हैं। रामू ठीक चाकरी करते-करते बार-बार प्यारपूर्ण दृष्टि से राजा साहब की ओर झाँक लेता है। दोनों की नजरा नजरा हुई। नजर तो दो हैं लेकिन प्रेम तो दोनों में एक ही छलकता है। भेद में भी अभेद का आनन्द आने लगा। राजा ने रामू का हाल-अहवाल पूछकर सब जान लिया। फिर दीवान से पूछाः
"यह लड़का अगर मेरी सेवा में..."
"हाँ हाँ महाराज ! आप ही रख लीजिए। बड़ा सज्जन लड़का है। बड़े चाव से उत्साहपूर्वक सेवा करता है।"
"बेटे ! मेरे पास रहेगा ?"
"महाराज ! मैं तो आपके दर्शन के लिए कई वर्षों से छटपटाता था और अब आपके पास रहने को मिलेगा ! अहोभाग्य !"
रामू लग गया राजा साहब की सेवा में। बड़ी तत्परता और आदर के साथ काम करने लगा। झाड़ू भी लगाये तो राजा को प्रसन्न करने के लिए और रसोईघर में काम करे तो भी राजा को प्रसन्न करने के लिए।
राजा उसे ले गये अपने महल में। रानी को दिखाया कि, "यह रामू नाम का लड़का है। बड़ी प्रीतिपूर्वक काम करता है। बहुत अच्छा है। मुझे तो बेटे जैसा लगता है। तेरे को कैसा लगता है ?"
रामू ने मातृभाव से, साक्षात् जगदम्बा मेरी माँ है ऐसा भाव करके माताजी को निहारा, विनयपूर्वक प्रणाम किये। माता जी के मुँह से भी उदगार निकल पड़ेः "बेटे ! यह तेरा घर ही है। प्रेम से रह। जो कुछ आवश्कता हो, अपना घर समझकर ही उपयोग कर। राजा साहब को दूध-नास्ता, भोजन आदि सब तू ही पहुँचाया कर। मुझसे अब ज्यादा काम होता नहीं और दासियों की सेवा राजा साहब को पसन्द भी नहीं है। अब तू ही हमारी अन्तरंग सेवा करना। तू हमारा पुत्र है बेटे !"
"माँ ! मैं आपकी शरण हूँ। पिता जी ! मैं आपका ही पुत्र हो गया।"
"हाँ बेटे हाँ।"
चार पैसे की चाकरी करने की जगह से रामू अपने गुणों के कारण राजा का पुत्र हो गया। कुछ ही दिनों में अपनी अनुनय सेवा से राजा-रानी का दिल जीत लिया। राजा के सब कार्यों में सहायक बनते-बनते रामू निपुण हो गया।
एक दिन राजा ने कहाः "बेटा रामू ! मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। राज कारबार से अब निवृत्त होकर आत्म-विश्रान्ति लेना चाहता हूँ। तुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके राज्यतिलक कर दें तो कैसा ?"
"महाराज ! नहीं.... नहीं....। मैं राजगद्दी का अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ। मुझे सेवा ही मिले तो अच्छा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।"
अपनी इच्छाएँ जितनी निवृत्त थीं उतना ही रामू राजा का कृपापात्र होता गया। आपको जो प्यार करता है वह आपको कुछ न कुछ दिये बिना नहीं रहता। हम लोग संत महात्मा सदगुरू के चरणों में फल-फूल, चीज वस्तु, मेवा-मिठाई रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि संत-महात्मा भूखे मर रहे हैं, हम दया करके देते हैं। नहीं.....। हम उनसे प्यार करते हैं और प्यार में कुछ न कुछ दिये बिना रहा नहीं जाता। हम लोगों के पास साधकों और भक्तों के पास संसार की चीजें हैं तो यही चीजें धरते हैं और संत महात्मा सदगुरू परमात्मा के पास अपना दिव्य आत्म अनुभव है। वे घुमा फिरा के वही अपना अनुभव देते हैं, हमें भी उस अनुभव में जगाते हैं, अपने आपसे मुलाकात कराते हैं। .....और हम घुमा-फिराके अपना संसार उन्हें देते हैं। प्रेम में ऐसा होता रहता है।
भक्त प्यार करता है। प्यार में वस्तुएँ दी जाती हैं। भगवान प्रेम करते हैं, संत महात्मा-सदगुरू परमात्मा प्रेम करते हैं। प्रेम में अपना आपा दिया जाता है।
रामू कहता हैः "महाराज ! मैं तो आपको प्यार करता हूँ और आप बदले में प्रेम कर रहे हैं। आप अपना सर्वस्व दे रहे हैं। मैं आपके सर्वस्व का अधिकारी नहीं। मैं तो आपकी सेवा का अधिकारी हूँ।"
"रामू ! तू चाहे न मान। लेकिन तेरे जैसा पुत्र मैं और कहाँ से लाऊँगा ? दैवयोग से देव ने हमारी गोद भर दी रामू !"
"महाराज ! आप अगर देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए।"
"एक क्या दो माँग ले। बोल क्या चाहिए ?"
"महाराज ! मैं कभी भी आपसे दूर नहीं रहूँ। सदा साथ ही रहूँ।"
"साथ तो रहता ही है। और कुछ माँग ले।"
"नहीं महाराज ! इतना ही पर्याप्त है।"
"अच्छा मेरे साथ ही रह सदा के लिए बस ? रामू ! मेरे मन में विचार आया कि मैं तुझे उत्तराधिकारी घोषित करके राजतिलक कर दूँ। जीवन का बुढ़ापा है। जाकर अरण्य में एकान्तवास करूँ। इन्द्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को निज-स्वरूप परमात्मा में लगाकर जीवन्मुक्त होकर परमात्म-पद को पा लूँ।"
"महाराज ! आप मुझे वचन दे चुके हैं। राज्य मुझे देकर आप अकेले एकान्त में कैसे जाएँगे ? मैं भी आपके साथ चलूँगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए।"
"वचन दे चुका हूँ तो अब मैं अपनी बात को बदलता हूँ। सुन। राज्य का भार तू वहन कर। मैं तेरे साथ रहूँगा।"
हाँ ना करते रामू का राज्याभिषेक हो गया। राजा उसके साथ रहकर राज्य की व्यवस्था कराने लगे। सब गतिविधियों में रामू को तालीम देते हुए अपने जैसा ही प्रजाहितकारी शासक बनाने लगे।
यह तो एक कल्पित कथा है। इस कथा में अब सिद्धान्त ले आओ। रामू एक जीव है जो प्रीतिपूर्वक भगवान का दीदार करना चाहता है। राजा की जगह पर बुद्धि के प्रकाशक ईश्वर, सच्चिदानंदघन परमात्मा है। दीवान की जगह पर बुद्धि है। पेशकार की जगह पर मन है। कन्हैया की जगह पर इन्द्रियाँ हैं। साधक की जगह पर रामू है। इन्द्रियों को समझाकर मन तक पहुँचा, मन को रिझाकर बुद्धि तक पहुँचा, बुद्धि को प्रसन्न करके आत्मा-परमात्मा तक पहुँचा। राजा परमात्मा है और राजा की रानी परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति है, भगवान की महामाया है। जो भगवान को प्यार करता है, भगवान की महामाया उसे अपना पुत्र समझकर भगवान से मिलाने में राजी रहती है। जो भगवान को प्यार न करके माया से कुछ नोचना चाहता है उसे महामाया भी नौकर समझकर चलाती रहती है, मजदूरी कराती रहती है। उसे पुत्र नहीं बनाती। भगवान को प्यार करता है उसे भगवान की लक्ष्मी भी गोद में उठाकर उसकी उन्नति करती है।
भगवान को प्यार नहीं करते तो महालक्ष्मी नहीं आती, वित्त आ सकता है। वित्त यानी धन। धन तो आता है, धन से सुविधाएँ मिलती हैं। सुविधाओं से अहंकार बढ़ता है। सुविधाओं से वासनाएँ भड़कती हैं, सुविधाओं से पिस्तौल के लाइसेन्स लेने की इच्छा होती है, सुविधाओं से इधर का उधर और उधर का इधर करने की इच्छा होती है। सुविधाओं से बम बनाने का आयोजन होता है। भगवान में जब प्रीति होती है तो आदमी निश्चिंत जीवन जीता है।
ददामि
बुद्धियोगं
तं येन
मामुपयान्ति
ते।
जिसको भगवान की ओर से बुद्धियोग मिलता है वह कन्हैया की शरण लेकर पेशकार तक पहुँचता है, पेशकार को रिझाकर दीवान तक पहुँचता है, दीवान के सहारे राजा साहब के पास आ जाता है। राजा साहब उसका त्याग नहीं करते। राजा साहब उसका राजतिलक कर देते हैं, वह पूजा जाता है, माना जाता है। राजा साहब उसको छोड़कर अरण्य में जाते नहीं। रामू भी ऐसा चतुर होता है कि वह भी राजा साहब को सदा अपने साथ रखकर राज्य करता है। इसलिए वह महाराज हो जाता है।
ऐसे कई रामूओं को मैं जानता हूँ जो महाराज हो गये हैं। वे तुच्छ राज्य नहीं करते, वे महान् राज्य करते हैं।
एक बार चाणक्य के घर सामुद्रिक लक्षण देखने वाले पण्डित जी आये। उस समय चाणक्य नन्हे-से थे। पण्डित जी ने बच्चे पर निगाह डाली और धन्यता व्यक्त करते हुए चाणक्य के पिता से बोलाः
"आपको भगवान ने कैसा अदभुत बालक दिया है ! सामुद्रिक विद्या के बल से मैं कहता हूँ कि आपका यह बेटा राजा होगा राजा। मेरी विद्या पर मुझे भरोसा है।"
उस शास्त्री जी ने सोचा कि यह समाचार सुनकर चाणक्य के पिता प्रसन्न हो जाएँगे। पिता प्रसन्न नहीं हुए, दुःखी हो गये कि अरे ! मेरा बेटा राजा बनेगा ? मैंने क्या पाप किया है ?
अपना बेटा अमेरिका जा रहा हो तो माँ-बाप खुश हो जाते हैं, अखबारों में फोटो छपवाते हैं। फिर चाहे वह अमेरिका में पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लग जाये।
भोगियों के देश में बेटा जाता है तो माँ बाप छाती फुलाकर गौरव का अनुभव करते हैं और हिमालय में योगियों के पास बेटा जाता है तो रोते हैं- "मेरा बेटा चला गया रे...."
दुनियाँ ने क्या उल्टा रंग लिया है ! किसी का बच्चा साधू बनता है तो आप उसके नतमस्तक हो जाते हैं, आदर करते हैं, उसका पैर छूते हैं। लेकिन आपका लड़का साधू बनता है तो आप रोते हैं। आप कितने चतुर लोग हैं..... ! कितने भोले महेश हैं....!
ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि हमारा मन इन्द्रियों के पक्ष में है। और पूरा समाज इन्द्रियों के पक्षवाला ही है। इन्द्रिय-जगत से ऊपर उठने वाले तो कोई-कोई विरले होते हैं।
हमारी माँ कथा सुनने को साधु-संतों के पास जाती थी। कथा सुनाने वाले वे साधु भी किसी के बेटे थे। हमारी माँ और कुटुम्बीजन उनको प्रणाम करते थे। हम जब साधू हुए तो वे ही लोग रोने लगे। ऐसे ही आप लोग मुझे प्रणाम करते हैं लेकिन आपका बेटा अगर साधू बनेगा तो आप रोना चालू कर देंगे।
आप क्यों रोते हैं ? क्योंकि अन्तःकरण की छोटी स्थितिवाले लोगों के बीच आप रहते हैं। 'अरे ! आपका बेटा साधू हो गया ? अररर...' जब आपका बेटा अमेरिका जाता है और साँस फुलाकर अखबार में छपा हुआ उसका फोटो लोगों को दिखाते हैं तो वे लोग प्रभावित हो जाते हैं। धन्यवाद देते हैं- "वाह ! बेटा अमेरिका जा रहा है ? बहुत अच्छा।"
अहंकार का पोषण होता है वहाँ आप खुश होते हैं और अहंकार मिटता है वहाँ आप नाराज होते हैं। जब बुद्धियोग मिलेगा तब अहंकार मिटने में आप राजी होंगे और अहंकार के पनपने में आप संकोच का अनुभव करेंगे। बुद्धियोग कब मिलेगा ?
तेषां
सतत
युक्तानां
भजतां
प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि
बुद्धियोगं
तं येन
मामुपयान्ति
ते।।
'उन निरन्तर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्त्वज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'
(भगवद् गीताः 10.10)
जब प्रीतिपूर्वक ईश्वर को भजोगे न, तो लड़का साधू बनेगा, ईश्वर के मार्ग में चलेगा तो आप खुश होंगे। 'मेरी गोद से बालक भगवान की ओर जा रहा है ! धन्य है !'
पावन
तेरा कुल हुआ
जननी कोख
कृतार्थ।
नाम
अमर तेरा हुआ
पूर्ण चार
पुरूषार्थ।।
बेटा राजा बनेगा यह सुनकर चाणक्य के पिता दुःखी हुए। पूछाः "महाराज ! कौन-से लक्षण से बेटा राजा बनेगा ?"
"इसका अमुक दाँत है न, वह लम्बा है। यह बताया है कि वह राजा बनकर ही रहेगा।"
पिता चाणक्य को ले गये कमरे में और उसका वह लम्बा दाँत कानस से घिस डाला। शास्त्री जी से बोलेः
"पण्डित जी ! बेटा राजा बनेगा तो इन्द्रियों के जगत में जीयेगा, भोग में, अहंकार में पुण्य का नाश करेगा। पुण्यों के बल से राजा बनेगा और भोगों से पुण्य खत्म करके नर्क का भागी बनेगा। तपेश्वरी राजेश्वरी... राजेश्वरी भोगेश्वरी.... भोगेश्वरी नरकेश्वरी...। मेरे घर में आने के बाद इसको नर्क में जाना पड़े तो धिक्कार है मेरे को बाप बनने में और धिक्कार है इसकी माँ को माँ बनने में। इसलिए महाराज ! मैंने इसका दाँत घिस डाला। अब बताओ, क्या होगा ?"
शास्त्री ने बताया किः "अब राजा तो नहीं बनेगा, राजाओं का गुरू बनेगा, महाराज बनेगा।"
रामू महाराज हो गया। राज्य में तो रहता था, लेकिन राज्य का कर्त्ता नहीं बनता था, राजा को साथ में रखता था। खुद केवल युवराज बना रहता था।
ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम संसारी मत बनो, संसार का व्यवहार करते समय अपने राजा को साथ में रखो। अपने प्रभु को साथ में रखो। जो कुछ करो उसमें प्रभु की प्रेरणा ले लो। जो कुछ कार्य पूरा हो जाये तब उन्हीं को समर्पित कर दो। प्रभु की ही सत्ता से बुद्धि को सत्ता मिली, बुद्धि की सत्ता से मन को चेतना मिली, मन से इन्द्रियों को मिली और इन्द्रियों से व्यवहार हुआ है। व्यवहार करने से पहले भी राम में आराम था, व्यवहार करने के बाद भी राम में आराम है। तो चालू व्यवहार में भी तुम थोड़ा अपने आपमें गोता मारते रहोगे तो तुम्हारा प्रीतिपूर्वक का व्यवहार भी सतत भजन हो जायगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
कुण्डलिनी
योग
जितने अंश में तुम्हारी प्राणशक्ति उन्नत है उतने अंश में तुम व्यवहार में, समाज में, स्वास्थ्य में उन्नत हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाँच तत्त्वों से यह शरीर बना है। इसका संचालन वायु तत्त्व से विशेष होता है। हमारे प्राण जितने सूक्ष्म होते हैं उतना हमारा मन बढ़िया होता है। प्राणशक्ति को जितनी-जितनी सूक्ष्मता होती है उतना-उतना योगी महान् हो जाता है। जिसने प्राणजय कर लिया वह योगी चाहे तो नक्षत्रों को, तारों को, चाँद और सूर्य को गेंद की तरह अपनी जगह से हिला सकता है। जिसने प्राणशक्ति पर विजय पा लिया वह अपने शरीर की आरोग्यता, मन की प्रसन्नता और बुद्धि की विलक्षणता में प्रवेश कर लेता है।
प्राणायाम प्राणशक्ति के विकास का एक नमूना है। जिनकी निगाहों से लोगों के चित्त में प्रसन्नता आ जाती है उन्होंने जाने या अनजाने प्राणशक्ति या मनःशक्ति की साधना की हुई है। इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिक्ख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या और कोई धर्म हो, उस धर्म के जो भी पीर, पैगम्बर, साधू, बाबा, फकीर, तीर्थंकर, भिक्षु आदि समाज में कुछ उन्नत हुए हैं उन्होंने जाने-अनजाने प्राणोपासना की है।
किसी वस्तु को एकटक देखते-देखते, शाम्भवी मुद्रा करते-करते मन रूका। मन रूकने से प्राण की गति रूकी और प्राणशक्ति का विकास हुआ। निष्काम भाव से सेवा करते-करते मन निर्वासनिक हुआ। मन निर्वासनिक होने से संकल्प-विकल्प कम हुए। संकल्प-विकल्प कम होने से प्राणशक्ति का विकास हुआ। आदमी उन्नत हुए।
सत्संग सुनते-सुनते, जगत की असारता विचारते-विचारते मन वासना रहित हुआ, प्राणशक्ति का विकास हुआ। व्यक्ति उन्नत हुआ।
हमारी सुषुप्त जीवन-शक्ति को चितिशक्ति कहते हैं, कुण्डलिनी शक्ति भी कहते हैं। यह शक्ति शरीर की नाभि के नीचे मूलाधार केन्द्र में सुषुप्त रहती है, सोयी पड़ी रहती है। ध्यान के द्वारा, संकल्प के द्वारा, कीर्तन के द्वारा हमारी प्राणशक्ति के धक्के उसको लगते हैं और वह जागृत होती है। हमारी नाड़ियों में जो विजातीय द्रव्य, मल आदि होता है उसका शोधन करती है। फिर प्राणोत्थान के प्रभाव से कुण्डलिनी शक्ति ज्यों-ज्यों ऊपर के केन्द्रों में आती है हमारे प्राण सूक्ष्म होते जाते हैं। हमें पता नहीं चलता इस बात का। जिन योगियों को पता चलता है वे शीघ्रता से साधना करते हैं। हमें पता नहीं चलता और स्वाभाविक थोड़ी-बहुत साधना होती है। हमारा प्राण जितने अंश में शुद्ध होता है, उन्नत होता है उतने अंश में हमारा चित्त प्रसन्न होता है, बुद्धि में दिव्यता आती है और संकल्प में सामर्थ्य आता है।
कीर्तन करते-करते लोग फिर ध्यान नहीं करते तो कीर्तन का विशेष लाभ नहीं उठा पाते। ध्यान करते-करते फिर आत्म-विचार नहीं करते तो ध्यान का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तुलसीदास जी कहाः
तन
सुकाय पिंजर
कियो धरे रैन
दिन ध्यान।
तुलसी
मिटै न वासना
बिना विचारे
ज्ञान।।
मनुष्य शरीर को सुखा दे, पिंजर बना दे, जब तक आत्मज्ञान का विचार नहीं करेगा तब तक आखिरी मंजिल पर नहीं पहुँचेगा। आखिरी मंजिल पर जाने के लिए बुद्धि को आध्यात्मिक बनाना ही पड़ेगा। बुद्धि को आध्यात्मिक बनाने के लिए नश्वर भोगों की पोल को जानना पड़ेगा और शाश्वत परमात्मा के रस की महिमा को जानना पड़ेगा। महिमा केवल सिद्धांतिक ही नहीं, ध्यान करके प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा।
मन जितना-जितना अन्तर आराम, अन्तर सुख और अन्तर ज्योत के तरफ जायगा उतना-उतना बाहर के विकारी सुख से हटेगा।
एक होता है इन्द्रियगत ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। इन्द्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच मन की वृत्ति काम करती है। आँख देखने का काम करती है। आँख ने एक आदमी दिखाया। मन ने कहाः यह ब्राह्मण है। बुद्धि ने कहाः यह विद्वान है। श्रद्धा ने कहाः यह सज्जन है। और साधन भजन किया तो पता चला कि यह सज्जन भी है, विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है और इसके आचार, विचार और गुण ऐसे हैं कि संत से मिलते जुलते हैं। आँखों ने नहीं बताया कि यह संत है। आँखों ने नहीं बताया कि यह विद्वान है, आँखों ने नहीं बताया कि यह सज्जन है। आँखों ने तो मनुष्य बता दिया।
इन्द्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच मन की धारा है। मन की धारा अगर इन्द्रियों से सहमत हो जाती है तो उसका ज्ञान छोटा रह जाता है। मन की धारा बुद्धि से सहमत होती है तो उसके ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान का जब विकास होता है तब बुद्धि परिणाम पर ध्यान देती है। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे बहना ऐसे इन्द्रियों का स्वभाव है विषय-सुख दिखे वहाँ रूक जाना। अब इतने लोग शान्ति से सत्संग सुन रहे हैं, गुरूजी को एकटक निहार रहे हैं। अगर यहाँ कोई सिंगार की हुई नटी आ जाय तो उस चंचला की ओर आँखें घूम जाएँगी। इन्द्रियों ने ऐसी चंचलाएँ कई बार देखी। इन्द्रियों का स्वभाव है गिरना। उस समय अगर बुद्धि का उपयोग करेंगे तो विचार जागृत होगा। अन्यथा आँखों के पीछे मन लगेगा। कई प्रकार के मनोराज खड़ा करेगा।
इन्द्रियाँ और बुद्धि के बीच मन की धारा है। इस धारा का आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह धारा इन्द्रियों से जुड़कर बुद्धि को क्षीण कर देती है। मन में जब भगवान का प्रेम भरते हैं तो मन बुद्धि के पक्ष में हो जाता है और बुद्धि परिणाम का विचार करती है। 'यह देख लिया फिर क्या ? यह खा लिया फिर क्या ? इतना इकट्ठा कर लिया फिर क्या ? इतना भोग लिया फिर क्या ?' इस प्रकार बुद्धि परिणाम का विचार करती है तो संसार की असारता समझ में आ जाती है, विकारों का दुःखद परिणाम याद आ जाता है। जरा से सुख के पीछे काफी दुःख सहना पडता है और जरा सा दुःख सह लो तो काफी समता और सामर्थ्य मिलता है। जो सुख को पचा लेता है, दुःख को पचा लेता है वह परम पद को पा लेता है। ऐसा बुद्धि में योग आता है तो बुद्धि जहाँ से ज्ञान लाती है उस सत्य के ज्ञान का प्रकाश होता है। रोम रोम में सत्यस्वरूप की चेतना बस रही है इसलिए उस सत्य का नाम राम रखा गया है। वह खुद ही है इसलिए इस्लाम ने उसे खुदा कहा। वह कल्याणस्वरूप है इसलिए उसका नाम शिव रखा गया। अपना आपा है इसलिए उसे आत्मा कहा गया। वैसे का वैसा सबकी आँख के द्वारा, सबकी बुद्धि के द्वारा वह प्रकाशित होता है, सबकी बुद्धियाँ उसी से ही प्रकाश लाती हैं इसलिए उसका नाम परमात्मा रखा गया।
प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन-यजन-स्मरण करने से बुद्धियोग मिलता है। बुद्धियोग को प्राप्त होने वाला साधक भी कभी-कभी फिसलता है, चढ़ता है, उतरता है।
तीन प्रकार के लोग होते हैं- पशुधर्मा, मध्यधर्मा और सिद्धधर्मा।
एक होते हैं, जैसा इन्द्रियों ने दिखाया उसी के पीछे सारा जीवन बिता दें। वे हैं पशुधर्मा लोग। शरीर का आकार तो मनुष्य का लेकिन बुद्धि पशुओं से आगे नहीं बढ़ी। जैसे गाय ने हरा घास देखा तो मुँह डाल दिया, खा लिया। किसका है, कैसा है कुछ नहीं देखा। पशु इन्द्रियगत ज्ञान के प्रभाव में ही जीते हैं। इस प्रकार के आदमी बाहर से चाहे बड़े दिखते हों, वे छोटे विचार के होते हैं। छोटे विचार के बड़े आदमी बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़े विचार के छोटे आदमी बड़ा काम कर लेते हैं।
पाशवी धर्मा मनुष्य अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन में समय और जीवन बिता देते हैं। जो जितना ज्यादा भीतर से कंगाल होता है वह उतना ही बाहर से धन की, मान की आवश्यकता महसूस करता है। ऐसा ब्रह्मवेत्ताओं का कहना है, शास्त्रों का कहना है। जो भीतर से जितना गिरा हुआ होता है उसे उतना ही बाहर के आडम्बर की आवश्यकता पड़ती है। भीतर से जितना कंगाल होता है उतना बाहर से चीजों की गुलामी करनी पड़ती है। भीतर से जितना उन्नत होता है उतना बाहर की चीजों से लापरवाही रहती है।
भीतर से उन्नत वे लोग होते हैं जिनके मन की धारा बुद्धि के तरफ है और बुद्धि की धारा चैतन्य के तरफ है।
दूसरे तरफ हैं सिद्धधर्मा लोग, शुकदेवजी महाराज जैसे, कौपीन पहने हुए। भीतर की मस्ती में इतने सराबोर हैं कि कौपीन का भी पता नहीं। त्याग की पराकाष्ठा है। दूसरी ओर परीक्षित हैं, भोग की पराकाष्ठा पर। वे ऐहिक जगत में उन्नत शिखर पर बैठे हैं। शुकदेव जी आध्यात्मिक जगत में उन्नत शिखर पर बैठे हैं। शुकदेवजी आध्यात्मिक जगत में उन्नत शिखर पर बैठे हैं।
परीक्षित ऐहिक जगत में उन्नत शिखर पर हैं लेकिन उन चीजों में उनकी आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है। मृत्यु आने वाली है, तक्षक डँसने वाला है। यह सब समझकर जीवन्मुक्त के शरण में आये हैं।
जीवन्मुक्त के जीवन में ऐसा कुछ अदभुत खजाना होता है कि वे भोगी को भी देते हैं, साधक को भी देते हैं, धर्मात्मा को भी देते हैं और परमात्मा को भी प्यार कर देते हैं। परमात्मा प्यार के प्यासे हैं। जीवन्मुक्त परमात्मा को भी प्यार देते हैं।
भोगी आदमी प्रेम नहीं कर सकता। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सेवा का मजा चला गया। स्वार्थी आदमी न सेवा कर सकता है न प्रेम कर सकता है। जिसका स्वार्थ चला गया है, जिसकी बुद्धि में योग मिल गया है वह सेवा भी बढ़िया कर सकता है, प्यार भी बढ़िया कर सकता है। वह 'पर' की सेवा करते-करते 'पर' में 'स्व' को देखता है, 'स्व' में 'पर' को देखता है. 'स्व' और 'पर' की भ्रांति मिटाकर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के अनुभव में जग जाता है।
प्रीति 'स्व' से की जाती है, सेवा 'पर' की की जाती है। ऐसा करते-करते 'पर' में 'स्व' के दर्शन होने लगते हैं। प्रारम्भ में 'पर' लगता है लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि पर दिखता था, वास्तव में पर जैसा कुछ है नहीं। पर और स्व ये अन्तःकरण की सीमाएँ बनी इसलिये दिखता है। अन्तःकरण की छोटी अवस्था के कारण दिख रहा है। वास्तव में जिससे आप बात करते हैं उसमें भी स्वयं आप ही हो। जब दूसरे का हितचिंतन करते हो तब तुम्हारा हृदय कितना पवित्र होता है ! दूसरों के काम में आते हो तो तुम्हारा हृदय कितना उन्नत होता है !
दायाँ और बायाँ हाथ अलग-अलग दिखते हैं, दोनों हैं तो तुम्हारे ही। ऐसे ही समग्र चराचर विश्व में भिन्न-भिन्न दिखता है, मूल में अभिन्न है। जिसकी बुद्धि में योग मिल जाता है वह भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हुए, भिन्न-भिन्न आचरण करते हुए भी अभिन्न की स्मृति बनाये रखता है। उसका भजन निरन्तर हो जाता है।
कुण्डलिनी योग के जगत में जो लोग जाते हैं उनका प्रारम्भ में प्राणोत्थान होता है। जीवन की अधोगामी धारा ऊर्ध्वगामी बनती है। कुण्डलिनी योग की साधना में त्रिबन्धयुक्त प्राणायाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। मूलबन्ध करने से साधक विकारी जीवन से बचकर निर्विकारी जीवन के तरफ उठता है। उड्डियान बन्ध करने से साधक आध्यात्मिकता में उड़ान कर लेता है। शीघ्र उन्नति होती है। जालन्धर बन्ध करने से बुद्धि का विकास होता है। ये त्रिबन्ध करके साधक प्राणायाम का अभ्यास करता है और ब्रह्मवेत्ता सदगुरू का सान्निध्य मिलता है तो भीतर का रस प्रकट होने लगता है। ज्यों-ज्यों भीतर का रस निखरने लगता है त्यों-त्यों विकारी रस में मन की फिसलाहट कम होती है।
तीन प्रकार के लोग हमने देखेः पशुधर्मा लोग, सिद्धधर्मा लोग शुकदेवजी महाराज जैसे और तीसरे होते हैं मध्यधर्मा। मध्यधर्मा साधक होता है। कभी वह इन्द्रियों के बहाव में बह जाता है कभी साधु पुरूषों का संग करके संयमी बनता है। कभी लगता है मैं ठीक चलता हूँ, कभी महसूस करता है मेरा पतन हो रहा है। जब छोटे व्यक्तियों के बीच होता है तब सोचता है वे लोग चाय पीते हैं, मैं नहीं पीता, वे संसारी वासना में गिरे हुए हैं, हम बचे हुए हैं। उन लोगों से हम उन्नत हैं। कभी-कभी साधक इन्द्रियत आकर्षणों में बह जाता है। जब सत्पुरूषों का सान्निध्य मिलता है तो उन्नत जीवन में चलता है।
साधक लोगों के मन में दोनों प्रकार की धाराएँ चलती हैं- इन्द्रियगत जगत का भी आकर्षण है और आध्यात्मिकता का भी आकर्षण है। जीवन की गाड़ी कभी इधर को जाती है कभी उधर को जाती है। गाड़ी जब उन्नति की ओर जाती है तब मन में लगता है कि हाश ! आज का दिन बढ़िया गया। आज कुछ अच्छी कमाई की। जब उन्नति से थोड़ा लथड़ गये तो परेशानी नहीं लगती। उनको लगता है किः "हम मौज करते हैं। तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट का धुआँ उड़ाते हैं। ये लोग तो भगतड़े हैं....।'
उनको तो पता ही नहीं कि बाद में वे कैन्सर का शिकार बनेंगे। दूसरे जन्मों में वृक्ष होकर कुल्हाड़े के प्रहार सहन करने पड़ेंगे। कूकर-शूकर बनकर जो भोगना पड़ेगा बाद में, उसका ख्याल ही नहीं है। अभी तो जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया पहन लिया, जो मन में आया कर लिया लेकिन परिणाम का पता नहीं। वे मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतन्त्रता तो कीट, पतंग, मक्खी मच्छर को भी मिलती है। यह कोई स्वतन्त्रता नहीं है।
'स्व' के सुख में, आत्म-सुख में रमण करना यह स्वतन्त्रता है। वस्तुएँ पाकर जो सुखी होते हैं वे स्वतन्त्र नहीं है। वे तो लाचार हैं। सुख होता है क्षणभर का और परिणाम में लम्बी मुसीबत है। जरा सा सुख भोगे और लम्बा दुःख। जरा सा संयम करे तो शाश्वत सुख।
शाश्वत सुख की खबर उसी को पड़ती है जिसको भगवान बुद्धियोग देते हैं। बुद्धियोग उसी को मिलता है जो भगवान को स्नेह करता है, भगवत्प्रीति की तीव्र आकांक्षा रखता है।
रीत-रिवाज जानने वाले लोग बहुत हैं, यज्ञ याग करके सिद्धियाँ पाने की इच्छावाले लोग बहुत हो सकते हैं। भगवान की प्रीति के लिए जो कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं वे विरले हैं। काम-विकार से प्रेरित होकर बच्चों को जन्म देने वाले लोग तो कई होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार का कार्य करने वाले कोई विरले हैं।
जो कुछ करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
कबीर
जी की दीक्षा
कबीर जी ने सोचा कि गुरू किये बिना काम बनेगा नहीं। उस समय काशी में रामानन्द नाम के संत बड़े उच्च कोटि के महापुरूष माने जाते थे। कबीर जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर आकर विनती कीः "मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ।"
उस समय जात-पाँत का बड़ा आग्रह रहता था। और फिर काशी ! वहाँ पण्डितों और पाण्डे लोगों का अधिक प्रभाव था। कबीर जी किसके घर में पैदा हुए थे, हिन्दू के या मुस्लिम के, कुछ पता नहीं था। एक जुलाहे को रास्तें में किसी पेड़ के नीचे से मिले थे। उसने पालन-पोषण करके कबीर जी को बड़ा किया था। जुलाहे के घर बड़े हुए तो जुलाहे का धन्धा करने लगे। लोग मानते थे कि वे मुसलमान की संतान हैं।
द्वारपालों ने कबीरजी को आश्रम में जाने नहीं दिया। कबीर जी ने सोचा कि पहुँचे हुए महात्मा से अगर गुरूमंत्र नहीं मिलता तो मनमानी साधना से 'हरिदास' बन सकते हैं, हरिमय नहीं बन सकते। कैसे भी करके रामानन्दजी महाराज से मंत्रदीक्षा लेनी है।
कबीर जी ने देखा कि हर रोज सुबह तीन-चार बजे स्वामी रामानन्द खड़ाऊँ पहनकर 'टप...टप....' आवाज करते गंगा में स्नान करने जाते हैं। कबीर जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में और सब जगह बाड़ कर दी। एक ही मार्ग रखा और उस मार्ग में सुबह के अन्धेरे में कबीर जी सो गये। गुरू महाराज आये तो अन्धेरे के कारण कबीर जी पर पैर पड़ गया। उनके मुख से उदगार निकल पड़ेः "राम... राम... राम....।"
कबीरजी का तो काम बन गया। गुरूजी के दर्शन भी हो गये, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरूमुख से रामनाम का मंत्र भी मिल गया। अब दीक्षा में बाकी ही क्या रहा ? कबीर जी नाचते, गाते, गुनगुनाते घर वापस आये। रामनाम की और गुरूदेव के नाम की रट लगा दी। अत्यंत स्नेहपूर्वक हृदय से गुरूमंत्र का जप करते, गुरूनाम का कीर्तन करते साधना करने लगे। दिनोंदिन उनकी मस्ती बढ़ने लगी।
जो महापुरूष जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की अनुभूति उनका भावपूर्ण हृदय से चिन्तन करने वाले को भी होने लगती है।
काशी के पण्डितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर रामनाम जपता है, रामानन्द के नाम का कीर्तन करता है ! उस यवन को रामनाम की दीक्षा किसने दी ? क्यों दी ? मंत्र को भ्रष्ट कर दिया ! पण्डितों ने कबीर से पूछाः
"रामनाम की दीक्षा तेरे को किसने दी ?"
"स्वामी रामानन्दजी महाराज के श्रीमुख से मिली।"
"कहाँ दी ?"
"सुबह गंगा के घाट पर।"
पण्डित पहुँचे रामानन्द जी के पासः "आपने यवन को राममंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया, सम्प्रदाय को भ्रष्ट कर दिया। गुरू महाराज ! यह आपने क्या किया ?"
गुरू महाराज ने कहाः "मैंने तो किसी को दीक्षा नहीं दी।"
"वह यवन जुलाहा तो रामानन्द..... रामानन्द.... मेरे गुरूदेव रामानन्द" की रट लगाकर नाचता है, आपका नाम बदनाम करता है।"
"भाई ! मैंने उसको कुछ नहीं कहा। उसको बुलाकर पूछा जाय। पता चल जायेगा।"
काशी के पण्डित इकट्ठे हो गये। जुलाहा सच्चा कि रामानन्दजी सच्चे यह देखने के लिए भीड़ हो गई। कबीर जी को बुलाया गया। गुरू महाराज मंच पर विराजमान हैं। सामने विद्वान पण्डितों की सभा बैठी है।
रामानन्दजी ने कबीर से पूछाः "मैंने तुझे कब दीक्षा दी ? मैं कब तेरा गुरू बना ?"
कबीर जी बोलेः "महाराज ! उस दिन प्रभात को आपने मेरे को पादुका का स्पर्श कराया और राममंत्र भी दिया, वहाँ गंगा के घाट पर।"
रामानन्द जी कुपित से हो गये। कबीर जी को अपने सामने बुलाया और गरज कर बोलेः "मेरे सामने तू झूठ बोल रहा है ? सच बोल...."
"प्रभु ! आपने ही मुझे प्यारा रामनाम का मंत्र दिया था...."
रामानन्दजी को गुस्सा आ गया। खडाऊँ उठाकर दे मारी कबीर जी के सिर पर।
"राम... राम...राम....! इतना झूठ बोलता है....।"
कबीर जी बोल उठेः "गुरू महाराज ! तबकी दीक्षा झूठी तो अबकी तो सच्ची...! मुख से रामनाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी पावन पादुका का स्पर्श भी हो गया।"
स्वामी रामानन्द जी उच्च कोटि के संत-महात्मा थे। घड़ी भर भीतर गोता लगाया, शांत हो गये। फिर पण्डितों से कहाः "चलो, यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नम्बर का शिष्य यही है।"
ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरूषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले तो भी बेड़ा पार करती है और मार खाकर मिले तो भी बेड़ा पार कर देती है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
एक बार सिकंदर लोदी काशी से गुजरा तो एक मठ का भव्य द्वार देखा। पूछाः
"इतना बड़ा मठ किसका है ?"
"हजूर यह तो स्वामी रामानन्दजी महाराज का स्थान है। बड़े अच्छे संत महात्मा हैं।"
"भीतर शाही फरमान भेज दो कि मैं उनकी मुलाकात लेना चाहता हूँ।"
मठ से सन्देशा आया कि बाबाजी अहंकारी सम्राटों को मिलते नहीं। अभी ध्यानमग्न हैं।
सिकंदर लोदी ने सैनिकों के द्वारा जबरन दरवाजा खुलवाया और भीतर चला गया। स्वामी रामानन्द बैठे थे ध्यानस्थ। यवन ने आवाज लगायीः
"महाराज ! सम्राट आपसे मिलना चाहता है, दीदार करना चाहता है।"
महाराज ने शिष्य को आदेश दिया कि भगा दो सम्राट को, सम्राट के बाप को भी. यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सम्राटों के सम्राट मेरे परमात्मा में मुझे रहने दो।
अहंकारी का थोड़ा सा अपमान हो जाय तो जल भुन जाता है। म्यान में से तलवार निकाली और स्वामी जी का सिर काट दिया। सारे नगर में हाहाकार मच गया। उस समय सत्ताधारियों का बोलबाला था। राजसत्ता के आगे प्रजाजन क्या करें ? रामानन्दजी के शिष्य और भक्त लोग करूण आक्रन्द करने लगे।
आवेश में आकर आदमी क्रूर कर्म कर बैठता है। आवेश फिर वैसे का वैसा नहीं रहता, ठण्डा पड़ जाता है। किये हुए कृत्य का पछतावा होता है। थोड़ा बहुत समय बीता तो सिकंदर लोदी के भी हुआ कि गलती हो गई। अब क्या किया जाये ?
पण्डितों ने सुझाव दियाः "हजूर ! स्वामी रामानन्दजी का शिष्य है कबीर। बड़ा पहुँचा हुआ है। उसको शाही फरमान से बुलवाया जाय कि अपने गुरू को जिन्दा कर दे।"
ईर्ष्याखोर पण्डितों ने सोचा था कि एक काँटा तो गया। गुरू को जिन्दा करने के बहाने शिष्य को भी उड़वा देंगे। कबीर गुरू को जिन्दा नहीं करेगा तो झूठा सिद्ध हो जायगा। उसे सिकंदर लोदी के कोप का और समाज की अश्रद्धा का शिकार बना देंगे।
जगे हुए महापुरूषों के साथ अन्याय करने वालों ने सदा-सदा से अपने दाँवपेंच लड़ाये हैं। विवेकानन्द विदेश में गये थे लोगों को जगाने के लिए तो ईसाईयत ने स्वामी विवेकानन्द के लिए भरपेट कुप्रचार किया। जिसस के लिए विवेकानन्द को मान था लेकिन ईसाईयत ने विवेकानन्द का प्रकाश न फैले इसलिए विवेकानन्द पर बहुत-बहुत आरोप रखे। स्वामी रामतीर्थ गये तो उनका प्रभाव भी क्षीण करने के प्रयत्न किये गये। अभी भी भारत के साधु वहाँ जाते हैं तो वे लोग सतर्क होते हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव उन पर न पड़े इसलिए वे सावधान रहते हैं। यूरोप में जर्मनी आदि देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार होने नहीं देते हैं। उनको भय है कि इनकी संस्कृति यहाँ फैलने लगेगी तो हमारा बाह्य आडंबर से चलने वाला डिम डिम तुच्छ हो जायेगा। इसलिए सनातन संस्कृति के प्रति बालकों में प्रारम्भ से ही घृणा जगा देते हैं। स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वहाँ का कल्चर हमारी संस्कृति से प्रभावित न हो। जिन लोगों ने प्रभावित किया उन लोगों पर केस-वेस कराकर उनको बदनाम किया। पादरी संस्कारों से सम्पन्न लोगों राजसत्ता में जाकर भारतीय लोगों को बदनाम किया। पश्चिम में गये हुए जिन भारतीयों का थोड़ा-बहुत प्रभाव हुआ उनकी जड़ों पर उन लोगों ने कुठाराघात किया। अखबारों में, सामयिकों में बदनाम किया। उनकी जितनी बदनामी की जाती है उतने वे बदनाम नहीं होते हैं। उतने गिरे हुए वे नहीं हैं जितने अखबारों में चित्रित करके गिराये जाते हैं। अगर इतने गिरे हुए होते तो हजारों आदमी उनसे प्रभावित क्यों होते ?
कबीर जी को गिराने के लिए पण्डितों ने मौका लिया। लोग कबीर जी के पास जाने लगे थे। एक बार कबीर जी ने कह दिया था किः 'पण्डित वाद वदन्ति झूठा।' धर्म का बाह्य दिखावा करने वाले मुल्लाओं को भी कबीर जी ने सत्य सुना दिया किः
कंकड़
पत्थर जोड़ के
दीना मसीद
बनाय।
ता
पे मुल्ला
चढ़ी बाँग दे
क्या बहरा हुआ
खुदा ?
क्रिया-कांड करने वाले पंडे लोग जनता को ठगते। वे कहते कि 'तुम्हारा पिता स्वर्ग में ठण्डी से सिकुड़ रहा है। उसके लिए गद्दी, तकिये, रजाई दान में दे दो।' ऐसा करके समाज को गुमराह करते थे। श्रद्धालु लोगों की श्रद्धा का दुरूपयोग करने वालों के प्रति कबीर जी ने रोष व्यक्त किया तो वे पाखण्डी लोग कबीर जी के प्रति द्वेष करने लगे थे। आज कबीर जी का काँटा दूर करने का मौका आ गया है।
कबीर जी को बुलाया गया। सिकंदर लोदी ने कहा कि अपने गुरू को जिन्दा करो।
कबीर जी ने कहाः "मेरे बस की बात नहीं है।"
और सब शिष्य रो रहे थे, आक्रंद कर रहे थे। कबीर जी शांत थे। उनके चेहरे पर वही समता। लोगों को बहकाने के लिए पण्डितों और मुल्लाओं को अच्छा मौका मिला। अन्य शिष्यों से वे बोलेः "देखो, आपके गुरूजी स्वर्गवासी हुए तो आप रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं और यह देखो कबीर। आँखों में एक भी आँसू है ? गुरूजी के लिए थोड़ी सी छटपटाहट ? अगर सच्चा शिष्य होता तो हत्यारे के साथ भिड़ जाता, कुछ न कुछ सुना देता।"
कबीर उनकी बात सुनकर आवेश में आ जाते, लोदी से भिड़ जाते तो भी मामला साफ हो जायेगा। अगर नहीं भिड़ते तो रामानन्दजी के शिष्यों में कबीर के लिए अभाव फैल जायेगा। उन्होंने ठीक दाँव फेंका।
बुद्धिमानों की बुद्धि जब तक भगवत्प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ता से नहीं पकड़ती तब तक वह राग-द्वेष करके लोगों को नीचा दिखाकर अपना अहं पोसने में लगायी जाती है। कभी-कभी आश्रम में और धार्मिक संस्थाओं में भी ऐसे लोग घुस जाते हैं। आश्रम में भी राजकारण घुसेड़ देते हैं। आते हैं तो समाज से न ? वहाँ भी पार्टीबाजी खेल लेते हैं। उन अभागों को पता नहीं कि वह जीवित महापुरूष की जगह है। वहाँ कोई राजकारण की आवश्यकता नहीं। समाज में जो कचरा लग गया है वह सारा का सारा धो डालने की वह जगह है।
एक बात खास ध्यान में ले लेने जैसी है। एक ही गुरू के शिष्य परस्पर संघर्ष करते हैं तो गुरू की शक्ति ही खत्म कर रहे हैं। सजातीय विचारवाले आपस में टकराते हैं तो किसी को भी लाभ के बजाय हानि ही ज्यादा होती है। सजातीय संस्कारवालों में मेल होगा तो आसुरी शक्तियों और विजातीय संस्कारों पर जीनेवाले व्यक्तियों के प्रभाव से बच सकते हैं। विजातीय संस्कारवालों से भी उदारतापूर्वक ईश्वर-दृष्टि से व्यवहार करने से उनको भी सजातीय विचारवाले बना सकते हैं।
सजातीय विचारवालों के साथ मेल करने से विजातीय पर विजय होती है। विजातीय से उदारतापूर्वक व्यवहार करने से प्रकृति के गुणों पर अधिकार होने लगता है। सजातीय के साथ संघर्ष से अपनी शक्ति को बचाकर विजातीय पर विजय पाने के लिए लगानी चाहिए। विजातीय के साथ संघर्ष से शक्ति बचाकर प्रकृति के जन्म-मरण, राग-द्वेष आदि जो चक्र हैं उन पर विजय पाने में लगानी चाहिए।
लड़कर लड़ाकर विजय पाना यह चलते पुर्जों का काम है, साधक का नहीं। 'चलता पुर्जा' का अर्थ क्या है ? चलता पुर्जा यानी चतुर। इसको उसको लड़ाकर अपना क्षुद्र स्वार्थ सिद्ध कर लिया। यह चलता पुर्जा नाम सार्थक ही है क्योंकि वह चलता ही रहेगा, चौरासी चौरासी लाख माताओं के गर्भों में घूमता ही रहेगा। वह रूकेगा नहीं बेचारा। जो अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग साधन-भजन में नहीं करते बल्कि लड़ाई-झगड़े कराकर, अगवानी लेकर सत्ता का स्थान पचा लेने में करते हैं ऐसे लोग आत्म-विश्रांति के मार्ग से दूर ही दूर चले जाते हैं।
अभी हमारे आश्रम में या समिति में ऐसा कुछ नहीं बना लेकिन हो सकता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बुद्धि का और चतुराई का पूरा उपयोग करने वाले लोग आश्रम के वातारवरण में घुस जायें। मुझे डर लगता है कि ज्यों-ज्यों इस आश्रम की सुवास फैलती जायेगी त्यों-त्यों हो सकता है कि आश्रम के नाम से कोई चन्दा लेने निकल पड़े। 'गुरू महाराज ने माँगा है... गुरू महाराज की यह आवश्यकता है....' ऐसा करके नोटबुक लेकर कोई निकल पड़े। यह संभव है। ऐसा कोई करने न लग जाये इसके लिए समिति के लोग सावधान भी रहते हैं. सचमुच गुरू महाराज की कोई माँग है नहीं, आश्रम कोई चन्दा-वन्दा करता नहीं यह साधक लोग जानते हैं। इसीलिए लोग हिम्मत नहीं करते। कोई चलता पुर्जा ऐसी हिम्मत करे उसके पहले मैं आपको सावधान कर देता हूँ।
आश्रम आपसे चन्दा लेकर बिल्डिंगे बाँधने के लिए नहीं बना लेकिन आपसे अहं लेकर आपके दिल में दिलबर के गीत गुँजाने के लिए आश्रम बना है।
आप लोगों की यह तत्परता रहती है कि जहाँ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस जगह को सजायें, सँवारें। यह आपके उत्साह की बात है। भाव से सेवा कर लेते हो यह अलग बात है लेकिन कभी-कभी तो ऐसे टूटे-फूटे छपरे के नीचे भी आपको यहाँ जो आनन्द आता है वह आपके आलीशान बंगलों में नहीं आता।
ऊपर देखो, यह सत्संग-हॉल का छपरा कैसा है ? सीधा-सादा। फिर भी आपकी नजर इस छपरे पर नहीं है लेकिन छपरा और महल जिस प्रकृति में ठहरे हैं और प्रकृति जिस परमात्मा में ठहरी है उस परमात्मा की ओर आपकी नजर है इसीलिए आपको छपरे के नीचे भी आनन्द आता है। छपरा भी मधुर लग रहा है।
आश्रम को तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है, आश्रम को तुम्हारे दिलों की आवश्यकता है ताकि उसमें दिलबर को भर दिया जाये।
हम फिर से स्वामी रामानन्दजी के आश्रम में चलते हैं। धर्म के ठेकेदार उन पण्डों ने कबीर और सिकंदर लोदी को भिड़ाने की युक्ति की। कबीर जी ने देखा कि गुरू महाराज का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। सब शिष्य करूण आक्रंद कर रहे हैं। कबीर जी बोलेः
"रोने से क्या होगा ? रोने से गुरूजी थोड़े ही जग जाएँगे ? रोते क्यों हो ?"
संत
मरे क्या
रोइये जाये
अपने घर।
यह सुनकर विरोधी लोग आपस में गुसपुस करने लगेः देखो, ये कोई शिष्य के लक्षण हैं ?
वास्तव में कबीर जितना रामानन्द स्वामी से स्नेह करते थे और रामानन्द स्वामी जितना कबीर को चाहते थे यह तो वे ही दोनों जानते थे।
लोगों ने कबीर जी से प्रार्थना की किः "महाराज ! अब गुरूजी को जिन्दा करो। हमसे यह दृश्य देखा नहीं जाता।"
"मैं कौन होता हूँ गुरू को जिन्दा करने वाला ? मेरे गुरूजी कभी मरते हैं क्या ? मेरे गुरूजी कभी नहीं मरते।"
बात भी सही है। गुरू तत्त्व नहीं मरता। गुरू का देह है तभी गुरू हैं और देह नहीं है तभी भी सच्चे शिष्य को गुरू अमर भासते हैं। गुरू तत्त्व की सत्ता-स्फूर्ति महसूस होती है। हम लोग जब सत्शिष्यों की दुनियाँ में प्रवेश करते हैं तब इस राज का पता चलता है। हमारे सामने खड़े हैं तभी ही केवल वे उपस्थित नहीं हैं। गुरूमंत्र दिया तभी से सदा के लिए हमारे साथ बस जाते हैं। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, धन्यवाद देते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो भीतर सावधान भी करते हैं।
कबीर जी ने धड़ और सिर को मिला दिया। ऊपर चद्दर ओढ़ा दी। लोगों को बातों में लगा दिया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद पानी का कलश लेकर खड़े हुएः
"गुरू महाराज ! ये दास सब आपके दर्शन के लिए इन्तजार कर रहे हैं। ....और आपका संध्या करने का समय हो गया है प्रभु ! आज बहुत गहरी नींद सोये हैं मेरे रामानन्द भगवान ! उठिये, संध्या कीजिए प्रभु !"
चद्दर हिलने लगी। लोग आश्चर्य-मुग्ध होकर देख रहे थे। कहानी कहती है कि कबीर जी की प्रार्थना से रामानन्द स्वामी करवट लेकर उठे। अहंकारी सिकंदर लोदी दोनों गुरू शिष्य के चरणों में गिर पड़ा। गदगद होकर कण्ठ होकर बोलाः
"अरेरे ! मैं समझता था कि तुम काफिर हो लेकिन आपको काफिर समझाने वाले ही काफिर हैं।"
यह अचलमना पुरूष का प्रभाव है, इच्छाशक्ति का प्रभाव है। भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए कभी-कभी ऐसा कर देते हैं। अपने भक्तों के प्रकाश को अभक्तों तक फैलाकर भगवान अपनी रसमयी, प्रेममयी, माधुर्यमयी अनुभूति को जन-साधारण तक पहुँचाने के लिए कभी-कभी लीला कर लेते हैं।
मनमाना साधन अगर हम पकड़ रखते हैं तो साधन करने का अहं बना रहता है। साधन साधन बना रह जाता है, साधन रस में नहीं बदलता। सत्संग से ही साधन में रस आता है। सदगुरू की कृपा से ही साधन में रस आता है। जैसे गन्ना मीठा तो होता है, उसे अपनी मधुरता का पता नहीं होता, ऐसे ही तुम मधुर तो हो, तुम्हें मधुरता का पता नहीं है।
वे दिन अपने जल्दी लाओ। अपनी महिमा को पहचानो। अपने नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध आत्मा को जानो।
हे अमर आत्मा ! कब तक मरने-मिटने वाले वासना-विकारों से अपने को सताते रहोगे ? उठो जागो। लग जाओ आतंर यात्रा में। हरि ॐ... ॐ.... ॐ....
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
रामू
की गुरूभक्ति
संत परम हितकारी होते हैं। वे जो कुछ कहें, करने के लिए डट जाना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण निहित होता है। महापुरूष की बात को टालना नहीं चाहिए। वशिष्ठजी महाराज योगवशिष्ठ महारामायण में कहते हैं-
"हे राम जी ! त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके सुखी रह सके ?"
गुरूगीता में भगवान शंकर कहते हैं-
गुरूणां
सदसद्वापि
यदुक्तं तन्न
लंघयेत्।
कुर्वन्नाज्ञां
दिवारात्रौ
दासवन्निवसेद्
गुरौ।।
'गुरूओं की बात सच्ची हो या झूठी, उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरू की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु के सान्निध्य में दास बनकर रहना चाहिए।'
गुरूदेव की कही हुई बात चाहे झूठी दिखती हो फिर भी शिष्य को सन्देह नहीं करना चाहिए, कूद पड़ना चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए।
सौराष्ट्र में रामू नाम के बढ़िया गुरूभक्त शिष्य हो गये। लाल जी महाराज पर उनका खत आता रहता था। लालजी महाराज ने ही रामू के जीवन की घटना बतायी थी।
एक बार उनके गुरू ने कहाः "रामू ! घोड़ागाडी ले आ। भगत के घर भोजन करने जाना है।"
रामू घोड़ागाड़ी ले आया। गुरु नाराज होकर बोलेः "अभी सुबह के सात बजे हैं, भोजन तो 11-12 बजे होगा। बेवकूफ कहीं का, 12 बजे भोजन करने जाना है और गाड़ी अभी ले आया? बेचारा ताँगेवाला तब तक बैठा रहेगा?"
रामू गया, ताँगेवाले को छुट्टी देकर आ गया। गुरु ने पूछाः "क्या किया?"
"ताँगा वापस कर दिया।" हाथ जोड़कर रामू बोला।
गुरुजीः "जब जाना ही था तो वापस क्यों किया? जा ले आ।"
रामू गया और ताँगेवाले को बुला लाया।
"गुरुजी ! ताँगा आ गया।"
गुरुजीः "अरे ! ताँगा ले आया? हमें जाना तो बारह बजे है न? पहले इतना समझाया अभी तक नहीं समझा? भगवान को क्या समझेगा? ताँगे की छोटी-सी बात को नहीं समझता, राम को क्या समझेगा?"
ताँगा वापस कर दिया गया। रामू आया तो गुरु गरज उठे।
"वापस कर दिया? फिर समय पर मिले-न-मिले, क्या पता? जा, ले आ।"
नौ बार ताँगा गया और वापस आया। रामू यह नहीं कहता कि गुरु महाराज ! आपने ही तो कहा था। वह सत्पात्र शिष्य जरा-भी चिढ़ता नहीं। गुरुजी तो चिढ़ने का व्यवस्थित संयोग खड़ा कर रहे थे। रामू को गुरुजी के सामने चिढ़ना तो आता ही नहीं था, कुछ भी हो, गुरुजी के आगे वह मुँह बिगाड़ता ही नहीं था। दसवीं बार ताँगा स्वीकृत हो गया। तब तक बारह बज गये थे। रामू और गुरुजी भक्त के घर गये। भोजन किया। भक्त था कुछ साधन सम्पन्न। विदाई के समय उसने गुरुजी के चरणों में वस्त्रादि रखे और साथ में, रूमाल में सौ-सौ के दस नोट भी रख दिये और हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना कीः "गुरुजी ! कृपा करें, इतना स्वीकार कर लें। इनकार न करें।"
फिर वे ताँगे में बैठकर वापस आने लगे। रास्ते में गुरुजी ताँगवाले से बातचीत करने लगे। ताँगेवाले ने कहाः
"गुरुजी ! हजार रुपये में यह घोड़ागाडी बनी है, तीन सौ का घोड़ा लाया हूँ और सात सौ की गाड़ी। परंतु गुजारा नहीं होता। धन्धा चलता नहीं, बहुत ताँगेवाले हो गये हैं।"
"गुरुजीः "हजार रुपये में यह घोड़ागाड़ी बनी है तो हजार रुपये में बेचकर और कोई काम कर।"
ताँगेवालाः "गुरुजी ! अब इसका हजार रुपया कौन देगा? गाड़ी नयी थी तब कोई हजार दे भी देता, परंतु अब थोड़ी-बहुत चली है। हजार कहाँ मिलेंगे?"
गुरुजी ने उसे सौ-सौ के दस नोट पकड़ा दिये और बोलेः "जा बेटा ! और किसी अच्छे धन्धे में लग जा। रामू ! तू चला ताँगा।"
रामू यह नहीं कहता कि 'गुरुजी मुझे नहीं आता। मैंने ताँगा कभी नहीं चलाया'। गुरुजी कहते हैं तो बैठ गया कोचवान होकर।
रास्ते में एक विशाल वटवृक्ष आया। गुरुजी ने उसके पास ताँगा रुकवा दिया। उस समय पक्की सड़कें नहीं थीं, देहाती वातावरण था। गुरुजी सीधे आश्रम में जानेवाले नहीं थे। सरिता के किनारे टहलकर फिर शाम को जाना था। ताँगा रख दिया वटवृक्ष की छाया में। गुरुजी सो गये। सोये थे तब छाया थी, समय बीता तो ताँगे पर धूप आ गयी। घोड़ा जोतने के डण्डे थोड़े तप गये थे। गुरुजी उठे, डण्डे को छूकर देखा तो बोलेः
"अरे, रामू ! इस बेचारी गाड़ी को बुखार आ गया है। गर्म हो गयी है। जा पानी ले आ।"
रामू ने पानी लाकर गाड़ी पर छाँट दिया। गुरुजी ने फिर गाड़ी की नाड़ी देखी और रामू से पूछाः
रामूः "हाँ।"
गुरुजीः "तो यह गाड़ी मर गयी.... ठण्डी हो गयी है बिल्कुल।"
रामूः "जी, गुरुजी !"
गुरुजीः "मरे हुए आदमी का क्या करते हैं?"
रामूः "जला दिया जाता है।"
गुरुजीः "तो इसको भी जला दो। इसकी अंतिम क्रिया कर दो।"
गाड़ी जला दी गयी। रामू घोड़ा ले आया।
"अब घोड़े का क्या करेंगे?" रामू ने पूछा।
गुरुजीः "घोड़े को बेच दे और उन पैसों से गाड़ी का बारहवाँ करके पैसे खत्म कर दे।"
घोड़ा बेचकर गाड़ी का क्रिया-कर्म करवाया, पिण्डदान दिया और बारह ब्राह्मणों को भोजन कराया। मृतक आदमी के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब गाड़ी के लिए किया गया।
गुरुजी देखते हैं कि रामू के चेहरे पर अभी तक फरियाद का कोई चिह्न नहीं ! अपनी अक्ल का कोई प्रदर्शन नहीं ! रामू की अदभुत श्रद्धा-भक्ति देखकर बोलेः "अच्छा, अब पैदल जा और भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पैदल करके आ।"
कहाँ सौराष्ट्र (गुज.) और कहाँ काशी विश्वनाथ (उ.प्र.) !
रामू गया पैदल। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन पैदल करके लौट आया।
गुरुजी ने पूछाः "काशी विश्वनाथ के दर्शन किये?"
रामूः "हाँ गुरुजी।"
गुरुजीः "गंगाजी में पानी कितना था?"
रामूः "मेरे गुरुदेव की आज्ञा थीः 'काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ' तो दर्शन करके आ गया।"
गुरुजीः "अरे ! फिर गंगा-किनारे नहीं गया? और वहाँ मठ-मंदिर कितने थे?"
रामूः "मैंने तो एक ही मठ देखा है – मेरे गुरुदेव का।"
गुरुजी का हृदय उमड़ पड़ा। रामू पर ईश्वरीय कृपा का प्रपात बरस पड़ा। गुरुजी ने रामू को छाती से लगा लियाः "चल आ जा.... तू मैं है.... मैं तू हूँ.... अब अहं कहाँ रहेगा !"
ईशकृपा
बिन गुरु
नहीं, गुरु
बिना नहीं
ज्ञान।
ज्ञान
बिना आत्मा
नहीं गावहिं वेद
पुरान।।
रामू का काम बन गया, परम कल्याण उसी क्षण हो गया। रामू अपने आनन्दस्वरूप आत्मा में जग गया, उसे आत्मसाक्षात्कार हो गया....
आत्म-साक्षात्कार या तत्त्वबोध तब तक संभव नहीं जब तक ब्रह्मवेत्ता महापुरूष साधक के अन्तःकरण का संचालन नहीं करते। आत्मवेत्ता महापुरूष जब हमारे अन्तःकरण का संचालन करते हैं तब अन्तःकरण तत्त्व में स्थित हो सकता है, नहीं तो किसी अवस्था में, किसी मान्यता में, किसी वृत्ति में, किसी आदत में साधक रूक जाता है। रोज आसन किये, प्राणायाम किये, शरीर स्वस्थ रहा, सुख-दुःख के प्रसंग में चोटें कम लगीं, घर की आसक्ति कम हुई, पर व्यक्तित्व बना रहेगा। उससे आगे जाना है तो महापुरूषों के आगे बिलकुल मर जाना पड़ेगा। ब्रह्मवेत्ता सदगुरू के हाथों मे जब हमारे अन्तःकरण का स्टीयरिंगव्हील आता है तो तब आगे की यात्रा होती है। कबीर जी ने कहाः
सहजो
कारज संसार को
गुरू बिन होत
नाहीं।
हरि
तो गुरू बिन
क्या मिले समझ
ले मन
माँहीं।।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
कथा-अमृत
महात्मा
का मूल्य
ईरान में फरीदुद्दीन अत्तार आत्मज्ञान के ऊँचे शिखर पर पहुँचे हुए महापुरूष थे। उस समय ईरान और तुर्कस्तान के बीच घमसान युद्ध चल रहा था। तुर्कस्तान हार रहा था। एक बार तुर्कियों ने शक में फरीदुद्दीन अत्तार को पकड़ लिया और घोषणा कर दी कि अमुक तारीख को फरीदुद्दीन अत्तार को फाँसी पर लटकाया जायगा।
ईरान में समाचार पहुँचे। सर्वत्र हाहाकार मच गया। नगर के अमीर लोग इकट्ठे हुए, चर्चा-विचारणा की और नगरसेठ ने तुर्कियों को सन्देश भेजा कि फरीदुद्दीन अत्तार के वजन के बराबर हीरे, जवाहरात तौलकर हमसे ल लो और हमें वापस लौटा दो। उन्हें फाँसी पर मत चढ़ाओ।
तुर्की शासकों ने उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया। तब ईरान के युवकों ने सन्देश भेजा कि अगर आप लोग हमारे देश के एक आदमी को फाँसी पर लटकाकर अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहते हो तो उनके बदले में हम नवयुवक फाँसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। तुम फरीदुद्दीन अत्तार को छोड़ दो।
तुर्की लोग नहीं माने। आखिर ईरान के बादशाह ने सन्देशा भेजा कि आप फरीदुद्दीन अत्तार को फाँसी पर न चढ़ायें। उनके बदले में आपको चाहिए तो ईरान का तख्त दे सकता हूँ।
तुर्कियों ने सोचा, जिस तख्त का कब्जा लेने के लिए भीषण युद्ध कर रहे हैं वह तख्त सिर्फ एक आदमी के बदले में दे रहे हैं ? अजीब बात है ! इस आदमी में जरूर कोई रहस्य होगा। फाँसी का हुक्म केन्सल कर दिया गया। सन्देशवाहकों के द्वारा मिलन का दिन और स्थान निश्चित हुआ और तुर्कस्तान के अधिकारी लोग फरीदुद्दीन अत्तार को ले आये। ईरान के सम्राट को पूछाः
"एक इन्सान के बदले में आप ईरान का तख्त देने को तैयार हो ? क्या बात है ?"
ईरान का सम्राट कहता हैः "सत्ता का तख्त तो आता-जाता है जबकि ऐसे खुदा के प्यारे पूर्ण पुरूष तो कभी-कभी ही मिलते हैं। मेरे देश में ऐसे पुरूष की रक्षा न कर सकूँ, सँभाल न कर सकूँ तो मेरे देश पर लांछन लगेगा। इतिहास में हमारे देश पर काला धब्बा लगा रहेगा, दुनियाँ गाती रहेगी कि पूरा देश मिलकर भी खुदा के प्यारे एक फकीर की सेवा भी न कर सका। मेरा देश दुनियाँ की नजरों में तो गिरेगा ही, उस मालिक की नजरों में भी गिर जायेगा। जिसके दिल में पूरे मालिक प्रकट हुए हैं ऐसे महान् संत की सेवा न कर सकना यह पूरे ईरान का तख्त देने को तैयार हूँ। देश के तख्त से भी कहीं अधिक मूल्यवान है इन संत पुरूष का जीवन।"
जहाँ त्याग है, प्रेम है, समता की निगाहें हैं वहाँ सुलह और शान्ति होने में क्या देर लगेगी ? दोनों देशों के बीच समझौता हो गया। युद्ध रोक दिया गया। दोनों देश अपने-अपने ढंग से जीने लगे।
जिसके जीवन में आत्मज्ञान आ जाता है वह स्वयं तो शान्त और आनन्दित रहता है लेकिन बड़ी-बड़ी दुःखद अवस्थाओं में भी कोई उसके करीब आ जाता है तो उसकी दुःखद अवस्था भी विदा लेने लगती है, सुख में बदलने लगती है। ऐसा आत्मज्ञान का प्रभाव है। ऐसा आत्मज्ञान पाने वाला ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-
बहूनां
जन्मनामन्ते
ज्ञानवान्मां
प्रपद्यते।
वासुदेवः
सर्वमिति स
महात्मा
सुदुर्लभः।।
''बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्त्वज्ञान को प्राप्त पुरूष 'सब कुछ वासुदेव ही है' ऐसा जानता है वह महात्मा पुरूष अत्यंत दुर्लभ है।"
(गीताः 7.19)
ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन की दिशा थोड़ी बदलनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साधना में हमारा मन लगता नहीं। मन क्यों नहीं लगता है ? मन की दिशा बदलने की कला हम नहीं जानते। मन को जहाँ सुख मिलता है वहाँ बार-बार जाता है। मन को जहाँ दुःख दिखता है वहाँ से वापस लौटता है।
इन्द्रियों का स्वभाव है, जहाँ सुख मिलता है वहाँ भागती हैं। बुद्धि का स्वभाव है कि वह परिणाम को देखती है। आदमी जब बुद्धि का आदर करने लगता है तब विषय-वासना से बचने की कोशिश में होता है। बुद्धि का आदर नहीं करता तो इन्द्रियाँ मन को घसीट कर ले जाती हैं विषय-विकारों के खड्डों में।
मन की रूचि बदलने की आवश्यकता है। आप अपनी स्वतन्त्रता पर ध्यान दें। आप जो देखना चाहे देख सकते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। मन को जहाँ भेजना चाहो भेज सकते हो। आप अपनी स्वतन्त्रता भूल गये और जिसके कारण आप पराधीन होते हो उसीका पोषण करते हो इसीलिए मन भागता है, वश में नहीं रहता, जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ नहीं लगता।
आप अपनी स्वतन्त्रता पर ध्यान दो। मन और इन्द्रियों के पीछे क्यों घसीटे जाते हो ? तुम कितने स्वतन्त्र हो !
कितने ही पैसे आये और गये, तुम वही के वही। कितने ही दुःख आये और गये, तुम वही के वही। कितने ही मान के प्रसंग आये और गये, तुम वही के वही। कितनी अवस्थाएँ आयी और गई, तुम वही के वही। कितने शरीर आये और गये, तुम वही के वही। कितने ही दिन आये और गये, तुम वही के वही। कितनी ही रातें आयी और गई, तुम वही के वही।
तुम तो असंग चैतन्य हो। परिस्थितियों में आसक्त हो जाते हो, पकड़ लगाते हो इसलिए मन तुमको दगा देता है। परिस्थितियों के साथ अगर पकड़ न लगाओ तो मन तुम्हारा अनुगामी होने लगता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
मुचुकुन्द
और श्रीकृष्ण
राजा मुचुकुन्द ने देवताओं को संग्राम में सहाय की थी। उनको अब आराम की आवश्यकता थी। देवताओं ने उनको वरदान दिया कि तुम अब आराम से सो जाओ। तुम्हें कोई जगाएगा नहीं, विक्षेप नहीं डालेगा। अगर कोई जगाएगा तो तुम्हारी नजर उस पर पड़ते ही भस्म हो जाएगा।
मुचुकुन्द चले गये पहाड़ों की गुफा में। अच्छा एकान्त वातावरण खोजकर सो गये।
इधर कालयवन श्रीकृष्ण के पीछे पड़ा था मारने के लिए। कृष्ण भागते-भागते उसी गुफा में पहुँच गये। अपना पीतांबर धीरे से निद्राग्रस्त मुचुकुन्द राजा को ओढ़ा दिया और स्वयं गुफा के कोने में छिप गये। कालयवन भागता-भागता, श्रीकृष्ण को खोजता-खोजता गुफा में आया। वह समझा कि यहाँ आकर श्रीकृष्ण सो गये हैं। उसने मुचुकुन्द राजा को श्रीकृष्ण समझकर लात मारी। मुचुकुन्द जग गये। नींद में विक्षेप डालनेवाले पर कुपित हो गये। उनको तो देवताओं का वरदान मिला था। कुपित होकर कालयवन की ओर निहारा तो वह जलकर भस्म हो गया। मुचुकुन्द का क्रोध शान्त हुआ तो गुफा में अलौकिक शान्त प्रकाश दिखाई देने लगा। कोई विलक्षण मधुरता महसूस होने लगी। इधर-उधर देखा तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं।
श्रीकृष्ण तो गुफा में पहले भी थे लेकिन मुचुकुन्द सो रहे थे तो मुलाकात दर्शन नहीं हुए। कुपित हुए तब भी श्रीकृष्ण के दर्शन नहीं हुए। जब शान्त होकर बैठे तब श्रीकृष्ण दिखाई दिये।
ऐसे ही तुम्हारी दिलरूपी गुफा में वह चैतन्य परमात्मा सदा सदा से है। तुम आलस्य में, प्रमाद में जीवन बिताते हो तब भी परमात्म चैतन्य दिल की गुफा में होते हुए नहीं दिखता और तुम काम-क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त होते हो तभी भी नहीं दिखता। तुम जब शान्तमना होते हो तब उस श्रीकृष्ण तत्त्व की मुलाकात होती है, तब साक्षात्कार सम्भव बनता है।
राजा मुचुकुन्द ने भगवान से प्रार्थना कीः
"हे प्रभो ! आपके दर्शन तो हो गये, अब अपनी दृढ़ भक्ति दो। मुझे आत्मबोध हो जाये ऐसी भक्ति दो।"
श्रीकृष्ण ने कहाः "मुचुकुन्द ! जवानी में तुमने खूब भोग भोगे हैं इसलिए दृढ़ भक्ति अभी नहीं मिल सकती। थोड़ी और यात्रा करनी पड़ेगी, फिर दृढ़ भक्ति मिलेगी।"
वही मुचुकुन्द राजा कलियुग में नरसिंह मेहता हुए हैं और दृढ़ भक्त मिली है। उन्होंने गाया हैः
अखिल
ब्रह्माण्डमां
एक तुं
श्रीहरि
जूजवे रूपे
अनंत भासे....
पहले तो केवल श्रीकृष्ण में उनको प्रभु दिखता था, अब उनको कीड़ी में भी प्रभु दिखता है तो दरिया की लहर में भी प्रभु दिखता है। यशोगान करने वालों में भी प्रभु दिखता है और विरोध करने वालों में भी प्रभु दिखता है। जिसको सबमें प्रभु दिखता है उसका अन्तःकरण प्रभुमय बन जाता है। वह अन्तःकरण जिस शरीर में रहता है वह शरीर भी चिन्मय होने लगता है, दिव्य होने लगता है। नरसिंह मेहता ऐसी दिव्यता को प्राप्त हुए थे।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
मरने
से डरना क्यों
?
वेदव्यासजी के नाना निषादराज को मृत्यु का बहुत भय लगता था। एक दिन उन्हें देवर्षि नारद मिल गये। उनका अर्घ्य-पाद्य से पूजन किया। संत-महापुरूषों का आदर-सत्कार करने से बल, आयु, विद्या और बुद्धि बढ़ती है। जब श्रेष्ठ पुरूष पधारे तब खड़े होकर आदर देने से अपनी योग्यताएँ बढ़ती हैं। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
निषादराज उम्र में तो बड़े थे लेकिन भगवद् भजन में नारद जी बड़े थे। देवर्षि नारद पधारे तो वे खड़े हुए, अर्घ्य पाद्य देकर उनका पूजन किया। फिर विनती की किः "भगवन् ! मुझे मृत्यु का भय बहुत सताता है। आप कुछ भी करो, मुझे मृत्यु के भय से बचा दो। आप संत हैं। वैकुण्ठ तक जाने की योग्यता रखते हो। यमराज से कुछ लागवाग लगाओ और उनके लिस्ट में मेरे नाम पर चौकड़ी करवा दो। इतनी कृपा करो। यमराज की डायरी से मेरा नाम निकलवा दो। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा।"
नारद जी ने कहाः "देखो ! हम भजन की विधि बता सकते हैं, जप और ध्यान की विधि बता सकते हैं, साधना का मार्ग बता सकते हैं। यमराज की डायरी में गड़बड़ करना हमारे हाथ की बात नहीं है। उस काम के लिए जिसकी पहुँच हो ऐसे व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए। उनका नाम मैं बता देता हूँ।"
"हाँ बता दो।"
"वे आपके दोहित्र हैं, वेदव्यासजी। आप जिनके नाना लगते हैं वे वेदव्यासजी कारक पुरूष हैं। भगवान वेदव्यासजी संकल्पबल से यमराज के पास जायें और उनसे कहें तो आपका काम हो जायेगा। युक्ति मैं बताता हूँ, उपयोग आपको करना पड़ेगा।
पहले अर्घ्य पाद्य से पूजन करके प्रसन्न कर लेना। खुश हो जायें तब उनको वचनबद्ध कर देना कि मैं जो कहूँगा वह आप जरूर पूरा करेंगे। दूसरी बातः जब वे हाँ कह दें तब भी रूक नहीं जाना। हाँ बोलने के बाद वे करेंगे तो सही लेकिन पता नहीं कब करें। बड़े आदमी ठहरे। वे यमराज के पास पहुँचे उससे पहले वहाँ से यमदूत वारंट लेकर रवाना हो जाये ! वे छः महीने मे के बाद जायें और तुम्हारी मृत्यु तीन महीने के अन्दर हो जाय तो काम नहीं बनेगा। इसलिए तुम उनको साथ लेकर यमराज के पास जाना। अपनी नजरों के सामने यमराज की डायरी में अपना नाम केन्सल करवाना।
निषादराज को पक्का हो गया कि बात सही है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है। अपनी उपस्थिति में ही यह काम हो जाना चाहिए।
समय बीता। वेदव्यासजी आये। नारदजी के कहे अनुसार आदर-सत्कार किया, अर्घ्य-पाद्य देकर पूजन करके कहाः
"देखो, मैं उम्र में बड़ा हूँ। तुम्हारा नाना भी लगता हूँ। आज तक तुमसे कुछ नहीं माँगा।"
वेदव्यासजी बोल उठेः "नाना जी ! माँग लो।"
"मैं जो माँगूगा वह आप टालेंगे नहीं।"
"हाँ, हाँ नहीं टालूँगा।"
"वचन दे दो।"
"वचन है नाना जी ! आपको मेरा वचन है।"
"मुझे मृत्यु का भय लगता है। आप यमराज को बोल दो कि अपनी डायरी में से मेरा नाम निकाल दें।"
"अच्छा मैं कोशिश करूँगा।"
"नहीं, आप मेरे साथ चलो। मैं अपनी आँखों से देखूँ और यमराज की डायरी में से मेरा नाम कटे। आप वचन दे चुके हैं।"
कथा कहती है कि निषादराज और वेदव्यासजी पहुँचे यमपुरी में। यमराज ने आदर-सत्कार किया और वेदव्यासजी से बोलेः
"आप जैसे कारक पुरूष ब्रह्मवेत्ता इधर कैसे पधारे ? क्या सेवा करूँ ?"
"सेवा तो यह है कि ये मेरे नाना जी हैं, मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। अगर हो सके तो मृत्यु की डायरी में से मेरे नानाजी का नाम निकाल देना, यमदूत को भेजना मत।"
"मृत्यु की डायरी में हम इधर नाम नहीं रखते हैं। हमको काल के वहाँ से निर्देश होता है। यहाँ से केवल दूतों को उस निर्देश के मुताबिक रवाना करते हैं। अब आप जैसे महापुरूष आये हो तो चलो काल के पास। उधर ही मिल लेते हैं।"
तीनों पहुँच गये काल के पास। काल ने कहाः
"मेरी डायरी में नाम तब आता है जब विधाता का आदेश होता है। चलो, हम उन्हीं के पास जायें।"
चारों मिलकर विधाता के पास गये। वेदव्यासजी बोलेः
"आप तो जानते ही हैं, वेदव्यास मेरा नाम है। मैं यमराज के पास आया था। यमराज काल के पास ले गये और काल के वहाँ से सब यहाँ पहुँचे हैं।
ये निषादराज मेरे नाना जी हैं। इन्हें मृत्यु का बहुत भय लगता है। आप अपनी खाताबही में जरा रियाअत कर दीजिए। मृत्यु की लिस्ट में से इनका नाम कम कर दीजिए।"
विधाता बोलेः "मुझे पता है कि ये आपके नाना हैं। मृत्यु का इनको बड़ा भय है। इसीलिए मैंने ऐसी व्यवस्था की कि इनकी मृत्यु से जल्दी से होवे ही नहीं। उनकी मृत्यु की शर्तों में ऐसी आँटी-घूँटी रख दी के वे शर्तें पूरी होवे ही नहीं और इनको मरना पड़े ही नहीं। लाओ बही, मैं दिखाता हूँ।"
बही लायी गयी। उसमें लिखा था कि निषादराज स्वयं जब वेदव्यासजी को, यमराज को और काल को लेकर ही विधाता के पास जाएंगे तभी मृत्यु होगी, उसके पहले नहीं।
निषादराज को तो यह सुनना ही था कि मृत्यु ने अपना काम कर लिया।
मौत से बचने की इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद बी मौत का ग्रास होना पड़ता है। जब मरना इतना अवश्यं भावि है तो मरने से डरना क्यों ? डरने से मौत नहीं मिटती। दूसरी बार मौत न हो इसका यत्न करना चाहिए।
अनेक बार मौत क्यों होती है ? वासना से मौत होती है। वासना क्यों होती है ? वासना सुख के लिए होती है। अगर आत्मा-परमात्मा का सुख मिल गया तो वासना आत्मा-परमात्मा में लीन हो जायेगी। परमात्मा अमर है। वासना अगर परमात्म-सुख से तृप्त नहीं हुई तो देखने की वासना खाने की वासना, सूँघने की वासना, सुनने की वासना और स्पर्श की वासना बनी रहेगी। पाँच ही तो विषय हैं और जिनको पाँच विषय का सुख दिलाते हो उनको तो जला देना है।
योगी इस बात को जानते हैं इसलिए वे अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर ज्योत की ओर जाते हैं। भोगी इस बात को नहीं जानता, नहीं मानता इसलिए बाहर भटकता है। भगवान कहते हैं-
संतुष्टः
सततं योगी
यतात्मा
दृढ़निश्चयः।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो
मद् भक्तः स
मे प्रियः।।
'जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन-इन्द्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चयवाला है, वह मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है।'
(भगवद् गीताः 12.14)
एक बार केवल तीन मिनट के लिए अगर आत्म बोध हो जाय तो सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाये।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
हांडी
रे हांडी ऽऽऽ.......!
एक राजा की प्रिय रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा रानी में इतना मोह था कि वह भी रानी की अर्थों के साथ 'हाय रे हाय मेरी रानी ऽऽऽ....' करते हुए चिता में जलने के लिए जाने लगा।
गोरखनाथ को पता चला सोचाः 'अरेरे ! राजा इतना बुद्धिमान होते हुए भी रानी के पीछे कैसा नादान हो रहा है ! विकारों का सुख आदमी को कैसा मंदबुद्धि कर देता है ! कितना गिरा देता है ! राजा को सावधान करना चाहिए।'
राजा विह्वल होकर स्मशान की ओर जा रहा था। गोरखनाथ वहाँ आये। उनके हाथ में मिट्टी की हांडी थी। राजा के सामने आते ही हांडी को नीचे पटककर रोने लग गयेः
"हांडी रे हांडी ऽऽऽ.....! तेरे बिना भी क्या जीना ? तुझ ही में भिक्षा मांग कर खाता था, रात्री को तेरा ही सिरहाना बनाकर सोता था। तेरे बिना खाऊँगा कैसे ? तेरे बिना सोऊँगा कैसे ? तेरे में ही पानी भरके पीता था, धूप लगती थी तो टोपी की तरह पहन लेता था। बारिश में तू ही छाता बन जाती थी। हांडी रे हांडी ऽऽऽ....!"
राजा ऐहिक जगत में तो बुद्धिमान था जबकि गोरखनाथ संतुष्टः सततं योगी के जगत पहुँचे हुए थे। गोरखनाथ की बुद्धि राजा से कुछ ऊँची थी। ऐसे गोरखनाथ हांडी के लिए विलाप करने लगे। राजा देखता है कि, "मैं तो रो रहा हूँ, ये बाबाजी क्यों रोते होंगे ?" पास जाकर पूछाः
"महाराज ! क्यों रोते हो ?"
"क्या करूँ ? मेरा सर्वनाश हो गया। मेरी हांडी टूट गई। हांडी रे हांडी ऽऽऽ....!"
"महाराज ! हांडी टूटी इसमें क्या रोते हो ? ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। कभी बनते हैं कभी टूटते हैं। साधूबाबा होकर इसकी क्या चिन्ता करते हो ?"
"अरे तुम मुझे समझाते हो ? मैं तो रोकर काम चला रहा हूँ और तुम मरने को तैयार हुए हो।"
राजा को समझ आ गई कि अरे !.....
मोहनिशा
सब सोवनहारा।
देखहिं
सपने अनेक
प्रकारा।।
जिससे सम्बन्ध हो गया है वह आदमी जाता है तब दुःख तो होता है पर दुःखी होने से जाने वाला आदमी लौट आता हो तो खूब दुःख करो। दुःख करने से तो वह लौटता नहीं। उसकी अंतिम-क्रिया करो, विधि-विधान के मुताबिक सब करो, उसका कल्याण हो ऐसा करो लेकिन वह जीवात्मा भटकता-भटकता तुम्हारे वातावरण में आकर दुःख सहे ऐसा नहीं करना चाहिए।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जो लोग भूत-प्रेतों को फँसाते हैं उनका कहना है कि जितने प्रेत मुसलमानों के कब्रिस्तान से मिल सकते हैं उतने हिन्दुओं के श्मशान से नहीं मिलते। ऋषियों ने गहरा रिसर्च किया था जीव जिस शरीर में रहता है- पच्चीस-पचास साल, साठ, सत्तर, अस्सी साल तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है. जिस घर में आप दस बीस साल रहते हैं उस घर में आपकी ममता हो जाती है। जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हैं वह आपके लिये छोटा हो जाता है। उतने ही अन्तर वाला अनजाना रास्ता आपके लिए लम्बा हो जाता है। यह मन का स्वभाव है। जहाँ आदत बन जाती है वह सरल हो जाता है।
इस शरीररूपी घर में जीव पचास-साठ साल रहता है। मृत्यु के कारण जब घर छोड़कर जाना पड़ता है तो फिर उसी घर में जाने की इच्छा होती है।
अगर शरीर को कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाय तो जीव इसके इर्द-गिर्द भटकता है। इसलिए प्राचीन भारत के ऋषियों ने देखा की आगे की यात्रा रूक न जाय, मरे हुए देह के इर्द गिर्द उसको भटकना न पड़े इसका उपाय करना चाहिए। अतः जल्दी से जल्दी मुर्द को अग्नि दाह कर दो और मुंडी से शुरूआत करो, क्योंकि विचार और संकल्प मस्तिष्क में होते हैं। वहीं घुसने की संभावना रहती है। देह को इस प्रकार भस्मीभूत किया जाता है ताकि इसमें से निकले हुए जीव की देह में आस्था खत्म हो जाय। वह अपनी आगे की मंगलमय यात्रा पर चल पड़े। फिर भी उसकी वासना गहरी हो, मोह-ममता गहरी हो तो देह जल जाने के बाद भी जहाँ वह मरा है उस माहौल में मंडराता रहे तो ऋषियों ने तीसरा दिन मनाने की व्यवस्था की।
मृत्यु के बाद तीसरे दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं। थोड़ी देर उसके बारे में बातचीत हो जाती है और उसे आखिरी विदा दे देते हैं। अगर वहाँ जीव मंडराता है तो देख लेता है कि, 'सम्बन्धियों ने तो पूरा सम्बन्धविच्छेद कर दिया है। यहाँ अब हमारा कोई स्थान नहीं। चलो आगे....।' उसकी आगे की यात्रा शुरू हो जाती है।
फिर बारहवाँ दिन मनाया जाता है, पिण्डदान किया जाता है।
श्राद्ध में एक बात का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध करते समय आँसू नहीं बहने चाहिए, अन्यथा श्राद्ध प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध के प्रसंग में किसी बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। उनकी खुशामद में, सूक्ष्म रूप में आगन्तुक पितरों का अनादर हो जाता है।
श्राद्ध करते समय भगवद् गीता के सातवें अध्याय का माहात्म्य पढ़कर पाठ करना चाहिए। उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए।
एक श्राद्ध यह होता है कि हमारे मरने के बाद हमारे बेटे करें। दूसरा श्राद्ध संन्यासियों का होता है जो जीते जी अपनी षोडशी कर लेते हैं।
हम चाहते हैं कि आप साधक लोग भी जीते जी अपनी षोडशी कर डालो। जीते जी मर जाओ एक बार।
मरो
मरो सब कोई
कहे मरना न
जाने कोई।
एक
बार ऐसा मरो
कि फिर मरना न
होई।।
बुद्ध के पास जब कोई भिक्षु बनने को आता तो बुद्ध बोलते कि एक बार मरकर फिर आ जाओ।
"कैसे मरें ?"
"जाओ स्मशान में। कोई मुर्दा जलता हो उसको देखो। उसके साथ अपने शरीर का तादात्म्य सोचो। किसी के धन के साथ, किसी के रूप-लावण्य के साथ एकता नहीं हो सकती। किसी का शरीर जल रहा है तो हमारा भी जलेगा इसमें एकता हो सकेगी। जब मुर्दा जलता हो तो हमारा जी भी जलेगा इसमें एकता हो सकेगी। जब मुर्दा जलता हो तो तब समझो कि मैं ही जल रहा हूँ.... मैं ही जल रहा हूँ.... मैं ही जल रहा हूँ....। आज तक जिसको मैं मान रहे रो उसको ठीक तरह से जलाकर आओ मन ही मन।"
इस प्रकार नये होने वाले भिक्षुकों को बुद्ध छः महीना तक सादृश्य योग करवाते। बाद में उन्हें दीक्षा देते।
तुम लोग श्मशान में जाकर सादृश्य योग करो यह संभव नहीं है। 'ईश्वर की ओर' पुस्तक में यह सादृश्य योग पद्धति है। उसको बार-बार पढ़ो। तुम्हारे मन और बुद्धि झख मारके ईश्वर में आयेंगे.....आयेंगे.... आयेंगी ही। दूसरी जगह जाने की उसकी ताकत नहीं।
भागवत की कथा के प्रारम्भ में आता है कि भक्ति रो रही थी। क्यों ? उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे। जिस माँ के दो-दो बेटे मूर्छित पड़े हों वह माँ तो रोयेगी ही। कलियुग में अगर भक्ति करना हो तो उसके दो बेटे जो ज्ञान और वैराग्य हैं उनको सचेत करना पड़ेगा । कलियुग में श्मशान में ज्ञान-वैराग्य को निवास करने का वरदान मिला है। शरीर से श्मशान में नहीं जाते तो मन से ही कभी-कभी श्मशान की मुलाकात कर लिया करो। कोई अर्थी जाती हुई दिखे तो मन को समझा दो, तेरी भी यही हालत होने वाली है। इससे विवेक वैराग्य बढ़ेगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
साधना
में सातत्य
सौ छोटे-छोटे पातक एक महापातक बनता है। सौ छोटे-छोटे पुण्य एक महा पुण्य बनता है। जब पुण्य का सिलसिला चलता है तब जीव सुखी रहता है। इस समय पाप करता है तो भी उसको धन-संपत्ति, सुख सुविधाएँ मिलती रहती हैं क्योंकि अभी पुण्यकाल का प्रकरण चल रहा है। जब प्रारब्ध का पाप प्रकरण चलता है तब अच्छा काम करते हुए भी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं दिखता।
ऐसे समय में किसी को निराश नहीं होना चाहिए। अपना जप-तप-ध्यान-अनुष्ठान-आत्म-विचार प्रतिदिन चालू रखना चाहिए। कल्मष कटते जाएंगे, अन्तःकरण पावन होता जाएगा. महापातक दूर होते जाएँगे तब जप, ध्यान, कीर्तन आदि का पूरा लाभ दिखेगा। तुलसीदास जी कहते हैं-
तुलसी जाके
मुखनते धोखे
निकसे राम।
ताके
पग की पगतरी
मोरे तन को
चाम।।
धोखे से भी जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है वह आदमी भी आदर के योग्य है। जो प्रेम से भगवान का चिन्तन, ध्यान करता है, भगवतत्त्व का विचार करता है उसके आदर का तो कहना ही क्या ? उसके साधन-भजन को अगर सत्संग का संपुट मिल जाय तो वह जरूर हरिद्वार पहुँच सकता है। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। वह गंगा किनारे वाला हरि द्वार नहीं, जहाँ से तुम चलते हो वहीं हरि का द्वार हो। संसार में घूम फिरकर जब ठीक से अपने आप में गोता लगाओगे, आत्म-स्वरूप में गति करोगे तब पता चलोगे कि हरिद्वार तुमसे दूर नहीं, हरि तुमसे दूर नहीं और तुम हरि से दूर नहीं।
वो
थे न मुझसे
दूर न मैं
उनसे दूर था।
आता
न था नजर तो नजर
का कसूर था।।
अज्ञान की नजर हटती है। ज्ञान की नजर निखरते निखरते जीव ब्रह्ममय हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह अनुभव हो जाता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जब
तक जीना तब तक
सीना.....
कई लोग भगवान के रास्ते चलते हैं। गलती यह करते हैं कि 'चलो, सबमें भगवान हैं।' ऐसा करके अपने व्यवहार का विस्तार करते रहते हैं। तत्त्वज्ञान के रास्ते चलने वाले साधक सोचते हैं कि सब माया में हो रहा है। ऐसा करके साधन-भजन में शिथिलता करते हैं और व्यवहार बढ़ाये चले जाते हैं।
अरे, माया में हो रहा है लेकिन माया से पार होने की अवस्था में भी तो जाओ साधन भजन करके ! साधन भजन छोड़ क्यों रहे हो ? 'जब तक जीना तब तक सीना।' जब तक जीवन है तब तक साधन-भजन की गुदड़ी को सीते रहो।
थोड़ा वेदान्त इधर-उधर सुन लिया। आ गये निर्णय पर 'सब प्रकृति में हो रहा है।' फिर दे धमाधम व्यवहार में। साधन भजन की फुरसत ही नहीं।
जो साधन-भजन छोड़ देते हैं वे शाब्दिक ज्ञानी बनकर रह जाते हैं। 'मैं भगवान का हूँ' यह मान लेते हैं और संसार की गाड़ी खींचने में लगे रहते हैं। अपने को भगवान का मान लेना अच्छा है। साधन-भजन का त्याग करना अच्छा नहीं। भगवान स्वयं प्रातःकाल में समाधिस्थ रहते हैं। शिवजी स्वयं समाधि करते हैं। रामजी स्वयं गुरू के द्वार पर जाते हैं, आप्तकाम पुरूषों का संग करते हैं। श्रीकृष्ण दुर्वासा ऋषि को गाड़ी में बिठाकर, घोड़ों को हटाकर स्वयं गाड़ी खींचते हैं। उनको ऐसा करने की क्या जरूरत थी ?
हम लोगों को थोड़े रूपये-पैसे, कुछ सुख-सुविधाएँ मिल जाती हैं तो बोलते हैं- 'अब भगवान की दया है। जब मर जायेंगे तब भगवान हमें पकड़कर स्वर्ग में ले जायेंगे।'
अरे भाई ! तू अपनी साधना की गुदड़ी सीना चालू तो रख ! बन्द क्यों करता है ? साधन-भजन छोड़कर बैठेगा तो संसार और धन्धा-रोजगार के संस्कार चित्त में घुस जायेंगे। 'जब तक जीना तब तक सीना।' जीवन का मंत्र बना लो इसे।
चार पैसे की खेतीवाला सारी जिन्दगी काम चालू रखता है, चार पैसे की दुकानवाला सारी जिन्दगी काम चालू रखता है, चार पैसे का व्यवहार सम्भालने के लिए आदमी सदा लगा ही रहता है। मर जाने वाले शरीर को भी कभी छुट्टी की ? श्वास लेने से कभी छुट्टी ली ? पानी पीने से छुट्टी की ? भोजन करने से छुट्टी की ? नहीं। तो भजन से छुट्टी क्यों ?
'जब तक जीना तब तक सीना.... जब तक जीना तब तक सीना।' यह मंत्र होना चाहिए जीवन का।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जब
तक और तब तक
जब तक तुम्हें अपना लाभ और दूसरे का नुकसान सुखदायक प्रतीत होता है, तब तक तुम नुकसान ही उठाते रहोगे।
जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा प्यारी लगती है, तब तक तुम निन्दनीय ही रहोगे।
जब तक तुम्हें अपना सम्मान और दूसरे का अपमान सुख देता है, तब तक तुम अपमानित ही होते रहोगे।
जब तक तुम्हें अपने लिए सुख की और दूसरे के लिए दुःख की चाह है, तब तक तुम सदा दुःखी रहोगे।
जब तक तुम्हें अपने को न ठगाना और दूसरों को ठगना अच्छा लगता है, तब तक तुम ठगाते ही रहोगे।
जब तक तुम्हें अपने दोष नहीं दीखते और दूसरे में खूब दोष दीखते हैं, तब तक तुम दोषयुक्त ही रहोगे।
जब तक तुम्हें अपने हित की और दूसरे के अहित की चाह है, तब तक तुम्हारा अहित ही होता रहेगा।
जब तक तुम्हें सेवा कराने में सुख और सेवा करने में दुःख होता है, तब तक तुम्हारी सच्ची सेवा कोई नहीं करेगा।
जब तक तुम्हें लेने में सुख और देने में दुःख का अनुभव होता है, तब तक तुम्हें उत्तम वस्तु कभी नहीं मिलेगी।
जब तक तुम्हें भोग में सुख और त्याग में दुःख होता है तब तक तुम असली सुख से वंचित ही रहोगे।
जब तक तुम्हें विषयों में प्रीति और भगवान में अप्रीति है, तब तक तुम सच्ची शान्ति से शून्य ही रहोगे।
जब तक तुम शास्त्रों में अश्रद्धा और मनमाने आचरणों में रति है, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
जब तक तुम्हें साधुओं से द्वेष और असाधुओं से प्रेम है, तब तक तुम्हें सच्चा सुपथ नहीं मिलेगा।
जब तक तुम्हे सत्संग से अरूचि और कुसंग में प्रीति है, तब तक तुम्हारे आचरण अशुद्ध ही रहेंगे।
जब तक तुम्हें जगत में ममता और भगवान से लापरवाही है, तब तक तुम्हारे बन्धन नहीं कटेंगे।
जब तक तुम्हें अभिमान से मित्रता और विनय से शत्रुता है, तब तक तुम्हें तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा।
जब तक तुम्हें बाहरी रोगों से डर है और काम-क्रोधादि भीतरी रोगों से प्रीति है, तब तक तुम निरोगी नहीं हो सकोगे।
जब तक तुम्हें धर्म से उदासीनता और अधर्म से प्रीति है, तब तक तुम सदा असहाय ही रहोगे।
जब तक तुम्हें मृत्यु का डर है और मुक्ति की चाह नहीं है, तब तक तुम बार-बार मरते ही रहोगे।
जब तक तुम्हें घर-परिवार की चिन्ता है और भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है, तब तक तुम्हें चिन्तायुक्त ही रहना पड़ेगा।
जब तक तुम्हें प्रतिशोध से प्रेम है और क्षमा से अरूचि है, तब तक तुम शत्रुओं से घिरे ही रहोगे।
जब तक तुम्हें विपत्ति से भय है और प्रभु में अविश्वास है, तब तक तुम पर विपत्ति बनी ही रहेगी।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
राम
जी का जीवन
अनादि काल से सृष्टि चली आ रही है। हर प्राणी अनन्त जन्मों की यात्रा करता हुआ ईश्वर कृपा से मनुष्य तन पाता है। इस मानव को अपने आत्म-स्वभाव में जगाने के लिए परात्पर परब्रह्म परमात्मा साकार रूप धारण करके नरलीला करते हैं। काश ! नर अपने नारायण-स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाय।
श्रीरामचन्द्रजी मानव रूप में धरती पर रहते हैं। धरती पुत्र वाल्मीकि उनके चरित्र गायक हैं। धरती-पुत्री सीता उनकी धर्मपत्नी हैं। धरती को सिर पर धारण करने वाले शेष लक्ष्मण उनके भाई हैं। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी को धरती के लोगों से सम्बन्ध है।
हे धरती के लोगों ! श्रीरामचन्द्रजी के विलक्षण लक्षण अपने जीवन में बढ़ाते जाएँ। उनके ऐसे कोई गुण नहीं जो मनुष्य के लिए असंभव या अग्राह्य हो। सतत सावधान रहो। साधारण व्यक्तियों के लक्षण और आकर्षण से अपने को बचाकर श्रीरामचन्द्रजी के गुण और लक्षण अपने में प्रकटाते जाओ, बढ़ाते जाओ।
उनका धर्म केवल यज्ञशाला में ही सीमित नहीं होता है अपितु जीवन के सभी प्रसंगों में सम्पन्न हो रहा है। श्रीरामजी का जीवन आत्मज्ञान के मुताबिक चलता है और स्थितप्रज्ञ होने के लिए अनुकरणीय है। आओ, जरा देखें- श्री वाल्मीकि जी कितना सुन्दर वर्णन कर रहे हैं !
रामजी कभी महलों में रहते हैं तो कभी वनवास, कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कन्दमूल, कभी हँसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी प्रसन्न रहते हैं तो कभी व्याकुल भी हो जाते हैं, कभी संयोग होता है तो कभी वियोग होता है, कभी एकान्त में चिन्तन करते हैं तो कभी युद्धभूमि में युद्ध करना पड़ता है। सबके जीवन में सुख-दुःख आते हैं, अनुकूलता-प्रतिकूलता आती है, न्याय-अन्याय आता है। हम अपने मन को ठीक रखते हैं तो इन सारी परिस्थितियों में अपने साक्षीत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
श्रीरामचन्द्रजी भीतर से सदा शान्त और सम रहते थे। वे ऐसे मीठे वचन बोलते थे कि उनमें सुनने वाले के प्रति स्नेह, सान्त्वना और सहानुभूति भरी रहती थी।
आप भी प्यारे रामजी का अनुकरण कीजिए, आपका व्यवहार भक्ति होने लगेगा।
यदि रामचन्द्रजी से कोई कठोर बात कह देता था तो वे उसकी उपेक्षा कर देते थे, उसका उत्तर नहीं देते थे, चुप लगा जाते थे। आपके जीवन में जब ऐसा प्रसंग आये तो मन को समझाओः उसकी जगह पर मैं होता और मेरी बुद्धि ऐसी होती तो मैं भी ऐसा ही करता। अतः अपने ज्ञान और विवेक को सजग रखकर सम रहने का अभ्यास कीजिए।
'मैं राजपुत्र हूँ.... सर्वशक्तिमान हूँ..... इसने ऐसा क्यों कहा...?' इस प्रकार की और प्रतिरोध की भावना रामजी में नहीं आती थी।
अपने मन पर उनका इतना नियँत्रण था कि कोई चाहे सैंकड़ों अपराध करे, वे अपने मन में उसकी याद नहीं रखते। एक भी उपकार कोई कर दे तो उसको भूलते नहीं थे।
हम गलती यह करते हैं कि किसी के गुण हमसे याद नहीं रह पाते और उसके दोष पकड़ रखते हैं। रामजी किसी के दोष अपनी स्मृति में नहीं आने देते और सामने वाले के उपकार भूलते नहीं।
शीलवृद्धैज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च
सज्जनैः।
कथयन्नास्ति
वै
नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि।।
शास्त्रास्त्रों के अभ्यास के समय भी बीच-बीच में अवसर निकालकर शील, ज्ञान तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरूषों का सत्संग पाकर रामजी उनसे शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे।
शील किसे कहते हैं ?
अद्रोहः
सर्वभूतेषु
कर्मणा मनसा
गिरा।
अनुग्रहश्च
दानं च
शीलमेतत्
प्रतिष्ठते।।
'मन-वचन कर्म से किसी के प्रति द्रोह न करने का नाम ही शील है।'
जब मन में किसी के प्रति द्वेष आता है तब उसकी परिणति क्रोध के रूप में हो जाती है। फिर क्रोध हिंसा में बदल जाता है। हिंसा द्रोह का रूप धारण कर लेती है। इसलिए शीलवृद्ध सत्पुरूष अपने मन में द्वेष को स्थिर नहीं होने देते, उसे बार-बार धोते रहते हैं।
ज्ञानवृद्ध सत्पुरूषों की यह विशेषता है कि वे अज्ञानमूलक दोषों का निवारण करते रहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दोष आते हैं वे सब अज्ञानमूलक ही होते हैं। वेदान्तियों, नैयायिकों, यहाँ तक कि बौद्धों की भी यह मान्यता है कि अविद्या ही समस्त दोषों की जननी है। योग में अविद्या मानते हैं, सांख्य में अविवेक मानते हैं और वेदान्त में तो अज्ञान शब्द प्रसिद्ध है ही। इस अविवेक, अविद्या अथवा अज्ञान से ही सारे दोष उत्पन्न होते हैं।
कहीं-कहीं यह देखने में आता है कि ज्ञान हो जाने पर भी दोष बने रहते हैं। इसका कारण यही होता है कि हम प्रमादवश अपने ज्ञान के अनुसार जीवन का निर्माण नहीं कर पाते। यदि हमारे विवेक और हमारी चर्चा दोनों का मेल हो जाय तो मनुष्य का जीवन परम पवित्र हो जाता है।
इसी तरह जो आयु-वृद्ध होते हैं, उनके पास जीवन का विशाल अनुभव होता है और उस विशाल अनुभव के आधार पर मनुष्य अपने कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निर्णय करने में समर्थ होता है। मनुजी महाराज तो कहते हैं कि जो मनुष्य अपने से वयोवृद्धों का अभिवादन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करता रहता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल इन चारों चीजों की वृद्धि होती है।
अभिवादनशीलस्य
नित्यं
वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि
तस्य
वर्द्धन्ते
आयुर्विद्या
यशो बलम्।।
श्रीरामचन्द्रजी शीलवृद्धों, ज्ञानवृद्धों और आयुवृद्धों की संगति इसीलिए करते हैं कि उससे उनको एक समझ मिलती रहती है। जैसा संग होता है, वैसा ही रंग चढ़ता है। संग से ही पता चलता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है ?
वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे मृगनाभि में छिपी रहने पर भी कस्तूरी अपनी सुगन्धि फैलाती रहती है, वैसे ही श्रीरामचन्द्र के व्यक्तित्व की सुगन्धि सबको आह्लादित करती रहती है।
बुद्धिमान्
मधुराभाषी
पूर्वभाषी
प्रियंवदः।
वीर्यवान्न
य वीर्येण
महता स्वेत
विस्मितः।।
श्रीरामचन्द्रजी परम बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थे। जब कोई उनसे मिलता था तब वे बड़े प्रेम के साथ उससे बात करते थे और उसके बोलने के पहले ही अपनी ओर से बातचीत प्रारम्भ कर देते थे, जिससे कि उसको अपनी बात कहने में कोई संकोच न हो। अत्यंत बलवान और पराक्रमी होने पर भी उनको कभी अभिमान नहीं हुआ। उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि उनके पास आने वाला व्यक्ति पहले उनको नमस्कार करे, उनका अभिवादन करे और अपनी बात कह ले तब उसको उत्तर दें।
न
चानृतकथो
विद्वान
वृद्धानां
प्रतिपूजकः।
अनुरक्तः
प्रजाभिश्च
प्रजाश्चाप्यनुरज्यते।।
झूठी बात तो श्रीरामचन्द्रजी के मुख से निकलती नहीं थी। वे सदा अपने से बड़े-बूढ़ों का सम्मान किया करते थे। उनका प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। इसी प्रकार प्रजा भी उनसे बड़ा प्रेम करती थी।
सृष्टि में ध्वनि-प्रतिध्वनि सुविदित तथ्य है। इसलिएः
वाणी
ऐसी बोलिए जो
मनवा शीतल
होय।
औरन
को शीतल करे आपहुं
शीतल होय।।
फिर वाल्मीकि जी कहते हैं-
नाश्रेयसी
रतो यश्च न
विरूद्धकथारूचिः।
उत्तरोत्तरयुक्तीनां
वक्ता
वाचस्पतिर्यथा।।
अरोगस्तरूणो
वाग्मी
वपुष्मान्
देशकालवित्।
लोके
पुरूषसारज्ञः
साधुरेको
विनिर्मितः।।
श्रीरामचन्द्रजी जो कुछ बोलते थे, अवसरोचित बोलते थे। इस बात का बराबर ध्यान रखते थे कि उनकी वाणी से किसी को कोई उद्वेग न हो। अमंगलकारी वार्तालाप में उनकी कभी रूचि नहीं होती थी।
देखो, बहुधा लोग दुःखद समाचार पहुँचाने में बड़ी जल्दी क्रिया करते हैं। कभी-कभी तो ऐसे ढंग से सुनाते हैं कि सुननेवाले का दुःख और बढ़ जाये। उचित तो यह है कि दुःखद समाचार सुनाने पड़े तो ऐसी भूमिका बनाकर सुनाएँ, ऐसे ढंग से सुनाएँ कि सुनने वाले को दुःख कम हो।
श्रीराम सदा अवसरोचित भाषण करते थे। कई लोग इस कला से अनभिज्ञ होते हैं इसलिए समाज में उनकी वाणी का इतना आदर नहीं होता, वे मान नहीं पाते। अवसर हो शादी-ब्याह का वहाँ मृत्यु की बात करना, अवसर हो स्मशान यात्रा का वहाँ शादी-ब्याह की बात करना यह अवसर-अनुचित बात कही जाती है।
श्रीरामचन्द्रजी सामनेवाले की बात सुनते भी खूब थे। वे यह जानते थे कि यदि सामनेवाले की किसी बात से स्वयं उसकी अथवा अन्य किसी की हानि होती हो तब तो उसका विरोध कर देना चाहिए, अन्यथा यदि वह अपनी बात कह रहा है तो अकारण उसके विरूद्ध नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा गया कि श्रीरामचन्द्रजी विरूद्धभाषी नहीं थे।
यदि कहीं किसी विषय पर शास्त्र का तात्पर्य बताना हो और वहाँ दो पक्ष हो गये हों तो जिस पक्ष को श्रीरामचन्द्रजी ठीक समझते थे, उसका प्रतिपादन करने के लिए वे उत्तरोत्तर युक्तियाँ उपस्थित करते जाते थे। ऐसे अवसरों पर प्रतीत होता था कि वे साक्षात् बृहस्पति हैं। वे प्रतिपक्षी को मृदुतापूर्वक यह समझाने का प्रयास करते थे कि देखो, हमारे पक्ष का अमुक हेतु है और उसके समर्थन में अमुक प्रमाण हैं। आवश्यकता पड़ने पर श्रीरामचन्द्रजी इतिहास का भी उद्धरण उपस्थित करते हुए यह बताते थे कि उस समय जो निश्चत हुआ था, उससे उनके पक्ष का समर्थन होता है। उनका कहने का ढंग ऐसा होता था कि सामने वाले को क्षोभ न हो। वह अपमानित न हो और उसमें सही पक्ष का आदर होने लगे। ऐसा नहीं कि वह विरोधी बन जाय। इस प्रकार वे अपने मत का प्रतिपादन करते थे। उनको अकारण अपनी वाणी का अपक्षय करना पसन्द नहीं था।
दृढ़भक्ति
स्थिरप्रज्ञो
नासद् ग्राही
न दुर्वचः।
निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्च
स्वदोषपरदोषवित्।।
श्रीरामचन्द्रजी के हृदय में सदगुरूओं के प्रति दृढ़ भक्ति थी। वे स्थिर प्रज्ञ थे। उनके लिए असद् वस्तुएँ अग्राह्य थीं और उनके मुँह से कभी किसी के प्रति दुर्वचन नहीं निकलता था। उनका जीवन आलस्य एवं प्रमाद से सर्वथा रहित था। वे दूसरों के दोषों को तो जानते ही थे, उससे भी अधिक अपने दोषों से परिचित थे और उनके लिए पश्चाताप भी प्रकट करते थे।
एक बार श्रीरामचन्द्रजी को इस बात के लिए पछतावा होने लगा कि भरत जैसे शरणागत, सहृदय और भक्त पुरूष ने मेरे चरणों पर सिर रखकर मुझसे अयोध्या लौट चलने की बार-बार प्रार्थना की, लेकिन मैं उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर सका। इससे बढ़कर मेरा दोष और क्या हो सकता है !
श्रीराम यह अच्छी तरह जानते थे कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वथा निर्दोष नहीं है। अपराध मुझसे भी हुए हैं, जानकी से भी हुए हैं, लक्ष्मण से भी हुए हैं, यहाँ तक कि मेरे माता-पिता से भी हुए हैं। इसलिए हमको किसी के अपराध पर दृष्टि न डालकर उसकी अच्छाई पर दृष्टि डालनी चाहिए।
जिनकी ऐसी दृष्टि रहती है उनके पराये भी अपने हो जाते हैं। जिनकी दोष दृष्टि रहती है उनके अपने भी पराये हो जाते हैं। व्यक्ति अपने विकास के लिए अपने गुण भूल जाय और दूसरों के दोषों को भूल जाय। अपने दोषों को कठोरतापूर्वक, निकाले और दूसरों के गुणों का प्रयत्नपूर्वक आदर करे।
शास्त्रज्ञश्च
कृतज्ञश्च
पुरूषान्तरकोविदः।
यः
प्रग्रहानुग्रहयोर्यथान्यायं
विचक्षणः।।
श्रीरामचन्द्रजी शास्त्रज्ञ, कृतज्ञ और दूसरे पुरूषों के मनोभावों को जानने में तो कुशल थे ही, यह भी अच्छी तरह जानते थे कि कब कहाँ किसको दण्ड देना चाहिए तथा कब कहाँ किस पर अनुग्रह करना चाहिए। वे यह निर्णय करने में निपुण थे कि कहाँ संयम, कहाँ दण्ड और कहाँ क्षमा का प्रयोग करना चाहिए।
सत्संग्रहानुग्रहणे
स्थानविन्निग्रहस्य
च।
आयकर्मण्युपायज्ञः
संदृष्टव्यय-कर्मवित्।।
रामजी को अर्थ के उपार्जन, संरक्षण और वितरण की विधि का भी ज्ञान था। वे अर्थशास्त्र में इतने निपुण थे कि अपनी आय का यथायोग्य बँटवारा करके उसको अपने उपयोग में लाते थे।
दया में, धर्म में, दान में धन का सदुपयोग होता है तो वह धन इहलोक और परलोक में सुख देने वाला होता है। गृहस्थी को उचित है कि आय का 20 प्रतिशत संग्रह करे, 20 प्रतिशत परलोक, पुण्य-अर्जन के लिए खर्चे। कंजूस का धन न अपने परिजनों के लिए काम आता है न अपने लिए काम आता है और न परलोक सँवारने के काम आता है।
धन की तीन गतियाँ कही गई हैं- उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग, कनिष्ठ गति संग्रह। कनिष्ठ धन अग्नि, राजा या चोर हड़प लेते हैं।
धन का अगर सदुपयोग हो तो अपने लिए, अपने परिजनों के लिए और परलोक के लिए हितकर होता है। रामचन्द्रजी इस बात को अच्छी तरह जानते थे और व्यवहार में लाते थे। वे यज्ञयाग और दान पुण्य खूब करते थे।
जब दशरथ जी ने बहुत निकट से श्रीरामचन्द्रजी के विविध गुणों का अनुसन्धान कर लिया तब उनके मन में श्रीरामचन्द्रजी को युवराज-पद पर अभिषिक्त करने की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। उन्होंने इस सम्बन्ध में मंत्रणा करने के लिए एक बहुत बड़ी सभा बुलायी। उसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के राजा, सामन्त तथा मुख्य-मुख्य प्रजाजन सम्मिलित हुए। राजा दशरथ ने अपने पुरोहितों, मन्त्रियों के अतिरिक्त श्रीरामचन्द्रजी को भी उस सभा में बुला लिया और फिर सबके सामने कहाः
"सभासदों ! मैं अपनी शक्ति के अनुसार अपने पूर्वजों का यथानुसरण करता हुआ प्रजाजनों की रक्षा करता आ रहा हूँ। अब इस सात्त्विक श्वेत राजछत्र की छाया में शासन सँभालते-सँभालते मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है और मैं प्रजा-रक्षण का उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थता का अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने बड़े पुत्र रामचन्द्र को प्रजा की रक्षा में नियुक्त करके राज-कार्य से विश्राम ग्रहण करना चाहता हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि रामचन्द्र मुझसे सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। इनका बल-पराक्रम ऐसा है कि बड़े से बड़ा शक्तिशाली शत्रु इनके सामने टिक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों के लिए सर्वोत्तम स्वामी सिद्ध होंगे। यदि आप लोगों को मेरा प्रस्ताव अनुकूल जान पड़े और मैंने जो कुछ सोचा है, वह उचित प्रतीत होता हो तो आप लोग मुझे सहर्ष अनुमति दीजिए अथवा बताइये कि मुझे इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए। यद्यपि मेरे लिये रामचन्द्र को युवराज बनाना बड़ा आनन्दवर्धक है तथापि आप लोग संकोच में पड़कर मेरी हाँ-में-हाँ मत मिलाइये, गुण-अवगुण की दृष्टि से कोई दूसरी हितकर बात आप लोगों के ध्यान में हो तो मुझे निःसंकोच बताइये।"
कितनी विशाल दृष्टि है निर्णय लेने में ! गुणग्राह्यता, न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता और उम्र होने पर राजकाज से विश्राम ग्रहण करके अपनी विश्राम-प्रियता भी इसमें प्रकट की है।
प्रवृत्ति ऐसी हो कि प्रवृत्ति करने की आसक्ति मिट जाय। प्रवृत्ति करने का जहाँ से सामर्थ्य आता है उस परमात्मा में विश्रांति पाकर मुक्त हो जाय।
कर्म के पहले विश्रांति होती है। कर्म के बाद विश्रांति होती है। कर्म ऐसे हों कि जीव को अपने शिवस्वरूप में विश्रांति दिला दे।
दशरथ जी की बात सुनते ही सारी सभा ने एक स्वर से हर्ष-ध्वनि के साथ उसका अनुमोदन किया और कहा कि, "महाराज ! हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। निःसन्देह आप वृद्ध हो गये हैं। इसलिए आप पृथ्वी का पालन करने में समर्थ श्रीरामचन्द्र का युवराज पद पर अभिषेक अवश्य कीजिए।"
यह सुनकर राजा दशरथ को भीतर ही भीतर प्रसन्नता तो बहुत हुई, मगर वे उसको छिपाते हुए कहने लगे किः "आप लोगों ने जो बिना सोचे समझे मेरे विचार का इतनी जल्दी समर्थन कर दिया, इससे मुझे कुछ संशय हो रहा है। कृपया यह तो बताइये कि आप लोग मेरे रहते रामचन्द्र को युवराज क्यों बनाना चाहते हैं ?"
इस प्रश्न के उत्तर में सभा के प्रतिनिधि वक्ताओं ने कहा किः "महाराज ! हम लोग श्रीरामचन्द्रजी को इसलिए युवराज बनाना चाहते हैं कि उनमें बहुत सारे सदगुण हैं। वे अपनी प्रजा के लिए चन्द्रमा के समान सुखदायी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, पृथ्वी के समान क्षमाशील और देवराज इन्द्र के समान बलवान हैं। उनमें धर्मज्ञता है, कृतज्ञता है, सत्यवादिता है और जितेन्द्रियता है। वे स्थिर बुद्धि हैं, मृदुभाषी हैं, शीलवान हैं और दीन-दुःखियों के प्रति सहानुभूति संपन्न हैं। बहुश्रुत विद्वानों और वयोवृद्धों का सत्संग निरन्तर करते रहने के कारण उनके यश एवं तेज का विस्तार हो रहा है। उनका स्वभाव इतना कोमल और संवेदनशील है कि जब कभी नगर-निवासियों पर संकट आ जाता है तब वे उनसे भी अधिक दुःखी हो जाते हैं, उनके दुःख निवारण के लिए तत्पर हो जाते हैं।
वे जब किसी को दुःखी देखते हैं तब यह अनुभव करते हैं कि मैं अपने पिता दशरथ जी की छत्रछाया में अपनी प्रजा की देखभाल करता हूँ। इसलिए यदि किसी को दुःख होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी ही असावधानी के कारण इसको इतना दुःख हो रहा है। यह सोचकर वे स्वयं दुःखी होते और दुःखी व्यक्ति के दुःख का निवारण करते।"
ऐसी रीति-नीति थी भगवान श्रीरामचन्द्रजी की।
सभासदों ने आगे कहा किः "महाराज ! श्रीरामचन्द्रजी ऐसे हैं जो सदा सबसे मुस्कुराकर बात करते हैं। उन्होंने सब प्रकार से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे सबकी भलाई करते हैं। निन्दनीय बातों की चर्चा में तो कभी उनकी रूचि होती ही नहीं। वे कभी ऐसी कोई बात करना पसन्द नहीं करते कि किसी से बिगाड़ हो जाय, विग्रह हो जाय।
बहुत सारे बिगाड़ और विग्रह निन्दनीय बातों से और विचारों से होते हैं। शस्त्र का घाव तो भर जाता है लेकिन कटु वचन का घाव नहीं मिटता। अतः निंदनीय बातें और कटु वचन अपने दिल को भी उद्विग्न करते हैं, अपनी योग्यताएँ क्षीण करते हैं। व्यर्थ का वैमनस्य और विग्रह पैदा होता है।
जीवन बड़ा कीमती है। वैमनस्य और विग्रह में अपनी शक्तियों को क्षीण क्यों करे ? हे साधक ! व्यर्थ की चर्चा और व्यर्थ वाणी-विलास करने से अपने को बचाओ। जीवन में श्रीरामचन्द्रजी के गुण प्रकटाओ और स्थिर प्रज्ञ हो जाओ।
रामो
विग्रहवान्
धर्मः।
धर्म की मूर्ति को प्रत्यक्ष देखना हो तो श्रीरामचन्द्रजी को देख लो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सत्गुरू
का प्यार लिख
दे
लिखनेवाले तू हो के दयाल लिख दे,
मेरे हृदय के अन्दर सत्गुरू का प्यार लिख दे।
माथे पे लिखे दे ज्योति गुरों की,
नयनों में उनका दीदार लिख दे।। मेरे.....।।
जिभ्या पे लिख दे नाम गुरू का,
कानों में शब्द झंकार लिख दे।।मेरे......।।
हाथों पे लिख दे सेवा गुरू की,
तन मन धन उनपे वार लिख दे।।मेरे........।।
पैरों पे लिख दे जाना गुरू के द्वार,
सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे।।मेरे......।।
इक मत लिखना गुरू का बिछड़ना,
चाहे तू सारा संसार लिख दे।।मेरे........।।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
दर्शन-श्रवण
को दिव्य
बनाएँ
आँखों से और कानों से संसार भीतर घुसता है। आँखों को भगवान के प्राकृतिक दृश्य दिखाते जाएँ, भगवान के श्रीविग्रह दिखाते जाएँ, हृदय में भगवतभाव बढ़ाते जाएँ। कानों से भगवान की गुणलीला अथवा भगवान का तात्त्विक साक्षी स्वरूप का श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके नश्वर आकर्षणों को मिटाते जाएँ, अपने शाश्वत आत्म खजाने को पाते जायें।
सुनने
और देखने में
सावधान !
ऐसे ढंग से देखो कि जिससे देखा जाता है उसकी याद आ जाय। ऐसा सुनो कि जिसके श्रवण के बाद सुनना, जानना, पाना कुछ बाकी न रहे। यही तुम्हारा उत्तम पुरूषार्थ है। चलते-फिरते, हँसते-रोते, खाते-पीते, लेते-देते, घर में, बाजार में जो यह उत्तम धर्म निभाता है उसके सारे कर्म यज्ञार्थ हो जाते हैं। वह जीते जी मुक्त, सब आपदाओं से रहित हो जाता है। सारी सफलता और सुखों का स्रोत उसे मिल जाता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ