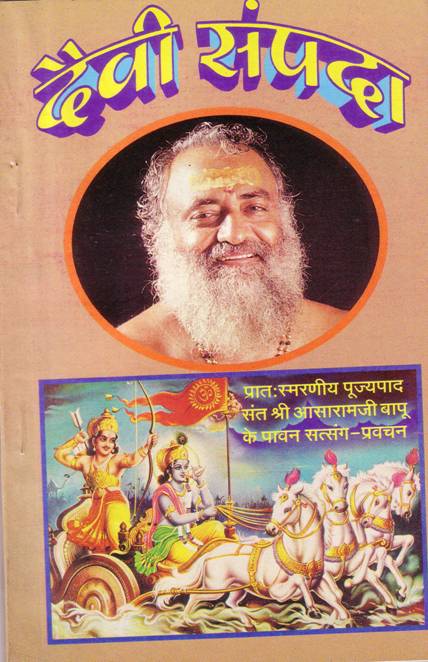
प्रातः
स्मरणीय परम
पूज्य
संत
श्री
आसारामजी
बापू के
सत्संग-प्रवचन
दैवी
संपदा
निवेदन
जितने भी दुःख, दर्द, पीड़ाएँ हैं, चित्त को क्षोभ कराने वाले.... जन्मों में भटकानेवाले...... अशांति देने वाले कर्म हैं वे सब सदगुणों के अभाव में ही होते हैं
भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन में कैसे सदगुणों की अत्यंत आवश्यकता है यह भगवद् गीता के 'दैवासुरसम्पदाविभागयोग' नाम के सोलहवें अध्याय के प्रथम तीन श्लोंकों में बताया है। उन दैवी सम्पदा के छब्बीस सदगुणों को धारण करने से सुख, शांति, आनन्दमय जीवन जीने की कुंजी मिल जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि दैवी सम्पदा आत्मदेव की है।
इस ग्रंथ में संतों ने सरल और उत्साह-प्रेरक प्रवचनों के द्वारा दैवी सम्पदा में स्थित भक्तों के, संतों के जीवन-प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए हमें प्रसाद बाँटा है। आप इस ज्ञान-प्रसाद का पठन-मनन करेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे।
विनीत,
श्री
योग वेदान्त
सेवा समिति
अहमदावाद
आश्रम
'गुरुत्यागात्
भवेन्मृत्युः.....'
दैवी
सम्पदा – (१)
(दिनांकः २२-७-१९९० रविवार, अहमदावाद आश्रम)
अभयं
सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः
।
दानं
दमश्च
यज्ञश्च
स्वाध्यायस्तप
आर्जवम् ।।
'भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञान के लिए ध्यानयोग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्त्विक दान, इन्द्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेदशास्त्रों का पठन-पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का संकीर्तन, स्वधर्मपालन के लिए कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता – ये सब दैवी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं।'
(भगवद्
गीताः१६.१)
जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। भय पाप है, निर्भयता जीवन है। जीवन में अगर निर्भयता आ जाय तो दुःख, दर्द, शोक, चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं। भय अज्ञानमूलक है, अविद्यामूलक है और निर्भयता ब्रह्मविद्यामूलक हैं। जो पापी होता है, अति परिग्रही होता है वह भयभीत रहता है। जो निष्पाप है, परिग्रह रहित है अथवा जिसके जीवन में सत्त्वगुण की प्रधानता है वह निर्भय रहता है।
जिसके जीवन में दैवी लक्षण हैं वह यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक भी उसके लिए सुखमय हो जाता है। जिसके जीवन में दैवी लक्षण की कमी है वह यहाँ भी दुःखी रहता है और परलोक में भी दुःख पाता रहता है। जीवन में अगर सुख, चैन, आराम, अमन-चमन चाहिए तो 'अमन होना पड़ेगा। अमन माना मन के संकल्प-विकल्प कम हों। अमनी भाव को प्राप्त हो तो जीवन में चमन बढ़ता है।
मनुष्य की वास्तविक अंतरात्मा इतनी महान् है कि जिसका वर्णन करते वेद भगवान भी 'नेति.... नेति.....' पुकार देते हैं। मानव का वास्तविक तत्त्व, वास्तविक स्वरूप ऐसा महान् है लेकिन भय ने, स्वार्थ ने, रजो-तमोगुण के प्रभाव ने उसे दीन-हीन बना दिया है।
दुःख मनुष्य का स्वभाव नहीं है इसलिए वह दुःख नहीं चाहता है। सुख मनुष्य का स्वभाव है इसलिए वह सुख चाहता है। जैसे, मुँह में दाँत रहना स्वाभाविक है तो कभी ऐसा नहीं होता कि दाँत निकालकर फेंक दूँ। जब तक दाँत तन्दुरुस्त रहते हैं तब तक उन्हें फेंकने की इच्छा नहीं होती। भोजन करते वक्त कुछ अन्न का कण, सब्जी का तिनका दाँतों में फँस जाता है तो लूली (जिह्वा) बार-बार वहाँ लटका करती है। जब तक वह कचरा निकला नहीं जाता तब तक चैन नहीं लेती। क्योंकि दाँतों में वह कचरा रहना स्वाभाविक नहीं है।
ऐसे ही सुख तुम्हारे जीवन में आता है तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन दुःख आता है तो उसे निकालने के लिए तुम तत्पर हो जाते हो। दाँतों में तिनका रहना अस्वाभाविक लगता है वैसे हृदय में दुःख रहना तुम्हें अस्वाभाविक लगता है। दुःख होता है रजो-तमोगुण की प्रधानता से।
भगवान कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव कर दें। जीवन में भय न आवे। निर्भय रहें। निर्भय वही हो सकता है जो दूसरों को भयभीत न करें। निर्भय वही रह सकता है जो निष्पाप होने की तत्पर हो जाय। जो विलासरहित हो जायगा वह निर्भय हो जायगा।
निर्भयता ऐसा तत्त्व है कि उससे परमात्म-तत्त्व में पहुँचने की शक्ति आती है। किसी को लगेगा कि 'बड़े-बड़े डाकू लोग, गुन्डा तत्त्व निर्भय होते हैं....' नहीं नहीं..... पापी कभी निर्भय नहीं हो सकता। गुन्डे लोग तो कायरों के आगे रोब मारते हैं। जो लोग मुर्गियाँ खाकर महफिल करते हैं, दारू पीकर नशे में चूर होते हैं, नशे में आकर सीधे-सादे लोगों को डाँटते हैं तो ऐसी डाँट से लोग घबरा जाते हैं। लोगों की घबराहट का फायदा गुन्डे लोग उठाते हैं। वास्तव में चंबल की घाटी का हो चाहे उसका बाप हो लेकिन जिसमें सत्त्वगुण नहीं है अथवा जो आत्मज्ञानी नहीं है वह निर्भय नहीं हो सकता। निर्भय वही आदमी होगा जो सत्त्वगुणी हो। बाकी के निर्भय दिखते हुए लोग डामेच होते हैं, पापी और पामर होते हैं। भयभीत आदमी दूसरे को भयभीत करता है। डरपोक ही दूसरे को डराता है।
जो पूरा निर्भय होता है वह दूसरों को निर्भय नारायण तत्त्व में ले जाता है। जो डर रहा है वह डरपोक है। डामेच और गुंडा स्वभाव का आदमी दूसरों का शोषण करता है। निर्भीक दूसरों का शोषण नहीं करता, पोषण करता है। अतः जीवन में निर्भयता लानी चाहिए।
बंगाल में हुगली जिले के देरे गाँव में खुदीराम नाम के व्यक्ति रहते थे। गाँव के जुल्मी जमींदार ने उन्हें अपने मुकद्दमें में झूठी गवाही देने के लिए दम मारा। उन्हें डराते हुए वह बोलाः
"राजा के आगे मेरे पक्ष मं गवाही दे दो। राजा तुम पर विश्वास करेंगे और मेरा काम बन जायेगा। अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले तो जानते हो, मैं कौन हूँ? मैंने कइयों के घरों को बरबाद कर दिया है। तुम्हारा भी वही हाल होगा। देरे गाँव में रहना असंभव हो जाएगा।"
खुदीराम ने निर्भयता से जवाब दे दियाः "गाँव में रहना असंभव हो जाये तो भले हो जाय लेकिन मैं झूठी गवाही हरगिज नहीं दूँगा। मैं तो जो सत्य है वही बोल दूँगा।"
उस दुष्ट ने खुदीराम को परेशान करना शुरु कर दिया। खुदीराम बेचारे सीधे सादे प्रामाणिक इन्सान थे। वे गाँव छोड़कर चले गये। कई बिघा, जमीन, गाय-भैंस, घर-बार की हानि हुई फिर भी सत्य पर खुदीराम अडिग रहे।
लोगों की नजरों में खुदीराम को हानि हुई होगी थोड़ी-बहुत लेकिन सत्य की गवाही देने में अडिग रहने से खुदीराम ईश्वर को, परमात्मा को स्वीकार हो गये। गाँव छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़नी पड़ी, निर्भीक रहकर सत्य के पक्ष में रहे, झूठी गवाही नहीं दी ऐसे सज्जन को दुष्ट ने बाह्य हानि पहुँचा दी लेकिन ऐसी बाह्य हानि पहुँचने पर भी भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ता यह सिद्ध करने के लिये भगवान ने उन्हीं देहाती आदमी खुदीराम के घर एक महान् आत्मा को अवतरित किया। वे महान् आत्मा श्री रामकृष्ण परमहंस होकर प्रसिद्ध हुए। उनकी कृपा पाकर विवेकानन्द विश्वविख्यात हुए। धन्य है उस देहाती खुदीराम की सच्चाई और सत्य निष्ठा।
जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। पाप के सामने, अनाचार के सामने कभी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। समाज में लोग डरपोक होकर गुण्डा तत्त्वों को पोसते रहते हैं और स्वयं शोषे जाते हैं। कुछ अनिष्ट घटता हुआ देखते हैं तो उसका प्रतिकार नहीं करते। 'हमारा क्या..... हमारा क्या.....? करेगा सो भरेगा....।' ऐसी दुर्बल मनोदशा से सिकुड़ जाते हैं। सज्जन लोग सिकुड़ जाते हैं, चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी गुण्डे तत्त्वों को हाथ में रखना पड़ता है। क्योंकि समाज के डरपोक लोगों पर उन्हीं की धाकधमकी चलती है।
अतः अपने जीवन में और सारे समाज में अमन-चमन लाना हो तो भगवान श्रीकृष्ण की बात को आज ध्यान से सुनें।
निर्भयता का यह मतलब नहीं है कि बहू सास का अपमान कर देः 'मैं निर्भय हूँ....।' निर्भयता का यह मतलब नहीं कि छोरा माँ-बाप का कहना माने नहीं। निर्भयता का यह मतलब नहीं कि शिष्य गुरु को कह दे कि, 'मैं निर्भय हूँ, आपकी बात नहीं मानूँगा।' यह तो खड्डे में गिरने का मार्ग है। लोग निर्भयता का ऐसा गलत अर्थ लगा लेते हैं।
हरिद्वार में घाटवाले बाबा वेदान्ती संत थे। सत्संग में बार-बार कहते कि निर्भय रहो। उनकी एक शिष्या ने बाबाजी की यह बात पकड़ ली। वह बूढ़ी थी। दिल्ली से बाबाजी के पास आती थी। एक दिन खट्टे आम की पकौड़ियां बना कर बाबाजी के पास ले आयी। बाबाजी ने कहाः "अभी मैंने दूध पीया है। दूध के ऊपर पकौड़े नहीं खाने चाहिए।"
वह बोलीः बाबाजी ! "मैंने मेहनत करके आपके लिय बनाया है। खाओ न....।"
"मेहनत करके बनाया है तो क्या मैं खाकर बीमार पड़ूँ? नहीं खाना है, ले जा।"
"बाबाजी ! आज कुछ भी हो जाए ,मैं खिलाकर छोडूंगी।"
बाबाजी ने डाँटते हुए कहाः "क्या मतलब?"
"आप ही ने तो कहा है कि निर्भय रहो। मैं निर्भय रहूँगी। आप भले कितना भी डाँटो। मैं तो खिलाकर रहूँगी।" वह महिला बोली।
गुरु शिष्या का वह संवाद मैं सुन रहा था। मैंने सोचाः राम.... राम.... राम....। महापुरुष कैसी निर्भयता बता रहे हैं और मूढ़ लोग कैसी निर्भयता पकड़ लेते हैं ! निर्भय बनने का मतलब यह नहीं कि जो हमें निर्भय बनायें उनका ही विरोध करके अपने और उनके जीवन का ह्रास करें। निर्भयता का मतलब नकट्टा होना नहीं। निर्भयता का मतलब मन का गुलाम होना नहीं। निर्भयता का मतलब है जिसमें भगवद् गीता के मुताबिक दैवी सम्पदा के छब्बीस लक्षण भर जायें।
निर्भय
जपे सकल भव
मिटे।
संत
कृपा ते
प्राणी
छूटे।।
ऐसे निर्भय नारायण तत्त्व में जगने को निर्भयता चाहिए। इसलिये अंतःकरण में भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए।
अंतःकरण निर्मल होगा तो निर्भयता आयेगी। ज्ञानयोग में स्थिति होगी, आत्माकार वृत्ति बनाने में रूचि होगी वह आदमी निर्भय रहेगा। ईश्वर में दृढ़ विश्वास होगा तो निर्भयता आयेगी।
जीवन में दान-पुण्य का भी बड़ा महत्त्व है। दान भक्त भी करता है और ज्ञानी भी करता है। भक्त का दान है रूपया-पैसा, चीज-वस्तुएँ, अन्न-वस्त्रादि। ज्ञानी का दान है निर्भयता का, ज्ञानी का दान है आत्म-जागृति का।
नश्वर चीजों को दान में देकर कोई दानी बन जाय वह भक्त है। अपने आपको, अपने स्व-स्वरूप को समाज में बाँटकर, सबको आत्मानंद का अमृत चखानेवाले ज्ञानी महादानी हो जाते हैं।
दीन-हीन, लूले-लँगड़े, गरीब लोगों को सहायता करना यह दया है। जो लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, सत्त्वगुण प्रधान है। जो ज्ञानदान करते कराते हैं ऐसे लोगों की सेवा में जो चीजें अर्पित की जाती हैं वह दान कहा जाता है। भगवान के मार्ग में चलने वाले लोगों का सहाय रूप होना यह दान है। इतर लोगों को सहाय रूप होना यह दया है। दया धर्म का मूल है। दान सत्त्वगुण बढ़ाता है। जीवन में निर्भयता लाता है।
ज्ञानयोग में निरंतर दृढ़ स्थिति करने के लिए जीवन में दान और इन्द्रिय दमन होना चाहिए। इन्द्रिय दमन का मतलब है जितना आवश्यक हो उतना ही इन्द्रियों को आहार देना। आँख को जितना जरूरी हो उतना ही दृश्य दिखाओ, व्यर्थ में इधर-उधर न भटकाओ। कान को जो जरूरी हो वह सुनाओ। व्यर्थ चर्चा, किसी की निन्दा सुनाकर कान की श्रवण-शक्ति का अपव्यय न करो। बोलने-चखने में जिह्वा का उपयोग जितना जरूरी हो उतना करो। व्यर्थ में इन्द्रियों की शक्ति को बाहर क्षीण मत करो। इन्द्रियों की शक्ति क्षीण करने से जीवन की सूक्ष्म शक्ति का ह्रास होता है। फलतः आदमी बहिर्मुख रहता है, चित्त में शांति नहीं रहती और आत्मा में स्थिति करने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है।
अगर जीवन को दिव्य बनाना है, परम तेजस्वी बनाना है, सब दुःखों से सदा के लिए दूर होकर परम सुख-स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करना है तो सूक्ष्म शक्तियों की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म शक्तियाँ इन्द्रियों के संयम से विकसित होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। इन्द्रियों का असंयम करने से सूक्ष्म शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। रोजी-रोटी के लिए तड़फनेवाले मजदूर में और योगी पुरुष में इतना ही फर्क है। सामान्य आदमी ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों का जतन नहीं किया जबकि योगी पुरुष शक्तियों का संयम करके सामर्थ्यवान बन जाते हैं।
चलते-चलते बात करते हैं तो दिमाग की शक्ति कमजोर हो जाती है। न खाने जैसा खा लेते हैं, न भोगने जैसा भोग लेते हैं। वे न संसार का सुख ठीक से भोग जाते हैं न आत्मा का सुख ले पाते हैं। दस-बीस रूपये की लाचारी में दिनभर मेहनत करते हैं। खाने-पीने का ढंग नहीं है, भोगने का ढंग नहीं है तो बेचारे रोगी रहते हैं।
योगी पुरुष इहलोक का ही नहीं, ब्रह्मलोक तक का सुख भी भोगते हैं और मुक्तिलाभ भी लेते हैं। वे जानते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों का सदुपयोग कैसे किया जाय।
सूक्ष्म शक्तियों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अपने आहार-विहार में सजग रहना जरूरी है। दोपहर को भर पेट भोजन किया हो तो शाम को जरा उपवास जैसा कर लेना चाहिए। दिनभर भूखे रहे तो रात्रि को सोने के दो घण्टे पहले अच्छी तरह भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के बीच में पानी पीना पुष्टिदायक है। अजीर्ण में पानी औषध है। भूखे पेट पानी पीना विष हो जाता है। खूब भूख लगी है और गिलास दो गिलास पानी पी लिया तो शरीर दुबला-पतला और कमजोर हो जायगा।
क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना..... क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, किससे बोलना.... क्या सुनना, कब सुनना, कितना सुनना, किसका सुनना.... इस प्रकार हमारे स्थूल-सूक्ष्म सब आहार में विवेक रखना चाहिए। भोले भाले लोग बेचारे जिस किसी की जैसी तैसी बातें सुन लेते हैं, निन्दा के भोग बन जाते हैं।
'मैं क्या करूँ.....? वह आदमी मेरे पास आया....। उसने निन्दा सुनाई तो मैंने सुन ली।'
अरे भाई ! तूने निन्दा सुन ली? निन्दकों की पंक्ति में शामिल हो गया?
कबीरा
निन्दक ना
मिलो पापी
मिलो हजार।
एक
निन्दक के
माथे पर लाख
पापीन को
भार।।
इस जीवन में अपना ही कर्म कट जाय तो भी काफी है। दूसरों की निन्दा सुनकर क्यों दूसरों के पाप अपने सिर पर लेना? जिसकी निन्दा करते हैं, सुनते है वह तो आइस्क्रीम खाता होगा और हम उसकी निन्दा सुनकर अशांति क्यों मोल लें। कब सुनना, क्या सुनना, किसका सुनना और उस पर कितना विश्वास रखना इसमें भी अक्ल चाहिए। अक्ल बढ़ाने के लिए भी अक्ल चाहिए। तप बढ़ाने के लिए भी तप चाहिए। धन बढ़ाने के लिए भी धन चाहिए। जीवनदाता से मिलने के भी जीवन जीने का सच्चा ढंग चाहिए। जीवन में दैवी संपदा होनी चाहिए। दैवी संपदा के कुछ लक्षण बताते हुए भगवान श्रीकृष्ण यह श्लोक कह रहे हैं-
'भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञान के लिए ध्यानयोग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेदशास्त्रों का पठन-पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म-पालन के लिए कष्टसहन और शरीर व इन्द्रियों के सहित, अंतःकरण की सरलता ये सब दैवी सम्पदावान पुरुष के लक्षण हैं।'
भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा से तप-तेज बढ़ता है। भगवान या किसी ब्रह्मवेत्ता सदगुरु के चित्र के समक्ष जब मौका मिले, बैठ जाओ। शरीर को स्थिर करके उन्हें एकटक निहारते जाओ। नेत्र की स्थिरता के द्वारा मन को स्थिर करने का अभ्यास करो। ऐसे तप होता है। तप से तेज बढ़ता है। इन्द्रिय-संयम बढ़ता है। जीवन की शक्तियों में वृद्धि होती है, बुद्धि में सूक्ष्मता आती है। समस्याएँ सुलझाने की प्रेरणा मिलती है। व्यवहार में भी आदमी सफल होता है, परमार्थ में भी आगे बढ़ता है।
जीवन में ऐसा अभ्यास है नहीं, इन्द्रिय-संयम है नहीं और ठाकुरजी के मंदिर में जाता है, घंट बजाता है। फिर भी रोता रहता है। सूद पर रूपये लाता है, आर्थिक बोझ में दबता चला जाता है। शिकायत करता रहता है कि, 'यह दुनियाँ बहुत खराब है। मैं तो आपघात करके मर जाऊँ तो अच्छा।'
अरे, डूबा दे जो
जहाजों को उसे
तूफान कहते
हैं।
जो
तूफानों से
टक्कर ले उसे
इन्सान कहते
हैं।।
व्यवहार जगत के तूफान तो क्या, मौत का तूफान आये उससे भी टक्कर लेने का सामर्थ्य आ जाय इसका नाम है साक्षात्कार। इसका नाम है मनुष्य जीवन की सफलता।
जरा जरा-सी बात में डर रहे हैं? जरा जरा-सी बात में सिकुड़ रहे हैं? हो होकर क्या होगा? जो भी हो गया वह देख लिया। जो हो रहा है वह देख रहे हैं। जो होगा वह भी देखा जायेगा। मूँछ पर ताव देते हुए.... भगवान को प्यार करते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ।
निर्भय..... निर्भय.... निर्भय.... निर्भय..... निर्भय.....।
अरे, भगवान का दास होकर, गुरु का सेवक होकर, मनुष्य का तन पाकर पापी पामरों से, मुर्गियाँ खानेवाले कबाबी-शराबी लोगों से डर रहे हो? वे अपने आप अपने पापों में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन जैसा आदमी दुर्योधन से डर रहा है। सोच रहा है कि ऐसे-ऐसे लोग उसके पक्ष में हैं।
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा किः
क्लैब्यं
मा स्म गमः
पार्थ
नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं
हृदयदौर्बल्यं
त्यक्त्वोत्तिष्ठ
परंतप।।
'हे अर्जुन ! नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तेरे लिये यह उचित नहीं है। हे परंतप ! हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा।'
(गीताः२.३)
समाज में सज्जन लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन सज्जन लो सज्जनता-सज्जनता में सिकड़ जाते हैं और दुर्जन लोग सिर पर सवार हो जाते हैं।
तुम डरो मत। घबराओ मत। अभयं सत्त्वसंशुद्धि.... निर्भय बनो। विकट परिस्थितियों में मार्ग खोजो। मार्ग अगर नहीं मिलता हो तो भगवान अथवा सदगुरु के चित्र के समक्ष बैठ जाओ, ॐकार अथवा स्वस्तिक के चित्र समक्ष बैठ जाओ। एकटक निहारो.... निहारो.... निहारो....। सुबह में सूर्योदय से पहल उठ जाओ, स्नानादि करके पाँच-सात प्राणायाम करो। शरीर की स्थिरता, प्राण और मन की स्थिरता करो। फिर 'प्रोब्लेम का सोल्यूशन' खोजो। यूँ चुटकी बजाते मिल जायेगा।
जितने तुम डरते हो, जितने जितने तुम घबराते हो, जितने जितने तुम विनम्र होकर सिकुड़ते हो उतना ये गुण्डा तत्त्ववाले समझते हैं कि हम बड़े हैं और ये हमसे छोटे हैं। तुम जितना भीतर से निर्भीक होकर जीते हो उतना उन लोगों के आगे सफल होते हो।
हमें
मिटा सके ये
जमाने में दम
नहीं।
हमसे
जमाना है
जमाने से हम
नहीं।।
हमारा चैतन्य-स्वरूप ईश्वर हमारे साथ है, हम ईमानदारी से जीते हैं, दूसरों का हम अहित नहीं करते, अहित नहीं चाहते फिर हमारा बुरा कैसे हो सकता है? बुरा होता हुआ दिखे तो डरो मत। सारी दुनिया उल्टी होकर टँग जाय फिर भी तुम सच्चाई में अडिग रहोगे तो विजय तुम्हारी ही होगी।
तामसी तत्त्वों से, आसुरी तत्त्वों से कभी डरना नहीं चाहिए। भीतर से सत्त्वगुण और निर्भयता बढ़ाकर समाज का अमन-चमन बढ़ाने के लिए यत्न करना चाहिए।
'हमारा क्या.....? जो करेगा सो भरेगा...' ऐसी कायरता प्रायः भगतड़ों में आ जाती है। ऐसे लोग भक्त नहीं कहे जाते, भगतड़े कहे जाते हैं। भक्त तो वह है जो संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए माया से पार रहे।
भगत
जगत को ठगत है
भगत को ठगे न
कोई।
एक
बार जो भगत
ठगे अखण्ड
यज्ञ फल होई।।
भक्त उसका नाम नहीं जो भागता रहे। भक्त उसका नाम नहीं जो कायर हो जाय। भक्त उसका नाम नहीं जो मार खाता रहे।
जिसस ने कहा थाः 'तुम्हें कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल धर देना, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो। उसमें भी भगवान है।'
जिसस ने यह कहा, ठीक है। इसलिए कहा था कि कोई आवेश में आ गया हो तो तुम थोड़ी सहन शक्ति जुटा लो, शायद उसका द्वेष मिट जाय, हृदय का परिवर्तन हो जाये।
जिसस का एक प्यारा शिष्य था। किसी गुंडा तत्त्व ने उसका तमाचा ठोक दिया। फिर पूछाः "दूसरा गाल कहाँ है?" शिष्य ने दूसरा गाल धर दिया। उस दुष्ट ने यहाँ भी तमाचा जमा दिया। फिर भी उस असुर को संतोष नहीं हुआ। उसने कहाः
"अब तीसरा कहाँ रखूँ?"
जिसस के शिष्य ने उस दुष्ट के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोलाः "तीसरा गाल यह है।"
"तुम्हारे गुरु ने तो मना किया था। उनका उपदेश नहीं मानते?"
"गुरु ने इसलिए मना किया था कि अहिंसा की सुरक्षा हो। हिंसा न हो। लेकिन तुम्हें दो बार मौका मिला फिर भी तुम्हारा हिंसक स्वभाव नहीं मिटा। तुम असुर हो। सबक सिखाये बिना सीधे नहीं होओगे।"
अनुशासन के बिना आसुरी तत्त्व नियंत्रण में नहीं रहते। रावण और दुर्योधन को ऐसे ही छोड़ देते तो आज हम लोगों का समाज शायद इस अवस्था में न जी पाता। नैतिक और सामाजिक अन्धाधूंधी हो जाती। जब-जब समाज में ऐसा वैसा हो जाय तब सात्त्विक लोगों को सतर्क होकर, हिम्मतवान बनकर तेजस्वी जीवन बिताने का यत्न करना चाहिए। आप निर्भय रहे, दूसरों को निर्भय करे। सत्त्वगुण की वृद्धि करे। जीवन में दैवी बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। केवल व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए कि, 'हे मेरे भगवान ! हे मेरे प्रभु " मेरी रक्षा करो... रक्षा करो...।'
मैंने सुनी है एक कहानी।
गुलाम नबीर ने रोजे रखे। थोड़ा बहुत भगत था और ठगतों के साथ दोस्थी भी थी। उसका धन्धा चोरी करने का था। रोजे के दिनों में उसने चोरी छोड़ रखी थी। मित्रों ने समझायाः "ऐसा भगतड़ा बनेगा तो काम कैसे चलेगा? फलाने किसान के वहाँ बढ़िया बैल आये हैं। जा, खोल के ले आ।"
गुलाम नबीर बैल चुराने चला गया। नया सिक्खड़ था। बैल खोलकर ले जाने लगा तो बैल के गले में बँधी हुई घंटियाँ बजने लगीं। लोग जग गये और चोर का पीछा किया। गुलाम नबीर आगे चला तो पीछे हल्ला गुल्ला सुनाई देने लगा। उसने डरके मारे खुदा से प्रार्थना कीः "हे खुदाताला ! मैंने रोजा रखा है, मैं कमजोर हो गया हूँ। तू मुझे सहाय कर। मेरे ऊपर रहमत कर। दुबारा यह धन्धा नहीं करूँगा। इस बार बचा ले।"
उसके हृदयाकाश में आकाशवाणी हुई, प्रेरणा मिली कि, "बैलों को छोड़कर भाग जा तो बच जायगा। दुबारा चोरी मत करना।"
"मालिक ! मैं रोजा रख रहा हूँ। मुझमें दौड़ने की शक्ति नहीं है। दया करके आप ही मुझे बचाओ।"
"अच्छा, तू दौड़ नहीं सकता है तो जल्दी से चलकर सामनेवाली झाड़ी में छुप जा। बैलों को छोड़ दे।"
"मुझमें इतनी भी शक्ति नहीं है। तू रहमत कर.... तू रहमत कर....." गुलाम नबीर इस प्रकार गिड़गिड़ाता रहा। इतने में लोगों ने आकर उसे पकड़ लियाः
"मूर्ख ! बोलता है 'रहमत कर... रहमत कर....?' माल चुराते समय रहमत नही की और अब पकड़ा गया तो रहमत कर.. रहमत कर...?" लोगों ने बराबर मेथीपाक चखाया, रात भर कोठरी में बन्द रखा, सुबह में पुलिस को सौंप दिया।
गुलाम नबीर अंतःप्रेरणा की आवाज सुनकर हिम्मत करता तो बच जाता।
हिम्मते
मर्दा तो मददे
खुदा।
बेहिम्मत
बन्दा तो
बेजार खुदा।।
जो नाहिम्मत हो जाता है उसको बचाने में भगवान भी बेजार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। अपना पुरुषार्थ जगाना चाहिए, हिम्मतवान बनना चाहिए।
यह
कौन-सा उकदा
जो हो नहीं
सकता?
तेरा
जी न चाहे तो
हो नहीं सकता।
छोटा-सा
कीड़ा पत्थर
में घर करे....
इन्सान
क्या दिले
दिलबर में घर
न करे?
तुममें ईश्वर की अथाह शक्ति छुपी है। परमात्मा का अनुपम बल छुपा है। तुम चाहो तो ऐसी ऊँचाई पर पहुँच सकते हो कि तुम्हारा दीदार करके लोग अपना भाग्य बना लें। तुम ब्रह्मवेत्ता बन सकते हो ऐसा तत्त्व तुममें छुपा है। लेकिन अभागे विषयों ने, तुम्हारे नकारात्मक विचारों ने, दुर्बल ख्यालों ने, चुगली, निन्दा और शिकायत की आदतों ने, रजो और तमोगुण ने तुम्हारी शक्ति को बिखेर दिया है। इसीलिए श्रीकृष्ण कहते हैं-
अभयं
सत्त्वसंशुद्धिः.....।
जीवन में दैवी सम्पदा के लक्षण भरो और निर्भय बनो। जितनी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी उतनी ठीक से सामाजिक उन्नति भी होगी। अगर आध्यात्मिक उन्नति शून्य है तो नैतिक उन्नति मात्र भाषा होगी। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति नहीं हो सकती। नैतिक उन्नति नहीं होगी तो भौतिक उन्नति दिखेगी लेकिन वास्तव में वह उन्नति नहीं होगी, जंजीरें होगी तुम्हारे लिये। लोगों की नजरों में बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियाँ, बहुत रूपये-पैसे दिखेंगे लेकिन तुम्हारे भीतर टेन्शन ही टेन्शन होगा, मुसीबतें ही मुसीबतें होगी।
आध्यात्मिक उन्नति जितने अनुपात में होती है उतने अनुपात में नैतिक बल बढ़ता है। जितने अनुपात में नैतिक बल बढ़ता है उतने अनुपात में तुम जागतिक वस्तुओं का ठीक उपयोग और उपभोग कर सकते हो। लोग जगत की वस्तुओं का उपभोग थोड़े ही करते हैं, वे तो भोग बन जाते हैं। वस्तुएँ उन्हें भोग लेती हैं। धन की चिन्ता करते-करते सेठ को 'हार्ट-अटैक' हो गया तो धन ने सेठ को भोग लिया। क्या खाक सेठ ने भोगा धन को? कार में तो ड्रायवर घूम रहा है, सेठ तो पड़े हैं बिस्तर में। लड्डू तो रसोईया उड़ा रहा है, सेठ तो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। भोग तो नौकर-चाकर भोग रहे हैं और सेठ चिन्ता में सूख रहे हैं।
अपने को सेठ, साहब और सुखी कहलानेवाले तथा-कथित बड़े-बड़े लोगों के पास अगर सत्त्वगुण नहीं है तो उनकी वस्तुओं का उपभोग दूसरे लोग करते हैं।
तुम्हारे जीवन में जितने अनुपात में सत्त्वगुण होगा उतने अनुपात में आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होगी। जितने अनुपात में आध्यात्मिक शक्तियाँ होगी उतने अनुपात में नैतिक बल बढ़ेगा। जितने अनुपात में नैतिक बल होगा उतने अनुपात में व्यवहारिक सच्चाई होगी, चीज-वस्तुओं का व्यावहारिक सदुपयोग होगा। तुम्हारे संपर्क में आनेवालों का हित होगा। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तो नैतिक बल नहीं आएगा। उतना ही जीवन डावाँडोल रहेगा। डावाँडोल आदमी खुद तो गिरता है, उसका संग करने वाले भी परेशान होते हैं।
इन्द्रियों का दमन नहीं करने से सूक्ष्म शक्तियाँ बिखर जाती हैं तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती।
वाणी का संयम करना माने चुगली, निन्दा नहीं करना, कटु भाषा न बोलना, झूठ-कपट न करना, यह वाणी का तप है। आचार्य की उपासना करना, भगवान की उपासना करना, यह मन का तप है। शरीर को गलत जगह पर न जाने देना, व्रत-उपवास आदि करना यह शारीरिक तप है।
व्रत-उपवास की महिमा सुनकर कुछ महिलाएँ लम्बे-लम्बे व्रत रखने लग जाती है। जो सुहागिन स्त्रियाँ है, जिनका पति हयात है ऐसी महिलाओं को अधिक मात्रा में व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। सुहागिन अगर अधिक उपवास करेगी तो पति की आयु क्षीण होगी। सप्ताह में, पन्द्रह दिन में एक उपवास शरीर के लिए भी ठीक है और व्रत के लिए भी ठीक है।
कुछ लोग रोज-रोज पेट में ठूँस-ठूँसकर खाते हैं, अजीर्ण बना लेते हैं और कुछ लोग खूब भूखामरी करते हैं, सोचते हैं कि मुझे जल्दी भगवान मिल जाय। नहीं, व्यवहार में थोड़ा दक्ष बनने की जरूरत है। कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, कब व्रत रखना, कैसे रखना यह ठीक से समझकर आदमी अगर तपस्वी जीवन बिताता है तो उसका बल, तेज बढ़ता है।
प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। प्राणायाम से प्राण की रिधम अगर ठीक हो जाय तो शरीर में वात और कफ नियंत्रित हो जाते हैं। फिर बाहर की दवाइयों की ओर 'मेग्नेट थेरापी' आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्जैक्शन की सुइयाँ भोंकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। केवल अपने प्राणों की गति को ठीक से समझ लो तो काफी झंझटो से छुट्टी हो जायगी।
जप करने से एक प्रकार का आभामण्डल बनता है, सूक्ष्म तेज बनता है। उससे शरीर में स्फूर्ति आती है, मन-बुद्धि में बल बढ़ता है। जप करते समय अगर आसन पर नहीं बैठोगे तो शरीर की विद्युत् शक्ति को अर्थींग मिल जायगा। आभा, तेज, ओज, बल की सुरक्षा नही होगी। अतः आसन पर बैठकर प्राणायाम, जप-तप, ध्यान-भजन करना चाहिए। शरीर तन्दुरुस्त रहेगा, मन एकाग्र बनेगा, बुद्धि तेजस्वी होगी, जीवन में सत्त्वगुण की वृद्धि होगी।
सत्त्वात्
संजायते
ज्ञानम्।
सत्त्वगुण की वृद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है।
आदमी जितना भी पामर हो, उसमें कितने भी दोष हों, अगर थोड़े ही दिन इन साधनों का अवलंबन ले तो उसके दोष अपने आप निकलने लगेंगे।
सूक्ष्म शक्तियों से स्थूल शक्तियाँ संचालित होती हैं। मोटरकार में पेट्रोल से इंजिन के भीतर थोड़ी-सी आग जलती है। इससे इतनी बड़ी गाड़ी भागती है। ट्रेन के बोइलर में थोड़े गेलन पानी होता है, उबलता है, वाष्प बनता है, उससे हजारों मन, लाखों टन वजन को लेकर इंजिन को भागता है।
ऐसे ही मन जब ध्यान-भजन करके सूक्ष्म होता है तो लाखों मुसीबतों को काटकर अपने भगवत्प्राप्त रूपी मोक्ष के द्वार पर पहुँच जाता है। बाहर की गाड़ी तो वाष्प के बल से तुम्हें अहमदावाद से दिल्ली पहुँचाती है जबकि तुम्हारी दिल की गाड़ी अगर सत्त्वगुण बढ़े तो दिलबर तक परमात्मा तक, पहुँचा देती है।
मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक राह को रोशन करने वाले राहबर मिले हैं, साधना का उत्तम वातावरण मिल रहा है, इन बातों को आत्मसात् करने के लिए श्रद्धा-भक्ति और बुद्धि भी है तो जितना हो सके, अधिक से अधिक चल लेना चाहिए। किसी भी दुःखों से, किसी भी परिस्थितियों से रुकना नहीं चाहिए।
गम
की अन्धेरी
रात में दिल
को न बेकरार
कर।
सुबह
जरूर आयेगी
सुबह का
इन्तजार कर।।
घबराहट से तुम्हारी योग्यता क्षीण हो जाती है। जब डर आये तो समझो यह पाप का द्योतक है। पाप की उपज डर है। अविद्या की उपज डर है। अज्ञान की उपज डर है। निर्भयता ज्ञान की उपज है। निर्भयता आती है इन्द्रियों का संयम करने से, आत्मविचार करने से। 'मैं देह नहीं हूँ.... मैं अमर आत्मा हूँ। एक बम ही नहीं, विश्वभर के सब बम मिलकर भी शरीर के ऊपर गिर पड़ें तो भी शरीर के भीतर का जो आत्मचैतन्य है उसका बाल बाँका भी नहीं होता। वह चैतन्य आत्मा मैं हूँ। सोऽहम्.... इस प्रकार आत्मा में जागने का अभ्यास करो। 'सोऽहम् का अजपाजाप करो। अपने सोऽहम् स्वभाव में टिको।
विकारों से ज्यों-ज्यों बचते जाओगे त्यों-त्यों आध्यात्मिक उन्नति होगी, नैतिक बल बढ़ेगा। तुम संसार का सदुपयोग कर पाओगे। अभी संसार का सदुपयोग नहीं होता। सरकनेवाली चीजों का सदुपयोग नहीं होता, उनक दुरुपयोग होता है। साथ ही साथ हमारे मन-इन्द्रियों का भी दुरुपयोग हो जाता है, हमारे जीवन का भी दुरुपयोग हो जाता है। कहाँ तो दुर्लभ मनुष्य जन्म..... देवता लोग भी भारत में मनुष्य जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं... वह मनुष्य जन्म पाकर आदमी दो रोटी के लिए इधर उधर धक्का खा रहा है। दो पैसे के मकान के लिए गिड़गिड़ा रहा है ! चार पैसे की लोन लेने के लिए लाईन में खड़ा है ! साहबों को और एजेन्टों को सलाम करता है, सिकुड़ता रहता है। जितना सिकुड़ता है उतना ज्यादा धक्के खाता है। ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। तब कहीं लोन पास होता है। यह क्या मनुष्य का दुर्भाग्य है? मानव जीवन जीने का ढंग ही हम लोगों ने खो दिया है।
विलासिता बढ़ गई है। ऐश-आरामी जीवन (Luxurious Life) जीकर सुखी रहना चाहते हैं वे लोग ज्यादा दुःखी हैं बेचारे। जो भ्रष्टाचार (Corruption) करके सुखी रहना चाहते हैं उनको अपने बेटों के द्वारा, बेटियों के द्वारा और कोई प्रोब्लेम के द्वारा चित्त में अशांति की आग जलती रहती है।
अगर
आराम चाहे तू
दे आराम खलकत
को।
सताकर
गैर लोगों को
मिलेगा कब अमन
तुझको।।
दूसरों का बाह्य ठाठ-ठठारा देखकर अपने शांतिमय आनन्दमय, तपस्वी और त्यागी जीवन को धुँधला मत करो। सुख-वैभव की वस्तुएँ पाकर जो अपने को सुखी मानते है उन पर तो हमें दया आती है लेकिन ऐसे लोगों को सुखी समझकर उन जैसे होने के लिए जो लोग नीति छोड़कर दुराचार के तरफ लगते हैं उन पर हमें दुगनी दया आती है। ये लोग जीवन जीने का ढंग ही नहीं समझते। बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया यह हो, बढ़िया वह हो तो आदमी सुखी हो जाय? अगर ऐसा होता तो रावण पूरा सुखी हो जाता। दुर्योधन पूरा सुखी हो जाता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।
शक्कर
खिला शक्कर
मिले टक्कर
खिला टक्कर
मिले।
नेकी
का बदला नेक
है बदों को
बदी देख ले।
दुनियाँ
ने जान इसको
मियाँ सागर की
यह मझदार है।
औरों
का बेड़ा पार
तो तेरा बेड़ा
पार है।।
कलजुग
नहीं करजुग है
यह इस हाथ दे
उस हाथ ले।।
मैंने सुनी है एक सत्य घटना।
अमदावाद, शाहीबाग में डफनाला के पास हाईकोर्ट के एक जज सुबह में दातुन करते हुए घूमने निकले थे। नदी के तरफ दो रंगरूट जवान आपस में हँसी-मजाक कर रहे थे। एक ने सिगरेट सुलगाने के लिए जज से माचिस माँगा। जज ने इशारे से इन्कार कर दिया। थोड़ी देर इधर-उधर टहलकर जज हवा खाने के लिए कहीं बैठ गये। देख रहे थे उन दोनों को। इतने में वे रंगरूट हँसी-मजाक, तू-मैं-तू-मैं करते हुए लड़ पड़े। एक ने रामपुरी चक्कू निकालकर दूसरे को घुसेड़ दिया, खून कर डाला और पलायन हो गया। जज ने पुलिस को फोन आदि सब किया होगा। खून का केस बना। सेशन कोर्ट से वह केस घूमता घामता कुछ समय के बाद आखिर हाई कोर्ट में उसी जज के पास आया। केस जाँचा। उन्हें पता चला कि केस वही है। उस दिन वाली घटना का उन्हें ठीक स्मरण था। उन्होंने अपराधी को देखा तो पाया कि यह उस दिन वाला अपराधी तो नहीं है।
वे जज कर्मफल के अकाट्य सिद्धान्त को माननेवाले थे। वे समझते थे कि लांच-रिश्वत या और कोई भी अशुभ कर्म उस समय तो अच्छा लगता है लेकिन समय पाकर उसके फल भोगने ही पड़ते हैं। पाप करते समय अच्छा लगता है लेकिन भोगना पड़ता है। कुछ समय के लिए आदमी किन्हीं कारणों से चाहे छूट जाय लेकिन देर सवेर कर्म का फल उसे मिलता है, मिलता है और मिलता ही है।
जज ने देखा कि यह अपराधी तो बूढ़ा है जबकि खून करने वाला रंगरूट तो जवान था। उन्होंने बूढ़े को अपनी चेम्बर में बुलाया। बूढ़ा रोने लगाः
"साहब ! डफनाला के पास, साबरमती का किनारा.... यह सब घटना मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। भगवान की कसम, मैं निर्दोष मारा जा रहा हूँ।"
जज सत्त्वगुणी थे, सज्जन थे, निर्मल विचारों वाले, खुले मन के थे। निर्भय थे। निःस्वार्थी और सात्विक आदमी निर्भय रहता है। उन्होंने बूढ़े से कहाः
"देखो, तुम इस मामले में कुछ नहीं जानते यह ठीक है लेकिन सेशन कोर्ट में तुम पर यह अपराध बिल्कुल फिट हो गया है। हम तो केवल कानून का चुकादा देते हैं। अब हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते।
इस केस में तुम नहीं थे ऐसा तो मेरा मन भी कहता है फिर भी यह बात भी उतनी ही निश्चित है कि अगर तुमने जीवनभर कहीं भी किसी इन्सान की हत्या नहीं की होती तो आज सेशन कोर्ट के द्वारा ऐसा जड़बेसलाक केस तुम पर बैठ नहीं सकता था।
काका ! अब सच बताओ, तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी, अपनी जवानी में किसी मनुष्य को मारा था?"
उस बूढ़े ने कबूल कर लियाः "साहब ! अब मेरे आखिरी दिन हैं। आप पूछते हैं तो बता देते हूँ कि आपकी बात सही है मैंने दो खून किये थे। लांच-रिश्वत देकर छूट गया था।"
जज बोलेः "तुम तो देकर छूट गये लेकिन जिन्होंने लिया उनसे फिर उनके बेटे लेंगे, उनकी बेटियाँ लेंगी, कुदरत किसी न किसी हिसाब से बदला लेगी। तुम वहाँ देकर छूटे तो यहाँ फिट हो गये। उस समय लगता है कि छूट गये लेकिन कर्म का फल तो देर-सवेर भोगना ही पड़ता है।"
कर्म का फल जब भोगना ही पड़ता है तो क्यों न बढ़िया कर्म करें ताकि बढ़िया फल मिले? बढ़िया कर्म करके कर्म भगवान को ही क्यों न दे दें ताकि भगवान ही मिल जायें?
नारायण..... नारायण.... नारायण...... नारायण.... नारायण......
सत्त्वसंशुद्धि के लिए, निर्भयता के लिए भगवान का ध्यान भगवन्नाम का जप, भगवान के गुणों का संकीर्तन, भगवान और गुरुजनों का पूजन आदि साधन हैं। अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना सत्त्वगुण बढ़ाने के लिए हितावह है। पहले के जमाने में यज्ञ-याग होते थे। फिर उसका स्थान इष्ट की मूर्तिपूजा ने लिया। मूर्तिपूजा भी चित्तशुद्धि का एक बढ़िया साधन है। वेदशास्त्रों का पठन-पाठन, जप, कीर्तन आदि से सत्त्वगुण बढ़ता है। सत्त्वगुण बढ़ने से मनोकामना जल्दी से पूर्ण होती है। हल की कामना करने से तप का खर्च हो जाता है। ऊँचे से ऊँची यह कामना करें कि, 'हे भगवान् ! हमारी कोई कामना न रहे। अगर कोई कामना रहे तो तुझे पाने की ही कामना रहे।' ऐसी कामना से तप घटता नहीं, और चार गुना बढ़ जाता है।
जप-तप करके, भगवन्नाम संकीर्तन से सत्त्वगुण बढ़ाओ। स्वधर्मपालन करने में जो कष्ट सहना पड़े वह सहो। तुम जहाँ जो कर्त्तव्य में लगे हो, वहाँ उसी में बढ़िया काम करो। नौकर हो तो अपनी नौकरी का कर्त्तव्य ठीक से बजाओ। दूसरे लोग आलस्य में या गपशप में समय बरबाद करते हों तो वे जानें लेकिन तुम अपना काम ईमानदारी से उत्साहपूर्वक करो। स्वधर्मपालन करो। महिला हो तो घर को ठीक साफ सुथरा रखो, स्वर्ग जैसा बनाओ। आश्रम के शिष्य हो तो आश्रम को ऐसा सुहावना बनाओ कि आने वालों का चित्त प्रसन्न हो जाय, जल्दी से भगवान के ध्यान-भजन में लग जाय। तुम्हें पुण्य होगा।
अपना स्वधर्म पालने मे कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। सर्दी-गर्मी,भूख-प्यास,मान-अपमान सहना पड़ेगा। अरे, चार पैसे कमाने के लिए रातपालीवालों को सहना पड़ता हैता है, दिनपालीवालों को सहना पड़ता है तो 'ईश्वरपाली' करने वाला थोड़ा सा सह ले तो क्या घाटा है भैया?
.....तो स्वधर्मपालन के लिए कष्ट सहें। शरीर तथा इन्द्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता रखें। चित्त में क्रूरता और कुटिलता नहीं रखें। जब-जब ध्यान-भजन में या ऐसे ही बैठें तब सीधे, टट्टार बैठें। झुककर या ऐसे-वैसे बैठने से जीवन-शक्ति का ह्रास होता है। जब बैठें तब हाथ परस्पर मिले हुए हों, पालथी बँधी हुई हो। इससे जीवन-शक्ति का अपव्यय होना रुक जायगा। सूक्ष्म शक्ति की रक्षा होगी। तन तन्दुरुस्त रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। सत्त्वगुण में स्थिति करने में सहाय मिलेगी। स्वधर्मपालन में कष्ट सहने पड़े तो हँसते-हँसते सह लो यह दैवी सम्पदावान पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे पुरुष की बुद्धि ब्रह्मसुख में स्थित होने लगती है। जिसकी बुद्धि ब्रह्मसुख में स्थित होने लगती है उसके आगे संसार का सुख पाले हुए कुत्ते की तरह हाजिर हो जाता है। उसकी मौज पड़े तो जरा सा उपयोग कर लेता है, नहीं तो उससे मुँह मोड़ लेता है।
जिसके जीवन में सत्त्वगुण नहीं हैं, दैवी संपत्ति नहीं है वह संसार के सुख के पीछे भटक-भटककर जीवन खत्म कर देता है। सुख तो जरा-सा मिला न मिला लेकिन दुःख और चिन्ताएँ उसके भाग्य में सदा बनी रहती हैं।
सब दुःखों की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति अगर कोई करना चाहे तो अपने जीवन में सत्त्वगुण की प्रधानता लाये। निर्भयता, दान, इन्द्रियदमन, संयम, सरलता आदि सदगुणों को पुष्ट करे। सदगुणों में प्रीति होगी तो दुर्गुण अपने आप निकल जायेंगे। सदगुणों में प्रीति नहीं है, इसलिए दुर्गुणों को हम पोसते हैं। थोड़ा जमा थोड़ा उधार.... थोड़ा जमा थोड़ा उधार... ऐसा हमारा खाता चलता रहता है। पामरों को, कपटियों को देखकर उनका अनुकरण करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करके भी धन इकट्ठा करने की चाह रखते हैं। अरे भैया ! वे लोग जो करते हैं वे भैंसा बन कर भोगेंगे, वृक्ष बनकर कुल्हाड़े के घाव सहेंगे, यह तो बाद में पता चलेगा। उनकी नकल क्यों कर रहे हो?
जीवन में कोई भी परिस्थिति आये तो सोचो कि कबीर होते तो क्या करते? रामजी होते तो क्या करते? लखनलाला होते तो क्या करते? सीताजी होती तो क्या करती? गार्गी होती तो क्या करती? मदालसा होती तो क्या करती? शबरी भीलनी होती तो क्या करती? ऐसा सोचकर अपना जीवन दिव्य बनाना चाहिए। दिव्य जीवन बनाने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। दृढ़ संकल्प के लिए सुबह जल्दी उठो। सूर्योदय से पहले स्नानादि करके थोड़े दिन ही अभ्यास करो, तुम्हारा अंतःकरण पावन होगा। सत्त्वगुण बढ़ेगा। एक गुण दूसरे गुणों को ले आता है। एक अवगुण दूसरे अवगुणों को ले आता है। एक पाप दूसरे पापों को ले आता है और एक पुण्य दूसरे पुण्यों को ले आता है। तुम जिसको सहारा दोगे वह बढ़ेगा। सदगुण को सहारा दोगे तो ज्ञान शोभा देगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
दैवी
सम्पदा – २
(दिनांकः
२९-७-१९९०
रविवार, अहमदावाद
आश्रम)
अहिंसा
सत्यमक्रोधस्त्यागः
शान्तिरपैशुनम्।
दया
भूतेष्वलोलुप्तवं
मार्दवं
ह्रीरचापलम्।।
'मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्त्तापन के अभिमान का त्याग, अन्तःकरण की उपरति अर्थात् चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निन्दा आदि न करना, सब भूतप्राणियों में हेतु रहित दया, इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव (ये दैवी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं।)
(भगवद्
गीताः १६-२)
साधक को कैसा होना चाहिए, जीवन का सर्वांगी विकास करने के लिए कैसे गुण धारण करने चाहिए, जीवन का सर्वांगी विकास करने के लिए कैसे गुण धारण करने चाहिए इसका वर्णन भगवान श्रीकृष्ण 'दैवीसम्पद्विभागयोग' में करते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके जीवन में ये गुण जन्मजात होते हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके जीवन में भक्ति-भाव से ये गुण धीरे-धीरे आते हैं। उनको यदि सत्संग मिल जाय, वे थोड़ा पुरुषार्थ करे तो गुण जल्दी से आते हैं। साधक लोग साधन-भजन करके गुण अपने में भर लेते हैं।
दैवी सम्पदा आत्मानुभव की जननी है। दैवी सम्पदा आत्मा के निकट है, आत्मा का स्वभाव है, जिनमें दैवी सम्पदा होती है वे लोग बहुत लोगों के प्यारे होते हैं। दैवी सम्पदा में छब्बीस सदगुण बताये गये हैं।
आपने व्यवहार में भी देखा होगा कि आदमी कितना भी बेईमान हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, डाकू हो लेकिन वह नहीं चाहता है कि मेरे साथ दूसरा कोई बदमाशी करे। बेईमान आदमी भी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है। बदमाश आदमी भी अपना कोषाध्यक्ष या साथी, संगी ईमानदार चाहता है। ईमानदार लोग तो ईमानदार आदमी को प्यार करते ही हैं लेकिन बेईमान लोगों को भी ईमानदार आदमी की आवश्यकता होती है। अर्थात् दैवी गुण आत्मा के निकटवर्ती हैं इसलिए दैवी गुणवालों को प्रायः सब लोग प्यार करते हैं। आसुरी स्वभाव के लोग भी दैवी गुणवाले के प्रति भीतर से झुके हुए होते हैं, केवल बाहर से फुफकारते हैं। श्रीरामजी के प्रति रावण भीतर से झुका हुआ था लेकिन बाहर से फुफकारते फुफकारते मर गया। कंस श्री कृष्ण के प्रति भीतर से प्रभावित था लेकिन बाहर से दुष्टता करता रहा। इस प्रकार जिसमें दैवी गुण होते हैं उसके कुटुम्बी, पड़ोसी आद बाहर से चाहे उसकी दिल्लगी उड़ायें, उपहास करें लेकिन भीतर में उससे प्रभावित होते जाते हैं। अतः साधक को चाहिए कि अगर आसुरी स्वभाव के दस-बीस लोग उसका मजाक उड़ायें, उसका विरोध करें, उसकी निन्दा करें या कोई आरोप-लांछन लगायें तो साधक को चिंतित नहीं होना चाहिए। साधक को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे सदा याद रखना चाहिए किः
इलजाम
लगाने वालों
ने इलजाम
लगाये लाख
मगर।
तेरी
सौगात समझ हम
सिर पे उठाये
जाते हैं।।
ये संत-महात्मा-सत्पुरुष-सदगुरुओं की महानता है। वशिष्ठजी महाराज कहते हैं-
"हे रामजी ! मैं बाजार से गुजरता हूँ तब पापी लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं यह सब मैं जानता हूँ लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है।"
साधक के जीवन में भी भीतर दया होनी चाहिए। दया का मतलब यह नहीं है कि सदा मूर्ख बना रहे। कभी दुष्टजन के प्रति फूफकार भी कर दे लेकिन भीतर से अपने चित्त को चैतन्य के रस से सराबोर करता जाय।
भगवान श्रीकृष्ण साधक के जीवन में साध्य तत्त्व का जल्दी से साक्षात्कार हो जाय इसलिए दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। दैवी सम्पदा के गुण देव की अनुभूति के करीब ले जाते हैं। देव वह परमेश्वर है जो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। कहा है किः 'मातृदेवो भव..... पितृदेवो भव.... आचार्यदेवो भव.... अतिथिदेवो भव.....।' इन माता, पिता, आचार्य, अतिथि आदि हाथ-पैर, नाक-मुँहवाले देवों में जो वास्तविक देव है, जो अन्तर्यामी देव है वह परमात्मा तुम्हारे अन्तःकरण में भी बैठा है। उस देव का अनुभव करने के लिए दैवी सम्पदा नितान्त आवश्यक है। दैवी सम्पदा आत्मा-परमात्मा के साक्षात्कार तक पहुँचा देती है।
स्थूल-शरीरधारी को सर्वथा अहिंसक होना तो संभव नहीं लेकिन अपने स्वार्थ के कारण किसी के चित्त को, किसी के तन-मन को, किसी के जीवन को कष्ट न देना यह अहिंसा है। डॉक्टर शल्य क्रिया करता है, मरीज को पीड़ा पहुँचाता है लेकिन उसका पीड़ा पहुँचाने का स्वार्थ नहीं है। उसका स्वार्थ है कि मरीज निरोग हो जाय। इसलिय अंगों की काटाकुटी करना, रक्त बहाना डॉक्टर के लिए हिंसा नहीं मानी जाती।
हिंसा का जन्म तमोगुण से होता है। प्रतिहिंसा रजोगुण से पैदा होती है। अहिंसा सत्त्वगुण से पैदा होती है। श्रीकृष्ण की अहिंसा सत्त्व-रजो-तमोगुणजन्य नहीं है। श्रीकृष्ण की अहिंसा यह है कि जिस तत्त्व की कभी मृत्यु नहीं होती उसमें टिककर व्यवहार करना। यह परम अहिंसा है, अहिंसा का सूक्ष्मतम स्वरूप है।
अहिंसा
परमो धर्मः।
परम तत्त्व में जो टिक गया, अचल तत्त्व में जो प्रतिष्ठित हो गया वही इस परम धर्म को उपलब्ध होता है।
प्रकृतेः
क्रियमाणानि
गुणैः
कर्माणि सर्वशः।
अहंकारविमूढात्मा
कर्ताहमिति
मन्यते।।
'वास्तव में सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी 'मैं कर्त्ता हूँ' ऐसा मानता है।'
(गीताः
३-२७)
प्रकृति में होने वाले कर्मों को जो कर्त्ता बनकर अपने में थोपता है वह कितना भी अहिंसक हो जाय फिर भी उसके द्वारा हिंसा हो जायगी और अपने स्वरूप में टिककर नरो वा कुंजरो वा की लीला करवाकर पापी तत्त्वों को जगत से हटवाते हैं तभी भी श्रीकृष्ण सदा अहिंसक हैं।
सत्य का मतलब है यथार्थ और प्रिय भाषण। अंतःकरण और इन्द्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम है सत्य भाषण। सत्य मधुर और हितकारी होता है। माँ मधुर वचन बोलती है, उसमें बालक हित है लेकिन डाकिनी मधुर वचन बोलती है लेकिन उसका वचन हितकारी नही होता। वेश्या मधुर वचन बोलती है लेकिन उसका वचन आदमी के तेज-ओज-वीर्य का सत्यानाश करने वाला होता है।
'सेल्समैन' मधुर वचन बोलता है तो उसमें अपना सौदा करने का स्वार्थ भरा होता है। माँ मधुर वचन बोलती है तो उसके वचन में अपने संतान-पुत्र-पुत्री-कुटुम्बी का हित छुपा हुआ है। अतः मधुर वचन सत्य होना चाहिए और साथ ही साथ हितकर होना चाहिए। अहिंसा वह है जिसमें मन, कर्म, वचन से किसी के तन-मन-जीवन को स्वार्थ के लिए सताने का प्रयास न किया जाय।
क्रोध का न होना अक्रोध है। श्रीरामचन्द्रजी के चित्त में पूरी शान्ति थी। उनके निकटवर्ती लोगों को चिन्ता हुई कि रामजी इतने शान्त रहेंगे तो रावण मरेगा कैसे? उन्होंने राम जी से विनती की किः "प्रभु ! आप क्रोध कीजिए।" फिर रामजी ने क्रोध का आवाहन कियाः 'हे क्रोध ! अहं त्वं आवाहयामि। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ।' श्रीरामजी ने उपयोग करने के लिए क्रोध को बुलाया।
परिवार में अनुशासन करने के लिए, व्यवहार-जीवन में फुफकारने के लिए कभी क्रोध करना पड़े यह एक बात है लेकिन हम लोग प्रायः क्रोध का उपयोग नहीं करते अपितु क्रोध से आक्रान्त हो जाते है, क्रोध हमारे ऊपर सवार हो जाता है। क्रोध आग जैसा खतरनाक है। घर में चोरी हो जाय तो कुछ न कुछ सामान बचा रहता है, बाढ़ का पानी आ जाय फिर भी सामान बचा रहता है, बाढ़ का पानी आ जाय फिर भी सामान बचा रहता है लेकिन घर में आग लग जाय तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं। उसी प्रकार अपने अन्तःकरण में यदि लोभ, मोहरूपी चोर प्रविष्ट हो जाय तो कुछ पुण्य क्षीण हो जाय, फिर भी चित्त में शांति और प्रसन्नता का कुछ अंश बचता है लेकिन अन्तःकरण में क्रोधरूपी आग लग जाय तो सारी शांति भंग हो जाती है, जप-तप-दान आदि पुण्य-प्रभाव क्षीण होने लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं- जीवन में अक्रोध लाना चाहिए। स्वभाव में से क्रोध को विदा करना चाहिए।
प्रश्न होगा कि दुर्वासा आदि इतना क्रोध करते थे फिर भी महान् ऋषि थे। यह कैसे?
दुर्वासा ज्ञानी थे। क्रोध करते हुए दिखते थे, श्राप देते हुए दिखते थे। फिर भी वे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। ज्ञानी को संसारी तराजू में नहीं तोला जाता। सामान्य आदमी क्रोध करे तो उसका तप क्षीण हो जाता है। उसका वचन सिद्ध नहीं होता।
दुर्वासा कहीं अपनी मस्ती में बैठे थे। आधा मील दूर से कोई ब्राह्मण गुज़र रहा था। दुर्वासा ने चिल्ला कर उसे अपने पास बुलायाः
"एइ.... इधर आ, ब्राह्मण के बच्चे....!"
वह पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोलाः
"जी महाराज !"
"कहाँ गया था तू?"
"मैं तप करने गया था। बेटा नहीं हो रहा था। माता जी की प्रसन्नता के लिए मैंने तीन साल तक तप किया। माँ प्रकट हुई, मुझे पुत्र-प्राप्ति का वरदान दिया।"
"हाँ, पुत्र-प्राप्ति का वरदान दिया....! तुझे पता नहीं, दुर्वासा यहाँ बैठे हैं? प्रणाम किये बिना तू उधर से ही चला जाता है? जा, वरदान केन्सल है। तुझे पुत्र नहीं होगा। क्या समझता है..."
दूर से गुजरते हुए आदमी को इस प्रकार श्राप दे देना...! इतना क्रोध होने पर भी दुर्वासा का वचन फलित होता था, क्योंकि दुर्वासा ब्रह्मवेत्ता थे। दुर्वासा क्रोध करते हुए दिखते थे। उस ब्राह्मण के वास्तविक कल्याण के लिए यह होना जरूरी था इसलिए दुर्वासा के द्वारा क्रोध हो गया।
दुर्वासा श्रीकृष्ण के वहाँ अतिथि होकर रहे, चित्र-विचित्र चेष्टाएँ करके उनको उद्विग्न करने का, क्रोधित करने का प्रयास किया लेकिन श्रीकृष्ण अपनी सत्तासमान में स्थित रहे। श्रीकृष्ण की समता का जगत को दर्शन कराने के लिए दुर्वासा ने लीला की थी। उन्हें जिस खण्ड में ठहराया गया था उस खण्ड में जो बढ़िया चीज वस्तुएँ थी, सर-समान था, सुन्दर बिछौने, गद्दी-तकिये, चन्दनकाष्ठ की बनी हुई चीजें आदि सब खण्ड के बीच इकट्ठा करके आग लगा दी। अपने बाल खोलकर वहाँ 'होली... होली....' करके नाचने लगे फिर भी श्री कृष्ण को क्रोध नहीं आया।
दुर्वासा ने खाने के लिए बहुत सारी खीर बनवाई। कुछ खीर खाई। बाकी बची हुई जूठी खीर श्रीकृष्ण को देते हुए आज्ञा कीः 'यह खीर अपने शरीर पर चुपड़ दो।' श्रीकृष्ण ने गुरुदेव की बची हुई खीर उठा कर अपने मुख सहित सर्व अंगों पर चुपड़ दी। दुर्वासा ने देखा कि श्रीकृष्ण के चित्त में कोई शिकायत नहीं है।
मुस्कराकर
गम का जहर जिनको
पीना आ गया।
यह
हकीकत है कि
जहाँ में उनको
जीना आ गया।।
श्रीकृष्ण की प्रसन्नता और मस्ती ज्यों-की-त्यों बनी रही। क्या अदभुत है समता ! किससे व्यवहार करना, कहाँ करना, कब करना, कैसा करना, कितना करना यह श्रीकृष्ण जानते हैं। वे ज्ञान की मूर्ति हैं। दुर्वासा उनको क्रोधित करने के लिए, उद्विग्न करने के लिए चेष्टा करते हैं लेकिन श्रीकृष्ण के चित्त में कोई शिकायत नहीं है। एक बार दुर्वासा ऋषि के आगे सिर झुका दिया, अतिथि देव की आवभगत कर दी फिर उनके लिए शिकायत कैसी?
जो
मंजिल चलते
हैं वे शिकवा
नहीं किया
करते।
जो
शिकवा किया
करते हैं वे
मंजिल नहीं
पहुँचा करते।।
रूक्मिणी गुरु-शिष्य की लीला देख रही है, मुस्कुरा रही है कि गुरु तो पक्के हैं लेकिन चेले भी कच्चे नहीं हैं, चेले भी गुरु ही हैं। उनका चित्त प्रसन्न हो रहा है कि मेरे कृष्ण का चित्त कितनी समता में स्थित है !
दुर्वासा की नजर रुक्मिणी के हास्य पर गई तो गरज उठेः
"अरे ! तू हँस रही है? इधर आ।"
रुक्मिणी जी के बाल पकड़कर उनके मुख पर दुर्वासा ने अपने हाथ से जूठी खीर चुपड़ दी। फिर तिरछी आँख से श्रीकृष्ण की ओर निहारते हैं। श्रीकृष्ण स्वरूप में शान्त और सम हैं। दुर्वासा ने देखा कि यह बाण भी फेल हो गया। अब नया निशाना ताकाः
"ऐ कृष्ण ! मुझे रथ पर बैठकर नगरयात्रा करनी है। घोड़ों के बदले तुम दोनों रथ खींचोगे।"
"जो आज्ञा।"
श्रीकृष्ण और रुक्मिणी दोनों रथ में जुत गये और दुर्वासा रथारूढ़ हुए। नगर के राजमार्ग से रथ गुजर रहा है। दुर्वासा दोनों पर कोड़े फटकारते जा रहे हैं। कोमल अंगना रुक्मिणी जी की क्या हालत हुई होगी ! बाजार के लोग आश्चर्य में डूबे जा रहे हैं कि द्वारकाधीश श्रीकृष्ण कौन से बाबा के चक्कर में आ गये हैं !
श्रीकृष्ण कहते हैं कि चौरासी के चक्कर से निकलना हो, मन के चक्कर से निकलना हो तो दुर्वासा ऋषि जैसे किसी बह्रमवेत्ता सद्गुरूओं के चरणों में और उनके चक्करों में जरूर आना चाहिए।
कोई स्त्री के चक्कर में है, कोई बच्चों के चक्कर में है, कोई धन के चक्कर में है, कोई सत्ता के चक्कर में है, कोई मन के चक्कर में है। इन सारे चक्करों से निकलने के लिए कन्हैया गुरु के चक्कर में है।
भगवद् गीता का इतना माहात्म्य क्यों है? क्योंकि उसमें श्रीकृष्ण जो कहते हैं वह उनके जीवन में है। अक्रोध माना अक्रोध। क्रोध कहाँ करना चाहिए यह वे भली प्रकार जानते हैं। कंस को आलिंगन करते-करते यमसदन पहुँचा दिया। फिर उसकी उत्तरक्रिया कराने में श्रीकृष्ण के चित्त में द्वेष नहीं है। रावण, कुंभकर्ण और इन्द्रजीत की उत्तरक्रिया कराने में श्रीरामजी को कोई द्वेष नहीं था क्योंकि समता उनका सहज सिद्ध स्वभाव है।
समत्वं
योग उच्यते।
हजार वर्ष तक शीर्षासन करो, वर्षों तक पैदल तीर्थयात्रा करो, भूखे रहो, खड़ेश्वरी और तपेश्वरी होकर तपश्चर्या करो फिर भी एक क्षण की चित्त की समता के तप के आगे वह तुम्हारा तप छोटा हो जायगा। अतः चित्त को समता में स्थिर करो।
काम आता है तो पीड़ित कर देता है, क्रोध आता है तो जलाने लगता है, लोभ आता है तो गुगला कर देता है। इन विकारों से आक्रान्त मत हो जाओ। काम का उपयोग करो, क्रोध का उपयोग करो, लोभ का उपयोग करो।
तुम कमरे में बैठे हो। अपनी मौज से भीतर से दरवाजा बन्द करके बैठो यह तुम्हारा स्वातन्त्र्य है। आधा घण्टा बैठो, चाहे दो घण्टा बैठो, चाहे चार घण्टा बैठो, कोई बन्धन नहीं है। अगर दूसरा कोई बाहर से कुंडा लगाकर तुमको कमरे में बन्द कर दे तो यह तुम्हारी पराधीनता है, चाहे वह दस मिनट के लिए ही क्यों न हो।
साधनों का उपयोग करना यह स्वाधीनता है। साधनों से अभिभूत हो जाना, साधनों के गुलाम हो जाना यह पराधीनता है। क्रोध आ गया तो अशांत हो गये, लोभ आ गया तो हम लोभी हो गये, काम आ गया तो हम कामी हो गये, मोह आया तो हम मोही हो गये। विकार हमारा उपयोग कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का स्वतन्त्र ढंग से उपयोग करना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल है। उसको सूँघा, अच्छा लगा। ठीक है, उसकी सुगन्ध का उपयोग किया। अगर फूल की सुगन्ध में आसक्ति हुई तो हम बँध गये।
अपने चित्त में किसी भी विकार का आकर्षण नहीं होना चाहिए। विकारों का उपयोग करके स्वयं को और दूसरों को निर्विकार नारायण में पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि विकारों में फँस मरना चाहिए। कूँआ बनाया है तो शीतल पानी के लिए, न कि उसमें डूब मरने के लिए।
श्रीकृष्ण के चित्त में दुर्वासा की अँगड़ाइयों के कारण क्षोभ नहीं हुआ। दुर्वासा ने देखा कि मैंने इतने-इतने अशान्त करने के बाण फेंके लेकिन श्रीकृष्ण की शांति अनूठी है। आखिर दुर्वासा से रहा नहीं गया। वे बोल उठेः
"कृष्ण ! अब बताओ, तुम क्या चाहते हो?"
"गुरुदेव ! आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। मेरे लिए दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले लेकिन मेरे गुरुदेव मेरे से न रूठें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ।"
श्रीकृष्ण गुरु की जगह पर पूरे गुरु हैं। कृष्णं वन्दे जगदगुरुम् और शिष्य की जगह पर पूरे शिष्य हैं।
दुर्वासा ने छलकते हुए आशीर्वाद दियाः "कन्हैया ! मैं तो तेरे पर प्रसन्न हूँ ही लेकिन जो तेरा नाम लेगा वह भी प्रसन्न हो जायेगा। देख भैया ! तूने एक गल्ती की। मैंने तुझे सारे शरीर पर खीर चुपड़ने को कहा था। जहाँ-जहाँ वह खीर लगी वे सब तेरे अंग वज्र जैसे अभेद्य बन गये लेकिन पैरों के तलों को तूने खीर नहीं लगायी। वह भाग कच्चा रह गया। अपने पैरों के तलुवों को बचाना, बाकी सब जगह तुम वज्रकाय बन गये हो।"
हम जानते हैं कि आखिर में उन्हीं पैर के तलुवे में व्याध का बाण लगा और उसी निमित्त से वे महानिर्वाण को प्राप्त हुए।
श्रीकृष्ण ने भगवदगीता में अक्रोध कह दिया तो वे स्वयं भी अक्रोध होने में उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे जीवन में भी जब क्रोध आये तब हम सावधान हों। सोचें कि मेरी जगह पर श्रीकृष्ण होते तो क्या करते? श्रीराम होते तो क्या करते? बुद्ध होते तो क्या करते? कबीरजी होते तो क्या करते?
क्रोध करने की जगह तो उस समय क्रोध करो लेकिन हृदय में क्रोध उत्पन्न न हो, बाहर से क्रोध करने का नाटक हो। अगर क्रोध आता हो तो देखो कि क्रोध आ रहा है। उस समय शांत हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। बाद मे किसी को समझाना हो तो समझाओ, क्रोध का नाटक कर लो, फुफकार मार दो। अपने पर क्रोध को हावी मत होने दो। हम क्या करते हैं? क्रोध को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रोध दबता नहीं और हम भीतर से उलझते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, जलते रहते हैं।
जीवन में त्याग कैसा होना चाहिए? जो बीत गया है उसको याद कर-करके अपने चित्त को खराब न करो। उसे भूल जाओ। भोग-सामग्री का अति संग्रह करके अपने चित्त को बोझिल न बनाओ।
त्यागात्
शांतिरनन्तरम्।
'त्याग से तत्काल शांति मिलती है।'
(गीता)
जीवन में भीतर से जितना त्याग होगा उतनी ही शांति रहेगी। फिर चाहे तुम्हारे पास सोने की द्वारिका हो और वह डूब रही हो फिर भी चित्त में शोक न होगा। श्रीकृष्ण की द्वारिका समुद्र में डूबी फिर भी उनके चित्त में कोई आसक्ति नहीं थी। उनका चित्त त्याग से पूर्ण था।
गांधारी ने श्रीकृष्ण को शाप दिया कि ३६ साल के बाद तुम्हारे देखते ही तुम्हारा यादव वंश नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा और श्रीकृष्ण के देखते-देखते ही यदुवंश का नाश हुआ। फिर भी श्रीकृष्ण उद्विग्न नहीं हुए।
जीवन में त्याग होना चाहिए, शांति होना चाहिए। शांति त्याग का अनुगमन करती हुई अपने आप आ जाती है।
“ अपैशुनम् ” का अर्थ है चाड़ी-चुगली न करना। कभी किसी की निन्दा, चाड़ी-चुगली, आलोचना नहीं करना चाहिए। कोई आदमी किसी की निन्दा करता है तो सुनने वाला उसमें अपना अर्थ जोड़ लेता है, कुछ ज्यादा मसाला भर देता है। वह जब तीसरे आदमी के आगे बोलेगा तो वह भी अपने मन का रंग उसमें मिला देता है। वह जब चौथे के आगे बात करेगा तो और कचरा जुड़ जायगा। मूल में बात कोई छोटी-मोटी होती है लेकिन बात करने वालों के अपने-अपने ढंग के विकृत स्वभाव होने से वह बात न जाने कैसा रूप ले लेती है। जरा सी बात ने महाभारत का युद्ध करवा दिया।
अस्त्र-शस्त्र का घाव तो समय पाकर भर जाता है मगर बिना हड्डी की लूली (जिह्वा) का घाव नहीं मिटता, मरने पर भी नहीं मिटता। इसलिए वाणी बोलते समय खूब सावधान रहो।
वाणी
ऐसी बोलिये
मनवा शीतल
होय।
औरन
को शीतल करे
आपहुँ शीतल
होय।।
शाह हाफिज ने कहाः "हे इन्सान ! तू हजार मंदिर तोड़ दे, हजार मस्जिद तोड़ दे लेकिन किसी का जिन्दा दिल मत तोड़ना, क्योंकि उस दिल में दिलबर खुद रहता है।"
कबीर जी ने कहाः
कबीरा
निन्दक ना
मिलो पापी
मिलो हजार।
एक
निन्दक के
माथे पर लाख
पापीन को
भार।।
हे इन्सान ! ईश्वर के मार्ग पर जाने वाले साधक की श्रद्धा मत तोड़।
विवेकानन्द कहते थेः 'तुम किसी का मकान छीन लो यह पाप तो है लेकिन इतना नहीं। वह घोर पाप नहीं है। किसी के रूपये छीन लेना पाप है लेकिन किसी की श्रद्धा की डोर तोड़ देना यह सबसे बड़ा घोर पाप है क्योंकि उसी श्रद्धा से वह शांति पाता था, उसी श्रद्धा के सहारे वह भगवान के तरफ जाता था।
तुमने किसी का मकान छीन लिया तो किराये के मकान से वह जीवन गुजार लेगा लेकिन तुमने उसकी श्रद्धा तोड़ दी, श्रद्धा का दुरुपयोग कर दिया, ईश्वर से, शास्त्र से, गुरु से, भगवान के मार्ग से, साधन-भजन से उसको भटका दिया तो वह अपने मकान में होते हुए भी स्मशान में है। रूपयों के बीच होते हुए भी वह बेचारा कंगाल है। उसके दिल की शांति चली गई जीवन से श्रद्धा गई, शांति गई, साधन-भजन गया तो भीतर का खजाना भी गया। बाहर के खजाने में आदमी कितना भी लोट-पोट होता हो लेकिन जिसके पास भक्ति, साधन, भजन, श्रद्धा का खजाना नहीं है वह सचमुच में कंगाल है।
श्रीकृष्ण कहते हैं-
श्रद्धावाँल्लभते
ज्ञानं
तत्परः
संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं
लब्धवा परां
शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।
'जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलम्ब के तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है।'
(गीताः
४-३९)
मनुष्य श्रद्धालु हो, तत्पर हो और थोड़ा संयम करे तो जल्दी से बेड़ा पार हो जाय।
जिसस किसी गाँव से गुज़र रहे थे। लोगों ने देखा कि संत आ रहे हैं। सज्जन लोगों ने सत्कार किया, निन्दकों ने निन्दा की। पहले से ही जिसस की अफवाह फैली हुई थी कि 'मेकडेलीन जैसी सुन्दर वैश्या जिसस के पास आती है, इत्र से जिसस के पैर धुलाती है, अपने लम्बे-लम्बे रेशम जैसे बालों से जिसस के पैर पोंछती है।' आदि आदि। कुप्रचार करने वालों ने जोरो का कुप्रचार किया था। इसीलिए जिसस को देर-सबेर क्रॉस पर चढ़ना पड़ा था। हाँ, जिसस तो क्रॉस पर नहीं चढ़े थे, जिसस का शरीर जरूर क्रॉस पर चढ़ा होगा। जिन्होंने कुप्रचार किया था वे लोग न जाने किन नरकों में सड़ते होंगे, जलते होंगे जबकि जिसस को अभी भी लाखों जानते हैं, मानते हैं।
जिसस गाँव में आये तो सज्जन लोग, पवित्र बुद्धिवाले लोग कुप्रचार सुनने के बावजूद भी जिसस का दर्शन करने पहुँचे। जिनकी मलिन मति थी वे जिसस का नाम सुनकर आगबबूला हुए।
सज्जन लोगों ने पूछाः "हे फरिश्ते ! इस इलाके में अकाल पड़ रहा है। खेतों में पानी नहीं बरस रहा है। क्या कारण है?"
जिसस ने क्षणभर शांत होकर कहाः "इस गाँव में कई निन्दक, चुगलखोर लोग रहते हैं। उनके पापों के कारण ऐसा हो रहा है।"
"ऐसे कौन लोग हैं? आप उनके नाम बताइये, हम उनको ठीक कर देंगे या गाँव से निकाल देंगे।" सज्जन लोगों ने जिसस से विनती की।
जिसस ने कहाः "उन लोगों का नाम बताने से मुझे भी चुगलखोर होना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊँगा।" जिसस वहाँ से आगे बढ़ गये।
हमारे चित्त में भी दया होनी चाहिए। ज्ञानीजनों का तो दयालु होना स्वतः स्वभाव बन जाता है। जैसे दीवार गई तो दीवार पर अंकित चित्र भी गया, जैसे बीज जल गया तो बीज में छुपा हुआ वृक्ष भी जल गया, ऐसे ही जिसकी देह-वासना गई है, जिसका देहाभ्यास गया है, परिच्छिन्न अहं गया है उनका अपने कर्मों का कर्त्तापन भी चला जाता है। सरिता यह नहीं सोचती कि गाय पानी पी रही है उसको अमृत जैसा जल और शेर पानी पीने आवे उसको विष जैसा पानी बना दूँ। नहीं.... वह तो सभी के लिए कल कल छल छल बहती है, सबको अपने शीतल जल से तृप्त करती है। फिर कोई उसमें डूब जाय तो उसकी मर्जी की बात है, सरिता किसी को कष्ट नहीं देती। ऐसे ही जिनके हृदय में दया भरी हुई है, प्राणीमात्र का जो कल्याण चाहते हैं ऐसे संतों की तरह जिसका दिल है वह वास्तव में दयालुदिल कहा जाता है। जैसे बच्चे का दुःख देखकर माँ का दिल द्रवित हो जाता है ऐसे ही प्राणीमात्र का दुःख देखकर दयालु पुरुषों का दिल द्रवित हो जाता है, उसका दुःख मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। ऐसी दया से चित्त की शुद्धि होती है।
तुमने अगर प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन दिया तो उसकी भूख-प्यास मिटी और तुम्हारे अंतःकरण का निर्माण हुआ। दुःखी जन को तो ऐहिक दुःख मिटा लेकिन तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हुआ, जन्म-जन्म के दुःख मिटने का साधन बन गया।
सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार तो सब कर सकते हैं लेकिन दुर्जन की गहराई में अपने प्रियतम परम सज्जन को देखने की जो आँख है, अपने आत्मा की मधुरता, अपने आत्मा की शाश्वतता, अपने परमेश्वर की अमरता देखने की जो आँख है वह खुल जाय तो दुर्जन के प्रति भी हृदय में करुणा होगी। फिर उसकी योग्यता के अनुसार उसके साथ व्यवहार होगा।
दुर्जन को सज्जनता के मार्ग पर लाना यह भी दया है। दुर्जन को उसके कल्याण के लिए थोड़ा सबक सिखाना यह भी उसके प्रति दया है। लेकिन दुर्जन के प्रति क्रूर होकर उसका विनाश करना यह क्रूरता है। फिर भी, उसकी मृत्यु में भी उसका कल्याण हो ऐसा विचार करके श्रीकृष्ण और श्रीरामचन्द्र जी ने दुर्जनों को मृत्यु दण्ड दे दिया इसमें भी उनकी दया है। क्योंकि उन दुर्जनों की दुर्जनता बिना ऑपरेशन के दूर नहीं हो सकती थी।
डॉक्टर मरीज का हित चाहते हुए बाहर से क्रूर दिखने वाली शस्त्रक्रिया करता है तो भी उसके चित्त में क्रूरता नहीं होती। ऐसे ही जो दयालु पुरुष हैं, माता-पिता, गुरुजन और भगवान आदि के चित्त में कभी, किसी के लिए भी क्रूरता नहीं होती।
एक माँ का बेटा डाकू हो गया था। डकैती में नामचीन हो गया, पकड़ा गया और कई क्रूर अपराधों के कारण फाँसी की सजा मिली। फाँसी से पहले पूछा गया कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? वह बोला कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ को नजदीक लाया गया तो उस लड़के ने खूब नज़दीक लपककर अपने दाँतों से माँ का नाक काटकर अलग कर दिया।
न्यायाधीश ने पूछाः "तुझे माँ के प्रति इतना द्वेष और क्रोध क्यों?"
वह बोलाः "इस मेरी माँ ने ही मुझे इतना बड़ा डाकू बनने में सहयोग दिया है। मैं बचपन में जब छोटी-छोटी चोरियाँ करके घर में आता था, किसी की पेन्सिल चुराकर, किसी की रबड़ चुराकर माँ के पास जाता था तब मेरी उन गलतियों के प्रति माँ लापरवाह रही। मेरी गलतियों को पोषण मिलता रहा। ऐसा करते करते मैं बड़ा डाकू हो गया और आज इस फाँसी का फंदा मेरे गले में आ पड़ा है। मेरे जीवन के सत्यानाश के कारणों में माँ का निमित्त बड़ा है।"
खेत में खेती के पौधों के अलावा कई प्रकार का दूसरा घास-फूस भी उग निकलता है। उसके प्रति किसान अगर लापरवाह रहे तो खेत में काम के पौधों के बदले दूसरी ही भीड़-भाड़ हो जाती है, खेती निकम्मी हो जाती है। बगीचा जंगल बन जाता है। ऐसे ही जीवन में थोड़ी-थोड़ी लापरवाही आगे चलकर बड़ी हानिकारक सिद्ध होती है।
एक शिष्य था। गुरुसेवा करता था लेकिन लापरवाह था। गुरु उसको समझाते थे किः "बेटा ! लापरवाही मत कर। थोड़ी सी भी लापरवाही आगे चलकर दुःख देगी।" शिष्य कहताः "इसमें क्या है? थोड़ा-सा दूध ढुल गया तो क्या हुआ? और सेर भर ले आता हूँ।"
यहाँ जरा से दूध की बात नहीं है, आदत बिगड़ती है। दूध का नुकसान ज्यादा नहीं है, जीवन में लापरवाही बड़ा नुकसान कर देगी। यह बात शिष्य के गले नहीं उतरती थी। गुरु ने सोचा कि इसको कोई सबक सिखाना पड़ेगा।
गुरुजी ने कहाः "चलो बेटा ! तीर्थयात्रा को जाएँगे।"
दोनों तीर्थयात्रा करने निकल पड़े। गंगा किनारे पहुँचे, शीतल नीर में गोता मारा। तन-मन शीतल और प्रसन्न हुए। सात्त्विक जल था, एकांत वातावरण था। गुरु ने कहाः
"गंगा बह रही है। शीतल जल में स्नान करने का कितना मजा आता है ! चलो, गहरे पानी में जाकर थोड़ा तैर लेते हैं। तू किराये पर मशक ले आ। मशक के सहारे दूर-दूर तैरेंगे।"
मशकवाले के पास दो ही मशक बची थी। एक अच्छी थी, दूसरी में छोटा-सा सुराख हो गया था। शिष्य ने सोचाः इससे क्या हुआ? चलेगा। छोटे-से सुराख से क्या बिगड़ने वाला है। अच्छी मशक गुरुजी को दी, सुराखवाली मशक खुद ली। दोनों तैरते-तैरते मझधार में गये। धीरे-धीरे सुराखवाली मशक से हवा निकल गई। शिष्य गोते खाने लगा। गुरुजी को पुकाराः
"गुरुजी ! मैं तो डूब रहा हूँ....।"
गुरुजी बोलेः "कोई बात नहीं। जरा-सा सुराख है इससे क्या हुआ?
"गुरुजी, यह जरा सा सुराख तो प्राण ले लेगा। अब बचाओ.... बचाओ.....!"
गुरुजी ने अपनी मशक दे दी और बोलेः "मैं तो तैरना जानता हूँ। तेरे को सबक सिखाने के लिए आया हूँ कि जीवन में थोड़ा-सा भी दोष होगा वह धीरे-धीरे बड़ा हो जायगा और जीवन नैया को डुबाने लगेगा। थोड़ी-सी गलती को पुष्टि मिलती रहेगी, थोड़ी सी लापरवाही को पोषण मिलता रहेगा तो समय पाकर बेड़ा गर्क होगा।"
"एक बीड़ी फूँक ली तो क्या हुआ?..... इतना जरा-सा देख लिया तो क्या हुआ? .... इतना थोड़ा सा खा लिया तो क्या हुआ?...."
अरे ! थोड़ा-थोड़ा करते-करते फिर ज्यादा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक मन धोखा देगा। साक्षात्कार हो गया तो तुम परमात्मा में टिकोगे। धोखे के बीच होते हुए भी भीतर से तुम सुरक्षित होगे।
उठत
बैठत वही
उटाने।
कहत
कबीर हम उसी
ठिकाने।।
प्राणायाम करने से कर्मेन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। श्वासोच्छ्वास को निहारते हुए अजपाजाप करने से मन की चँचलता कम हो जाती है। मन की चँचलता कम होते ही अपनी गलतियाँ निकालने का बल बढ़ जाता है।
मनः
एव
मनुष्याणां
कारणं
बन्धमोक्षयोः।
मनुष्यों का मन ही अपने बन्धन और मुक्ति का कारण है।
अगर किसी का उत्कर्ष देखकर चित्त में ईर्ष्या होती है तो समझो अपना चित्त मलिन है। 'उसका यश का प्रारब्ध है तो उसको यश मिलेगा। उसके यश में भी मेरा ही परमात्मा है.... ऐसा सोचकर उसके यश का आनन्द लो। किसी को ऊँचे आसन पर बैठा देखकर उससे ईर्ष्या करने के बजाये तुम भी ऊँचे कर्म करो तो तुम भी ऊँचे आसन पर पहुँच जाओगे।' अभी जी ऊँचे आसन पर बैठे हैं उनमें परमेश्वर की कृपा से ऊँचाई है। वाह प्रभु ! तेरी लीला अपंरपार है....' ऐसा सोचकर तुम ऊँचे चले आओ।
ऊँचे आसन पर बैठने से आदमी ऊँचा नहीं हो जाता। नीचे आसन पर बैठने से आदमी नीचा नहीं हो जाता। नीची समझ है तो आदमी नीचा हो जाता है और ऊँची समझ है तो आदमी ऊँचा हो जाता है। ऊँची समझ उन्हीं की है जिनके स्वभाव में अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति आदि दैवी गुणों का विकास होता है।
विषयों में लोलुपता नहीं होनी चाहिए।
रंगअवधूत महाराज नारेश्वरवाले बैठे थे। वलसाड़ से कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया किस्म के आम अवधूतजी के समक्ष लाया। आम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा और काट कर अवधूतजी के सामने रखकर खाने के लिए विनती कीः
"गुरुजी ! ये बहुत बढ़िया आम हैं। आपके लिए वलसाड़ से खास लाये हैं। खाइये।"
अवधूत जी ने कहाः "तुम सहज भाव से दे देते तो मैं खा लेता लेकिन तुमने इनकी इतनी प्रशंसा की कि ये आम ऐसे हैं..... वैसे हैं..... केसरी हैं.... बहुत मीठे हैं.... सुगन्ध आती है.... इतनी प्रशंसा करने पर भी अभी तक मेरे मुँह में पानी नहीं आया। तुम ऐसा कुछ करो कि मेरे मुँह में पानी आ जाय। मैं खाने के लिए लम्पटू हो जाऊँ फिर खाऊँगा, अब नहीं खाता। अपनी श्रद्धा-भक्ति से आम दो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं खा लूँगा लेकिन तुम आम की प्रशंसा करो और मेरे मुँह में पानी आ जाय तो मेरी अवधूती मस्ती को धिक्कार है।"
महादेव गोविन्द रानडे का नाम आपने सुना होगा। उनकी पत्नी ने बढ़िया आम काटकर उन्हें दिया। रानडेजी की एक चीरी खायी फिर हाथ धो लिये। बोलेः
"वह नौकर है न रामा, उसको भी यह आम देना, बच्चों को भी देना, पड़ोस की बच्ची को भी देना।"
"इतना बढ़िया आम है....! आप ही के लिए काटा है। खट्टा है क्या?" पत्नी ने पृच्छा की।
रानडेजी बोलेः "नहीं, आम खट्टा नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा है, स्वादिष्ट है।"
"बहुत बढ़िया है, मीठा है तो आप क्यों नहीं खाते?"
"इसलिए नहीं खाता हूँ कि बढ़िया चीज बाँटने के लिए होती है, भोगने के लिए नहीं होती।"
किसी चीज
को बढ़िया
समझकर भोगने
लग गये तो लोलुपता
आ जायगी।
बढ़िया चीज
दूसरों को
बाँटो ताकि बढ़िया
का आकर्षण घट
जाय, लोलुपता
चली जाय,
अनासक्तियोग
सिद्ध हो जाय,
बढ़िया से
बढ़िया जो
आत्मा-परमात्मा
है उसमें
स्थिति हो
जाय।
श्रीकृष्ण
कहते हैं- अलोलुप्त्वम्।
हम लोग क्या करते हैं? कोई चीज बढ़िया होती है तो ठूँस-ठूँसकर खाते हैं, फिर अजीर्ण हो जाता तो दरकार नहीं। कोई भी चीज बढ़िया मिले तो उसे बाँटना सीखो ताकि उसकी लोलुपता चित्त से हट जाय। लोलुपता बड़ा दुःख देती है।
देह का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए लोग क्या-क्या करते हैं। सौन्दर्य-प्रसाधनों का उपयोग किया जाता है वे चीजें बनाने के लिए कई जीव-जन्तु-प्राणियों की हिंसा होती है, हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। पफ-पावडर, लाली-लिपस्टिक से सजाया हुआ बाहर का दैहिक सौन्दर्य तो उधार का सौन्दर्य। उससे तो तुम्हारा, पति का, तुम पर जिनकी निगाह पड़ती है उनका पतन होता है लेकिन जब हृदय का सौन्दर्य खिलता है तब तुम्हारा, तुम्हारे सम्पर्क में आने वाले का, पति और पड़ोसियों का भी कल्याण होता है। मीरा का सौन्दर्य ऐसा ही था, शबरी का सौन्दर्य ऐसा ही था, गार्गी का सौन्दर्य ऐसा ही था, मदालसा का सौन्दर्य ऐसा ही था। दिल तुम्हारा दिलबर के रँग जाय यह असली सौन्दर्य है। कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधनों से सजाया हुआ सौन्दर्य कब तक टिकेगा ? सच्चे भक्त के हृदय की पुकार होती है किः
"हे भगवान ! तू ऐसी कृपा कर कि तेरे में मेरा मन लग जाय।" भगवान करे कि भगवान में हमारा मन लग जाय। भगवान में मन लगता है तो सचमुच में मन सुन्दर होता है। भोगों में मन लगता है तो मन भद्दा हो जाता है। जब चैतन्य स्वरूप ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के चिन्तन में, ईश्वर के ज्ञान में हमारा मन लगता है तब मन सुन्दर होता है। ज्यों-ज्यों विकारों में, काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में मन लगता है त्यों-त्यों हमारा तन और मन असुन्दर होता है।
ईसरदान नामका एक कवि था। पत्नी चल बसी तो बड़ा दुःखी हो रहा था। काका ने कहा कि चलो, द्वारिका जाकर आयें। देव-दर्शन हो जायेंगे और मन को भी मोड़ जल जायगा।
काका-भतीजा दोनों चले। बीच में जामनगर आता था। वहाँ का राजा जाम कविता-शायरी आदि का बड़ा शौकीन था। इन्होंने सोचा राजा कविता की कद्र करेगा, इनाम मिलेगा तो यात्रा का खर्च भी निकल आयगा और अपना नाम भी हो जायगा।
दोनों राजा जाम के राजदरबार में गये। अपना कवित्व प्रस्तुत किया। कविता-शायरी में राजा की प्रशस्ति अपनी छटादार शैली में सुनायी। राजा झूम उठा। दरबारी लोग वाह वाह पुकार उठे। मंत्री लोग भी चकित हुए कि आज तक ऐसी कविता नहीं सुनी।
कवियों को कितना इनाम देना, कैसी कद्र करना इसका निर्णय करने के लिए राजा ने एक उच्च कोटि के विद्वान राजगुरु पीताम्बरदास भट्ट को आदरपूर्वक अपने दरबार में रखा था। ईसरदान की कविता सुनकर राजा खुश हुए राजा ने कवि को पुरस्कार देने के लिए पीतांबर भट्ट की ओर निहारा।
"जो उचित लगे वह इनाम इस कवि को दे दिया जाय।"
पीतांबर भट्ट ने निर्णय सुना दिया कि इस कवि के सिर पर सात जूते मार दिये जायँ। सुनकर सभा दँग रह गई। पीतांबर भट्ट का सभा में प्रभाव था। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाय? कवि के सिर पर सात जूते मार दिये गये। कवि के दिल में चोट लग गई। 'इतनी बढ़िया कविता सुनाई और पुरस्कार में सात जूते? भरी सभा में ऐसा अपमान? और बिना किसी अपराध के? कुछ भी हो, मैं इस पण्डित को देख लूँगा।' ईसरदान का खून उबल उठा।
कवि सभा छोड़कर चला गया। मन ही मन निर्धारित कर लिया कि, 'इस पीतांबर भट्ट को आज ही यमसदन पहुँचा दूँगा। पत्नी मरने का दुःख इतना नहीं जितना मेरी सरस्वती माता के अपमान से दुःख हुआ है। मेरी कविता का अपमान हुआ है।
कवि ने तलवार तेज कर ली। रात्रि में पीतांबर भट्ट का उनके घर में शिच्छेद करने के इरादे छुपकर कवि उनके घर पहुँचा। पीतांबर भट्ट दिन को कहीं और जगह गये थे। रात्री को देर से अपने घर पहुँचे।
सारे नगर में बिजली की तरह सभावाली बात पहुँच गई थी। जगह-जगह चर्चा हो रही थी कि पीतांबर भट्ट ने आज सभा में एक युवान छटादार कवि का घोर अपमान करवा दिया। उसकी कविता से पूरी सभा नाच उठी थी, राजा जाम भी प्रसन्न हो गये थे। लेकिन पीतांबर भट्ट के प्रभाव में आकर राजा ने कवि को भरी सभा में सात जूते लगवाये... बड़ा अन्याय हुआ।
पीतांबर भट्ट की पत्नी सरस्वती ने यह सब जाना। वह चिढ़ गई कि, 'सरस्वती की पूजा-उपासना करने वाली कवि का ऐसा अपमान मेरे पति ने किया !' वह रूठ गई। रोष में आकर घर का दरवाजा भीतर से बन्द करके, कुंडा लगाकर झूले पर बैठ गई, 'आज उनको घऱ में नहीं आने दूँगी....।'
पीतांबर भट्ट घर लौटे। भट्टजी ने देखा कि घर का दरवाजा भीतर से बन्द है ! हररोज तो पत्नी इन्तजार करती थी, पानी लेकर पैर धुलाने के लिए तैयार रहती थी ! आज कहाँ गई? दरवाजा खटखटाया तो पत्नी की आवाज आयीः
"ऊंह....! क्या है? मैं दरवाजा नहीं खोलूँगी।"
"प्रिये ! तुझे क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोलेगी?" भट्टजी चकित हुए।
पत्नी झुंझलाकर बोलीः "आप वे ही भट्ट जी है जिन्होंने एक कवि को भरी सभा में सात-सात जूते लगवाये? मेरे घर में आपके लिए जगह नहीं है।"
पीतांबर भट्ट कहते हैं- "लोग तो मुझे नहीं समझ पाये लेकिन सरस्वती ! तू भी मुझे नहीं समझती?"
"इसमें क्या समझना है? किसी कवि को सात-सात जूते मरवाना....! आप राजगुरु हो गये तो क्या हो गया? ऐसा घोर अन्याय....?" सरस्वती का रोष नहीं उतरा।
भट्टजी ने कहाः "देवी ! मैंने राजगुरु के मद में या ईर्ष्यावश होकर जूते नहीं मरवाये। तू दरवाजा खोल, तेरे को सारी बात बताता हूँ।"
पत्नी ने द्वार खोला। भट्टजी बैठे झूले पर। पत्नी चरणों में बैठी। राजगुरु कहने लगेः
"कवि की कविता तो बढ़िया थी लेकिन उनमें नारायण के गुण नहीं गाये थे, नर के गुण गाये थे। कवि ने राजा की वाहवाही की थी, खुशामद की थी लेकिन ऐसे हाड़-मांस के हजारों-हजारों राजाओं को बना-बनाकर जो मिटा देता है फिर भी जिसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे सर्वश्वर परमात्मा के लिए एक भी शब्द नहीं था उसकी कविता में।"
छुपकर बैठा हुआ कवि ईसरदान चौकन्ना होकर पति-पत्नी का संवाद सुन रहा था। भट्टजी आगे कहने लगेः
"भगवान ने कवि को कवित्व-शक्ति दी है तो क्या इन राजा-महाराजाओं की, अहंकार के पुतलों की प्रशंसा करके उन्हें अधिक अहंकारी बनाकर नरक की ओर भेजने के लिए दी है? सर्वेश्वर परमेश्वर के गीत गाने के लिए कवित्व-शक्ति मिली है। जिहृवा दी है जीवन दाता ने तो उसके गुणगान करने के लिए दी है कवि अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं अपितु दुरुपयोग कर रहा था। वह बड़ा विद्वान था, सरस्वती का उपासक था लेकिन उसकी पूरी कविता में एक भी शब्द भगवान के लिए नहीं था। जिस जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं, जिस दिल में परमात्मा के लिए प्यार नहीं, जिस कविता में परमात्मा के लिए पुकार नहीं वह कविता है कि बकवास है? मैंने उस होनहार कवि को सजा करवा दी, ताकि वह अपने गौरव में जाग जाय, शायद....।"
पीतांबर भट्ट की वाणी सुनते ही ईसरदान का दिल पिघल गयाः 'ये पीतांबर भट्ट वास्तव में सुलझे हुए महापुरुष हैं। इनका वध करने को आया था....! धिक्कार है मुझे !'
प्रायश्चित से पाप जल जाते हैं। ईसरदान आकर भट्ट जी के चरणों में गिर पड़ा। अपने आँसुओं से उनके चरणों पर अभिषेक किया। राजगुरु ने कवि को उठाकर अपने गले लगा लिया और आश्चर्य भी हुआ।
"कविराज कविराज....! ऐसी अंधेरी मध्यरात्री में यहाँ कैसे?"
"महाराज ! आया था आपकी हत्या करने के लिये लेकिन अब पता चला कि जन्मों-जन्मों से मैं अपनी हत्या कर रहा था। आज आपने मेरे दिलरूपी कपाट पर जोरदार चोट मारकर अनंत का द्वार खोल दिया है। कविता वास्तव में उस परम कवीश्वर के लिए होनी चाहिए, जिह्वा वास्तव में उस जीवनदाता के लिए चलनी चाहिए। जीवन इतना कीमती है यह मैं नहीं जानता था। महाराज ! मैं आपका बालक हूँ। मुझे क्षमा करना। मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों में बैठकर भागवत की कथा श्रवण करूँ, भागवत पढ़ूँ, भक्तिरस-पान करूँ। मुझमें प्राणबल तो है, क्रियाबल तो है लेकिन भावबल आप मिलायेंगे तब मुझ निर्बल को उस परमेश्वर का, उस देवेश्वर का, उस विश्वेवश्वर का प्रेमबल प्राप्त होगा जिससे जीवन सार्थक हो जायगा। महाराज ! मुझे स्वीकार कीजिए। आपके चरणों में बैठने का अधिकार दीजिए। महाराज ! मुझे भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। भावना के बिना का जो बल है वह रावण और कंस जैसा है और भावना सहित का जो बल है वह बुद्ध पुरुषों का बल है। महाराज ! मुझमें भगवद् भाव भर जाय ऐसी कथा कृपा करके सुनाइये।"
पीतांबर भट्ट प्रसन्न हुए। कवि को भागवत की कथा सुनाई। भगवच्चर्चा, भगवत्-ध्यान, भगवद् गुणानुवाद से कवि भावविभोर हो गया। फिर उसने 'भक्तिरस' नाम का ग्रन्थ लिखा। अपनी कविता में भागवत लिखा और द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करने को गया। कथा कहती है कि कवि ज्यों ही अपन ग्रंथ भगवान को अर्पित करने को गया तो भगवान की मूर्ति मुस्कुरायी और हाथ लम्बा करके कवि के उस ग्रंथ को स्वीकार कर लिया।
हमारी वाणी, हमारी कविता, हमारी अक्ल और हमारी हुशियारी में अगर परमात्म-प्राप्ति की दिशा नहीं है तो ऐसी वाणी, कविता, अक्ल और हुशियारी से क्या लाभ? तुलसीदास जी कहते हैं-
चतुराई
चूल्हे पड़ी
पूर पर्यो
आचार।
तुलसी
हरि के भजन
बिन चारों
वर्ण चमार।।
वह चतुराई किस काम की जिस चतुराई में चैतन्य का प्यार न हो ! वह कविता किस काम की जिस कविता में राम के गीत न भरे हों... प्रभु के गीत न गूँजते हों? वह जीवन किस काम का जिस जीवन में जीवनदाता की ओर यात्रा न हो? ऐसे तो लोहार की धौंकनी भी श्वासोच्छ्वास भरती है, निकालती है।
पैसे बढ़ जाय तो क्या बड़ी बात है? गाड़ी आ जाय तो क्या बड़ी बात है? मुसीबत बढ़ी और क्या हुआ?
साहेब
ते इतना
माँगूं नव
कोटि सुख
समाय।
मैं
भी भूखा ना
रहूँ साधू भी
भूखा न जाय।।
तुम्हारी भक्ति बढी कि नहीं बढ़ी, तुम्हारी समता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तुम्हारी अहिंसा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तुम्हारी प्रेम की धारा बढ़ी कि नहीं बढ़ी अपने भीतर का खजाना देखो। रूपये बढ़ गये, मकान बढ़ गये, गाड़ियाँ बढ़ गईं तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ गई। साधन बढ़ें उसके साथ साधना नहीं बढ़ी तो आदमी भीतर से कंगाल होता जायेगा। भीतर से कंगाल होने के बजाय बाहर से कंगाल होना हजार गुना अच्छा है।
इन्द्रियों का अलोलुप्त्व दृढ़ होना चाहिए। रंभा आ गई फिर भी शुकदेव जी चलित नहीं हुए। सोलह हजार एक सौ आठ अंगनाएं श्रीकृष्ण के आगे ठुमक-ठुमक कर रही हैं फिर भी श्रीकृष्ण का चित्त चलित नहीं होता। इन्द्रियों के विषय उपलब्ध होते हुए भी चित्त में अलोलुप्त्व आ जाय तो समझ लेना, हृदय में भगवान की भक्ति फल गई, चित्त में आत्म प्रसाद जगमगा रहा है, जीवन धन्य हुआ है। उसकी मीठी निगाह भी जिन पर पड़ती है वे भी धन्य होने लगती हैं।
दुर्योधन के साथ केवल शकुनि ही रहता, भीष्म जैसे प्रतिज्ञा में दृढ़ और कर्ण जैसे दानी नहीं रहते तो भारत की दशा जो आज है उससे बहुत कुछ उन्नत होती। भीष्म और कर्ण जैसे लोग श्रीकृष्ण के दैवी कार्य में अपनी शक्ति और ओज लगाते, ज्ञान, भक्ति और सत्कर्म के प्रचार-प्रसार में अपना सामर्थ्य अर्पित करते तो आज के समाज की रौनक कुछ और होती। ये महारथी दुर्योधन और शकुनि के बीच जी-जीकर, उनके टुकड़े खा-खाकर बँध गये। उनमें तेज और सत्त्व तो था लेकिन ढँक गया था।
सज्जन आदमी दुर्जन के सम्पर्क में ज्यादा रहे, निन्दक के संग में ज्यादा रहे तो सज्जन आदमी भी घसीटा जाता है। जैसे कर्ण घसीटा गया, युधिष्ठिर घसीटे गये और देश को सहना पड़ा।
हम लोग
भी अपने अड़ोस-पड़ोस
में दुर्जन के
वातावरण में
घसीटे न जायें, अपनी
सज्जनता को
परमात्मा के
ज्ञान से, परमात्मा
के ध्यान से, परमात्मा
के जप से,
परमात्मा
के स्मरण से
दिव्य बनाकर
श्रीकृष्ण-तत्त्व
के
साक्षात्कार
में लगायें, संत और
भगवान के दैवी
कार्य में
लगायें....।
नारायण.... नारायण..... नारायण..... नारायण.... नारायण.....।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
साधक को विश्वास करना चाहिए कि भगवान मुझे इसी वर्त्तमान जन्म में ही अभी मिल सकते हैं। इसमें कोई कठिनता नहीं है। क्योंकि भगवान से हमारी देशकाल की दूरी नहीं है। वे हमारी जाति के हैं और हमारे जीवन में उनको प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। भगवान के शरण होते हुए ही भगवान हमें तुरन्त अपना लेंगे। हमारे अनन्त जन्मों के दोष तुरन्त मिटा देंगे। हमारे अभिमान ने ही हमें बाँध रखा है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
दैवी
सम्पदा - ३
(दिनांकः
५-८-१९९०
रविवार, अहमदावाद
आश्रम)
तेजः
क्षमा धृतिः
शौचमद्रोहोनातिमानिता।
भवन्ति
संपदं
दैवीमभिजातस्य
भारत।।
'तेज, क्षमा, धैर्य, आंतर-बाह्य शुद्धि, किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव – ये सब तो हे अर्जुन ! दैवी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं।'
(भगवद्
गीताः १६-३)
जिसके जीवन में भी दैवी सम्पदा का प्रभाव है उसमें एक विलक्षण तेज आ जाता है। खा-पीकर, चिकने पदार्थ, पफ-पावडर, लाली-लिपस्टिक लगाकर देदीप्यमान बनना यह तो राजसी तेज है। बाह्य सौन्दर्य वास्तविक सौन्दर्य नहीं है। वास्तविक सौन्दर्य दैवी सम्पदा है। दैवी सम्पदा के तेज और सौन्दर्य से व्यक्ति आप भी खुश रहता है, तृप्त रहता है। निर्विकारी सुख पाता है और दूसरों को भी निर्विकारी नारायण के आनन्द में सराबोर कर देता है।
राजसी और आसुरी सुख आप भी मुसीबत और हिंसा अहिंसा का सहारा भोगा जाता है और जिनसे यह सुख भोगता है उन लोगों का भी शोषण होता है।
जिसके जीवन में दैवी सम्पदा है उसमें ज्ञानवान का तेज होता है। ज्ञानवान के समीप बैठने से अपना चित्त शांत होने लगता है, ईश्वर के अभिमुख होने लगता है। उन महापुरुष की उपस्थिति में हमारे कुविचार कम होने लगते हैं। उनका तेज ऐसा होता है कि हृदय को शांति, शीतलता और ज्ञान-प्रसाद से पावन करता है। कभी कभी तो अति क्रोधी, अति क्रूर आदमी या गुंडा तत्त्वों के कहने से भी लोग काम करने लगते हैं लेकिन गुंडा तत्त्वों का तेज विकार का तेज है। वे अपना मनचाहा करवा लेते हैं। सामनेवाला उनका मनचाहा कर तो देगा लेकिन उसके भीतर आनन्द और शांति नहीं होगी। महापुरुष का तेज ऐसा है कि वे अपने मनचाहे कीर्तन, ध्यान, भजन, साधना, सदाचार आदि में लोगों को ढाल देते हैं, ईश्वर के अभिमुख बना देते हैं। महापुरुष के संकेत के अनुसार जो ढलते हैं उनको भीतर आनन्द, शांति, सुख और कुछ निराला अलौकिक अनुभव होता है।
कभी किसी के डण्डे के तेज से कोई काम कर दे तो काम करने वाले का कल्याण नहीं होता। काम कराने वाले का उल्लू सीधा होता है। महापुरुषों का तेज ऐसा होता है कि अपना चित्त तो परमात्म-रस से पावन होता ही, जिनसे वे भक्ति, ज्ञान, सेवा, स्मरण, साधना करवाते हैं, जिनको भीतर से दैवी शक्ति का धक्का लगाते हैं उनके जीवन का भी उद्धार हो जाता है। महापुरुषों का ऐसा सात्त्विक तेज होता है। दूसरी विशेष बात यह है कि जिनमें ये दैवी गुण होते हैं उन महापुरुषों में अभिमान नहीं होता कि मुझमें ये दैवी गुण हैं, मुझमें तेज है, मुझमें क्षमा है, मुझमें धैर्य, शौच, उदारता, आचार्योपासना, दान, दम इत्यादि है। इस प्रकार का अहं उनके चित्त में नहीं होता। वे जानते हैं कि दैवी गुण देव के होते हैं। देव तो परमात्मा है। विभु, व्यापक, सच्चिदानन्द देव है। गुण हैं देव के और कोई अपने मान ले तो दैवी गुणों के साथ-साथ चित्त में जो आसुरी स्वभाव है उसका रंग लग जाता है। किसी का सत्य बोलने का आग्रह, अच्छी बात है, बहुत सुन्दर बात है लेकिन 'मुझमें सत्य बोलने का गुण है' यह अगर दिख रहा है, उसका अहं आ रहा है तो यह अहं आसुरी है। किसी में ब्रह्मचर्य-पालन का गुण है, क्षमा का गुण है, लेकिन 'मैं क्षमावान हूँ या मैं ब्रह्मचारी हूँ' इस प्रकार का भीतर अहं होता है तो दैवी गुण के साथ जो आसुरी स्वभाव का जो हिस्सा पड़ा है वह काम करता है।
जिसके जीवन में दैवी स्वभाव ओतप्रोत हो गया है उसको यह भी नहीं होता है कि 'मैं सत्यवादी हूँ... मैं ब्रह्मचारी हूँ... मैं तेजस्वी हूँ... मैं क्षमावान हूँ.... मैं सच्चा हूँ... मैं उदार हूँ.... मैं आचार्योपासक हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ.... फिर मुझे दुःख क्यों मिलता है? .... मैंने इतनी भक्ति की फिर भी मेरा ऐसा क्यों हो गया?...।' उसके जीवन में इस प्रकार की छोटी-मोटी कल्पना की शिकायत नहीं होती। अगर शिकायत होती है तो दैवी सम्पदा से सम्पन्न महापुरुष उसे समझाते हैं किः हे वत्स !
अपने
दुःख में रोने
वाले !
मुस्कुराना
सीख ले।
दूसरों
के दर्द में
आँसू बहाना
सीख ले।।
जो
खिलाने में
मजा है आप
खाने में
नहीं।
जिन्दगी
में तू किसी
के काम आना
सीख ले।।
अपनी वासना मिटेगी तो दैवी सम्पदा बढ़ेगी।
अंतःकरण की अशुद्धि दो कारणों से होती हैः एक कारण है सुख की लालसा और दूसरा कारण है दुःख का भय। सुख की लालसा और दुःख का भय हमारा अंतःकरण मलिन कर देता है। अंतःकरण मलिन होने से हम तत्त्वतः देव से निकट होते हुए भी अपने को देव से दूर महसूस करते हैं। संसार की उलझनों में उलझ जाते हैं। अतः अंतःकरण में जो सुख की लालच है उसको मिटाने के लिए सुख देना सीख ले, दूसरे के काम आना सीख ले। अपने दुःख में रोने वाले ! तू मुस्कुराना सीख ले।
जो अपने दुःख को पकड़कर रोते रहते हैं उनको मुस्कुराकर अपने दुःख को पचा लेना चाहिए और सुख बाँटना चाहिए। इससे अंतःकरण की मलिनता दूर हो जायगी। अंतःकरण की मलिनता दूर होते ही वह तेज आने लगेगा।
खा-पीकर पुष्ट होकर अथवा ठण्डे प्रदेश में रहकर चमड़ी का रंग बदलकर तेजस्वी होना यह उल्लू के पट्ठों का काम है, ब्रह्मवेत्ताओं का काम कुछ निराला होता है।
'मैं बड़ा तेजस्वी बनकर आया, क्योंकि इंग्लैण्ड मे रहा था, अमेरिका मे रहा था।'
अरे भैया ! इंग्लैण्ड में अगर तेजस्वी हो जाते हो, अमेरिका में तेजस्वी हो जाते हो, हिमालय में रहकर तेजस्वी हो जाते हो तो यह तेज की विशेषता चमड़ी की विशेषता है, तुम्हारे उस प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की विशेषता का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र महाराज कहाँ गये थे इंग्लैण्ड और अमेरिका में चमड़ा बदलने को? उनका शरीर तो आठ वक्रताओं से अभिभूत था। ऐसे अष्टावक्र का तेज विशाल राज्य, विशाल बाहु, विशाल विद्या, विशाल धनराशि के स्वामी राजा जनक को आकर्षित करता है, आत्मशांति प्रदान करता है। अष्टावक्र के अंग टेढ़े, टाँगे टेढ़ी, चाल टेढ़ी, लेकिन उनकी वाणी में ब्रह्मतेज था, चित्त में आत्मतेज था उसको देखकर राजा जनक उनके चरणों में बैठे। मीरा का तेज ऐसा था कि उसकी निन्दा और विरोध करने वाले लोग उसकी हत्या करने के लिए तैयार होकर मीरा के पास आये तो उनका चित्त बदल गया।
भगवान के भक्तों का और ब्रह्मवेत्ताओं का तेज दूसरों के दुःख-दर्द को निवारनेवाला होता है। साधक को यह तेज अपने में लाना चाहिए।
कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दैवी सम्पदा के गुण जन्मजात होते हैं। जैसे नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, शुकदेवजी महाराज, मीरा, सुलभा आदि में ये गुण स्वभाव से ही थे। उनका क्षमा, धैर्य, ब्रह्मचर्य के तरफ झुकाव अपने आप था। साधक को साधन-भजन, नियम-व्रत का सहारा लेकर ये गुण अपने में लाने होते हैं। जिनमें ये गुण जन्मजात हैं उन्होंने कभी न कभी ये गुण साधे होंगे। हम लोग अभी साध सकते हैं। जिनके कुछ गुण साधे हुए हैं वे ज्यादा साधकर देव में स्थित हो सकते हैं।
दैवी सम्पदा के गुणों में से जितने अधिक गुण अपने जीवन में होंगे उतना जीवन 'टेन्शन' रहित, चिंतारहित, भयरहित, शोकरहित, दुःखरहित, उद्वेगरहित होगा। दैवी सम्पदा के गुण जितने गहरे होंगे उतना आदमी उदार होगा, सहनशील होगा, क्षमावान होगा, शूरवीर होगा, धैर्यवान होगा, तेजस्वी होगा। ये सारे गुण उसके लिए और उसके सम्पर्क में आने वालों के लिए सुखद हो जाते हैं।
महापुरुषों की उस शक्ति का नाम 'तेज' है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रवृत्तिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायचरण और दुराचार से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं।
महापुरुषों में दूसरा गुण है क्षमा।
क्षमा मोहवश भी की जाती है, भयवश भी की जाती है लेकिन दैवी सम्पदा की क्षमा कुछ विलक्षण है। पुत्र ने, पत्नी ने, कुटुम्ब ने कुछ अपराध किया, उनमें मोह है तो चलो, घूँट पी लिया, सह लिया। यह मोहवश की गई क्षमा है।
इन्कमटैक्स का इन्सपैक्टर आ गया। ऐसा-वैसा बोलता है, कुछ कड़वी-मीठी सुना रहा है। दिल में होता है कि 'यह न बोले तो अच्छा है, यहाँ से टले तो अच्छा है। फिर भी क्या करें? चलो जाने दो।' यह भयवश की गई क्षमा है। अगर कुछ बोलेंगे तो वह कागजों से कड़क व्यवहार करेगा, धन की हानि हो जायेगी।
नौकर गलती करता है। डाँटेंगे तो चला जायेगा। दूसरा आदमी अभी मिलता नहीं, चलो इसको क्षमा कर दो। जब अच्छा नौकर मिल जायेगा तो इसे निकाल देंगे।
मोह से, भय से, स्वार्थ से या और किसी कारण से जो क्षमा की जाती है वह दैवी सम्पदा का गुण नहीं है। दैवी सम्पदावाले की क्षमा की कुछ निराली होती है। जैसे, भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषशैय्या पर लेटे हैं। भृगु ऋषि ने उनकी छाती में लात मार दी। नारायण अपने नारायण तत्त्व में इतने आनन्दित और प्रसन्न हैं, तृप्त हैं कि बाहर से विक्षेप आने पर भी अपना आनन्द-स्वभाव प्रकटाने में उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता।
'मुनीश्वर ! आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? दैत्य-दानवों के साथ युद्ध करके हमारा हृदय जरा कठोर हो गया है। इस कठोर हृदय पर आपका कोमल चरण लगा है तो आपके चरण को कोई ठेस तो नहीं पहुँची?'
क्षमा
बड़न को होत
है छोटन को
उत्पात।
विष्णु
को क्या घटी
गयो जो भृगु
ने मारी लात।।
ब्रह्मवेत्ताओं में क्षमा इस प्रकार की क्षमा होती है।
क्षमाशील होने में दो बातें चाहिए। अपने लिए बाहर की वस्तुओं के सुख-भोग का आकर्षण न हो। कोई अपना कुछ बिगाड़े तो उसका अहित करने का भाव न हो। ऐसा आदमी क्षमाशील हो जाता है। वही सच्चा क्षमाशील होता है।
जिसके पास क्षमारूपी शस्त्र है, शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसको कुछ चाहिए, बदला लेना है अथवा सुख लेना है, जिसको कुछ लेना है उसमें क्रूरता है। जिसको कुछ लेना नहीं, देना ही देना है उसके जीवन में क्षमा ही क्षमा है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनन्द ही आनन्द है।
धृति का अर्थ है धैर्य। जो सत्कर्म करते हैं या ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो कोई विघ्न-बाधा आये तो धैर्य से सहें। थोड़ा सा विघ्न आया, कष्ट पड़ा तो सोचने लगा किः "मैं आत्महत्या कर लूँ.... मैं कहीं भाग जाऊँ.... अथवा अलग मकान लेकर रहूँ.....' यह दैवी सम्पदा नहीं है, आसुरी सम्पदा है। यह आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। दैवी स्वभाव यह है कि कितने भी कष्ट आ जाय, कितनी भी मुसीबतें आ जाय लेकिन चित्त पर क्षोभ नहीं होता, चित्त विघ्नों से प्रभावित नहीं होता।
मीरा के जीवन में न जाने कितने विघ्न आये ! मीरा के ससुर सांगा राणा के देहावसान के बाद मीरा के देवर रतनसिंह और ननद उदा ने मीरा को सताना चालू कर दिया। रतनसिंह ने मीरा को सुधारने के लिए अपनी बहन उदा और उसकी सहेली को काम सौंपा। 'मेवाड़ की रानी होकर मीरा साधु-बाबाओं से, न जाने कैसे-कैसे लोगों से मिलती है.....बात करती है? उसको सुधारो।'
अब, मीरा को क्या सुधारना है? वह तो प्रभु के गीत गाती है। बिगड़े हुए लोग किसी को सुधारने का ठेका लेते हैं तो सत्संगियों को सुधारने का ही ठेका लेते हैं।
उदा ने मीरा को बहुत दुःख दिया लेकिन मीरा ने कभी नहीं सोचा कि, 'मैं अलग महल में रहूँ.... मैं भाग जाऊँ... किसी को जहर दे दूँ और बदला लूँ....' नहीं, मीरा तो भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। दैवी सम्पदा से सम्पन्न व्यक्ति बड़ा शांत होता है। उसका चित्त विलक्षण लक्षणों से सम्पन्न होता है।
मीरा की भक्ति देखकर उदा जलती थी। उसको काम सौंपा गया था कि मीरा को सुधारो। कृष्ण-कन्हैया बंसी बजैया की सेवा-सुश्रूषा छोड़कर जैसे और लोग काम-क्रोध के, लोभ-मोह के दलदल में फँस मरते हैं ऐसे ही मीरा भी फँस मरे ऐसा उनका प्रयोजन था। संसार के दलदल में फँस मरने वाले ऐसा नहीं मानते कि हम फँस मरते हैं। फँस मरने वाले समझते हैं कि यही सच्चा जीवन है, भगत का जीवन ही बेकार है। भक्त सोचता है कि ये बेचारे फँस मरे हैं, इनको निकालूँ तभी इन्हें सच्चे जीवन का पता चलेगा।
जब तक व्यक्ति के जीवन में आंतरिक प्रकाश नहीं आता तब तक समझता है कि खाना-पीना, बढ़िया कपड़े पहनना, पेट को दिल्ली दरवाजा का बाजार बनाकर उसमें ठूँसते ही जाना, यही जिन्दगी है।
नही...। ठूँस-ठूँसकर खाने को जिन्दगी नहीं कहते, ड्रायक्लीन कपड़े पहनने को जिन्दगी नहीं कहते। हजार-हजार दुःख और मुसीबतों की आँधी और तूफान आये फिर भी दिल को न हिला सके ऐसे दिलबर के साथ एक हो जाने को ही जिन्दगी कहते हैं।
न
खुशी अच्छी है
न मलाल अच्छा
है।
यार
जिसमें रख दे
वह हाल अच्छा
है।।
हमारी
न आरजू है न
जुस्तजू है।
हम
राजी हैं
उसमें जिसमें
तेरी रजा है।।
प्रभु की मस्ती में जो मस्त हैं उनको दुनिया के भोग-विलासों की आवश्यकता क्या है? वे भोजन तो करेंगे औषधवत्। वस्त्र तो पहनेंगे शरीर की आवश्यकता के मुताबिक। आवास में तो रहेंगे लेकिन आवास के लिए जिन्दगी बरबाद नहीं करेंगे। भोजन और वस्त्रों के लिए जिन्दगी बरबाद नहीं करेंगे। वे तो जिन्दगी को आबाद करेंगे जिन्दगी के अधिष्ठान को जानने के लिए। ये दैवी सम्पदा के लोग होते हैं। ऐसे पुरुषों का तेज निराला होता है। उनमें काफी धैर्य होता है।
शौच का अर्थ है शुद्धि। शुद्धि दो प्रकार की होती हैः आंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि तो साबुन, मिट्टी, पानी से होती है और आन्तर शुद्धि होती है राग, द्वेष, वासना आदि के अभाव से। जिनकी आन्तर शुद्धि हो जाती है उनको बाह्य शुद्धि की परवाह नहीं रहती। जिनकी बाह्य शुद्धि होती है उनको आन्तर शुद्धि करने में सहाय मिलती है। पतंजलि महाराज कहते हैं कि शरीर को शुद्ध रखने से वैराग्य का जन्म होता है। शरीर को शुद्ध रखने से वैराग्य का जन्म कैसे? जिसमें शारीरिक शुद्धि होती है उसको अपने शरीर की गन्दगी का ज्ञान हो जाता है। जैसी गन्दगी अपने शरीर में भरी है ऐसी ही गन्दगी दूसरों के शरीर में भी भरी है। अतः अपने शरीर में अहंता और दूसरों के शरीर के साथ विकार भोगने की ममता शिथिल हो जाती है। हृदय में छुपा हुआ आनन्द-स्वरूप चैतन्य, ईश्वर, परमात्मा हमारा लक्ष्य है – इस ज्ञान में वे लग जाते हैं।
पतंजलि महाराज कहते हैं-
शौच
प्रतिष्ठायां
स्वांगजुगुप्सा
परैरसंसर्गः।
'जब आन्तर-बाह्य दोनों प्रकार के शौच दृढ़ हो जाते हैं तो योगी को अपने शरीर पर एक प्रकार की घृणा उत्पन्न होती है और दूसरों के शरीर के संसर्ग की इच्छा भी नहीं होती।'
शौच से शरीर में आसक्ति कम होती है। शरीर से निकलने वाली गन्दगी से घृणा होकर आदमी का चित्त वासना से निर्मुक्त होने लगता है।
बुद्ध के जमाने में काशी में एक नगर सेठ था। उसके पुत्र का नाम था यशकुमार। यशकुमार के लिए पिता ने तीन मौसम के लिए तीन महल बनाये थे। राग-रागिनी आलापने वाली गायिकाएँ, नर्तकियाँ, दासियाँ यशकुमार को घेरे रहती थीं। अपार धनराशि थी। पिता को बड़ी उम्र में बेटा हुआ था इससे अत्यंत लाडला था। उसे कहीं वैराग्य न लग जाय, बुद्ध के भिक्षुकों का रंग न लग जाय इसके लिए यह सब इन्तजाम किया गया था। जैसे सिद्धार्थ (बुद्ध) के लिए उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को ऐहिक सुखों में गरकाव करने के लिए व्यवस्था की थी ऐसे ही यशकुमार को उसके पिता ने ऐहिक सुखों में गरकाव कर दिया। लेकिन भगवान अपने प्यारों को सदा गन्दगी में, गन्दे-विचारों में पचने नहीं देना चाहते।
एक रात्रि को गायन-वादन सुनते-सुनते, नृत्य देखते-देखते यशकुमार किसी कारणवशात् जल्दी से सो गया। नींद आ गई। रात्रि को जल्दी सोने से शरीर की थकान बहुत अच्छी तरह से मिटती है। इतर समय की नींद की अपेक्षा रात्रि को नौ से बारह की नींद ढाई गुना ज्यादा लाभ करती है। बारह से तीन की नींद दुगना लाभ करती है। तीन से छः की नींद डेढ़ गुना लाभ करती है। सूर्योदय के बाद की नींद जीवन में आलस्य-प्रमाद लाकर हानि करती है।
दैवयोग से एक दिन राजकुमार जल्दी सो गया। मध्यरात्रि के बाद डेढ़ दो बजे उनकी नींद खुल गई। देखता है कि नाचने गाने वाली स्त्रियाँ सब सोई पड़ी है। खुर्राटे भर रही हैं.... किसी के मुँह से लार निकल रही है, किसी का हाथ विचित्र ढंग में पड़ा है, पफ-पावडर, लाली-लिपस्टिक का 'मेक-अप' उस जमाने में जो कुछ होगा वह सब गड़बड़ हो गया है, बाल बिखरे पड़े हैं। यशकुमार दीये की लौ तेज करके सबकी हालत देख रहा है। शाम के वक्त हार-सिंगार, वस्त्र-आभूषणों से सजी-धजी, हास्य-विलास करती हुई रमणियाँ अभी घृणास्पद हालत में पड़ी हुई वीभत्स लग रही हैं। वह सोचने लगाः
"क्या इन्ही अंगनाओं के पीछे मैं पागल हुए जा रहा हूँ? जिनके मुँह से लार निकल रही है, जिनके नाक में गन्दगी भरी है ये ही स्त्रियाँ मुझे सुन्दर लग रही थी? इनमें सुन्दरता जैसा है क्या? मेरा नाम यशकुमार है पर अपयश हासिल हो ऐसा काम कर रहा हूँ !
इन हाड़-मांस के सुन्दर दिखने वाले पुतलों में सौन्दर्य अपना नहीं है। सौन्दर्य तो किसी और का है। उस तत्त्व का संपर्क (कनेक्शन) टूट जाय तो मुर्दे हो जाते हैं। धिक्कार है मुझे कि मैं इनके हाड़-मांस के शरीर को प्यार करते हुए इनके साथ अपना भी यौवन नष्ट करता हूँ। इस छोटी-सी उम्र में मुझे बुढापे के लक्षणों ने घेर लिया है ! मैं यौवन में ही बूढ़ा हो रहा हूँ ! मेरा शरीर अभी से रुग्ण होने जा रहा है !'
जितना
माणिया भोग
उतना भया रोग।
"हाय ! यह मैं क्या कर रहा हूँ?"
यशकुमार को अपने आप पर ग्लानि हुई। उसका दिमाग चकराने लगा। वह धरती पकड़कर बैठ गया। फिर से उन थूक और लार टपकाती हुई, खुर्राटे भरती, गन्दी और अस्तव्यस्त लाशों जैसी पड़ी हुई नर्तकियों को निहारने लगा। यह देखकर उसके चित्त में वैराग्य का तूफान उठा।
अपने दोषों की निन्दा करने से पाप जल जाते हैं। दूसरों की निन्दा करने से पुण्य जल जाते हैं।
यशकुमार का अंतःकरण थोड़ा शुद्ध हुआ। यशकुमार उठा। सीढ़ी का हाथा पकड़ते हुए धीरे से नीचे उतरा। चुपचाप... दरवाजे का खटका किये बिना बाहर निकला। महल और संसार का त्याग करके यशकुमार वहाँ से रवाना हो गया।
प्रभात काल में भगवान बुद्ध गंगाकिनारे अपने विहार में टहल रहे थे। उनके चरणों में यशकुमार जा पड़ा। बोलाः
"भन्ते ! संसार धोखा है, दुःख रूप है। उससे बाहर निकलना दुष्कर है, मुश्किल है।"
बुद्ध ने कहाः "संसार धोखा जरूर है, दुःखरूप जरूर है लेकिन उससे निकलना आसान है अगर किसी संत का सान्निध्य मिल जाय तो।"
"भगवन् ! मैं आपकी शरण आया हूँ। मुझे स्वीकार करो।"
बुद्ध ने यशकुमार को अपना लिया, थोड़ा उपदेश दिया।
सुबह हुई। महल में नर्तकियाँ, दासियाँ जागीं। देखती हैं कि यशकुमार का कहीं पता नहीं है। 'कहाँ गये हमारे स्वामी? हमारे सर्वेसर्वा? हमारे प्रियतम्?'
स्वामी, सर्वेसर्वा, प्रियतम सदा के लिए तो किसी के रहते नहीं हैं। किसी का भी संबंध सदा के लिए नहीं रहता। कैसा भी प्रियतम हो, कैसी भी प्रिया हो लेकिन कभी न कभी, कहीं न कहीं झगड़ा, विरोध, विनाश अवश्य हो आता ही है। जो एक दूसरे के हाड़-मांस-चाम को देखकर शादी कर लेते हैं उनमें झगड़ा होना बिल्कुल नियत है। यह जरूरी भी है। प्रकृति का यह विधान है कि जो प्रेम परमात्मा से करना चाहे वह प्रेम गन्दगी भरे नाक से किया तो तुम्हें धोखा मिलना ही चाहिए। जो प्यार ईश्वर से करना चाहिए वह अगर चमड़े-रक्त-नसनाड़ियों से, लार और थूक से भरे शरीर से किया, शरीर के भीतर बैठे परमात्मा की ओर निगाह नहीं गई तो उन शरीरों से दुःख, दर्द, बेचैनी, मुसीबत, अशांति, कलह मिलना ही चाहिए। यह प्रकृति का अकाट्य नियम है। जो भरोसा परमेश्वर पर करना चाहिए वह अगर बाहर की सत्ता पर किया तो गये काम से। जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए वह भरोसा अगर किसी पद पर, प्रतिष्ठा पर, किसी वस्तु या व्यक्ति पर किया तो व्यक्ति, वस्तु, पद-प्रतिष्ठा खींच लिये जायेंगे।
ईश्वर के सिवाय का जो भी सहारा अंतःकरण में घुस गया है उस सहारे में विघ्न आता ही है। विघ्न इसलिए आते हैं कि मौत के समय ये सहारे छूट जाएँ उससे पहले शाश्वत सहारे को पाकर अमर हो जाओ।
यशकुमार के पिता महल में आये, माँ आयी। पूछने लगेः "पुत्र कहाँ है... बेटा कहाँ है?"
नर्तकियाँ, दासियाँ से रही हैं। किसी ने दिखावे का रोना रो लिया तो माँ ने मोहयुक्त रोना से लिया। शोकमग्न माहौल बन गया। अनुचरों ने यशकुमार के पदचिन्हों का पीछा करके पता लगा लिया कि यशकुमार बुद्धविहार में पहुँचा है। माता-पिता पुत्र के पास गये, समझाने लगे किः
"हे पुत्र ! इतना धन-वैभव, सुख-संपत्ति छोड़कर तू भिक्षुक होकर इधर फकीरों के पास रहता है? चल बेटा ! घल चल मेरे लाडले !"
बुद्ध ने देखा कि अभी-अभी इस युवक के चित्त में वैराग्य के अंकुर पनपे हैं। अभी इन अंकुरों को सींचना चाहिए, न कि संसार के विषयों की तपन देकर जलाना चाहिए। वे यशकुमार के माता-पिता से कहने लगेः
"हे श्रेष्ठि ! अभी इसके पुण्य उदित हुए हैं इसलिए नश्वर छोड़कर शाश्वत की ओर आया है। अब तुम्हारे कहने से फिर संसार के कीचड़ में हाड़-मांस चाटने-चूँथने में अपनी जिन्दगी बरबाद नहीं करेगा।" बुद्ध ने यशकुमार के वैराग्य को सहारा दिया।
जो बोधवान पुरुष हैं उनमें यह तेज होता है कि जिससे विलासी और विकारी लोगों में निर्विकार नारायण की ओर यात्रा करने की रूचि हो जाय। कहीं फिसलते हों तो ऐसे महापुरुषों का सान्निध्य-सेवन करें तो फिसलाहट से बच जाएँ। ऐसा दिव्य महापुरुषों का प्रभाव होता है।
बुद्ध ने कुछ वचन यशकुमार को कहे और माता-पिता को ज्ञान-वैराग्य समझाया। इतने में यशकुमार की बहन रोती आयीः
"भैया ! तुम घर चलो...।''
"भैया तो घर चले लेकिन मृत्यु जब आयगी तब मृत्यु से भैया को तू नहीं बचा पायेगी, बहन !" अब यशकुमार अपने कुटुम्बीजनों को समझाने लगा।
"हे माता-पिता ! मौत मुझे पकड़कर शूकर-कूकर बना देगी तब आप लोग मेरा साथ नहीं दे पाओगे। मौत आकर मुझे शूकर-कूकर की योनि में धकेल दे, वृक्ष-पाषाण बना दे उससे पहले मैं बुद्ध के चरणों में बैठकर परमात्मा को पा लूँ। इसमें आप लोग मुझे सहयोग दो।"
कथा कहती है कि यशकुमार के दृढ़ निश्चय, बुद्ध के शुभ संकल्प और सत्संग का प्रभाव उसके माता-पिता तथा भगिनी पर भी पड़ा। वे भी बुद्ध के शिष्य बन गये।
किसी के चित्त में थोड़ा-सा भी विवेक-वैराग्य आ जाय और बोधवान महापुरुष का सान्निध्य मिल जाय तो गिराने वाले चाहे कितने भी आ जाय फिर भी सँभालनेवाले अकेले महापुरुष सँभाल लेते हैं। बुद्ध पुरुष के पक्के शिष्य को हजार गिराने वाले लोग भी गिरा नहीं सकते। जबकि सत् शिष्य हजारों का हाथ पकड़कर उन्हें उबार सकता है। यह दैवी गुणों का प्रभाव है।
जिसके चित्त में शुद्धि है उसकी बाहर भी शुद्धि स्वाभाविक रहने लगती है। जिसकी बाह्य शुद्धि होती है उसको आन्तर शुद्धि में सहायता मिलती है। दैवी सम्पदावाले पुरुष में शारीरिक शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि स्वाभाविक फुरने लगती है।
फिर आता है अद्रोह।
द्रोह से अपना चित्त जलता रहता है। कभी-कभी रजो, तमोगुण के प्रभाव से चित्त में द्रोह आ जाता है। जिनके जीवन में सत्त्वगुण है उनमें द्रोह नहीं होता।
दैवी सम्पदा का आखिरी गुण है नातिमानिता।
अतिमानिता का अर्थ है अपने को श्रेष्ठ मानना। "मैं अति श्रेष्ठ हूँ..... इन्होंने मुझे मान दिया लेकिन कम दिया....' इस प्रकार की अति मान की वासना है वह अहंकार की शूल भोंकती है। आदमी व्यर्थ में बोझिला जीवन जीता है। जिसके जीवन में अति मान का शूल नहीं है वह कई मुसीबतों से अशांति पैदा करने वाले व्यवहार से, दुःखद परिस्थितियों के प्रादुर्भाव से सहज ही बच जाता है।
अति मान चाहने वाला व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी बात में दोष-दर्शन करके अपना चित्त चलित करता रहता है। ऐसा आदमी न जाने कितनी ही वृथा मुसीबतें मोल लेकर अपने आपको कोसता रहता है। जो अति मान की वासना छोड़ देता है उसका जीवन सरल हो जाता है, सहज में सुखद बन जाता है।
लोग थोड़ा-सा अच्छा काम करके फिर चाहते हैं कि हमारा सम्मान समारोह हो जाय। समारोह में जब सम्मान दिया जाता है तब सिकुड़कर निरभिमान होने की चेष्टा करते हुए बोलता तो है कि, "इसमें मेरा कुछ नहीं है.... सब भगवान की कृपा है.... मैं तो निमित्त मात्र हूँ...'' आदि आदि। लेकिन ऐसा बोलकर भी अपने को अच्छा कहलाने की वासना है।
अच्छा कहलाने का जो भीतर भूत बैठा है वह आदमी से बहुत कुछ बुरा करवा लेता है। अच्छा काम तो करे लेकिन अच्छा कहलाने का, अति मान चाहने का जो दोष है उससे दैवी सम्पदा के लोग स्वाभाविक ही बचते हैं। राजसी सम्पदा के लोग उपदेश से बचते हैं और तामसी लोग उस दोष के शिकार हो जाते हैं।
देवों और दानवों का युद्ध होता ही रहता था।
एक बार दानव लोग गये ब्रह्माजी के पास गया और पूछाः
"ब्रह्मन् ! यह क्या बात है कि भगवान जब-जब अवतार लेते हैं तब-तब देवों का ही पक्ष लेते हैं? हम लोगों के पास इतना बल होने के बावजूद भी हम अशांत और दुःखी रहते हैं। देवता बड़े शांत, सुखी रहते हैं और पूजे जाते हैं। हमको कोई पूछता नहीं है। क्या कारण है?"
ब्रह्माजी ने देखा कि ये उपदेश के अधिकारी नहीं है। इनको तो 'प्रेक्टीकल ऑपरेशन्' की जरूरत है। उन्होंने दानवों से कहाः "देवों और दानवों का भोज-समारोह रखेंगे, उसमें तुमको प्रयोगात्मक उपदेश दूँगा।"
ब्रह्माजी के वहाँ भोज समारोह रखा गया। दानव भीतर ही भीतर सोचने लगे कि, 'ब्रह्माजी तो देवों को पहले खिलाएँगे, बढ़िया-बढ़िया खिलायेंगे, हमको तो बाद में देंगे कुछ छोटा-मोटा पदार्थ।' कब खिलाएँगे, क्या खिलाएँगे, कैस खिलाएँगे इसकी चिन्ता में, संशय में दानवों का चित्त उलझने लगा। देवों के चित्त में शांति थी। 'ब्रह्मदेव ने भोजन के लिए बुलाया है, पितामह जो कुछ करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे।' वे बड़े शांत थे।
ब्रह्माजी ने घोषणा की कि पहले दानवों को भोजन कराया जायगा और बाद में देवों को। दोनों के लिए एक समान ही भोज्य-पदार्थ, पकवान-व्यंजन आदि होंगे। दैत्यों को लगा कि वाह ! पितामह तो पितामह ही हैं, बड़े कृपालु हैं।
पहले दानवों की पंगत लगी। आमने सामने सब दानवों को पंक्तियाँ लगाकर बिठाया गया। पत्तल में बढ़िया-बढ़िया भोजन परोसा गया। किस्म-किस्म के मिष्ठान्न और नमकीन पदार्थ, कई प्रकार की सब्जी और आचार, विभिन्न व्यंजन और पकवान। मधुर खुशबू उठ रही है।
ज्यों ही दानवों ने भोजन शुरु किया कि तुरन्त ब्रह्माजी के संकल्प से सभी दानवों के हाथ की कोहनियों ने मुड़ने से इन्कार कर दिया। पत्तल से ग्रास उठायें तो सही लेकिन हाथ को मोड़े बिना मुँह में डालें कैसे? हाथ को सिर से ऊपर उठाकर मुँह को ऊँचा करके उसमें डालें तो आधा ग्रास मुँह में बाकी का आँख में पड़े, इधर पड़े उधर पड़े। बड़ी मुश्किल से थोड़ा खाया थोड़ा गिराया। आँखें जलने लगीं, नाक में कुछ कण जाने से छींक आने लगी। हाथ-पैर-पेट-कपड़े सब जूठे हो गये। भोजन तो बढ़िया था, चटपटा था, मसालेदार था, नमकीन था, मधुर था, सुन्दर था, सब किस्म का था लेकिन ब्रह्माजी के संकल्प के प्रभाव से हाथ कोहनी से न मुड़ने से सब गुड़ गोबर हो गया।
दानव आखिर अतृप्त होकर उठ गये।
अब देवों की बारी आयी। उनको भी वही भोजन परोसा गया। उनके लिए भी ब्रह्माजी का वही संकल्प था। उनकी कोहनियों ने भी मुड़ने से इन्कार कर दिया। लेकिन देवों के पास सत्त्वगुण था। उनके चित्त में झट से सुझाव आया कि हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं तो कोई बात नहीं, ग्रास सामने वाले के मुँह में डाल दो। सामनेवाले ने भी इसके मुँह में डाल दिया। आमने-सामने वाले लोगों ने एक दूसरों को खिलाकर तृप्त कर दिया। दानव तो देखते ही रह गये। अब वे सोचने लगे कि हम भी ऐसा करते तो ? ऐसा करते तो सही लेकिन तुम असुरों के पास ऐसी दैवी अक्ल कहाँ से आवे?
अक्ल तो सब जगह चाहिए, ब्रह्मलोक में भी अक्ल चाहिए तो मृत्युलोक में भी अक्ल चाहिए, आश्रम में बैठने की भी अक्ल चाहिए। घर में उठने बैठने की भी अक्ल चाहिए, खाने और बोलने की भी अक्ल चाहिए। अक्ल कमाने की भी अक्ल चाहिए। इससे भी ज्यादा अक्ल मोक्ष पाने के लिए चाहिए और वह आती है दैवी गुणों से। व्यक्ति में जितने-जितने दैवी गुण स्थित होते हैं उतनी-उतनी अक्ल विकसित होती है।
दैवी सम्पदा वाले पुरुष से और लोग बड़े सन्तुष्ट रहते हैं। जिसमें दैवी सम्पदा आती है उसका चित्त देव के समीप रहता है। देव माने आत्मदेव। आत्मा सबको प्यारा है। इसीलिए आत्मज्ञानी सबको प्यारा होता है। नारदजी आत्मवेत्ता थे। उनके वचन देवता भी मानते थे और दैत्य भी मानते थे। उनके वचन मनुष्य तो मानते ही थे।
लोग अपेक्षा रखते हैं कि हम चाहे जैसा बर्ताव करें लेकिन दूसरे लोग हमें मान दें। ऐसा नहीं हो सकता। जिसके जीवन में अतिमान का दोष होता है वह अपने सुधरने की या अपमान की बात नहीं सुन सकता। कोई सुनाये तो सफाई दे देगाः मैं तो बड़ा निर्दोष हूँ। मुझमें तो केवल गुण ही गुण हैं। अवगुण का नामोनिशां नहीं है।
जो गलती करता है और अपनी गलती ढूँढता नहीं यह तो गलती है लेकिन कोई उसकी गलती बताता है फिर भी स्वीकार नहीं करता वह ज्यादा गलती करता है। कोई अपनी गलती सुनाए तो सुनानेवाले को आदर से प्रणाम करना चाहिए।
उत्तम मनुष्य अपनी गलतियाँ ढूँढने में लगे रहते हैं, परहित में लगे रहते हैं, ध्यान-भजन में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं परमात्म-मस्ती में, हरिरस पीने और पिलाने में।
जीव अगर सजातीय प्रवृत्ति नहीं करेगा तो विजातीय प्रवृत्ति होगी, सत्कर्म नहीं करेगा तो दुष्कर्म होगा। ईश्वर के रास्ते नहीं चलेगा तो शैतान के रास्ते चलेगा।
अपनी कोई गलती दिखाये तो उसका धन्यवाद दो, आदर सहित उसका सत्कार करो ताकि हमारे चित्त में उसके लिए नफरत न रहे और गलती दिखाने में उसको संकोच न हो।
मीरा को सुधारने का जिसने ठेका ले रखा था उस उदा ने मीरा को समझाया-बुझाया, डाँटा। मीरा उसे प्रणाम करती है :
"ननद जी ! आप जो कहती हैं वह सब ठीक है लेकिन मेरी आदत पड़ गई है गिरधर गोपाल के गीत गाने की। मैं क्या करूँ?"
मीरा जानती थी कि यह गलती नहीं है, वे लोग ही गलत हैं फिर भी मीरा के चित्त में अति मान का दोष नहीं था। अपमान करने वालों को भी मीरा ने मान दे दिया, भक्ति नहीं छोड़ी।
एक बार रात्रि में उदा को लगा कि मीरा किसी परपुरुष से बात कर रही है। उदा भागती-भागती अपने भाई रतनसिंह के पास आयी। कान का कच्चा, अक्ल का कच्चा, मूर्ख रतनसिंह तलवार लेकर भागा।
'अब मीरा महल में जी नहीं सकती। महल में परपुरुष के साथ बात !'
रतनसिंह ने मीरा को बहुत पीड़ा दी थी। उसके बाद राणा विक्रम आया उसने भी मीरा को त्रास देने में कोई कसर नहीं रखी थी। मीरा में देखो, कितनी सहनशक्ति थी ! भक्ति में कितनी दृढ़ता थी !
लोग पूजवाना तो चाहते हैं लेकिन पूजवाने से पहले जो बलिदान देना पड़ता है उससे दूर भागते हैं। महान् बनना चाहते हैं, पूजवाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सदा सुखी होना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं और जरा-से मान से, अपमान से, मुसीबत से, दुःख से, संघर्ष से, विघ्न से, बाधा से पूँछ दबाकर भागते फिरते हैं।
उदा मीरा पर न जाने कितने-कितने लांछन लगाती थी लेकिन मीरा कभी शिकायत नहीं करती। रतनसिंह ने मीरा को गलत समझकर कई बार कुछ का कुछ सुनाया होगा लेकिन मीरा के चित्त में वही हरिरस की मधुरता बनी रही।
उदा की बात सुनकर रतनसिंह मध्यरात्रि को तलवार लेकर मीरा के आवास में घुस गया। आवेश में घुस तो गया लेकिन देखा तो मीरा बैठी है अपने शांत भाव में। मीरा के मुख मण्डल पर दिव्य आभा जगमगा रही है और वह बोले जा रही है किः
"प्रभु ! मैं जैसी हूँ, तुम्हारी हूँ। तुम हमारे हो। यह संसार देखने भर को है। यहाँ के सब सगे-सम्बन्धी कहने मात्र के हैं। तुम ही प्राणीमात्र के सच्चे सगे-सम्बन्धी हो।"
फिर मीरा के हृदय से पुरुष की आवाज में श्रीकृष्ण बोलेः
"तू चिन्ता मत कर। इस संसार में आसक्ति न हो इसलिए दुःख, दर्द और पीड़ा मेरे भक्तों को देता हूँ ताकि वे कहीं संसार में चिपक न जाएँ, कहीं फँस न जाएँ। उन्हें मुसीबतों के बीच रखकर परिपक्व करता हूँ।"
रतनसिंह चकित हो गया कि मीरा ही बोलती है और मीरा ही सुनती है। कोई परपुरुष वहीं नहीं है। मीरा के शीतल दैवी तेज में रतनसिंह का रूख बदल गया। उसकी आँखों से पश्चाताप के आँसू बहे। वह मीरा से बड़ा प्रभावित हुआ।
बाहर उदा इन्तजार कर रही थी कि अब कुछ घटना घटेगी लेकिन वह देखती रह गयी कि तलवार के प्रहार से मीरा की चीख निकलनी चाहिए, भय से मीरा का आर्तनाद निकलना चाहिए जबकि वहाँ तो सन्नाटा है ! रतनसिंह खुली तलवार के साथ मीरा के पास गया है, क्या पता क्या कर रहा है?
इतने में रतनसिंह बाहर आया। आँखों में आँसू हैं, मुख पर कोमल भाव उभर आया है, हृदय में पश्चाताप है। तलवार नीचे पटक दी और मीरा के प्रति अहोभाव के वचन बोलने लगाः
"मीरा को हम पहचानते नहीं। वहाँ कोई परपुरुष नहीं था। वह तो भगवान से वार्तालाप कर रही थी....।"
उदा उबल पड़ीः "क्या जादू मार दिया उस रांड ने तेरे पर?"
एक स्त्री दूसरी स्त्री से स्वाभाविक ही ईर्ष्या करती है। चार स्त्रियाँ इकट्ठी होगी तो सारे गाँव की निन्दा-कूथली में लग जाएगी।
बड़बड़ाते हुए उदा कमरे में गई तो मीरा का वही स्थान... वही सात्त्विक दिव्य शांत तेज.... उदा देखकर दंग रह गई। मीरा के मुखमण्डल की शांत प्रसन्न आभा.... आँखों से अश्रूपात... वह अश्रूपात सुख का भी नहीं था दुःख का भी नहीं था। वह था भक्ति के रस का। एकटक मीरा को निहारते-निहारते उदा की आँख पवित्र हो गई। पवित्र आँख दिल को भी पवित्र कर देती है।
ज्ञानेन्द्रियों में दो इन्द्रियाँ बड़ी सूक्ष्म और संवेदनशील हैं। चित्त पर उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। एक है नेत्र और दूसरी है जिह्वा। जिसकी जिह्वा और आँख नियन्त्रित है वह जल्दी उन्नत हो सकता है। दर्शन और वचन के द्वारा आदमी जल्दी उन्नत होता है।
मीरा जो बोले जा रही थी वे वचन उदा के कान में पड़ते थे। मीरा को सुनते-सुनते और देखते-देखते उदा का चित्त ऊर्ध्वगामी होने लगा। जो रतनसिंह ने कहा वही उदा ने भी कहाः
"मीरा ! सचमुच हम लोग तुझे नहीं जानते। हमने तुमको इतना-इतना सताया लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। आज भी मैंने अपने भाई को बहकाकर भेजा कि तू किसी परपुरुष से बात कर रही है लेकिन तू तो पुरुषोत्तम से बात कर रही थी। यह मुझे पता नहीं था। तेरे पास मैं क्षमायाचना करूँ इतनी मुझमें योग्यता नहीं है लेकिन तेरी उदारता देखकर यह पापी उदा तेरे पैर पकड़ती है....।"
मीरा के चरणों में ननद उदा लिपट रही है। मीरा ने यह नहीं कहा कि, 'चल चल रांड ! तूने मुझको इतना सताया.... भगवान तेरा सत्यानाश करे।' नहीं नहीं। मीरा ने उदा को दोनों हाथों से उठाकर गले लगा लिया।
"कोई बात नहीं बहन जी ! अगर तुम इतना नहीं करती तो शायद मैं कहीं संसार में भटक जाती। भगवान के प्यारों पर तो कष्ट आने ही चाहिए। कष्टमय और मुसीबत वाले संसार से सदा के लिए निकलने के लिए भगवान के प्यारों पर कष्ट और मुसीबत आनी ही चाहिए। मुझे मुसीबत देने में तुमने भी कितनी मुसीबत सही ! तुमने अपना चित्त कितना मलिन किया ! इसलिए हे उदा ! तुम मुझे माफ करो। मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हारे अंतःकरण को मलिन होना पड़ा। मेरी साधना बढ़ाने के लिए तुम्हें मेरा विरोध करना पड़ा।"
"अरे भाभी ! तुम्हारी साधना बढ़ाने के लिए नहीं, साधना मिटाने के लिए सब किया, मुझे क्षमा करो।" उदा रो पड़ी।
मीरा बोलीः "नहीं, मिटाने का भाव से भी उस प्यारे ने तो मेरी भक्ति बढ़ा दी। तुम्हारा इसमें उपयोग हुआ।"
उदा कहती है 'तुम मुझे क्षमा करो' और मीरा कहती है 'तुम मुझे माफ करो।' दैवी सम्पदा में कितना तेज है ! कितनी समझ है ! कितना स्नेह है ! कितनी उदारता है !
अलौकिक, दिव्य, सात्त्विक, शांत तेज के आगे आसुरी तेजवाला विरोधी भी रूपांतरित हो जाता है।
जीवन में कुछ इकट्ठा करना हो तो दैवी सम्पदा को इकट्ठा करो, आत्मज्ञान के विचारों को इकट्ठा करो, मोक्ष के विचारों को इकट्ठा करो।
नारायण.... नारायण.... नारायण..... नारायण..... नारायण......।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जीवन-विकास
और
प्राणोपासना
मनुष्य के जीवन में विकास का क्रम होता है। विकास उसको बोलते हैं जो स्वतन्त्रता दे। विनाश उसको बोलते हैं जो पराधीनता की ओर ले जाय।
'स्व' के तंत्र होना विकास है। 'स्व' आत्मा है, परमात्मा है। अपने परमात्म-स्वभाव में आना, टिकना, आत्म-साक्षात्कार के मार्ग पर चलना यह विकास है और इस मार्ग से दूर रहना यह विनाश है।
विकास में तीन सोपान हैं। एक होता है कर्म का सोपान। अंतःकरण अशुद्ध होता है, मलिन होता है तो आदमी पापकर्म की ओर जाता है, भोग, आलस्य, तंद्रा आदि की ओर जाता है। ऐसे लोग तमोगुण प्रधान होने से मृत्यु के बाद वृक्ष, भूंड, शूकर, कूकर आदि अधम योनियों में जाते हैं.... विनाश की ओर जाते हैं।
रजोगुण की प्रधानता हो तो चित्त में विक्षेप होता है। विक्षेप से आदमी छोटी-छोटी बातों में दुःखी हो जाता है।
दुनियावाले
ने दुनिया ऐसी
बनायी है।
हजारों
खुशियाँ होते
हुए आख्रिर
रूलाई है।।
कितनी भी खुशियाँ भोगो लेकिन आखिर क्या? खुशी मन को होती है। जब तक तन और मन से पार नहीं गये तब तक खुशी और गम पीछा नहीं छोड़ेंगे।
अंतःकरण की मलिनता मिटाने के लिए निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है। उपासना से चित्त का विक्षेप दूर होता है। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। फिर आदमी विकास की पराकाष्ठा पर पहुँचता है।
हमारा शरीर जब भारी होता है तब वात और कफ का प्रभाव होता है। हम जब उपासना आदि करते हैं तब शरीर में भारीपन कम होने लगता है। आलस्य, प्रमाद, विक्षेप आदि कम होने लगते हैं।
पित्त की प्रधानता से तन में स्फूर्ति आती है। मन, प्राण और शरीर इन तीनों की आपस में एकतानता है। प्राण चंचल होता है तो मन चंचल बनता है। मन चंचल होता है तो तन भी चंचल रहता है। तन चंचल बनने से मन और प्राण भी चंचल हो जाते हैं। इन तीनों में से एक भी गड़बड़ होती है तो तीनों में गड़बड़ हो जाती है।
बच्चे के प्राण 'रिधम' से चलते हैं। उसमें कोई आकांक्षा, वासना, कोई प्रोब्लेम, कोई टेन्शन नहीं है। इसलिए बच्चा खुशहाल रहता है। जब बड़ा होता है, इच्छा वासना पनपती है तो अशांत-सा हो जाता है।
अब हमें करना क्या है? प्राणायाम आदि से अथवा प्राण को निहारने के अभ्यास आदि साधनों से अपने शरीर में विद्युत तत्त्व बढ़ाना है ताकि शरीर निरोग रहे। प्राणों को तालबद्ध करने से मन एकाग्र बनता है। एकाग्र मन समाधि का प्रसाद पाता है। पुराने जमाने में अस्सी अस्सी हजार वर्ष तक समाधि में रहने वाले लोग थे ऐसा बयान शास्त्रों में पाया जाता है। लेकिन 80 हजार वर्ष कोई नींद में नहीं सो सकता। बहुत-बहुत तो कुंभकर्ण जैसा कोई पामर हो, तपश्चर्या करके नींद का वरदान ले तो भी छः महीना ही सो सकता है। अस्सी हजार साल तो क्या 80 साल तक भी कोई सो नहीं सकता।
नींद तमोगुण है। समाधि सत्त्वगुण की प्रधानता है।
सरोवर के ऊपरी सतह पर कोई बिना हाथ पैर हिलाये ठीक अवस्था में लेट जाय तो घण्टों भर तैर सकता है। लेकिन पानी के तले घण्टों भर रहना आसान नहीं है। अर्थात् नीचे रहना आसान नहीं है और ऊपर रहना सहज है। समाधि में और सुख में आदमी वर्षों भर रह सकता है। लेकिन विक्षेप और दुःख में आदमी घड़ी भर भी रहना चाहता नहीं। अतः मानना पड़ेगा कि दुःख, मुसीबत और विक्षेप तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है।
मुँह में दाँत होना स्वाभाविक है। लेकिन रोटी सब्जी खाते-खाते कोई तिनका दाँतों में फँस जाता है तो बार बार जिह्वा वहाँ जाती है। जब तक वह निकल नहीं जाता तब तक वह चैन नहीं लेती क्योंकि तिनका मुँह में रहना स्वाभाविक नहीं है। उसको निकालने के लिए लकड़ी की, प्लास्टिक की, पित्तल की, ताँबे की, चाँदी की, न जाने कितनी कितनी सलाइयाँ बनाई जाती हैं। मुँह में इतने पत्थर (दाँत) पड़े हैं उसकी कोई शिकायत नहीं होती जबकि एक छोटा सा तिनका भी असह्य बन जाता है। ....तो मुँह में दाँत होना स्वाभाविक है जबकि तिनका आदि होना अस्वाभाविक है।
ऐसे ही सुख हमारा स्वभाव है। विक्षेप और दुःख हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए कोई दुःख नहीं चाहता, कोई विक्षेप नहीं चाहता। फिर भी दुनियावाले ने दुनिया ऐसी बनायी है कि तुम्हें दुःख और विक्षेप निकालने का तरीका मिल जाय और तुम स्वतंत्र हो जाओ। 'स्व' के 'तंत्र'। 'स्व' केवल एक आत्मा है।
अस्सी हजार वर्ष की समाधि लग सकती है लेकिन नींद उतनी नहीं आ सकती। मन और प्राण को थोड़ा नियंत्रित करें तो हम समाधि के जगत में प्रवेश कर सकते हैं।
जिन लोगों को विचार समाधि प्राप्त हुई है, ज्ञानमार्ग में प्रवेश मिला है उन लोगों का मन सहज में आत्मविचार में रहता है तो जो आनन्द मिलता है, प्रसन्नता मिलती है उससे नींद की मात्रा थोड़ी कम हो जाय तो उनको परवाह नहीं होती। डेढ़ दो घण्टा भी सो लें तो शरीर के आराम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। समाधि का, ध्यान का, आत्मविचार का जो सुख है वह नींद की कमी पूरी कर देता है। कोई अगर आठ घण्टे समाधि में बैठने का अभ्यास कर ले तो वह सोलह घण्टे जाग्रत रह सकता है। उसको नींद की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम जो खाते पीते हैं वह कौन खाता पीता है? गलती से हम मान लेते हैं कि हम खाते पीते हैं। जुड़ गये प्राण से, मन से, शरीर से। वास्तव में भूख और प्यास प्राणों को लगती है। सुख-दुःख मन को होता है। राग-द्वेष बुद्धि को होता है। प्राण, मन, बुद्धि शरीर आदि सब साधन हैं। हमें ज्ञान नहीं है इसलिए साधन को ‘मैं’ मानते हैं और अपने साध्य तत्त्व से पिछड़े रहते हैं।
बिछड़े
हैं जो प्यार
से दर-ब-दर
भटकते फिरते हैं।
कभी किसी की कूख में तो कभी किसी की कूख में। कभी किसी पिता की इन्द्रिय से पटके जाते हैं तो कभी किसी माता से गर्भ में लटक जाते हैं। वह माता चाहे चार पैरवाली, पाँच पच्चीस पैर वाली हो, सौ पैर वाली हो या दो पैर वाली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर योनि में मुसीबत तो सहनी ही पड़ती है।
तन
धरिया कोई न
सुखिया देखा।
जो
देखा सो
दुखिया रे....।।
इस प्रकार विचार करके जो साधक अपना सहज स्वातंत्र्य पाना चाहते हैं, 'स्व' के तंत्र होना चाहते हैं उन लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग सर्वस्व है।
हमारा प्राण नियंत्रित होगा तो शरीर में विद्युतशक्ति बनी रहेगी। शरीर निरोग रहेगा, मन एकाग्र बनेगा, बुद्धि का विकास होगा। अगर मन को एकाग्र करोगे तो प्राण नियंत्रित रहेंगे।
समाधि में आंतरिक सुख से मन का समाधान हो जाय तो बाहर के सुख की याचना नहीं रहती। आकर्षण भी नहीं रहता। दुःख तभी होता है जब बाहर के सुख की आंकाक्षा होती है। जिसको आंकाक्षा नही होती उसको उन चीजों के न मिलने पर दुःख नहीं होता और मिलने पर कोई बन्धन नहीं होता। दुःख का मूल है वासना और वासना होती है सुख पाने के लिए। वास्तव में सुख हमारा स्वभाव है। दुःख हमारा स्वभाव नहीं है। मुँह में दाँत रहना स्वभाव है, तिनका रहना स्वभाव नहीं है। सरोवर की सतह पर घण्टों भर तैरना संभव है लेकिन सरोवर के तले में दीर्घकाल तक रहना सहज संभव नहीं है। ऐसे ही दुःख नीचाई है। हम कभी उसे पसन्द नहीं करते लेकिन वासना के कारण गिरते हैं, दुःख पाते हैं।
अब हमें क्या करना चाहिए? प्राणों को, मन को और शरीर को एकतान रखना चाहिए।
जब तुम जप करो तब कोई एक आसन पसन्द कर लो सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि। किसी एक आसन में बैठकर ही जप करो। जितना हो सके, जप करते समय इधर उधर झाँके नहीं। दृष्टि नासाग्र रखें, श्वास पर रखें या गुरु गोविन्द के चित्र पर रखें। तन एकाग्र होगा तो मन भी एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो स्थूल प्राण को सूक्ष्म करने के लिए कुण्डलिनी शक्ति जागृत होगी। फिर शरीर रिधम से हिलेगा। शरीर में कहीं वात-पित्त-कफ के दोष होंगे तो उन्हें शुद्ध करने के लिए भीतर से धक्का लगेगा प्राणों को तो अपने आप यथा योग्य आसन होने लगेंगे, तेजी से प्राणायाम होने लगेगा। प्रारम्भ में प्रतिदिन आठ-दस प्राणायाम करने का नियम तो ले लें किन्तु जब प्राणोत्थान होगा तो प्राणायाम और विभिन्न आसन अपने आप होने लगेंगे। समर्थ सदगुरु जब संप्रेक्षण शक्ति से मंत्रदीक्षा देते हैं तब साथ ही साथ, संकल्प के द्वारा साधक के चित्त में बीज बो देते हैं। साधक अहोभाव से साधन-भजन में लगा रहता है तो वह बीज शीघ्र ही पनप उठता है। साधक तीव्र गति से साधना में आगे बढ़ने लगता है। महामाया कुण्डलिनी शक्ति उसकी साधना की डोर सँभाल लेती है।
प्रारंभ में इस बात का पता नहीं चलता कि कितना बढ़िया बीज हमारे चित्त में बोया गया है। जैसे, किसान खेत में बोआई करता है तब देखनेवाला जान नहीं सकता कि जमीन में बीज पड़े हैं कि नहीं। लेकिन किसान जानता है। जब खेत की सिंचाई होती है और बीज अंकुरित होकर पनप उठते हैं, छोटी-छोटी पत्तियाँ निकल आती हैं, सारा खेत लहलहा उठता है तब राहदाही भी जान सकते हैं कि किसान ने बीज बोये थे।
ऐसे ही मंत्रदीक्षा के समय साधक को जो मिलता है वह सबको ज्ञान नहीं होता। जब साधक साधना में लगा रहता है तो समय पाकर वह बीज कहो, गुरुदेव का संकल्प कहो, आशीर्वाद कहो, शक्तिपात कहो, चाहे जो कुछ कहो, वह पनपता है।
माँ के उदर में जब गर्भाधान होता है, बच्चा आ जाता है उस समय नहीं दिखता। कुछ महीने के बाद माँ को महसूस होता है और उसके बाद दूर के लोगों को भी महसूस होता है कि यह महिला माँ होने वाली है।
साधक को जब दीक्षा मिलती है तब उसका नवजन्म होता है।
दीक्षा का मतलब इस प्रकार हैः दी = दीयते, जो दिया जाय। क्षा = जो पचाया जाय।
देने योग्य तो सचमुच केवल आध्यात्मिक प्रसाद है। बाकी की कोई भी चीज दी जाय, वह कब तक रहेगी?
जो ईश्वरीय प्रसाद देने की योग्यता रखते हैं वे गुरु हैं। जो पचाने की योग्यता रखता है वह साधक है, शिष्य है। देने वाले का अनुग्रह और पचाने वाले की श्रद्धा, इन दोनों का जब मेल होता है तब 'दीक्षा' की घटना घटती है।
दीक्षा तीन प्रकार की होती हैः शांभवी दीक्षा, जो निगाहों से दी जाती है। स्पर्श दीक्षा, जैसे शुकदेवजी ने परीक्षित के सिर पर हाथ रखकर दी थी। तीसरी है मांत्रिक दीक्षा। गुरु-गोविन्द का, भगवान का कोई नाम दे देना।
मांत्रिक दीक्षा में मंत्र देने वाले का चित्त जैसी ऊँचाई पर होता है वैसा उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। कोई भाड़भूँजा तुम्हें कह दे कि 'राम राम जपो, कल्याण हो जायगा....' तो इतना गहरा कल्याण नहीं होगा जितना कोई ब्रह्मवेत्ता सत्पुरुष राम मंत्र दें और कल्याण हो जाय। रामानंद स्वामी ने ऐसे ही 'राम.... राम' उच्चारण किया और कबीर जी ने गहरी श्रद्धा से पकड़ लिया कि गुरुदेव के श्रीमुख से मंत्र मिल गया है, तो कबीर जी उस मंत्र से सिद्ध हो गये। मंत्र तो वही है लेकिन मंत्र देने वाले की महिमा है। कोई चपरासी कुछ कह दे तो उसकी अपनी कीमत है और प्रधान मंत्री वही बात कह दे तो प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा।
आध्यात्मिकता में जो उन्नत हैं उनके द्वारा मंत्र मिलता है और सामने वाला श्रद्धा से साधना करता है तो मंत्र उसको तार देता है। मंत्र का अर्थ ही हैः मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसका मनन करने से जो त्राण करे, रक्षा करे वह है मंत्र। अंतर में मनन करने से मंत्र मन को तार देता है।
मांत्रिक दीक्षा में जितने शब्द कम होते हैं और मंत्रोच्चारण जितना तालबद्ध होता है उतनी साधक को सुविधा रहती है, वह जल्दी से आगे बढ़ता है।
मांत्रिक दीक्षा में अगर कोई संप्रदाय चलाना है, कोई मजहब पकड़ रखना है तो उसमें ख्याल रखा जायगा कि मंत्र दूसरों से कुछ विलक्षण हो। ऐसे मजहब-संप्रदायों में साधक की उन्नति मुख्य नहीं है, संप्रदाय का गठन मुख्य है। संप्रदाय का गठन करने वाले जो भी संप्रदाय के आचार्य हैं उनको उनका कार्य मुबारक हो। नारदजी ऐसे सांप्रदायिक संत नहीं थे। नारदजी के लिए सामने वाले की उन्नति मुख्य थी। सामने वाले के जीवन की उन्नति जिनकी दृष्टि में मुख्य होती है वे लोक संत होते हैं। नारद जी ने वालिया लुटेरा को मंत्र दिया 'रा....म'। 'रा' लम्बा और 'म' छोटा। वालिया मूलाधार केन्द्र, स्वाधिष्ठान केन्द्र में जीने वाला आदमी है। उन केन्द्रों में इस मंत्र के आन्दोलन पड़ेंगे तो धीरे-धीरे वह अनाहत केन्द्र में, हृदय केन्द्र में पहुँचेगा ऐसा समझकर नारदजी ने मांत्रिक दीक्षा देते समय शांभवी दीक्षा का भी दान कर दिया, निगाहों से उसके अंतर में अपने किरण डाल दिये। वालिया लुटेरा लग गया मंत्र जाप में। 'मरा... मरा.... मरा...मरा...' तालबद्ध मंत्र जपते-जपते उसकी सुषुप्त कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत हुई और वालिया लुटेरा आगे जाकर वाल्मीकि ऋषि बन गया।
मंत्रदीक्षा देने वाले महापुरुष और लेने वाला साधक दोनों बढ़िया होते हैं तो साधना और सिद्धि भी बढ़िया हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मंत्रदीक्षा लेने वाले की अत्यंत श्रद्धा है, साधना में अत्यंत लगन है, नियमबद्ध अभ्यास है तो देने वाला कोई साधारण व्यक्ति भी हो फिर भी लेने वाला आगे निकल सकता है। अधिक लाभ तो तब होता है जब देने वाला भी खूब ऊँचे हों और लेने वाला भी अडिग हो। ऐसे मौके पर कार्य अधिक सुन्दर और सुहावना होता है।
साधक अगर आसन, प्राणायाम आदि नियम से करता रहे तो उसका तन निरोगी रहेगा, प्राण थोड़े नियंत्रित रहेंगे। प्राणायाम करने से प्राणों में तालबद्धता आती है। हमारे प्राण तालबद्ध नहीं हैं इसलिए छोटी-छोटी बातों में हमारा मन चंचल हो जाता है। साधारण लोग और योगियों में इसी बात का फर्क है। योगी बड़ी-बड़ी आपत्तियों में इतने विक्षिप्त नहीं होते क्योंकि उन्होंने प्राणायाम आदि करके मन और प्राण को तालबद्ध किया हुआ होता है। उनमें सब पचा लेने की शक्ति होती है।
पहले समय में लकड़े के पुल होते थे। सेना की कोई बटालियन जब कूच करती है तब एक... दो.... एक..... दो, इस प्रकार तालबद्ध कदम मिलाकर चलती है। उस समय में जब लकड़े के पुल पर से सेना गुजरती तब केप्टन सेना को आज्ञा देता कि ताल तोड़ो। तालबद्ध कदम पड़ने से ताकत पैदा होती है और उससे लकड़े का पुल टूट सकता है।
तालबद्धता में शक्ति है। कोई बिना ताल के गीत गाये तो मजा नहीं आएगा। साधनों के साथ स्वर मिलाकर गाया जाय तो पूरी सभा डोलायमान हो सकती है। संगीत के साधन सबके स्वर मिलाने में सहयोग देते हैं।
तालबद्धता में एक प्रकार का सुख और सामर्थ्य छुपा है। हमारे प्राण अगर तालबद्ध चलने लग जायें तो सूक्ष्म बनेंगे। श्वास तालबद्ध होगा तो दोष अपने आप दूर हो जायँगे। श्वास सूक्ष्म और तालबद्ध नहीं है इसलिए काम सताता है। श्वास तालबद्ध नहीं है इसलिए क्रोध प्रभाव डाल देता है। रोग, शोक, मोह आदि सब प्राणों की तालबद्धता के अभाव में होते हैं। प्रतिदिन अगर थोड़ा समय भी श्वास या प्राणों की तालबद्धता के लिए निकालें तो बहुत-बहुत लाभ होगा।
मानो, हमें क्रोध आ रहा है। उस समय जाँचो तो पता चलेगा कि श्वास का ताल विशेष विकृत होगा। उस समय क्या करना चाहिए? अपने श्वास को देखो, सावधान होकर निहारो प्राण की गति को। क्रोध पर नियंत्रण आ जाएगा।
हम कभी चिन्ता में हैं। चित्त में कुछ बोझा है। तो क्या करें? शुद्ध हवा में मुँह के द्वारा लम्बे-लम्बे श्वास लो। नथुनों से बाहर निकालो। फिर मुँह से लम्बे श्वास लो और नथुनों से निकालो। इस प्रकार दस बारह बार करो। तुम्हारी उदासी में, चिन्ता में जरूर परिवर्तन आ जायगा।
मान लो, किसी के चित्त में कोई पुरानी गन्दी आदत है। कई युवकों को हस्तमैथुन की आदत होती है। पाप की पराकाष्ठा है वह। ऐसी आदतवाले युवक को अगर बदलना है तो उसको प्राणायाम सिखाया जाय।
हस्तमैथुन जैसी भद्दी आदतवाला युवक रात को सोता है और सुबह को जब उठता है तब उसका चेहरा देखकर पता चलता है कि वह रात को अपनी ऊर्जा का सत्यानाश करता है। मनुष्य भीतर दुःखी होता है तो और दुःख का सामान इकट्ठा करता है। सत्संग नहीं मिलता है, साधन-भजन नियमित नहीं होता है, भीतर का थोड़ा-बहुत रस नहीं आता। तब आदमी कामचेष्टा या और पाप कर्म करता है।
ऐसे लोगों को भी मोड़ना है, आगे बढ़ाना है तो उन्हें प्राणायाण सिखाया जाय। उनके प्राणों में थोड़ी सूक्ष्मता लायी जाय। वे बदल जाएँगे। उनके जीवन में मानो जादू हो जाएगा।
इन्द्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। योगियों का कहना है कि अगर प्राण का पूरा प्रभुत्व आ जाय तो चंदा और सूरज को गेंद की तरह अपनी इच्छा के मुताबिक चला सकते हो। सती शाण्डिली ने सूरज को रोका था। नक्षत्रों को अपनी जगह से तुम हिला सकते हो, अगर प्राणशक्ति को अत्यंत सूक्ष्म कर लो तो।
जिसने केवली कुंभक की साधना कर ली है उसके आगे संसारी लोग अपनी शुभ कामना की मनौती माने तो उनके कार्य होने लगते हैं। प्राणायाम का ऊँचा फल जिसने पाया है, प्राणों पर नियंत्रण पाकर जिसने मन को जीत लिया है उसने सब कुछ जीत लिया है। जिसने मन को जीत लिया उसने प्राण को जीत लिया।
कभी अपने को हताश और निराश न करो, क्योंकि तुम प्राण लेते हो और मन भी तुम्हारे पास है। थोड़ा-बहुत साधना का मार्ग भी तुम्हारे पास है। ऐसी बात समझने की थोड़ी बहुत श्रद्धा, भक्ति और बुद्धि भी भगवान ने दी है। अतः घबराना नहीं चाहिए। कैसी भी कमजोरी हो, पहले का कैसा भी पलायनवाद घुसा हो फिर भी उत्साहपूर्वक निश्चय करो किः
"मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईश्वर का अनन्त बल मुझमें सुषुप्त पड़ा है। मैं उसे जगाऊँगा।"
मन और प्राण प्रकृति के हैं। प्रकृति परमात्मा की है। मन और प्राण का उपयोग तो करो, फिर मन और प्राण भी परमात्मा को अर्पण कर दो। प्राणायाम आदि करो, मन को एकाग्र करो, अपने नियंत्रण में लाओ, फिर ऐसा चिन्तन करो कि 'इन सब को देखने वाला मैं साक्षी, चैतन्य आत्मा हूँ।' ऐसा चिन्तन किया तो मन और प्राण ईश्वर को अर्पित हो गये। यह हो गया भक्ति योग। इससे भाव की शुद्धि होगी और बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होगी।
जो कर्मकाण्ड का अधिकारी है उसको कर्मकाण्ड में रूचि बढ़े ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए। जो उपासना का अधिकारी है, उसको उपासना में दृढ़ता रहे, उपासना में प्रीति बढ़े ऐसे वातावरण में और ऐसे संग में रहना चाहिए। उपासना करने वाला अगर विचार करेगा, बुद्धि का उपयोग करेगा तो उपासना से च्युत हो जायगा। उपासना का मार्ग यह है कि तुम श्रद्धा से उन्नत हो जाओ। जैसे, है तो शालिग्राम लेकिन आदि नारायण हैं। है तो शिवलिंग लेकिन कैलासपति भगवान शंकर हैं। कैलासपति मानकर उपासना करते हैं तो ठीक है लेकिन उपासक अगर विचार करे कि, 'कैलास में भगवान शंकर हैं कि नहीं, क्या पता....' तो वह उपासना से च्युत हो जायगा। पहले के जमाने में पैदल जाना होता था। कैलास में कैलासपति है कि नहीं यह पता लगाने का कोई साधन नहीं था। वहाँ भगवान हैं ही ऐसी श्रद्धा बनी रहती थी। लेकिन आजकल हेलिकोप्टर आदि साधनों से कहीं भी खोजबीन की जा सकती है पर उपासना के लिए ऐसी बुद्धि चलाना इष्ट नहीं है। उपासक को तो अपनी श्रद्धा बढ़ा-बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ विचार की आवश्यकता नहीं है।
कर्मकाण्डी अगर सीधा उपासना में आ जाएगा तो कर्म में उसकी रूचि टूट जाएगी। उपासक अगर विचार में आ जाएगा तो उपासना में रूचि टूट जाएगी। अतः जिस समय जो करते हैं उसमें लग जाओ। जिस साधक को जो साधन ज्यादा अनुकूल पड़ता हो उसमें दृढ़ता से लग जाये। तत्परता से साधना करे।
अगर प्राणोपासना में कोई ठीक से लग जाय तो उसका केवली कुंभक सिद्ध होता है। जिसका केवली कुंभक सिद्ध हो गया हो उसके आगे दूसरे लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होने लगती हैं तो उसकी अपनी कामनाओं का तो पूछना ही क्या?
मन, प्राण और शरीर इन तीनों का आपस में जुड़वे भाई जैसा सम्बन्ध है। शरीर भारी रहता हो तो प्राणायाम आदि करने से वह हल्का बन सकता है। एक बात खास याद रखें कि कभी बिना आसन के न बैठो। कोई भी एक आसन पंसन्द करो, बार-बार उसी आसन में बैठो। इससे मन पर थोड़ा प्रभाव आएगा। मन पर प्रभाव आएगा तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। कुण्डलिनी जगेगी। फिर जो कुछ क्रिया होने लगे उसको रोको नहीं। ध्यान करते समय शरीर घण्टी की तरह घूमता है या उछलकूद मचाता है तो उसको रोको मत। लेकिन ऐसे ही भजन में बैठे हो तो शरीर को चंचल मत रखो। बन्दर की तरह इधर हिले, उधर हिले, इधर झाँका, उधर झाँका..... ऐसे नहीं। बिना प्रयोजन की फालतू चेष्टाओं से शरीर को बचाओ। इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी।
हम साधन-भजन करते हैं तो मन थोड़ा-सा एकाग्र होता है, प्राण थोड़े सूक्ष्म होते हैं। शरीर में एक प्रकार की बिजली पैदा होती है, पित्त का प्रभाव बढ़ता है। शरीर का भारीपन और आलस्य दूर होता है, स्फुर्ति आती है।
तुलसी के पत्ते सात दिन तक बासी नहीं माने जाते। बेलफल तीन दिन तक बासी नहीं माना जाता। कमल का फूल दो दिन तक बासी नहीं माना जाता। दूसरे फल एक दिन तक बासी नहीं माने जाते।
तुलसी के पाँच पत्ते चबाकर पानी पियें तो शरीर में विद्युत शक्ति बढ़ती है। तुलसी में विद्युत तत्त्व ज्यादा है। तो क्या तुलसी दल ज्यादा खा लें? नहीं, नहीं। पाँच पत्ते ही काफी हैं। शरीर को तन्दुरुस्त रखने में सहायक होंगे।
कभी-कभी अपने इष्ट को प्यार करते हुए ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। वे इष्ट चाहे भोलेनाथ हों, भगवान राम हों, भगवान कृष्ण हों, कोई देवी देवता हो चाहे अपने सदगुरुदेव हों, जिनमें तुम्हारी अधिक श्रद्धा हो उन्हीं के चिन्तन में रम जाओ। रोना हो तो उन्हीं के विरह में रोओ। हँसना हो तो उन्हीं को प्यार करते हुए हँसो। एकाग्र होना तो उन्हीं के चित्र को एकटक निहारते हुए एकाग्र बनो।
इष्ट की लीला का श्रवण करना भी उपासना है। इष्ट का चिन्तन करना भी उपासना है। इष्ट के लिए रोना भी उपासना है। मन ही मन इष्ट के साथ चोरस खेलना भी उपासना। इष्ट के साथ मानसिक कबड्डी खेलना भी उपासना है। इष्ट के कुस्ती खेलना भी उपासना है। ऐसा उपासक शरीर की बीमारी के वक्त सोये सोये भी उपासना कर सकता है। उपासना सोते समय भी हो सकती है, लेटे लेटे भी हो सकती है, हँसते हँसते भी हो सकती है, रोते रोते भी हो सकती है। बस, मन इष्टाकार हो जाय।
मेरे इष्ट गुरुदेव थे। मैं नदी पर घूमने जाता तो मन ही मन उनसें बातें करता। दोनों की ओर होने वाला संवाद मन ही मन घड़ लेता। मुझे बड़ा मजा आता था। दूसरे किसी इष्ट के प्रत्यक्ष में कभी बात हुई नहीं थी, उसकी लीला देखी नहीं थी लेकिन अपने गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाहजी भगवान का दर्शन, उनका बोलना-चालना, व्यवहार करना आदि सब मधुर लीलाएँ प्रत्य़क्ष में देखने को मिलती थी, उनसे बातचीत का मौका भी मिला करता था। अतः एकान्त में जब अकेला होता तब गुरुदेव के साथ मनोमन अठखेलियाँ कर लेता। अभी भी कभी-कभी पुराने अभ्यास के मुताबिक घूमते-फिरते अपने साँईं से बातें कर लेता हूँ, प्यार कर लेता हूँ। साँईं तो साकार नहीं हैं, अपने मन के ही दो हिस्से हो जाते हैं। एक साँईं होकर प्रेरणा देता है दूसरा साधक होकर सुनता है। क्योंकि साँईं तत्त्व व्यापक होता है, गुरुतत्त्व व्यापक होता है।
कभी-कभी उपासक शिकायत करता है कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता है। इसी प्रकार करे तो ही भगवान में मन लगा है। ऐसी बात नही है । और किसी ढंग से भी मन भगवान में लग सकता है। जो लोग थोड़े भी उन्नत उपासक हैं उनका मन जब चाहे तब भगवान में लग सकता है।
मेरे गुरुदेव कभी-कभी अकेले कमरे में बैठे-बैठे भगवान के साथ विनोद करते। उनका भगवान तो तत्त्व रूप में था। वे जगे हुए महापुरुष थे। वे एकांत में कभी-कभी ठहाका मारकर हँसते। मोर की तरह आवाज करतेः
"पियू ऽऽऽऽ....!"
फिर अपने आपको कहतेः
"बोल,लीलाशाह !"
वे अपने आपको 'शाह' नहीं बोलते थे, पहले दो अक्षर ही अपने लिए बोला करते थे, लेकिन मुझसे वह नाम बोला नहीं जाता। वे अपने आपसे संवाद-वार्ता-विनोद करतेः
"बोल,लीलाशाह !"
"जी साँईं !"
"रोटी खाएगा?"
"हाँ, साँईं ! भूख लगी है।"
"रोटी तब खायगा जब सत्संग का मजा लेगा। लेगा न बेटा ?"
"हाँ महाराज ! लूँगा, जरूर लूँगा।"
"कितनी रोटी खाएगा। ?"
"तीन तो चाहिए।"
"तीन रोटी चाहिए तो तीनों गुणों से पार होना है। बोल, होगा न ?"
"हाँ, साँईं, पार हो जाऊँगा लेकिन अभी तो भूख लगी है।"
"अरे भूख तुझे लगी है ? झूठ बोलता है ? भूख तेरे प्राणों को लगी है।"
"हाँ साँई, प्राणों की लगी है।"
"शाबाश ! अब भले रोटी खा, लीलाशाह ! रोटी खा !"
ऐसा करके विनोद करते और फिर भोजन पाते। उनकी उपासना-काल का कोई अभ्यास पड़ा होगा तो नब्बे साल की उम्र में भी ऐसा किया करते थे.
यह सब बताने के पीछे मेरा प्रयोजन यह है कि तुम्हें भी उपासना की कोई कुंजी हाथ लग जाय।
इष्ट का चिन्तन करना अथवा इष्टों का इष्ट आत्मा अपने को मानना और शरीर के अपने से अलग मानकर चेष्टा और चिन्तन करना यह भी उपासना के अंतर्गत आ जाता है।
लड़की जब ससुराल जाती है तब मायका छोड़ते हुए कठिनाई लगती है। जब ससुराल में सेट हो जाती है तो मायके कभी-कभी ही आती है। आती है तब भी उसके पैर अधिक टिकते नहीं। कुछ ही समय में वह चाहती है कि अब जाऊँ अपने घर। आज तक जिसको अपना घर मान रही थी वह धीरे-धीरे भाई का घर हो जाता है, बाप का घर हो जाता है। पति का घर ही अपना घर हो जाता है।
ऐसे ही उपासक अपने इष्ट के साथ ब्याहा जाता है तो उसको इष्ट का चिन्तन अपना लगता है और संसार का चिन्तन पराया लगता है।
संसार तुम्हारा पराया घर है। असली घर तो है भगवान, आत्मा-परमात्मा। वह प्यारा तुम्हारा बाप भी है, भाई भी है, पति भी है, सखा भी है, जो मानो सो है। लड़की का पति सब नहीं हो सकता लेकिन साधक का पति सब हो सकता है। क्योंकि परमात्मा सब कुछ बना बैठा है।
गुरु को जो शरीर में ही देखते हैं वे देर-सबेर डगमग हो जाते हैं। गुरु को शरीर मानना और शरीर को ही गुरु मानना यह भूल है। गुरु तो ऐसे हैं जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। 'शिवमहिम्न स्तोत्र' में आता हैः
नास्ति
तत्त्वं
गुरोः परम्।
गुरु से ऊपर कोई भी तत्त्व नहीं है। गुरु तत्त्व सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होता है। अतः गुरु को केवल देह में ही देखना, गुरु को देह मानना यह भूल है।
मैं अपने गुरुदेव को अपने से कभी दूर नहीं मानता हूँ। आकाश से भी अधिक सूक्ष्म तत्त्व हैं वे। जब चाहूँ तब गोता मारकर मुलाकात कर लेता हूँ।
ऐसे सर्वव्यापक परम प्रेमास्पद गुरुतत्त्व को इसी जीवन में पा लेने का लक्ष्य बना रहे। साधक यह लक्ष्य न भूले। ध्यान-भजन में भी लक्ष्य भूल जाएगा तो निद्रा आयेगी, तंद्रा आयेगी।
साधक चिंतन करता रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहे। निद्रा, तंद्रा, रसास्वाद आदि विघ्न आ जायें तो उससे बचना है। ध्यान करते समय श्वास पर ध्यान रहे, दृष्टि नासाग्र या भ्रूमध्य में रहे अथवा अपने को साक्षी भाव से देखता रहे। इसमें भी एकाध मिनट देखेगा, फिर मनोराज हो जायेगा। तब लम्बा श्वास लेकर प्रणव का दीर्घ उच्चारण करेः 'ओ....म् ऽऽऽऽ....'
फिर देखे कि मन क्या कर रहा है। मन कुछ न कुछ जरूर करेगा, क्योंकि पुरानी आदत है। तो फिर से गहरा श्वास लेकर होंठ बन्द करके 'ॐ' का गुंजन करे। इस गुंजन से शरीर में आंदोलन जगेंगे, रजो-तमोगुण थोड़ा क्षीण होगा। मन और प्राण का ताल बनेगा। आनन्द आने लगेगा। अच्छा लगेगा। भीतर से खुशी आयेगी। तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न है तो बाहर से भी प्रसन्नता बरसाने वाला वातावरण सहज में मिलेगा। भीतर तुम चिंतित हो तो बाहर से भी चिंता बढ़ाने वाली बात मिलेगी। भीतर से तुम जैसे होते हो, बाहर के जगत से वैसा ही प्रतिभाव तुम्हें आ मिलगा।
जगत तीन प्रकार के हैं- एक स्थूल जगत है जो हम आँखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, इस जिह्वा से चखते हैं, इस नासिका से सूँघते हैं। यह स्थूल जगत है, दूसरा सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत लौकिक जगत है, दूसरा अलौकिक जगत है। इन दोनों से पार तीसरा है लोकातीत जगत। यह है लौकिक अलौकिक दोनों का आधार, दोनों का साक्षी।
जगत को देखने की दृष्टि भी तीन प्रकार की हैः एक है स्थूल दृष्टि या चक्षुदृष्टि, दूसरी मनदृष्टि और तीसरी वास्तविक दृष्टि।
स्थूल जगत में जो कुछ दिखता है यह स्थूल आँखों से दिखता है। सूक्ष्म जगत अंदर के मनः चक्षु से दिखता है। जैसे, किसी साधना के द्वारा हम अपने इष्ट या सदगुरु से अनुसंधान कर लें तो हमें दूर का कुछ अजीब-सा दर्शन होगा। वह लौकिक नहीं होगा, अलौकिक होगा। कभी संगीतवाद्यों के मधुर स्वर सुनाई पड़ेंगे। कभी अलौकिक सुगन्ध आने लगेगी। इस प्रकार के अनुभव हों तब जानना कि मन लौकिक जगत से हटकर अलौकिक जगत में प्रविष्ट हुआ है, बाह्य चक्षु से हटकर आंतरक्षु में गया है। आंतरचक्षु वाले साधक एक दूसरे को समझ सकते हैं जबकि दूसरे लोग उनकी बातों की मजाक उड़ायेंगे।
साधक को अपने आंतर जगत के अनुभव अत्यंत बहिर्मुख लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि बहिर्मुख लोग तर्क-कुतर्क करके साधक के अनुभव को ठेस पहुँचा देगा। बाहर के आदमी में तर्क करने की योग्यता ज्यादा होगी और साधक तर्क के जगत में नहीं है, भावना के जगत में है। भाववाला अगर बौद्धिक जगत वाले के साथ टकराता है तो उसके भाव में शिथिलता आ जाती है। इसीलिए साधकों को शास्त्र की आज्ञा है कि अपना आध्यात्मिक अनुभव नास्तिक और निगुरे, साधारण लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव जितना गोप्य रखा जाए उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता है।
मन, प्राण और शरीर इन तीनों का एक दूसरे के साथ जुड़वे भाई जैसा सम्बन्ध है। इसलिए शरीर को ऐसा खुराक मत खिलाओ कि ज्यादा स्थूलता आ जाय। अगर नींबू प्रतिकूल न पड़ता हो तो साधक को भोजन में नींबू लेना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी के पत्ते चबाने चाहिए। नंगे पैर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। नंगे पैर चलने फिरने से शरीर का विद्युत तत्त्व भूमि में उतर जाता है। भजन के प्रभाव से बढ़ा हुआ विद्युत तत्त्व कम हो जाने से शिथिलता आ जाती है।
शरीर में भारीपन रहने से ध्यान-भजन में मजा नहीं आता, काम करने में भी मजा नहीं आता। जिसको ध्यान-भजन में मजा आता है उस साधक को लौकिक जगत में से अलौकिक सूक्ष्म जगत में जाने की रूचि जगती है। लौकिक जगत में तो कर्म करके, परिश्रम करके थोड़ा सा मजा मिलता है जबकि भावना के जगत में बिना कर्म किये, भावना से ही आनन्द मिलता है। ध्यान के द्वारा, प्रेमाभक्ति के द्वारा साधक को जो मजा मिलता है वह लौकिक जगत के पदार्थों से नहीं मिल सकता। भीतर का मजा ज्यों-ज्यों आता जाएगा त्यों-त्यों बाहर के पदार्थों का आकर्षण छूटता जाएगा। आकर्षण छूटा तो वासना कम होगी। वासना कम होगी तो मन की चंचलता कम होगी। मन की चंचलता कम होगी तो बुद्धि का परिश्रम कम होगा। बुद्धि स्थिर होने लगेगी तो ज्ञानयोग में अधिकार मिल जाएगा।
निष्काम कर्म उपासना का पासपोर्ट देता है उपासना ज्ञान का पासपोर्ट देती है। फिर भी यदि किसी ने पहले उपासना कर रखी है, बुद्धि बढ़िया है, श्रद्धा गहरी है और समर्थ सदगुरु मिल जाते हैं तो सीधा ज्ञान के मार्ग पर साधक चल पड़ता है। जैसे राजा जनक चल पड़े थे वैसे कोई भी अधिकारी साधक जा सकता है। कोई उपासना से शुरु कर सकता है। प्रायः ऐसा होता है कि सत्कर्म, शुभकर्म करते हुए, सदाचार से चलते हुए साधक आगे बढ़ता है। फिर उपासना में प्रवेश होता है। उपासना परिपक्व होने पर ज्ञान मार्ग में गति होने लगती है।
प्रारंभिक साधक को समाज में रहते हुए साधना करने से यह तकलीफ होती है कि उसके इर्दगिर्द पच्चीस लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और साधक होता है सदाचारी। वे पच्चीस लोग इसे मूर्ख मानेंगे। उन भ्रष्टाचारियों को पता नहीं होता कि वे अपना मन और जीवन मलिन करके जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं उसका भोग तो उनके भाग्य में जितना होगा उतना ही कर पाएँगे। बाकी से तो उनका आहार, तन और मन अशुद्ध होगा और दुःख देगा। लेकिन वे लोग समझते नहीं और साधक का मजाक उड़ाते हैं।
भोगी विलासी लोग रजो-तमोगुण बढ़ानेवाले आहार लेते हैं और मानते हैं कि हम 'फर्स्ट क्लास' भोजन करते हैं लेकिन वास्तव में इन्हीं आहारों से आदमी 'थर्ड क्लास' होता है। दुनिया की नजरों में अच्छा आहार है उसको साधक समझता है कि यह नीचे के केन्द्रों में ले जाने वाला आहार है। यह 'थर्ड क्लास है।' 'फर्स्ट क्लास' के आहार तो शरीर को तन्दुरुस्त रखता है मन को प्रसन्न रखता है और बुद्धि को तेजस्वी बनाता है।
मैंने सुनी है एक कहानी।
एक मुल्ला की प्रसिद्धि दूसरे मुल्ला-मौलवियों की असह्य हो रही थी। जब तक आत्म-साक्षात्कार नहीं होता तब तक धार्मिक जगत हो जा व्यावहारिक जगत हो, राग-द्वेष चलता रहता है, एक दूसरे के पैर खींचने की चेष्टाएँ होती ही रहती हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक ऐसा होता ही रहेगा। दोनों शरीरों से जो पार गया, आत्मज्ञानी हो गया उसके लिए यह झंझट नहीं है, बाकी के लिए तो झंझट रहेगी ही।
दूसरे मौलवियों ने इस मुल्ला के लिए बादशाह को शिकायत कर दी। उसके चारित्र्य विषयक कीचड़ उछाल दी। बादशाह ने सोचा कि यह प्रसिद्ध मुल्ला है। इसको अगर दंड आदि देंगे तो राज्य में भी इसके चाहकों की बददुआ लगेगी। वजीरों की राय ली तो उन्होंने कहा कि ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे साँप भी मर जाए और लाठी भी बच जाय। उन्होंने उपाय भी बता दिया। बादशाह ने उस प्रकार अपने महल के चार कमरे में व्यवस्था कर दी। फिर मुल्ला को बुलवाकर कहा गया कि आप रात भर यहाँ अकेले ही रहेंगे। दूसरा कोई नहीं होगा। इन चार कमरों में से किसी भी एक कमरे का उपयोग करोगे तो बादशाह सलामत खुश होंगे और आपको छोड़ दिया जायगा। अगर उपयोग नहीं किया तो जहाँपनाह का अनादर माना जाएगा। फिर वे जो फरमान करेंगे वैसा होगा।
उन चारों कमरों में मुल्ला ने देखा। पहले कमरे में फाँसी लटक रही थी। इस कमरे का उपयोग करना माने फाँसी खाकर मर जाना। मुल्ला आगे बढ़ गया। दूसरे कमरे में हार-सिंगार करके नाज-नखरे करती हुई वेश्या बैठी थी। तीसरे कमरे में मांस-कबाब-अंडे आदि आसुरी खुराक खाने को रखे गये थे। चौथे कमरे में दारू की बोतलें रखी गईं थीं।
मुल्ला ने सोचा कि ऐसी नापाक चीजों का उपयोग मैं कैसे करूँ। मैं दारू क्यों पिऊँ ? मांसाहार भी कैसे कर सकता हूँ ? वेश्यागमन से तो खुदा बचाय ! तो क्या फाँसी खाकर मर जाऊँ ? क्या किया जाय ?
मुल्ला इधर-उधर चक्कर काट रहा है। रात बीती जा रही है। प्यास भी लगी है। उसने सोचाः दारू में पानी भी होता है। पानी से हाथ भी साफ किये जाते हैं। अब बात रही थोड़ी-सी। जरा-सा दारू पी लूँगा। प्यास भी बुझ जायगी और बादशाह सलामत की बात भी रह जायेगी। मैं मुक्त हो जाऊँगा।
मुल्ला ने थोड़ा दारू पी लिया। जिह्वा पर थोड़ा अशुद्ध आहार आ गया तो मन पर भी उसका प्रभाव पड़ गया। थोड़ा और पी लूँ तो क्या हर्ज है ? ऐसा सोचकर किस्म-किस्म के दारू के घूँट भरे, नशा चढ़ा। भूख भी खुली। मन, बुद्धि, प्राण नीचे आ गये। भूख लगी है और खुदा ने तैयार रख ही दिया है तो चलो, खा लें। मुल्ला ने मांस-अंडे-कबाब आदि भर पेट खा लिया। अंडे खाये तो इन्द्रियाँ उत्तेजित हो गईं तो चला गया वेश्या के कमरे में। 'वह बेचारी इन्तजार कर रही है। किसी के मन को खुश करना यह भी तो पुण्यकर्म है।' मन कैसा बेवकूफ बना देता है इन्सान को?
मुल्ला वेश्या के कमरे में गया। सुबह होते-होते उसका सत्त्व खत्म हो गया, शरीर में बल का बुरी तरह ह्रास हो गया। मुल्ला का चित्त ग्लानि से भर गया। 'हाय ! यह मैंने क्या कर लिया? दारू भी पी लिया, अभक्ष्य भोजन भी खा लिया और वेश्या के साथ काला मुँह भी कर लिया। मैं धार्मिक मुल्ला ! पाँच बार नमाज पढ़नेवाला ! और यह मैंने क्या किया ? लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा ?'
हीन भाव से मुल्ला आक्रान्त हो गया और चौथे कमरे में जाकर फाँसी खाकर मर गया। पतन की शुरुआत कहाँ से हुई ? 'जरा-सा यह पी लें।' बस 'जरा-सा.... जरा-सा...' करते-करते मन कहाँ पहुँचाता है ! जरा-सा लिहाज करते हो तो मन चढ़ बैठता है। दुर्जन को जरा सी उँगली पकड़ने देते हो तो वह पूरा हाथ पकड़ लेता है। ऐसे ही जिसका मन विकारों में उलझा हुआ है उसके आगे लिहाज रखा तो अपने मन में छुपे हुए विकार भी उभर आयेंगे। अगर मन को संतों के तरफ, इष्ट के तरफ, सेवकों के तरफ, सेवाकार्यों के तरफ थोड़ा-सा बढ़ाया तो और सेवकों का सहयोग मिल जाता है। उपासना के तरफ मन बढ़ाया तो और उपासक मिल जाते हैं। इस मार्ग में थोड़ा-थोड़ा बढ़ते-बढ़ते मन नारायण से मिलता है और उधर अगर मन मुड़ जाता है तो आखिर में असुर से मिलता है।
असुर से मिलता है, तमस् से मिलता है तो मन नीची योनियों में जाता है। मन अगर साधकों का संग करता है, सत्संग करता है, इष्ट के साथ जुड़ता है तो इष्ट के अनुभव से एक हो जाता है, अहं ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लेता है। गुरु का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है, श्रीकृष्ण का अनुभव हो जाता है, शिवजी का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है, रामजी का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है। अन्यथा तो फिर पशु-पक्षी, वृक्ष आदि योनियों में भटकना पड़ता है।
मनुष्य जीवन मिला है। पराधीनता की जंजीरों में जकड़ने वाले विनाश की ओर चलो या परम स्वातंत्र्य के द्वार खोलने वाले विकास की ओर उन्मुक्त बनो, मरजी तुम्हारी।
नारायण..... नारायण.... नारायण.... नारायण.... नारायण....।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सत्संग
संचय
१. ज्ञानयोग
श्री योगवाशिष्ठ महारामायण में 'अर्जुनोपदेश' नामक सर्ग में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं-
"हे भारत ! जैसे दूध में घृत और जल में रस स्थित होता है वैसे ही सब लोगों के हृदय में तत्त्व रूप से स्थित हूँ। जैसे दूध में घृत स्थित है वैसे ही सब पदार्थों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूँ। जैसे रत्नों के भीतर-बाहर प्रकाश होता है वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर-बाहर स्थित हूँ। जैसे अनेक घटों के भीतर-बाहर एक ही आकाश स्थित है वैसे ही मैं अनेक देहों में भीतर बाहर अव्यक्त रूप स्थित हूँ।"
जैसे आकाश में सब व्याप्त है वैसे मैं चिदाकाश रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ। बन्धन और मुक्ति दोनों प्रकृति में होते हैं। पुरुष को न बन्धन है न मुक्ति है। जन्म-मृत्यु आदि जो होता है वह सब प्रकृति में खेल हो रहा है। पानी में कुछ नहीं, तरंगों में टकराव है। आकाश में कुछ नहीं, घड़ों में बनना बिगड़ना होता है।
तुम चिदघन चैतन्य आत्मा हो। जैसे दूध में घी होता है, मिठाई में मिठाश होती है, तिलों में तेल होता है ऐसे ही चैतन्य सर्वत्र व्याप्त होता है, सबमें ओतप्रोत है। तिलों में से तेल निकाल दो तो तेल अलग और फोतरे अलग हो जाएँगे लेकिन चैतन्य में ऐसा नहीं है। जगत में से ब्रह्म अलग निकाल लो, ऐसा नहीं है। तिलों में से तो तेल निकल सकता है लेकिन जगत में से ब्रह्म नहीं निकल सकता।
जैसे जगत में से आकाश नहीं निकल सकता ऐसे ही आकाश में से भी चिदाकाश नहीं निकल सकता। यह चिदाकाश ही परमात्म-तत्त्व है। वही हर जीव का अपना आपा है लेकिन जीव 'मैं' और 'मेरा' करके इन्द्रियों के राज्य में भटक गया है इसलिए जन्म-मरण हो रहा है। नहीं तो जर्रा-जर्रा खुदा है। खुदा की कसम, जर्रा-जर्रा खुदा है। कोई उससे जुदा नहीं है।
सब
घट मेरा
साँईया खाली
घट ना कोय।
बलिहारी
वा घट की जा घट
परगट होय।।
कबीरा
कुँआ एक है
पनिहारि
अनेक।
न्यारे
न्यारे
बर्तनों में
पानी एक का
एक।।
ज्ञानयोग में निष्ठुर होकर ज्ञान का विचार करें। वहाँ लिहाज नहीं करना है। श्रद्धा करें, उपासना करें तो अन्धा होकर श्रद्धा करें। उपासना में अन्धश्रद्धा चाहिए, गहरी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा में विचार की जरूरत नहीं है, अन्यथा श्रद्धा तितर-बितर हो जायेगी। है तो पत्थर, है तो शालिग्राम लेकिन भगवान है। वहाँ विचार मत करो। है तो मिट्टी का पिंड, लेकिन दृढ़ भावना रखो कि शिवलिंग है, साक्षात भगवान शिव हैं। श्रद्धा में विचार को मत आने दो।
हम लोग क्या करते हैं? श्रद्धा में विचार घुसेड़ देते हैं.... विचार में श्रद्धा घुसेड़ देते हैं। नहीं...। जब आत्मविचार करो तब निष्ठुर होकर करो। 'जगत कैसे बना ? ब्रह्म क्या है ? आत्मा क्या है ? मैं आत्मा कैसे ?' कुतर्क तो नहीं लेकिन तर्क अवश्य करो। 'तर्क्यताम्... मा कुतर्क्यताम्।' विचार करो तो निष्ठुर होकर करो और श्रद्धा करो तो बिल्कुल अन्धे होकर करो। अपने निश्चय में अडिग। चाहे कुछ भी हो, सारी दुनिया, सारी खुदाई एक तरफ हो लेकिन मेरा इष्ट, मेरा खुदा, मेरा भगवान अनन्य है, मेरे गुरु का वचन आखिरी है।
ध्यानमूलं
गुरोर्मूर्तिः
पूजामूलं
गुरोः पदम्।
मंत्रमूलं
गुरोर्वाक्यं
मोक्षमूलं
गुरोः कृपा।।
श्रद्धा करो तो ऐसी। विचार करो तो निष्ठुर होकर। श्रद्धालु अगर कहे किः 'अच्छा ! मैं सोचूँगा.... विचार करूँगा....' तो 'मैं' बना रहेगा, फिर रोता रहेगा।
कर्म करो तो एकदम मशीन होकर करो। मशीन कर्म करती है, फल की इच्छा नहीं करती। वह तो धमाधम चलती है। यंत्र की पुतली की तरह कर्म करो। काम करने में ढीले न बनो। झाड़ू लगाओ तो ऐसा लगाओ कि कहीं कचरा रह न जाय। रसोई बनाओ तो ऐसी बनाओ कि कोई दाना फालतू न जाय, कोई तिनका बिगड़े नहीं। कपड़ा धोओ तो ऐसा धोओ कि साबुन का खर्च व्यर्थ न हो, कपड़ा जल्दी न फटे फिर भी चमाचम स्वच्छ बन जाय। कर्म करो तो ऐसे सतर्क होकर करो। ऐसा कर्मवीर जल्दी सफल जो जाता है। हम लोग थोड़े कर्म में, थोड़े आलस्य में, थोड़े Dull थोड़े Lazy थोड़े पलायनवादी होकर रह जाते हैं। न ही इधर के रहते हैं नहीं उधर के।
कर्म करो तो बस, मशीन होकर, बिल्कुल सतर्कता से, Up-to-date काम करो।
प्रीति करो तो बस, लैला मजनूँ की तरह।
एक बार लैला भागी जा रही थी। सुना था कि मजनूँ कहीं बैठा है। मिलन के लिए पागल बनकर दौड़ी जा रही थी। रास्ते में इमाम चद्दर बिछाकर नमाज पढ़ रहा था लैला उसकी चद्दर पर पैर रखकर दौड़ गई। इमाम क्रुद्ध हो गया। उसने जाकर बादशाह को शिकायत कीः "मैं खुदा की बन्दगी कर रहा था.... मेरी चद्दर बिछी थी उस पर पैर रखकर वह पागल लड़की चली गई। उसने खुदाताला का और खुदा की बन्दगी करने वाले इमाम का, दोनों का अपमान किया है। उसे बुलाकर सजा दी जाय।"
इमाम भी बादशाह का माना हुआ था। बादशाह ने लैला को बुलाया, उसे डाँटते हुए कहाः
"मूर्ख पागल लड़की ! इमाम चद्दर बिछाकर खुदाताला की बन्दगी कर रहा था और तू उसकी चद्दर पर पैर रखकर चली गई ? तुझे सजा देनी पड़ेगी। तूने ऐसा क्यों किया ?"
"जहाँपनाह ! ये बोलते हैं तो सही बात होगी कि मैं वहाँ पैर रखकर गुजरी होऊँगी लेकिन मुझे पता नहीं था। एक इन्सान के प्यार में मुझे यह नहीं दिखा लेकिन ये इमाम सारे जहाँ के मालिक खुदाताला के प्यार में निमग्न थे तो इनको मैं कैसे दिख गई ? मजनूँ के प्यार में मेरे लिए सारा जहाँ गायब हो गया था जबकि इमाम सारे जहाँ के मालिक खुदाताला के प्यार में निमग्न थे तो इनको मैं कैसे दिख गई ? मजनूँ के प्यार में मेरे लिये सारा जहाँ गायब हो गया था जबकि इमाम सारे जहाँ के मालिक से मिल रहे थे फिर भी उन्होंने मुझे कैसे देख लिया ?"
बादशाह ने कहाः "लैला ! तेरी मजनूँ में प्रीति सच्ची और इमाम की बन्दगी कच्ची। जा तू मौज कर।"
श्रद्धा
करो तो ऐसी
दृढ़ श्रद्धा
करो। विश्वासो
फलदायकः।
आत्मविचार करो तो बिल्कुल निष्ठुर होकर करो। उपासना करो तो असीम श्रद्धा से करो। कर्म करो तो बड़ी तत्परता से करो, मशीन की तरह बिल्कुल व्यवस्थित और फलाकांक्षा से रहित होकर करो। भगवान से प्रेम करो तो बस, पागल लैला की तरह करो, मीरा की तरह करो, गौरांग की तरह करो।
गौरांग की तरह कीर्तन करने वाले आनंदित हो जाते हैं। तुमने अपनी गाड़ी का एक पहिया ऑफिस में रख दिया है, दूसरा पहिया गोदाम में रखा है। तीसरा पहिया पंक्चरवाले के पास पड़ा है। स्टीयरिंग व्हील घर में रख दिया है। इंजिन गेरेज में पड़ा है। अब बताओ, तुम्हारी गाड़ी कैसी चलेगी?
ऐसे ही तुमने अपनी जीवन-गाड़ी का एक पुर्जा शत्रु के घर रखा है, एक पुर्जा मित्र के घर रखा है, दो पुर्जे फालतू जगह पर रखे हैं। तो यह गाड़ी कैसी चलेगी यह सोच लो। दिल का थोड़ा हिस्सा परिचितों में, मित्रों में बिखेर दिया, थोड़ा हिस्सा शत्रुओं, विरोधियों के चिन्तन में लगा दिया, थोड़ा हिस्सा ऑफिस में में, दुकान में रख दिया। बाकी दिल का जरा सा हिस्सा बचा उसका भी पता नहीं कि कब कहाँ भटक जाय ? बताओ, फिर उद्धार कैसे हो?
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
२. राम के
दीवाने
जिनके पास ज्ञान की शलाका आ गई है, उनको रोम-रोम में रमनेवाले रामतत्त्व का अनुभव हो जाता है। वे राम के दीवाने हो जाते हैं। राम के दीवाने कैसे होते हैं?
राम
के दीवानों को
जग के सुख की
चाह नहीं।
मुसीबतों
के पहाड़ टूटे
मुँह से निकलती
आह नहीं।।
स्वामी रामतीर्थ बोलते थेः "हे भगवान ! आज मुसीबत भेजना भूल गये क्या? हम रोज ताजी मुसीबत चाहते हैं। आज कोई मुसीबत नहीं आयी? कोई प्रोब्लेम नहीं आया?"
रामतीर्थ के लिए कई कुप्रचार फैलाये जाते थे, कई अफवाहें चलती थीं। राम बादशाह तो ॐ....ॐ....ॐ..... आनन्द.... मैं ब्रह्म हूँ....' इस प्रकार आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में मस्त रहते, हँसते रहते, नाचते रहते। तथा कथित सयाने लोग उनकी आलोचना करते की ऐसा कोई संत होता है ? उन्माद हो गया है उन्माद। ऐसी चिट्ठियाँ भी लोग लिख देते थे।
स्वामी राम कहतेः
"मुझे सीख देने वाले ! मुझे तो भले उन्माद हो गया है लेकिन तुम्हें तो उन्माद नहीं हुआ है। जाओ, तुम्हें रमणियाँ बुलाती हैं। उनके हाड़ मांस तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ, चाटो.... चूसो। मैं तो मेरे राम की मस्ती में हूँ। मुझे तो यही उन्माद काफी है। तुम भले रमणियों के उन्माद में खुशी मनाओ। लेकिन सावधान ! वह उन्माद बाबरा भूत है ! दिखता है अच्छा, सुन्दर, सुहाना लेकिन ज्यों ही आलिंगन किया तुरन्त सत्यानाश होगा। राम रस के उन्माद का अनुभव एक बार करके देखो, फिर जन्मों के उन्माद दूर हो जायेंगे।"
किसी ने रामतीर्थ को खत लिखा कि, "आपके निकटवर्ती शिष्य एन. एस. नारायण ने संन्यासी के वस्त्र उतार कर पेन्ट कोट पहन लिया, संन्यासी में से गृहस्थी हो गया ज्ञानी का शिष्य, साधु बना और फिर गुलाम बन गया, नौकरी करता है ! उसको जरा सुधारो।"
रामतीर्थ ने जवाब दियाः "राम बादशाह आप में ही समाता नहीं है। राम बादशाह कोई गङरिया नहीं है कि भेड़-बकरियों को सँभालता रहे। वह अपनी इच्छा से मेरे पास आया, अपनी मरजी से साधु बना, उसकी मरजी। सब सबकी सँभाले, राम बादशाह अपने आप में मस्त हैं।"
ज्ञानी को सब समेट लेने में कितनी देर लगती है? शिष्यों को सुधारने के लिए पाँच-दस बार परिश्रम कर लिया, अगर वे नहीं सुधरते तो जायें। ज्ञानी उपराम ही जाते हैं तो घाटा उन्हीं मूर्खों को पड़ेगा। ज्ञानी को क्या है? वैसे मूर्खों को हम आज नहीं जानते लेकिन स्वामी रामतीर्थ को लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग जानते हैं।
आप भी कृपा करके राम की मस्ती की ओर उन्मुख बनें। उन सौभाग्यशाली साधकों के अनुभव की ओर चलिए किः
राम
के दीवानों को
जग के सुख की
चाह नहीं ।
मुसीबतों
के पहाड़ टूटे
मुँह से
निकलती आह नहीं
।।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
३.
यमराज का 'डिपार्टमेन्ट'
पृथ्वी पर कुछ आत्म-साक्षात्कारी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष आ गये। उनका दर्शन पाकर लोग खुशहाल हो जाते थे। उनके अमृतवचन सुनकर लोगों के कान पावन हो जाते थे। उनके उपदेश का मनन करने से मन पवित्र हो जाता था। उनके ज्ञान में गोता मारने से बुद्धि बलवती हो जाती थी, जीवन तेजस्वी हो जाता था। लोग पुण्यात्मा बनते थे, संयतेन्द्रिय होते थे। सूक्ष्म शक्तियों का विकास करते थे। वे लोग तो तर जाते थे लेकिन उनके पूर्वज भी जहाँ जाते थे वहाँ से ऊर्ध्वगति प्राप्त कर लेते थे। नरक में पड़े हुए लोग अपने इन सुपात्र संतानों के पुण्यबल से नरक की यातनाओं से छूटकर स्वर्ग में चले जाते थे। नरक खाली होने लगा। नये लोग नरक में आते नहीं और पुराने छूटकर चले जाते। नरक का कारोबार ठप्प हो गया।
यमराज चिन्तित हो उठे कि मेरे 'डिपार्टमेन्ट' में कोई काम नहीं रहा! सब बेकार हो गये!
अपना डिपार्टमेन्ट धमाधम चलता है तो आदमी खुशहाल रहता है। 'डिपार्टमेन्ट' बन्द होने लगे तो चिन्ता आ घेरती है।
यमराज पहुँचे ब्रह्माजी के पास। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीः
"ब्रह्मण ! मेरे नरक में कोई पापी अब आते नहीं और पुराने पापी जो बन्द थे उनके पुत्र-परिवार वाले मृत्युलोक में ब्रह्मज्ञानियों का सत्संग सुनकर इतने पुण्यात्मा हो जाते हैं कि उनके ये पूर्वज भी पुण्यप्रताप से नरक छोड़कर स्वर्ग में चले जाते हैं। मेरा डिपार्टमेन्ट खतरे में है। कृपा करके आप कुछ उपाय बताइये। कम-से-कम मेरा विभाग तो चलता रहे।"
ब्रह्माजी ने पद्मासन बाँधा। कमण्डलु से पानी लेकर जहाँ से योगेश्वरों का योग सिद्ध होता है, जिसमें शिवजी रमण करते हैं, जिसमें भगवान नारायण विश्राम पाते हैं, जिसमें ज्ञानेश्वर महाराज प्रतिष्ठित होते थे, जिसमें और ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी सत्पुरुष विराजमान हैं उसी आत्म-परमात्मदेव में स्थित होकर संकल्प किया किः "जब-जब पृथ्वी लोक में कोई ब्रह्मज्ञानी जाएँगे। तब-तब कोई न कोई निन्दक लोग पैदा हुआ करेंगे। ये निन्दक लोग तो डूबेंगे ही, उनकी निन्दा सुनकर भी लोग डूबेंगे। ये सब लोग तुम्हारे पास नरक में आयेंगे। तुम्हारा डिपार्टमेन्ट चलता रहेगा।"
तब से लेकर आज तक यमराज का डिपार्टमेन्ट बन्द नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया।
वशिष्ठजी महाराज बोलते हैं- "हे रामजी ! मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिये क्या-क्या बकवास करते हैं, यह मैं जानता हूँ।"
कबीरजी के लिए लोग बोलते थे। ऋषि दयानंद को लोगों ने बाईस बार जहर दिया। विवेकानन्द के लिए लोग बकते थे, रामकृष्ण के लिए लोग बकते थे, रामतीर्थ के लिए लोग बकते थे, मुहमद के भी विरोधी थे।
ब्रह्म परमात्मा चाहे राम होकर आ जायें चाहे श्रीकृष्ण होकर आ जायें चाहे जगदगुरु शंकराचार्य होकर आ जायें फिर भी निन्दक तो मिलते ही हैं, क्योंकि यमराज का डिपार्टमेन्ट चालू रखना है। उस डिपार्टमेन्ट में जो अपने कुटुम्ब-परिवार को भेजना चाहता है वह जरूर संतों की निन्दा करे, भगवान, भक्त और साधकों के विरोध में रहे।
श्रीकृष्ण के जमाने में, श्रीराम के जमाने में वह डिपार्टमेन्ट चालू रहा था तो अब क्या बन्द गया होगा ? अभी तो कलजुग है। वह डिपार्टमेन्ट बहुत बड़ा बन गया होगा। ज्यादा लोग रह सकें ऐसी व्यवस्था हुई होगी।
नारायण.... नारायण..... नारायण.... नारायण..... नारायण....।
जब वशिष्ठ जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, कबीर और नानक को नहीं छोड़ा, श्रीराम और श्रीकृष्ण को नहीं छोड़ा तो जब तुम्हारी निन्दा करे तो तुम घबराओ नहीं। सिकुड़ो मत। कोई निन्दा करे तो भगवान का मार्ग मत छोड़ो। कोई स्तुति करे तो फूलो मत, निन्दा करे तो मुरझाओ मत। संसार इन्द्रियों का धोखा है। निन्दा स्तुति आने जाने वाली चीज है। तुम लगे रहो अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
४. सदगुरु-महिमा
गुरुबिन
भवनिधि तरहिं
न कोई।
चाहे
विरंचि शंकर
सम होई।।
ब्रह्माजी जैसा सृष्टि सर्जन का सामर्थ्य हो, शंकरजी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो फिर भी जब तक सदगुरु तत्त्व की कृपा नहीं होती तब तक आवरण भंग नहीं होता, आत्म-साक्षात्कार नहीं होता। दिल में छुपा हुआ दिलबर करोड़ों युगों से है, अभी भी है फिर भी दिखता नहीं।
आदमी अपने को आँखवाला समझता है। वास्तव में वह आँख है ही नहीं। बाहर की आँख चर्म की आँख है। वह तुम्हारी आँख नहीं है, तुम्हारे शरीर की आँख है। तुम्हारी आँख अगर एक बार खुल जाय तो सुख ब्रह्माजी को मिलता है, जिसमें भगवान शिव रमण करते हैं, जिसमें आदि नारायण भगवान विष्णु विश्राम पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित रहकर भगवान श्रीकृष्ण लीला करते हैं, जिसमें ब्रह्मवेत्ता सत्पुरुष मस्त रहते हैं वह परम सुख-स्वरूप आत्मा-परमात्मा तुम्हारा अपना आपा है।
आदमी को अपने उस दिव्य स्वरूप का पता नहीं और कहता रहता हैः 'मैं सब जानता हूँ।'
अरे नादान ! चाहे सारी दुनिया की जानकारी इकट्ठी कर लो लेकिन अपने आपको नहीं जानते तो क्या खाक जानते हो ? आत्मवेत्ता महापुरुषों के पास बैठकर अपने आपको जानने के लिए तत्पर बनो। अपने ज्ञानचक्षु खुलवाओ। तब पता चलेगा कि वास्तव में तुम कौन हो। तभी तुम्हारे लिए भवनिधि तरना संभव होगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
५. ढाई
अक्षर प्रेम
का......
एक बार चैतन्य महाप्रभु को विद्वानों ने घेर लिया। पूछने लगेः
"आप न्यायशास्त्र के बड़े विद्वान हो, वेदान्त के अच्छे ज्ञाता हो। हम समझ नहीं पाते कि इतने बड़े भारी विद्वान होने पर भी आप 'हरि बोल.... हरि बोल....' करके सड़कों पर नाचते हो, बालकों जैसी चेष्टा करते हो, हँसते हो, खेलते हो, कूदते हो !"
चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दियाः "बड़ा भारी विद्वान होकर मुझे बड़ा भारी अहं हो गया था। बड़ा धनवान होने का भी अहं है और बड़ा विद्वान होने का भी अहं है। यह अहं ईश्वर से दूर रखता है। इस अहं को मिटाने के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ......मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है सो तू है और तेरा है। ऐसा स्मरण करते-करते, हरि को प्यार करते-करते मैं जब नाचता हूँ, कीर्तन करता हूँ तो मेरा 'मैं' खो जाता है और उसका ‘मैं’ हो जाता है। ‘मैं’ जब उसका होता है तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्द होता है और मैं जब देहाध्यास का होता है तो अशुद्ध और भयभीत रहता है।"
हरिकीर्तन करते-करते गौरांग कभी-कभी इतने मस्त हो जाते कि उनकी निगाह जिन पर पड़ती वे लोग भी मस्ती में आ जाते थे। बालवत् जीवन था उनका, आनन्द में रहते थे, मस्ती लूटते थे। विद्वान लोग बाल की खाल उतारने में व्यस्त रहते थे, शास्त्रों के सिद्धान्त रटकर खोपड़ी में भर लेते थेः 'ब्रह्म ऐसा है, माया ऐसी है, अविद्या ऐसी है... भगवान गोलोकवासी हैं, साकेत-धामवासी हैं....' अरे भाई ! ब्रह्म का अनुभव करने के लिए सत्त्वगुण चाहिए, अंतःकरण की सरलता चाहिए, इन्द्रियों का संयम चाहिए। संयम, सरलता और सत्त्वगुण के बिना कोरे विद्वान हो गये, अंतःकरण से, देहाध्यास से तादात्म्य तोड़ा नहीं तो क्या लाभ ? कबीर जी ने कहाः
पोथी
पढ़ पढ़ जग
मूंआ पंडित
भया न कोई।
ढाई
अक्षर प्रेम
का पढ़े सो
पंडित होई।।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
६. सफलता की
नींव एकाग्रता
गुजरात के भूतपूर्व गवर्नर श्रीमन्नारायण विज्ञान जगत के बड़े सुप्रसिद्ध जाने माने वैज्ञानिक आइन्सटाइन से मिलने गये। बातों के सिलसिले में श्रीमन्नारायण ने आइन्सटाइन से उनकी इतनी बढ़िया सुविकसित योग्यता का कारण पूछा। जवाब में आइन्स्टाइन उनका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गये। वहाँ कोई सुन्दर महँगा राचरचीला नहीं था, सोफासेट आदि राजसी ठाठ नहीं था। आडम्बर की कोई चीजें नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली, साफ-सुथरा था। वहाँ केवल एक चित्र और आसन था।
लोग अपने कमरे को फर्नीचर से ऐसा भर देते हैं कि मानो कोई गोदाम हो। चलने-फिरने की भी जगह नहीं बचती। किसी के घर का कचरा देख आते हैं तो अपने घर में भी ले आते हैं। कुर्सियाँ, टेबल, सोफासेट, टिपोय, डाइनिंग टेबल, तिजोरी.... न जाने क्या क्या रख देते हैं। सुख के लिए घर को गोदाम बना देते हैं लेकिन वे ही सुख के साधन दुःख रूप हो जाते हैं। उन्हीं साधनों की साफ-सफाई में लगे रहते हैं। दिल साफ करने के लिए जीवन मिला था, वह फर्नीचर साफ करने में पूरा हो जाता है।
आइन्स्टाइन ने श्रीमन्नारायण को अपने खाली कमरे में आसन और चित्र दिखाते हुए कहाः
"मेरी शक्तियों का, सफलता का और प्रसिद्धि का कारण यह है। मैं रोज यहाँ बैठकर एकाग्रचित्त होता हूँ, ध्यान करता हूँ।"
शांत एकांत स्थान में, विद्युत का अवाहक हो ऐसा आसन (हो सके तो गरम आसन) बिछाकर बैठो। आँख की पलकें न गिरे इस प्रकार किसी भी चित्र के तरफ एकटक निहारो। आँखों से पानी गिरे तो गिरने दो। कुछ दिनों के अभ्यास से एकाग्रता आयेगी। आपके शरीर में एक प्रकार का आभामण्डल बनेगा। इन्द्रियाँ और मन संयत होंगे। वात और कफ का प्रभाव कम होगा। तन से दोष दूर होंगे।
दुनियाभर के इलाज और औषधियाँ करते रहो लेकिन एकाग्रता और संयम का पाठ नहीं पढ़ा तो सफल नहीं होगे। इलाज करने वाले डॉक्टर खुद बीमार रहते हैं बेचारे।
घर छोड़ने से पहले मेरे तन में बहुत सारी बीमारियाँ थीं। पेट की तकलीफें थी, अपेन्डीक्स था, कई बार एक्स-रे फोटो निकलवाये, ब्लड चेक करवाया, शुगर चेक करवाई, डॉक्टरों के वहाँ चक्कर काटे, न जाने क्या-क्या किया। जब मुझे सदगुरु मिल गये और साधना-मार्ग पा लिया तब तन के सारे दुःख दर्द गायब हो गये। फिर आपने 28 साल में आज तक कभी नहीं सुना होगा कि आज बापू बीमार हैं।
जीवन जीने का थोड़ा-सा ढंग आ जाय तो आदमी अपने आपका वैद्य हो जाता है। अन्यथा तो बाहर के हकीम, वैद्य, डॉक्टरों के वहाँ चक्कर काटता ही रहता है। सलाह उनकी होती है और जेब अपनी होती है, दवाइयाँ डालने के लिए पेट अपना होता है।
मैं यह चाहता हूँ कि मेरे साधक हकीम के यार न बने।
मेरे गुरुदेव कहा करते थेः
हकीम
का यार सदा
बीमार।
गाँधी जी कहा करते थेः "वकील और डॉक्टर हमारे देश में भले रहें, हम मना नहीं करते। लेकिन हे भगवान ! वे लोग मेरे गाँव से तो सत्रह कोस दूर होने चाहिए।"
वकील बढ़ेंगे और डॉक्टर बढ़ेंगे तो बीमारियाँ बढ़ेगी। डॉक्टर लोग भी क्या करें बेचारे ! हम लोग असंयमी होते हैं तो बीमारियाँ हो जाती हैं। बड़े में बड़ा संयम आंतर चेतना से प्राप्त होता है। एकाग्रता के द्वारा आंतर चेतना को जगाना चाहिए।
श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने कहा कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है इन्द्रियों ओर मन का संयम।
ऋषि ने कहाः
तपःषु
सर्वेषु
एकाग्रता
परंतपः।
श्री कृष्ण ने कहाः
तपस्विभ्योऽधिको
योगी
ज्ञानिभ्योऽपि
मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्चाधिको
योगी
तस्माद्योगी
भवार्जुन ।।
'योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है इससे हे अर्जुन ! तू योगी हो।'
(गीताः
६-४६)
जो योग नहीं करता वह वियोगी होता है। वियोगी सदा दुःखी रहता है।
'योग' शब्द बड़ा व्यापक है। आयुर्वेद में दो औषधियों के मेल को 'योग' कहा। संस्कृत के व्याकरण ने दो शब्दों की संधि को 'योग' कहा। पतंजली महाराज ने चित्त की वृत्ति का निरोध करने को 'योग' कहा। श्रीकृष्ण का योग अनूठा है। वे कहते हैं-
समत्वं
योग उच्यते।
जिसके जीवन में समता के दो क्षण आ जाय तो उसके आगे पचास वर्ष की तपश्चर्यावाला तपस्वी भी नन्हा मुन्ना लगेगा। चित्त की समता लाने के लिए एकाग्रता बड़ी सहाय करती है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
७. 'गुरुत्यागात्
भवेन्मृत्युः.....'
राजसी और तामसी भक्तों को देखकर सात्त्विक भक्त कभी कभी हिल जाते हैं। किसी को भी देखकर भक्त को अपने मार्ग से डगमग नहीं होना चाहिए।
समर्थ रामदास के इर्दगिर्द राजसी और भोजन-भगत बहुत हो गये थे। तुकारामजी की भक्त मण्डली सादगी युक्त थी। तुकारामजी कहीं भी भजन-कीर्तन करने जाते तो कीर्तन करानेवाले गृहस्थ का सीरा-पूड़ी, मालमलिदा आदि नहीं लेते थे। सादी-सूदी रोटी, तंदूर की भाजी और छाछ। पैदल चलकर जाते। घोड़ागाडी, ताँगा आदि का उपयोग नहीं करते। तितिक्षु तपस्वी का जीवन था।
तुकारामजी की शिष्य-मण्डली का एक शिष्य देखता है कि समर्थ रामदास की मण्डली में जो लोग जाते हैं वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सीरा-पूड़ी खाते हैं, माल-मलिदा खाते हैं। कुछ भी हो, समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु हैं, राजगुरु हैं। उनके खाने-पीने का, अमन-चमन का, खूब मौज है। उनके शिष्यों को समाज में मान भी मिलता है। हमारे गुरु तुकारामजी महाराज के पास कुछ नहीं है। मखमल के गद्दी-तकिये नहीं, खाने-पहनने की ठीक व्यवस्था नहीं। यहाँ रहकर क्या करें ?
ऐसा शिकायतवाला चिन्तन करते-करते उस शिष्य को समर्थ रामदास की मण्डली में जाने का आकर्षण हुआ। पहुँचा समर्थ के पास। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीः
"महाराज ! आप मुझे अपना शिष्य बनायें। आपकी मण्डली में रहूँगा, भजन-कीर्तन आदि करूँगा। आपकी सेवा में रहूँगा।"
समर्थ जी ने पूछाः "तू पहले कहाँ रहा था ?"
"तुकारामजी महाराज के वहाँ।" शिष्य बोला।
"तुकारामजी महाराज से तूने मंत्र लिया है तो मैं तुझे कैसे मंत्र दूँ ? अगर मेरा शिष्य बनना है, मेरा मंत्र लेना है तो तुकारामजी को मंत्र और माला वापस दे आ। पहले गुरुमंत्र का त्याग कर तो मैं तेरा गुरु बनूँ।"
समर्थजी ने उसको सत्य समझाने के लिए वापस भेज दिया। चेला तो खुश हो गया कि मैं अभी तुकारामजी का त्याग करके आता हूँ।
गुरुभक्तियोग के शास्त्र में आता है कि एक बार गुरु कर लेने के बाद गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु का त्याग करने से तो यह अच्छा है कि शिष्य पहले से ही गुरु न करे और संसार में सड़ता रहे, भवाटवी में भटकता रहे। एक बार गुरु करके उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर भी गुरुगीता में कहते हैं-
गुरुत्यागात्
भवेन्मृत्युः
मंत्रत्यागात्
दरिद्रता।
गुरुमंत्रपरित्यागी
रौरवं नरकं
व्रजेत्।।
‘गुरू का
त्याग करने से
मृत्यु होती
हैं। मंत्र का
त्याग करने
करने से दरिद्रता
आती हैं। गुरु
एवं मंत्र का
त्याग करने से
रौरव नरक मिलता
हैं।’
तुकाराम जैसे सदगुरु, जिनको सत्य में प्रीति है, जो आत्म-साक्षात्कारी महापुरुष हैं, जिनका हृदय वैकुण्ठ है ऐसे सदगुरु का त्याग करने की कुबुद्धि आयी ?
समर्थजी ने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया।
चेला खुश होता हुआ तुकारामजी के पास पहुँचाः
"महाराज ! मुझे आपका शिष्य अब नहीं रहना है।"
तुकारामजी ने कहाः "मैंने तुझे शिष्य बनाने के लिए खत लिखकर बुलाया ही कहाँ था ? तू ही अपने आप आकर शिष्य बना था, भाई ! कण्ठी मैंने कहाँ पहनाई है ? तूने ही अपने हाथ से बाँधी है। मेरे गुरुदेव ने जो मंत्र मुझे दिया था वह तुझे बता दिया। उसमें मेरा कुछ नहीं है।"
"फिर भी महाराज ! मुझे यह कण्ठी नहीं चाहिए।"
"नहीं चाहिए तो तोड़ दो।"
चेले ने खींचकर कण्ठी तोड़ दी।
"अब आपका मंत्र ?"
"वह तो मेरे गुरुदेव आपाजी चैतन्य का प्रसाद है। उसमें मेरा कुछ नहीं है।"
"महाराज ! मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे तो दूसरा गुरु करना है।"
"अच्छा, तो मंत्र त्याग दे।"
"कैसे त्यागूँ ?"
"मंत्र बोलकर पत्थर पर थूक दे। मंत्र का त्याग हो जायगा।"
उस अभागे ने गुरुमंत्र का त्याग करने के लिए मंत्र बोलकर पत्थर पर थूक दिया। तब अजीब-सी घटना घटी। पत्थर पर थूकते ही वह मंत्र उस पत्थर पर अंकित हो गया।
वह गया समर्थ जी के पास। बोलाः "महाराज ! मैं मंत्र और कण्ठी वापस दे आया हूँ। अब मुझे अपना शिष्य बनाओ।"
"मंत्र का त्याग किया उस समय क्या हुआ था ?"
"वह मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया था।"
"ऐसे गुरुदेव का त्याग करके आया जिनका मंत्र पत्थर पर अंकित हो जाता है ? पत्थर जैसे पत्थर पर मंत्र का प्रभाव पड़ा लेकिन तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कमबख्त मेरे पास क्या लेने आया है ? पत्थर से भी गया बीता है तो इधर तू क्या करेगा ? लड्डू खाने के लिए आया है ?"
"महाराज ! वहाँ गुरु का त्याग किया और यहाँ आपने मुझे लटकता रखा ?"
"तेरे जैसे लटकते ही रहते हैं। अब जा, घंटी बजाता रह। अगले जन्म में बैल बन जाना, गधा बन जाना, घोड़ा बन जाना।"
गुरु का दिया हुआ मंत्र त्यागने से आदमी दरिद्र हो जाता है। गुरु को त्यागने से आदमी हृदय का अन्धा हो जाता है। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार तुम दस वर्ष तक चलो, आनन्दित हो जाओ, फिर अगर गुरु में सन्देह करो या गुरुनिन्दा में लग जाओ तो वापस वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से शुरु हुए थे। दस साल की कमाई का नाश हो जाएगा।
समर्थ जी सुना दियाः "तेरे जैसे गुरुद्रोही को मैं शिष्य बनाऊँगा ? जा भाई, जा। अपना रास्ता नाप।"
वह तो रामदासजी के समझ कान पकड़कर उठ-बैठ करने लगा, नाक रगड़ने लगा। रोते-रोते प्रार्थना करने लगा। तब करुणामूर्ति स्वामी रामदास ने कहाः
"तुकारामजी उदार आत्मा हैं। वहाँ जा। मेरी ओर से प्रार्थना करना। कहना कि समर्थ ने प्रणाम कहे हैं। अपनी गलती की क्षमा माँगना।"
शिष्य अपने गुरु के पास वापस लौटा। तुकारामजी समझ गये कि समर्थ का भेजा हुआ है तो मैं इन्कार कैसे करूँ ? बोलेः
"अच्छा भाई ! तू आया था, कण्ठी लिया था। हमने दी, तूने छोड़ी। फिर लेने आया है तो फिर दे देते हैं। समर्थ ने भेजा है तो चलो ठीक है। समर्थ की जय हो !"
संत उदारात्मा होते हैं। ऐसे भटके हुए शिष्यों को थोड़ा-सा सबक सिखाकर ठिकाने लगा देते हैं।
कभी दो गुरु नहीं हैं, एक ही हैं और शिष्य का पतन होता है तो गुरु समझाते हैं। तब उल्टी खोपड़ी का शिष्य समझता है कि मुझे शिष्य बनाये रखने के लिए गुरु गिड़गिड़ाते हैं। अरे मूर्ख ! वे गिड़गिड़ाते नहीं हैं, तेरा सत्यानाश न हो जाय इसलिए तुझे समझाते हैं।
जिस शिष्य में कुछ सत्त्व होता है वह फिसलते-फिसलते भी बच जाता है। जिसके जीवन में सत्त्व नहीं होता वह कितना भी संसार की चीजों से बचा हुआ दिखे फिर भी उसका कोई बचाव नहीं होता। आखिर में यमदूत उसे घसीट ले जाते हैं। फिर वह बैल बनता है बेचारा, पेड़ बनता है, शूकर, कूकर बनता है। न जाने कितने-कितने धोखे खाता है ! इसलिए कबीरजी ने कहाः
कबीरा
इस संसार में
बहुत से कीने
मीत।
जिन
दिल बाँधा एक
से वे सोये
निश्चिन्त।।
एक परमात्मा से जो दिल बाँध देता है उसका सत्त्वगुण बढ़ता है, उसके जीवन में अंतरात्मा का सुख आता है। वह यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुख सुख-स्वरूप ईश्वर में मिल जाता है। वह तरता है, उसका कुल भी तरता है, उसके पूर्वजों का भी हृदय प्रसन्न बनता है।
तरति
शोकं
आत्मवित्।
वह आत्मवेत्ता होकर संसार के शोक सागर से तर जाता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
८.पुष्प-चयन
मनुष्य यदि अपनी विवेक शक्ति का आदर न करे, उसका सदुपयोग न करके भोगों के सुख को ही अपना जीवन मान ले तो वह पशु-पक्षियों से भी गया-बीता है। क्योंकि पशु-पक्षी आदि तो कर्मफल-भोग के द्वारा पूर्वकृत कर्मों का क्षय करके उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं किन्तु विवेक का आदर न करने वाला मनुष्य तो उलटा अपने को नये कर्मों से जकड़ रहा है, अपने चित्त को और भी अशुद्ध बना रहा है।
अतः साधक को चाहिए कि प्राप्त विवेक का आदर करके उसके द्वारा इस बात को समझे कि यह मनुष्य शरीर उसे किसलिए मिला है, इसका क्या उपयोग है। विचार करने पर मालूम होगा कि यह साधन-धाम है। इसमें प्राणी चित्त शुद्ध करके अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।
मनुष्य जब समुद्र की ओर देखता है तब उसे समुद्र ही समुद्र दिखता है और पीछे की ओर देखता है तो स्थल ही स्थल नजर आता है। इसी प्रकार संसार की ओर देखने से संसार ही संसार दिखेगा और संसार की ओर पीठ कर लेने पर प्रभु ही प्रभु दिखलाई देंगे।
कर्म सीमित होता है इसलिए उसका फल भी कर्म के अनुरूप सीमित ही मिलता है। प्रभु अनन्त हैं, उनकी कृपा भी अनन्त है अतः उनकी कृपा से जो कुछ मिलता है वह भी अनन्त मिलता है। प्रभु की प्राप्ति का साधन भी प्रभु की कृपा से ही मिलता है ऐसा मानकर साधक को अपने साधन में सदभाव रखना चाहिए। साधन में अटल विश्वासपूर्वक सदभाव होने से ही साध्य की प्राप्ति होती है।
जो साधक किसी प्रकार के अभाव में दीन नहीं होता अर्थात् उसकी चाह नहीं करता एवं प्राप्त वस्तु या बल का अभिमान नहीं करता अर्थात् उसे अपना नहीं मानता, सब कुछ अपने प्रभु को मानता है, वह सच्चा भक्त है। चाहरहित होने से ही दीनता मिटती है। जहाँ किसी प्रकार के सुख का उपभोग होता है, वहीं मनुष्य चाह की पूर्ति के सुख में आबद्ध हो जाता है और पुनः नयी चाह उत्पन्न हो जाती है। उसकी दीनता का अन्त नहीं होता। दीनता मिटाने के लिए चाह को मिटाओ।
कामना की निवृत्ति से होनेवाली स्थिति बड़ी उच्च कोटि की है। उस स्थिति में निर्विकल्पता आ जाती है, बुद्धि सम हो जाती है, जितेन्द्रियता प्राप्त हो जाती है। उसके प्राप्त होने पर मनुष्य स्वयं 'कल्पतरू' हो जाता है। जिसको लोग कल्पतरू कहते हैं उससे तो हित और अहित दोनों ही होते हैं। पर यह कल्पतरू तो ऐसा है, जिससे कभी किसी का भी अहित नहीं होता। इससे मनुष्य को योग, बोध और प्रेम प्राप्त होता है।
किसी भी वस्तु को अपना न मानना त्याग है। त्याग से वीतरागता उत्पन्न होती है। राग की निवृत्ति होने पर सब दोष मिट जाते हैं।
कठिनाई या अभाव को हर्षपूर्वक सहन करना तप है। तप से सामर्थ्य मिलता है। इस सामर्थ्य को सेवा में लगा देना चाहिए।
अहंता और ममता का नाश विचार से होता है। सत्य के बोध से समस्त दुःख मिट जाते हैं। सत्य के प्रेम से अनन्त रस, परम आनन्द प्राप्त होता है। अपने को शरीर न मानने से निर्वासना आती है और सदा रहने वाली चिर शांति मिलती है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
भक्तिमति
रानी
रत्नावती
जयपुर के पास आंबेरगढ़ है। वहाँ के राजा का नाम था मानसिंह। मानसिंह का छोटा भाई था माधवसिंह। माधवसिंह की पत्नी रत्नावती। रत्नावती का स्वभाव बड़ा मधुर था। दासियों के साथ भी मधुर व्यवहार करती थी। वह ठीक से समझती थी, मानती थी कि हम जिससे व्यवहार करते हैं वह कोई मशीन नहीं है, मनुष्य है। उसे भी सांत्वना चाहिए, सहानुभूति चाहिए, प्यार चाहिए। अपने मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी से, बढ़िया आचरण से सारे महल में आदरणीय स्थान प्राप्त कर चुकी थी। दासियाँ भी उसके प्रति बड़ा आदर-भाव रखती थीं।
मान देने वाले को मान मिलता है, प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है।
औरों
को शक्कर देता
है वह खुद भी
शक्कर खाता है।
औरों
को डाले चक्कर
में वह खुद भी
चक्कर खाता है।।
इन नियति के मुताबिक, जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों को स्नेह, मान, आदर, प्रेम देता है, दूसरे लोग भी उसका हित चाहते हैं, स्नेह, मान, आदर, प्रेम देते हैं। सब में छुपा हुआ चैतन्य परमात्मा उसका परम हित कर देता है।
रत्नावती का मधुर, उदार, नीतिपूर्ण, सरल और सहानुभूति व्यवहार दास-दासियों के साथ महल के सारे परिवार जनों को सन्तुष्ट रखता था। जिसका व्यवहार अनेकों को संतुष्ट करता है वह स्वयं तुष्टिवान बनता है। उसके चित्त में भगवान का प्रसाद आ जाता है। उसके हृदय में प्रभु भक्ति के अंकुर फूटते हैं।
अद्वेष्टा
सर्वभूतानां
मैत्रः करूण
एव च।
निर्ममो
निरहंकारः
समदुःखसुखः
क्षमी।।
संतुष्टः
सततं योगी यतात्मा
दृढ़निश्चयः।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो
मदभक्तः स मे
प्रियः।।
'जो पुरुष सब भूतों में द्वेषभाव से रहित, स्वार्थरहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख-दुःख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात् अपराध करनेवाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए हैं और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
(गीताः
१२-१३,१४)
एक मध्य रात्रि को रत्नावती ने देखा कि अपनी विशेष कृपापात्र दासी अपने कमरे में बैठी आँसू बहा रही है.... रो रही है। दास-दासियों के सुख-दुःख में सहभागी होने वाली वात्सल्यमयी रत्नावती ने जाकर पूछाः
"बहन ! क्यों रो रही है ? तुझे क्या दुःख है ? क्या तकलीफ, पीड़ा, आपत्ति है ? किसने तुझे सताया है ? पूनम की रात है.... चाँद चमक रहा है.... और तू रो रही है पगली ? मुझे बता मैं तेरा कष्ट दूर कर दूँगी।"
दासी खिलखिलाकर हँस पड़ी। बोलीः
"माता जी ! आपके होते हुए इस राजमहल में मुझे कोई दुःख नहीं है।"
"दुःख नहीं है तो फिर मध्यरात्रि में रो क्यों रही है ?"
"रानी साहिबा ! मैं सच कहती हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है। मै आनन्द में हूँ। मुझे भीतर से जो मधुरता मिल रही है न ! वह कैसे बताऊँ ? मेरी आँखों में तो आनन्द के आँसू हैं। मैं बहुत बहुत खुशी में हूँ।" दासी के मुख पर मधुर मुस्कान उभर आई।
रत्नावती को आश्चर्य हुआः "रो रही है और बोलती है 'मैं आनन्द में हूँ !' आँखों में आँसू और मुख पर मुस्कान एक साथ ! कमाल है !''
संसारियों को हँसने में भी मजा नहीं आता वह मजा भगवान के प्यारों को भगवान के विरह में रोने में आता है। उस आनन्द की तो बात ही निराली है। भोग-विलास, खान-पान और अन्य विषयों से जो मिलता है वह तो हर्ष है, आनन्द नहीं है। भगवान की भक्ति में जो सुख है, जो आनन्द है वह कुछ निराला ही है।
रानी रत्नावती देखकर ठगी-सी रह गई। दासी के बदन पर दिव्य तेज था, ओज था, पवित्र मुस्कान थी, प्रभुभक्ति की मस्ती थी। उसके आँसुओं में कुछ अमृत दिख रहा था। वे शिकायत के आँसू नहीं थे, निराशा के आँसू नहीं थे, हताशा के आँसू नहीं थे। वे ऐसे आँसू थे कि एक-एक आँसू पर विश्वभर के सब मोती न्यौछावर कर दो फिर भी जिसका मूल्य न चुक सके ऐसे दिलबर के लिए आँसू थे, प्रभुप्रेम के आँसू थे, भगवदभक्ति के आँसू थे।
रत्नावती आश्चर्यमुग्ध होकर पूछने लगीः
"इन आँसूओं में तुझे मजा आता है ? आँसूओं को मैं दुःखदायी मानती थी। अरे पगली ! बता तो सही, इतना आनन्द किस बात का है ? तेरे पास कोई भोग-विलास नहीं है, विशेष खान पान नहीं है, फिर भी तेरे भीतर खुशी समाती नहीं। चेहरे पर उभर आती है। क्या बात है?"
दासी ने कहाः "माता जी! ये तो प्रभु प्रेम के आँसू हैं, भगवद् भक्ति की मस्ती है। यह तो परमात्मा का प्रसाद है।"
"अच्छा ! भगवान की भक्ति में इतना मजा आता है ! यह भक्ति कैसे की जाती है ? मुझे बतायेगी ?" रत्नावती की जिज्ञासा अब अंकुरित होने लगी।
अब संयत होकर दासी कहने लगीः
"रानी साहेबा ! आप तो महलों में रहने वाली, रेशमी वस्त्र, रत्नजड़ित सुवर्ण-अलंकार धारण करने वाली, सोने-चाँदी के बर्तनों में भोजन करने वाली महारानी हैं..... राजा साहब की प्रिया हैं। आपको मैं क्या बताऊँ ? मैं तो आपकी सेविका ठहरी।"
"नहीं नहीं, ऐसा मत बोल बहन ! सच्ची और कल्याणकारी बात तो बच्चों से भी ली जाती है। तू संकोच मत कर। मुझे भी तेरे आनन्द में सहभागी होने दे।"
"महारानी ! भगवान की भक्ति करना कोई सहज नहीं है। यह तो शूरों का मार्ग है। सिर का सौदा करके भक्ति का प्रसाद मिल सकता है।" दासी ने अपनी ओजस्वी मुद्रा में कहा।
रानी जानती थी कि अपनी प्रिय दासी पवित्र स्वभाव की है, भक्त है, सत्त्वशील नारी है। प्रातःकाल जल्दी उठकर बिस्तर में सर्वप्रथम परमात्मा का चिन्तन करती है, फिर दिनचर्या का प्रारंभ करती है। दिन में भी बार-बार दीनानाथ का स्मरण करती है। उस दासी के लिए रत्नावती को मान था, स्नेह था। वह उत्कंठित होकर पूछने लगीः
"अभी-अभी तू आँसू बहा रही थी, भाव विभोर भी हो रही थी.... भक्ति में कैसा होता है ? तुझे क्या अनुभव हो रहा था, मुझे बता न !"
"माता जी ! जाने दो, यह बात मत पूछो। भगवान और भक्त के बीच जो घटनाएँ घटती हैं उन्हें भगवान और भक्त ही जानते हैं। रानी साहेबा ! क्षमा करो। मुझे आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा में लग जाऊँ।"
रत्नावती समझ गई की दासी बात टाल रही है। उसने कुछ रहस्यमय अमृत पाया है। उसके बदन पर इतनी मधुरता, इतनी शांति छा गई है तो उसके अंतःकरण में कितनी मधुरता भरी होगी ! रत्नावती की जिज्ञासा पैनी हो उठी। वह फिर से प्रेमपूर्वक दासी को पूछने लगी, रहस्य बताने के लिए मनाने लगीः
"बहन ! मुझे बता, तुझे क्या हुआ है ? तेरी आँखों में आँसू हैं और चेहरे पर दिव्यता दिखाई दे रही है ! तू अभी क्या कर रही थी ? तुझे क्या मिला है ?"
दासी ने हँसते हुए कहाः "माता जी ! मैं कुछ भी नहीं करती थी। मन जो विचार कर रहा था उसे देखती थी। मैं अपने गिरधर गोपाल को स्नेह करती थी, और कुछ नहीं करती थी। 'हे प्रभु ! करण-करावणहार तू ही चैतन्य परमात्मा है।' इस प्रकार अपने हृदयेश्वर के साथ गोष्ठि कर रही थी, भाव-माधुर्य का आस्वाद ले रही थी।"
"सखी, मुझे विस्तारपूर्वक बता।"
दासी भक्ति की गोपनीय बात बताने में हिचकिचाने लगी, बात टालने लगी तो रत्नावती की उत्सुकता और बढ़ गई। इन्कार भी आमंत्रण देता है।
रत्नावती की उत्कंठा बढ़ गई। कैसे भी करके भक्तिमार्ग विषयक रहस्य बताने के लिए दासी को राजी कर लिया। दासी ने अपनी अनुभूतियों का वर्णन किया क्योंकि रानी रत्नावती अधिकारी नारी थी। भगवद् भक्ति के लिए उपयुक्त सदगुण उसमें थे। उसके चित्त में दीन-दुःखी लोगों के लिए सहानुभूति थी, दया-भावना थी। उसके स्वभाव में रानी पद का अहंकार नहीं था। ऐसे सदगुणों के कारण रानी को अधिकारी समझकर दासी ने भगवद् भक्ति के रहस्य उसके आगे प्रकट किये। रानी के चित्त में प्रभुप्रीति की प्राप्ति के लिए तड़प जाग उठी। वह सोचने लगीः
"मैं कहलाती हूँ रानी लेकिन मुझे जो सुख और आनन्द नहीं मिलता वह सुख और आनन्द यह गरीब सी दासी पा रही है। सुख और आनन्द अगर रानीपद में या धन-वैभव में होता तो सब धनवान और सत्तावान स्त्री-पुरुष सुखी और आनन्दित होते। सुख अन्तःकरण की संपत्ति है। अन्तःकरण जितना अंतरतम चैतन्य में प्रविष्ट होता है उतना वह आदमी सुखी रहता है। साधन एक सुविधा मात्र है। सुख उससे निराली चीज है। सुविधा शरीर को मिलती है जबकि सुख अंतःकरण को मिलता है। लोग सुविधा को सुख मानकर अपने को सच्चे सुख से वंचित रख देते हैं।
रानी को अंतःकरण के खजाने खोलने की उत्कंठा जाग उठी। भगवान की भक्ति के लिए चित्त व्याकुल हो उठा। दासी कहने लगीः
"माता जी ! आप रहने दो। यह दुर्गम मार्ग है। इस मार्ग पर चलना कठिन है। लोग टोकेंगे, हैरान करेंगे, मुझे भी कड़ी नज़र से देखेंगे। जीवन जैसे चलता है वैसे ही चलने दो। भक्ति के मार्ग पर प्रारंभ में खूब सहना पड़ता है। हाँ, जब मिलता है तब अमूल्य और शाश्वत खजाना मिलता है। उसके लिए विषय-विलास और अहंपने का मूल्य चुकाना पड़ता है। अहं का मूल्य दिये बिना वह अमूल्य मिलता नहीं है। बीज अपने आपका बलिदान दे देता है तब वृक्ष बन पाता है। सासांरिक मोह-ममता, विषय भोगों का बलिदान देने से परमात्म-प्रीति का द्वार खुलता है। अतः रानी साहेबा ! यह गोतेखोरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर आयेंगी तो महल में मुझे कुछ का कुछ सुनना पड़ेगा।"
रत्नावती ने कहाः "बहन ! तू घबराना मत। आज से तू मेरी गुरु है। तेरा अनुभव सुनकर मुझे नटवर नागर, गिरिधर गोपाल के लिए प्रीति जागी है। धिक्कार है इस विषय-विलास वाले रानी पद को ! हम लोग महलों में रहकर विकारी सुख में जीवन घिस डालते हैं और तू एक झोंपड़ी में भी निर्विकारी नारायण के सुख में जीवन धन्य कर रही है। महल भी सुख का साधन नहीं है और झोंपड़ा भी सुख का साधन नहीं है। सुख का सच्चा साधन तो तुम्हारा वह साध्य परमात्मदेव है।"
रत्नावती को भक्ति का रंग लगा। दासी के सत्संग से उसमें सत्त्वगुण बढ़ा। भक्ति जिसके अंतःकरण में हो, दिल में हो, हृदय में हो वह चाहे दासी के शरीर में हो चाहे दासी के शरीर में हो, जड़भरत जी के शरीर में हो चाहे, शुकदेव जी के शरीर मे हो, उसको हजार-हजार प्रणाम है।
भक्तिमती दासी के सत्संग से रानी सत्संगी बन गई। रेशमी वस्त्राभूषण उतारकर सूती सादे वस्त्र पहन लिये। कण्ठ में चमकती हुई मोतियों की माला उतार कर तुलसी की माला धारण कर ली। हाथ में रत्नजड़ित कंगन और सुवर्ण की अँगूठियाँ शोभा दे रही थीं वे सब उतार दीं।
जब भक्ति शुरु होती है तब भीतर का कल्मष दूर होने लगता है। दूसरे भक्तों का संग अच्छा लगता है। आहार-विहार बदल कर सात्त्विक हो जाता है। सदगुण पनपने लगते हैं। व्यक्ति के चित्त में दिव्य चेतना का प्रभाव और आनन्द विकसित होने लगता है।
रानी के अंतःकरण में रस-स्वरूप परमात्मा का प्रसाद विकसित होने लगा। जहाँ विलासभवन था वहाँ भगवान का लीलाभवन बन गया। भगवान का नामजप, साधन-भजन-कीर्तन, पूजा-पाठ, पुष्प-चंदन, धूप-दीप होने लगे। सारी दिनचर्या भगवान से ओतप्रोत बन गई। उसका बोलना चालना कम हो गया, हास्य-विलास कम हो गया। इन्द्रियों की चंचलता की जो सामग्री थी वह रानी लेती नहीं। आवश्यकता होती उतना ही खाती, आवश्यकता होती उतना ही बोलती। उसकी वाणी में बड़ा आकर्षण आ गया।
जो कम बोलता है, केवल जरूरी होता है उतना ही बोलता है उसकी वाणी में शक्ति आती है। जो व्यर्थ की बड़बड़ाहट करता है, दो लोग मिलें तो बोलने लग जाता है, मण्डली बनाकर बकवास करता रहे वह अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ क्षीण कर देता है। उसकी वाणी का कोई मूल्य नहीं रहता।
रत्नावती की वाणी में संयम का ओज प्रकट हो रहा था।
स्त्री में यह गुण है। एक बार अगर भक्ति को, ज्ञान को, सेवा को ठीक से पकड़ लेती है तो फिर जल्दी से छोड़ती नहीं। पुरुष छोड़ देता है। स्त्री नहीं छोड़ती। मीरा ने श्रीकृष्ण की भक्ति पकड़ ली तो पकड़ ली। शबरी ने मतंग ऋषि के चरणों में अपना जीवन सेवा और साधनामय कर लिया।
स्त्री में ऐसे गुण भी होते हैं। भय, कपट, अपवित्रता आदि दुर्गुण पुरुष की अपेक्षा स्त्री शरीर में विशेष रूप से रहते हैं तो श्रद्धा, समर्पण, सेवा आदि सदगुण, सेवा आदि सदगुण भी पुरुष की अपेक्षा विशेष रूप से रहते हैं।
रत्नावती ने अपने सदगुण बढ़ाये तो दुर्गुण क्षीण हो गये।
भक्ति
करे कोई सूरमा
जाति वरण कुल
खोय।
भक्ति का मार्ग ऐसा है कि एक बार थोड़ा-सा किसी को मिल जाता है। उसका रंग-ढंग ही बदल जाता है। एक बार उस गिरिधर गोपाल की, माधुर्यदाता की मधुरता की थोड़ी सी ही झलक मिल जाय फिर यह जगत फीका पड़ जाता है। षडरस सब फीके पड़ जाते हैं। अंतर का रस ही ऐसा है।
रत्नावती ने भोग विलास के भवन को हरिभक्ति का भवन बना दिया। वह कभी नाचती है तो कभी भक्ति रस के पद गाती-आलापती है, कभी आरती करती है, कभी मौन धारण करती है।
चित्त में एक सदगुण आता है तो दूसरों को वह खींच ले आता है। जंजीर की एक कड़ी हाथ में आ गई तो व्यक्ति पूरी जंजीर को खींच सकता है।
रत्नावती की पुण्याई बढ़ी तो उसे रामायण की चोपाई चरितार्थ करने की उत्कंठा अपने आप जागी।
प्रथम
भक्ति संतन कर
संगा.....।
उसने दासी से कहाः "हे दासी ! तू तो मेरे लिए संत है ही। और संत भी गाँव में आये हैं। सावन का महीना है। अगर यह रानीपद का खूँटा न होता तो मैं तेरे साथ आती।"
फिर सोचते-सोचते रत्नावती को विचार आया किः "मैं रानी हूँ तो मुझमें क्या रानी है ? मेरा हाथ रानी है कि पैर रानी है ? मेरा मुँह रानी है कि मस्तक रानी है ? यह रानीपद कहाँ घुसा है ?' दासी को अपना विचारविमर्श बताने पर दासी ने कहाः
"रानी जी ! यह तो सुन-सुनकर पक्का किया है, वास्तव में रानीपद है ही नहीं।"
"तब तो मैंने इस रानीपद को छोड़ा।" रत्नावती कहने लगीः "चलो, हम संत-दर्शन को चलें।"
प्रथम तो दासी घबड़ायी, फिर सहमत होकर रानी के साथ संतों की मण्डली मे गई।
उस जमाने में रानी साधू-मण्डली में जाय तो हो गया पूरा। सब उंगली उठाने लगे। सारे गाँव में बात फैल गई।
अरे भैया ! कथा में तो तू भगवान का है और भगवान तेरे हैं। अपने पद और प्रतिष्ठा को छोड़ दे।
लोग कहने लगेः "रानी साहेबा ! घर चलो। आप यहाँ कैसे आये..... क्यों आये....?" आदि आदि।
रानी को हुआ कि यह कौन से पाप का फल है कि कथा सुनने में भी मुझे तकलीफ पड़ रही है ? ये पद-प्रतिष्ठा तो कथा सुनने की जगह पर बैठने भी नहीं देते।
भक्ति
करे कोई सूरमा
जाति वरण कुल
खोय।
कामी
क्रोधी लालची
उनसे भक्ति न
होय।।
काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को छोड़ने की हिम्मत हो उसी की भक्तिरूपी बेलि बढ़ती है।
रत्नावती ऐसी निडर थी। उसने हिम्मत की, सच्चे हृदय से प्रार्थना की किः "हे प्रभु ! मैं तो तेरी हूँ। रानीपद को आग लगे। मुझे तो तेरी भक्ति देना। मैं रानी नहीं, तेरी भगतनी बन जाऊँ ऐसा करना।"
पवित्र स्थान में किया हुआ संकल्प जल्दी फलता है। जहाँ सत्संग होता हो, हरिचर्चा होती हो, हरिकीर्तन होता हो वहाँ अगर शुभ संकल्प किया जाय तो जल्दी सिद्ध होता है। अपने पाप का प्रायश्चित करके दुबारा वह पाप नहीं करने का निश्चय किया जाय तो जल्दी निष्पाप हुआ जाता है।
रानी की मनोकामना फली। उसने ऐसा निश्चय किया कि अब मैं ऐसी रहूँगी कि लोग मुझे देखें तो उन्हें 'रानी आयी' ऐसा नहीं अपितु 'भगताणी आयी' ऐसा महसूस हो।
बार-बार सत्संग करने से भक्ति पुष्ट होती है। साधन-भजन से सत्संग में रूचि होती है। सत्संग करने से साधन में रूचि होती है। जैसे मेघ सरोवर को पुष्ट करता है और सरोवर मेघ को पुष्ट करता है वैसे ही सत्संग साधन को पोसता है और साधन सत्संग को पोसता है।
रत्नावती की साधना बढ़ी। उन दिनों राजा माधवसिंह दिल्ली में था। रत्नावती के भक्ति भाव की बात गाँव में फैली तब वजीर ने चिट्ठी लिखी की रत्नावती को भक्ति का रंग लगा है। राजमहल छोड़कर मोड़ों के (साधुओं के) संग मे घण्टों तक बैठी रहती है। अब आपकी जो आज्ञा।
माधवसिंह लालपीला हो गयाः 'मेरी पत्नी राजमहल छोड़कर मोड़ों की मण्डली में !' उसका हाथ तलवार पर गया। पास में उसका लड़का खड़ा था प्रेमसिंह। उसने कहाः
"पिता जी ! आप क्रोध मत करो।"
प्रेमसिंह पूर्वजन्म का कोई सत्पात्र होगा। माँ की भक्ति का रंग लगा तो उसने भी गले में तुलसी की माला पहन ली थी। पुत्र के गले में तुलसी की माला और ललाट पर तिलक देखकर माधवसिंह का गुस्सा और भड़का। उसने जोर से डाँटाः
"जा मोड़ी का ! मेरे सामने क्यों आया ?"
प्रेमसिंह कहता हैः "पिताजी ! आप धन्य हैं कि मेरी माता को मोड़ी कह दिया। मैं भी अब मोड़ी का बेटा होकर दिखाऊँगा।"
पिता के क्रोध का भी उसने अच्छा ही अर्थ निकाला। माँ को पत्र लिखा किः
"माँ ! तू धन्य है। तेरी कोख से मैंने जन्म लिया है। मेरे पिता को तेरी भक्ति का समाचार मिला तो कोपायमान हुए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे प्रति अच्छे भाववाली बात करते जानकर मुझे तो वरदान ही दे दिया है, 'चला जा मोड़ी का ! तू भी मोड़ा हो जा, साधुड़ी का साधू हो जा। मैंने तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य की है। मेरी माँ साध्वी बने और मैं साधू बनूँ तभी मेरे पिता के वचन का पलन होगा। तो माता ! मैं तेरी कोख से जन्मा हूँ। मेरे पिता का वचन खाली न जाय।"
प्रेमसिंह ने दिल्ली में माँ को ऐसा पत्र लिख दिया। माँ को बड़ा आनन्द हुआ कि, 'वाह ! मेरा पुत्र साधू होता है ! धन्य है !'
अब भक्तिमती रत्नावती भी रानीपने के थोड़े बहुत जो भी चिन्ह थे उन्हें छोड़कर एकदम सादे वस्त्र से युक्त होकर पवित्र, तेजस्वी, पुण्यशीला साध्वी बन गई।
आप कैसे वस्त्र पहनते हो उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। कैसी पुस्तक पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कमरे में कैसा फर्नीचर और कैसे चित्र रखे हैं उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता है। आपके विचारों के अनुरूप सूक्ष्म परमाणु आपकी ओर प्रवाहित होते हैं। क्रोधी को क्रोधाग्नि बढ़े ऐसे परमाणु मिलते हैं। अशांत को अशांति बढ़े, संशयात्मा का संशय बढ़े, प्रेमी का प्रेम बढ़े और भक्त की भक्ति बढ़े ऐसे ही परमाणु और माहौल मिल जाता है।
नारायण.... नारायण.... नारायण.... नारायण..... नारायण.....।
बाई रत्नावती को पक्का रंग लग गया। उसने भगवान के आगे संकल्प किया कि, "मेरे बेटे को 'मोड़ी का बेटा' कहा है तो मैं भी सच्ची भक्तानी होकर रहूँगी। वाह मेरे प्रभु ! मैंने तो केवल मेरे लिए ही भक्ति माँगी थी। तूने तो माँ और बेटे, दोनों को उसके पिता से वरदान दिला दिया। वाह मेरे प्रभु !
ये मेरे कोई नहीं थे। आज तक मैं मानती थी कि मेरा पति है, मेरा देवर है लेकिन वे अपनी वासनाओं के गुलाम हैं। वे मुझे प्यार नहीं करते थे, अपनी इच्छा-वासनाओं को प्यार करते थे, अब मुझे पता चला। मुझे तो हे विश्वनाथ ! तू ही प्यार करता है अमर बनाने के लिए।"
पति और पत्नी का सम्बन्ध वास्तव में वासना की कच्ची दीवार पर आधारित है। सेठ और नौकर का सम्बन्ध लोभ और धन की दीवार पर आधारित है। मित्र-मित्र का सम्बन्ध भी प्रायः ऐसा ही होता है। कोई कोई मित्र हो उनकी बात अलग है। संसार के जो-जो सम्बन्ध हैं वे दूसरों से अपना उल्लू सीधा करने के लिए हैं।
भक्त और संत का सम्बन्ध, गुरु और शिष्य का सम्बन्ध ईश्वर के नाते होता है। इसलिए यह शुद्ध सम्बन्ध है, बाकी के सारे सम्बन्ध स्वार्थमूलक हैं।
भगत और जगत का कब बना है ? भगत-जगत का विरोध सदा से चलता आ रहा है। स्त्री को रंग लग जाता है तो पुरुष नाराज हो जाता है। पुरुष को रंग लग जाता है तो स्त्री शिकायत करती है।
तुकाराम का एक कठोर निन्दक शिवोबा निन्दा करते-करते तुकाराम के अधिक संपर्क में आया तो उसको रंग लग गया, वह भक्त बन गया।
कई लोगों को रंग लगता है लेकिन पुण्यों में कमी होती है तो वे निन्दक बन जाते हैं। कभी निन्दक भी बदलकर साधक बन जाता है। ऐसा होता रहता है। इसी का नाम संसार है। मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है।
शिवोबा तुकारामजी का साधक बन गया तो उसकी पत्नी को लगा कि मेरे पति को इस महाराज ने भगत बना दिया, मैं महाराज को देख लूँगी। उसने उबलता हुआ पानी तुकारामजी की पीठ पर ढोल दिया।
पति को भक्ति का रंग लगता है तो पत्नी का चित्त उबलता है, पत्नी को रंग लगता है तो पति का चित्त उबलता है। दोनों को रंग लगता है तो दूसरे कुटुम्बी नाराज होते हैं। सारे कुटुम्ब को रंग लगता है तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं कि सारा भगतड़ा हो गया है।
जिनको रजो-तमोगुण और विकारों को पोसकर जीना है और जिनको ईश्वरीय मस्ती में जीना है, सत्त्वगुणी होकर जीना है उन दोनों की दिशाएँ अलग हो जाती हैं। जैसे, प्रह्लाद और हिरण्यकशिपु, मीरा और विक्रम राणा।
भक्ति के मार्ग पर आदमी चलता है तो कभी-कभी तामसी तत्त्व वाले लोग विरोध करते हैं लेकिन भक्त उस विरोध के कारण भक्ति छोड़ नहीं देता है।
रानी रत्नावती भी संत-चरित्र सुन-सुनकर पुष्ट हो गई थी। अपने मार्ग पर अडिगता से आगे बढ़ रही थी।
माधवसिंह उसी समय वहाँ से चला आँबेरगढ़ के लिए। अपने नगर में आया तब शराबी-कबाबियों ने रत्नावती के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर सुनाया। क्रोधी को क्रोध बढ़ानेवाला सामान मिल गया। उन्हीं लोगों और मंत्रियों से विचार-विमर्श किया कि रानी को मृत्युदण्ड दिया जाय। मंत्रियों ने कहाः
"अपनी ही रानी को आप मृत्युदण्ड देंगे तो कुल पर कलंक लगेगा और राज्य में रोष फैलेगा।"
राजा ने कहाः "दूसरा कोई उपाय खोजो। अब उसका मुँह नहीं देखना है। खुद भी बिगड़ी, लड़के को भी बिगाड़ा।"
बिगड़े हुए लोगों को भगवान के भक्त बिगड़े हुए दिखते हैं। वास्तव में वे भक्त ही सुधरते हैं।
सुनो
मेरे भाईयों !
सुनो मेरे
मितवा !
कबीरो
बिगड़ गयो रे...
काशी में और कोई दारू नहीं पीता होगा ? बस, केवल कबीर ही मिल गये दारू पीनेवाले ? कबीर मांस खाते हैं..... कबीर वेश्या के पास जाते हैं.....' कबीर तो कभी गये भी नहीं होंगे मगर बिगड़े हुए लोग भक्तों को ऐसे परेशान करते हैं, क्योंकि परापूर्व से कुदरत का ऐसा नियम है। भक्त की भक्ति मजबूत करनी हो तो ऐसा कुछ चाहिए।
सबने मिलकर षडयंत्र रच दियाः "भूखे शेर को पिंजरे में बन्द करके पिंजरा मोड़ी के महल के द्वार पर रखकर दरवाजा खोल देंगे। भूखा शेर मनुष्य की गन्ध आते ही मोड़ी का शिकार कर लेगा। हमारा काँटा दूर हो जाएगा। नगर में जाहिर कर देंगे कि नौकरों की असावधानी से शेर खुल गया और दुर्घटना में रानी खप गई। हम पर कलंक नहीं लगेगा।'
कलंकित व्यक्ति कितना भी बचना चाहे पर कलंक लगे लगे और लगे ही।
परमात्मा परम दयालु हैं। भक्त की लाज रखने में, अभक्त को जरा चमत्कार दिखाने में भगवान पीछे नहीं रहते।
शाम का समय था। पिंजरा लाया गया। पिंजरे का दरवाजा खुला कि शेर गर्जना करता हुआ रानी रत्नावती के कमरे की ओर गया। भक्तिमति रत्नावती प्रभु-मंदिर में ठाकुरजी की मूर्ति के सामने भावविभोर बैठी थी। ध्यान-मग्न जैसी दशा.... आँखों में से हर्ष के अश्रू बह रहे हैं। दासी ने शेर को देखा तो चिल्ला उठीः
"माता जी ! शेर आया.... शेर....!!"
रत्नावती ने सुना, देखा, उदगार निकलाः
"नहीं नहीं..... ये तो नृसिंह भगवान हैं।" रानी पूजा की थाली लेकर शेर के सामने गई।
'जले विष्णुः स्थले विष्णुः......' शेर के अंतर में भी वही चैतन्य आत्मा है। रानी को वह सिंह नृसिंह के रूप मे दिखा। उसका पूजन किया। राजा के षडयंत्रबाज नौकर लोग देखते रहे कि यह भूखा शेर चुपचाप खड़ा है ! ....और उसकी पूजा !
उनको शेर दिखता है और रानी को परमात्मा। दृष्टिरेव सृष्टिः। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
दासी देख रही है और रत्नावती भावपूर्वक शेर का पूजन कर रही हैः
"भगवान ! प्रह्लाद के आगे आप नृसिंह के रूप में आये थे। आज मेरे आगे सिंह के रूप में आये हो ! मेरे गिरधर ! मेरे चैतन्य ! आज यह देश लेकर आये ? आप तो प्राणीमात्र के आधार हो। हे सर्वाधार ! आप सिंह बने हो ?"
ऐसा कहते हुए रत्नावती प्रणाम करती है, मन-ही-मन भाव समाधि का आस्वादन लेती है। वह बिल्कुल शांत हो गई है।
बाहर लोगों ने सोचा, रत्नावती को शेर खा गया। शेर ने रत्नावती को तो खाया नहीं लेकिन रत्नावती के देहाध्यास को उस देहातीत तत्त्व ने अपने चरणों में समा लिया।
जाको
राखे साँईयाँ
मार न सके
कोई।
बाल
न बाँका कर
सके चाहे जग
वैरी होय।।
जिसमें सत्त्वगुण बढ़ता है, भाव की दृढ़ता बढ़ती है उसके लिए शत्रु कितना भी आयोजन कर ले, अगर उसका प्रारब्ध शेष है तो कोई उसे मार नहीं सकता। यदि प्रारब्ध शेष नहीं है तो सब मिलकर जला भी नहीं सकते भैया ! अतः भगवान का भक्त इन तत्त्वों से डरता नहीं, अपनी भक्ति छोड़ता नहीं।
शेर अब वहाँ से लौटा और जो दूर से देख रहे थे उनको स्वधाम पहुँचा दिया। किसी का नास्ता किया, किसी को ऐसे ही सीधा यमपुरी पहुँचाया। सबको ठीक करके शेर वापस पिंजरे में घुस गया।
माधवसिंह महल की अटारी से यह सब देख रहा था। उसको लगा कि भगवान के प्रभाव के बिना यह नहीं हो सकता। शेर कमरे में जाय और रानी उसकी आरती उतारे, शेर सिर झुकाकर वापस आवे और नौकरों को खा जाय.... यह चमत्कार है। वास्तव में मैंने रानी को समझने में भूल की है। ऐसी रानी कभी गुस्से में आकर मुझे कुछ कह देगी तो मेरा क्या होगा ? राज्य का क्या होगा ?
भोगी को चारों ओर से भय के विचार घेरे ही रहते हैं। आपने कई बार कथाएँ सुनी होगी कि किसी मुनि ने तपस्या की और इन्द्र का आसन हिला। जब-जब हिलता है तब-तब इन्द्र का आसन ही हिलता है, कभी भी यमराज का आसन पाडा हिला हो ऐसा सुना ? कभी नहीं। वास्तव में तो यमराज का पाडा हिलना चाहिए। मगर जब हिला है तब इन्द्र का आसन ही हिला है। जहाँ भोगवृत्ति हो, लगाव हो उसका ही दिल हिलता है। जहाँ त्याग हो, अनुशासन हो वहाँ क्या हिलेगा ? आज तक मैंने यह नहीं सुना कि किसी तपस्वी मुनि ने तपस्या की और यमराज का पाडा हिला। यह तो सुना है कि विश्वामित्र ने तप किया, नर-नारायण ने तप किया और इन्द्र का आसन हिला। आपने भी सुना होगा।
राजा घबड़ाया। पुण्यशील सुशील व्यक्ति का दर्शन करने से भी अंतर में, आँखों में पवित्रता आती है। माधवसिंह को लगा कि मैंने रानी के साथ अन्याय किया है। वह रानी के महल में गया और आदरपूर्वक रानी को प्रणाम करने लगाः
"हे देवी ! मुझे क्षमा करो।"
रानी तो भाव-समाधि में निमग्न थी। दासी ने कहाः "रत्नावती माँ ! राजा साहब प्रणाम कर रहे हैं।"
रानी ने कहाः "मुझे प्रणाम नहीं करते, वे तो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं।"
माधवसिंह की दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल जाय तो सृष्टि सुखमय हो जाय। रानी तो वही की वही थी। उसको द्वेषबुद्धि से देखकर राजा का खून गरम हो गया था। अब भक्तिबुद्धि से देखकर राजा के हृदय में भक्ति बढ़ी।
भक्त तो वही का वही होता है। कोई उसमें दोषबुद्धि करे तो वह पाप का भागी होता है और आदरबुद्धि करे तो पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य बढ़ता है तो परम पुण्यशील परमात्मा की भक्ति उसे मिलती है।
अब रानी स्वतंत्र होकर भक्तिभाव में सर्वथा लग गई। माधवसिंह ने उसकी मर्जी के मुताबिक सब व्यवस्था बदल दी।
एक दिन माधवसिंह अपने बड़े भाई मानसिंह के साथ यात्रा पर गया। नदी पार करना था। नदी बाढ़ में आयी हुई थी। पानी का वेग बड़ा प्रबल था। नाव उलट-पलट हो रही थी। माधवसिंह ने मानसिंह से कहाः
"भाई ! अब बचना मुश्किल है। मगर मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपकी अनुजवधू अर्थात् मेरी पत्नी भगवान की परम भक्त है। उसका पुत्र भी भक्त है, उसकी दासी भी भक्त है। उसके नाश के लिए मैंने षडयंत्र रचा तो भी मुझे भक्ति मिली। अब हम दोनों मिलकर सच्चे हृदय से उसे याद करें तो हमारी सुरक्षा हो जायेगी, अन्यथा बेमौत मरना पड़ेगा।"
भाई सहमत हो गया। दोनों ने पतवार छोड़ दी। सच्चे हृदय से भावपूर्वक भक्तिमती रानी रत्नावती का स्मरण करने लगे। मानो, उसके चिन्तन में तल्लीन हो गये। अनजाने में अपनी अंतरात्मा में पहुँच गये।
दैवयोग कहो, भगवान की लीला कहो, रत्नावती की पुण्याई कहो, कैसे भी करके बाढ़ के तूफान में टकराती नाव आखिर किनारे पहुँच गई। माधवसिंह को तो रत्नावती में श्रद्धा थी ही, अब मानसिंह को भी श्रद्धा हो गई।
भोगी को अगर योग मिले, अभक्त को अगर भक्ति मिले, अशांत को अगर परम शांति देनेवाला रास्ता मिले तो वह मनुष्य ऊँचा भी उतना ही उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है। जो रानी राजमहल मे भोग-विलास में, संसार के कीचड़ में फँसी जा रही थी उसे भक्तहृदया दासी का संपर्क हुआ तो वह रानी स्वयं तो तर गई, उसका चिन्तन करने वाले लोग भी पार हो गये।
भक्ति
करे पाताल में
प्रकट होय
आकाश।
दाबी
पण दूबे नहीं
कस्तूरी
सुवास।।
हरि की भक्ति, हरिज्ञान और हरि के भक्तों का संग जिसको मिल गया उसको सच्चा धन मिल गया। उसके सिवाय जो कुछ मिला वह उपाधि है।
हरिकथा
ही कथा बाकी
सब जगव्यथा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
साधक को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अमुक वस्तु, व्यक्ति, अवस्था या परिस्थिति के न मिलने के कारण साधना नहीं हो सकती है या उस व्यक्ति ने साधना में विघ्न डाल दिया। उसे तो यही मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति साधना में विघ्न नहीं डाल सकता। भगवान तो विघ्न डालते नहीं, सब प्रकार से सहायता करते हैं और अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है। अतः मेरी दुर्बलता ही विघ्न है।
वास्तव में तो साधक का विश्वास और प्रेम ही साधना में रूचि और तत्परता उत्पन्न करता है। साधना के लिए बाह्य सहायता आवश्यक नहीं है।
साधक को चाहिए कि करने योग्य हरेक काम को साधन समझे। छोटे-से-छोटा जो भी काम प्राप्त हो, उसे पूरी योग्यता लगाकर उत्साहपूर्वक, जैसे करना चाहिए वैसे ठीक-ठीक करे। जो काम भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए किये जाते हैं वे सभी काम साधना हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ