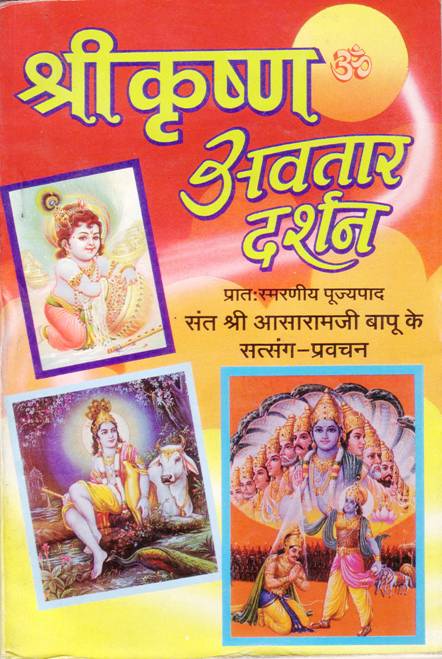
प्रातः
स्मरणीय
पूज्यपाद संत
श्री
आसारामजी
बापू के
सत्संग-प्रवचन
श्रीकृष्ण
अवतार दर्शन
निवेदन
श्रीकृष्ण के जीवन को तत्त्वतः समझना अत्यन्त कठिन है। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं-
कश्चिन्मां
वेत्ति
तत्त्वतः।
'कोई विरला ही मुझे तत्त्व से जानता है।'
ईश्वर को तत्त्वतः जानना और यथारूप विवेचन कर उसे दूसरों को समझना तो और भी कठिन है। कोई विरले महापुरूष ही यह कार्य लोकभोग्य शैली में कर पाते हैं।
इस छोटे से ग्रन्थ में भारत के तत्त्ववेत्ता महापुरूष पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू की अनुभवसम्पन्न योगवाणी में भगवान श्रीकृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है।
संत श्री के वचनामृत त्रिविध तापों से संतप्त मानवजीवन को केवल शीतलता ही प्रदान नहीं करते हैं, अपितु उनका मनन करने वालों को तत्त्वज्ञान के उच्च शिखर पर आरूढ़ होने में भी सहायता करते हैं।
प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित श्रीकृष्ण के जीवनादर्शों का अनुसरण कर आत्मकल्याण के इच्छुक साधक नित्य-निरन्तर तत्परतापूर्वक साधनापथ पर अग्रसर होंगे, इसी आशा के साथ.......
विनीत,
श्री
योग वेदान्त
सेवा समिति
अहमदाबाद
आश्रम
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
उद्धव
को भगवान श्रीकृष्ण
का उपदेश
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
श्रीकृष्ण
का प्रागट्य
श्रीमद् भगवदगीता के चौथे अध्याय के सातवें एवं आठवें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं-
यदा
यदा ही
धर्मस्य
ग्लानिर्भवति
भारत।
अभ्युत्थानधर्मस्य
तदात्मानं
सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय
साधूनां
विनाशाय च
दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय
संभवामि युगे
युगे।।
'हे भरतवंशी अर्जुन ! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुजनों (भक्तों) की रक्षा करने के लिए, पापकर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भाँति स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ।'
जिस समय समाज में खिंचाव, तनाव व विषयों के भोग का आकर्षण जीव को अपनी महिमा से गिराते हैं, उस समय प्रेमाभक्ति का दान करने वाले तथा जीवन में कदम कदम पर आनंद बिखेरने वाले श्रीकृष्ण का अवतार होता है। श्रीकृष्ण का जन्मदिवस या अवतार ग्रहण करने का पावन दिवस ही जन्माष्टमी कहलाता है।
श्रीमद् भागवत में भी आता है कि दुष्ट राक्षस जब राजाओं के रूप में पैदा होने लगे, प्रजा का शोषण करने लगे, भोगवासना-विषयवासना से ग्रस्त होकर दूसरों का शोषण करके भी इन्द्रिय-सुख और अहंकार के पोषण में जब उन राक्षसों का चित्त रम गया, तब उन आसुरी प्रकृति के अमानुषों को हटाने के लिए तथा सात्त्विक भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान का अवतार हुआ।
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो श्रीकृष्ण का जन्म पाँच हजार दौ सौ तेइस वर्ष पूर्व माना जा सकता है। प्राचीन ऋषि-मुनि इतिहास पर ज्यादा जोर नहीं देते थे अपितु उन घटनाओं पर ध्यान देते थे जिनसे तुम्हारी भीतर की चेतना जागृत हो सके तथा तुम्हारा जीवन आत्ममस्ती से पूर्ण हो।
काल की दृष्टि से देखा जावे तो मनुष्य के वर्ष तथा देवताओं के वर्ष अलग-अलग हैं। मनु महाराज तथा ब्रह्माजी के वर्षों में भी अन्तर है। आपके 360 वर्ष बीतते हैं तब देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं के ऐसे 12000 वर्ष बीतते हैं तब एक चतुर्युगी होती है तथा ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तब एक मन्वन्तर होता है... तब कहीं जाकर ब्रह्माजी का एक दिन होता है।
ब्रह्माजी के इस एक दिन में 14 इन्द्र बदल जाते हैं तथा ब्रह्माजी की उम्र 100 वर्ष होती है। ऐसे ब्रह्माजी भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं।
मनु ब्रह्माजी के पुत्र हैं फिर भी दोनों का समय अलग-अलग होता है। छगनलाल के घर मगनलाल का जन्म हुआ तो छगनलाल का समय और मगनलाल का समय अलग नहीं होता, पिता-पुत्र के वर्ष-काल अलग नहीं होते लेकिन ब्रह्माजी का वर्ष और उनके ही पुत्र मनु का वर्ष अलग-अलग होता है।
ब्रह्माजी के एक दिन तथा मनु के एक दिन में, हमारे एक दिन और देवताओं के एक दिन में जमीन-आसमान का अंतर होता है। अतः काल भी अपनी-अपनी अपेक्षा रखता है। देश और काल सापेक्ष होते हैं अतः अलग-अलग कथाओं अलग-अलग विचार मिलेंगे। इन पर ऐतिहासिक दृष्टि से आप सोचेंगे-समझेंगे तो आप भी अश्रद्धा के शिकार हो सकते हैं। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं अपितु तत्त्व की दृष्टि व प्रेम की निगाहों से देखेंगे तो इन अवतारों का अपना बड़ा अस्तित्त्व है।
अतः भक्त लोग 'श्रीकृष्ण कब हुए' इस बात पर ध्यान नहीं देते बल्कि 'उन्होंने क्या कहा' इस बात पर ध्यान देते हैं, उनकी लीलाओं पर ध्यान देते हैं। भक्तों के लिए श्रीकृष्ण प्रेमस्वरूप हैं और ज्ञानियों को श्रीकृष्ण का उपदेश प्यारा लगता है फिर भी सामान्य रूप से यही माना जाता है कि आज से 5223 वर्ष पूर्व, द्वापर के 863875 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में, बुधवार के दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ।
वसुदेव-देवकी के यहाँ श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तभी से भगवान श्रीकृष्ण हैं, ऐसी बात नहीं है। ऋगवेद में श्रीकृष्ण का बयान आता है, सामवेद के छान्दोग्योपनिषद में श्रीकृष्ण का बयान मिलता है। योगवाशिष्ठ महारामायण में कागभुशुण्ड एवं वशिष्ठजी के संवाद से पता चलता है कि श्रीकृष्ण आठ बार आये, आठ बार श्रीकृष्ण का रूप उस सच्चिदानंद परमात्मा ने लिया।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जन्म
के प्रकार
जन्म के प्रकार के संबंध में भारतीय शास्त्रों में छः प्रकार के जन्म वर्णित हैं-
1. माता पिता के मैथुन व्यवहार से जो रज-वीर्य का मिलन होता है इसे लौकिक जन्म कहा जाता है अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि मन की वासना के अनुसार जो जन्म मिलता है, यह जनसाधारण का जन्म है।
2. दूसरे प्रकार का जन्म संतकृपा से होता है। जैसे, किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया, फल दे दिया और उससे गर्भ रह गया। तप करे, जप करे, दान करे अथवा किसी साधु पुरूष के हाथ का वरदान मिल जाये, उस वरदान के फल से जो बच्चा पैदा हो, वह जनसाधारण के जन्म से कुछ श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरणार्थः भागवत में आता है कि धुन्धुकारी का पिता एक संन्यासी के चरणों में गिरकर संतानप्राप्ति हेतु संन्यासी से फल लाया। वह फल उसने अपनी पत्नी को दिया तो पत्नी ने प्रसूति पीड़ा से आशंकित होकर अपनी बहन से कह दिया कि, "तेरे उदर में जो बालक है वह मुझे दे देना। यह फल मैं गाय को खिला देती हूँ और पति को तेरा बच्चा दिखला दूँगी।" ऐसा कहकर उसने वह फल गाय को खिला दिया।
उसकी बहन के गर्भ से धुन्धुकारी पैदा हुआ तथा संन्यासी द्वारा प्रदत्त फल गाय ने खाया तो गाय के उदर से गौकर्ण पैदा हुआ जो भागवत की कथा के एक मुख्य पात्र हैं।
3. कोई तपस्वी क्रोध में आकर शाप दे दे और गर्भ ठहर जाय यह तीसरे प्रकार का जन्म है।
एक ऋषि तप करते थे। उनके आश्रम के पास कुछ लड़कियाँ गौरव इमली खाने के लिए जाती थीं। लड़कियाँ स्वभाव से ही चंचल होती हैं, अतः उनकी चंचलता के कारण ऋषि की समाधि में विघ्न होता था। एक दिन उन ऋषि ने क्रोध में आकर कहाः "खबरदार ! इधर मेरे आश्रम के इलाके में अब यदि कोई लड़की आई तो वह गर्भवती हो जायेगी।"
ऋषि का वचन तो पत्थर की लकीर होता है। वे यदि ऊपर से ही डाँट लें तो अलग बात है लेकिन भीतर से यदि क्रोध में आकर कुछ कह दें तो चंद्रमा की गति रूक सकती है लेकिन उन ऋषि का वचन नहीं रूक सकता। सच्चे संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता।
दूसरे दिन भी रोज की भाँति लड़कियाँ आश्रम के नजदीक गई। उनमें से एक लड़की चुपचाप अन्दर चली गयी और ऋषि की नजर उस पर पड़ी। वह लड़की गर्भवती हो गई क्योंकि उस ऋषि का यही शाप था।
4. दृष्टि से भी जन्म होता है। यह चौथे प्रकार का जन्म है। जैसे वेदव्यासजी ने दृष्टि डाली और रानियाँ व दासी गर्भवती हो गई। जिस रानी ने आँखें बन्द की उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए। जो शर्म से पीली हो गई। उसने पांडु को जन्म दिया। एक रानी ने संकोचवश दासी को भेजा। वह दासी संयमी, गुणवान व श्रद्धा-भक्ति से संपन्न थी तो उसकी कोख से विदुर जैसे महापुरूष उत्पन्न हुए।
5. पाँचवें प्रकार का जन्म है कारक पुरूष का जन्म। जब समाज को नई दिशा देने के लिए अलौकिक रीति से कोई जन्म होता है हम कारक पुरूष कहते हैं। जैसे कबीर जी। कबीर जी किसके गर्भ से पैदा हुआ यह पता नहीं। नामदेव का जन्म भी इसी तरह का था।
नामदेव की माँ शादी करते ही विधवा हो गई। पतिसुख उसे मिला ही नहीं। वह मायके आ गई। उसके पिता ने कहाः "तेरा संसारी पति तो अब इस दुनिया में है नहीं। अब तेरा पति तो वह परमात्मा ही है। तुझे जो चाहिए, वह तू उसी से माँगा कर, उसी का ध्यान-चिंतन किया कर। तेरे माता-पिता, सखा, स्वामी आदि सब कुछ वही हैं।"
उस महिला को एक रात्रि में पतिविहार की इच्छा हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि 'हे भगवान ! तुम्हीं मेरे पति हो और आज मैं पति का सुख लेना चाहती हूँ।' ऐसी प्रार्थना करते-करते वह हँसती रोती प्रगाढ़ नींद में चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि मैं किसी दिव्य पुरूष के साथ रमण कर रही हूँ। उसके बाद समय पाकर उसने जिस बालक को जन्म दिया, वही आगे चलकर संत नामदेव हुए।
जीसस के बारे में भी ऐसा ही है। जीसस मरियम के गर्भ से पैदा हुए थे। मरियम जब कुंवारी थी तभी जीसस गर्भ में आ गये थे। सगाई के दौरान 'मरियम गर्भवती है' ऐसा सुनकर उसके भावी पति के परिवार वाले सगाई तोड़ रहे थे। कहते हैं कि भावी पति को स्वप्न आया कि 'मरियम कुंवारी ही है यदि तू सगाई तोड़ेगा तो तेरी बुरी हालत हो जाएगी।'
फिर सगाई के बाद मरियम की शादी भी हुई लेकिन जीसस बिना बाप के ही पैदा हुए ऐसा कहा जाता है।
6. जन्म की अंतिम विधि है अवतार। श्रीकृष्ण का जन्म नहीं, अवतार है। अवतार व जन्म में काफी अन्तर होता है। सच पूछो तो तुम्हारा भी कभी अवतार था किन्तु अब नहीं रहा।
अवतरति
इति अवतारः।
अर्थात् जो अवतरण करे, ऊपर से नीचे जो आवे उसका नाम अवतार है। तुम तो विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा थे सदियों पहले, और अवतरण भी कर चुके थे लेकिन इस मोहमाया में इतने रम गये कि खुद को जीव मान लिया, देह मान लिया। तुम्हें अपनी खबर नहीं इसलिए तुम अवतार होते हुए भी अवतार नहीं हो। श्रीकृष्ण तुम जैसे अवतार नहीं हैं, उन्हें तो अपने शुद्ध स्वरूप की पूरी खबर है और श्रीकृष्ण अवतरण कर रहे हैं।
श्रीकृष्ण का अवतार जब होता है तब पूरी गड़बड़ में होता है, पूरी मान्यताओं को छिन्न भिन्न करने के लिये होता है। जब श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ तब समाज में भौतिकवाद फैला हुआ था। चारों ओर लग जड़ शरीर को ही पालने-पोसने में लगे थे। धनवानों और सत्तावानों का बोलबाला था।
भगवान का जन्म प्रत्येक युग में युग के अनुसार ही होता है। अब यदि श्रीकृष्ण आ जाएँ तो जरूरी नहीं कि वे हठ करेंगे कि पहले बँसी बजाई थी, अब भी बजाऊँगा, माखन चुराया था, अब भी चुराऊँगा या घोड़ागाड़ी ही चलाऊँगा। नहीं। अब यदि श्रीकृष्ण आते हैं तो मर्सीडीज भी चला सकते हैं, बुलेट भी चला सकते हैं। उनके जीवन में कोई जिद नहीं, कोई आग्रह नहीं।
....और तात्त्विक दृष्टि से श्रीकृष्ण आते हैं, न जाते हैं। एक सच्चिदानंद की सत्ता ही है जो श्रीकृष्ण का रूप लेकर, श्रीराम का रूप लेकर लीला करती है और समाज को मार्गदर्शन दे जाती है लेकिन अन्य अवतारों की अपेक्षा श्रीकृष्ण का अवतार बड़ा सहज है। उनके जीवन में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई ग्रहण नहीं। बस, उनका तो सदा सहज जीवन है। मौका आया तो गा लिया, मौका आया तो नाच लिया, बँसी बजा ली, मक्खन चुरा लिया। रथ चला लिया। और तो और, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के मैदान में अर्जुन को तत्त्वज्ञान का उपदेश भी दे दिया। श्रीकृष्ण का जीवन बड़ा ही निराला जीवन है।
कई लोग अवतरण या अवतार के संबंध में शंका करते हैं कि भगवान जब आप्तकाम हैं तो उन्हें ऊपर से नीचे आने की क्या जरूरत है ? जो शुद्ध है, निरन्तर है, अविनाशी है, निराकार है उन्हें साकार होने की क्या जरूरत है ?
वेदान्त के महापुरूष लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार हैं। परमात्मा का वास्तव में कोई जन्म नहीं है। वास्तव में न तो श्रीकृष्ण आये हैं, न गये हैं लेकिन माया के जगत में जब सारा जगत मायामय है, मिथ्या है, तो इस मिथ्या जगत में आना भी मिथ्या है और जाना भी मिथ्या है। इसलिए श्रीकृष्ण आने वालों की नजर से आये भी और जाने वालों की नजर से गये भी।
ज्ञानी बोलते है कि भगवान तो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं। निराकार का अवतार संभव नहीं है। निराकार में कृति हो जाय, यह संभव नहीं है।
हकीकत में निराकार का अवतार होना संभव नहीं है लेकिन अवतार उस निराकार का नहीं हुआ वरन् 'मायाविशिष्ट चैतन्य' ही श्रीकृष्ण का आकार लेकर प्रगट हुआ।
भक्तों का कहना है कि भगवान का अवतार हुआ और ज्ञानियों का कहना है कि माया का अवतार हुआ। माया ऊपर नीचे होती है, तुम्हारा शरीर ऊपर नीचे होता है लेकिन तुम्हारे ज्ञान की सवित् ऊपर-नीचे नहीं होती। तुम्हारा मन ऊपर नीचे होता है किन्तु सबको देखने वाला जो चैतन्य है, वह अपनी महिमा में ज्यों का त्यों होता है। इस प्रकार ईश्वर का अवतार होते हुए भी ईश्वर ने अवतार नहीं लिया और अवतार लेते हुए भी उनको कोई समस्या नहीं, ऐसा ज्ञानमार्गी कहते हैं।
भक्त कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में, भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे कंस के कारागार में श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ है। कृष्णपक्ष की अंधेरी रात में ही ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है।
भागवताकार कहते हैं कि वसुदेव-देवकी शादी के बाद जब अपने घर को जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई किः "ऐ कंस ! तू जिसे छोड़ने जा रहा है उस देवकी के उदर से जो बालक पैदा होगा वही तेरा काल होगा।'
देहाभिमानी व भोगी व्यक्ति सदा भयभीत रहता है और मृत्यु से डरता है। कंस ने तत्क्षण ही तलवार निकालकर देवकी का अंत करना चाहा तब वसुदेव ने समझायाः "देवकी तो तेरी बहन है, जिसे शादी करवाकर अभी तू विदा कर रहा है। उसे मारने से क्या होगा? मृत्यु तो सबकी होती है। मृत्यु के बाद जन्म तथा जन्म के बाद मृत्यु, यह क्रम तो सदा चलता रहता है। वास्तविक मृत्यु तो अज्ञान की करना है। अज्ञान की एक बार मौत कर दे फिर तेरी कभी मौत होगी ही नहीं और इस देह को तू कितना भी संभाले लेकिन अंत में यह मृत्यु के बिना रहेगी नहीं।"
जो पामर होते हैं उन्हें सज्जन पुरूषों के वचन समझ में नहीं आते हैं। बुद्धि में तमोगुण और रजोगुण होता है तो देहासक्ति बढ़ती है। यदि तामस प्रकृति बढ़ जाती है तो वह फिर दंड व अनुशासन से ही सुधरती है। कंस ने वसुदेव की बात नहीं मानी और समझाने के बाद भी वसुदेव-देवकी को कंस ने कैद कर लिया।
श्रीकृष्ण जब आने को थे तब वसुदेव का तेज बढ़ गया और उन्होंने देवकी को निहारा तो वह तेज देवकी में प्रविष्ट हो गया। भगवान नारायण का चतुर्भुजी रूप वसुदेव-देवकी ने देखा। फिर भगवान अन्तर्धान हो गये और श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट हुए।
वसुदेव और देवकी के यहाँ जेल में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव अर्थात् शुद्ध सत्त्वगुण और देवकी अर्थात् निष्ठावान भावना। इन दोनों का जब संयोग होता है तब आपकी देहरूपी जेल में उस आनंदकंद परमात्मा का जन्म होता है, ऐसा तत्त्व की दृष्टि से आप समझ सकते हैं।
श्रीकृष्ण का जन्म अलौकिक है। माता-पिता हथकड़ियों के साथ जेल में बंद हैं। चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं और उन विपत्तियों के बीच भी श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए अवतार ले रहे हैं। मानो यह संदेश दे रहे हों कि भले ही चारों ओर विपत्तियों ने घेर रखा हो किन्तु तुम एक ऐसे हो जिस पर विपत्तियों का असर हो नहीं सकता।
यमुना में बाढ़ आई हुई है। श्रीकृष्ण को उस पार ले जाना है और वसुदेव घबरा रहे हैं किन्तु श्रीकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। कथा कहती है कि श्रीकृष्ण ने अपना पैर पानी को छुआया और यमुना की बाढ़ का पानी उतर गया।
जिसे अपनी महिमा का पता है, जिसने अपना घात नहीं किया है, जो अपने को देह नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति के संकल्प में अदभुत सामर्थ्य होता है। कई ऐसे बालक जो भविष्य में अपने स्वरूप को जान सकते हैं, उनके बाल्यकाल में ऐसा चमत्कार नहीं देखा गया किन्तु श्रीकृष्ण के साथ तो जन्म से ही चमत्कार घटते रहे हैं।
जिन्होंने गूढ़ और सूक्ष्म तत्त्वज्ञान को समझाने का प्रयास किया तथा समाज को अपने प्रेम और अठखेलियों से प्रभावित किया ऐसे ब्रह्मज्ञान के प्रचारक, सदा समता में स्थित रहने वाले श्रीकृष्ण का जन्म सच पूछो तो जन्माष्टमी की रात के 12 बजे ही नहीं होता, अपितु तुम जब जन्म करवाना चाहो, तब होता है।
कहते हैं शुभ घड़ी में भगवान श्रीकृष्ण पैदा हुए। मैं कहूँगा - गलत है। जिन घड़ियों में भगवान श्रीकृष्ण पैदा हुए वे घड़ियाँ शुभ हो गयीं। जिसको मुस्कुराना आ जाता है, निर्वासनिक होना आ जाता है, अपने-आप में रमण करना आ जाता है, वह जहाँ जाता है, वहाँ मंगल हो जाता है, शुभ हो जाता है। वह जो करता है, देखता है और देता है वह भी शुभ होता है क्योंकि वह स्वयं परम शुभ से जुड़ा है।
क्या जन्माष्टमी ही श्रीकृष्ण का जन्मदिन है ? नहीं। ऐसे अनेक बार जन्मदिन हुए। आप जब चाहो, याद कर जन्मदिन मनाकर उसका मजा ले सकते हो क्योंकि वह तत्त्व कभी गया नहीं। गया इसलिये नहीं कि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। वह तो अजन्मा है..... अनादि है.... अनंत है.... लेकिन तुम जब भावना से मनाते हो तब जन्मदिन हो जाता है। तुम रोज मनाना चाहो तो रोज मना सकते हो, हर दिल में.... हर साँस में मना सकते हो। वास्तव में उसके सिवा तो कोई जन्मा ही नहीं। जन्म देने की सत्ता प्रकृति की है लेकिन प्रकृति को सत्ता देने वाला भी वही एक चैतन्य है।
आपके जीवन में भी जन्माष्टमी तब होगी जब श्रीकृष्ण प्रगट होंगे। ये श्रीकृष्ण तो वसुदेव देवकी के यहाँ जन्मे थे और यशोदा के घर पले थे अर्थात् विवेक और समता के यहाँ श्रीकृष्ण का जन्म होता है तथा यशस्विनी बुद्धि, ऋतंभरा प्रज्ञा के पास वह पलता है। विवेक की मूर्ति वसुदेव हैं और समता की मूर्ति देवकी हैं। यशोदा यशस्विनी बुद्धि की परिचायक हैं।
तुम जब प्रखर विवेक और समता रखोगे तब तुम्हारे अंतर में भी श्रीकृष्णतत्त्व प्रगट हो सकता है।
निरंजन, निराकार, सच्चिदानंद परमात्मा ने साकार प्रगट होकर श्रीकृष्ण के रूप में अनेक लीलाएँ प्रगट कीं। लीलाएँ तो अनेक थीं किन्तु उन सबके पीछे लक्ष्य यही था कि आप भी अपने कृष्णतत्त्व को जान लो। आप स्वयं कृष्णतत्त्व ही हो, प्रत्येक व्यक्ति कृष्णतत्त्व है लेकिन वह देह को मैं मानता है इसलिए गड़बड़ में पड़ जाता है। यदि आत्मा को मैं मानें तो आप ही का नाम कृष्ण है।
यह बड़ा ही रहस्य भरा महोत्सव है। समाज के पहले से लेकर आखिरी व्यक्ति तक का ध्यान रखते हुए उसके उत्थान के लिए भिन्न-भिन्न तरीकों को अपनाते हुए, इन्सान की आवश्यकताओं व महत्ता को समझाकर उसके विकास के लिए निर्गुण, निराकार परात्पर ब्रह्म सगुण-साकार होकर गुनगुनाता, गीत गाता, नाचता, खिलाता और खाता, अनेक अठखेलियाँ करता हुआ, इस जीव को अपनी असलियत का दान करता हुआ, उसे अपनी महिमा में जगाता हुआ प्रगट हुआ है। उसी को श्रीकृष्णावतार कहते हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
श्रीकृष्ण
की मधुर
बाललीलाएँ
श्रीकृष्ण का सर्वस्व मधुर है। तभी तो कहते हैं-
अधरं
मधुरं वदनं
मधुरं नयनं
मधुरं हसितं
मधुरम्।
हृदयं
मधुरं गमनं
मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं
मधुरम्।।
श्रीकृष्ण की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक लीला मधुर है और बाललीला का तो कहना ही क्या ? प्रत्येक मन को आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे, ऐसी हैं उनकी बाललीलाएँ। फिर चाहे नंदबाबा हो चाहे माँ यशोदा, चाहे गोपियाँ हों चाहे गोपबाल, सभी उनकी लीलाओं से आनंदित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। उनकी बाललीलाएँ किसी सामान्य बालक की तरह नहीं रही। उसमें भी अनेक गूढ़
संदेश छुपे हुए हैं और हो भी क्यों न ? क्योंकि ये सच्चिदानंद ब्रह्म द्वारा साकार रूप में की गई लीलाएँ हैं। मनुष्य चाहे तो उससे ज्ञान प्राप्त करे और चाहे तो उनके प्रेम में रंग जाय। यह उस पर निर्भर करता है। वह नटखटिया तो ज्ञान और प्रेम दोनों देता है।
एक बार यशोदा माँ से किसी ने फरियाद की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा पूछती हैं- 'बोल तूने मिट्टी खाई ?"
श्रीकृष्ण कहते हैं- "नहीं माँ ! नहीं खाई।"
यशोदाः "तू झूठ बोल रहा है। मुख खोलकर बता।"
श्रीकृष्ण ने मुख खोलकर बताया तो यशोदा माँ को उसमें त्रिभुवन के दर्शन हो गये और वह चकित हो गई। श्रीकृष्ण ने अपनी माया समेट ली तो फिर यशोदा अपने मातृभाव में आ गई।
सामर्थ्य होने पर भी श्रीकृष्ण में बालक होने की योग्यता है।
हमारे पास धन आता है तो छोटे बनने में हमें तकलीफ होती है। सत्ताधीश हो जाते हैं और सत्ता चली जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है। महान् बनने के बाद छोटा बनते है तो तकलीफ होती है किन्तु श्रीकृष्ण के साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उनका जीवन सर्वांगी है इसलिए ऋषियों ने उन्हें पूर्णावतार कहा है।
श्रीकृष्ण का अन्तःकरण इतना शुद्ध व विकसित है कि उन्होंने चौसठ दिन में चौसठ कलाएँ सीख लीं। बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण पूरे बालक, युवावस्था में पूरे निर्भय और प्रौढ़ावस्था में पूर्ण ज्ञानी हैं। तभी तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया।
बालकृष्ण की बाललीलाएँ ऐसी हैं कि यशोदा माँ को भी आश्चर्य हुए बिना न रहे और प्रभावती भी प्रसन्न हुए बिना न रहे। यमुनाजी के प्रवाह में कूद पड़े हैं और कालियानाग के सिर पर नाच रहे हैं। धेनुकासुर, बकासुर को ठीक कर दिया है और 'छछियन भरी छाछ' के लिए नाचने को भी तैयार हैं।
देवांगना नाम की अहीर की लड़की गौशाला में गोबर उठाते समय सोच रही है कि 'कब यह काम पूरा होगा ? कन्हैया के दर्शन करने जाना है... वह तो बंसी बजाता रहता है और मैं यहाँ गोबर उठाती रहती हूँ। हाय......। अब कोई जाओ। अरे कन्हैया ! अब तू ही आ जा। मन से पुकारती हुई वह गोबर उठाती जा रही है, इतने में वहाँ पर तेज पुंज प्रगट हुआ है उसमें कन्हैया मुस्करा रहा है।
देवांगना बोलीः "तुम खड़े-खड़े क्या मुस्कुरा रहे हो ? यहाँ आकर तगारे तो उठवाओ। ....श्रीकृष्ण तगारे उठवाने लगे हैं। कितनी सरलता है....! इससे उनका बड़प्पन नहीं चला गया।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "मैं तो मक्खन लेने आया हूँ और तू मुझसे तगारे उठवा रही है ?"
देवांगनाः "मक्खन तो दूँगी लेकिन पहले ये तगारे उठवा।"
श्रीकृष्णः "कितना दोगी ?"
देवांगनाः "एक तगारा उठवायेगा तो एक लोंदा मक्खन का दूँगी।"
श्रीकृष्ण ने एक..... दो.... तीन.... चार... तगारे उठवाये। उनको तो बाललीला करनी है अतः वे बोलेः "तू तो तगारे उठाती जाती है, फिर गिनेगा कौन ? मैं उठाने वाला एक आदमी हूँ। दूसरा गिनने वाला कहाँ से लाऊँ ? जा, मैं नहीं उठवाता।" कहकर श्रीकृष्ण खड़े रह गये।
देवांगना बोलीः "अरे ! कन्हैया !! उठवा..... उठवा, मैं गिनूँगी।"
श्रीकृष्णः "तू भूल जाएगी तो ?"
देवांगनाः "नहीं भूलूँगी। देख, तू जितने तगारे उठवाता जाएगा, उतने तेरे मुँह पर मैं गोबर के टिल्ले करती जाऊँगी।"
श्रीकृष्ण कहते हैं- "ठीक है।"
उन्हें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि श्रीकृष्ण अपने को देह नहीं मानते हैं। उनका मैं त अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। वह कभी बिगड़ नहीं सकता।
मानो इस लीला से श्रीकृष्ण यही बताना चाहते हैं कि तुम भी अपने वास्तविक मैं को पहचान लो। इसलिए वे नाचकर, उपदेश देकर, विनोद करके, टिल्ले लगवाकर भी तुम्हें अपने आकर्षक स्वरूप की ओर ले जाते हैं और वह आकर्षक स्वरूप तुम्हारे ही हृदय में छुपा हुआ है।
तुम आनंदस्वरूप, सुखस्वरूप हो इसलिए तुम सुख और आनंद के लिए प्रयास करते हो किन्तु हकीकत में सुख लेने की नहीं, देने की चीज है यह श्रीकृष्ण के जीवन से सीखना चाहिए। कभी बंसी बजा कर सुख दे रहे हैं तो कभी माखन चुरा कर सुख दे रहे हैं। गोबर के तगारे उठवाते-उठवाते देवांगना मुख पर गोबर के टिल्ले करती है तब भी वे सुख ही बरसा रहे हैं।
किसी सेठ सत्ताधीश, या अधिकारी को उनका कोई हितैषी या नौकर आकर कहे कि, साहब ! इतने गोबर के तिलक करने दो आपके चेहरे पर। तो क्या वह करने देगा ? नहीं। ''मेरी इज्जत जायेगी.... लोग क्या कहेंगे ?" यही उसका प्रतिभाव होगा।
हमारे पास चार पैसे आ जाते हैं और हम ड्रायवर रख लेते हैं क्योंकि फिर स्वयं को गाड़ी चलाने में संकोच होता है। क्योंकि इज्जत का सवाल है। लेकिन उस विश्वंभर को घोड़ागाड़ी चलाने में भी संकोच नहीं होता। कितना सरल स्वभाव है !
यहाँ श्रीकृष्ण देवांगना के तगारे उठवा रहे हैं, देखते-देखते पूरी गौशाला साफ हो गई और श्रीकृष्ण का मुँह गोबर के तिलकों से भर गया। जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही श्रीकृष्ण के मुख पर टिल्ले टिमटिमा रहे हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं- "लाओ मक्खन।" कमर पर अपने पीताम्बर की गाँठ बाँधकर झोली बनाते हुए कहते हैं- "चल, इसमें रखती जा।"
देवांगना मक्खन का एक-एक लौंदा रखती जाती है और एक-एक टिल्ला पोंछती जाती है।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "मैं केवल मक्खन थोड़े खाऊँगा ! साथ में थोड़ी ही मिश्री भी दे दे।"
देवांगनाः "मिश्री मुफ्त में थोड़ी ही मिलेगी ! उसके लिए दूसरा कुछ करो।"
श्रीकृष्णः "क्या करूँ ?"
देवांगनाः "थोड़ा नाच कर दिखाओ।"
श्रीकृष्ण नाच रहे हैं। उनकी अंगड़ाइयों में सुख के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ प्रेम मिलता है। वास्तव में देखो तो जैसे थे वैसे ही अकर्त्ता। यह श्रीकृष्ण की बाललीलाओं में देखने को मिलता है।
श्रीकृष्ण ने एक माखनचोर कंपनी बनाई थी जिसके सदस्य यह बताते थे कि आज अमुक-अमुक घर मक्खन बना है। जो अधिक चतुर गोपियाँ होतीं वे अपना मक्खन किसी दूसरे के घर रख आती थीं।
उनमें से प्रभावती बड़ी चतुर थी। चतुर व्यक्ति आत्मानंद से दूर रह जाता है, भले ही आत्मानंद उसके पास आता हो। प्रभावती कई बार यशोदा से श्रीकृष्ण की शिकायत कर चुकी थी तब यशोदा ने कहा थाः "मैं तो तब मानूँगी जब उसको रंगे हाथ पकड़कर लाओ।"
एक बार प्रभावती ने अपनी चतुराई से श्रीकृष्ण को रंगे हाथ पकड़ने की सारी योजना बनाई। उसने सींके पर मक्खन रख दिया और नीचे रस्सियाँ इस ढंग से बाँधी कि रस्सी के छूते ही घंटियाँ बज उठें फिर वह स्वयं छुप कर बैठ गई।
श्रीकृष्ण आये और देखा कि सींका तो बँधा है किन्तु आज कुछ षड्यंत्र है। पहले तो फौज को भेजते थे किन्तु आज स्वयं गये और गोपबालों से कहाः "ठहरो । आज कुछ गड़बड़ है, रूको जरा।"
श्रीकृष्ण ने इधर-उधर देखा कि कोई है तो नहीं ! फिर धीरे से सींके के पास गये। वहाँ देखा कि हर रस्सी में घंटी लगी हैं और किसी का भी हाथ लगते ही बज उठेगी। फिर भी मक्खन तो चुराना ही है। जैसे साधक संसार की गड़बड़ सुनते हुए भी अपनी साधना नहीं छोड़ता तो भगवान संसार की गड़बड़ देखकर अपना मक्खन क्यों छोड़ेंगे भैया ?
भगवान ने शब्द के अधिष्ठाता देव को आदेश दियाः
"मेरी इस आज्ञा का पालन हो कि मैं अथवा मेरे साथी रस्सियों को छू भी लें अथवा गलती से हाथ-पैर लग जाय तो भी बजना मत। मेरी आज्ञा का पूरा पालन करना।"
देव ने श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन किया। सब बच्चे भीतर आ गये फिर भी घंटियाँ बजी नहीं। बच्चे एक दूसरों के कन्धों पर चढ़कर खड़े रहे और उन सब पर चढ़कर श्रीकृष्ण पहुँच गये सींके तक।
आज तक श्रीकृष्ण पहले सबको खिलाते थे, किन्तु इस बार देखा कि षड्यंत्री के घर का माल है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ! क्योंकि वे कंपनी के नेता थे न ! नेता का यह गुण होना चाहिए कि सुख के समय साथियों को आगे करे किन्तु विपत्ति में स्वयं पहले जावे, इसलिए पहले श्रीकृष्ण स्वयं खाने लगे। ज्यों ही उनका हाथ खाने के लिए होठों तक पहुँचा कि टन.... टन..... टन.... टन..... करती घँटियाँ बज पड़ीं। श्रीकृष्ण ने डाँटकर कहाः "हे शब्द के अधिष्ठाता देव ! प्रगट हो जाओ।"
कथा कहती है कि शब्दब्रह्म साकार रूप होकर प्रगट हुए। श्रीकृष्ण ने कहाः "हे नादब्रह्म ! मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया ?"
तब शब्दब्रह्म ने कहाः "भगवान् ! हम आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। शास्त्र भी तो आपकी ही आज्ञा है। शास्त्रों में लिखा है कि और समय घंटियाँ न बजे लेकिन भगवान जब भोग लगायें तब तो बजना ही चाहिए।"
घंटियाँ बजने से घर की मालकिन प्रभावती आ गई। प्रभावती का तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि संसार में प्रभावशाली है, वह परमात्मप्रेम को नहीं देख पाती है। जिसका प्रभाव शरीर के सुख में ही खर्च हो जाता है, वह आत्मसुख नहीं ले पाता है और आत्मसुख यदि उसके हाथ में आता भी है तो छूट जाता है। यही बात बताने का प्रयास वेदव्यासजी ने इस प्रसंग में किया है।
प्रभावती भागती-भागती आई लड़कों के सरदार श्रीकृष्ण को पकड़ लिया।
वे सरदार ही तो हैं ! लड़कों की कंपनी में लड़कों के योगियों की कंपनी में योगियों के, योद्धाओं की कंपनी में योद्धाओं के, नाचने वालों की कंपनी में नाचने वालों के वे सरदार नटवर नागर हैं क्योंकि वह चैतन्य सबका सरदार ही है।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "छोड़ दे, छोड़ दे..... भूल हो गई। दूसरी बार नहीं करूँगा।"
प्रभावती कहती हैः "आज तो मैं नहीं छोड़ूँगी। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है।" प्रभावती श्रीकृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटते हुए यशोदा के पास ले जा रही है।
प्रभावती का लड़का कहता हैः "माँ....माँ....! इसको छोड़ दे, इसके बदले में मुझे पकड़ ले।"
प्रभावतीः "तू तो मेरा बेटा है।"
जिसको मेरा बेटा 'मेरा' लगता है, दूसरे का बेटा, 'दूसरे का बेटा' लगता है, उसके हाथ में आया हुआ आनंद भी टिकता नहीं।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "छोड़ दे..... छोड़ दे......।"
प्रभावतीः "नहीं छोडूँगी।"
वह तो आगे बढ़ती चली। आखिर श्रीकृष्ण तो युक्तियों के राजा हैं। प्रभावती ने छोटा-सा घूँघट तान रखा था। श्रीकृष्ण उसके ससुर की आवाज में खाँसे तो प्रभावती ने अपना घूँघट और खींचा। परिस्थिति की अनुकूलता देखते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं- "अब तू छोड़ती है तो ठीक है और नहीं छोड़ती है तो मेरा यह हाथ थक गया है। तू यह हाथ ढीला कर। मैं तुझे अपना दूसरा हाथ पकड़ा देता हूँ।"
श्रीकृष्ण ने साथ चल रहे प्रभावती के बेटे को इशारे से बुलाकर उसका हाथ प्रभावती के हाथ में थमा दिया और खुद बीच के छोटे-से रास्ते से घर पहुँचकर अपने कमरे में जाकर सो गये।
प्रभावती अपने बेटे को लेकर यशोदा के घर पहुँची। वह अभी भी यही समझ रही है कि श्रीकृष्ण को पकड़कर आ रही हूँ।
उसने यशोदा का दरवाजा खटखटायाः "यशोदा माँ.....! यशोदा माँ....! द्वार खोलो। आज तो रंगे हाथों पकड़कर लाई हूँ तुम्हारे कन्हैया को। रोज यही चोरी करता है। इसने बहुत सताया है। केवल मेरे घर ही नहीं, सबके घर की चोरी यही करता है।
यशोदा माँ द्वार खोलती है तो प्रभावती कहती हैः
"देखो, तुम्हारे लाल को लाई हूँ। यही चोरी करता है।"
यशोदाः "तू घूँघट के पट तो खोल, देख तो जरा, किसको पकड़कर लाई है ?"
प्रभावती देखती है तो उसका ही बेटा निकलता है।
यशोदा कहती हैः "चोरी तो तेरा बेटा करता है और नाम तू मेरे बेटे का लगाती है !"
तभी श्रीकृष्ण 'ऊँ.... ऊँ.... करके करके करवट बदलते हैं और कहते हैं- "माँ, मुझे सपने में प्रभावती दिखती है... बड़ी बड़ी आँखें दिखाकर डरा रही है।" फिर बाहर आकर पूछते हैं-
"माँ ! क्या है ? यह कौन है ?"
यशोदाः "बेटा ! यह प्रभावती है। अपने बेटे को लेकर आई है और कहती है कि तेरा कृष्ण ही चोरी करता है।"
श्रीकृष्णः "माँ ! चोरी तो रोज इसका बेटा ही करता है और नाम यह मेरा लेती है। देख, मैं तो घर में ही सोया हूँ।"
देखो, प्रभावती का बेटा ही चोरी करता है, श्रीकृष्ण कभी चोरी नहीं करते। प्रभावती यानि मति, अक्ल, होशियारीवाला मन ही संसारी पदार्थ चुराता है। आत्मारामी कभी कुछ नहीं चुराते क्योंकि सारा विश्व उनकी अपनी मिल्कियत होती है फिर भला वे कहाँ से और क्यों कर चुरायेंगे ?
श्रीकृष्ण स्वयं आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। उन्हीं की तो सारी मिल्कियत है, तो तुम श्रीकृष्ण को चोर कैसे कह सकते हो ?
फिर भी एक बार माखनचोरी के आरोप में माँ यशोदा ने श्रीकृष्ण को ऊखल से बाँधने का प्रयास किया, तब योगमाया ने हस्तक्षेप किया। ज्यों यशोदा रस्सी बाँधे त्यों रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ जाय।
ज्ञानवान को कभी कोई बंधन नहीं बाँध सकता तो तुम भला कैसे बाँध सकते हो ? कर्म तो सूक्ष्म होते हैं, वे बाँध नहीं सकते तो तुम श्रीकृष्ण को कैसे बाँध सकते हो ?
हाँ ! श्रीकृष्ण यदि स्वयं बँधना चाहे तो थोड़ी देर के लिए ओखली से बँध जाते हैं बाकी तो सब रस्सियाँ छोटी पड़ जाती हैं। रस्सी का दो अंगुल पड़ना इस बात का संकेत करता है कि जो बुद्धि से या दादागिरी से परब्रह्म चैतन्य को या आत्मा के आनंद को बाँधना चाहता है, वह दो कदम पीछे रह जाता है किन्तु यदि प्रेम और समर्पण से कोई बाँधना चाहे तो परब्रह्म परमात्मा वहाँ स्वयं बँध जाता है।
श्रीकृष्ण ने देखा कि माँ को दुःख होगा कि 'अरे ! मैं उसे बाँध न पाई।' अतः श्रीकृष्ण ने योगमाया को आदेश दियाः "तू बीच में क्यों पड़ती है ? मुझे बँध जाने दे।' .......और श्रीकृष्ण ऊखल से बँध गये।
यशोदा के चले जाने के बाद ऊखल को खींचते-खींचते श्रीकृष्ण वहाँ पहुँचे जहाँ नारदजी के श्राप से शापित दो वृक्ष खड़े थे। उन दो वृक्षों के बीच में से ऊखल को ले जाकर जोर से खींचने पर वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े और उसमें से दो दिव्य पुरूष प्रगट होकर स्तुति करने लगेः
"हे सच्चिदानंदस्वरूप परमात्मा ! हम जब मोहवश क्रीड़ा कर रहे थे तब नारदजी जैसे महान ऋषि आये और हम उनका आदर सत्कार न कर सके। हमारे मद को, हमारे विकारों को दूर करने के लिए नारदजी ने श्राप दिया कि 'देवताओं के सौ वर्ष बीतें तब तुम्हें वृक्ष जैसी जड़ योनि में रहना पड़ेगा। उसके बाद भगवान अवतार लेंगे और तुम लोगों का उद्धार होगा।' हे भगवन् ! तब से हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके स्पर्श से आज हम मुक्त हो गये हैं, हमारी सारी थकान मिट गई है।'
श्रीकृष्ण का ऊखल से बँधना भी कल्याणकारी हो गया। हालाँकि यह उनकी बाललीला का ही एक अंग था किन्तु उसमें भी शापग्रस्त देवताओं का उद्धार छुपा था।
इस तरह श्रीकृष्ण ने अनेक बाललीलायें कीं। वे एक सामान्य ग्वालबाल की तरह जंगल में गायें चराने जब जाते थे तब अपने बालसखाओं के साथ भी बालसुलभ क्रीडाएँ किया करते थे। उनके साथ गायें चराना, गायों की पूँछ पकड़कर दौड़ना, ग्वालबालों के साथ खेलना और यहाँ तक कि साथ-साथ मिलकर भोजन करना, भोजन में भी छीनाझपटी करना.... इस प्रकार सहज रूप से बाललीला करते हुए सबको श्रीकृष्ण आनंदित कर रहे थे।
श्रीकृष्ण की इन बालसुलभ लीलाओं व चेष्टाओं को देखकर एक बार ब्रह्माजी को भी संदेह हुआ कि ये साक्षात् परब्रह्म नारायण हैं कि क्या हैं ? कुछ पता नहीं चलता। श्रीकृष्ण ग्वालबालों जैसे सामान्य लोगों के साथ रहते हैं, खाते-पीते, चलते-घूमते और वन में विहार करते हैं, लकड़ी लेकर गायों के पीछे दौड़ते हैं, बछड़ों से प्रेम करते हैं। यदि भगवान हैं तो नजर मात्र से भी सबका कल्याण कर सकते हैं, फिर उन्हें यह सब करने की क्या जरूरत है ? ग्वालबालों के साथ जंगल में अपनी गायें चराने वाला गोपाल परात्पर ब्रह्म ! यह कैसे हो सकता है ?
जिस समय ब्रह्मा जी वहाँ आये, उस समय ग्वालबालों की नजर भोजन पर थी और बछड़ों की नजर हरी-हरी घास पर। ग्वालबाल भोजन की तैयारी कर रहे थे और बछड़े चरने के लिए श्रीकृष्ण से दूर निकल गये थे। ब्रह्माजी ने अपनी माया से बछड़े चुरा लिये और सोचा कि देखें, अब श्रीकृष्ण क्या करते हैं। आकर देखा तो श्रीकृष्ण ग्वालबालों के साथ खा रहे हैं। भोजन के समय कोई विधिविधान की मानो उन्हें आवश्यकता ही नहीं। सब एक-दूसरे का भोजन आपस में मिश्रित करके खा रहे हैं।
श्रीकृष्ण जब बछड़ों को देखने गये तो ब्रह्माजी ने ग्वालबालों को भी चुरा लिया। उनको अचेत करके छुपाकर ब्रह्माजी अपने लोक में चले गये। फिर श्रीकृष्ण ने अपने संकल्प मात्र से वैसे से वैसे ग्वालबाल एवं बछड़े बना दिये और एक वर्ष (ब्रह्माजी का एक सेकेंड) तक ग्वालबालों व बछड़ों के साथ लीला करते रहे।
जब ब्रह्माजी पुनः व्रज में आये तो देखा कि उनके छुपाये हुए ग्वालबाल व बछड़े तो अचेतावस्था में पड़े हैं लेकिन श्रीकृष्ण तो उन्हीं जैसे दूसरे ग्वालबाल व बछड़ों के साथ विनोद कर रहे हैं। यह देखकर ब्रह्माजी चकित हो गये व सोच में डूब गये कि ये ग्वालबोल सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैंने छुपाया है ?
उन्होंने आँखें बन्द कर ध्यान में देखा तो सामने मौजूद सभी ग्वालबालों व बछड़ों में श्रीकृष्ण को ही बैठा पाया। वे अपनी आँखों से भगवान के उन रूपों को देखने में असमर्थ हो गये, उनकी आँखें चौंधिया गई।
ब्रह्मजी ने श्रीकृष्ण की परीक्षा लेनी चाही थी लेकिन वे स्वयं ही उलझ गये। श्रीकृष्ण ने जब ब्रह्माजी की यह दशा देखी तब तुरन्त ही अपनी माया का पर्दा हटा लिया। ब्रह्माजी को श्रीकृष्ण में साक्षात् नारायणस्वरूप का दर्शन हुआ। उन्होंने अत्यधिक विनम्र भाव से भगवान की स्तुति की जो श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंध के चौदहवें अध्याय में आती है।
श्रीकृष्ण की बाललीलाओं को देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया क्योंकि श्रीकृष्ण जो भी करते हैं सहज रूप से करते हैं। बालकों के साथ बालकों की तरह सहज व्यवहार था। उसे देखकर ब्रह्माजी को संशय हुआ था जिसे श्रीकृष्ण ने दूर कर दिया। यह केवल उनके लिए ही सम्भव है क्योंकि वे परात्पर ब्रह्म हैं। उनकी बाललीलाएँ उनके लिए तो सहज हैं किन्तु हमारे लिए चमत्कारपूर्ण, ज्ञानयुक्त और मार्गदर्शक भी हैं।
स्वयं परात्पर ब्रह्म होते हुए भी उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि 'मैं भगवान हूँ।' यशोदा को त्रिभुवन के दर्शन करवा दिये, यमलार्जुन वृक्ष का ऊखलबन्धन के माध्यम से उद्धार कर दिया और सृष्टिकर्त्ता द्वारा गाय-बछड़े एवं ग्वालबाल चुरा लेने पर पुनः वैसे के वैसे नये ग्वालबाल और गाय बछड़े बना दिये फिर भी उनमें तनिक भी कर्त्तापन का भाव नहीं क्योंकि वे अकर्त्ता है, अभोक्ता हैं, पूर्ण हैं और ऐसा ही बनने का संदेश इन लीलाओं के माध्यम से हमें देते हैं।
यदि हम भी कार्यों को करते हुए भी स्वयं को कर्त्ता न मानें, भोगों को भोगते हुए भी भोक्ता न मानें और दुःख, रोग एवं कष्ट के समय में भी हम अपने को नित्य, शुद्ध एवं मुक्त मानें तो जो सच्चिदानंद, निर्गुण, निराकार परमात्मा ग्वालबालों के, गोपियों के, यशोदा एवं अन्य गोकुलवासियों के समक्ष प्रकट हुआ है, जो श्रीकृष्ण के अंतःकरण में प्रकट हुआ है वह सच्चिदानंदस्वरूप हमारे अंतःकरण में भी प्रकट हो सकता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
पूर्णपुरूषः
श्रीकृष्ण
श्रीकृष्ण बालकों के साथ पूरे बालक, युवाओं के साथ पूरे युवक, गोपियों के बीच पूरे प्रेमस्वरूप, योगियों के बीच महायोगी, राजाओं के बीच महाराजा, राजनीतिज्ञों के बीच पूरे राजनीतिज्ञ, शत्रुओं के बीच काल के समान और मित्रों के बीच पूर्ण प्रेमस्वरूप, आनन्दस्वरूप हैं। वे अर्जुन के लिए वत्सल सखा है तो वसुदेव-देवकी के लिए आनन्दकारी हितकारी पुत्र हैं। श्रीकृष्ण गुरूओं के समक्ष पूरे शिष्य और शिष्यों के लिए पूरे गुरू हैं ऐसे श्रीकृष्ण को वन्दन......
कृष्णं
वन्दे जगद्
गुरूम्।
कंस को मारकर जब श्रीकृष्ण वसुदेव के पास गये तब वसुदेवजी ने कहाः "मैंने तुम्हारे लिये हनुमानजी की मनौती मानी थी।"
श्रीकृष्ण बोलते हैं- "हाँ..... जब मैं मल्लयुद्ध कर रहा था तब एक बड़ी-बड़ी पूँछवाला कोई पुरूष मुझे मदद कर रहा था.... क्या वे हनुमानजी थे ?"
वसुदेव जी कहते हैं- "हाँ, हाँ, बेटा ! वे हनुमान जी ही होंगे। उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की।"
वसुदेव जी बेटा मानते हैं तो श्रीकृष्ण भी उनके साथ पुत्रवत् व्यवहार ही करते हैं। रानियों के लिये, पत्नियों के लिये जो पूरे पति हैं और पुत्रों के लिए जो पूरे पिता हैं अर्थात् जहाँ भी देखो, जिसके साथ भी देखो, वे सच्चिदानंदघन आनंदकंद श्रीकृष्ण पूरे के पूरे हैं। इसीलिए श्रीकृष्ण को पूर्णपुरूष कहा गया है।
शरीर विज्ञान एवं मनोविज्ञान के ज्ञाताओं का कहना है कि हर पुरूष में स्त्रीत्व छिपा होता है और हर स्त्री में पुरूषत्व छिपा होता है। किसी पुरूष में 70 प्रतिशत पुरूष का स्वभाव है तो 30 प्रतिशत स्त्री का, किसी स्त्री में 40 प्रतिशत पुरूषतत्त्व है तो 60 प्रतिशत स्त्रीतत्त्व, किसी में 50-50 प्रतिशत दोनों होता है।
यदि स्त्री में पुरूषतत्त्व अधिक हो जाता है तो वह स्त्री घर में पुरूष हो जाती है और पुरूष में पुरूषतत्त्व अधिक होता है तो वह स्त्री को अपनी आज्ञा में रखता है।
श्रीकृष्ण पूरे पुरूष हैं और राधा पूर्ण स्त्री हैं, रूक्मिणी पूरी स्त्री नहीं है। राधा में पुरूषतत्त्व नहीं है और श्रीकृष्ण में स्त्रीतत्त्व नहीं है, इसलिए श्रीकृष्ण यदि अकेले होते तो इतने नहीं चमकते क्योंकि प्रकृति और पुरूष का संयोग चाहिए।
आधी प्रकृति और आधा पुरूष हो उसमें भी आनंद नहीं है लेकिन पूरी प्रकृति और पूर पुरूष का जीवन देखना हो तो श्रीकृष्ण का जीवन है, इसलिए श्रीकृष्ण से पूर्व राधा का नाम लिया जाता है.... राधा-कृष्ण।
महावीर पूर्ण पुरूष भी नहीं हैं और पूर्ण स्त्री भी नहीं हैं। वे वर्षों तक तप करते रहे। यदि उनके आगे तुम बंसी या मोरपंख ले जाओ तो वे नाराज हो जाएँगे, बोलेंगे कि यह क्या पागलपन है ? लेकिन श्रीकृष्ण का जीवन इतना समग्र है कि बस ! बंसी लाओ तो वह भी बजा देंगे, शंख रखो तो उसमें भी फूँक मार देंगे और ढोलक रखो तो वह भी बजा लेंगे, मोरपंख दो तो वह भी मुकुट में लगा लेंगे ऐसा श्रीकृष्ण का समग्र जीवन है।
भगवद् गीता के छठवें अध्याय में योग की महिमा बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं-
तपस्विभ्योऽधिको
योगी
ज्ञानिभ्योऽपि
मतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको
योगी
तस्माद्योगी
भवार्जुन।।
'योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे अर्जुन ! तू योगी हो।'
(गीताः 6.46)
श्रीकृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वैसे तो उपदेश का नियम है कि जो श्रद्धालु हो, जिज्ञासु हो, वह नीचे बैठे, वक्ता का सिंहासन ऊँचा हो तब उपदेश दिया जाता है लेकिन श्रीकृष्ण का जीवन इतना अनुपम है कि श्रोता ऊपर बैठा है और वक्ता रथ हाँक रहा है। युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है अर्थात् उनके लिए कोई नियम नहीं है। सब सर्वोत्तम है। वे जो करते हैं वह भी सब उत्तम है क्योंकि उनको सदा अपना ही स्वरूप सामने प्रत्यक्ष होता है कि मैं ही अर्जुन होकर शोक कर रहा हूँ और श्रीकृष्ण होकर उपदेश दे रहा हूँ और यहाँ का ज्ञान वहाँ पहुँच जाये तो घाटा ही क्या है ! यही तो उनके जीवन की पूर्णता है।
सौराष्ट्र में एक जगह श्रीकृष्ण का मंदिर है उससे एक मील की दूरी पर रूक्मिणी का मंदिर है। श्रीकृष्ण के इर्द-गिर्द गोपियाँ हैं, राधा हैं लेकिन रूक्मिणीजी एक मील दूर है। क्यों....? क्योंकि रूक्मिणी पूर्ण स्त्री नहीं है, उसमें पुरूष छिपा है जबकि श्रीकृष्ण पूर्ण पुरूष हैं और राधा पूर्ण स्त्री हैं। राधा का कोई आग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है। राधा ऐसी स्त्री हैं कि उनमें पुरूषतत्त्व एक प्रतिशत भी नहीं है। ऐसी पूर्ण शरणागति है राधा की.... इसलिए राधा का नाम पहले आता है, बाद में श्रीकृष्ण का।
प्रकृति अपनी महिमा में पूरी हो और पुरूष भी अपनी महिमा में पूरे हों तो वे राधा-कृष्ण जैसे हो जाते हैं। उस मंदिर में ऐसा दिखाया गया है कि श्रीकृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजा रहे हैं और राधा साथ में हैं, जबकि रूक्मिणी का मंदिर एक मील की दूरी पर है जिसमें प्रतिमा की आँखे तिरछी हैं, जो फरियाद करने का स्वरूप है।
श्रीकृष्ण बताते हैं कि जिसके जीवन में कुछ फरियाद है, कुछ आग्रह है, वह मुझसे मीलों दूर है और जिसके जीवन में न आग्रह है, न फरियाद है वह मेरे नृत्य में नृत्य हो जाता है, मेरे साथ एक हो जाता है।
एक बार गौएँ चराते-चराते श्रीकृष्ण के बालसखाओं को बड़ी जोरों की भूख लगी। तब श्रीकृष्ण ने कहाः "जाओ, यज्ञ करने वाले जो कर्मकाण्डी हैं उनके पास से भोजन ले आओ।"
सब ग्वालबाल गये और उनसे भोजन माँगा। वे कर्मकाण्डी अपने को शुद्ध मानते हैं और श्रीकृष्ण को मूर्ख मानते हैं। वे कहने लगेः "अरे ! गोपबालकों ! यज्ञ तो पूरा कर लेने दो !''
यदि जीव को देहाध्यास है तो श्रीकृष्ण कुछ माँग रहे हैं फिर भी उन्हें कुछ देगा नहीं लेकिन स्वाहा... स्वाहा... करके आहूतियाँ डालेगा। स्वाहा-स्वाहा करके भी तुम क्या चाहते हो ? ...स्वर्ग। और स्वर्ग से क्या चाहते हो.....? थोड़ा सा सुख।
अरे ! सुख का सागर तुम्हारे पास उमड़ रहा है भैया.....!
श्रीकृष्ण के लिए उन्होंने भोजन नहीं दिया। श्रीकृष्ण ने कहाः "ये आधे पुरूष हैं। जाओ, गोपियाँ पूर्ण स्त्री हैं। उनके पास जाओ, वे भोजन दे देंगी।"
स्त्री का हृदय जरा नरम होता है। उन गोपियों ने, ब्राह्मण-पत्नियों ने ग्वालों को भोजन दे दिया।
श्रीकृष्ण सुख के लिए कुछ नहीं चाहते क्योंकि श्रीकृष्ण का जीवन पूर्ण विकसित जीवन है, मुस्कान का जीवन है। वे स्वयं में पूर्ण हैं।
श्रीकृष्ण की गीता पर असंख्य टीकाएँ हुई हैं। तिलक ने कर्मवाद ढूँढ लिया। गाँधी ने अहिसा परमो धर्मः ढूँढ लिया। शंकराचार्य ने अद्वैत, रामानुज ने भक्तिमार्ग, योद्धाओं ने युद्ध करने का कर्त्तव्य और सांख्यवादियों ने दर्शन ढूँढ लिया।
अर्थात् जिस जिसने जैसे चश्मे से देखा, श्रीकृष्ण की गीता में उसे वैसा ही मिल गया। जिसने नजर से जहाँ देखा, वहाँ श्रीकृष्ण पूर्ण ही दिखे क्योंकि श्रीकृष्ण सर्वत्र स्वयं में पूर्ण हैं फिर तुम जिस नजर से देखो। योद्धाओं में देखो तो श्रीकृष्ण के समान कोई योद्धा नहीं। राजनीति में देखना हो तो श्रीकृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ नहीं और राजा के रूप में भी देखो तो श्रीकृष्ण पूर्ण हैं।
समाज के नैतिक मूल्य और सामाजिक जीवन के उत्थान के साथ-साथ बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करवाना, यह श्रीकृष्ण का कार्य कर रहा है।
यदि उनके किसी व्यवहार में समाज ने फरियाद की है तो एक बात में की हैः "जब श्रीकृष्ण कंस मामा को स्वधाम पहुँचाकर मथुरा में रहने लगे तब पड़ोसी राजा उत्पात करने लगे क्योंकि वे सब कंस के ही आदमी थे। मथुरा की जनता ने श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि जब से आप मथुरा आये हैं, यहाँ की जनता को बहुत सहन करना पड़ रहा है।
जिस नगर में, जिस राज्य में झगड़े होते रहते हैं, वहाँ की प्रजा को सहन करना ही पड़ता है। श्रीकृष्ण जब इससे अवगत हुए तो उन्होंने जाना कि कंस का विनाश करने से और राजाओं ने वैरभाव मोल ले लिया है, इसलिए आपत्ति आ रही है। अतः श्रीकृष्ण समाज के हित का ख्याल रखते हुए मथुरा छोड़कर अज्ञातवास में चले गये।
अज्ञातवास में भी श्रीकृष्ण और बलराम चुप नहीं बैठे। वहाँ श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र एवं बलराम ने हल की रचना की। वह भी अपने लिये नहीं वरन् जिन्होंने कहा कि 'श्रीकृष्ण आये तब से हमारे ऊपर आपत्तियाँ आईं।' उन्हीं की सेवा व कल्याण के लिए सुदर्शन की रचना की। श्रीकृष्ण की कितनी उदारता है ! कितनी करूणा है ! कितनी समता है और कितना रचनात्मक जीवन है !
श्रीकृष्ण कभी आलसी या प्रमादी होकर नहीं बैठे हैं। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्त्तृत्व की आसक्ति नहीं है। फल भोग रहे हैं लेकिन भोक्तृत्व का भाव नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आलोचनाएँ सुनकर त्यागपत्र दे दिया। नहीं। वे स्वयं में पूर्ण हैं।
राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं और रण छोड़कर भागने का मौका मिला तो भाग रहे हैं। यह नहीं सोचते कि लोग मुझे कायर कहेंगे। नहीं... ऋषि का वरदान फलित करने के लिए भाग रहे हैं। कितनी समता है !
श्रीकृष्ण राजनीति में भी पूरे हैं। उनमें अपने सुख के लिए राजनीति का कपट न था अपितु धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश, आसुरी वृत्तियों के दमन तथा सात्त्विक वृत्ति का सृजन करने के लिए, प्रजा के पालन के लिए तथा आसुरी वृत्तिवालों को भी अपने धाम में ले जाने के लिए श्रीकृष्ण उसका उपयोग करते थे।
श्रीकृष्ण के जीवन में सर्वोच्च एवं प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में अपने स्व के छन्द में मस्त रहते थे। ऐसा नहीं कि श्रीकृष्ण आये और उनको मिसरी ही खाने को मिली, पूतना जहर लेकर भी तो आयी थी ! ऐसा नहीं कि उनके जीवन में चारों तरफ सफलताएँ ही थी और ऐसा भी नहीं कि श्रीकृष्ण सबके लिये मधुर-मधुर ही बोलते थे। वे डाँटते इस तरह थे मानो तलवार की तीक्ष्ण धार।
जब भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन के यहाँ संधिदूत बनकर गये तो दुर्योधन ने आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन कीजिये।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "दुर्योधन ! तुम्हारे यहाँ मैं भोजन क्यों करूँ ? तुझे पता नहीं कि भोजन दो कारण से लिया जाता है। पहला तो जहाँ प्रीति होती है, वहाँ लिया जाता है। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं और मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं, फिर मैं तुम्हारे घर में भोजन कैसे कर सकता हूँ ? दूसरा, किसी के यहाँ भोजन उस व्यक्ति को करना पड़ता है जो अन्न में महंगा हो तो मैं अन्न में महँगा भी नहीं। अन्न तो मुझे कहीं भी मिल जायेगा।
इतना स्पष्ट कहने में भी श्रीकृष्ण पूर्ण समर्थ थे और थोड़ी सी छाछ के लिए नाचने को भी पूर्ण तैयार थे। कूटनीतिज्ञ कहते हैं कि श्रीकृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। अरे, श्रीकृष्ण का जीवन ऐसा समग्र है कि जो कुछ उनमें देखना चाहो, वह सब मिल जायेगा क्योंकि वे जो भी करते हैं, वह पूर्ण ही होता है। विनोद भी करेंगे तो पूरा करेंगे, रास्ता भी बतायेंगे तो पूरा बतायेंगे, भाग भी जायेंगे तो पूरे भाग जायेंगे, नाचेंगे तब भी पूरे नाचेंगे।
महाभारत के युद्ध के आरंभ के युद्धक्षेत्र में अलग-अलग योद्धाओं ने अलग-अलग शंख बजाये। किसी ने कुछ बजाया तो किसी ने कुछ। श्रीकृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। पाँचजन्य का बजाना इस बात का द्योतक है कि हमारी जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनमें प्राण फूँकता हूँ अर्थात् मैं पूरे का पूरा यहीं हूँ। दूसरे जो योद्धा थे उनमें से किसी का एक हिस्सा युद्धभूमि में था अर्थात् किसी की एक इन्द्रिय, किसी की दो और किसी की तीन इन्द्रियाँ वहाँ पर थीं लेकिन श्रीकृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ उनकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के साथ पूर्ण होते हैं अर्थात् श्रीकृष्ण जहाँ भी होते हैं पूरे होते हैं, जबकि हम बँटे हुए होते हैं।
हम जब सत्संग में होते हैं, तब कहीं और भी होते हैं। दुकान पर होते हैं तो थोड़े घर भी होते हैं और घर पर होते हैं तो थोड़े बाजार में भी होते हैं। बाजार में होते हैं तो थोड़े परिवार में भी होते हैं। परिवार में होते हैं तो थोड़े धर्म में भी होते हैं लेकिन श्रीकृष्ण जैसे व्यक्ति जहाँ भी होते हैं, पूर्ण ही होते हैं।
चीरहरण-लीला बताती है कि चीरहरण करके श्रीकृष्ण वृक्ष पर बैठ गये हैं और बंसी बजा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे ? कुछ नहीं। विनोद में भी पूरे। पूरा वही हो सकता है जिसका जीवन विकारी नहीं। जिसके जीवन में सहजता है वह तो पूर्ण ही है।
कई लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने ऐसा किया, वैसा किया, चीरहरण-लीला की। वास्तव में चीरहरण लीला का आध्यात्मिक अर्थ तो यही है कि जब तक तुम अपने अहंकाररूपी वस्त्र को, देहाध्यासरूपी वस्त्र को अर्पित नहीं कर देते तब तक तुम मेरा नाद भी नहीं सुन सकते। यदि अपना अहंकाररूपी वस्त्र श्रीकृष्ण को दे दोगे तो फिर तत्त्वमसि का संगीत सुनने के भी अधिकारी हो जाओगे।
श्रीकृष्ण के जीवन में न पुकार है न आवाज है। श्रीकृष्ण के जीवन में केवल प्रसन्नता है। श्रीकृष्ण नाचते हैं तो पूरे नाचते हैं, हँसते हैं तो पूरे हँसते हैं। हम लोग हँसते हैं तो थोड़ा इज्जत-आबरू का, अड़ोस-पड़ोस का ख्याल रखकर हँसते हैं। आप हँसोगे तो इधर-उधर देखकर हँसोगे फिर भी पूरे नहीं हँसोगे। रोओगे तब भी पूरे नहीं रोओगे, नाचोगे तो भी पूरे नहीं नाचोगे किन्तु श्रीकृष्ण जिस समय जो करते हैं, पूरा करते हैं। खाते हैं तो पूरा, डाँटते हैं तो पूरा, नाचते हैं तो पूरा। इस अवतार ने, आदिनारायण ने हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही सारी लीलाएँ की हैं।
साधुओं को, सज्जनों को पूर्ण जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाने के लिए तथा जो दुर्जन हैं उनका मार्ग बदलने के लिये जो अनादि ब्रह्म का अवतरण हुआ है, उसका नाम है अवतार, फिर चाहे उसे श्रीराम कह दो या श्रीकृष्ण कह दो, मर्जी तुम्हारी है।
श्रीकृष्ण का जीवन नितांत सहज जीवन है। साधारण आदमी जो कुछ करता है, कुछ पाने के लिए या कुछ हटाने के लिए करता है लेकिन श्रीकृष्ण न पाने के लिए करते हैं, न हटाने के लिए, अपितु जो भी करते हैं, उसमें से पूर्णता की खबरें स्वतः ही प्रस्फुटित होती हैं। इसीलिए श्रीकृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
प्रेमस्वरूप
श्रीकृष्ण
अहंकार के सिर पर द्वेष होता है, धारणाएँ होती हैं, मान्यताएँ होती हैं, बाह्य आडम्बर होता है लेकिन प्रेम तो एकदम आवरणरहित होता है। प्रेम के पास कोई पकड़ नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, आडम्बर नहीं होता। प्रेम के पास बस, मुस्कान है, बलिहारी है, अहोभाव है, धन्यवाद है।
श्रीकृष्ण के भक्तों को देखोगे तो नाचते मिलेंगे, गाते मिलेंगे, गुनगुनाते मिलेंगे फिर चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, नरसिंह मेहता हों या मीरा बाई हों।
चैतन्य महाप्रभु जब पूर्वाश्रम में निभाई पंडित थे तब शास्त्रार्थ में बड़े-बड़े विद्वानों को भी परास्त कर देते थे। तर्क में उनका कोई सामना नहीं कर सकता था। उन्होंने देखा कि तर्क से लोगों को परास्त करने में अहंकार को तो थोड़ा पोषण मिलता है परंतु गंभीर शांति नहीं है, आनंद नहीं आता।
प्रेम के सिवाय आनन्द कहाँ है ? निर्दोषता के सिवाय आनन्द कहाँ है ? एक छोटा सा बालक निर्दोषता से नाचता है, तोतली भाषा बोलता है तो अपने माता-पिता की थकान उतार देता है क्योंकि बालक इस समय निरहंकारी है, निर्वासनिक है इसलिए बालक की मुस्कान से उसके माता-पिता दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीकृष्ण जब तक जिये छोटे होकर ही जिये, बालक होकर जिये।
जीवन जीने के दो ढंग हैं- एक तो एकदम छोटे होकर जियें, इतने छोटे होकर कि जैसे बालक जीता है। या फिर एकदम बड़े होकर जियें.... इतने बड़े हो जाओ कि तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ बचे ही नहीं। स्वयं को इतना फैला दो, इतना व्यापक कर दो कि केवल तुम ही तुम रहो।
श्रीकृष्ण प्रेमस्वरूप हैं। अक्रूर जी जब श्रीकृष्ण को लिवाने बृज जाते हैं तब सोचते हैं कि श्रीकृष्ण मुझे देखकर कही अन्तर्धान न हो जावें, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं कि श्रीकृष्ण मुझे मिलेंगे ही नहीं। ऐसा सोचते-सोचते अक्रूर जी निराश होते हैं, हताश होते हैं लेकिन जब श्रीकृष्ण की कृपा की ओर, सहजता की ओर, सरलता की ओर तथा प्रेम के विषय में सोचते हैं तो अक्रूर जी में हिम्मत आती है। उनका रथ जब बृज के करीब पहुँचता है तो अक्रूर जी को श्रीकृष्ण के पदचिह्न दिखाई पड़ते हैं। वे रथ से उतर कर चरणरज को अपने शरीर पर मलते हैं। फिर कहीं पदचिह्न दिखते हैं तो उस पदधूलि से अपने मन को, तन को ललाट को पावन करते हैं।
अक्रूर जी जब स्वयं की ओर देखते हैं तो निराश हो जाते हैं, ऐसे ही जीव भी जब अपने कर्मों की ओर देखेगा तो निराश हो जायगा, अपनी नादानी की ओर देखेगा तो निराश हो जायेगा लेकिन जब अपने स्वरूप की ओर, अपनी आत्मा की ओर देखेगा, श्रीकृष्ण के प्रेम की ओर देखेगा तो उसमें हिम्मत आ जायेगी।
गोपियाँ जब बंसी का नाद सुनती थीं तो उसकी ध्वनि में कौन-सा शब्द और कौन सा अर्थ है उसकी चिन्ता नहीं करती थी। बस, ध्वनि किसकी है ? मेरे कन्हैया की है। वह पूर्ण पुरूष हैं कि अपूर्ण... वह बृजराज का पुत्र है कि साधारण मनुष्य का..... वह अन्तर्यामी है कि एक साधारण ग्वाल है..... गोपियों ने यह कभी नहीं सोचा। गोपियाँ तो बस, प्रेम करती थीं और प्रेम के आगे कोई नेम (नियम) नहीं होता, प्रेम के आगे कोई फरियाद नहीं होती, प्रेम के आगे कोई आडंबर नहीं होता।
प्रेम एक ईमानदारी है, एक सच्चाई है। चैतन्य को जब प्रेम उमड़ता है तो कभी नाचने लग जाते, कभी चुप हो जाते। मीरा को जब प्रेम उमड़ता को कभी प्यारे के लिए नाचती, कभी उसका चित्र देखकर हँसती तो कभी उसी के विरह में रोती थी।
प्रेम ईमानदारी सिखाता है जबकि स्वार्थ बेईमानी सिखाता। प्रेम सहजता और सरलता सिखाता है जबकि स्वार्थ कपट और कुटिलता सिखाता है।
आज का मनुष्य बाहर से चतुर व भीतर से बेईमान बन गया है। वह न ईमानदारी से रो सकता है न हँस सकता है, न नाच सकता है न कह सकता है और न ही ईमानदारी से सुन सकता है।
तुम प्रार्थना करना कि हे भगवान ! हमें आज जन्माष्टमी के दिन निर्दोषता सिखा दो। हँसना आये तो हम भरपेट हँस लें, रोना आये तो हम से लें, तेरे लिये नाचने का मन हो तो हम नाच लें। गीत गाना आय तो गा लें किन्तु हे ईश्वर ! बस, हम न बचें। हमारी सामाजिक मान्यताएँ हैं, धारणाएँ हैं, वे न बचें। हे विश्वेश्वर....! हे गोवर्धनधारी......! हे गोपाल....! हे नंदनंदन.....! हे भक्तवत्सल....! हे गिरधारी......! हे मुरलीधर......! हे गोविन्द.....! हे कन्हैया.....! बस तू इतनी कृपा करना कि हम न बचें, तू ही रह जाय। कृष्ण कन्हैया.... बंसी बजैया.... वृन्दावन की कुँज गलिन में..... साधक की गलियों में.... ठुमक-ठुम्मक रास रचैया.....
वह अभी भी, इस समय, यहाँ भी है। वह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी विवशता को भी देख रहा है। वह अन्तर्यामी-रूप से सदा तुम्हारे साथ है। शर्त यही है कि तुम भीतर डूबते जाओ....
तुम जितना भीतर डूबोगे, प्रेम करोगे, निर्दोष बनोगे, पुकार करोगे उतने ही बाहर के लोगों की नजर में तुम पागल दिखोगे, किन्तु भीतर तुम सचमुच 'गल' को पा रहे होगे।
अक्रूरजी के नेत्रों से आँसू बह रहे थे, हृदय से भाव बह रहा था। भक्त जहाँ भगवान के भाव में दो आँसू गिरा देता है, वह जगह भी पावन हो जाती है। वहाँ का वातावरण भी रिद्धि-सिद्धि से पूर्ण हो जाता है।
अक्रूर जी भगवान श्रीकृष्ण से मिले। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गले लगाया, स्नानादि करवाया, वस्त्र पहनवाये तथा कुशलक्षेम पूछकर यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार किया। उन्हें कंस का कोई भय नहीं था। जिसके जीवन में कोई पकड़ नहीं, उसको शत्रु का भय कैसे हो सकता है ? अक्रूर जी ने श्रीकृष्ण को षडयंत्र की सारी व्यवस्था बता दी।
कंस के आमंत्रण पर श्रीकृष्ण जा रहे हैं। कंस ने महल के अतिथिनिवास में उनके लिए व्यवस्था की लेकिन श्रीकृष्ण कहते हैं कि मेरे माँ-बाप जेल में पड़े हैं और मै महल का अतिथि बनूँ ? यह नहीं हो सकता। हम तो जंगल के रहवासी, जंगल में गौएँ चराने वाले, हमें तो किसी जंगल अथवा बगीचे में रहने की व्यवस्था करवा दो।
श्रीकृष्ण ने तीन दिन बगीचे में निवास किया। महल में रहने पर खुलकर बात नहीं हो सकती, निर्दोष प्रेम भी नहीं बँट सकता था बाँटा भी नहीं जा सकता। जैसे तुम किसी के बंगले में जाकर रहते हो तो अपने ही परिवार के सदस्य या किसी मित्र से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। स्थान का भी अपना नियम होता है, स्वभाव होता है।
श्रीकृष्ण ने तीन दिन में लोगों को इतना तैयार कर दिया कि जिस सम्राट को मारा उसके अंगरक्षक आँख तक न उठा सके, इतना उन्हें अपना बना लिया। प्राणी मात्र प्रेम चाहता है और प्रेम तो श्रीकृष्ण के रोम रोम से टपकता है इसलिए तो शत्रु तक उनके मित्र बन गये फिर भक्तों की तो बात ही क्या है ?
एक बार श्रीकृष्ण के शरीर पर फफोले पड़ गये और शरीर में पीड़ा होने लगी। पटरानियाँ घबरा गईं। उद्धव के आँसू रूकते नहीं हैं। फफोले पड़े कैसे ? उसका कारण भी रहस्य युक्त था। प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे किसी ग्रहण के समय पटरानियाँ स्नान करने को आईं। भारत में ऐसी प्रथा है कि जब सूर्य ग्रहण एवं चंद्रग्रहण उतरते हैं नदी से संगमस्थान के स्नान से भी समुद्रस्नान का फल अधिक माना जाता है।
सागर तट पर एक हिस्से में ग्वालबाल एवं अन्य लोग स्नान कर रहे थे एवं दूसरे एकांत हिस्से में पटरानियाँ स्नान कर रही थीं। रानियों ने देखा कि उन ग्वालबालों एवं गोपियों के बीच एक महातेजस्वी नारी पटरानी जैसी चमक रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कौन होंगी ?
उन्होंने सोचाः 'चलो, जरा देखें।' जाकर उन्होंने कहाः "आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ नहाओ।"
तब वह परम तेजस्वी देवी कहती हैः "नहीं, हमें वहाँ आने का अधिकार नहीं है। वे मुझे जिस जगह पर छोड़कर गये हैं मेरा स्थान वहीं होना चाहिए।" इतना कहते-कहते उसकी आँखे भर आईं।
तब उन रानियों ने कहाः "तुम्हारा स्वागत करने के लिए और तो क्या दें तुम्हें ? हम दूध का प्याला तुम्हें देते हैं, इसे अस्वीकार मत करना।"
वह तेजस्वी महिला कहती हैः "मैंने आभूषण और कीमती वस्त्र धारण करना छोड़ दिया है। मक्खन और मिश्री ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। अब आप लोग बोलते हो तो दूध पी लेती हूँ किन्तु हे मेरे कृष्ण ! दुबारा ऐसा आग्रह का दिन मत लाना।"
श्रीकृष्ण की याद में उसकी आँखों से आँसू टपक पड़े और मुख से आह निकल पड़ी जिसके कारण दूध में विशेष गर्मी आई। वह दूध उसके पेट में गया, और फफोले श्रीकृष्ण को पड़ गये।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "हे उद्धव ! वह कोई साधारण रानी नहीं थी अपितु रानियो की रानी, महारानी राधा थी। राधा ने 'आह' करके दूध पिया था। उसके विरह की तपन ने मेरे शरीर को तपाया है जिसके कारण मेरे शरीर पर फफोले पड़ गये हैं।
उद्धव पूछते हैं- "प्रभु ! किस वैद्य को बुलायें ? कौन-सा इलाज करवायें ? आप इतने छटपटा रहे है अतः आप ही बताइये कि इसका क्या इलाज है ?"
श्रीकृष्णः "मेरे दर्द की दवा वैद्यों के पास नहीं है। इसका एकमात्र इलाज यह है कि उद्धव ! तुम राधा के पास जाओ और उसके आँसू रूकवाओ। उसे आश्वासन देकर आओ और जिस पल्लू से वह अपने आँसू पोंछ रही हैं वह पल्लू (साड़ी का पल्ला) ले आना। आँसूओं से भीगा हुआ वह पल्लू इन फफोलों पर लगाओगे तभी ये मिट सकते है, वरना नहीं मिट सकते।"
देखो.....! प्रेम के बदले में श्रीकृष्ण कैसा प्रेम देते है। श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थीं जो सदा उनके साथ रहती थीं लेकिन उनमें से किसी का भी नाम श्रीकृष्ण के साथ नहीं आता परन्तु भीतर से जो साथ में थी उस राधा का नाम आता है। राधाकृष्ण....
'सत्यभामा-कृष्ण, रूक्मिणी कृष्ण, जामवंती-कृष्ण आदि नहीं बोला जाता है जबकि 'राधा-कृष्ण' का नाम बड़े प्यार के साथ लिया जाता है।
'राधा' को उलट दो तो 'धारा' बन जाता है। धारा अर्थात् वृत्ति। चैतन्य से जो वृत्ति निकलती है वह यदि संसार की ओर जाती है तो तुच्छ हो जाती है किन्तु वही वृत्ति चैतन्य से निकलकर चैतन्य को ही याद करती है तो चैतन्य भी उसकी याद में ऐसा हो जाता है।
वह 'राधा' तुम्हारे पास भी है और 'श्रीकृष्ण' भी तुम्हारे पास ही हैं। सच पूछो तो तुम नहीं हो, राधाकृष्ण ही हैं। चैतन्य और चैतन्य की सुरता ही है लेकिन हमारा अहंकार बोलता है कि 'मैं हूँ' इसलिए 'राधाकृष्ण' छुपे हुए हैं। छुपे हुए राधाकृष्ण को जीवन में प्रगट करने का यही अवसर है।
जप से, कीर्तन से, ध्यान से मनुष्य में जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं वे जागृत होती है। ग्वाल-गोपियों के बीच छुपी हुई जो 'राधा' है अर्थात् जीवन में अनेक वृत्तियों के बीच छुपी हुई जो धारा है, ब्रह्माकार वृत्ति है, वह प्रगट हो सकती है। बस शर्त इतनी ही है कि तुम उससे प्रेम करो और वह तो प्रेमस्वरूप है ही। तुम्हारी पुकार सुनकर वह अवश्य ही प्रगट हो जायेगा.... बस, जरा अन्तरात्मा से पुकारना सीख लो भैया....!
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
पूतना-प्रसंग
भक्त जब भाव में होते हैं, प्रेम में होते हैं तो आनंद होता है और जब भाव एवं प्रेम में कमी होती है तो भक्त विषयों में गिर पड़ता है। इसी बात को समझाने के लिए भागवत में पूतना प्रसंग आता है।
जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण का जन्म होता है और छः दिन बाद चतुर्दशी को पूतना गोकुल पहुँचती है। पूतना के कई अर्थ लगाये गये है- 'पू' अर्थात् 'पवित्र'। 'तना' अर्थात् नहीं। यानि जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। उसे काम का भी रूप बताया गया है। भक्त के अन्दर का आनन्द जब नष्ट हुआ अर्थात् नंदबाबा गोकुल छोड़कर मथुरा गये तो गोकुल में अपशकुन होने लगे और पूतना गोकुल में पहुँच गयी।
नंद के आगे 'आ' रख दो तो वह आनंद हो जायेगा। आनंद गोकुल (गो-यानि इन्द्रियाँ और कुल यानी समूह) छोड़कर जाता है। तुम्हारा शरीर इन्द्रियों का समूह है। तुम्हारे भीतर से अर्थात् गोकुल से आनंद जब दूसरी जगह चला जाता है तो तुम्हारे अन्दर पूतना अर्थात् अपवित्रता आ जाती है, विकार आ जाते हैं। आनंद जब भीतर रहता है तो विकार जोर नहीं पकड़ते हैं और जब आनन्द खत्म हो जाता है तब विकार जोर पकड़ते है तथा अपशकुन हो जाता है।
योगियों का कहना है कि तुम आत्मानंद में मस्त होने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे पास पूतना नहीं आयेगी। ऐसा आहार न करो जिससे तमोगुण बढ़ जाये। ऐसा व्यवहार न करो जिससे रजोगुण बढ़ जाये। ऐसे वातावरण में न जिओ जिससे तुम्हारे मन की शांति और आनंद नष्ट हो जायें। आप प्रातः काल उठो, स्नान करके प्राणायाम करो।
स्नान से शरीर शुद्ध होता है। प्राणायाम से अंतःकरण शुद्ध होता है। प्राणायाम करने के बाद थोड़ा ध्यान करोगे तो तुम्हारा आनन्द बना रहेगा। जैसे गोकुल में नंदबाबा के रहने पर पूतना नहीं आ सकती, वैसे ही इन्द्रियों के समूह रूपी गोकुल (शरीर) में यदि सदा आनंद रहेगा तो वासनारूपी पूतना नहीं आ सकती। वासनारूपी पूतना से बचने के लिए तुम्हारे चित्त को सदा साक्षी भाव से देखते रहो।
जब भी वासना उठे तब तुम उसके दृष्टा हो जाओ क्योंकि जब वासना को बुद्धि सहयोग देती है तब वासना क्रियाशील होती है। वासना को यदि बुद्धि सहयोग न दे तो वासना में क्रिया करने की शक्ति नहीं है। जब किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि सहयोग दे देती है तब आपका शरीर, आपकी इन्द्रियाँ और आपका मन उस कार्य को करने में लग जाते हैं।
जब आपका कोई संकल्प होता है तब तुरन्त ही विकल्प भी उठता है। आपका अच्छा संकल्प बुरे संकल्प को काटता है तो आप सफल हो जाते हैं। बुरी वासना को अच्छी वासना द्वारा काट डालना चाहिए। जब बुरी वासना को अच्छी वासना काट नहीं पाती तब मनुष्यरूपी शिशु उस बुरी वासनारूपी पूतना के हाथों मारा जाता है लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि के, मन के तथा कर्म के दृष्टा बन जाएँ तो पूतना रूपी वासना के फंदे से अवश्य बच सकते हैं।
पूतना शिशुओं को मार डालती थी अर्थात् जो समझ मे, ज्ञान में, सयंम में शिशु हैं, बालक हैं, उन्हें पूतना मार देती है लेकिन जो श्रीकृष्ण जैसे कुशाग्रबुद्धि हैं उन्हें पूतना मार नहीं पातीं अपितु स्वयं उनके हाथों मर जाती है।
पूतना जब गोकुल आती है तो एक बड़े घराने की स्त्री का रूप लेकर आती है। उस समय श्रीकृष्ण झूले में झूल रहे थे। पूतना यशोदा से पूछती हैः "मैं तुम्हारे बेटे को जरा ले लूँ ?"
यशोदा कहती हैः "ले लो।"
जब पूतना लेने जाती है तो श्रीकृष्ण मुख घुमा देते हैं, करवट बदल देते हैं। यदि वह बायें जाती है तो श्रीकृष्ण दाँयें हो जाते हैं और दाँये जाती है तो बाँये हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने छः बार करवट बदली।
अलग-अलग भक्ति के आचार्य करवट बदलने के अलग-अलग अर्थ लगाते हैं। कोई कहता है कि श्रीकृष्ण ने करवट यह सोचकर बदली होगी किः 'अरे ! मैं तो गोकुल में आया था मक्खन-मिश्री खाने और भक्तों को आनंदित करने के लिए। उन्हें तो अभी मैंने पूरा आनंद दिया नहीं, उनके साथ अभी खेला ही नहीं, इसके पहले ही इस राक्षसी के साथ खेलना पड़ता है। अभी तो मैं नन्हा-मुन्ना हूँ और इस मौसी के साथ अभी-अभी मुलाकात....? मैं आया तो था मक्खन-मिश्री खाने और यह वासनारूपी पूतना जहर ले आई।'
वासना भी तो जहर के समान होती है, इसलिए श्रीकृष्ण ने करवट ली।
कुछ लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने करवट यह सोचकर ली थी किः 'जो मुक्ति यशोदा को, नंदबाबा को, देवकी को वसुदेव को दूँगा, वही मुक्ति इसे भी देनी पड़ेगी क्योंकि इसका स्पर्श कर लिया है।'
'मक्खन मिश्री खिलाने वाले को भी मुक्ति और जहर पिलाने वाले को भी मुक्ति। देखो मेरी क्या माया है....!' अपनी माया को निहार कर श्रीकृष्ण करवट बदल रहे हैं।
कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि श्रीकृष्ण ने यह सोचकर करवट बदली किः 'यह सारा संसार मिथ्या है, करवटें ले रहा है। अब मैं भी इस मिथ्या जगत में मिथ्या आकृति लेकर आया हूँ तथा यह मिथ्या पूतना मेरी ओर आई है इसलिए इसमें एक मिथ्या घुमावा और भी डाल दो ताकि जगत को बताऊँ कि मैं भी घूम रहा हूँ और यह भी घूम रही है। जो भी दिख रहा है, सब घूम रहा है।'
तत्त्वज्ञानियों के लिए यह एक इशारा है, संकेत है।
खून
पसीना बहाता
जा या तान के
चादर सोता जा।
यह
नाव तो चलती
जायगी, तू
हँसता जा या
रोता जा।।
जब सब घूम रहा है, सब चल रहा है तो तुम्हारा दुःख कैसे अचल रहेगा ? तुम्हारा शत्रु कैसे अचल रहेगा ? तुम्हें जहर पिलाने वाला भी कैसे अचल रह सकता है ? यह भी अब चलने को है, इस शरीर से अलविदा होने को है, इसलिए श्रीकृष्ण ने करवट घुमाई होगी।
श्रीकृष्ण का जीवन ऐसा समग्र है कि आप जो भी चाहो, अर्थ लगा सकते हो और वह संभावित हो सकता है।
छः बार करवट बदलने के बाद आखिर श्रीकृष्ण पूतना की गोद में गये और उसने अपना दूध पिलाना चालू किया। वासना बाहर से तो सुन्दर दिखती है किन्तु भीतर से कुरूप होती है। पूतना भी भीतर से कुरूप और बाहर से सुन्दरी होकर आई थी। ऊपर-ऊपर से दूध दिख रहा था और भीतर जहर भरा था।
वासना में भी ऊपर से दूध अर्थात् सुख दिखता है किन्तु भीतर तो केवल दुःख ही भरा होता है। स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण की लीला में कदम-कदम पर तत्त्वज्ञान लेने वालों को तत्त्वज्ञान मिल जाता है, विनोदप्रेमियों को विनोद मिल जाता है, प्रेम लेने वालों को प्रेम मिल जाता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा ही मिल जाता है।
पूतना दूध के बहाने जहर पिलाती है किन्तु श्रीकृष्ण तो सब हजम कर जाते हैं। उन्हें वासना क्या कर सकती है जो स्वयं में पूर्ण हो ? अमृत तो उनके आगे अमृत है ही, किन्तु वे जहर को भी अमृत बना देते है। श्रीकृष्ण जब अधिक नोचने लगे तो पूतना बोलती हैः "बस.... बस..... मेरे अंगों को पीड़ा हो रही है। छोड़ो.....छोड़ो...."
श्रीकृष्ण कहते हैं- "मौसी ! मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं और यदि मैं पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। लोग स्वयं मेरे पास आते हैं। पूतना ! मैं तेरे पास नहीं आया था, तू स्वयं मेरे पास आई है।"
ज्ञानी पुरूषों के पास जब तुम जाते हो तो अपनी मर्जी से जाते हो लेकिन लौटोगे उनकी मर्जी से।
पूतना बोलती हैः "छोड़-छोड़.....।"
श्रीकृष्ण बोलते है- "हम जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं।"
भगवान के या ज्ञानी के हाथ में यदि यह जीव आ गया और भगवान ने या गुरू ने पकड़ लिया तो फिर वे उसे छोड़ते नहीं हैं। किनारे लगाकर, पार करके ही वे चुप होते हैं।
सिंह की दाढ़ में आया हुआ शिकार शायद छूट जाये लेकिन संत के हृदय में, भगवान के हृदय में आया हुआ व्यक्ति नहीं छूटता। वह पार होकर ही रहता है। थोड़ी देर-सबेर जरूर हो सकती है।
पयःपान कराने से पूतना को अत्यधिक पीड़ा होने लगी। उसने चिन्तन के बल से अपना जो नकली रूप बनाया था, वह पीड़ा के कारण गायब हो गया और वह असली राक्षसी के रूप में प्रगट हो गई। जब वासना असली रूप ले लेती है तो भयभीत भी होती है। जब पूतना असली राक्षसी के रूप में प्रगट हुई तो लोग मार डालेंगे इस भय से श्रीकृष्ण को लेकर आकाश में उड़ी। वासना आनंद को लेकर भागती है व गायब कर देती है।
देखो ! कथा बनाने वाले वेदव्यासजी की कितनी पवित्र बुद्धि रही होगी, कितनी उदार और विशाल बुद्धि रही होगी ताकि जो भावप्रधान व्यक्ति हैं, उन्हें भी ज्ञान मिल जाय !
वासना (पूतना) श्रीकृष्ण अर्थात् आनन्द के खजाने को लेकर उड़ी तो सही किन्तु लम्बे समय तक उड़ न सकी और श्रीकृष्ण की इच्छा से मामा कंस के बगीचे में जा गिरी जिससे बगीचा भी नष्ट हो गया।
कथा कहती है कि श्रीकृष्ण को लेकर पूतना जब उड़ने लगी तब गोकुल के सभी ग्वालबाल और गोपियाँ घर का काम छोड़कर नंगे पैर भागते-भागते मथुरा पहुँचे। उनकी नजर आकाश में श्रीकृष्ण की ओर होने के बावजूद भी किसी को कोई चोट नहीं आई।
कथाकार यहाँ कितनी सुन्दर बात समझा रहे हैं कि ग्वाल-गोपियों की नजर श्रीकृष्ण पर थी, वासना पर नहीं अपितु आनंदस्वरूप परमात्मा पर थी, अतः उन्हें कोई चोट नहीं लगी।
नजर यदि वासना पर होती है और संभल कर भी चलोगे तब भी चोट तो लग ही जायगी किन्तु परमात्मा पर यदि तुम्हारी नजर होती है तो फिर भले ही तुम देखकर न भी चलो, जैसे गोपियों का, ग्वालों का ध्यान श्रीकृष्ण की तरफ था तो उन्हें चोट नहीं लगी।
यदि नजर निर्वासनिक तत्त्व पर हो, ज्ञान पर हो, तो उसमें आपको चोट नहीं लगती है। न जन्म की चोट लगती है, न मृत्यु की चोट लगती है, न वियोग की चोट लगती है, न संयोग का आकर्षण होता है, न शोक की चोट लगती है न भय की ही।
यदि वासना आनंद को, आत्मा को दबाना चाहती है तो फिर आत्मदेव का प्रभाव ऐसा है कि वह भले ही छोटा सा नन्हा मुन्ना दिखता है फिर भी बड़ी से बड़ी वासनारूपी को नष्ट करना उसके बाँये हाथ का खेल है।
पूतना धड़ाम से गिरी किन्तु श्रीकृष्ण अछूते व सुरक्षित ही रहे। इससे सिद्ध होता है कि वासना चाहे कैसा भी रूप लेकर आनन्द को नष्ट करना चाहे किन्तु आनंदस्वरूप परमात्मा का कभी नाश नहीं होता अपितु वासना स्वयं ही नष्ट हो जाती है।
वासना से तुमने जो महल खड़े किये हैं, वासनाओं से तुमने जो उपलब्धियाँ की हैं वे तो मर जाती है, तुम कभी नहीं मरते, तुम्हारा आत्मारूपी कृष्ण कभी नहीं मरता। चाहे आकाश से तुम्हारा शरीर गिरे फिर भी तुम नहीं गिरते, तुम नहीं मरते। तुम ज्यों के त्यों अपनी महिमा में ही रहते हो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
'परित्राणाय
साधूनां......'
एक बार युद्ध के समय श्रीकृष्ण अर्जुन को भीष्म के पास भेजते हैं। अर्जुन भीष्म से पूछता हैः "दादा ! तुम मरोगे कैसे ?"
भीष्मः "मुझे मारने का सामर्थ्य तुममें और तुम्हारे सैनिकों में नहीं है।"
श्रीकृष्ण ने सिखलाकर भेजा था अतः अर्जुन पुनः पूछता हैः
"फिर भी दादा ! कोई तो उपाय होगा !"
भीष्मः "मुझे मारने का और कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि मैं स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करता इसलिए यदि युद्धक्षेत्र में कोई स्त्री मेरे सामने खड़ी हो जाय तो मैं धनुष नहीं उठाऊँगा।"
भीष्म के पास से लौटकर अर्जुन श्रीकृष्ण से पूछता हैः "हे श्रीकृष्ण स्त्री को युद्ध में कैसे लाया जाये ?"
श्रीकृष्णः "भीष्म स्त्रियों को नहीं मारते और यह भी जानते हैं कि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था, अतः तू उसको सामने रख और पीछे से तीर चला। भले ही भीष्म मेरे भक्त है लेकिन वे दुराचारी और अहंकारी के पक्ष में है। अहंकार को विसर्जित करने वालों के पक्ष में नहीं है इसीलिए वे मारने योग्य हैं।"
युद्ध में जब अर्जुन शिखंडी को भीष्म के सामने रखता है तो श्रीकृष्ण से पूछता हैः "कहीं दादा नाराज हो गये तो ?"
श्रीकृष्णः "तू तीर तो चला, वे नाराज नहीं होंगे क्योंकि वे वचन के पक्के हैं। यह मैं जानता हूँ।"
देखा जाये तो श्रीकृष्ण के व्यवहार से अनेक जगह संदेह हो सकता है। एक संत पुरूष भी अपने भक्त को नहीं मरवाना चाहते हैं और भगवान स्वयं ही धर्मात्माओं के शिरोमणि भीष्म को तीरों का निशाना बनवा रहे हैं।
परित्राणाय
साधूनां
विनाशाय च
दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय
संभवामि युगे
युगे।।
श्रीकृष्ण के वचन तो पूर्णतया सत्य हैं किन्तु हम लोगों की इतनी मति नहीं है कि हम उनकी लीला को समझ सकें। जैसे, आपका शरीर तो अपना ही है और आप अपने शरीर का अहित नहीं चाहते। फोड़ा आदि होने पर शरीर के किसी अंग को आप कटवा भी देते हैं, ऐसे ही श्रीकृष्ण समग्र संसार को अपना शरीर समझते हैं। समग्र में से यदि किसी का शरीर इधर-उधर हो जाये तो श्रीकृष्ण समझते हैं कि शरीर के मरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। साधक के हाथ से भीष्म मेरे सामने मरेंगे तो कोई हानि नहीं है। वैसे भी मूर्खों के संग में रहने की अपेक्षा तो साधक के हाथ से मरना श्रेष्ठ है, यह समझकर श्रीकृष्ण भीष्म को अर्जुन द्वारा मरवा देते हैं।
"कौरव तो बाहर के सुखों में उलझ गये हैं। उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी उनकी बुद्धि ही उनका साथ नहीं देती। ऐसे में यदि सज्जन पुरूष उनका साथ देते हैं तो उनका भी विनाश मुझे करवाना पड़ता है। क्रूरों के साथ यदि मेरा भक्त भी है तो उस भक्त के ऑपरेशन के लिए मुझे भी क्रूरता का थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ता है। यह भी मेरी करूणा है।"
खैर श्रीकृष्ण की महिमा तो श्रीकृष्ण ही जानें लेकिन भीष्म की गरिमा भी कम नहीं है। भीष्म इतने संयमी, श्रद्धालु, सदाचारी, ब्रह्मचारी व कृष्ण-भक्त हैं कि स्वयं श्रीकृष्ण उनका ध्यान करते हैं। फिर भी श्रीकृष्ण युद्ध के मैदान में भीष्म को बाण मारने की अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी श्रीकृष्ण में से भीष्म श्रद्धा नहीं जाती।
अर्जुन बाण चलाने में काँपता है किन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं- "तू बाण चला दे।" भीष्म इसे भी श्रीकृष्ण की कृपा समझते हैं। कितनी विशाल बुद्धि व धैर्य होगा भीष्म में...!
आज यदि गुरू किसी शिष्य को जरा-सा डाँट दें, जरा-सा अपमान कर दें तो....? अरे, हजार बार जिसे मान दिया और एक बार जरा सा अपमान कर दिया तो कहेंगे कि एकांत में डाँटा होता तो कोई बात नहीं लेकिन इतने लोगों के बीच मेरा अपमान कर दिया।
मेरे भाई अहंकार एकांत में थोड़े ही जाता है ! लोगों के बीच ही तो अहंकार फलता-फूलता है अतः लोगों के बीच किया गया अपमान ही तुम्हारे अहंकार की धुलाई करेगा।
जिसे
वे इश्क करते
है, उसी को
आजमाते हैं।
खजाने
रहमतों के इसी
बहाने
लुटवाते
हैं।।
श्रीकृष्ण की प्रत्येक क्रिया लोकहित में ही होती है। वे किसी का वध करवाते हैं या स्वयं करते हैं, उसमें भी प्राणी मात्र का कल्याण ही निहित होता है।
अपने बाल्यकाल में ही श्रीकृष्ण पूतना, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, चाणूर, मुष्टिक आदि का वध करते हैं। क्यों ? क्योंकि उनका अवतार ही साधु पुरूषों की रक्षा एवं दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है। विनाश भी कैसा की उन्हें परमधाम पहुँचा दिया.....।
भगवान श्रीकृष्ण ने बकासुर एवं अघासुर का वध किया। बक अर्थात् दंभ एवं अघ अर्थात् पाप। जीवन में जब दंभ और पाप आता है तो जीवन की बंसी गुनगुनाती नहीं है अर्थात् जहाँ जीवन में सहज स्वाभाविक प्रेम और आनंद छलकता है, वहाँ दम्भ और पाप विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं।
अघासुर अजगर के रूप में आया था। संस्कृत में अज बकरे को कहते हैं। बकरे को यानि अज को जो निगल जाय उसे अजगर कहते हैं।
अघासुर इतना विशाल मुँह खोलकर आया कि भोले-भाले ग्वालबालों को पता ही न चला। मनुष्य का हृदय तो विकसित हो किन्तु बुद्धि विकसित न हो तो वह कहाँ जाता है ? पाप में, अघ में।
अघासुर मुख में ग्वालबाल यह समझकर जाते हैं कि यह गुफा मनोहर है, सुन्दर है लेकिन उनको श्रद्धा थी कि कोई भी भूल होगी तो हमारा साथी कन्हैया हमें बचायेगा।
भक्तों को भी स्मरण होना चाहिए कि त्रुटि होने पर तुरन्त ही प्रभु से प्रार्थना करें कि यदिः
दुनिया
के हंगामों
में आँख हमारी
लग जाय।
तो
हे मालिक !
मेरे ख्वाबों
में आना प्यार
भरा पैगाम
लिये।।
हे मेरे प्रभु ! हे मेरे मित्र ! मुझसे कोई गलती हो जाय अथवा मैं 'मेरे-तेरे' में फँस जाऊँ, तो तू मुझे बचाते रहना। यदि ऐसा विश्वास हो जाये तो फिर आप पाप में, अवगुण में भी चले जाते हैं तो वह बचाने के लिए पीछे-पीछे छा जाता है।
श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए जब हम आदर करना चूक जाता है तो पापग्रस्त हो जाते हैं। ग्वालबाल श्रीकृष्ण के साथ रहते हैं, खाते-पीते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण का आदर नहीं किया तो उन्हें अघासुर निगल गया, फिर श्रद्धा के बल पर बच भी गये।
कथा कहती है कि श्रीकृष्ण के सब साथी अघासुर के मुँह जैसे विशाल मुख में चले गये तब अंत में श्रीकृष्ण भी गये और उस असुर के प्राणों को अवरूद्ध कर दिया। अघासुर का सूक्ष्म शरीर श्रीकृष्ण में समा गया। कितनी उदारता है श्रीकृष्ण की.....!
एक असुर जो उन्हें मारने आया था, उसे भी मुक्ति प्रदान कर दी। क्या ईश्वरीय लीला है.....! अघासुर ने न तप किया, न जप किया, न यज्ञादि किया, हवन, ध्यान व भजन भी नहीं किया। वह तो श्रीकृष्ण को मारने आया था फिर भी स्वयं मुक्त हो गया।
परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण की इस लीला से पता चलता है कि श्रीकृष्ण का विश्वात्मभाव कितना दृढ़ था ! कोई विधि करता है कि नहीं ? कोई पूजा करता है कि नहीं ? कोई तप करता है कि नहीं ? इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है अपितु उनके संपर्क में जो एक बार आ गया तो बस, दे..... फिर..... सीधा दे कि उल्टा दे। श्रीकृष्ण कैसे भी देते हैं लेकिन देते हैं और पहुँचा देते हैं अपने सुखद स्वरूप में। यही तो उनकी महिमा है !
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
श्रीकृष्ण
का जीवन-संदेश
कृष्ण का अर्थ हैः
कर्षति
आकर्षति इति
कृष्णः।
जो आकर्षित करता है, वह है कृष्ण। धन, सत्ता, पद आदि किसी को आकर्षित नहीं करते वरन् उनसे प्राप्त सुख ही मनुष्य को आकर्षित करता है।
कृष्ण अर्थात् जो सबको आकर्षित कर सके, शत्रुओं को भी आकर्षित करने की जिसमें क्षमता हो। ऐसा जीवन तुम्हारा भी होना चाहिए।
सच पूछो तो तुम श्रीकृष्ण से तनिक भी कम नहीं हो। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम बुद्ध से, महावीर से रत्ती भर भी कम नहीं हो लेकिन स्वयं को कम मान बैठे हो क्योंकि कमनसीब शरीर में अहंता आ गई है। शरीर को अपना और जगत को सच्चा मानना जब से शुरू किया तभी से दुर्भाग्य का आरम्भ हुआ।
श्रीकृष्ण धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं। ब्रह्मज्ञानियों की रक्षा के लिए नहीं किन्तु जो साधक अभी साधनापथ पर हैं, जो साधुवेश में हैं, उनके संसार की ओर खींचते मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो अवतार हुआ है उसका नाम है कृष्ण।
उपनिषदों के ज्ञाता एवं पुराणों के प्रणेता महापुरूषों का मत हैः "जो कर्षण करे अर्थात् जो आकर्षित करे उसका नाम है कृष्ण।"
आकर्षित तो तुम्हें आनंद करता है लेकिन जीव जब इन्द्रियों के विषयों में उलझ जाता है तथा संसार को सत्य मानकर हर्ष से जब प्रभावित होता है तो उन उलझे हुए अपने बच्चों का ठीक से लालन-पालन करने के लिए वे आदिनारायण, विष्णु कभी श्रीकृष्ण का रूप लेकर तो कभी श्रीराम का रूप लेकर तुम्हें अपनी आनन्दस्वरूप चेतना की ओर आकर्षित करते हैं अर्थात् जब सज्जन एवं साधु स्वभाव के लोग भी विषयों की ओर प्रेरित हो जाते हैं तब उनका परित्राण करने के लिए प्रगट होने वाली चेतना का ही नाम श्रीकृष्ण है।
बालक को वस्त्राभूषण आदि पहनाओ तो बालक की शोभा बढ़ती है किन्तु श्रीकृष्ण को पहनाने से उन वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ जाती है।
श्रीकृष्ण द्वारा धारण किया जाकर मोरपंख भी पूजनीय हो जाता है अर्थात् वस्त्राभूषण श्रीकृष्ण को शोभा नहीं देते वरन् स्वयं सुशोभित हो जाते हैं, गहने भी श्रीकृष्ण द्वारा धारण किये जाकर स्वयं शोभते हैं, बंसी भी शोभती है क्योंकि श्रीकृष्ण स्वयं शुभस्वरूप हैं।
श्रीकृष्ण का सब कुछ मधुर इसलिए भी लगता है कि वे सब कुछ सहज में करते हैं। सहज में किया हुआ कर्म उत्कृष्ट ही होता है।
कई लोग अपनी वृत्ति को अन्तर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं।
एक बार नारदजी यमुना तट की ओर आ रहे थे कि उन्हें वहाँ एक गोपी दिखाई पड़ी। वह आँखें बंद करके कुछ प्रयास कर रही थी। नारदजी ने पूछाः
"पगली क्या ध्यान कर रही है ? श्रीकृष्ण का चिन्तन कर रही है ? अब तो वे नन्दबाबा के यहाँ आये है, जाकर दर्शन कर ले। यहाँ पर बैठे रहने से क्या फायदा ? जब उसकी याद करती है तो उसी को जाकर देख ले।"
जिसकी याद आती है, उसकी याद करनी नहीं पड़ती और जिसकी याद करनी पड़ती है उसकी याद करते-करते फिर याद होने लगती है। याद आने लगे वह एक बात है लेकिन जिसको याद करते हैं, वह सामने आ जाये तो फिर बात पूरी हो जाती है।
श्रीकृष्ण की याद आना एक बात है, श्रीकृष्ण सामने आ जाएँ यह दूसरी बात है और यदि श्रीकृष्ण का तत्त्व समझ में आ जाय तो फिर बात ही निराली है।
याद करना एक बात है, याद आना दूसरी बात है। पहले तो याद करना पड़ता है फिर याद करते करते याद आना उसका स्वभाव हो जाता है। बार-बार जो किया जाता है वह स्वभाव बन जाता है। प्रारम्भ में अन्य यादों को छोड़ने के लिए श्रीकृष्ण की याद करनी पड़ती है। याद करते-करते श्रीकृष्ण की याद पक्की हो जाती है तो अन्य सारी यादें गौण हो जाती हैं।
श्रीकृष्ण की याद करते-करते श्रीकृष्ण स्वयं सामने आ जाते हैं और प्रगट हो जाते हैं तो और भी अच्छा है किन्तु यदि कृष्णतत्त्व का ज्ञान होकर इसमें आराम करने लग जाएँ तो सर्वोत्कृष्ट होगा क्योंकि जब कृष्णतत्त्व में आराम मिल रहा है तो श्रीकृष्ण की याद करने की फिर क्या जरूरत ? फिर भी यदि वह याद आती है तो बाधा है।
उस गोपी के पास जाकर नारदजी कहते हैं- "यहाँ क्या कर रही है ? जा, नन्दबाबा के यहाँ वह बाँके बिहारी आया है। जाकर दर्शन कर ले।"
तब गोपी कहती हैः "महाराज ! श्री बाँकेबिहारी के दर्शन करके तो मैं फंस गई हूँ। अब बाँके की याद और बाँके के दर्शन हट जाय तो मैं जरा और काम कर लूँ।"
बड़े-बड़े जपी-तपी ध्यान करना चाहते हैं, पगली गोपियाँ उनका ही ध्यान भूलाना चाहती हैं। उनका इतना उत्कट प्रेम है कि श्रीकृष्ण के सिवाय उन्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उससे फरियाद नहीं होती है, उसकी हर बात मानने के लिए प्रेमी तत्पर होता है। गोपियो का तो श्रीकृष्ण के लिए अटूट प्रेम है ही किन्तु अन्य गोकुल वासियों का भी प्रेम कम नहीं है।
यद्यपि उम्र के लिहाज से देखा जाय तो श्रीकृष्ण अत्यन्त छोटे थे किन्तु सभी का उन पर इतना प्रेम था कि सब उनकी बात मानते थे।
श्रीकृष्ण गाँववासियों को गोवर्धन की पूजा करने को कहते हैं तो सभी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसके पहले गोकुलवासी इन्द्र की पूजा करते थे।
इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्य। इन्द्र की खुशामद करते-करते युग बीत गये। ऐसे इन्द्र की पूजा की अपेक्षा आप लोग गोवर्धन की पूजा करो।
'गो' यानि उपनिषद। उसका जो वर्धन करे तथा औरों को कराये ऐसे पुरूष की पूजा होनी चाहिए। वहीँ पूजा करने चलो और वहीँ अपनी खुशियाँ मनाओ।
इन्द्र का तात्पर्य सत्ता के धन से है और गोवर्धन का तात्पर्य उपनिषदों के धन से है।
उपनिषदों के धन की पूजा अर्थात् आत्मज्ञानी महापुरूषों के चरणों में बैठकर अपने आत्मतत्त्व की पूजा। यही गोवर्धन की पूजा है। हो सकता है कि गोवर्धन की पूजा करने पर सत्ता और धन तुम्हें दबायें, तुम पर मेघ गर्जायें या तुम्हें भय दिखायें लेकिन यदि श्रीकृष्ण तुम्हारे साथ हैं, आत्मदेव तुम्हारे साथ हैं तो तुम अपनी छोटी-मोटी लकड़ियाँ लगाओ और वे अपनी छोटी सी कनिष्ठिका अंगुली लगा देंगे तो बड़े में बड़ा पहाड़ जैसा दुःख भी तुम्हें दुःख न देगा, तुम्हारे लिये वह छाता बन जायेगा।
वास्तव में देखा जाए तो श्रीकृष्ण के दुःख के आगे तुम्हारा दुःख तो कुछ भी नहीं है। श्रीकृष्ण का जीवन दुःखों की एक लंबी कहानी है फिर भी श्रीकृष्ण सदा मुस्कुराते रहे हैं। कभी पूतना विष लेकर आई है तो कभी बवंडर में से राक्षस प्रकट हुआ है। कभी कालियनाग का सामना करना पड़ा है तो कभी मामा कंस के भेजे हुए धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर आदि से निपटना पड़ा है। अनेक षडयन्त्रों से पार होते-होते अन्त में मामा कंस को आलिंगन करके, मर्दन करके स्वधाम पहुँचाना पड़ा है।
मामा को परम धाम पहुँचाने वाले भी श्रीकृष्ण है और अग्निदान देने वाले भी श्रीकृष्ण ही हैं। अनेक राजाओं को परास्त करने वाले भी श्रीकृष्ण हैं और रण छोड़कर भागने वाले भी श्रीकृष्ण ही हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई फरियाद नहीं है।
मुस्कुरा
के गम का जहर
जिसको पीना आ
गया।
यह
हकीकत है कि
जहाँ में उसको
जीना आ गया।।
श्रीकृष्ण के आचरण का अनुकरण करनेवाला कोई नहीं रहा। यहाँ तक कि स्वयं उनके बेटे भी न थे। श्रीकृष्ण ऋषि मुनियों का आदर करते थे, उनकी झूठी पत्तलें तक बड़े प्रेम से उठाते थे, जबकि उनकी संतानें ऋषि-मुनियों का मजाक उड़ाती थी। फिर भी श्रीकृष्ण निराश नहीं हुए क्योंकि श्रीकृष्ण सदा समता में स्थित रहे और गीता के माध्यम से हम सबका भी यही संदेश दिया किः
सुखदुःखे
समे कृत्वा
लाभालाभौ
जयाजयौ।
ततो
युद्धाय
युज्यस्व
नैवं
पापमवाप्स्यसि।।
'जय-पराजय, लाभ हानि और सुख-दुःख को समान समझकर युद्ध के लिये तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।'
(गीताः 2.38)
यह बात केवल कुरूक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए ही नहीं कही गई है अपितु प्राणीमात्र के लिये कही गई है क्योंकि हम सब भी अर्जुन की तरह ही संसाररूपी कुरूक्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सररूपी शत्रु दिन-रात हम पर धावा बोलते हैं। हमें उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है और यदि इन शत्रुओं को हमने जीत लिया तो फिर हम श्रीकृष्ण की तरह सदा के लिए अजेय हो जाएँगे। फिर कभी भी, कोई भी शत्रु हमारा बाल ता बाँका न कर सकेगा।
वास्तव में श्रीकृष्ण का पूरा जीवन ही एक संदेश है। रासलीला के एक प्रसंग के माध्यम से श्रीकृष्ण हमें देहाध्यास भुलाने को कहते हैं।
वे कहते हैं- पूर्णिमा की रात को बंसी बजाऊँगा। जो अधिकारी होंगे उन्हीं को सुनाई पड़ेगी, वे ही लोग आयेंगे। श्रीकृष्ण ने बंसी बजाई और वे लोग श्रीकृष्ण के पास आये तथा देहाध्यास को भुलाकर सब श्रीकृष्ण के आकर्षण में आकर्षित हो गये।
फिर उनके मन में विचार आया कि 'हम भाग्यशाली हैं, अधिकारी हैं तभी तो आ पाये। और लोग तो न आ सके।' वे ऐसा सोचकर पुनः देहाध्यास में आ गये। ज्यों ही वे देह में आ गये त्यों ही श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। फिर सब भटकने लगे, खोजने लगे कि 'श्रीकृष्ण कहाँ हैं.....? श्रीकृष्ण कहाँ हैं.....?'
तुम जब देह में आते हो तो श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो जाते हैं। श्रीकृष्ण थे तो मंडल में लेकिन पीताम्बर ओढ़ लिया था। सब ग्वाल-गोपियाँ जंगल में वृक्षों, लताओं, कदम्ब आदि से पूछते हुए अधमरे से हो गये। इस बीच राधा श्रीकृष्ण से मिली। राधा को भी लगा कि और गोपियाँ तो नहीं मिली लेकिन मैं श्रीकृष्ण से मिल गई। तब श्रीकृष्ण ने राधा से कहाः "तू थक गई होगी। आ, मेरे कन्धे पर चढ़ जा।"
राधा श्रीकृष्ण के कन्धे पर चढ़ने की कोशिश करती है तो वह लटकती रहती है। यदि तुम्हारी बुद्धिरूपी प्रकृति भी आत्मा के कन्धे पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो लटकती रहेगी त्रिशंकु की तरह..... न ऊपर न नीचे।
श्रीकृष्ण यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि तुम देह को 'मैं' मानना छोड़ दो, देहाध्यास को भुला दो। जब तक तुम देहाध्यास को भुलाए रखते हो तब तक मैं तुम्हारे समक्ष प्रगट ही रहता हूँ किन्तु जब तुम देहाध्यास में पुनः आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सामने होता हुआ भी अन्तर्धान हो जाता हूँ।
मैं तभी तक रहता हूँ जब तक 'तुम' नहीं रहते अर्थात् तुम देह को 'मैं' नहीं मानते। जब तुम अपने को देह मानना पूर्ण रूप से छोड़ दोगे, तब तुममें और मुझमें तनिक सी दूरी भी न रहेगी। तुम और मैं एक हो जाएँगे। कबीरजी ने कितनी सुन्दर बात कही है !
जब
मैं था तब हरि
नहीं, अब हरि
है मैं नांही।
प्रेम
गली अति
सांकरी, तामें
दो न समांही।।
अतः तुम अपने-आप को पूर्णरूपेण श्रीकृष्ण को समर्पित कर दो ताकि तुम न बचो। बस, वही रह जाये।
श्रीकृष्ण की लीला दिखाती है कि भाव के आगे जीव, जीव नहीं बचता और ईश्वर, ईश्वर नहीं बचता। भाव के आगे वृजराज, वृजराज नहीं बचते और वृज का एक नन्हा सा ग्वाल, ग्वाल नहीं बचता। सबका संबंध स्नेह से जुड़ जाता है।
जीवनरस को पाना है तो भावों का विकास होना जरूरी है, भावशक्ति का विकास होना जरूरी है, क्योंकि यदि क्रियाशक्ति का विकास नहीं होगा तो जीवन कभी भी उलझ सकता है। श्रीकृष्ण के जीवन में भावशक्ति, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति तीनों का विकास देखा जाता है।
क्रियाशक्ति और भावशक्ति के साथ ज्ञानशक्ति होना भी जरूरी है क्योंकि यदि ज्ञानशक्ति न हो तो क्रिया 'सिकन्दर क्रिया' हो जायेगी......'हिटलर क्रिया' हो जायेगी.... 'रावण क्रिया' हो जायेगी अर्थात् क्रिया विकृति का रूप ले लेगी।
यदि आप आवेश आकर कोई क्रिया करते हैं तो वह क्रिया विकृत हो जाती है, इसलिए श्रीकृष्ण के जीवन में देखा जाए तो कोई आवेश नहीं, उद्वेग नहीं, कोई निष्ठुरता नहीं, क्रूरता नहीं। जब देखो तब आनंदित और प्रसन्न.....। युद्ध के मैदान में भी चैन की बंसी बज रही है।
श्रीकृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा होना चाहिए।
श्रीकृष्ण के सामने ग्वाल है तो श्रीकृष्ण का व्यवहार कुछ है और राधिका सामने है तो व्यवहार कुछ और है। कंस के साथ श्रीकृष्ण का आचरण दूसरा है। वे ही श्रीकृष्ण यदि संतों के पास हैं तो उनकी झूठी पत्तलें तक उठाने को तैयार हैं। यदि श्रीकृष्ण वसुदेव के आगे खड़े रहते हैं तो बेटे होकर रहते हैं। गोपियों की चोटियाँ खींचने वाले श्रीकृष्ण, योगियों को योग बताने वाले श्रीकृष्ण, अर्जुन को गीता का ज्ञान देनेवाले श्रीकृष्ण तथा माँ को मुँह खोलकर सम्पूर्ण विश्व का दर्शन करानेवाले श्रीकृष्ण। उनके सामने जैसा व्यक्ति होता है, वैसी उनकी लीला होती है।
मनुष्य की भी जैसी दृष्टि होती है वैसे ही उसको श्रीकृष्ण दिखते हैं। श्रीकृष्ण को तुम जिस नजर से देखते हो – भावुक, भक्त, संसारी या अन्य किसी नजर से, श्रीकृष्ण वैसे दिखते हैं किन्तु वास्तव में वे ऐसे हैं नहीं। श्रीकृष्ण अपने को जिस नजर से देखते हैं, उस नजर से यदि तुमने श्रीकृष्ण को देखा तो तुम भी श्रीकृष्णरूप हो जाते, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाता।
श्रीकृष्ण स्वयं को समग्र विश्व में व्यापक मानते हैं.... जानते हैं, ऐसा ही यदि तुम भी मान लो तो कल्याण हो जायेगा।
श्रीकृष्ण के जीवन में आपको क्या-क्या नहीं मिलता ? श्रीकृष्ण योगियों के बीच योगियों जैसे दिखते हैं, राजाओं के साथ बिठाओ तो महाराजा है, राजकारिणियों के साथ बिठाओ तो श्रीकृष्ण जैसा कोई राजकारिणी नहीं है। आज तक श्रीकृष्ण के तुल्य न तो कोई राजा हुआ, न ही राजनीतिज्ञ। राज्य लिया और तुरन्त दे भी दिया।
श्रीकृष्ण ने अघासुर और बकासुर का नाश कियाः अघ यानि पाप एवं बक यानि दंभ। पाप एवं दंभ का वध यही बताती है कि पाप, दंभ और अत्याचार का नाश होने पर ही प्रेम का प्रागट्य होता है। निर्गुण निराकार का सगुण साकार मूर्ति में प्रागट्य जिस दिन होता है उसे ही जन्माष्टमी कहते हैं।
श्रीकृष्ण के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण बात झलकती है कि मुझे दियों को प्रकाश देने का कार्य और उलझे हुए दिलों को सुलझाने का काम तो वे करते ही हैं, साथ ही साथ इन कार्यों में आने वाले विघ्नों को भी किनारे लगा देते हैं। फिर चाहे वह मामा कंस हो या बुआ पूतना या अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर हो या फिर केशि हो।
साधक को भी चाहिए कि साधना में या ईश्वर-प्राप्ति में मददरूप जो व्यवहार, खान-पान, रंग-ढंग है, जो घड़ी भरके लिये थकान उतारने के काम में आ जाये, उसका उपयोग करते हुए... अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए वहाँ पहुँचने का तरीका पा लेना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि श्रीकृष्ण का अवतार रात्रि को बारह बजे ही मनाओ। श्रीकृष्ण का अवतार तो आप जब चाहो तब मना सकते हो। श्रीकृष्ण के अवतार से अभिप्राय है श्रीकृष्ण का आदर्श, श्रीकृष्ण का संकेत।
हमने 'कृष्ण कन्हैया लाल की जय' कह दी, मक्खन-मिश्री बाँट दिया, खा लिया, इतने से ही अवतार के उत्सव को मनाने की पूर्णाहूति नहीं होती।
श्रीकृष्ण जैसी मधुरता को, जीवन में तमाम परेशानियों के बीच रहकर भी चित्त की समता को बनाये रखने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए।
यह जन्माष्टमी अपने प्रेम को प्रगट करने का संदेश देती है। जितना अधिक हम आत्मनिष्ठा में आगे बढ़ते हैं, उतना उतना हम श्रीकृष्ण का आदर करते हैं और श्रीकृष्ण का अवतार मनाते है।
ऐसा नहीं कि रात्रि को जागरण किया और दूसरे दिन सोते रहे...... नहीं। श्रीकृष्ण की गीता का ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए।
हमारे नगर में, हमारे आस-पास में जो भाई-बहन है, वे भी इस जन्माष्टमी महोत्सव का लाभ लें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जिन लोगों को विधर्मी लोग अपने धर्म से च्युत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुनः गीता के ज्ञान से, श्रीकृष्ण के अमृत से लाभान्वित करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
आज हम संकल्प करें कि गीता के संदेश को, योग के संदेश को, आत्मज्ञान के अमृत को हम भी पियेंगे और हमारे भारतवासी भाइयों को भी पिलायेंगे।
श्रीकृष्ण का वास्तविक जन्म तब मनाया जायेगा, जब हम श्रीकृष्ण के सिद्धान्तों को समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जैसे गोकुल में कंस का राज्य नहीं हो सकता, ऐसे ही तुम्हारे इन्द्रियों के गाँव अर्थात् शरीर में भी कंस का अर्थात् अहंकार का राज्य नहीं रहे, परन्तु श्रीकृष्ण की बंसी बजे, प्रेम की बंसी बजे, यही इस पर्व का हेतु है।
श्रीकृष्ण का जीवन एक समग्र जीवन है। उसमें से आप जो कुछ भी पाना चाहें, पा सकते हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक लीला आपको कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती है। आप उन्हें अपना कर, उनका अनुसरण कर अवश्य ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ श्रीकृष्ण स्वयं हैं। आप श्रीकृष्ण के जीवन को अपना आदर्श बनाकर, उसके अनुसार आचरण कर, उस पथ के पथिक बन सकें, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
उद्धव को
भगवान
श्रीकृष्ण का
उपदेश
श्रीमद् भागवत के 11 वें स्कन्ध के 7 वें अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं-
यदिदं
मनसा वाचा
चक्षुर्भ्यां
श्रवणादिभिः।
नश्वरं
गृह्यमाणं च
विद्धि माया
मनोमयम्।।
'जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी, श्रवण, नेत्र आदि इन्द्रियों से अनुभव किया जाता है वह सब नाशवान है, मन का विलास है, मायामात्र है।'
(श्रीमद् भागवतः 11.7)
तुलसीदासजी कहते हैं-
देखिये,
सुनिये,
गुनिये मन
माहिं।
मोह
मूल परमारथ
नाहिं।।
जो कुछ सुनने में आता है, देखने में आता है, मन के विचार में आता है, बुद्धि के निर्णय में आता है, इन्द्रियों की पकड़ में आता है, समाज की जकड़ में आता है वह सब अज्ञान से सच्चा भासता है। बाकी सब सपना है, मोह का मूल है।
मनुष्य जब बूढ़ा होता है और उसका पुत्र में मोह होता है तब पुत्र यदि कहने में नहीं चलता तो खेद होता है और कहने में चलता है तो राग होता है। जमाई अच्छा है तो अहंकार होता है और बुरा है तो विषाद होता है। पुत्र के घर पुत्र है और 'दादा-दादा' कहता है तो मोह होता है और पुत्र के घर संतान नहीं है तो चिंता होती है। जगत् के लोगों के साथ तुम्हारी मित्रता है तो तुम्हारा समय नष्ट कर देते हैं और द्वेष है तो अशांति कर देते हैं। अतः किसकी मित्रता करोगे ? कब तक लोगों के बीच रहोगे ? उठ जाओ और वैराग्य का आश्रय लो। जैसे साईकल के पहिए निकाल दो तो साईकल चलना मुश्किल है ऐसे ही जीवन से अभ्यास और वैराग्य हटा दो तो प्रभु की यात्रा होना मुश्किल है। अतः तुम ध्यान का अभ्यास करो और विवेक के साथ अपने भीतर छुपे हुए वैराग्य को जगाकर वैराग्य में ही राग रखो। वैराग्यरागरसिको भवः। संसार के राग से बचकर प्रभु परायण हो जाओ।
जैसे कोई व्यक्ति आँखों में शूल नहीं भोंकना चाहता ऐसे ही समझदार व्यक्ति अपने आप को विषयों के शूल नहीं भोंकना चाहता। जैसे कोई भी समझदार मनुष्य अपने भोजन में विष नहीं डालना चाहता, ऐसे ही हे उद्धव ! जिज्ञासु व्यक्ति अपने जीवन में विषयों का विष नहीं डालना चाहता।
अपने स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए जीव बिचारा विषय विकारों में भटक-भटककर अपना जीवन गँवा देता है। समझदार लोग समझते हैं कि शरीर की नश्वरता क्या है। आग लगने पर कुआँ खोदना पड़े, उसके पहले ही कुआँ खोदकर तैयार कर देते हैं। बुढ़ापा आने से पूर्व ही शरीर को विषय-विकारों में न गिराकर परमात्मा के ज्ञान में लगा देते हैं। सारी रात दूसरों की नींद खराब हो और लोग बोलने लगें कि बुढ्ढा जल्दी मर जाये तो अच्छा, उसके पहले वह अपने अहंकार को मार देता है, वासना को मार देता है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जायें और चेहरा भद्दा हो जाये उसके पहले वह अपना असली चेहरा देख लेता है। बाल सफेद होने से पूर्व वह अपना हृदय स्वच्छ कर लेता है। आँखें कमजोर हो जायें, कान बहरे हो जायें और मित्र-संबंधी सब पराये होने लग जायें, इसके पूर्व वह परमात्मा का हो जाने की कोशिश करता है।
जो समझदार है, विवेकी है, वे समझते हैं कि यह सब चार दिनों का खेलमात्र है। ये सब मित्र देखने भर के ही हैं। यह सारा संसार सपने की तरह बहता चला जा रहा है। मौत आकर उसे मार दे, उसके पहले ही अमिट आत्मा का ज्ञान पाकर मुक्त हो जाता है। जैसे अजगर का सिरहाना बनाकर कोई आराम नहीं करता, अग्नि को आलिंगन करने की कोई इच्छा नहीं करता ऐसे ही विवेकवान मनुष्य विषयों की इच्छा नहीं करता। उसको तो बस, यही लगन लगी रहती है कि परमात्मा को कैसे पा लूँ।
हम कई जन्मों में कीट पतंगे, बंदर, हिरण , देवता आदि बन चुके हैं। अब यह अमूल्य मानव जन्म मिला है तो इसे सार्थक कैसे करें ? उस वैराग्यवान को तो देवताओं के सुख भोग कुत्ते के सड़े माँस जैसे लगते हैं, स्वर्ग की अप्सराएँ मरी हुई हिरणी जैसी लगती हैं, प्रतिष्ठा और वाहवाही शूकर की विष्ठा जैसी लगती हैं।
हम समझते होंगे कि जिन बुद्ध पुरूष की वाहवाही होती है उनको बड़ा मजा आता होगा। लेकिन उनको न मजा आता है न सजा लगती है। मूर्ख को प्रतिष्ठा से रस मिलता है, संसारी को प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, जिज्ञासु साधक के लिए वाहवाही झंझट है। ज्ञानी के लिए प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा सब मनोमात्र है, मायामात्र है।
तुम अपने मन की वृत्ति को अन्तर्मुख करके देखो, फिर निंदा और प्रशंसा तुम्हारे लिए कुछ न रहेगी, भोग और त्याग कुछ न रहेगा, मित्र और शत्रु कुछ न रहेंगे। जो समझदार है वह अपने एक-एक श्वास को अनमोल समझता है। एक भी श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देता। जैसे एक तैराक को पता लगता है कि मझधार में गहरा पानी है तो पहले से ही कमर में तुम्बा बाँध लेता है, ऐसे ही संसार सागर से पार होने के लिये विवेकी साधक ज्ञान का तुम्बा बाँध लेता है।
गुरू और शिष्य जा रहे थे। गुरू ने कहाः "देख बेटा ! कुछ बनना मत। बनेगा तो बिगड़ेगा।"
ऐसे ही साधक कुछ बनने की इच्छा नहीं करता। मूकवत्......जड़वत्......काष्ठवत् रहता है।
"बेटा ! तू सावधान रहना, कुछ बनना मत। सतर्क रहना।"
लेकिन जीव को बनने की पुरानी आदत है।
गुरू शिष्य घूमते-घामते किसी राजा के बगीचे में पहुँचे। वहाँ कुछ कमरे भी बने थे। राजा यदा-कदा उस बगीचे में घूमने फिरने आया करता था। शिष्य एक कमरे में जाकर सो गया एवं गुरू दूसरे कमरे में। इतने में राजा घूमता-घामता उधर आया और देखा कि उसके कमरे कोई सो रहा है।
राजा के नौकर ने पूछाः "तू कौन है ?"
शिष्यः "मैं साधू हूँ।"
नौकर ने उठाकर शिष्य के गाल पर एक थप्पड़ रख दी और डाँटाः "साधु है ? कैसा साधु है ? राजा के कमरे में, राजा के पलंग पर बिना पूछे सो गया ? साधु है फिर भी पलंग पर सोने का शौक नहीं गया ? साधु है फिर भी आराम चाहता है ?"
नौकर ने तीन-चार थप्पड़ और लगाकर, कान खींचकर शिष्य को भगा दिया। राजा घूमते-घामते दूसरे कमरे में पहुँचा। देखा तो वहाँ भी कोई सोया हुआ है।
राजा के वजीर ने पूछाः "कौन हो ?"
बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर बाबा को हिलाकर पूछाः "कौन हो ?"
बाबा चुप रहे। राजा ने कहाः "इनको डाँटो मत। ये कोई सिद्ध महात्मा मालूम होते हैं।" राजा ने आदर सहित महात्मा को प्रणाम किया।
जब जीव कुछ बनता है तब अहंता से जुड़ता है और अहंता ममता ही मार खाती है। इस अहंता ममता में कोई सार नहीं है। अज्ञानी, पामर और मूर्ख लोग जिसको सत्य समझकर अपना जन्म गँवा रहे हैं उस संसार में भी कोई सार नहीं है। यह शरीर क्या है ? हाड़-माँस, त्वचा, रक्त और मल-मूत्र से भरा हुआ देह। जैसे कोई श्वान की खाल में पड़ी हुई खीर की इच्छा नहीं करता, ऐसे ही विवेकी मनुष्य दूसरे गर्भ में जाकर माताओं का दूध पीने की इच्छा नहीं करता। जैसे कोई विष्ठा के पाईप में सोने की इच्छा नहीं करता ऐसे ही वैराग्यवान मनुष्य दूसरे जन्म में माता के गर्भ में नव महीने उल्टा लटकने की इच्छा नहीं करता, रक्त और पीब से भरे हुए कुण्ड में स्नान नहीं करना चाहता। जैसे कोई पामर और शराबी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाना चाहता, वैसे ही अज्ञानी मन के कहने में साधक नहीं चलता।
श्रीकृष्ण कहते हैः "हे उद्धव ! जैसे धधकती हुई अग्नि में कूदने की इच्छा कोई नहीं करता, ऐसे ही समझदार व्यक्ति इन्द्रियों के भोग में नहीं कूदता। बल्कि वह अपनी इन्द्रियों को अन्तर्मुख करके, मन को परमात्मशांति में डुबाकर मेरे को अभिन्न हो जाता है।"
शुकदेव जी महाराज सावधान करते हैः "हे परीक्षित ! विलासी व्यक्ति के लिए तो सारा संसार छोटा है, सारे संसार की चीजें कम हैं। लेकिन वैराग्यवान तो जो उसके पास है उसी में संतुष्ट है। वह तो सोचता है कि हाथ में भोजन लेकर खाने को मिल जाये तो बर्तन क्यों रखना ? हाथ की अंजुलि से पानी पी सकते हैं तो गिलास क्यों रखना ? भुजाओं को तकिया बनाकर आराम किया जा सके तो तकिया क्यों संभालना ? जिसको सात दिन में मुक्ति चाहिए उसको संग्रह तो नहीं करना चाहिए वरन् जो कुछ है उससे उपराम होकर सतत् हरिचिंतन करके हरिरूप हो जाना चाहिए। जिसके केश मृत्यु ने पकड़ रखे हैं उसको अधिक मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसे शुचि होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, गतव्यथा और अनपेक्ष अर्थात् अपेक्षारहित होना चाहिए।"
अनपेक्षः
शुचिर्दक्षः
उदासीनो
गतव्यथः।
सर्वारम्भपरित्यागी
योमद् भक्तः स
मे प्रियः।।
'जो पुरूष आकांक्षा से रहित, बाहर-भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुःखों से छूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है।'
(भगवद् गीताः 12.16)
किसी के धन, साम्राज्य या ऐश्वर्य देखकर उसे पाने की इच्छा न करें क्योंकि मन सत्यसंकल्प है। फिर उस अवस्था में आना पड़ेगा, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। इसलिए दक्ष बनना चाहिए। जैसे तैसे संकल्प करके अपने को कर्म के बंधन में न डालो लेकिन अपने संकल्पों से कर्म के बंधनों को काटने का प्रयास करो। अभी तुम्हारी जो स्थिति या अवस्था है, वह तुम्हारे संकल्पों का ही रूपान्तर है। अब कुछ होने की इच्छा न करो वरन् सतत सावधान रहकर उस आत्मपद को जान लो जिसे जानने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "हे उद्धव ! मैंने कई प्रकार के जीव और जन्तुओं की रचना की, वृक्षों की रचना की, पशु और पक्षियों की रचना की। किन्तु दो पैर और दो हाथवाले मनुष्य की अपेक्षा मुझे और कोई अधिक प्यारा नहीं है। उसी को आत्मज्ञान पाकर अपना जीवन सफल करने का अधिकार मिला है। विषय सुख तो और योनियों में भी बड़े सुविधापूर्ण ढंग से मिलते है। खाना-पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना, दुःख आये तो घबराना और सुख आये तो पूँछ हिलाना..... ये तो कई पशु, प्राणी, कुत्ते भी कर लेते है। किन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति के मनुष्य ही कर सकता है। उसके पास विवेक है। साधारण लोग तो विषय-भोग एवं 'हा हा ही ही' में ही अपना जीवन पूरा कर डालते हैं। उनको सत्संग नहीं रुचता और सत्संग में जाने का भी समय नहीं मिलता। किन्तु मेरा प्यारा जो भक्त है, जिसके पास विवेक है, वह साधु पुरूषों को खोज लेता है। निरभिमानी होकर उनके चरणों में प्रणाम करके अपने पाप और संताप निवृत्त करता है। उनके अनुभवयुक्त वचनों को वह अपने वचन बना लेता है।
हे उद्धव ! मैं और अधिक क्या कहूँ ? जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता वैसे ही विषय-भोग में जो उल्लू हो गये हैं उनको ज्ञानियों का ज्ञान नहीं दिखता। ऐसे हतभागी धन-ऐश्वर्य में अपना जीवन गँवाकर अंत में बुढ़ापे में पश्चाताप करते-करते मरेंगे। फिर विष्ठा के कीड़े बनकर दुःखी रहेंगे, पुत्र-पौत्र के मोह में फँसकर दुःखी और संतप्त रहेंगे।"
तुलसीदासजी महाराज कहते है-
जो न
तरै भवसागर,
नरसमाज अस
पाइ।
सो
कृत निंदक
मंदमति,
आत्माहन गति
जाइ।।
जो मनुष्य ऐसा सत्संग पाकर भी भवसागर से तरने का प्रयास नहीं करता, जन्म-मरण के चक्र से छूटने का प्रयास नहीं करता वह कृतघ्न है, निंदनीय है, मंदमति है। ऐसा आत्महत्यारा अधोगति को जाने वाला होता है। फिर उसे कुत्ते, गधे, घोड़े, कीड़े जैसी नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा, वृक्ष बनकर कुल्हाड़े सहने पड़ेंगे। अतः बुद्धिमान मनुष्य कभी-भी भोगियों का, मंदमतियों का अनुकरण नहीं करता बल्कि साधु पुरूषों के संग से अपने जीवन को ऊँचा बनाता है।
"हे उद्धव ! भोगी लोग तो वैराग्य की बात सुनते ही भाग जाते हैं। जिनके पाप बहुत बढ़ गये हैं उनको ज्ञान-वैराग्य की बातों में रूचि नहीं होती है। जो पुण्यात्मा हैं, जिन पर मेरी कृपा है, माता-पिता का आशीर्वाद है, गुरूजनों की कृपा है, जिन्होंने विवेक वैराग्य का सहारा लिया है, उनकी बुद्धि ही काम देती है और वे संसार-सागर में डूबने से पहले आत्मज्ञान का किनारा ढूँढ लेते हैं।
हे उद्धव ! अधिक तुझे क्या कहूँ ? 'यह पुत्र मेरे हैं, ये परिवार मेरा है....' ऐसी दुर्बुद्धि को त्यागकर, इन सबको मनोमात्र समझकर, मायामात्र समझकर इनका मोह त्याग दे।
हे उद्धव ! अब तू बदरिकाश्रम चला जा। इन्द्रियों की चपलता छोड़ दे। जगत् की वस्तुओं की वासना छोड़ दे। ये सब मोह के मूल है। इसमें कोई सार नहीं है। धनी होने में सार नहीं है तो निर्धन होने में भी सार नहीं है। सब असार है, मायामात्र है।
शरीर वीभत्स हो जाये, पड़ोसी कहने लगे कि बूढ़ा रात भर नींद खराब करता है, रोग घेर लें, उसके पहले ही बुद्धिमान मनुष्य नीरोगी आत्मा को जान लेता है। लोग कंधे पर चढ़ाकर श्मशान में पहुँच आयें, उसके पहले ही वह अपने मन को आत्मा में पहुँचाने का यत्न करता है। मित्र और कुटुम्बीजन मुँह मोड़ लेता है। बुढ़ापे में पैर शिथिल हो जायें उसके पूर्व ही वह संत के द्वार पर पहुँच जाता है। बुढ़ापे में कान बहरे हो जायें उसके पहल ही वह ब्रह्मविद्या सुन लेता है। आँखों की रोशनी मारी जाये उसके पहले ही वह महापुरूषों के दर्शन करके आत्मशान्ति को पा लेता है। बुद्धि अस्थिर हो जाये उसके पहले ही वह बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर लेता है।
हे उद्धव ! ये आँख के विषय, कानों के विषय, नाक के विषय, जिह्वा के विषय, शिश्ना के विषय ही मनुष्य को भटका देते हैं। मछली जैसे स्वाद में अपना जीवन बरबाद कर देती है ऐसे ही तू जिह्वा के स्वाद में अपना जीवन बरबाद मत करना। हिरण जैसे शब्द में अपना जीवन बरबाद कर देता है, ऐसे ही तू बाहर के गीत-गान में अपना जीवन बरबाद मत करना। पतंगा जैसे दृश्य में अपने जीवन को नष्ट कर डालता है ऐसे ही तू अपने जीवन को दृश्य में मत उलझा डालना। भ्रमर जैसे सुगंध में अपना जीवन समाप्त कर डालता है, ऐसे ही सुगन्धों के पीछे तू अपना जीवन बरबाद मत करना। हाथी हथिनी को देखकर स्पर्श सुख लेने जाता है और गढ्ढे में गिर जाता है। फिर सारा जीवन महावत की गुलामी सहता रहता है। मायारूपी महावत की गुलामी सारी जिंदगी सहकर अंत में क्या मिलता है ? अंत में क्या हाथ लगता है ?"
जैसे चूने के लड्डू मक्खन के पिंड जैसे लगते हैं लेकिन खाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही विषय बाहर से सुखरूप दिखते हैं किन्तु भोगने से बल, बुद्धि, तेज और आयुष्य का नाश हो जाता है। अतः जैसे समझदार व्यक्ति समुद्र का जल पीने की इच्छा नहीं करता वैसे ही विवेकवान मनुष्य इन्द्रियों के भोग की इच्छा नहीं करता।
श्रीकृष्ण कितनी सुन्दर बात कह रहे हैं-
"मैं जो कहता हूँ उसको समझकर संसार से उपराम हो जाओ। मैं तुम्हारे हृदय में छुपा हूँ। उसमें तुम आराम करो। फिर मेरे में और तुम्हारे में कोई भेद न रहेगा। विषय की गुलामी करने से तुम तुच्छ हो जाते हो, दीन हो जाते हो और अपने आत्मा में आराम करने से तुम परमेश्वर हो जाते हो। उद्धव ! चुनाव तुम्हारा है।"
श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं- "हे उद्धव ! मेरे साथ जाने की इच्छा छोड़ दे। उस अन्तर्यामी आत्मा का सहारा ले, वैराग्य का सहारा ले, विवेक का सहारा ले। तू बदरिकाश्रम चला जा और मैंने तुझे जो उपदेश दिया है उसको विचार कर अपने निज स्वरूप को पा ले। एक बार निज स्वरूप का ज्ञान हो जाने से तेरे हृदय में शोक और मोह का स्थान ही न रहेगा। तू उस परम शांति को पा लेगा जहाँ मैं स्वयं विश्राम करता हूँ।"
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
प्रपत्तियोग
आत्म-साक्षात्कार करना बड़ा आसान है, सुगम है। राजा जनक को घोड़े के रकाब में पैर डालते-डालते हो गया था, खटवाँग को एक मुहूर्त में हो गया था, परीक्षित राजा को सात दिन में हो गया था। और भी कई नामी-अनामी महापुरूषों को आत्म-साक्षात्कार हुआ है। इतना सरल होने पर भी सबको आत्म-साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों ?
भगवान श्रीकृष्ण कहते है-
दैवी
ह्येषा
गुणमयी मम
माया
दुरत्यया।
मामेव
ये
प्रपद्यन्ते
मायामेतां
तरन्ति ते।।
'यह अलौकि, अति अदभुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरूष मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं।'
(भगवद् गीताः 7.14)
यह अति अदभुत, त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। इसका थाह नहीं पाया जा सकता है। यह माया लौकिक नहीं है, अलौकिक है। कोई आदमी अपनी लौकिक बुद्धि से, अपनी कल्पना के बल से, अपनी अक्ल-होशियारी का तुंबा बाँधकर इससे तरना चाहे तो नहीं तर सकता है। इस माया से कौन तर सकता है ? ज्यादा पढ़ा-लिखा या अनपढ़ ? निर्धन या धनवान ? देवी-देवता या भूत-प्रेत को रिझाने वाला या अवतार का सुमिरन करने वाला ? नहीं..... भगवान श्रीकृष्ण कहते है कि जो मुझ अन्तर्यामी की शरण रहेगा वह इस दुस्तर माया को आसानी से तर जायेगा।
अन्तर्यामी ईश्वर क्या है और ईश्वर की शरण जाना क्या है इस बात को जब हम ठीक से जान लेते हैं, तब शरणागति सफल होती है।
किसी तालाब में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने के लिए खड़ा था। वह दाँयी ओर, बाँयी ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, चारों ओर जाल फेंकता था। उस जाल में छोटी-बड़ी, चतुर बुद्धु सब मछलियाँ फँस जाती थीं पर एक मछली ऐसी थी, जो मछुआरे के पैरों के इर्द-गिर्द ही घूमती थी। मछुआरा वहाँ तो जाल फेंक नहीं सकता था। इसलिए वह उसके जाल में फँसने से बच जाती थी।
ऐसे ही त्रिगुणमयी माया के जाल में चतुर भी फँसे हैं, बुद्धू भी फँसे हैं, मूर्ख भी फँसे है और विद्वान भी फँसे हैं, भोगी भी फँसे हैं और त्यागी भी फँसे हैं। इतना ही नहीं, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, भूचर, जलचर, नभचर सभी इस माया के तीन गुणों में से किसी न किसी गुण में फँसे हैं। पर माया का जो आधार है, उस ईश्वर की शरण में रहने वाला माया के जाल में फँसने से बच जाता है।
कोई कहता हैः "मैं तो भगवान की शरण हूँ।"
तू भगवान की शरण में है तो 'तू' कौन है ? यह पहले बता।
'मैं तो गोविन्दभाई हूँ।'
नहीं..... तुम वह नहीं हो। यह तुमने सुन-सुनकर मान लिया है। पहले तुम अपने को जानो और 'भगवान क्या है' यह समझो। तब 'शरण जाना क्या है' इस बात का पता चलेगा। मैं भगवान की शरण हूँ। यह मान लेना अलग बात है, सचमुच में भगवान की शरण जाना अलग बात है। अगर मानी हुई शरण ईमानदारी की है तो सचमुच में शरण जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जायगा।
माया में रहकर माया से तरना कठिन है। पर यदि ईश्वर की शरण में रहे, आत्मा में रहे तो माया तो अति तुच्छ है। जैसे स्वप्न में तो बहुत कुछ होता दिखाई देता है, पर स्वप्न से जाग जाते हैं, तब पता चलता है कि उसमें कोई सार नहीं था, कुछ सत्य नहीं था। सब मेरी ही करामात थी। ऐसे ही जब तक हम माया के गुण में फँसे होते हैं तब तक बहुत कुछ करने कराने में लगे रहते हैं, संसारसागर में गोते खाते रहते हैं, बार-बार जन्मते और मरते रहते है। पर जगतरूपी स्वप्न से जब जाग जाते हैं, तब उसका कोई प्रभाव नहीं बचता है। हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं।
माया में रहकर जो आदमी सुखी होना चाहता है वह दुःख ही पाता है। जैसे कोई हाथी कीचड़ में फँसा है। वह निकलना तो चाहता है, पर ज्यों-ज्यों निकलने का प्रयत्न करता है त्यों-त्यों अधिक फँसता जाता है।
'मैं शरीर हूँ और कुटुंब-परिवार, नात-जात सब मेरा है' ऐसी जो मान्यता है वह माया का खिलवाड़ है। इसमें आदमी फँस मरता है। अपने को जानता नहीं है, देह को ही 'मैं' मानता है। इसलिए माया के गुण उसे बाँध लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आलसी, प्रमादी आदमी ही डूबता है, रजोगुणी और सत्त्वगुणी तो क्या स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक जाने वाला आदमी भी माया के अन्तर्गत है, माया से पार नहीं हुआ है।
यह माया ऐसा अहं ले आती है कि आदमी जप-तप, सेवा-पूजा सत्कर्म नहीं करता है और अपने को पापी मानता है तो उसमें पापीपना आ जाता है। दान-पुण्य करता है तो दानीपना आ जाता है। साधन-भजन करता है, कुछ ज्ञान की बातें सुनता है और याद रखता है तो ज्ञानीपना आ जाता है, योगीपना आ जाता है। मन में हर्ष आता है तब खुश हो जाता है, अपने को भाग्यशाली मानता है। मन में शोक आता है तब अपने को अभागा मानता है। ऐहिक लाभ या हानि होती है तब अपने को लाभ या हानिवाला मानता है। कोई राजसी कर्म करके अपने को बड़ा मानता है। कोई तामसी कर्म करके अपने को बड़ा मानता है। कोई सात्त्विक कर्म करके अपने को बड़ा मानता है। यह सब हो रहा है गुणों में, अहं में। पर गुणों को जो सत्ता दे रहा है उसका पता नहीं है, अपने निर्गुण स्वभाव का बोध नहीं है। इसलिए सब अपने में आरोपित कर लेता है। यहीं गड़बड़ हो जाती है। यह गड़बड़ कई सदियों से, कई जन्मों से होती चली आ रही है। यह आदत पुरानी हो गयी है, इसलिये सच्ची भी लग रही है। हर कोई व्यक्ति अपनी मान्यताएँ बताये रखता है, चाहे अच्छी हों या बुरी और उसका अहंकार भी करता है।
अहंकार के साथ कर्त्तापना भी आ जाता है। अच्छे कर्म करने का भी अहंकार, बुरे कर्म करने का भी अहंकार और कुछ नहीं करने का भी अहंकार होता है। 'मैं तो कुछ नहीं करता। सब भगवान करवाता है।' इसमें 'मैं नम्र हूँ' इस बात का अहंकार तो रहता ही है।
जेल में कोई नया कैदी आया तो जेलर ने उसे अन्य कैदियों के साथ रख दिया। वहाँ किसी पुराने कैदी ने उसे आवाज लगाईः
"अरे दोस्त ! कितने महीने की सजा मिली है ?"
नया कैदी बोलाः "छः महीने की।"
तब पुराने कैदी ने कहाः "अरे यह तो सिक्खड़ है। भाई ! तू दरवाजे पर ही अपना बिस्तर लगा। यहाँ तो 20 सालवाले बैठे हैं। तूने ज्यादा से ज्यादा किसकी टांग तोड़ी होगी। हम तो तीन-तीन खून करके बैठे हैं। तूने डाका कितने का डाला था।
नया कैदीः "5000 रूपये का।"
पुराना कैदीः "अरे ! इतना छोटा काम को हमारे बच्चे ही कर लेते हैं। हमने तो दो लाख का डाका डाला और तीसरी बार जेल में आया हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ... पुराना खिलाड़ी हूँ इस मामले में तो। जेल को तो अपना घर ही बना लिया है, हाँ !"
अशुद्ध और निंदित कर्म में जो कर्त्तापना और अहंकार है वह तो भटकाता ही है पर साधारण अहंकार भी गिराने वाला होता है। जब भी तुममें कर्त्तापना आ जाता है, तब सहजता, सरलता खो जाती है। तुम आरती कर रहे हो और कोई उसे देख रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है, ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हारी आरती लम्बी हो जाती है। कोई गौर से किसी की भजन सुन रहा है तो भजन सुनाने वाले के राग लम्बे होते जाते है। ढोलक बजाने वाले के ताल में जोश आ जाता है। तुम साईकिल चला रहे हो और कोई देख रहा है तो तुम्हारे पेड़ल मारने में रौनक आ जाती है। यह माया का गुण है जो तुम्हारे कर्त्तृत्व को, अहंकार को जगा देता है। अकेले में तुम कुछ और होते हो।
रमण महर्षि के पास कई लोग आते थे। कभी-कभी रमण महर्षि किसी व्यक्ति की ओर बार-बार अथवा एकटक देखते थे तो उसका अहंभाव जग जाता था। वह सोचने लगता कि 'मैं कुछ विशेष हूँ..... महर्षि मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।' अतः महर्षि को उस पर से दृष्टि हटा देनी पड़ती थी। जब उसकी ओर देखते ही नहीं तो उसको दुःख होता था कि महर्षि पहले, शुरू-शुरू में हम आये तब तो खूब ध्यान देते थे, अब आँख उठाकर देखते भी नहीं।
मनुष्य की यह बड़ी कमजोरी है। जिस पर कोई थोड़ा विशेष ध्यान देता है तो उसे होता है कि मैं कुछ विशेष हूँ और ध्यान नहीं देते हैं तो उसे लगता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। 'मैं' तो बना ही रहता है। जब तक 'मैं' बना रहेगा तब तक कभी हानि कभी लाभ, कभी सुख कभी दुःख, कभी जीवन कभी मृत्यु सताता रहेगा।
इस गुणमयी माया के तीन गुण हैं- सत्व, रजस, तमस। इन तीन गुणों के विभिन्न प्रकार के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का अनुभव होता है। कई लोग ईंट-चूना, लोहे लक्कड़ के मकान-दुकान, फैक्ट्री पाकर अपने को सुखी मानते हैं। कई लोग बाह्य विद्या, ऐहिक विद्या पढ़कर अपने को विद्वान मानते हैं। कई लोग बाह्य धन पाकर अपने को धनवान मान लेते हैं। इन चीजों के शिकंजे से छूटकर, इस भ्रांतिपूर्ण माया से निकलकर, कोई भगवान के रास्ते चलता है तो तुष्टि नाम की अवस्था आ जाती है। वह भी माया का रूप है। साधना-भजन करने लगे तो लोग भगत कहने लगे। ध्यान-साधना आदि किया, कुछ अनुभव होने लगे, भगवान का रूप दिखने लगा। कुछ होने वाली बात का पहले पता चलने लगा तो आदमी समझने लगता है, बस मेरा भजन हो गया। यह तुष्टि है। जैसे कोई चौथी-पाँचवीं कक्षा तक पढ़ ले और अपने को विद्वान मानने लग जाय, ऐसे ही ईश्वर के रास्ते चलते समय थोड़ी ऊँची अवस्था आ जाती है तब सूक्ष्म अहंकार आ जाता है वह तुष्टि है, माया का खेल है।
माया क्या है ? कहाँ रहती है ? माया माने धोखा। या मा सा माया। जो नहीं है फिर भी सच्ची दिखती है। वह अज्ञान के कारण टिकती है, जीव की कल्पना में रहती है और तुष्टि आदि के रूप में आती है। थोड़ा सा आभासज्ञान हुआ, थोड़ी-सी झलक मिली, थोड़ी सी वाह वाही मिली तो आदमी उसी में रूक जाता है।
माया
रची तू आप ही
है, आप ही तू
फँस गया।
कैसा
महा आश्चर्य
है, तू भूल
अपने को गया।।
संसार
सागर डूबकर
गोते पड़ा है
खा रहा।
अज्ञान
से भवसिन्धु
में बहता चला
है जा रहा।।
जिसे यहाँ पर छोड़कर जाना है, उसके पीछे दिन-रात एक करके लगे रहते हैं और जो सदा साथ में है, जिसे जाने बिना दुर्भाग्य मिटने वाला नहीं, उसके लिये समय नहीं है। यही माया है। परन्तु भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-
मामेव
ये प्रपद्यन्ते
मायामेतां
तरन्ति ते।
जो मेरी शरण आता है, वह माया से तर जाता है। श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं कहा है कि 'कृष्ण-कृष्ण' करते रहो तो तर जाओगे। उनका कहना है कि जो अन्तर्यामी कृष्णतत्त्व है उसकी शरण में रहो। जिसने अंतर्यामी कृष्णतत्त्व को 'मैं' रूप में जान लिया उसने सारी दुनिया के 'मैं' को जान लिया, वह माया से पार हो गया।
ईश्वर की देने की कला ऐसी है कि लेने वाले को पता ही नहीं चलता है कि यह किसी का दिया हुआ है। लेने वाला हर चीज को अपनी मान लेता है। जिस शरीर को वह 'मैं' मानता है, वह पानी की एक बूँद ही तो है, जो पिता के शरीर से पसार हुआ, माता के गर्भ में विकसित हुआ और प्रकृति के अन्न जल से उसका पोषण होकर बड़ा हुआ। अब शरीर ही 'मेरा' नहीं है तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, धन, मकान, दुकान, पढ़ाई-लिखाई, सत्ता, पद-प्रतिष्ठा 'मेरी' कैसे हो सकती है ? ईश्वर इस ढंग से देता है कि वह दाता दिखता ही नहीं है, लेकिन लेने वाला उस चीज को अपनी मान लेता है और माया के जाल में फँस जाता है। बड़े-बड़े तीसमारखाँ भी इस माया के बहाव में बह गये। जो साक्षात् श्रीकृष्ण के दीदार करते थे ऐसे नारदजी भी माया के जाल से नहीं बच पाये।
एक बार नारदजी अपनी मस्ती में मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे। श्रीकृष्ण वहाँ पधारे। नारदजी की सेवा-भक्ति से श्रीकृष्ण संतुष्ट थे, प्रसन्न थे। उन्होंने नारदजी से कहाः
"देवर्षि ! तुम्हारे व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ। तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए ? जो भी इच्छा हो, वह माँग लो।"
नारदजीः "प्रभु ! मैं क्या माँगू ? मुझे आपके चरणों की भक्ति का वरदान दो।"
श्रीकृष्णः "वत्स ! तुम्हारी भक्ति से तो मैं संतुष्ट हूँ। तुम और कुछ माँग लो।"
नारदजीः "यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मुझे आपकी माया दिखलाइये।"
श्रीकृष्णः "मैं, जो सदा तुम्हारे साथ हूँ, अंतर्यामीरूप से सत्ता, स्फूर्ति, प्रेरणा देता हूँ उसे तुम देखो। माया देखने की जिद मत करो।"
नारदजीः "भगवन् ! आपको तो मैं देख रहा हूँ।"
श्रीकृष्णः "तुम मुझे नहीं देख रहे हो। इस शरीर को देख रहे हो। तुम मुझे देखो।"
नारदजीः "आपको अंतर्यामी के रूप में तो कभी न कभी देख लूँगा। पहले आप अपनी माया दिखाइये। आपकी माया को देख लूँगा तो माया से तर जाऊँगा।"
नारदजी माया में जी रहे हैं फिर भी माया को देखना चाहते हैं।
श्रीकृष्ण कहते हैं- "माया को देख लोगे तो माया से तर जाओगे ऐसा नहीं है। जब मुझे देख लोगे, मुझ अन्तर्यामी कृष्ण को जान लोगे तब तर जाओगे।"
नारदजीः "प्रभु ! आपको तो देख ही रहा हूँ। कृपा करके अब आपकी माया दिखाइये।"
श्रीकृष्णः "नारद ! यह तुष्टि है। मेरे साकार रूप का दर्शन किया और आनंद आया यह ठीक है। पर अभी तुमने मेरे पूर्ण व्यापक रूप को नहीं जाना है, उसे पहले जान लो।"
भक्त तो बालक जैसे होते हैं। बालक माता-पिता से अपनी बात मनवाता है ऐसे ही भक्त की बात भगवान को माननी पड़ती है।
नारदजी ने कहाः "प्रभु "! मुझे तो आपकी माया ही दिखलाइय़े। आप तो कहते हैं 'मैं संतुष्ट हुआ हूँ... तू कुछ माँग ले।' जब माँगता हूँ तो बात टालते हैं, देना नहीं चाहते हैं।"
श्रीकृष्ण ने देखा कि इसको अभी ठोकर खाने की मर्जी है। उन्होंने कहाः "अभी मुझे प्यास लगी है। तुम जरा सरस्वती से पानी भर कर लाओ।"
नारदजी गये पानी लेने के लिए। 'भगवान के लिए पानी भरना है तो शुद्ध होकर भरूँ' यह सोचकर उन्होंने पानी में जरा गोता मारा तो नारद में से नारदी बन गये। स्त्री का शरीर, कपड़े-गहने, हाव-भाव सब आ गया। बड़ी सुंदर शर्मीली कन्या हो गई। वे भूल ही गये कि मैं नारद हूँ। किसी मल्लाह ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। उसी मल्लाह के साथ शादी हो गई। वह अब मल्लाहन बन गयी। अब वह मल्लाह के लिए रोटी बनाती, फिर भोजन देने जाती। दिन बीते, सप्ताह बीते, साल बीते। ऐसा करते-करते तेरह साल में नौ बच्चे हो गये। अब नारदी का परिवार बहुत बड़ा हो गया। इतने बड़े परिवार के पालन पोषण की चिन्ता में मल्लाह बीमार रहने लगा और जल्दी ही मर गया तो नारदी रोने लगीः "अरे ! मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गये.... अब मेरा क्या होगा रे....!' उसे रोती हुई देखकर बच्चे भी रोने लगे।
इतने में श्रीकृष्ण वहाँ आये। उन्होंने कहाः "अरे ! तुम क्या करते हो ? मैंने तुम्हें पानी भरकर लाने को कहा था। अभी तक नहीं लाये ?"
नारदी होने की भ्रांति थी तो अपने कपड़े संभालते हुए गोता मारकर नारदजी बाहर निकले। देखते हैं तो न बच्चे हैं न मरा हुआ मल्लाह। नारदजी कुछ खोये-खोये से लगते थे। नारदजी ने श्रीकृष्ण से कहाः
"भगवन् ! यह लो पानी..... लेकिन मुझे कुछ हो गया।"
"क्या हुआ ?"
"मैं किसी मल्लाह की स्त्री बन गया था, मेरे कितने ही बच्चे हो गये थे। यह सब क्या था ?"
भगवानः "इसी का नाम माया है। तुम वही के वही थे पर तुम्हें यह सब महसूस हो रहा था। जो महसूस हुआ वह रहा नहीं, तुम तो रहे। तो तुम असलियत हो, बाकी जो दिख रहा था वह मिथ्या आभास था। यही तो मेरी माया है। इसे तरना आसान भी है और कठिन भी है। माया में रहकर माया से तरना चाहो तब कठिन है पर जब अपने-आप में ठहरते हो, तो माया से तरना आसान है।"
हमारे शरीर मन बुद्धि प्रकृति के हैं, हमारा व्यवहार प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति में बदलाहट होती रहती है। प्रकृति में उत्पत्ति, स्थिति और लय का चक्र चलता रहता है। हमारे मन, बुद्धि आदि भी बदलते रहते हैं। बचपन के मन-बुद्धि जवानी में वैसे ही नहीं रहते हैं और जवानी के मन-बुद्धि बुढ़ापे में बदल जाते हैं। बुढ़ापे में स्मृति में भ्रम हो जाता है, लेकिन इन सब बदलाहट को देखने वाला जो अबदल, अविनाशी आत्मा है वह मैं हूँ, इस बात का पता चल जाय तो हम प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जायेंगे। सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि-लाभ कुछ भी हो, इनसे प्रभावित नहीं होते हैं तो हमारा भीतर का आनंद, भीतर का हौसला बना रहता है।
कभी-कभी तो लोग भगवान का भजन तो करते है साथ में सुविधाओं का भजन भी करते हैं। सुंदर वातावरण है, ठंडी-ठंडी हवा आ रही है, भगवान का भजन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। पर यदि जरा किसी की कोहनी लग गई तो भजन-भगवान सब गायब ! ध्यान कर रहे हैं.... भगवान की मस्ती में हैं.....'अहा... हा... वाह..... प्रभु ! देखा अपने आपको मेरा दिल दीवाना हो गया.... आ..... हा.... आनंद ही आनंद है....' पर किसी ने जरा अपमान कर दिया कि आनंद गायब ! तो भगवान का भजन तो होता है, साथ में देह का भजन भी होता है, अपनी मान्यताओं का भजन भी साथ में चालू रहता है।
जो केवल अपनी मान्यताओं को पकड़कर बैठे हैं, उसमें ही उलझे हैं उनसे तो भगवान के साथ मान्यताओं को भी भजने वाला ठीक है। लेकिन जब तक मान्यताएँ मौजूद हैं तब तक वह संसारसागर से पूरा तर नहीं सकेगा। युद्ध करता हो, आमने-सामने बाणों की बौछारें हो रही हों, फिर भी अपने में कर्त्तृत्व न दिखे। चाहे क्रॉस पर या शूली पर चढ़ा दिया जाये पर उसे शूली शूली न दिखाई दे व चढ़ाने वाला दिखाई दे। तीनों लोकों का नाश कर दे या तीनों लोकों को जीवन दे दे फिर भी 'मैं कर रहा हूँ' ऐसा भाव न हो। 'सब माया में हो रहा है, तीन गुणों से प्रकृति में हो रहा है। मैं इनसे परे हूँ।' इस बात को ठीक से जान लेने वाला माया से तर जाता है। वह भले फिर माया में रहता हुआ दिखे लेकिन उसकी वृत्ति कुछ अलौकिक हो जाती है।
करता
हुआ भी नहीं
करे सो
प्राज्ञ
जीवन्मुक्त है।
जो लोग सतत भगवान का स्मरण करते हैं वे माया से पार हो गये हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान का स्मरण ही नहीं, साक्षात् भगवान जिनके साथ हैं, ऐसे उद्धवजी को श्रीकृष्ण कह रहे हैं-
यदिदं
मनसा वाचा
चक्षुर्भ्यां
श्रवणादिभिः।
नश्वरं
गृह्यमाणं च
विद्धि माया
मनोमयम्।।
"जो मन से, वाणी से, आँखों से, कानों से देखने में, सुनने में और सोच विचार में आता है, वह सब त्रिगुणमयी माया का खिलवाड़ है, सब मनोमय है, नश्वर है। इसलिए हे उद्धव ! तू बद्रिकाश्रम जा और एकान्त में जाकर ज्ञान का विचार करे। तू चाहता है कि मैं साथ चलूँ पर साथ में कोई आया नहीं है, साथ में कोई जायेगा भी नहीं। कितने भी साथ में रहे फिर भी अलगाव रहेगा लेकिन सब शरीरों के बीच मैं बस रहा हूँ यह जान ले।
मयि
सर्वामिदं
प्रोतं
सूत्रे
मणिगणा इव।
यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गूँथा हुआ है। यह मुझ चैतन्य को, कृष्णतत्त्व को तू अपने में जान लेगा और उसकी शरण रहेगा तो फिर कभी मुझसे अलगाव होगा ही नहीं। जब तक तू मुझ अन्तर्यामी की शरण नहीं जायेगा तब तक माया के गुण तुझे बाँधते रहेंगे, माया अपने बहाव में तुझे बहाती रहेगी।"
माया का मतलब है धोखा। कभी सात्विक धोखा, कभी राजस धोखा, कभी कभी तामस धोखा। जिन गुणों का प्रमाण ज्यादा होता है उस अनुसार उसका प्रभाव दिखाई देता है। जब सत्त्वगुण बढ़ता है तो आदमी स्वस्थ, फुर्तीला, प्रसन्न लगता है। वह अपने को ज्ञानी-ध्यानी मानता है। जब सत्त्वगुण कम होता है और रजोगुण बढ़ता है तो अति प्रवृत्तिशील होता है, अपने को चतुर, चालाक, धनी, दानी मानता है। जब सत्त्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है तब आदमी आलसी-प्रमादी बन जाता है, क्षुद्र अहंकार में उलझा रहता है।
आदमी जिस गुण के प्रभाव में जीता है, ऐसी ही इच्छाएँ, वासनाएँ, रूचियाँ पैदा हो जाती हैं।
जैसे, किसी गडरिये का 11 साल का लड़का हो और भैंसे चराता हो, तो वह 15 भैंसे तो आसानी से चरा लेता है पर उसे 15 अक्षर लिखने में कठिनाई मालूम पड़ती है। ऐसे ही हम सदियों से प्रकृति के गुणों के आधीन जीते आये हैं। अभी भी प्रकृति के गुणों के आधीन जीते हैं। शरीर को 'मैं' और संसार को सच्चा मानते हैं तो बुद्धि संसार में ही उलझी रहती है, अपनी ओर नहीं आती। हलकी बुद्धिवाले, हलके कर्म करने वाले लोग सत्संग में नहीं आ पाते हैं। उन्हें सत्संग अच्छा नहीं लगाता है।
तामसी लोग कहते हैं- "मैं कोई जैसा-तैसा आदमी नहीं हूँ। चार चिलम पी जाता हूँ और हमारे दादागुरू सबके सरदार थे। मैं ऐसे गुरू का चेला हूँ। दो चिलम पीता हूँ, फिर तीन घंटे भजन में बैठता हूँ।"
भजन में क्या बैठता है खाक ? वीर्यनाश हो जाता है, ज्ञानतन्तु शून्य हो जाते हैं, तो पड़ा रहता है तीन घंटे सुनसान होकर। यह भजन हुआ क्या ? यह तो तामसी माया है।
रजोगुणी आदमी प्रवृत्तिपरायण रहता है। कुछ न कुछ करते रहना, घूमना फिरना, मिलना-जुलना, सिनेमा-थियेटर जाना आदि उसे अच्छा लगता है।
एक लड़का अपने दोस्त से कह रहा हैः "तुझे मिले बिना चैन नहीं आता। जब तक तेरा दीदार नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे आँधी हो या तूफान, तुझे मिले बिना नहीं रह पाता हूँ।"
वह लड़का जब जाने लगा तब दोस्त ने उससे पूछाः
"जा रहे हो ? कल आओगे न ?"
लड़काः "आऊँगा......कोशिश करूँगा.....।"
अभी तो कहता था 'तेरे बिना चैन नहीं।' अब कहता है 'कोशिश करूँगा।' जीव को बेचारे को पता ही नही है कि वह करना क्या चाहता है और करता क्या है। यह भी माया का ही खेल है।
जो माया के खेल के पार होना चाहते है, उन्हें अपने अंतर्यामी की शरण जाना चाहिए, अपने असली स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए।
वशिष्ठजी कहते हैं- "हे राम जी ! जो देह को 'मैं' मानते हैं उनके लिये तो संसारसागर पार करना बड़ा कठिन है। लेकिन जिनके पाप नष्ट हो गये है, जो विचार वान हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, जो सत्त्वप्रधान हैं, जिनको सदगुरू की छाया मिली है, उनके लिये संसारसागर से तरना आसान है।"
सदगुरू की छाया तो मिले पर सदगुरू में अटूट श्रद्धा बनी रहे यह बात जरूरी है। ईश्वर में तो श्रद्धा हो सकती है लेकिन सदगुरू में श्रद्धा बनी रहे यह कठिन है। लाखों-लाखों शिष्यों में से कोई विरला ऐसा मिलेगा जिसको गुरूओं में कोई दोष न दिखे क्योंकि गुरू तो देहधारी होते हैं और हमारी तरह ही उठते-बैठते, खाते-पीते, लेते देते दिखते हैं। पर उनकी भीतर की स्थिति हम नहीं जान पाते है। वे देह में होते हुए भी देह से पार, तीनों गुणों से पार बैठे हुए होते हैं। हम देह में जीते हैं तो गुरू को भी देह बुद्धि के तराज में ही तोलते हैं। चाहे हजारों देवी देवताओं को मनाते रहो, रिझाते रहो, जब तक सदगुरू मे अटूट श्रद्धा नहीं हुई तब तक काम नहीं बनेगा। कोई कपड़े और गहने से अपने को सजाए रखने में मानता है, कोई पद-प्रतिष्ठा को मानता है, रूपये पैसे को मानता है। इनसे तो देवी देवता को मानने वाला ठीक है। लेकिन सारी मान्यताएँ जिस अंतःकरण से उत्पन्न होती हैं, उस अंतःकरण को सत्ता देने वाले आत्मा को जानना है। उसे जानना दुर्गम भी है और सुगम भी उतना ही है।
वशिष्ठ जी कहते है- "हे राम जी ! फूल पत्ती को तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा को जानने मे कोई परिश्रम नहीं है।"
......और कठिन भी उतना ही है कि आकाश चला जाय, पाताल चला जाय, स्वर्ग या नर्क चला जाय यह आसान है पर यहाँ, हृदय गुहा में केवल आधा इंच दूरी पर आना कठिन है।"
तुम बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, लंदन, अमेरिका जाओगे और लौटकर अपने घर आ जाओगे। लेकिन यहाँ आत्मा में आने में एक इंच भी दूरी नहीं और आज तक वहाँ पहुँचे नही हैं, क्योंकि कठिन है। सरल भी उतना ही है कि वहाँ पहुँचने में कोई झंझट नहीं है। न टिकट चाहिए न वीसा, न जाना है, न जाकर आना है। जहाँ है वहीं जरा भीतर गोता मार लिया कि पहुँच गये। एक बार ठीक से वहाँ पहुँच गये, फिर लौटने की बात ही नहीं। जहाँ जाओ वहाँ वही नजर आयेगा। संसार में इस देह से तो तुम अहमदाबाद मे होते हो तो बम्बई में नहीं होते हो और बंबई में होते हो तो अहमदाबाद में नहीं होते हो। जहाँ जाते हो वहाँ से अपने स्थान में लौटना पड़ता है लेकिन जब आत्मा में पहुँचोगे तो अपने को पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए व्यापक स्वरूप में पाओगे।
यह ऊँचे में ऊँचा स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पद भी तुम्हारी व्यापकता में तुच्छ नजर आएँगे। यह रहस्य समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता है। इस ऊँचाई को पाना दुस्तर है, असंभव नहीं है। यह कठिन इसलिए लगता है कि हम गुणों में जी रहे हैं, गुणों से प्रभावित शरीरों में, ऐसे व्यक्तियों के बीच जीते हैं। सारा वक्त गुणों की बातों में, माया की बातों में गँवा देते हैं।
जो गुणों से पार हुए हों और हमें भी गुणों से पार ले जा सकें ऐसे ज्ञानी गुरूओं का, महापुरूषों का संग नही है। कइयों को संग मिल जाता है पर....'उसका लड़का ऐसा है... उसकी बहू वैसी है.....।' बस जहाँ देखो वहाँ, जब देखो तब यही आकृतियों की चर्चा होती है, मरने वाले हाड़-मांस के शरीरों की चर्चा होती है और बदलने वाली परिस्थितियों की चर्चा होती है। अबदल आत्मा का ज्ञान तो बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। बहुमति गुणों में जीने वालों की है, उन्हें आत्मज्ञान की, तत्त्वज्ञान की बाते सुनाएँगे तो रूखापन आ जायगा पर गुणों की बात करेंगे तो रस आने लगेगा।
बड़ी उम्रवाले पति-पत्नी बम्बई की एक फाईव स्टार होटल में गये। हेयर डाई और मेक-अप आदि करने से कुछ बुढ़ापा भी छिप रहा था, वे कुछ जवान लग रहे थे। दोनों ने पहले आईस-क्रीम मँगवाया और खा लिया। फिर बैरे को आर्डर दियाः "एक डिनर प्लेट लाओ। बैरे ने डिनर प्लेट रख दी।
बैरा बड़े गौर से उन्हें देखता था। डिनर की प्लेट रखता जाय और टेढ़ी आँख से इन पति पत्नी की ओर देखता जाय। पति भोजन कर रहा है, पत्नी पंखा हाँक रही है। बैरे को लगा यह लैला मजनूँ की जोड़ी कहाँ से आई ! थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरी प्लेट मँगवाई। अब पत्नी खा रही है और पति पंखा हाँक रहा है। बैरे से रहा नहीं गया। आखिर उसने पूछ ही लियाः "आप दोनों में इतना स्नेह है तो आपने दोनों डिनर प्लेट साथ में क्यों नहीं मँगवाई ?"
उन्होंने कहाः "तेरी बात तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच दाँत की चौखट एक ही है। इसलिए बारी-बारी से अलग-अलग डिनर मँगवाये।"
ऐसी बातें तो रसीली लगेंगी क्योंकि हम गुणों में जीते हैं। निर्गुण तत्त्व में शुरू में तो रस नहीं आता है, पर सारे रस उसी से आते हैं।
जिनका हृदय शुद्ध है, जो ज्ञानवान हैं तथा जो इस त्रिगुणात्मक माया से तर चुके हैं ऐसे सदगुरूओं की बातों में हमारी रूचि पैदा नहीं होती है। उनके श्रीचरणों में श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा हो भी जाय उनकी बातों में, रूचि भी पैदा हो जाये पर उसमें लगे रहने की दृढ़ता नहीं होती है तो जीव बेचारा माया में ही अटक जाता है। माया से पार नहीं हो पाता है।
जो देह को 'मैं' मानते हैं ऐसे लोग देह से संबंधित व्यवहार में और चीज वस्तु की उपलब्धियों में ही अपने को सुखी मानते हैं। देह से संबंधित व्यवहार में कुछ गड़बड़ हुई या चीज वस्तुएँ चली गई तो अपने को अभागा मानते हैं। ऐसे अभागों की तो भीड़ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देह से संबंधित व्यवहार भी संभालते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद ऊँचे लोक में जाते हैं लेकिन कोई-कोई ऐसे होते हैं जो देह को, देह से संबंधित व्यवहार और उपलब्धियों को तथा सभी लोकों को मायामात्र जानकर, अपने को अन्तर्यामी चैतन्य आत्मा, साक्षी, दृष्टा, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन जानकर उसी पद में स्थित रहते हैं। वे माया से पार होकर परम कार्य साध लेते हैं।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
आत्मखोज
करो
अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सुख-दुःख के सर्जक हैं। अनुकूलता को हमने सुख माना और प्रतिकूलता को हमने दुःख माना। मन जब विषय-विकारों में लगेगा तब कभी अनुकूलता मिलेगी, कभी प्रतिकूलता मिलेगी। हमेशा प्रतिकूलता नहीं मिलेगी और चाहने पर भी सर्वत्र अनुकूलता नहीं मिलेगी। मन कभी सुख की तो कभी दुःख की थप्पड़ें खाते-खाते क्षीण होता जाएगा। मन का सामर्थ्य, एकाग्रता की क्षमता नष्ट होती जाएगी।
इसलिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का जो सुख-दुःख है उसको पकड़ो नहीं, उसको देखो। अनुकूलता से जो सुख मिला उसे मिला हुआ ही मानो। मिला हुआ मानोगे तो उसमें आसक्ति नहीं होगी क्योंकि जो मिली हुई चीज है वह अपनी नहीं है, परिस्थितियों की है। मिली हुई चीज सदा नहीं रहेगी लेकिन मन को देखने वाला सदा रहता है। मिली हुई घटना, मिली हुई वस्तु, मिला हुआ पदार्थ सदा नहीं रहता। लेकिन 'मिला-बिछुड़ा' जिससे महसूस होता है उस मन को देखने वाला सदा रहता है। 'मन को देखने वाला मैं कौन हूँ ?' उसकी अगर खोज करो तो अपने आपको पा लोगे.... मुक्ति का द्वार खुल जायेगा।
मनुष्य का मन दो धारी तलवार जैसा है। एक ओर मनुष्य चाहता है कि मैं दिव्य बनूँ.... अच्छा बनूँ..... मुक्त रहूँ..... यहाँ भी सुखी रहूँ और परलोक में भी सुखी रहूँ। दूसरी ओर मनुष्य यह भी चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाये लेकिन जैसा मेरे मन में आये वैसा होना ही चाहिए। इस तरह मन विषय विकार की तरफ भी झुका रहता है और दिव्यता के तरफ भी आकर्षित रहता है।
मनुष्य मन का यह स्वभाव है कि वह दोष दूसरों के देखता है और गुण अपने देखता है। किन्तु मनुष्य का मन अगर दर्पण बन जाये और जैसे दूसरों के दोष देखता है ऐसे अपना दोष देखने लग जाय एवं दूसरों के गुणों के प्रति जैसे बेपरवाह होता है ऐसे अपने गुणों के प्रति भी बेपरवाही रखने लग जाये तो मनुष्य का मन जल्दी शुद्ध होने लगता है। वह मुक्ति का कारण बन जाता है। साधक को हमेशा दूसरों ने अपने प्रति किया हुआ अपकार और खुद ने दूसरों के प्रति किया हुआ उपकार भूल जाना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है।
साधक को चाहिए कि वह हमेशा तीन बातों को शिरोधार्य करेः 1. वेदवचनों को 2. माता-पिता एवं गुरू के वचनों को और 3. अपनी गल्ती बताने वाले के वचनों को। इससे साधक ऊँचा उठ जायेगा।
किन्तु मनुष्य को अपनी गल्ती क्षमा करने में देर नहीं लगती और दूसरों की गल्ती बड़ी देखने में देर नहीं लगती।
अल्मारी से रद्दियों का बन्डल गिर पड़ा। उसमें छः मासिक परीक्षा के परिणाम की मार्कशीट भी थी। बुद्धु हलवाई ने देखा कि गणित में चार मार्क, भूगोल में तीन, समाजशास्त्र में शून्य मार्क....। वह गुस्से में आ गया। अपने बेटे को बुलाकर डाँटने लगाः "सातवीं कक्षा में ऐसा परिणाम ? तू क्या समझता है ?" बुद्धु हलवाई ने लड़के को चांटा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि लड़का बोल पड़ाः "पप्पा ! यह मार्कशीट तो पुरानी है, ऊपर से गिरी है। इस पर नाम आपका लिखा है। मेरी मार्कशीट तो मेरे पास है।"
तब बुद्धु हलवाई का क्रोध शांत हो गया। चांटा मारने का फोर्स चला गया। अपनी गल्ती दिखी तब वह अपने-आप शांत हो गया। ऐसे ही आध्यात्मविद्या कहती है कि दूसरी आकृतियों, दूसरी शरीरों में जब तुम अपने को देखने की आदल डालोगे तब तुम्हारा भय, क्रोध, विकार सब शांत हो जायेगा। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो द्वैतभाव से पैदा न होता हो और ऐसा कोई सदगुण नहीं है जो अद्वैत भाव से प्रकट न होता हो। इसलिए जीवन में अद्वैतज्ञान की आवश्यकता है। यही परमार्थ है।
मनुष्य सुखी कब होता है ? मनुष्य को विश्रान्ति कब मिलती है ? दुनिया के सब गहने मिलने से मनुष्य सुखी होता है ? दुनिया के सब सुंदर कपड़े मिलने से मनुष्य सुखी होता है ? नहीं। मनुष्य सुखी तो तब होगा जब-जब उसका मन अपने कारण स्वरूप में एकाग्र होगा। अपनी आत्मा में विश्रान्ति पायेगा तभी मनुष्य सुखी होगा।
बच्चा सोचता है कि आठवीं कक्षा पास कर लूँ, दसवीं पास कर लूँ, कालेज पूरा कर लूँ तो सुखी हो जाऊँ...... निश्चिंत हो जाऊँ.....
कालेज हो गई पूरी। फिर ? नौकरी मिल जाय तो सुखी हो जाऊँ। मिल गई नौकरी भी। फिर ? शादी हो जाये तो निश्चिंत हो जाऊँ। हो गई शादी। फिर ? बच्चा हो जाय तो सुखी हो जाऊँ। बच्चा भी हो गया। फिर ? फिर.... बच्चे के यहाँ बच्चा हो जाये तो सुखी हो जाऊँ... किन्तु ऐसा करते-करते जिंदगी पूरी हो जाती है। जो लोग मन के साथ जुड़कर जीते हैं उनकी न जाने कितनी कितनी सुख की कल्पनाएँ होती हैं किन्तु फिर भी पूर्ण सुख नहीं मिलता। नरसिंह मेहता कहते हैं-
ज्यों
लगी
आत्मतत्त्व
चीन्यों नहीं
त्यां
लगी साधना
सर्व झूठी।
'जब तक आत्मा-परमात्मा को नहीं पहचाना तब तक सब साधनाएँ झूठी हैं।'
रूपये कमाने की साधना, देवी-देवताओं को रिझाने की साधना, प्रसिद्ध होने की साधना, सुन्दर होने की साधना, विद्वान होने की साधना, ये सब साधनाएँ मृत्यु का झटका लगने से झूठी हो जाने वाली हैं। निर्धन समझता है धनवान होने में सुख है। अरे ! धनवान होने में भी सुख नहीं है और निर्धन रहने में भी सुख नहीं है। विद्वान होने में भी सुख नहीं है और 'अंगूठाछाप' रहने में भी सुख नहीं है। सुख तो वहाँ है जहाँ संत का मन ठहरता है। अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है।
योगवाशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठजी महाराज कहते हैं- "हे रामचंद्रजी ! मैंने बड़े बड़े विचार विमर्श किया है। मनुष्य को विश्रांति कहीं नही है। स्वर्ग के देवताओं को देखा तो वहाँ भी प्रतियोगिता (कम्पीटिशन) है। वहाँ कोई अपनी बराबरी का होता है तो संघर्ष होता है, अपने से बड़ा होता है तो ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या से पुण्यनाश होता है तो पतन होता है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है। गंधर्वों एवं यक्षों के पास भी ऐसा ही है। न देव सुखी है न गंधर्व सुखी हैं, न वितल में सुख है न तलातल में सुख है, न पाताल में सुख है न स्वर्ग में सुख है। हे रामजी ! मैं चौदह लोकों में घूमा। कहीं भी शाश्वत सुख नहीं है। केवल एक जगह मुझे शाश्वत सुख दिखा। जहाँ संत का मन ठहरता है वहीं सुख है और कहीं भी सुख नहीं।"
संत का मन कहाँ ठहरता है ? निर्वषय पद में।
बंधस्थ
विषयासंगी
मुक्तो
निर्विषयस्तथा।
मन जब निर्विषय हो जाता है तब सुख मिलता है। मन निर्विषय कैसे हो ? हकीकत में विषय छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। बचपन छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। बचपन के खिलौनों को तुमने छोड़ा कि छूट गये ? तोतली-तोतली भाषा को तुमने छोड़ा कि छूट गयी ? बचपन के मित्रों को तुमने छोड़ा कि छूट गये ? छूट ये। बचपन छूट गया, किशोरावस्था भी छूट गयी और जवानी भी छूट रही है। जो छूट गया है उसको छूटने वाला समझो और जो अभी मिला है उसको पकड़ने की कोशिश न करो। वह भी छूट रहा है ऐसा समझ में आ जाये तो मन निर्विषयी होने लगेगा। संसार ने हमको बाँधा नहीं विषयों ने हमको बाँधा नहीं, लेकिन विषयों में सत्यबुद्धि करके, संसार में सत्यबुद्धि करके मन को सत्ता देकर हम आप ही उसमें फँस जाते हैं।
पहले के जमाने में तोते को पकड़ने के लिए नलिका का उपयोग करते थे। तोता जब उसके ऊपर बैठता था तो तोते के वजन से वह घूम जाती थी। उसके घूमने से तोता नीचे आ जाता था। वह समझता कि मुझे किसी ने उलट दिया है। तब वह और जोर से नलिका को पकड़ लेता था। हालाँकि वह वहाँ से आकाशगामी हो सकता था किन्तु उसको ऐसी भ्रांति घुस जाती थी कि किसी ने मुझे गिरा दिया। बंदर को पकड़ने वाले लोग संकरे मुंह के बर्तन में खाने पीने का सामान डालते हैं। बंदर मुट्ठी पकड़कर बैठ जाते हैं तो हाथ बाहर नहीं निकल पाता। वे समझते हैं कि अन्दर से किसी ने हाथ को पकड़ा है। यद्यपि वह मुट्ठी से सामान छोड़ दे तो उसी क्षण उसका हाथ बाहर निकल सकता है। किन्तु 'किसी के द्वारा हाथ पकड़ा गया है' इस भ्रम के कारण वह बेचारा सचमुच पकड़ा जाता है। ऐसे ही मन को सत्ता देकर हम विषयों को पकड़ लेते हैं और जन्म मरण के भागी हो जाते हैं। मौत हमें पकड़ ले, ऐसे हम हो जाते हैं।
हमारी नासमझी के कारण हमे विषयों में सत्यबुद्धि होती है। विषयों में सत्यबुद्धि होने के कारण चित्त में वासना रह जाती है। इसीलिए बंधन में पड़ जाते हैं। फिर वासनाओं के अनुसार हम भटकते रहते हैं, जन्मों की यात्रा करते रहते हैं।
यदि मनुष्य गुरूओं की वाणी एवं शास्त्रवचनों का पालन करे तो मनुष्य में इतनी सारी शक्ति है कि अपने एक जीवन में हजारों बार आत्मसाक्षात्कार कर सकता है। हालाँकि एक बार आत्मसाक्षात्कार हो जाये तो दुबारा करने की जरूरत नहीं है। किन्तु हम विषय-भोग को इतना महत्त्व देते हैं कि हम विषयों को नहीं भोगते, वे विषय ही हमको भोग जाते हैं और हम विकारों के संस्कार में बँध जाते हैं।
यदि व्यतीत हुई परिस्थितियों को आप छोड़ते जायें और नयी परिस्थितियों को आप अंदर से पकड़ें नहीं तो आपका मन मुक्ति का भागी हो जायेगा। हम लोग गल्ती यह करते हैं कि किसी के धन को देखकर धनवान होने की इच्छा करते है और इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। किसी के रूप को देखकर रूपवान होने की इच्छा हो जाती है। यह ज्ञान होता ही नहीं कि धनवान हो, रूपवान हो चाहे सत्तावान हो लेकिन ये सब हैं मेरे ही आत्मा के विलासमात्र। ये सब मुझ चेतन की ही अभिव्यक्तियाँ हैं और अंत में यह दिखनेवाला रूप, धन, सत्ता आदि जो कुछ है वह सब काल-कराल की धारा में बीता जा रहा है। इस प्रकार के ज्ञान का अगर हम अवलंबन लें तो हमें कुछ बनने की इच्छा नहीं रहेगी। हम जहाँ हैं वहीं विश्रान्ति पाने का सौभाग्य खुल जायगा और हमारा बेड़ा पार हो जायगा।
भोक्ता अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता है इसलिए वह कुछ करके, कुछ पाकर, कुछ दिखाकर, कहीं जाकर सुखी होना चाहता है इसलिए मकान बनवाते हैं तो ऊपर नाम लिखवाते हैं- 'मगन-निवास.... छगन-निवास.....' ताकि लोग जानें मानें। तुम अपने-आप को नहीं जानते, इसीलिए लोगों से कुछ-कुछ मनवाना चाहते हो और लोग कुछ मानेंगे तो मानने वाले भी तो समय की धारा में बह जाएँगे। इस बात का हम ख्याल नहीं रखते।
परमात्मा तो तुम्हारी राह देख रहा है कि तुम्हारा मन कब संसार से उपराम हो ? कब तुम्हें ऐसी समझ आय कि संसार सब दुःख मिटाने में समर्थ नहीं है और संसार पूरा सुख देने में भी समर्थ नहीं है ? इस संसार ने तो भगवान राम के पिता राजा दशरथ को भी रुला दिया। संसार ने तो भगवान श्रीकृष्ण के होते हुए उनके बेटों को आपस में लड़वाकर मरवा दिया। जब स्वयं भगवान के जीवन में ऐसा हो सकता है तो फिर हमारे जीवन में दुःख आयें तो क्या आश्चर्य है या। संसार ने तो भगवान श्रीकृष्ण के होते हुए उनके बेटों को आपस में लड़वाकर मरवा दिया। जब स्वयं भगवान के जीवन में ऐसा हो सकता है तो फिर हमारे जीवन में दुःख आयें तो क्या आश्चर्य है ?
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा है। हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं, पत्नी को सुधारने में लगे हैं, पति को सुधारने में लगे हैं। पहले आप अपने मन को सुधारो फिर लोग अपने-आप सुधरने लग जायेंगे। विषयों की आसक्ति और जगत् में सत्यबुद्धि, ये दो बंधन के कारण हैं। विषयों में वैराग्यवृत्ति और परमात्मा में सत्यबुद्धि ये दो मुक्ति के कारण हैं।
पहले के जमाने में लोग जब आपस में मिलते थे तो पूछते थेः "क्या हालचाल है ? आपका चित्त अपने मूल कारण में तो है न ? आपका मन स्वरूप के चिन्तन में तो है न ? आपकी तपस्या ठीक से चलती है न ? आप स्वस्थ तो हो ? 'स्व' माने आत्मा। उसमें तो स्थित हो न ?' फिर जमाने ने करवट ली। आदमी कुछ नीचे गिरा, तब पूछने लगाः "कैसे हालचाल हैं ? धंधा-पानी कैसा है ? राज-काज कैसा चलता है ?" अब आदमी पूछता हैः "कैसी है तबियत ? अर्थात् हाड़-माँस, वात-पित्त-कफ, थूक बराबर है कि कम-ज्यादा हो गया ?"
आपका यह स्थूल शरीर है, जो हररोज श्मशान की ओर जा रहा है, कल उसको जितनी आयुष्य थी उतनी आज नहीं है और अभी जितनी है उतनी कल नहीं रहेगी। ऐसे नश्वर शरीर का हालचाल पूछा जाने लगा है।
एक बाबाजी को किसी ने सुंदर दुशाला ओढ़ा दिया। कोई एक लफंगा आदमी उस दुशाले को लेकर भागा। बाबाजी जरा मनोबलवाले थे लेकिन बूढ़े थे। उन्होंने उस लफंगे का पीछा कियाः "मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। तू समझता क्या है ?" ऐसा कहकर दस-बीस कदम दौड़े। फिर बाबा ने मूँछ मरोड़ते हुए कहाः "तू कहीं भी जा, मैं तेरे को छोड़ूँगा नहीं।" ऐसा कहकर बाबाजी दूसरी दिशा में दौड़ने लगे।
लोगों ने विपरीत दिशा में दौड़ते देखकर बाबाजी को कहाः "आप 'नहीं छोडूँगा.... नहीं छोडूँगा....'' ऐसा कहते जाते हो और दौड़ते उल्टी दिशा में हो ! वह गाँव की ओर जा रहा है और आप गाँव के बाहर श्मशान की ओर जा रहे हो ! ऐसा क्यों ?"
तब बाबाजी ने कहाः "वह कितना भी गाँव में घुस जाये लेकिन आखिर आयेगा तो श्मशान में ही। कितना भी गाँव में भाग जाये, बाहर भाग जाये लेकिन मैं श्मशान में जाकर बैठता हूँ क्योंकि उसका आखिरी एड्रेस (पता) तो वही है।"
ऐसे ही मनुष्य कितना भी छल-कपट करे, 'मेरा-तेरा' करे लेकिन मनुष्य को यह याद रहना चाहिए की इस स्थूल शरीर का आखिरी एड्रेस तो श्मशान ही है।
पड़ा
रहेगा माल
खजाना छोड़
त्रिया सुत
जाना है।
कर
सत्संग अभी से
प्यारे, नहीं
तो फिर पछताना
है।।
खिला-पिलाकर
देह बढ़ायी,
वह भी अग्नि
में जलाना है।
कर
सत्संग अभी से
प्यारे नहीं
तो फिर पछताना
है।।
मन को कभी-कभी यह समझाया करो। इस देह की मृत्यु कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। मन के जिन भावों से व्यक्ति बंधन बना लेता है उन्हीं भावों के कारण आदमी दीन-दुःखी हो रहा है और दर-दर की ठोकरें खा रहा है, हजारों माताओं के गर्भ में उल्टा लटककर दुःखी हो रहा है, अपमानित हो रहा है, वे भाव यदि बदल जायें तो वही आदमी देव होकर पूजा जाता है।
योगवाशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठजी कहते हैं- "हे रामजी ! जिन्होंने पुरूषार्थ का त्याग किया है वे नीच गति को प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने पुरूषार्थ का अवलंबन लिया है वे महान् हो गये हैं। अभी जो लोकपाल होकर बैठे हैं या यमराज की पदवी को शोभायमान कर रहे हैं, वे भी किसी समय के साधारण मनुष्यों में से पुरूषार्थ करके महान् बने हैं। हजार आँखों वाले जो इन्द्रदेव बने हैं, देवों पर शासन करते हैं वे भी पुरूषार्थ के बल से ही इन्द्र बने हैं। जीव यदि पुरूषार्थ का त्याग कर देता और विषय-विकारों को भोगने लगता है तो फिर नीच से नीच गति को पाकर कीड़ा होकर भटकता है। वही जीव है जो पुरूषार्थ करके इन्द्र बन जाता है और वही जीव है जो पुरूषार्थ त्यागकर कीड़ा बनकर रेंगता है। चलते-चलते पैर के नीचे आ जाता है, कुचला जाता है और कराहता रहता है। कोई उसकी फरियाद तक नहीं सुनता।
वही पुरूषार्थ करने वाला चैतन्य, भगवान विष्णु होकर विराजमान है, वही पुरूषार्थ करने वाला चैतन्य, शिव होकर पूजा जा रहा है और वही पुरूषार्थहीन चैतन्य, चूहा होकर बिल्ली से जान बचाने के लिए बिल में भागे जा रहा है। अतः मनुष्य जैसा पुरूषार्थ करता है उसके अनुसार उसे गति प्राप्त होती है।
पुरूषार्थ करना आपके हाथ की बात है। मंदिर में जाना अच्छा है, जाना चाहिए। शास्त्र, गुरू, मंदिर, माता-पिता ये कुछ हद तक तो सहायक हैं लेकिन आदमी अपना पुरूषार्थ अगर नहीं करता तो मोक्ष के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं।
जो मन जगत को सच्चा मानकर उलझ जाता है और बंधन बनाता है, उसी मन में यह शक्ति है कि तत्त्वविचार करके, मोह नष्ट करके, अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति करके मुक्ति का अनुभव कर ले और अभी अभी मुक्त हो जाये।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के विध्वंसकारी, विकारी हिस्से को शांति, सर्जन और सत्कर्म में बदलकर, सत्यस्वरूप का ध्यान और ज्ञान पाकर परम-पद पाने के रास्ते सजग हो जाये।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जागो
अपनी महिमा
में.........
आत्मबल ही वास्तविक बल है, आत्मभाव ही वास्तविक भाव है, आत्मदृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है और आत्मप्रीति ही वास्तविक प्रीति है।
किसी भी व्यक्ति का बाहर से तब तक पतन नहीं होता जब तक उसका भीतर से पतन नहीं होता। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का बाह्य पतन तब तक संभव नहीं होता जब तक कि उसका भीतरी पतन न हो जाये। किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का तब तक उत्थान भी नहीं होता जब तक कि उसका भीतरी उत्थान न हो। अर्थात् मनुष्य पहले भीतर से गिरता है फिर बाहर से गिरता है और पहले भीतर से उठता है तब बाहर से उठा हुआ दिखता है।
भीतरी पतन या उत्थान क्या है ? आध्यात्मिक उत्थान या पतन ही भीतरी उत्थान या पतन है। आध्यात्मिक पतन के कारण ही अनेक राष्ट्रों का पतन हुआ है। अतः अब भीतर से उठो। कहते है कि 'खटखटाओ तो खुलेगा और माँगो तो मिलेगा।' लेकिन खटखटाना क्या है और माँगना क्या है ?
'खटखटाओ तो खुलेगा' – इसका मतलब है कि ज्ञान के द्वार को खटखटाओ, अपने को खोजो। उपदेश सुनते-सुनते बहुत समय बीत गया। संसार की भट्टी में पचते-पचते युग बीत गये। लेकिन अब जरा अपने भीतर के द्वार खटखटाओ। दिन-रात होने वाली अपने भीतर की 'शिवोऽहम्' की आवाज को सुनो। अपने व्यावहारिक वेदान्त को अब जीवन में भी लाओ।
जो व्यक्ति अपने आत्मरत्न को छोड़कर, अपने आत्मदेव को छोड़कर अन्य किसी के आगे माँगता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है उसकी माँग पूरी नहीं होती। उसकी इच्छाएँ, उसकी माँगे तो तब पूरी होती हैं जब उसे नश्वर जगत की कोई इच्छा ही न रहे। जाने अनजाने देहाध्यास का त्याग हो जाता और अनजाने में ही अथवा जानकर आदमी इच्छाओं से पार हो जाता है उसी के हृदय में से स्फुरति शुद्ध संकल्प फलित हो जाता है। सारे रहस्यों की यह कुंजी है।
यही वह भारत देश है जहाँ कभी लोगों की दृष्टि में एकत्व विषय-भोगों के प्रति बेपरवाही थी। उस समय भारत उच्चता के शिखर पर आसीन था। सोने के बर्तनों में भोजन कराकर वे बर्तन भी अतिथि को अर्पण कर दिये जाते थे और अतिथि उन्हें ले जाने को तैयार तक न होते थे। फिर भी घर में धन-धान्य बढ़ता रहता था। और आज....?
जब भारत का भीतर से पतन होने लगा, लोग इच्छाओं-वासनाओं के गुलाम होने लगे तबसे भारत में परेशानियाँ भी बढ़ने लगीं। लोग अध्यात्म को भूलने लगे तो भौतिक सुख-सुविधाएँ भी उन्हें छोड़ने लगीं।
यदि अपनी आत्ममहिमा में जाग जाओ तो अब भी तुम अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हो। अपने भूले हुए अध्यात्म पथ पर पुनः चल पड़ो, इच्छा वासनाओं से ऊपर उठो और अपने ज्ञान के द्वार को खटखटाओ, फिर देखो, तुम कितने महान हो.....! कितने ऊँचे हो....! कितने अमर हो....!
दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं। दोनों से पूछोगे तो दोनों की गहराई से आवाज आयेगीः "मैं निर्दोष हूँ।"
केस कोर्ट में गया। वहाँ न्यायाधीश मुजरिम से पूछता हैः
"तुमने यह गुनाह किया है ?"
जवाब होगाः "मैं निर्दोष हूँ।"
केस चला। अपराधी को सजा मिली। अपील में भी उसकी सुनवाई न हुई। उसको जेल भेज दिया गया। वहाँ कोई पूछेः "क्या बात है ?"
वह बोलेगाः "आजकल सरकार ऐसी है.... न्याय अंधा है... गवाह बेवकूफ थे... दुश्मन थे... मैं निर्दोष हूँ।"
हाँ भैया ! तू वास्तव में निर्दोष है। तेरे असली स्वरूप में निर्दोषता है। इसलिए कितने भी दोष होने के बावजूद भी हर पक्ष का व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करना चाहता है। यह क्या तुम्हारे निर्दोषपने का स्वभाव नहीं है ?
रोज देखते हो कि जो फूल खिलते हैं वे मुरझा जाते हैं। जो पेड़ पौधे दिखते हैं वे एक दिन गिर पड़ेंगे। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि जितने भी जीव पैदा हुए हैं वे एक दिन मर जाएँगे, नष्ट हो जायेंगे। सब जानते हैं कि जो जन्मता है वह एक दिन अवश्य मरता है। परदादा, दादा, काका, मामा आदि कई गये और अभी भी जा रहे हैं, फिर भी हर इन्सान चाहता है कि 'मैं तो जिन्दा रहूँ।' पचास सालवाला साठ साल देखना चाहता है, साठवाला सत्तर, सत्तरवाला अस्सी साल तक जीना चाहता है। अस्सी वाला सौ साल तक जीना चाहता है। किसी के सौ पूरे हो भी जायें फिर पूछोः 'मरना चाहते हो ?' बाहर से तो वह बोलेगा कि, 'हाँ, मर जाऊँ तो कोई हरकत नहीं। संसार में कुछ रखा नहीं।' लेकिन जब मौत आकर खड़ी हो जाती है तब दवाओं-इन्जेक्शनों का सहारा लेता है।
वेदान्त कहता है कि तुम्हारी गहराई में जो अमरता है वही तुम्हें न मरने की प्रेरणा देती है। तुम वास्तव में ऐसे हो जिसने कभी मौत देखी ही नहीं, जिसको मौत पसंद ही नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, तुम वास्तव में अमर आत्मा हो। लेकिन इस शरीर की अमरता कब तक रहेगी ? इस पंचभौतिक शरीर को पकड़कर कब तक अमर होगे ? इस देह, मन और इन्द्रियों के साथ जुड़कर कब तक अपने को निर्दोष मानोगे ?
गहराई में तुम्हारा स्वरूप निर्दोष है इसीलिए इससे दोष होने पर भी तुम अपने को दोषी नहीं मानते। गहराई में तुम्हारा स्वरूप अमर होने के कारण ही तुम मरना नहीं चाहते। अपने 'मैं' को निर्दोष साबित करना ही तुम्हारा स्वभाव है। अमरता तुम्हारा स्वभाव है। तुम वास्तव में निर्दोष आत्मा हो, चैतन्य हो, अमर हो। अपने निर्दोष स्वभाव को, अपने अमर स्वभाव को याद करो तो तुम अभी मुक्त हो।
किन्तु अपने निर्दोष स्वभाव को भूलकर, अपने अमर स्वभाव को भूलकर जब लोग शरीर और इन्द्रियों में उलझ जाते हैं, पंचभौतिक शरीर को ही, देह को ही मैं मानने लग जाते हैं, देहाध्यास आ जाता है, कल्पित संसार में आसक्त होने लगते हैं, क्षुद्र इच्छा-वासनाओं के पीछे भागने लगते हैं तभी उन व्यक्तियों का, समाज का और राष्ट्र का पतन होने लगता है। जिन राष्ट्रों में व्यावहारिक वेदान्त आ जाता है उनका भौतिक उत्थान भी होता है। जिन फकीरों के जीवन में, जिन संतों और साधकों के जीवन में, व्यावहारिक वेदान्त आता है, चहुँ ओर से सफलताएँ उनका इन्तजार करती है। लेकिन जो छल का आश्रय लेता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। छल दूसरे से किया जाता है, भय दूसरे से होता है। निर्भय रहना, छलरहित रहना यह वेदान्त है, अध्यात्म है। छलरहित होते ही चित्त निर्दोष होने लगता है।
मन, क्रम,
बचन छांडी छल
जब लग जनन
तुम्हार।
तब
लगि
स्वप्नेहुँ
सुख नहीं करे
कोटि उपचार।।
छलरहित होना, भयरहित होना, क्रोधरहित होना, वासनारहित होना यह वास्तविक वेदान्त है। इन सबको छोड़कर अपनी महिमा में जाग जाना ही वास्तविक वेदान्त है। जब तुम अपनी महिमा में आराम पाते हो, अपने-आप में जब तुम होते हो तब तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा संकल्प भी प्रकृति के नियमों को बदल देता है। जब तुम अपनी महिमा में होते हो तब प्रकृति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए करवटें लिया करती हैं और जब तुम अपनी महिमा से दूर हो जाते हो तब प्रकृति तुम्हें पद-पद पर ठोकरें मारती है, तमाचे मारती है ताकि तुम पुनः सुधर जाओ।
इसलिए वेदान्तरूपी सिंह को अपने जीवन में लाओ। निर्भयता, प्रेम और निःस्वार्थता के उदात्त गुणों को विकसित करो। यही भाव रखो कि, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए और संसार मुझे सब देने में समर्थ भी नहीं है। किसी ब्रह्मवेत्ता के चरणों में बैठकर ब्रह्मज्ञान का श्रवण करो।
सारी दुनिया मिलकर भी एक ब्रह्मवेत्ता की सेवा कर सकने में समर्थ नहीं है। जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है ऐसे ब्रह्मवेत्ता को सारी दुनिया भी मिलकर खुश नहीं कर सकती, रिझा नहीं सकती क्योंकि उसने ऐसी खुशी को पाया है, वह अपने आप में ऐसा रिझा है कि दुनिया की तुच्छ चीजें उसे क्या रिझायेंगी ? संसार के पास है ही क्या जो वह ब्रह्मवेत्ता को दे सके ? ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप में, अपने अनंत ब्रह्माण्डों में व्यापक चैतन्य में जगे हैं। उन्हें संसार क्या दे सकता है ?
अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को आप भी जान लो। फिर आप भी महसूस करोगे किः संसार के पास ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे दे सके। संसार यदि देगा भी तो मेरे इस नश्वर शरीर को दे सकता है, मेरे नश्वर शरीर के व्यवहार सहयोग दे सकता है लेकिन मुझ अनंत तक उसकी पहुँच ही कहाँ ? मुझ चैतन्यस्वरूप में सारे संसार के सहयोग का कोई प्रवेश ही नहीं है।
तुम सहायता लेने की इच्छा मत रखो वरन् देने की इच्छा रखो। खुद याचक के नहीं, दाता के स्थान पर बैठो। दूसरों को मदद करने की भावना से, दूसरों का दुःख निवृत्त करने का सोचते ही तुम्हारे दुःख निवृत्त होने लगते हैं। किन्तु इसका मतलब यह नहीं किः 'मेरा दुःख निवृत्त हो इसलिए मैं दूसरों के दुःख दूर करूँ।' दिखावे के लिए दूसरों का सोचो और भीतर में अपना दुःख मिटाने की भावना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरन् तुम तो यही सोचो कि, 'मेरा संसार में कुछ नहीं है और मुझे संसार से कुछ चाहिए भी नहीं। मेरा केवल परमात्मा है' और इससे 'मैं खुद परमात्मा हूँ, देवों का देव हूँ, शाहों का शाह हूँ...' ऐसा अनुभव होने लगेगा। तुम अपने आत्मभाव में जाग जाओगे।
तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति में लग जाना, छोटी-छोटी बातों में उलझ जाना, छोटी-छोटी चीजों से आकर्षित हो जाना – ये पतन के कारण हैं। इन्द्रियों के द्वारा संसार का सुख लेने की इच्छा ही हमें छोटा बना देती है और इन इच्छाओं के त्याग से, अपने स्वभाव में जागने से हम महिमावंत होने लगते हैं। संसार की तुच्छ इच्छाएँ जितनी बढ़ती हैं उतना ही मनुष्य भीतर से छोटा होता जाता है और जितना इच्छाओं का त्याग करता है उतना ही वह महान होता जाता है।
किसी वस्तु की इच्छा हुई और पदार्थ मिल गया तो लोग समझते हैं कि इच्छा पूरी हुई। इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं वरन् गहरी घुस जाती हैं। इच्छा पूरी करने के लिए उद्योग किया... सुख मिला तो इच्छा औऱ गहरी हो गयी। दुःख मिला तो भय हो गया। इस प्रकार नासमझी से इच्छा उत्पन्न होती है, मजदूरी से इच्छा पूरी होती है और परिणाम हर्ष-शोक की थप्पड़ें लगती हैं। जबकि विवेक से इच्छा निवृत्त हो जाती है और मनुष्य अपने आत्मसिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है।
ऐसी बुद्धि का विकास हो तो मनुष्य विवेक के द्वारा ही साक्षात्कार कर ले। नहीं तो, ध्यान-भजन के द्वारा योग्यता हासिल की, सामर्थ्य प्राप्त किया और फिर उसी सामर्थ्य को अगर ऐहिक क्षणभंगुर पदार्थों में नष्ट कर दिया तो यात्रा लम्बी हो जाती है। जितनी-जितनी वासनाएँ होती हैं उतना-उतना आदमी भीतर से गिरने लगता है। फिर बाहर से भी गिरने लगता है और चित्त की निःसंकल्प अवस्था जितनी-जितनी बढ़ती जाती है उतना-उतना आदमी महान् होता जाता है।
चाह
चमारी चूहड़ी,
अति नीचन की
नीच।
तू
तो पूरण
ब्रह्म था, जो
चाह न होती
बीच।।
चाह उठे तब सावधानी से उसको निहारो और सोचो कि चाह उठी... पूरी हो गयी... फिर क्या ? आखिर सब स्वप्न। अतः जब-जब सुख लेने की इच्छा उठे तब-तब अन्य लोगों को सुख देना आरम्भ कर दो।
रबिया खरीदी हुई गुलाम थी लेकिन जब उसके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश हुआ तब उसको खरीदने वाला उसका मालिक ही उसके चरणों में गिर पड़ा। क्यों ? क्योंकि रबिया को सुख की चाह न थी, विषय-विलासों की चाह न थी..... उसकी एकमात्र चाह तो केवल परमात्मा को पाने की ही थी। रबिया प्रार्थना करती थीः 'हे मालिक ! मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मुसीबतों से बचने के लिए तुझे प्यार नहीं करती लेकिन तू प्यारा है इसीलिए मैं तुझे प्यार करती हूँ। मैं दोजख से बचने के लिए तुझे नहीं रिझाती हूँ और बिस्त पाने की चाह भी मुझे नहीं है। किन्तु हे खुदा ! तू सचमुच में रिझाने योग्य है, सचमुच में मेरा है इसलिए मैं तुझे रिझा रही हूँ, प्यार कर रही हूँ।"
निर्दोष हृदय की प्रार्थना हो स्वीकार की जाती है, बिना फरियाद की प्रार्थना ही सुनी जाती है। तृष्णावान् से तो वृक्ष भी भय पाते हैं जबकि वासनारहित मनुष्य से समस्त संसार आनंदित होता है तो उसकी प्रार्थना परमात्मा शीघ्र कैसे न सुनेगा ?
तुमने अनुभव किया होगा कि घर में जो मेहमान आकर कुछ-न-कुछ माँगता ही रहता है उससे तुम ऊब जाते हो और उसे देने का दिल भी नहीं होता और जिसे कुछ नहीं चाहिए उस अतिथि की सेवा करके तुम आनंद का अनुभव करते हो।
मान लो, तुम बस स्टेण्ड पर खड़े हो। कोई भिखारी तुमसे कुछ माँगे तो ऐसा नहीं कि तुम खुश होकर देते हो बल्कि 'यह बला टले' इसलिए देते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को तुम अठन्नी (पचास पैसे) देने का विचार करते हो किन्तु वह ज्यादा माँगता है तो पाँच-दस पैसे में ही निपटा देते हो और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई शात स्वभाव का है, ऐसे ही खड़ा है, केवल थोड़ा-सा माँगने का संकेत करता है, माँगने की तीव्र इच्छा नहीं है, उसको आप चवन्नी के बदले रूपया देने को राजी हो जाते हो।
.....तो जिसको लेने की इच्छा है उसको देने में आप राजी नहीं होते और जिसको कोई इच्छा ही नहीं उसकी सेवा करके आप संतोष का अनुभव करते हो। अतः आप स्वयं भी इच्छाओं से ऊपर उठो... इच्छाओं का त्याग करो... फिर देखोगे कि सारी दुनिया आपकी सेवा करने को पीछे दौड़ी चली आयेगी।
भागती
फिरती थी
दुनिया जब तलब
करते थे हम।
अब
ठुकरा दी तो
वो बेकरार आने
को है।।
ज्यों-ज्यों तुम इच्छाओं, वासनाओं के पीछे लगते हो त्यों-त्यों ठुकराये जाते हो और ज्यों-ज्यों तुम क्षुद्र इच्छाओं से, क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठते हो त्यों ही इच्छित पदार्थ तुम्हारा पीछा करने लगते हैं। फिर तुम यश न चाहोगे तो भी यश मिलेगा, मान न चाहोगे तब भी हजारों लोग मान देंगे। स्वर्ग न चाहोगे तब भी स्वर्ग के दूत तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जायेंगे। तुम तो बस, अपनी महिमा में जाग जाओ, अपने-आप में आराम पा लो एक बार।
अपने-आप में कैसे जगें ? अपने स्वभाव को जान लो एक बार। तुम अपने को निर्दोष मानते हो, तुम अपने को सदा अमर बनाये रखना चाहते हो, तुम सब कुछ जानना चाहते हो। शरीर, मन एवं बुद्धि में हजारों-हजारों दोष होते हुए भी तुम निर्दोष हो, हजारों-हजारों बार शरीर के मरने पर भी तुम अमर हो इस असली स्वभाव को जान लो एक बार....। मन, बुद्धि आदि में दोष होते हुए भी तुम्हारा वास्तविक रूप कभी दूषित नहीं होता और शरीर, मन, बुद्धि के चमकने से तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी नहीं चमकता ऐसे तुम निस्संग हो। आलीशान महल होने से तुम आलीशान नहीं हो जाते और तुम्हारी झोंपड़ी टूटी-फूटी होने से तुम टूटते-फूटते नहीं हो। समाज में ऊँचा पद मिलता है उससे तुम ऊँचे नहीं होते और कोई तुम्हें नहीं पहचानता उससे तुम नीचे नहीं होते। तुम तो ऐसी चीज हो कि प्रकृति में चाहे कितनी भी उथल-पुथल मच जाये किन्तु तुम्हारा एक बाल तक बाँका नहीं होता। ऐसे अपने अपरिवर्तनीय स्वभाव को याद करो....
कभी
न छूटे पिण्ड
दुःखों से,
जिसे ब्रह्म
का ज्ञान
नहीं।
जरा सा अपमान होता है तो विह्वल हो जाते हो, अहं को जरा सी चोट लगती है तो परेशान हो जाते हो। कब तक जुड़े रहोगे देहाध्यास से ? कब तक जुड़े रहोगे अहं से ? कब तक क्षुद्र वासनाओं और क्षुद्र 'मैं' को पकड़ो रखोगे ? तुम तो बस, अपनी महिमा में जाग जाओ। इस क्षुद्र 'मैं' के बुलबुले को फूट जाने दो। तुच्छ इच्छा वासनाओं को नष्ट हो जाने दो। मिट जाने दो मान-अपमान को। तभी तुम अपने आप में जाग सकोगे।
ऐसी जगह जाओ जहाँ अपमान होता हो इस अहंकार का। इस अहंकार को मिटाने के लिए ही बड़े-बड़े राजा-महाराजा गुरू के चरणों में जाते थे और गुरू लोग उनको बोलते थे कि जाओ, भिक्षा माँगकर आओ। गुरू आज्ञा को शिरोधार्य करके बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी भिक्षा लेने के लिए गाँव-गाँव में जाते थे क्योंकि वे जानते थे कि अपनी महिमा में जगाने में केवल सदगुरू की समर्थ हैं एवं उनकी आज्ञा के पालन में ही शिष्य का परम कल्याण निहित है।
अपने क्षुद्र सुख से ऊपर उठकर सबके सुखों की ओर ध्यान दो। पड़ोसियों का ख्याल रखो। अनेक शरीरों में एक का एक मेरा अपना आपा है इस भाव से कार्य करो। जैसे तुम अपने शरीर के प्रत्येक अंग का ख्याल रखते हो वैसे ही अपने पड़ोस का, अपने वातावरण का ख्याल रखकर जब भारत जीता था उस समय भारत के यश में चार चाँद लगे हुए थे। लेकिन अब घर-घर में, पड़ोस-पड़ोस में क्षुद्र स्वार्थ के लिए ही कार्य होता है, परिच्छिन्नता बढ़ गई है, लोग आध्यात्मिकता से गिर गये हैं इसीलिए दुःख बढ़ गया है।
जहाँ भीतर से आत्मभाव होता है वहाँ व्यवहार में भी सफलता मिलती है, आदमी प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और उसकी बुद्धि ठीक निर्णय लेती है। किन्तु जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ लोगों की बुद्धि के निर्णय भी ऐसे ही हो जाते हैं। जहाँ देहाध्यास आ जाता है वहाँ विचार भी हलके हो जाते हैं। 'मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा....'
'स्वामी रामतीर्थ बोलते थेः "पहले जो भारतवासी मूर्तिपूजा करते थे वे ईमानदारी से करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि अब व्यक्ति तत्त्वविचार में स्थिर नहीं रह सकता तो चलो, मूर्तियों की परंपरा चालू कर दो। मूर्तिपूजा इसलिए रखी गयी कि प्रार्थना करते-करते मनुष्य अपना अहं मिटा सके और परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सके। लकिन आदमी ने अहं मिटाने पर तो ध्यान नहीं दिया और उल्टा 'मैं मंदिर जाता हूँ... इतने साल से माला करता हूँ, यह कोई कम है क्या ?' ऐसा सोचकर अपना क्षुद्र अहं और बढ़ा दिया। फिर प्रार्थना करने लगा कि 'मैं गुलाम हूँ.... मैं पापी हूँ... मैं दीन हूँ.... मैं हीन हूँ.... मैं गुलाम हूँ.... मैं गुलाम हूँ....' ऐसा सोचा तो गोरे और यवन आकर गुलाम बना गये।
'मैं दीन हूँ.... हीन हूँ.... ' करके अपनी महिमा को भूल गये इसीलिये दीनता, हीनता और तुच्छता व्याप्त हो गई। भारत के पतन के अनेक कारणों में एक कारण यह भी है। दूसरा कारण है असहिष्णुता और ईर्ष्या। ईर्ष्या दूसरे से होती है। अपने आत्मतत्त्व के ज्ञान से, अध्यात्म के ज्ञान से, वेदान्त के ज्ञान से जब नीचे आते हैं तभी ईर्ष्या होती है। भय भी तभी होता है जब दूसरा होता है। अपने वेदान्तज्ञान में तो भय, ईर्ष्या, दीनता-हीनता को कोई स्थान ही नहीं है। किन्तु भारतवासी उसको भूल बैठे हैं इसीलिए दुःखी हो रहे हैं।
ईश्वर के पाँच महाभूत भी भेदभाव नहीं करते। दुराचारी से दुराचारी आदमी को भी रहने के लिए पृथ्वी जगह देती है। गंगा कभी ऐसा नहीं सोचती कि जो सज्जन है उसे मैं शीतल जल दूँ और दुर्जन को गरम जल दूँ अथवा गाय पीती है तो अमृत जैसा जल दूँ और सिंह आये तो जहरीला जल दूँ। सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चंद्रमा सभी को समान रूप से चाँदनी देता है। हवाएँ बहने में कभी विषमता नहीं करतीं, सूर्य-चंद्रमा कभी विषमता का व्यवहार नहीं करते, पृथ्वी कभी विषमता का व्यवहार नहीं करती। जब ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में, ईश्वर के बनाये हुए भूतों में समता है तो ईश्वर में विषमता कैसे हो सकती है ? अतः तुम भी ईश्वरत्व को पाना चाहते हो तो किसी से भी विषमता का व्यवहार मत करो। सबके प्रति समता रखो। किन्तु समता का मतलव कायरता नहीं, समता का मतलव पलायनवादिता नही। समता का मतलब है सब में एक ही परमात्मा को निहारना, सबका कल्याण चाहना।
भगवान स्वयं सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दण्ड देते हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा हैः
परित्राणाय
साधूनां
विनाशाय च
दुष्कृताम्।
भगवान कहते हैं कि, 'मैं साधुओं की रक्षा एवं दुष्टों का विनाश करता हूँ।' लेकिन जिसके अन्दर समता है। जैसे आप अपने पैर के फोड़े को चिरवा डालते हैं तो उस पैर से आपकी दुश्मनी थोड़े ही है। ऐसे ही भगवान दुष्टों का विनाश भी करते हैं तो उनके कल्याण के लिए ही। माँ बच्चे को डाँटती है, मारती है और चॉकलेट भी देती है। तो जैसे माँ का चॉकलेट देना प्यार है वैसे ही थप्पड़ मारना भी प्यार ही है क्योंकि इसमें भी बालक का हित ही छुपा हुआ होता है। ऐसे ही भगवान दुष्टों को मारकर, उनको पाप करने से रोककर उन्हें सदगति ही देते हैं। इसलिए भगवान उन्हें मारकर भी समत्व में ही होते हैं।
हम अगर किसी से कलह करते हैं तो उसके कल्याण के लिए करते हैं क्या ? हम किसी को डाँटते हैं तो उसके मंगल के लिए डाँटते हैं क्या ? नहीं, वरन् अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्षुद्र अहं को पोसने के लिए दूसरों को डाँटते है। यदि किसी के मंगल के लिये यह सब करते हो, कल्याण के लिए करते हो तो तुम आध्यात्मिकता में हो। लेकिन किसी को डराकर कुछ हड़प कर लेना या अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को प्यार करना यह आध्यात्मिकता नहीं है। तुम दुकान पर ग्राहकों से प्यार से बात करते हो तो बताओ, वह प्यार आध्यात्मिकता का है स्वार्थयुक्त है ? जीवन में जितना-जितना स्वार्थ होता है उतना-उतना हम आध्यात्मिकता से नीचे, वेदान्त से नीचे आ जाते हैं और जितनी-जितनी निःस्वार्थता होती है उतने ही हम वेदान्त के करीब होते हैं।
कोई कह सकता हैः "बाबा जी ! यदि हम पूरे निःस्वार्थी हो जायेंगे तो कमायेंगे कैसे ? खायेंगे क्या ?" अरे ! यदि तुम स्वार्थरहिर हो जाओगे तो रूपये-पैसे तुम्हारे गुलाम बन जायेंगे। जगत की वस्तुएँ तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेंगी। जितना तुम वेदान्त को जीवन में लाओगे उतनी ही संसार की वस्तुएँ तुम्हारे पीछे पाले हुए कुत्ते की तरह आयेंगी। प्रार्थनाएँ तभी स्वीकार होती हैं जब आप जाने-अनजाने में निर्वासनिक हो जाते हो, फिर भले चाहे एक क्षण के लिए ही क्यों न हो। उस समय आपके मन में जो संकल्प उठता है वह फलित हो जाता है।
महापुरूष लोग निर्वासनिक पद में ही प्रतिष्ठित होते हैं। यही कारण है कि उनके आगे हजारों-हजारों लोगों को लाभ होता है, उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। वास्तविक महापुरूष भी हैं जिन्हें अपने लिये कुछ नहीं चाहिए, जो अपनी महिमा में जगे हुए होते हैं। तुम भी अपने असली स्वरूप को जानो, अपनी महिमा को जानो, क्षुद्र स्वार्थ को त्याग कर निर्वासनिक पद में आरूढ़ हो जाओ।
.......और यह कठिन भी नहीं है क्योंकि पूरा अध्यात्म का खजाना तुम्हारे भीतर ही है। इतना खजाना तुम्हारे अंदर है और तुम दर-दर की ठोकरें खा-खाकर, अनेकों माताओं के गर्भ में लटक-लटक कर, सुखों के पीछे भटक-भटक कर कब तक यात्रा करते रहोगे ? अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जानकर मुक्त हो जाओ। इच्छाओं के पीछे अपना जीवन मत गँवाओ, वरन् जब वे उठें तब उन्हें निहारो। ऐसा करने से वे कम होने लगेंगे और इच्छाओं का, संकल्पों का प्रभाव कम होते ही तुम्हारा अपना प्रभाव तुम्हें पता चलेगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
तीन
प्रकार की
विद्याएँ
तीन प्रकार की विद्याएँ होती हैं-
1. लौकिक विद्याः जिसे हम स्कूल कालेज में पढ़ते हैं। यह विद्या केवल पेट भरने की विद्या है।
2. योगविद्याः इस लोक और परलोक के रहस्य जानने कि विद्या।
3. आत्मविद्याः आत्मा-परमात्मा की विद्या, परमात्मा के साक्षात्कार की विद्या, परमात्मा के साथ एकता की विद्या।
लौकिक विद्या शारीरिक सुविधा के उपयोग में आती है। योगविद्या से इस लोक एवं परलोक के रहस्य खुलने लगते हैं एवं आत्मविद्या से परमात्मा के साथ एकता हो जाती है। जीवन में इन तीनों ही विद्याओं की प्राप्ति होनी चाहिए। लौकिक विद्या प्राप्त कर ली, किन्तु योगविद्या नहीं है तो जीवन में लौकिक चीजें बहुत मिलेंगी किन्तु भीतर शांति नहीं होगी। अशांति होगी, दुराचार होगा। लौकिक विद्या को पाकर थोड़ा कुछ सीख लिया, यहाँ तक कि बम बनाना सीख गये, फिर भी हृदय में अशांति की आग जलती रहेगी। अतः लौकिक विद्या के साथ आत्मविद्या अत्यावश्यक है।
जो लोग योगविद्या एवं आत्मविद्या का अभ्यास करते हैं, सुबह के समय थोड़ा योग का अभ्यास करते हैं, वे लोग लौकिक विद्या में भी शीघ्रता से सफल होते हैं। योग विद्या एवं ब्रह्मविद्या का थोड़ा सा अभ्यास करें तो लौकिक विद्या उनको आसानी से आ जाती है। लौकिक विद्या के अच्छे-अच्छे रहस्य वे लोग खोज सकते हैं।
जो वैज्ञानिक हैं वे भी जाने-अनजाने थोड़ा योगविद्या की शरण जाते हैं। रीसर्च करते-करते एकाग्र हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तब कोई रहस्य उनके हाथ लगता है। वे ही वैज्ञानिक अगर योगी होकर रीसर्च करें तो आध्यात्मिक रहस्य उनके हाथ लग सकते है। योगियों ने ऐसे-ऐसे रीसर्च कर रखे हैं जिनका बयान करना भी आज के आदमी के वश की बात नहीं है।
नाभि केन्द्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाये तो शरीर की सम्पूर्ण रचना ज्यों की त्यों दिखती है। योगियों ने शरीर को काटकूट कर (ऑपरेशन करके) भीतर नहीं देखा। वरन् उन्होंने स्थूल भौतिक शरीर को भी ध्यान की विधि से जाना है। यदि नाभि केन्द्र पर ध्यान स्थित करो तो तुम्हारे शरीर की छोटी-मोटी सब नाड़ियों की अदभुत रचना का पता चलेगा। योगियों ने ही खोज करके बताया है कि नाभि से कन्धे तक 72664 नाड़ियाँ हैं। ऐहिक विद्या से जिन केन्द्रों के दर्शन नहीं होते उन मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा और सहस्रार चक्रों की खोज योगविद्या द्वारा ही हुई है। एक-एक चक्र की क्या-क्या विशेषताएँ हैं यह भी योगविद्या से ही खोजा गया है। उन चक्रों का रूपान्तर कैसे किया जाये यह भी योगविद्या के द्वारा ही जाना गया है।
यदि मूलाधार केन्द्र का रूपान्तरण होता है तो काम, राम में बदल जाता है। व्यक्ति की दृष्टि विशाल हो जाती है। उसके कार्य 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी हो जाता है। उसके पदचिह्नों पर चलने के लिए कई लोग तैयार होते हैं। जैसे – महात्मा गाँधी का काम केन्द्र राम में रूपान्तरित हुआ तो वे विश्वविख्यात हो गये।
दूसरा केन्द्र है स्वाधिष्ठान। उसमें भय, घृणा, हिंसा और स्पर्धा रहती है। यह दूसरा केन्द्र यदि रूपान्तरित होता है तो भय की जगह पर निर्भयता का, हिंसा की जगह अहिंसा का, घृणा की जगह प्रेम का और स्पर्धा की जगह समता का जन्म होता है। व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ा प्यारा हो जाता है। अपने लिए एवं औरों के लिए बड़े काम का हो जाता है।
अपने शरीर में ऐसे सात केन्द्र हैं। इसकी खोज योगविद्या द्वारा ही हुई है। लौकिक विद्या ने इन केन्द्रों की खोज नहीं की। ऐसे ही, सृष्टि का आधार क्या है ? सृष्टिकर्त्ता से कैसे मिलें ? जीते जी मुक्ति का अनुभव कैसे हो ? यह खोज ब्रह्मविद्या के द्वारा ही हुई है।
लौकिक विद्या, योगविद्या और ब्रह्मविद्या। हम लोग लौकिक विद्या में तो थोड़ा-बहुत आगे बढ़ गये हैं लेकिन योग विद्या का ज्ञान नहीं है अतः व्यक्ति का शरीर जितना तंदुरूस्त होना चाहिए और मन जितना प्रसन्न एवं समझयुक्त होना चाहिए, वह नहीं है। इसीलिये चलचित्र देखकर कई ग्रेज्युएट व्यक्ति तक आत्महत्या कर लेते हैं। 'मरते हैं एक दूजे के लिए' फिल्म देखकर कई युवान-युवतियों ने आत्महत्या कर ली।
ऐहिक या लौकिक विद्या के साथ योग विद्या का सहारा नहीं है तो लौकिक विद्यावाला भी करप्शन (भ्रष्टाचार) करेगा। लड़ाई-झगड़े करके पेटपालु कुत्तों की नाई अपना जीवन बिताएगा। ऐहिक विद्या की यह एक बड़ी लाचारी है कि उसके होने के बावजूद भी जीवन में कोई सुख-शांति नहीं होती, शरीर का स्वास्थ्य और मन की दृढ़ता नहीं होती। आजकल की ऐहिक विद्या ऐसी हो गयी है कि विद्यार्थी गुलाम होकर ही युनिवर्सिटी से निकलते हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद सर्विस की खोज में लगे रहते हैं। सर्विस मिलने पर कहते हैं-
'I am the best servant of Indian Government..... I
am the best servant of British Government.'
आजकल की विद्या मनुष्य को Servant (नौकर) बनाती है। इन्द्रियों एवं मन का गुलाम बनाती है। ऐहिक विद्या मनुष्य को अहंकार का गुलाम बनाती है। ऐहिक विद्या मनुष्य को ईर्ष्या और स्पर्धा से नहीं छुड़ाती, काम-क्रोध की चोटों से नहीं बचाती। ऐहिक विद्या इन्सान को लोक-लोकान्तर की गतिविधियों का ज्ञान नहीं कराती। ऐहिक विद्या आदमी को पेट पालने के साधन प्रदान करती है, शरीर की सुविधाएँ बढ़ाने में मदद करती है। मनुष्य शरीर की सुविधाओं का जितना अधिक उपयोग करता है उतनी ही लाचारी उसके चित्त में घुस जाती है। शारीरिक सुविधाएँ जितनी भोगी जाती हैं और योगविद्या की तरफ जितनी लापरवाही बर्ती जाती है उतना ही मनुष्य अशांत होता जाता है। पाश्चात्य जगत् ने ऐहिक विद्या में, तकनीक के जगत में खूब तरक्की की किन्तु साथ ही साथ अशान्ति भी उतनी ही बढ़ी।
ऐहिक विद्या में अगर योग का संपुट दिया जाये तो मनुष्य ओजस्वी तेजस्वी बनता है। ऐहिक विद्या का आदर करना चाहिए किन्तु योगविद्या और आत्मविद्या को भूलकर ऐहिक विद्या में ही पूरी तरह से लिप्त हो जाना मानो अपने ही जीवन का अनादर करना है। जिसने अपने जीवन का ही अनादर कर दिया वह जीवनदाता का आदर कैसे कर सकता है ? जो अपने जीवन का एवं जीवनदाता का आदर नहीं कर सकता वह पूर्ण सुखी भी कैसे रह सकता है ?
ऑटोरिक्शा में तीन पहिये होते हैं। आगेवाला पहिया ठीक है, पीछे एक पहिया नहीं है और आगे वाला स्टीयरिंग नहीं है तो ऑटोरिक्शे की बॉडी (ढाँचा) दिखेगी, लेकिन उससे यात्रा नहीं होगी। ऐसे ही जीवन में ऐहिक विद्या तो हो, लेकिन उसके साथ योगविद्यारूपी पहिया न हो और ब्रह्मविद्यारूपी स्टीयरिंग न हो तो फिर मनुष्य अविद्या में ही उत्पन्न होकर, अविद्या में ही जीकर, अंत में अविद्या में ही मर जाता है। जैसे व्हील और स्टीयरिंग रहित ऑटोरिक्शा वहीं का वहीं पड़ा रहता है वैसे ही मनुष्य अविद्या में ही पड़ा रह जाता है, माया में ही पड़ा रह जाता है। माताओं के गर्भों में उल्टा लटकता ही रहता है, जन्म मरण के चक्र में फँसता ही रहता है क्योंकि ऐहिक विद्या के साथ-साथ ब्रह्मविद्या और योग विद्या नहीं मिली।
ऐहिक विद्या को पाने का तो एक निश्चित समय होता है किन्तु योग विद्या को, ब्रह्मविद्या को पाने के लिए दस-पन्द्रह या बीस वर्ष की अवधि नहीं होती। ऐहिक विद्या के साथ-साथ योगविद्या और ब्रह्मविद्या चलनी ही चाहिए। यदि मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में (साढ़े तीन बजे) उठकर योगविद्या का, ध्यान का अभ्यास करे तो उस समय कया हुआ ध्यान बहुत लाभ करता है।
जो लोग ब्रह्ममुहूर्त में जाग जाते हैं वे बड़े तेजस्वी होते हैं। जीवन की शक्तियाँ ह्रास होने का और स्वप्नदोष होने का समय प्रायः ब्रह्ममुहूर्त के बाद का ही होता है। जो ब्रह्ममुहूर्त में जाग जाता है उसके ओज की रक्षा होती है। जो ब्रह्ममुहूर्त में जगकर ध्यान के अभ्यास में संलग्न हो जाता है उसको जल्दी ध्यान लग जाता है। जिसका ध्यान लगने लगता है उसके बल, ओज, बुद्धि एवं योगसामर्थ्य बढ़ते हैं और आत्मज्ञान का मार्ग उसके लिए खुला हो जाता है।
सूर्योदय से दो पाँच मिनट पहले और दो पाँच मिनट बाद का समय संधिकाल है। इस समय एकाग्र होने में बड़ी मदद मिलती है। यदि ब्रह्ममुहूर्त में उठकर ध्यान करे, सूर्योदय के समय ध्यान करे, ब्रह्मविद्या का अभ्यास करे तो.... शिक्षकों से थोड़ी लौकिक विद्या तो सीखे किन्तु दूसरी विद्या उसके अंदर से ही प्रगट होने लगेगी। जो योगविद्या और ब्रह्मविद्या में आगे बढ़ते हैं उनको लौकिक विद्या बड़ी आसानी से प्राप्त होती है।
संत तुकाराम लौकिक विद्या पढ़ने में इतना समय न दे सके थे किन्तु उनके द्वारा गाये गये अभंग बम्बई यूनिवर्सिटी के एम. ए. के विद्यार्थियों को पढ़ाये जाते हैं।
संत एकनाथजी लौकिक विद्या भी पढ़े थे, योगविद्या भी पढ़े थे। विवेकानंद लौकिक विद्या पढ़े थे, योगविद्या भी पढ़े थे। उन्होंने आत्मविद्या का ज्ञान भी प्राप्त किया था। जो लौकिक विद्या सीखा है और उसे योगविद्या मिल जाये तो उसके जीवन में चार चाँद लग जाते हैं। उसके द्वारा बहुतों का हित हो सकता है।
योगविद्या एक बलप्रद विद्या है। वह बल अहंकार बढ़ाने वाला नहीं, वरन् जीवन के वास्तविक रहस्यों को प्रगटाने वाला और सदा सुखी रहने के काम आने वाला है। अगर मनुष्य के पास योग बल नहीं है तो फिर उसके पास धनबल, सत्ताबल और बाहुबल हो तो भी वह उस बल का क्या कर डाले ? कोई पता नहीं। सत्ता और धन का कैसा उपयोग करे ? कोई पता नहीं। जीवन में यदि योगविद्या और ब्रह्मविद्या साथ में हो तो...... भगवान राम के पास लौकिक विद्या के साथ योगविद्या और ब्रह्मविद्या थी तो हजारों विघ्न-बाधाओं के बीच भी उनका जीवन बड़ी शांति, बड़े आनंद और बड़े सुख से बीता, बड़ी समता से व्यतीत हुआ। श्रीकृष्ण के जीवन में लौकिक विद्या, योगविद्या और ब्रह्मविद्या तीनों थीं। उनके जीवन में भी हजारों विघ्न-बाधाएँ आयीं लेकिन वे सदा मुस्कुराते रहे।
जितने अंश में योगविद्या और ब्रह्मविद्या है, उतने अंश में ऐहिक विद्या भी शोभा देती है। किन्तु केवल लौकिक विद्या है, योगविद्या और ब्रह्मविद्या नहीं है तो फिर ऐहिक विद्या के प्रमाणपत्र मिल जाते हैं। उसे कुछ धन या कुछ सत्ता मिल जाती है किन्तु गहराई से देखो त भीतर धुंधलापन ही रहता है। भीतर कोई तसल्ली नहीं रहती, कोई तृप्ति नहीं रहती, कोई शांति नहीं रहती। भविष्य कैसा होगा ? कोई पता नहीं। आत्मा क्या है ? कोई पता नहीं। मोक्ष क्या है ? कोई पता नहीं। जीवन अज्ञान में ही बीत जाता है।
अज्ञान में जो ज्ञान होता है वह भी अज्ञान का रूपान्तर होता है। जैसे, रस्सी में साँप दिखा तो कोई बोलता है - 'यह साँप है।' दूसरा बोलता है - 'यह साँप नहीं यह तो दरार है।' तीसरा बोलता है - 'यह दरार नहीं, यह तो पानी का बहाव है।' चौथा बोलता है - 'यह मरा हुआ साँप है।' कोई बोलता है - 'अच्छा, जाऊँ, जरा देखूँ।' वह जाता तो है किन्तु दोनों तरफ भागने की जगह खोजता है। अज्ञान में ज्ञान हुआ है। रस्सी में साँप का ज्ञान हुआ है। ऐहिक विद्या अविद्या में ही मिलती है। अज्ञान दशा में ही ऐहिक शिक्षा का समावेश होता है।
आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा-परमात्मा क्या है ? उसका ज्ञान नहीं है और हम लौकिक शिक्षा पाते हैं तो अज्ञान दशा में जो कुछ जाना जाता है, वह अज्ञान के अन्तर्गत ही होता है। हकीकत में जानकारी मिलती है बुद्धि को और समझते हैं कि हम जानते हैं। हम डॉक्टर हो गये तो बुद्धि तक, वकील हो गये तो बुद्धि तक, उद्योगपति हो गये तो बुद्धि तक। लेकिन बुद्धि के पार की जो विद्या है वह है ब्रह्मविद्या।
जहाँ से विश्व की तमाम बुद्धियों को, दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों की बुद्धियों को, बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों की, साधु-संतों की बुद्धियों को प्रकाश मिलता है उस प्रकाश के ज्ञान को ब्रह्मज्ञान कहते हैं। जहाँ से विश्व को अनादिकाल से ज्ञान मिलता आ रहा है.... चतुरों की चतुराई, विद्वानों की विद्या संभालने की योग्यता, प्रेम, आनंद, साहस, निर्भयता, शक्ति, सफलता, इस लोक और परलोक के रहस्यों का उदघाटन करने की क्षमता..... ये सब जहाँ से मिलता आया है, मिल रहा है और मिलता रहेगा एवं एक तृण जितनी भी जिसमें कमी नहीं हुई, उसे कहते हैं ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म-परमात्मा को, आत्मा को जानने की विद्या को ही ब्रह्मविद्या कहते हैं।
ब्रह्मविद्या ब्रह्ममुहूर्त में बड़ी आसानी से फलती है। उस समय ध्यान करने से, ब्रह्मविद्या का अभ्यास करने से, मनुष्य बड़ी आसानी से प्रगति कर सकता है। सुबह का समय ध्यान का समय है। व्यक्ति जितने अंश में ध्यान में सफल होता है उतनी ही लौकिक विद्या में भी अच्छी प्रगति कर सकता है।
लौकिक विद्या तो जरूर पढ़ो, किन्तु साथ ही साथ योग विद्या और आत्मविद्या का अभ्यास भी करोगे तो जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकोगे। फिर महान् बनना तुम्हारे लिए अत्यंत सहज एवं सरल हो जायेगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
'परिप्रश्नेन.....'
पूज्य
गुरूदेव के
श्रीचरणों
में साधकों
द्वारा पूछे गये
प्रश्न
साधकः
स्वामी जी !
परमात्माप्राप्ति
के,
तत्त्वज्ञानप्राप्ति
के अभिलाषी
साधकों को
कैसा जीवन
जीना चाहिए ?
पू. बापूः जिन्हें इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार करना है, उन्हें वशिष्ठजी के मतानुसार दिन के दो भाग कर लेने चाहिए। एक भाग अर्थात् 12 घंटे खाने, सोने इत्यादि के लिये तथा दूसरा भाग (12 घंटे) ईश्वरप्राप्ति में लगा देना चाहिए।
12 घंटे में चार प्रहर होते हैं। इनमें से एक प्रहर प्रणव का जप करें, एक प्रहर परमात्मा का ध्यान करें, एक प्रहर योगवाशिष्ठ जैसे महाग्रन्थ का स्वाध्याय करें तथा एक प्रहर सदगुरू क सेवाकार्यों में संलग्न रहे। आधी अविद्या तो इससे ही कट जायेगी। यहाँ तक पहुँच गये और तीव्र जिज्ञासा हो तो खान-पान के लिए कमाने में समय न गँवायें। आजीविका तो स्वतः मिलेगी।
शेष 12 घंटों में से छः घंटे शयन करें और शेष छः घंटे अपने अन्य कार्यों में लगा दें।
इस प्रकार जीवन की व्यवस्था की जाय तो इसी जन्म में तत्त्वज्ञान हो जायेगा।
साधकः
स्वामी जी ! हर
किसी का मन
भगवान में
क्यों नहीं
लगता है ?
पू. बापूः हर किसी के पास इतना पुण्य नहीं है, इतनी समझ नहीं है इसलिए हर किसी आदमी का मन भगवान में नहीं लगता लेकिन प्रत्येक का मन देर-सबेर भगवान में लगेगा ही। इस जन्म में नहीं लगा तो ठोकरें खाते-खाते अगले जन्मों में लगेगा लेकिन लगेगा सही, ऐसी ईश्वर की व्यवस्था है।
ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो वहाँ से फिर दुःख ही मिलता है। इन्सान अन्य सहारे तलाशता है लेकि जब वे भी छूट जाते हैं तो आखिरी सहारा ढूँढते-ढूँढते ईश्वर के सहारे आना ही पड़ता है... फिर चाहे आर्तभाव से आवे, अर्थार्थी भाव से आवे या जिज्ञासु भाव से आवे। उसको आना ही पड़ता है। सीधे-अनसीधे ईश्वर के रास्ते जाने के सिवाय अन्य कोई रास्ता ही नहीं है।
नान्या
पंथा विद्यते
अयनाय।
पूर्व के पाप जोर करते हैं तो ईश्वर में मन नहीं लगता, वासना का जोर होता है, अहंकार का जोर होता है तथा भौतिक वस्तुओं में आस्था होती है इसलिए ईश्वर में मन नहीं लगता। उन भौतिक सुखों में जब उपद्रव होते है तो मजबूर होकर भी यह स्वीकारना पड़ता है कि इनके अतिरिक्त भी ईश्वर की कोई सत्ता है।
गजेन्द्र जब अपने परिवार में, अपने सुख में मस्त था तब कुछ नहीं, लेकिन जब उसे ग्राह ने पकड़ा और देखा कि अब अपने बल से कुछ नहीं होगा तो सीधा ही अदृष्ट सत्ता की शरण में गया कि 'जो भी कोई सृष्टिकर्त्ता हों, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे बचाने की कृपा करें।' तब उसे भगवान आदिनारायण की कृपा का एहसास हुआ।
तुलसी
पूर्व के पाप
से, हरिचर्चा
न सुहाए।
जैसे
ज्वर के जोर
से, भूख विदा न
हो जाय।।
हर किसी का मन भगवान में नहीं लगता क्योंकि पापवासना का जोर होता है। पापवासना के अनुकूल चीज मिलती है तो मोह होता है एवं प्रतिकूल मिलती है तो द्वेष होता है। मोह और द्वेष से आदमी संसार में फँसता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है।
साधकः
हे गुरूदेव !
संसार में
सर्वत्र दुःख,
अशांति और
तनाव क्यों है
?
पू. बापूः दुःख, अशांति और तनाव सर्वत्र नहीं है। जो संसार के रास्ते जाते हैं, उन्हें दुःख, अशांति और तनाव होता है लेकिन जो ज्ञानवानों के दिखलाये मार्ग का अनुसरण करते हैं वे दुःख, अशांति और तनाव के वातावरण में भी सुख, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं।
दुःख और अशांति से पीड़ितों का बहुमत हो सकता है। जो गल्ती करते हैं वे दुःखी अशान्त हो सकते हैं किन्तु जो गल्तियों से पार हो गये हैं, उनके पास दुःख और अशान्ति नहीं है।
दुःख, अशांति और तनाव का कारण है बिना ब्रेक के गाड़ी भगाना। ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेन्ट क्यों होता है ? इसलिए कि बिना ब्रेक के गाड़ी भगा रहे थे अथवा निर्णय लेने में कोई गड़बड़ी की इसलिए एक्सीडेन्ट होता है।
आपका जन्म दुःख, तनाव, अशांति और मुसीबत के लिये नहीं हुआ है। आप तो सुख, शांति, माधुर्य और मुक्ति के लिए धरती पर आये हैं, लेकिन उस माधुर्य, आनन्द और मुक्ति के दर्शन नहीं होते, परम शांति के दर्शन नहीं होते अपितु अशांति की ही वृद्धि होती है। क्यों ? क्योंकि हम अपने जीवन से संयम की ब्रेक खो बैठे हैं, सदाचार का स्टीयरिंग नहीं है, हमार सोचने का ढंग गलत हो गया।
पाश्चात्य प्रभाव से हम इतने आकर्षित हो गये हैं कि हम भी उनकी तरह ही बाहर के विषय-विकारों में सुख ढूँढने के लिए कूद पड़े हैं। आप भोजन, कपड़ा, मकान, मोटर आदि वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उपयोग की जगह जब उपभोग आ जाता है, मजा लेने की वृत्ति बढ़ जाती है तो असंयम आ जाता है और संयमरूपी ब्रेक फेल हो जाने से गाड़ी गड्डे में गिर जाती है। .....तो मानना पड़ेगा कि आज जो अशांति, तनाव व दुःख हैं, उसके पीछे सही समझ की कमी है और असंयम का बोलबाला है।
हर आदमी चाहता है कि अधिक से अधिक वस्तुएँ एकत्रित करूँ, अधिक से अधिक भोग भोगकर सुखी हो जाऊँ लेकिन वह औषधि की तरह इन्द्रियों का उपयोग करे तो मनुष्य जीवन स्वस्थ और सुखी रह सकता है। पति-पत्नी का व्यवहार संयमित रहे तो दोनों स्वस्थ रहते हैं लेकिन स्त्री पुरूष के शरीर से आये और पुरूष स्त्री के शरीर से उपभोग करके सुख लेने लगे इसलिए एड्स की बीमारी विदेशों में फैली और उसकी दुर्गन्ध अब यहाँ भारत में पहुँच गई है।
पाँच इन्द्रियाँ है – देखने, सुनने, सूँघने, चखने और स्पर्श करने की। यदि आँख का दुरूपयोग किया टी.वी., फिल्म आदि देखने में तो चश्मे जल्दी आने लगते हैं। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के द्वारा भी अतिभोग से स्वास्थ्य गिरने लगता है।
अति
सर्वत्र वर्जयेत्।
अतः इन पाँचों इन्द्रियों का उपभोग नहीं, उपयोग करें और वह भी औषधि के समान। संसार में सर्वत्र दुःख, अशांति इसलिए है कि हम संयम-सदाचार भूलकर विषय-विकारों में फँसते चले गये। दवाई रोग मिटाने के लिए खायी जाती है ऐसे ही देखना, खाना-पीना आदि वासना मिटाने के लिये किया जाता है। यह सब वासना को बढ़ाने के लिए किया और वासना निवृत्त करने की बात भूल गये तो फिर अशांति और दुःख आयेंगे ही।
इन्द्रियों के विषयों में आज का इन्सान अति करने लगा है क्योंकि वह धर्म से दूर चला गया है। शास्त्र कहते हैं-
यतो
धर्मस्ततो
जयः ततो अभ्युदयः।
जहाँ धर्म है, वहाँ जय है और अभ्युदय (सुख-समृद्धि) है। धर्म का आशय यहाँ किसी मत, पंथ, मजहब या संप्रदाय से नहीं। संयम की विधि, स्वस्थ रहने की विधि, शांत और साहसी बनने की विधि तथा छुपी हुई चेतना जगाने की विधि जिसमें भरी है उसे धर्म कहते हैं।
धर्म जीवन में अनुशासन, साहस, शक्ति, सदाचार, संयम लाता है जिससे अशांति के स्थान पर शांति, दुःख के स्थान पर शाश्वत सुख तथा तनाव के स्थान पर आनंद की वृद्धि होती है, सर्वत्र सुख, शांति, आनंद व माधुर्य छा जाता है तथा देर-सबेर वह धर्म उपासना में एवं उपासना ज्ञान में परिवर्तित होकर जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है।
साधकः
बापू जी !
जीवन का
वास्तविक
विकास कैसे हो
सकता है ?
पू. बापूः आप जिस शरीर को जीवन मानते हैं, वास्तव में वह शरीर आपका जीवन नहीं है, वह तो मुर्दा है क्योंकि वह नित्य मृत्यु की ओर जा रहा है। यह पहले आपके साथ नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिदिन आपका साथ छोड़ता जा रहा है, शरीर के कण बदलते जा रहे हैं।
आपका वास्तविक जीवन तो जीवनदाता से जुड़ा है। बीजरूप में प्राणीमात्र के पास उस अनंत ब्रह्मांडनायक परमेश्वर की चेतना है, ज्ञान है। वह ज्ञान 'आँख देखती है कि नहीं' उसको भी देख रहा है तथा 'बुद्धि का निर्णय ठीक है कि नहीं' उसको भी देख रहा है। वह ईश्वर का ज्ञानस्वरूप, ईश्वर का सत्यस्वरूप और ईश्वर का चेतनस्वरूप, आपसे अभिन्न है और वही वास्तव में आपका जीवन है।
उसका विकास कैसे हो ? जैसे बीज को विकसित होने के लिए धरती चाहिए, हवा, पानी, खाद व सूर्य का प्रकाश चाहिए ऐसे ही वास्तविक जीवन के विकास के लिए धर्म, उपासना, सत्संग, ज्ञान, श्रद्धा, संयम, सदाचार आदि चाहिए।
साधकः
गुरू बिना
परमात्मा की
प्राप्ति
नहीं होती है
ऐसा सुना जाता
है। भगवान तो
सबके हैं और
जो भी भगवान
को पाना चाहे
उसे भगवान मिल
जाना चाहिए।
फिर गुरू
क्यों जरूरी
हैं ?
पू. बापूः बात तो ठीक है लेकिन..... जैसे आटा पड़ा हो तो भी हर कोई रोटी नहीं बना सकता क्योंकि रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने तथा रोटी बेलने, सेंकने की कला आनी चाहिये। यह कला भी किसी गुरू (माता, बहन या भाभी) से सीखी जाती है तो भगवान को पाने की कला सिखाने के लिये भी तो कोई गुरू चाहिए।
सहजो
कारज संसार को
गुरू बिन होत
नाहीं।
हरि
तो गुरू बिन
क्या मिले सोच
ले मन माहीं।।
सूर्य तो दिखता है लेकिन 'यह सूर्य है' ऐसा ज्ञान कराने वाला कोई था तभी आप सूर्य को सूर्य के रूप में पहचानते हैं। किसी ने बतलाया होगा तभी तो आपने जाना होगा कि 'यह चन्द्रमा है, ये तारे हैं।'
मनुष्य जीवन में जानने की क्षमता छुपी है इसीलिए बच्चों की जैसे-जैसे समझ निखरती है तो पूछता है कि 'यह क्या है.... वह क्या है....?' माता-पिता बतलाते हैं कि 'यह अमुक वस्तु है.... यह चिड़िया है..... यह कौआ है।' जब तक हमें चिड़िया-कौए का ज्ञान नहीं था, तब तक हम चिड़िया को चिड़िया कौए को कौआ नहीं बोल सकते थे। यह ज्ञान भी तो किसी ने दिया ही है ना !
ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ है लेकिन अव्यक्त है। वह इन्द्रियों का, आँखों का विषय नहीं है। उपनिषद कहती हैः
यतो
वाचो
निवर्तन्ते
अप्राप्य
मनसा सह।
यह वाणी का विषय नहीं है। चिड़िया को आप वाणी से बता सकते हो या आँखों से दिखा सकते हो लेकिन भगवान को आप बतला या दिखला नहीं सकते कि 'यह रहा भगवान....।'
जैसे दूध में घी छुपा है ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में सच्चिदानंद परमात्मा छुपा है। दूध में घी क्यों नहीं दिखता ? दूध को पहले गर्म करो, दही जमाओ, फिर बिलोओ, मक्खन निकालो और उसे गरम करो तब घी का साक्षात्कार होता है। ऐसे ही इस नश्वर देह एवं बदलने वाले संसार में भी अबदल और शाश्वत तत्त्व छुपा है। थोड़ा व्रत-नियम का तप करो, फिर थोड़ा जमाओ अर्थात् ध्यान करो और विचार करो कि 'ध्यान करने वाला कौन है ? जिसका ध्यान करते हो उस परमेश्वर का स्वरूप क्या है ?' तत्पश्चात् ज्ञानाग्नि से अपनी वासनाओं तथा कर्मों को जलाकर उस मक्खन में से घी निकालो।
ध्यान की एकाग्रता और संयम का जो दही जमाया और मक्खन निकला, उसे घी बनाने के लिए बाकी की विधि करो तो घी प्रकट हो जाता है। ईश्वर को कोई क्यों नहीं पा सकता है ? जैसे दूध में से घी बिना ज्ञान के नहीं बना सकते, कोई न कोई ज्ञान बताने वाला चाहिए। थोड़ी सी रसोई बनाने की कला बताने वाला कोई अनुभवी गुरू (माता आदि) चाहिए तो फिर परमात्मा का, जीवनदाता का ज्ञान बिना गुरू के कैसे संभव हो सकता है.....?
भगवान शंकर कहते है-
गुरू
बिन भव निधि
तरइ न कोई।
जौं
बिरंचि संकर
सम होई।।
अखंडानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि जिसका गुरू नहीं है, उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है।
जिसका कोई गुरू नहीं, वह या तो मूर्ख है या घमंडी है, जिसका सिर कहीं झुकता नहीं है। भगवान श्रीराम के भी गुरू थे, श्रीकृष्ण के भी गुरू थे फिर भी पूछते हैं कि गुरू के बिना भगवान क्यों नहीं मिलता।
अरे, भगवान तो मिला मिलाया है लेकिन गुरू मिलें तब तो इस बात का अनुभव होवे ना ! गुरू बनाये बिना इस प्रकार की यात्रा करना तो मानो 'बिना दही जमाये या बिना क्रीम निकाले घी क्यों नहीं मिलता ?' पूछने के समान है। गुरू की कृपा के बिना भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं होता।
यदि कोई कहे कि, "हम गुरू को नहीं मानते। हम तो 'सीताराम-सीताराम करेंगे... भगवान कृपा करेंगे।" भगवान सदा कृपा करें – यह भी अच्छा है किन्तु 'सीताराम-सीताराम' से भगवान कृपा करेंगे – यह भी तो किसी से तुमने सुना होगा ?
'सीता' और राम का अर्थ क्या है ? उनका स्वरूप क्या है ? यह बताने वाला भी तो कोई गुरू चाहिए... नहीं तो करते रहो 'सीताराम-सीताराम.....' कहाँ मना है ? 'सीताराम-सीताराम' करोगे तो देर-सबेर सीताराम की कृपा होगी ही और वे आत्मा होकर प्रेरणा करेंगे कि 'जा, किसी आत्मज्ञानी गुरू की शरण ले।' मुझे तो अपने साधनाकाल के दौरान अनेकों बार ऐसे अनुभव हुए थे।
जिस किसी ने भी ईमानदारी से भगवान की शरण ली है, वह देर-सबेर ब्रह्मवेत्ता सदगुरू के सान्निध्य में पहुँचा ही है। सनातन धर्म के पाँच भगवान हैं- सूर्य, गणपति, शिव, विष्णु (अथवा इनके अवतार) एवं भगवती जगदंबा। इन पाँच देवों में से किसी भी देव को इष्ट मानकर यदि किसी ने सच्चाई से भजन, पूजन या सेवा की है और उसकी पूजा फली है तो उन देवों की कृपा से उसकी अन्तरात्मा में प्रेरणा होगी कि सदगुरू के पास जाना चाहिए। यदि किसी ने नानक, कबीर जैसे महापुरूषों को मन ही मन गुरू मानकर भजन किया तो वे गुरू भी कृपा करेंगे और हृदय में किसी जीवित ब्रह्मज्ञानी गुरू का नाम स्फुरित करायेंगे कि 'जाओ ! अमुक गुरू के पास जाओ।'
अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरू की अनिवार्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
साधकः
गुरूदेव !
मंत्रजाप
करते समय मन
इधर-उधर भटकता
हो तो क्या
करना चाहिए ?
पू. बापूः मंत्रजाप के समय मन भटकता है इसका कारण यह है कि मन में भगवान से भी अधिक किसी अन्य वस्तु के गहरे संस्कार पड़े हैं, जिसमें सत्यबुद्धि व प्रीति होने के कारण 'वह हमें मिले' इस भावना से मन भटकता है। यह पुरानी आदत सबमें घर कर बैठी है। इसे बदलना है तो प्रभु को अपना मानकर उससे स्नेह करें, जोर-जोर से नामोच्चार या मंत्रोच्चार करें, पंजों के बल थोड़ा कूदें अथवा कुछ गहरे श्वास लें और छोड़ें...... श्वास लें और छोड़ें.... तो इससे मन के भटकाव में फर्क पड़ेगा।
मंत्रजाप करते समय मन भटकाने लगे तो कभी-कभी जप छोड़कर मन को देखो और बोलोः
'जा बेटा ! कहाँ-कहाँ भटकता है.....' जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ उसे प्रभु की सत्ता का आभास कराओ।
मान लो मन एक घंटे में हजार बार भटकता है। आप यह अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसका भटकना 150 बार हो गया... फिर 900..... 800.....700..... 600... 500 बार हो गया। एक दिन में ही तो मन एकाग्र नहीं होगा, उसकी भटकान बन्द नहीं होगी लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास करते रहें तो भटकान कम होती जायेगी।
दृढ़ संकल्प करो कि 'मन भटके तो भटके, मुझे तो नियम करना ही है।' गुरूदेव की तस्वीर की ओर, इष्टदेव की ओर निहारकर त्राटक करो, प्रार्थना करो, गुरूदेव के सत्संग का विचार करो। मन को भटकना है तो आत्मज्ञान के विचार में भटकाओ। 'भटकना ही है तो फिर जंगल में क्यों जायें, नन्दनवन में ही चलते हैं' ऐसा करके मन को आत्मविचार में लगा दो। 'सत्संग में यह सुना था.... वह सुना था....' इसमें मन को भटकाओ।
मन जब ज्ञान में भटकेगा तो अज्ञान की भटकान मिट जायेगी और ज्ञान तथा अज्ञान का जो साक्षी है उस परमात्मा में विश्रांति मिल जाएगी। एक बार मन को हरि का चस्का लग जाए तो उसकी भटकान कम हो जायेगी। इसीलिये 'ध्यान योग शिविर' भरने वाले साधकों को मन की एकाग्रता-वृद्धि में काफी लाभ होता है।
साधकः
स्वामी जी !
ईश्वरप्राप्ति
के मार्ग में
विघ्न-बाधाएँ
क्यों आती हैं
?
पू. बापूः अरे भैया ! बचपन में जब तुम स्कूल में दाखिल हुए थे तो 'क... ख... ग...' आदि का अक्षरज्ञान तुरन्त ही हो गया था कि विघ्न बाधाएँ आई थीं ? लकीरें सीधी खींचते थे कि कलम टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती थी ? जब साईकिल चलाना सीखा तब एकदम सीखे थे या इधर-उधर गिरकर सीखे थे ? अरे, जब चलना सीखा था तब भी तुम एकदम सीखे थे क्या ? नहीं। कई बार गिरे, कई बार उठे, चालनगाड़ी पकड़ी, अंगुली पकड़ी तब चलने के काबिल बने और अब तुम दौड़ सकते हो।
अब मेरा सवाल है कि जब तुम चलना सीखे तो विघ्न क्यों आये ? तुम्हारा जवाब होगा किः 'बाबाजी ! हम कमजोर थे, अभ्यास नहीं था।'
ऐसे ही ईश्वर के लिए भी तुम्हारा प्रेम कमजोर है और चलने का अभ्यास भी नहीं है, इसीलिए विघ्न आते और दिखते हैं। हालाँकि साधक तो विघ्न-बाधाओं से खेलकर मजबूत होता है।
बाधाएँ
कब बाँध सकी
हैं आगे बढ़ने
वालों को।
विपदाएँ
कब रोक सकी
हैं पथ पर
चलने वालों
को।।
स्वामी रामतीर्थ कहते थेः "हे परमात्मा ! रोज ताजा मुसीबत भेजना।"
माता कुन्ती भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना करतीं थीं-
विपदः
सन्तु नः
शश्वत्तत्र
तत्र जगद्
गुरो।
भक्तो
दर्शनं
यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्।।
'हे जगद् गुरो ! हमारे जीवन में सर्वदा पद-पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है।'
(श्रीमद् भागवतः 1.8.25)
एक बीज को वृक्ष बनने तक कितने विघ्न आते हैं ? कभी पानी मिला कभी नहीं मिला, कभी आँधी आई कभी तूफान आया, कभी पशु-पक्षियों ने मुँह-चोंचे मारीं.... ये सब सहते हुए भी वृक्ष खड़े हैं तो तुम भी सब सहन करते हुए ईश्वर के लिए खड़े हो जाओ तो तुम ब्रह्म हो जाओगे।
भले
आज तूफान उठकर
के आयें।
बला
पर चली आ रही
हो बलायें।।
भारत
का वीर है
दनदनाता चला
जा।
कदम
अपने आगे
बढ़ाता चला
जा।।
साधकः
हे गुरूदेव !
हमारा कल्याण
कैसे होगा ?
पू. बापूः जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी संतों की शरण जाने से, उनका संग करने से ही कल्याण होगा। जिसके पास जो चीज होती है, वह वही देता है। शराबी का संग शराबी, जुआरी का संग जुआरी, भंगेड़ी का संग भंगेड़ी बना देता है, ऐसे ही ईश्वरप्राप्त महापुरूषों या संतों का संग करोगे तो वह संग परम कल्याणस्वरूप की ओर ले जायेगा। उसी में तो कल्याण है।
श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं कि मनुष्य का कल्याण किसमें है ? शुकदेव जी कहते हैं-
तस्मात्सर्वात्मना
राजन् हरिः
सर्वत्र सर्वदा।
श्रोतव्यः
कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यो
भगवान्नृणाम्।।
'हे परीक्षित ! इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय और सभी स्थितियों में अपनी सम्पूर्ण शक्ति से भगवान श्रीहरि का ही श्रवण-कीर्तन और स्मरण करें।' (2.2.36)
भगवत्स्वरूप का स्मरण करे, चिन्तन करे, कीर्तन करे – इसमें मनुष्य का कल्याण है। कीर्तन से, मंत्रजाप से तुम्हारे रक्त के कण बदलते हैं, रोगप्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। शरीर तन्दुरूस्त और मन प्रसन्न रहेगा तो शराब-कबाब, परस्त्रीगमन आदि पापों की ओर प्रवृत्ति न होगी। संयम से रहोगे तो स्वस्थता, प्रसन्नता रहेगी और निजस्वरूप परमात्मा का ध्यान करोगे तो उससे बड़ा कल्याण क्या हो सकता है ?
धन मिलने से कल्याण होता तो सब धनवान सुखी हो जाते कुर्सी मिलने से कल्याण होता है तो कुर्सीवाले सब सुखी हो जाते और कुर्सी बिना कल्याण होता तो बिना कुर्सी वाले सब निश्चिन्त हो जाते।
कल्याण... कल्याण तो भाई ! कल्याणस्वरूप ईश्वर को पाये हुए संतों के संग से ही होता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जन्माष्टमी
यह बड़ा ही रहस्य भरा महोत्सव है। समाज के पहले से लेकर आखिरी व्यक्ति तक का ध्यान रखते हुए उसके उत्थान के लिए भिन्न-भिन्न तरीकों को अपनाते हुए, इन्सान की आवश्यकताओं व महत्ता को समझाकर उसके विकास के लिए निर्गुण, निराकार परात्पर ब्रह्म सगुण-साकार होकर गुनगुनाता, गीत गाता, नाचता, खिलाता और खाता, अनेक अठखेलियाँ करता हुआ, इस जीव को अपनी असलियत का दान करता हुआ, उसे अपनी महिमा में जगाता हुआ प्रगट हुआ है। उसी को श्रीकृष्णावतार कहते हैं।
श्रीकृष्ण के जीवन में न पुकार है न आवाज है। श्रीकृष्ण के जीवन में केवल प्रसन्नता है। श्रीकृष्ण नाचते हैं तो पूरे नाचते हैं, हँसते हैं तो पूरे हँसते हैं। हम लोग हँसते हैं तो थोड़ा इज्जत-आबरू का, अड़ोस-पड़ोस का ख्याल रखकर हँसते हैं। आप हँसोगे तो इधर-उधर देखकर हँसोगे फिर भी पूरे नहीं हँसोगे। रोओगे तब भी पूरे नहीं रोओगे, नाचोगे तो भी पूरे नहीं नाचोगे किन्तु श्रीकृष्ण जिस समय जो करते हैं, पूरा करते हैं। खाते हैं तो पूरा, डाँटते हैं तो पूरा, नाचते हैं तो पूरा। इस अवतार ने, आदिनारायण ने हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ही सारी लीलाएँ की हैं।
श्रीकृष्ण के जीवन की प्रत्येक घटना कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती है। उन्हें अपनाकर आप अवश्य ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ स्वयं श्रीकृष्ण हैं। आप श्रीकृष्ण के जीवन को अपना आदर्श बनाकर, उसके अनुसार आचरण कर उस पथ के पथिक बन सकें, यही हार्दिक शुभकामना.......
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ