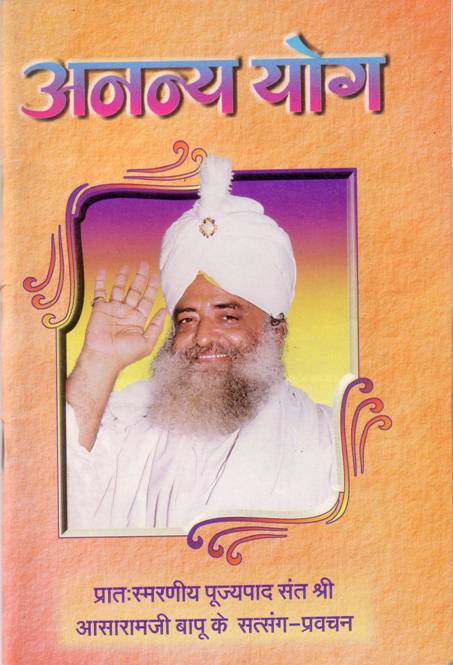
प्रातः
स्मरणीय
पूज्यपाद
संत
श्री
आसारामजी
बापू के
सत्संग-प्रवचन
अनन्य
योग
हम धनवान होंगे या नहीं, यशस्वी होंगे या नहीं, चुनाव जीतेंगे या नहीं इसमें शंका हो सकती है परंतु भैया ! हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है ? विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, गाड़ी छूटने का समय निश्चित होता है परंतु इस जीवन की गाड़ी छूटने का कोई निश्चित समय है?
आज तक आपने जगत का जो कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है.... आज के बाद जो जानोगे और प्राप्त करोगे, प्यारे भैया ! वह सब मृत्यु के एक ही झटके में छूट जायेगा, जाना अनजाना हो जायेगा, प्राप्ति अप्राप्ति में बदल जायेगी।
अतः सावधान हो जाओ। अन्तर्मुख होकर अपने अविचल आत्मा को, निजस्वरूप के अगाध आनन्द को, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो। फिर तो आप ही अविनाशी आत्मा हो।
जागो.... उठो.... अपने भीतर सोये हुए निश्चयबल को जगाओ। सर्वदेश, सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीन-हीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गये तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके।
सदा स्मरण रहे कि इधर-उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना-काल में आत्मचिन्तन में लगाओ और व्यवहार-काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हर कोई कार्य करो। सदा शान्त वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारवन्त एवं प्रसन्न रहो। जीवमात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो। दिल को व्यापक रखो। आत्मनिष्ठा में जगे हुए महापुरुषों के सत्संग एवं सत्साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदान्त से पुष्ट एवं पुलकित करो।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
हजारों-हजारों भक्तजनों, जिज्ञासु साधकों के लिये प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसारामजी बापू की जीवन-उद्धारक अमृतवाणी नित्य निरन्तर बहा करती है। हृदय की गहराई से उठने वाली उनकी योगवाणी श्रोताजनों के हृदयों में उतर जाती है, उन्हें ईश्वरीय आह्लाद से मधुर बना देती है। पूज्यश्री की सहज बोल-चाल में तात्त्विक अनुभव, जीवन की मीमांसा, वेदान्त के अनुभूतिमूलक मर्म प्रकट हो जाया करते हैं। उनका पावन दर्शन और सान्निध्य पाकर हजारों-हजारों मनुष्यों के जीवन-उद्यान नवपल्लवित-पुष्पित हो जाते हैं। उनकी अगाध ज्ञानगंगा से कुछ आचमन लेकर प्रस्तुत पुस्तक में संकलित करके आपकी सेवा में उपस्थित करते हुए हम आनन्दित हो रहे हैं.....।
विनीत,
श्री
योग वेदान्त
सेवा समिति
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
तर्क्यताम्..... मा कुतर्क्यताम्
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
मयि
चानन्ययोगेन
भक्तिरव्यभिचारिणी
।
विवक्तदेशसेवित्वरतिर्जनसंसदि
।।
"मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना (यह ज्ञान है)।"
(भगवद् गीताः १३-१०)
अनन्य भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति अगर भगवान में हो जाय, तो भगवत्प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान प्राणी मात्र का अपना आपा है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय अन्य पुरूष में पतिभाव नहीं रखती, ऐसे ही जिसको भगवत्प्राप्ति के सिवाय और कोई सार वस्तु नहीं दिखती, ऐसा जिसका विवेक जाग गया है, उसके लिए भगवत्प्राप्ति सुगम हो जाती है। वास्तव में, भगवत्प्राप्ति ही सार है। माँ आनन्दमयी कहा करती थी - "हरिकथा ही कथा...... बाकी सब जगव्यथा।"
मेरे अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकान्त स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति न होना.... इस प्रकार की जिसकी भक्ति होती है, उसे ज्ञान में रूचि होती है। ऐसा साधक अध्यात्मज्ञान में नित्य रमण करता है। तत्त्वज्ञान के अर्थस्वरूप परमात्मा को सब जगह देखता है। इस प्रकार जो है, वह ज्ञान है। इससे जो विपरीत है, वह अज्ञान है।
हरिरस को, हरिज्ञान को, हरिविश्रान्ति को पाये बिना जिसको बाकी सब व्यर्थ व्यथा लगती है, ऐसे साधक की अनन्य भक्ति जगती है। जिसकी अनन्य भक्ति है भगवान में, जिसका अनन्य योग हो गया है उसको जनसंपर्क में रूचि नहीं रहती। सामान्य इच्छाओं को पूर्ण करने में, सामान्य भोग भोगने में जो जीवन नष्ट करते है, ऐसे लोगों में सच्चे भक्त को रूचि नहीं होती। पहले रूचि हुई तब हुई, किन्तु जब अनन्य भक्ति मिली तो फिर उपरामता आ जायेगी। व्यवहार चलाने के लिए लोगों के साथ 'हूँ...हाँ...' कर लेगा, पर भीतर महसूस करेगा कि यह सब जल्दी निपट जाय तो अच्छा।
अनन्य भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है, तब पहले का जो कुछ किया होता है वह बेगार-सा लगता है। एकान्त देश में रहने की रूचि होती है। जन-संपर्क से वह दूर भागता है। आश्रम में सत्संग कार्यक्रम, साधना शिविरें आदि को जन-संसर्ग नहीं कहा जा सकता। जो लोग साधन-भजन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, देहाध्यास बढ़ा रहे हैं, उनका संसर्ग साधक के लिए बाधक है। जिससे आत्मज्ञान मिलता है वह जनसंपर्क तो साधन मार्ग का पोषक है। जन-साधारण के बीच साधक रहता है तो देह की याद आती है, देहाध्यास बढ़ता है, देहाभिमान बढ़ता है। देहाभिमान बढ़ने पर साधक परमार्थ तत्त्व से च्युत हो जाता है, परम तत्त्व में शीघ्र गति नहीं कर सकता। जितना देहाभिमान, देहाध्यास गलता है, उतना वह आत्मवैभव को पाता है। यही बात श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने कहीः
गलिते
देहाध्यासे
विज्ञाते
परमात्मनि।
यत्र
यत्र मनो याति
तत्र तत्र
समाधयः।।
जब देहाध्यास गलित हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ समाधि का अनुभव होता है, समाधि का आनन्द आता है।
देहाध्यास गलाने के लिए ही सारी साधनाएँ हैं। परमात्मा-प्राप्ति के लिये जिसको तड़प होती है, जो अनन्य भाव से भगवान को भजता है, 'परमात्मा से हम परमात्मा ही चाहते हैं.... और कुछ नहीं चाहते.....' ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति जिसके हृदय में है, उसके हृदय में भगवान ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं।
जो धन से सुख चाहते हैं, वैभव से सुख चाहते हैं, अथवा परिश्रम करके, साधना करके कुछ पाना चाहते हैं वे लोग साधना और परिश्रम के बल पर रहते हैं लेकिन जो भगवान के बल पर भी भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसे भक्त अनन्य भक्त हैं।
गोरा कुम्हार भगवान का कीर्तन करते थे। कीर्तन करते-करते देहाध्यास भूल गये। मिट्टी रोंदते-रोंदते मिट्टी के साथ बालक भी रोंदा गया। पता नहीं चला। पत्नी की निगाह पड़ी। वह बोल उठीः
"आज के बाद मुझे स्पर्श मत करना।"
"अच्छा ठीक है....।"
भगवान में अनन्य भाव था तो पत्नी नाराज हो गई फिर भी दिल को ठेस नहीं पहुँची। ‘स्पर्श नहीं करना...’ तो नहीं करेंगे। पत्नी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि गलती हो गई। अब वंश कैसे चलेगा ? अपने पिता से कहकर अपनी बहन की शादी करवाई। सब विधि सम्पन्न करके जब वर-वधू विदा हो रहे थे, तब पिता ने अपने दामाद गोरा कुम्हार से कहाः
"मेरी पहली बेटी को जैसे रखा है, ऐसे ही इसको भी रखना।"
"हाँ.. जो आज्ञा।"
भगवान से जिसका अनन्य योग है, वह तो स्वीकार ही कर लेगा। गोरा कुम्हार दोनों पत्नियों को समान भाव से देखने लगे। दोनों पत्नियाँ दुःखी होने लगीं। अब इनको कैसे समझाएं? तर्क-वितर्क देकर पति को संसार में लाना चाहती थीं लेकिन गोरा कुम्हार का अनन्य भाव भगवान में जुड़ चुका था।
आखिर दोनों बहनों ने एक रात्रि को अपने पति का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने शरीर तक लाया। गोरा कुम्हार ने सोचा कि मेरा हाथ अपवित्र हो गया। उन्होंने हाथ को सजा कर दी।
भगवान ने अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्य भाव माने : जैसे पतिव्रता स्त्री और किसी पुरूष को पतिभाव से नहीं देखती ऐसे ही भक्त या साधक भी और किसी साधन से अपना कल्याण होगा और किसी व्यक्ति के बल से अपना मोक्ष होगा ऐसा नहीं सोचता । 'हमें तो भगवान की कृपा से भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा तभी हमारा कल्याण होगा। भगवान की कृपा ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा और किसी साधन में हम नहीं रूकेंगे.... हे प्रभु ! हमें तो केवल तेरी कृपा और तेरे स्वरूप की प्राप्ति चाहिए.... और कुछ नहीं चाहिए।' भगवान पर जब ऐसा अनन्य भाव होता है तब भगवान कृपा करके भक्त के अन्तःकरण की पर्तें हटाने लगते हैं।
हमारा अपना आपा कोई गैर नहीं है, दूर नहीं है, पराया नहीं है और भविष्य में मिलेगा ऐसा भी नहीं है। वह अपना राम, अपना आपा अभी है, अपना ही है। इस प्रकार का बोध सुनने की और इस बोध में ठहरने की रूचि हो जायेगी। अनन्य भाव से भगवान का भजन यह परिणाम लाता है।
अनन्य भाव माने अन्य-अन्य को देखे, पर भीतर से समझे कि इन सबका अस्तित्त्व एक भगवान पर ही आधारित है। आँख अन्य को देखती है, कान अन्य को सुनते हैं, जिह्वा अन्य को चखती है, नासिका अन्य को सूँघती है, त्वचा अन्य को स्पर्श करती है। उसके साक्षी दृष्टा मन को जोड़ दो, तो मन एक है। मन के भी अन्य-अन्य विचार हैं। उनमें भी मन का अधिष्ठान, आधारभूत अनन्य चैतन्य आत्मा है। उसी आत्मा परमात्मा को पाना है। न मन की चाल में आना है न इन्द्रियों के आकर्षण में आना है।
इस प्रकार की तरतीव्र जिज्ञासावाला भक्त, अनन्य योग करने वाला साधक हल्की रूचियों और हल्की आसक्तियों वाले लोगों से अपनी तुलना नहीं करता।
चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछाः "हरि का नाम एक बार लेने से क्या लाभ होता है ?"
"एक बार अनन्य भाव से हरि का नाम ले लेंगे तो सारे पातक नष्ट हो जायेंगे।"
"दूसरी बार लें तो ?"
"दूसरी बार लेंगे तो हरि का आनन्द प्रकट होने लगेगा। नाम लो तो अनन्य भाव से लो। वैसे तो भीखमंगे लोग सारा दिन हरि का नाम लेते हैं, ऐसों की बात नहीं है। अनन्य भाव से केवल एक बार भी हरि का नाम ले लिया जाये तो सारे पातक नष्ट हो जाएँ।
लोग सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हमारा बेटा ठीक नहीं होता है। अन्तर्यामी भगवान देख रहे हैं कि यह तो बेटे का भगत है।
'हे भगवान ! मेरे इतने लाख रूपये हो जायें तो उन्हें फिक्स करके आराम से भजन करूँगा.....' अथवा 'मेरा इतना पेन्शन हो जाय, फिर मैं भजन करूँगा...' तो आश्रय फिक्स डिपोजिट का हुआ अथवा पेन्शन का हुआ। भगवान पर तो आश्रित नहीं हुआ। यह अनन्य भक्ति नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है:
भोंय
सुवाडुं भूखे
मारूँ उपरथी
मारूं मार ।
एटलुं
करतां हरि भजे
तो करी नाखुं
निहाल ।।
जीवन में कुछ असुविधा आ जाती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं- 'यह दुःख दूर को दो प्रभु !' हम भगवान के नहीं सुविधा के भगत हैं। भगवान का उपयोग भी असुविधा हटाने के लिए करते हैं। असुविधा हट गई, सुविधा हो गई तो उसमें लेपायमान हो जाते हैं। सोचते हैं, बाद में भजन करेंगे। यह भगवान की अनन्य भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति अनन्य भाव से की जाय तो तत्त्वज्ञान का दर्शन होने लगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा जाग उठे। जन-संसर्ग से विरक्ति होने लगे।
एकान्तवासो
लघुभोजनादि ।
मौनं निराशा
करणावरोधः।।
मुनेरसोः
संयमनं षडेते ।
चित्तप्रसादं
जनयन्ति
शीघ्रम् ।।
'एकान्त में रहना, अल्पाहार, मौन, कोई आशा न रखना, इन्द्रिय-संयम और प्राणायाम, ये छः मुनि को शीघ्र ही चित्तप्रसाद की प्राप्ति कराते हैं।'
एकान्तवास, इन्द्रियों को अल्प आहार, मौन, साधना में तत्परता, आत्मविचार में प्रवृत्ति... इससे कुछ ही दिनों में आत्मप्रसाद की प्राप्ति हो जाती है।
हमारी भक्ति अनन्य नहीं होती, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। कुछ यह कर लूं... कुछ यह देख लूं... कुछ यह पा लूं.... इस प्रकार जीवन-शक्ति बिखर जाती है।
स्वामी रामतीर्थ एक कहानी सुनाया करते थेः
एटलान्टा नामक विदेशी लड़की दौड़ लगाने में बड़ी तेज थी। उसने घोषणा की थी कि जो युवक मुझे दौड़ में हरा देगा, मैं अपनी संपत्ति के साथ उसकी हो जाऊंगी। उसके साथ स्पर्धा में कई युवक उतरे, लेकिन सब हार गये। सब लोग हारकर लौट जाते थे।
एक युवक ने अपने इष्टदेव ज्युपीटर को प्रार्थना की। इष्टदेव ने उसे युक्ति बता दी। दौड़ने का दिन निश्चित किया गया। एटलान्टा बड़ी तेजी से दौड़नेवाली लड़की थी। यह युवक स्वप्न में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था फिर भी देव ने कुछ युक्ति बता दी थी।
दौड़ का प्रारंभ हुआ। घड़ी भर में एटलान्टा कहीं दूर निकल गई। युवक पीछे रह गया। एटलान्टा कुछ आगे गई तो मार्ग में सुवर्णमुद्राएं बिखरी हुई देखी । सोचा कि युवक पीछे रह गया है। वह आवे, तब तक मुद्राएं बटोर लूं। वह रूकी... मुद्राएं इकट्ठी की। तब तक युवक नजदीक आ गया। वह झट से आगे दौड़ी। उसको पीछे कर दिया। और आगे गई तो मार्ग में और सुवर्णमुद्राएं देखी। वह भी ले ली। उसके पास वजन बढ़ गया। युवक भी तब तक नजदीक आ गया था। फिर लड़की ने तेज दौड़ लगाई। आगे गई तो और सुवर्णमुद्राएँ दिखी। उसने उसे भी ले ली। इस प्रकार एटलान्टा के पास बोझ बढ़ गया। दौड़ की रफ्तार कम हो गई। आखिर वह युवक उससे आगे निकल गया। सारी संपत्ति और रास्ते में बटोरी हुई सुवर्णमुद्राओं के साथ एटलान्टा को उसने जीत लिया।
एटलान्टा तेज दौड़ने वाली लड़की थी पर उसका ध्यान सुवर्णमुद्राओं में अटकता रहा। विजेता होने की योग्यता होते हुए भी अनन्य भाव से नहीं दौड़ पायी, इससे वह हार गई।
ऐसे ही मनुष्य मात्र में परब्रह्म परमात्मा को पाने की योग्यता है। परमात्मा ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि इसीलिए दे रखी है कि उसको आत्मा-परमात्मा के ज्ञान की जिज्ञासा जाग जाय, आत्मसाक्षात्कार हो जाय। रोटी कमाने की और बच्चों को पालने की बुद्धि तो पशु-पक्षियों को भी दी है। मनुष्य की बुद्धि सारे पशु-पक्षी-प्राणी जगत से विशेष है ताकि वह बुद्धिदाता का साक्षात्कार कर सके। बुद्धि जहाँ से सत्ता-स्फूर्ति लाती है उस परब्रह्म-परमात्मा का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म हो जाय। केवल कुर्सी-टेबल पर बैठकर कलम चलाने के लिए ही बुद्धि नहीं मिली है। बुद्धिपूर्वक कलम तो भले चलाओ लेकिन बुद्धि का उपयोग केवल रोटी कमाकर पेट भरना ही नहीं है। कलम भी चलाओ तो परमात्मा को रिझाने के लिये और कुदाली चलाओ तो भी उसीको रिझाने के लिए।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, जिसके पास कुछ भी योग्यता न हो, जो किसी को मानता न हो। हर मनुष्य जरूर किसी न किसी को मानता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें जानने की जिज्ञासा न हो। वह कुछ न कुछ जानने की कोशिश तो करता ही है। करने की, मानने की और जानने की यह स्वतः सिद्ध पूँजी है हम सबके पास। किसी के पास थोड़ी है तो किसी के पास ज्यादा है, लेकिन है जरूर। खाली कोई भी नहीं।
हम लोग जो कुछ करते हैं, अपनी रूचि के अनुसार करते हैं। गलती क्या होती है कि हम आवश्यकता के अनुसार नहीं करते। रूचि के अनुसार मानते हैं, आवश्यकता के अनुसार नहीं मानते हैं। रूचि के अनुसार जानते हैं, आवश्यकता के अनुसार नहीं जानते । बस, यही एक गलती करते हैं। इसे अगर हम सुधार लें तो किसी भी क्षेत्र में आराम से, बिल्कुल मजे से सफल हो सकते हैं। केवल यह एक बात कृपा करके जान लो।
एक होती है रूचि और दूसरी होती है आवश्यकता। शरीर को भोजन करने की आवश्यकता है। वह तन्दुरूस्त कैसे रहेगा, इसकी आवश्यकता समझकर आप भोजन करें तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। रूचि के अनुसार भोजन करेंगे तो बीमारी होगी। अगर रूचि की आसक्ति से बन्धायमान होकर आप भोजन करेंगें तो कभी रुचि के अनुसार भोजन नहीं मिलेगा और यदि भोजन मिलेगा तो रूचि नहीं होगी। जिसको रूचि हो और वस्तु न हो तो कितना दुःख ! वस्तु हो और रूचि न हो तो कितनी व्यर्थता !
खूब ध्यान देना कि हमारे पास जानने की, मानने की और करने की शक्ति है। इसको आवश्यकता के अनुसार लगा दें तो हम आराम से मुक्त हो सकते हैं और रूचि के अनुसार लगा दें तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों में भी काम नहीं बनता। कीट, पतंग, साधारण मनुष्यों में और महापुरूषों में इतना ही फर्क है कि महापुरूष माँग के अनुसार करते हैं और साधारण मनुष्य रूचि के अनुसार करते हैं।
जीवन की माँग है योग। जीवन की माँग है शाश्वत सुख। जीवन की माँग है अखण्डता। जीवन की माँग है पूर्णता।
आप मरना नहीं चाहते, यह जीवन की माँग है। आप अपमान नहीं चाहते। भले सह लेते हैं पर चाहते नहीं। यह जीवन की माँग है। तो अपमान जिसका न हो सके, वह ब्रह्म है। अतः वास्तव में आपको ब्रह्म होने की माँग है। आप मुक्ति चाहते हैं। जो मुक्त स्वरूप है, उसमें अड़चन आती है काम, क्रोध आदि विकारों से।
काम एष
क्रोध एष
रजोगुणसमुदभव: ।
महाशनो
महापाप्मा
विद्धयेनमिह वैरिणम्।।
'रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खानेवाला अर्थात् भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान।'
(भगवद् गीताः ३-३७)
काम और क्रोध महाशत्रु हैं और इसमें स्मृतिभ्रम होता है, स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश होता है। बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। अगर रूचि को पोसते हैं तो स्मृति क्षीण होती है। स्मृति क्षीण हुई तो सर्वनाश।
एक लड़के की निगाह पड़ोस की किसी लड़की पर गई और लड़की की निगाह लड़के पर गई। अब उनकी एक दूसरे के प्रति रूचि हुई। विवाह योग्य उम्र है तो माँग भी हुई शादी की। अगर हमने माँग की ओर, कुल शिष्टाचार की ओर ध्यान नहीं दिया और लड़का लड़की को ले भागा अथवा लड़की लड़के को ले भागी तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। किसी होटल में रहे, कभी कहाँ रहे – अखबारों में नाम छपा गया, 'पुलिस पीछे पड़ेगी,' डर लग गया। इस प्रकार रूचि में अन्धे होकर कूदे तो परेशान हुए। अगर विवाह योग्य उम्र हो गई है, गृहस्थ जीवन की माँग है, एक दूसरे का स्वभाव मिलता है तो माँ-बाप से कह दिया और माँ-बाप ने खुशी से समझौता करके दोनों की शादी करा दी। यह हो गई माँग की पूर्ति और वह थी रूचि की पूर्ति। रूचि की पूर्ति में जब अन्धी दौड़ लगती है तो परेशानी होती है, अपनी और अपने रिश्तेदारों की बदनामी होती है। ...तो शादी करने में बुद्धि चाहिए कि रूचि की पूर्ति के साथ माँग की पूर्ति हो।
माँग आसानी से पूरी हो सकती है और रूचि जल्दी पूरी होती नहीं। जब होती है तब निवृत्त नहीं होती, अपितु और गहरी उतरती है अथवा उबान और विषाद में बदलती है। रूचि के अनुसार सदा सब चीजें होंगी नहीं, रूचि के अनुसार सब लोग तुम्हारी बात मानेंगें नहीं। रूचि के अनुसार सदा तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं। अन्त में रूचि बच जायेगी, शरीर चला जायगा। रूचि बच गई तो कामना बच गई। जातीय सुख की कामना, धन की कामना, सत्ता की कामना, सौन्दर्य की कामना, वाहवाही की कामना, इन कामनाओं से सम्मोह होता है। सम्मोह से बुद्धिभ्रम होता है, बुद्धिभ्रम से विनाश होता है।
करने की, मानने की और जानने की शक्ति को अगर रूचि के अनुसार लगाते हैं तो करने का अंत नहीं होगा, मानने का अंत नहीं होगा, जानने का अंत नहीं होगा। इन तीनों योग्यताओं को आप अगर यथा योग्य जगह पर लगा देंगे तो आपका जीवन सफल हो जायगा।
अतः यह बात सिद्ध है कि आवश्यकता पूरी करने में शास्त्र, गुरू, समाज और भगवान आपका सहयोग करेंगे। आपकी आवश्यकता पूरी करने में प्रकृति भी सहयोग देती है। बेटा माँ की गोद में आता है, उसकी आवश्यकता होती है दूध की। प्रकृति सहयोग देकर दूध तैयार कर देती है। बेटा बड़ा होता है और उसकी आवश्यकता होती है दाँतों की तो दाँत आ जाते हैं।
मनुष्य की आवश्यकता है हवा की, जल की, अन्न की। यह आवश्यकता आसानी से यथायोग्य पूरी हो जाती है। आपको अगर रूचि है शराब की, अगर उस रूचि पूर्ति में लगे तो वह जीवन का विनाश करती है। शरीर के लिए शराब की आवश्यकता नहीं है। रूचि की पूर्ति कष्टसाध्य है और आवश्यकता की पूर्ति सहजसाध्य है।
आपके पास जो करने की शक्ति है, उसे रूचि के अनुसार न लगाकर समाज के लिए लगा दो। अर्थात् तन को, मन को, धन को, अन्न को, अथवा कुछ भी करने की शक्ति को 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' में लगा दो।
आपको होगा कि अगर हम अपना जो कुछ है, वह समाज के लिए लगा दें तो फिर हमारी आवश्यकताएँ कैसे पूरी होंगी?
आप समाज के काम में आओगे तो आपकी सेवा में सारा समाज तत्पर रहेगा। एक मोटरसाइकल काम में आती है तो उसको संभालने वाले होते हैं कि नहीं ? घोड़ा गधा काम में आता है तो उसको भी खिलाने वाले होते हैं। आप तो मनुष्य हो। आप अगर लोगों के काम आओगे तो हजार-हजार लोग आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए लालायित हो जायेंगे। आप जितना-जितना अपनी रूचि को छोड़ोगे, उतनी उतनी उन्नति करते जाओगे।
जो लोग रूचि के अनुसार सेवा करना चाहते हैं, उनके जीवन मे बरकत नहीं आती। किन्तु जो आवश्यकता के अनुसार सेवा करते हैं, उनकी सेवा रूचि मिटाकर योग बन जाती है। पतिव्रता स्त्री जंगल में नहीं जाती, गुफा में नहीं बैठती। वह अपनी रूचि पति की सेवा में लगा देती है। उसकी अपनी रूचि बचती ही नहीं है। अतः उसका चित्त स्वयमेव योग में आ जाता है। वह जो बोलती है, ऐसा प्रकृति करने लगती है।
तोटकाचार्य, पूरणपोडा, सलूका-मलूका, बाला-मरदाना जैसे सत् शिष्यों ने गुरू की सेवा में, गुरू की दैवी कार्यों में अपने करने की, मानने की और जानने की शक्ति लगा दी तो उनको सहज में मुक्तिफल मिल गया। गुरूओं को भी ऐसा सहज में नहीं मिला था जैसा इन शिष्यों को मिल गया। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य को गुरूप्राप्ति के लिए कितना कितना परिश्रम करना पड़ा ! कहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ी ! ज्ञानप्राप्ति के लिए भी कैसी-कैसी साधनाएँ करनी पड़ी ! जबकि उनके शिष्य तोटकाचार्य ने तो केवल अपने गुरूदेव के बर्तन माँजते-माँजते ही प्राप्तव्य पा लिया।
अपनी करने की शक्ति को स्वार्थ में नहीं अपितु परहित में लगाओ तो करना तुम्हारा योग हो जायेगा। मानने की शक्ति है तो विश्वनियंता को मानो। वह परम सुहृद है और सर्वत्र है, अपना आपा भी है और प्राणी मात्र का आधार भी है। जो लोग अपने को अनाथ मानते हैं, वे परमात्मा का अनादर करते हैं। जो बहन अपने को विधवा मानती है, वह परमात्मा का अनादर करती है। अरे ! जगतपति परमात्मा विद्यमान होते हुए तू विधवा कैसे हो सकती है ? विश्व का नाथ साथ में होते हुए तुम अनाथ कैसे हो सकते हो ? अगर तुम अपने को अनाथ, असहाय, विधवा इत्यादि मानते हो तो तुमने अपने मानने की शक्ति का दुरूपयोग किया। विश्वपति सदा मौजूद है और तुम आँसू बहाते हो ?
"मेरे पिता जी स्वर्गवास हो गये.... मैं अनाथ हो गया.........।"
"गुरुजी आप चले जायेंगे... हम अनाथ हो जाएँगे....।"
नहीं नहीं....। तू वीर पिता का पुत्र है। निर्भय गुरू का चेला है। तू तो वीरता से कह दे कि, 'आप आराम से अपनी यात्रा करो। हम आपकी उत्तरक्रिया करेंगे और आपके आदर्शों को, आपके विचारों को समाज की सेवा में लगाएँगे ताकि आपकी सेवा हो जाय।' यह सुपुत्र और सत् शिष्य का कर्त्तव्य होता है। अपने स्वार्थ के लिये रोना, यह न पत्नी के लिए ठीक है न पति के लिए ठीक है, न पुत्र के लिए ठीक है न शिष्य के लिए ठीक है और न मित्र के लिए ठीक है।
पैगंबर मुहम्मद परमात्मा को अपना दोस्त मानते थे, जीसस परमात्मा को अपना पिता मानते थे और मीरा परमात्मा को अपना पति मानती थी। परमात्मा को चाहे पति मानो चाहे दोस्त मानो, चाहे पिता मानो चाहे बेटा मानो, वह है मौजूद और तुम बोलते हो कि मेरे पास बेटा नहीं है.... मेरी गोद खाली है। तो तुम ईश्वर का अनादर करते हो। तुम्हारी हृदय की गोद में परमात्मा बैठा है, तुम्हारी इन्द्रियों की गोद में परमात्मा में बैठा है।
तुम मानते तो हो लेकिन अपनी रूचि के अनुसार मानते हो, इसलिए रोते रहते हो। माँग के अनुसार मानते हो तो आराम पाते हो। महिला आँसू बहा रही है कि रूचि के अनुसार बेटा अपने पास नहीं रहा। उसकी जहाँ आवश्यकता थी, परमात्मा ने उसको वहाँ रख लिया क्योंकि उसकी सृष्टि केवल उस महिला की गोद या उसका घर ही नहीं है। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्माण्ड उस परमात्मा की गोद में है। तो वह बेटा कहीं भी हो, वह परमात्मा की गोद में ही है। अगर हम रूचि के अनुसार मन को बहने देते हैं तो दुःख बना रहता है।
रूचि के अनुसार तुम करते रहोगे तो समय बीत जायगा, रूचि नहीं मिटेगी। यह रूचि है कि जरा-सा पा लें..... जरा सा भोग लें तो रूचि पूरी हो जाय। किन्तु ऐसा नहीं है। भोगने से रूचि गहरी उतर जायगी। जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो रूचिकर हो और मिलता भी रहे। या तो पदार्थ नष्ट हो जाएगा या उससे उबान आ जाएगी।
रूचि को पोसना नहीं है, निवृत्त करना है। रूचि निवृत्त हो गई तो काम बन गया, फिर ईश्वर दूर नहीं रहेगा। हम गलती यह करते हैं कि रूचि के अनुसार सब करते रहते हैं। पाँच-दस व्यक्ति ही नहीं, पूरा समाज इसी ढाँचे में चल रहा है। अपनी आवश्यकता को ठीक से समझते नहीं और रूचि पूरी करने में लगे रहते हैं। ईश्वर तो अपना आपा है, अपना स्वरूप है। वशिष्ठजी महाराज कहते हैं-
"हे रामजी ! फूल, पत्ते और टहनी तोड़ने में तो परिश्रम है, किन्तु अपने आत्मा-परमात्मा को जानने में क्या परिश्रम है ? जो अविचार से चलते हैं, उनके लिए संसार सागर तरना महा कठिन है, अगम्य है। तुम सरीखे जो बुद्धिमान हैं उनके लिए संसार सागर गोपद की तरह तरना आसान है। शिष्य में जो सदगुण होने चाहिए वे तुम में हैं और गुरू में जो सामर्थ्य होना चाहिए वह हममें है। अब थोड़ा सा विचार करो, तुरन्त बेड़ा पार हो जायगा।"
हमारी आवश्यकता है योग की और जीते हैं रूचि के अनुसार। कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम गर्म हो जाते हैं, लड़ने-झगड़ने लगते हैं। हमारी रूचि है अहं पोसने की और आवश्यकता है अहं को विसर्जित करने की। रूचि है अनुशासन करने की, कुछ विशेष हुक्म चलाने की और आवश्यकता है सबमें छुपे हुए विशेष को पाने की।
आप अपनी आवश्यकताएँ पूरी करो, रूचि को पूरी मत करो। जब आवश्यकताएँ पूरी करने में लगेंगे तो रूचि मिटने लगेगी। रूचि मिट जायगी तो शहंशाह हो जाओगे। आपमें करने की, मानने की, जानने की शक्ति है। रूचि के अनुसार उसका उपयोग करते हो तो सत्यानाश होता है। आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करोगे तो बेड़ा पार होगा।
आवश्यकता है अपने को जानने की और रूचि है लंदन, न्यूयार्क, मास्को में क्या हुआ, यह जानने की।
'इसने क्या किया... उसने क्या किया.... फलाने की बारात में कितने लोग थे.... उसकी बहू कैसी आयी....' यह सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारी रूचि है। अगर रूचि के अनुसार मन को भटकाते रहोगे तो मन जीवित रहेगा और आवश्यकता के अनुसार मन का उपयोग करोगे तो मन अमनीभाव को प्राप्त होगा। उसके संकल्प-विकल्प कम होंगे। बुद्धि को परिश्रम कम होगा तो वह मेधावी होगी। रूचि है आलस्य में और आवश्यकता है स्फूर्ति की। रूचि है थोड़ा करके ज्यादा लाभ लेने में और आवश्यकता है ज्यादा करके कुछ भी न लेने की। जो भी मिलेगा वह नाशवान होगा, कुछ भी नहीं लोगे तो अपना आपा प्रकट हो जायगा।
कुछ पाने की, कुछ भोगने की जो रूचि है, वही हमें सर्वेश्वर की प्राप्ति से वंचित कर देती है। आवश्यकता है 'नेकी कर कुएँ में फेंक'। लेकिन रूचि होती है, 'नेकी थोड़ी करूँ और चमकूँ ज्यादा। बदी बहुत करूँ और छुपाकर रखूँ।' इसीलिए रास्ता कठिन हो गया है। वास्तव में ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता रास्ता ही नहीं है, क्योंकि रास्ता तब होता है जब कोई चीज वहाँ और हम यहाँ। दोनों के बीच में दूरी हो। हकीकत में ईश्वर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हों और ईश्वर कहीं दूर हो। आपके और ईश्वर के बीच एक इंच का भी फासला नहीं, एक बाल जितना भी अंतर नहीं लेकिन अभागी रूचि ने आपको और ईश्वर को पराया कर दिया है। जो पराया संसार है, मिटने वाला शरीर है, उसको अपना महसूस कराया। यह शरीर पराया है, आपका नहीं है। पराया शरीर अपना लगता है। मकान है ईंट-चूने-लक्कड़-पत्थर का और पराया है लेकिन रूचि कहती है कि मकान मेरा है।
स्वामी रामतीर्थ कहते हैं-
"हे मूर्ख मनुष्यों ! अपना धन, बल व शक्ति बड़े-बड़े भवन बनाने में मत खर्चो, रूचि की पूर्ति में मत खर्चो। अपनी आवश्यकता के अनुसार सीधा सादा निवास स्थान बनाओ और बाकी का अमूल्य समय जो आपकी असली आवश्यकता है योग की, उसमें लगाओ। ढेर सारी डिजाइनों के वस्त्रों की कतारें अपनी अलमारी में मत रखो लेकिन तुम्हारे दिल की अलमारी में आने का समय बचा लो। जितनी आवश्यकता हो उतने ही वस्त्र रखो, बाकी का समय योग में लग जायेगा। योग ही तुम्हारी आवश्यकता है। विश्रान्ति तुम्हारी आवश्यकता है। अपने आपको जानना तुम्हारी आवश्यकता है। जगत की सेवा करना तुम्हारी आवश्यकता है क्योंकि जगत से शरीर बना है तो जगत के लिए करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता अपने आप पूरी हो जायगी।
ईश्वर को आवश्यकता है तुम्हारे प्यार की, जगत को आवश्यकता है तुम्हारी सेवा की और तुम्हें आवश्यकता है अपने आपको जानने की।
शरीर को जगत की सेवा में लगा दो, दिल में परमात्मा का प्यार भर दो और बुद्धि को अपना स्वरूप जानने में लगा दो। आपका बेड़ा पार हो जायगा। यह सीधा गणित है।
मानना, करना और जानना रूचि के अनुसार नहीं बल्कि, आवश्यकता के अनुसार ही हो जाना चाहिए। आवश्यकता पूरी करने में नहीं कोई पाप, नहीं कोई दोष। रूचि पूरी करने में तो हमें कई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जीवन खप जाता है किन्तु रूचि खत्म नहीं होती, बदलती रहती है। रूचिकर पदार्थ आप भोगते रहें तो भोगने का सामर्थ्य कम हो जायगा और रूचि रह जायगी। देखने की शक्ति खत्म हो जाय और देखने की इच्छा बनी रहे तो कितना दुःख होगा ! सुनने की शक्ति खत्म हो जाय और सुनने की इच्छा बनी रहे तो कितना दुर्भाग्य ! जीने की शक्ति क्षीण हो जाय और जीने की रूचि बनी रहे तो कितना दुःख होगा ! इसलिए मरते समय दुःख होता है। जिनकी रूचि नहीं होती उन आत्मरामी पुरूषों को क्या दुःख ? श्रीकृष्ण को देखते-देखते भीष्म पितामह ने प्राण ऊपर चढ़ा दिये। उन्हें मरने का कोई दुःख नहीं।
सूँघने की रूचि बनी रहे और नाक काम न करे तो ? यात्रा की रूचि बनी रहे और पैर जवाब दे दें तो ? पैसों की रूचि बनी रहे और पैसे न हों तो कितना दुःख ? वाहवाही की रूचि है और वाहवाही न मिली तो ?
अगर रूचि के अनुसार वाहवाही मिल भी जाय तो क्या रूचि पूरी हो जायगी ? नहीं, और ज्यादा वाहवाही की इच्छा होगी। हम जानते ही हैं कि जिसकी वाहवाही होती है उसकी निन्दा भी होती है। अतः वाहवाही से रूचिपूर्ति का सुख मिलता है तो निन्दा से उतना ही दुःख होगा। और इतने ही निन्दा करने वालों के प्रति अन्यायकारी विचार उठेंगे। अन्यायकारी विचार जिस हृदय में उठेंगे, उसी हृदय को पहले खराब करेंगे। अतः हम अपना ही नुकसान करेंगे।
एक होता है अनुशासन, दूसरा होता है क्रोध। जिन्हें अपने सुख की कोई रूचि नहीं, जो सुख देना चाहते हैं, जिन्हें अपने भोग की कोई इच्छा नहीं है, उनकी आवश्यकता सहज में पूरी होती है। जो दूसरों की आवश्यकता पूरी करने में लगे हैं, वे अगर डाँटते भी हैं तो वह अनुशासन हो जाता है। जो रूचिपूर्ति के लिए डाँटते हैं वह क्रोध हो जाता है। आवश्यकतापूर्ति के लिए अगर पिटाई भी कर दी जाय तो भी प्रसाद बन जाता है।
माँ को आवश्यकता है बेटे को दवाई पिलाने की तो माँ थप्पड़ भी मारती है, झूठ भी बोलती है, गाली भी देती है फिर भी उसे कोई पाप नहीं लगता। दूसरा कोई आदमी अपनी रूचि पूर्ति के लिए ऐसा ही व्यवहार उसके बेटे से करे तो देखो, माँ या दूसरे लोग भी उसकी कैसी खबर ले लेते हैं ! किसी की आवश्यकतापूर्ति के लिए किया हुआ क्रोध भी अनुशासन बन जाता है। रूचि पूर्ति के लिए किया हुआ क्रोध कई मुसीबतें खड़ी कर देता है।
एक विनोदी बात है। किसी जाट ने एक सूदखोर बनिये से सौ रूपये उधार लिये थे। काफी समय बीत जाने पर भी जब उसने पैसे नहीं लौटाये तो बनिया अकुलाकर उसके पास वसूली के लिए गया।
"भाई ! तू ब्याज मत दे, मूल रकम सौ रूपये तो दे दे। कितना समय हो गया ?"
जाट घुर्राकर बोलाः "तुम मुझे जानते हो न ? मैं कौन हूँ?"
"इसीलिए तो कहता हूँ कि ब्याज मत दो। केवल सौ रूपये दे दो।"
"सौ-वौ नहीं मिलेंगे। मेरा कहना मानो तो कुछ मिलेगा।"
बनिये ने सोचा कि खाली हाथ लौटने से बेहतर है, जो कुछ मिले वही ले लूँ।
अच्छा, तो तू जितना चाहे उतना दे दे ।
जाट ने कहाः "देखो, मगर आपको पैसे लेने हो तो मेरी इतनी सी बात मानो। आपके सौ रूपयें हैं ?"
"हाँ"।
"तो सौ के कर दो साठ।"
"ठीक है, साठ दे दो।"
"ठहरो, मुझे बात पूरी कर लेने दो। सौ के कर दो साठ.... आधा कर दो काट.. दस देंगे... दस छुड़ायेंगे और दस के जोड़ेंगे हाथ। अभी दुकान पर पहुँच जाओ।"
मिला क्या ? बनिया खाली हाथ लौट गया।
ऐसे ही मन की जो इच्छाएँ होती हैं, उसको कहेंगे कि भाई ! इच्छाएँ पूरी करेंगे लेकिन अभी तो सौ की साठ कर दे, और उसमें से आधा काट कर दे। दस इच्छाएँ तेरी पूरी करेंगे धर्मानुसार आवश्यकता के अनुसार। दस इच्छाओं की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है और शेष दस से जोड़ेंगे हाथ। अभी तो भजन में लगेंगे, औरों की आवश्यकता पूरी करने में लगेंगे।
जो दूसरों की आवश्यकता पूरी करने में लगता है, उसकी रूचि अपने आप मिटती है और आवश्यकता पूरी होने लगती है। आपको पता है कि जब सेठ का नौकर सेठ की आवश्यकताएँ पूरी करने लगता है तो उसके रहने की आवश्यकता की पूर्ति सेठ के घर में हो जाती है। उसकी अन्न-वस्त्रादि की आवश्यकताएँ पूरी होने लगती हैं। ड्रायवर अपने मालिक की आवश्यकता पूरी करता है तो उसकी घर चलाने की आवश्यकतापूर्ति मालिक करता ही है। फिर वह आवश्यकता बढ़ा दे और विलासी जीवन जीना चाहे तो गड़बड़ हो जायगी, अन्यथा उसकी आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति तो हो ही जाती है। आवश्यकता पूर्ति में और रूचि की निवृत्ति में लग जाय तो ड्रायवर भी मुक्त हो सकता है, सेठ भी मुक्त हो सकता है, अनपढ़ भी मुक्त हो सकता है, शिक्षित भी मुक्त हो सकता, निर्धन भी मुक्त हो सकता है, धनवान भी मुक्त हो सकता है, देशी भी मुक्त हो सकता है, परदेशी भी मुक्त हो सकता है। अरे, डाकू भी मुक्त हो सकता है।
आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का आदर करो। फिर चाहे गंगा के किनारे बैठकर आदर करो या यमुना के किनारे बैठकर आदर करो या समाज में रहकर आदर करो। ज्ञान का उपयोग करने की कला का नाम है सत्संग।
सबके पास ज्ञान है। वह ज्ञानस्वरूप चैतन्य ही सबका अपना आपा है। लेकिन बुद्धि के विकास का फर्क है। ज्ञान तो मच्छर के पास भी है। बुद्धि की मंदता के कारण रूचिपूर्ति में ही हम जीवन खर्च किये जाते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं, वह शरीर हमारा जीवन नहीं है। वास्तव में ज्ञान ही हमारा जीवन है, चैतन्य आत्मा ही हमारा जीवन है।
ॐकार का जप करने से आपकी आवश्यकतापूर्ति की योग्यता बढ़ती है और रूचि की निवृत्ति में मदद मिलती है। इसलिए ॐकार (प्रणव) मंत्र सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि संसारी दृष्टि से देखा जाय तो महिलाओं को एवं गृहस्थियों को अकेला ॐकार का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रूचियों को आवश्यकता का जामा पहनाकर ऐसा विस्तार कर रखा है कि एकाएक अगर वह सब टूटने लगेगा तो वे लोग घबरा उठेंगे। एक तरफ अपनी पुरानी रूचि खींचेगी और दूसरी तरफ अपनी मूलभूत आवश्यकता – एकांत की, आत्मसाक्षात्कार की इच्छा आकर्षित करेगी। प्रणव के अधिक जप से मुक्ति की इच्छा जोर मारेगी। इससे गृहस्थी के इर्द-गिर्द जो रूचि पूर्ति करने वाले मंडराते रहते हैं, उन सबको धक्का लगेगा। इसलिए गृहस्थियों को कहते हैं कि अकेले ॐ का जप मत करो। ऋषियों ने कितना सूक्ष्म अध्ययन किया है।
समाज को आपके प्रेम की, सान्त्वना की, स्नेह की और निष्काम कर्म की आवश्यकता है। आपके पास करने की शक्ति है तो उसे समाज की आवश्यकतापूर्ति में लगा दो। आपकी आवश्यकता माँ, बाप, गुरू और भगवान पूरी कर देंगे। अन्न, जल और वस्त्र आसानी से मिल जायेंगे। पर टेरीकोटन कपड़ा चाहिए, पफ-पॉवडर चाहिए तो यह रूचि है। रूचि के अनुसार जो चीजें मिलती हैं, वे हमारी हानि करती हैं। आवश्यकतानुसार चीजें हमारी तन्दुरूस्ती की भी रक्षा करती है। जो आदमी ज्यादा बीमार है, उसकी बुद्धि सुमति नहीं है।
चरक-संहिता के रचयिता ने अपने शिष्य को कहा कि तंदुरूस्ती के लिए भी बुद्धि चाहिए। सामाजिक जीवन जीने के लिए भी बुद्धि चाहिए और मरने के लिय भी बुद्धि चाहिए। मरते समय भी अगर बुद्धि का उपयोग किया जाय कि, 'मौत हो रही है इस देह की, मैं तो आत्मा चैतन्य व्यापक हूँ।' ॐकार का जप करके मौत का भी साक्षी बन जायें। जो मृत्यु को भी देखता है उसकी मृत्यु नहीं होती। क्रोध को देखने वाले हो जाओ तो क्रोध शांत हो जायेगा। यह बुद्धि का उपयोग है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो और देखते हुए चलाते हो तो खड्डे में नहीं गिरती और आँख बन्द करके चलाते हो तो बचती भी नहीं। ऐसे ही क्रोध आया और हमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो बह जायेंगे। काम, लोभ और मोहादि आयें और सतर्क रहकर बुद्धि से काम नहीं लिया तो ये विकार हमें बहा ले जायेंगे।
लोभ आये तो विचारों कि आखिर कब तक इन पद-पदार्थों को संभालते रहोगे। आवश्यकता तो यह है कि बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय इनका उपयोग किया जाये और रूचि है इनका अम्बार लगाने की। अगर रूचि अनुसार किया तो मुसीबतें पैदा कर लोगे। ऐसे ही आवश्यकता है कहीं पर अनुशासन की और आपने क्रोध की फूफकार मार दिया तो जाँच करो कि उस समय आपका हृदय तपता तो नहीं। सामने वाले का अहित हो जाये तो हो जाये किन्तु आपकी बात अडिग रहे – यह क्रोध है। सामने वाला का हित हो, अहित तनिक भी न हो, अगर यह भावना गहराई में हो तो फिर वह क्रोध नहीं, अनुशासन है। अगर जलन महसूस होती है तो क्रोध घुस गया। काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ-मोह और अहंकार बुरा नहीं है। धर्मानुकूल सबकी आवश्यकता है। अगर बुरा होता तो सृष्टिकर्ता बनाता ही क्यों ? जीवन-विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। दुःख बुरा नहीं है। निन्दा, अपमान, रोग बुरा नहीं है। रोग आता है तो सावधान करता है कि रूचियाँ मत बढ़ाओ। बेपरवाही मत करो। अपमान भी सिखाता है कि मान की इच्छा है, इसलिए दुःख होता है। शुकदेव जी को मान में रूचि नहीं है, इसलिए कोई लोग अपमान कर रहे हैं फिर भी उन्हें दुःख नहीं होता। रहुगण राजा कितना अपमान करते हैं, किन्तु जड़भरत शांतचित्त रहते हैं।
अपमान का दुःख बताता है कि आपको मान में रूचि है। दुःख का भाव बताता है कि सुख में रूचि है। कृपा करके अपनी रूचि परमात्मा में ही रखो।
सुख, मान और यश में नहीं फँसोगे तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे। योगी का योग सिद्ध हो जायेगा, तपी का तप और भक्त की भक्ति सफल हो जायगी। बात अगर जँचती है तो इसे अपनी बना लेना। तुम दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम अपने अनुभव का तो आदर करो। आपको रूचि अनुसार भोग मिलते हैं तो भोग भोगते-भोगते आप थक जाते हैं कि नहीं ? ऊबान आ जाती है कि नहीं ? ... तो इस ज्ञान का आदर करो। योगमार्ग पर चलते हुए या आवश्कतानुसार 'बहुजनहिताय-बहुजनसुखाय' काम करते हो तो आपको आनन्द आता है। आपका मन एवं बुद्धि विकसित होती है। यह भी आपका अनुभव है। सत्संग के बाद आपको यह महसूस होता है कि बढ़िया कार्य किया। शांति, सुख एवं सुमति मिली। ....तो अपने अनुभव की बात को आप पक्की करके हृदय की गहराई में उतार लो कि रूचि की निवृत्ति में ही आनन्द है और आवश्यकता तो स्वतः पूरी हो जायेगी।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जो अपने को शुद्ध-बुद्ध निष्कलंक नारायणस्वरूप मानता है, उसके सारे कल्मष मिट जाते हैं, ब्रह्महत्या जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं और अंतरतम चैतन्य स्वरूप का सुख प्रकट होने लगता है। देवताओं से वह पूजित होने लगता है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर उसके दीदार करके अपना भाग्य बना लेते हैं।
मुनिशार्दूल वशिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी से कहते हैं- "जीव को अपना परम कल्याण करना हो तो प्रारम्भ में दो प्रहर (छः घण्टे) आजीविका के निमित्त यत्न करे और दो प्रहर साधुसमागम, सत्शास्त्रों का अवलोकन और परमात्मा का ध्यान करें। प्रारम्भ में जब आधा समय ध्यान, भजन और शास्त्र विचार में लगायेगा तब उसकी अंतरचेतना जागेगी। फिर उसे पूरा समय आत्म-साक्षात्कार या ईश्वर-प्राप्ति में लगा देना चाहिए।"
श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहाः
यस्त्वात्मरतिरेव
स्यादात्मतृप्तश्च
मानवः ।
आत्मन्येव
च
संतुष्टस्तस्य
कार्यं न विद्यते
।।
'जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्त्तव्य नहीं है।'
(भगवद् गीताः ३-१७)
आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मप्रीति जिसको मिल गई, उसके लिए बाह्य जगत का कोई कर्त्तव्य रहता नहीं। उसका आत्मविश्रांति में रहना ही सब जीवों का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करना है। जो पुरूष विगतस्पृहा है, विगतदुःख है, विगतज्वर है, उसके अस्तित्व मात्र से वातावरण में बहुत-बहुत मधुरता आती है। प्रकृति उनके अनुकूल होती है। तरतीव्र प्रारब्धवेग से उनके जीवन में प्रतिकूलता आती है तो वे उद्विग्न नहीं होते। ऐसे स्थितप्रज्ञ महापुरूष के निकट रहने वाले साधक को चाहिए कि वह दिन का चार भाग कर दे। एक भाग वेदान्त शास्त्र का विचार करे। एक भाग परमात्मा के ध्यान में लगावे। परमात्मा का ध्यान कैसे ? 'मन को, इन्द्रियों को, चित्त को जो चेतना दे रहा है वह चैतन्य आत्मा मैं हूँ। मैं वास्तव में जन्मने-मरने वाला जड़ शरीर नहीं हूँ। क्षण क्षण में सुखी-दुखी होने वाला मैं नही हूँ। बार-बार बदलने वाली बुद्धि वृति मैं नही हूँ। देह में अहं करके जीने वाला जीव मैं नहीं हूँ।अंहकार भी मैं नहीं हूँ। मैं इन सबसे परे, शुद्ध-बुद्ध सनातन सत्य चैतन्य आत्मा हूँ। आनन्द स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं बोध स्वरूप हूँ.... ज्ञान स्वरूप हूँ।' जो ऐसा चिन्तन करता है वह वास्तव में अपने ईश्वरत्व का चिंतन करता है, अपने ब्रह्मत्व का चिंतन करता है। इसी चिन्तन में निमग्न रहकर अपने चित्त को ब्रह्ममय बना दे।
फिर तीसरा प्रहर संतसेवा, सदगुरूसेवा में लगावे। आधी अविद्या तो सदगुरू की सेवा से ही दूर हो जाती है। बाकी की आधी अविद्या ध्यान, जप और शास्त्रविचार इन तीन साधनों से दूर करके जीव मुक्त हो जाता है।
बड़े में बड़ा बन्धन है कि अविद्या में रस आ रहा है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिये छटपटाहट नहीं होती। अविद्या उसे कहते हैं, जो अविद्यमान वस्तु हो।
वस्तुएँ दो हैं- एक अविघमान वस्तु और दूसरी विद्यमान वस्तु। अविद्यमान वस्तु प्रतीत होती है। विद्यमान वस्तु प्राप्त होती है। जो प्रतीत होती है, उसमें धोखा होता है और जो प्राप्त होती है, उसमें पूर्णता होती है। जैसे, स्वप्न में भिखारी को प्रतीत होता है कि मैं राजा हूँ। इन्द्र को स्वप्न आ जाय कि मैं भिखारी हूँ। स्वप्न में भिखारी होना भी धोखा है, राजा होना भी धोखा है। धोखे के समय प्रतीति सच्ची लगती है। प्रतीति ऐसे ढंग से होती है कि प्रतीति प्राप्ति लगती है। भिखारी सोया है सड़ी-गली छत के नीचे फटी हुई गुदड़ी पर। स्वप्न में हो गया राजा। तेजबहादुर सोया है अपने महल में और स्वप्न में हो गया भिखारी। जिस समय भिखारी होने का स्वप्न चालू है, उस समय तेजबहादुर को कोई कह दे कि तू भिखारी नहीं है, बादशाह है तो वह नहीं मानेगा, क्योंकि प्रतीति प्राप्ति लगती है। वास्तविक प्राप्ति हुई नहीं इसलिए प्रतीति प्राप्ति लगती है। वास्तविक प्राप्ति क्या है ? वे दोनों स्वप्न से जाग जायें तो अपने को जान लें कि वास्तविक क्या हैं।
नींद में दिखने वाली स्वप्न जगत की माया हिता नाम की नाड़ी में दिखती है। जाग्रत की माया विता नाम की नाड़ी में दिखती है। यह केवल प्रतीति हो रही है। प्रतीति तब तक नहीं मिटती, जब तक प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति होती है नित्य वस्तु की। प्रतीति होती है अनित्य वस्तु की। 'मैं M.B.B.S. हूँ' यह प्रतीति है। मृत्यु का झटका आया, डिग्री खत्म हो गई। 'मैं M.D. हूँ... मैं L.L.B. हूँ... मैं उद्योगपति हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ... मैं कंगाल हूँ, मैं पटेल हूँ... मैं गुजराती हूँ... मैं सिंधी हूँ... मुझे यह समस्या है... मुझे यह पाना है.. मुझे यह पकड़ना है.. मुझे यह छोड़ना है..." ये सब प्रतीति है। प्रतीति जब तक सत्य लगती रहेगी, प्रतीति में प्रतीति का दर्शन नहीं होगा, प्रतीति में प्राप्ति का दर्शन होगा, तब तक दुःखों का अंत नहीं आयगा।
कभी न
छूटे पिण्ड
दुःखों से।
जिसे
ब्रह्म का
ज्ञान नहीं।।
एक दुःख नहीं, हजार दुःख मिटा दो, फिर भी कोई न कोई दुःख रह जाता है। जब प्राप्ति होती है, तब हजार विघ्न आ जायें फिर भी उद्विग्न नहीं करते, सुख में स्पृहा नहीं कराते।
प्रतीति होती है माया में और प्राप्ति होती है अपने परब्रह्म परमात्मा-स्वभाव की। प्राप्त होने वाली एक ही चीज है, प्राप्त होने वाला एक ही तत्त्व है और वह है परमात्म-तत्त्व। उसकी ही केवल प्राप्ति होती है।
प्रतीति होती है वृत्तियों से।
आज 20 मई है। अगले वर्ष की 20 मई के दिन आपको लगा होगा कि, 'मुझे यह सुख मिला.... मैंने यह खाया... वह पिया... सुबह में चाय मिली.. दोपहर को भोजन मिला....' आदि आदि। लेकिन अब बताओ, उसमें से अब आपके पास कुछ है ? गत वर्ष के कई महीने की २० तारीख को जो कुछ सुख-दुःख मिला, मान-अपमान मिला, अरे पूरे मई महीने में जो कुछ सुख-दुःख, मान-अपमान मिले वे अभी हैं ? वह सब प्रतीति थी। सब प्रतीत होकर बह गया। प्रतीति का साक्षी दृष्टा चैतन्य परमात्मा रह गया।
जो रह गया, वह जीवन है और जो बह गया, वह मृत्यु है। एक दिन शरीर भी बह जायेगा मृत्यु की धारा में लेकिन तुम रह जाओगे। अगर अपने को जानोगे तो सदा के लिए निर्बंध नारायण स्वरूप में स्थित हो जाओगे।
जो बाहर से मिलेगा, वह सब प्रतीति मात्र होगा। शरीर भी प्रतीति मात्र है कि 'मैं फलाना हूँ..... मैं न्यायाधीश हूँ......... मैं उद्योगपति हूँ....' यह व्यवहार काल में केवल प्रतीति है। 'मैं गरीब हूँ...' यह प्रतीति है।
जैसे स्वप्न की चीजों को साथ में लेकर आदमी जाग नहीं सकता, ऐसे ही प्रतीति को सच्चा मानकर परमात्म-तत्त्व में जाग नहीं सकता। शिवजी पार्वती से कहते हैं-
उमा
कहों मैं
अनुभव अपना ।
सत्य
हरि भजन जगत
सब सपना ।।
स्वप्न में जो कुछ मिलता है, वह सचमुच में प्राप्त होता है कि मिलने की मात्र प्रतीति होती है ? प्रतीति होती है।
बचपन में आपको खिलौने मिले थे, सुख-दुःख मिले थे, मान-अपमान मिला था वह प्राप्त हुआ था कि प्रतीत हुआ था ? प्रतीत हुआ था। कल जो कुछ सुख-दुःख मिला, वह भी प्रतीत हुआ। ऐसे ही आज भी जो कुछ मिलेगा, वह भी प्रतीति मात्र होगा।
बचपन भी प्रतीति, युवानी भी प्रतीति, बुढ़ापा भी प्रतीति तो जीवन भी प्रतीति और मृत्यु भी प्रतीति। यह वास्तव में प्रतीति हो रही है। इस प्रतीति को सच्चा मान रहे हैं.... प्राप्ति मान रहे हैं, इसलिए प्राप्ति पर परदा पड़ा है।
प्राप्ति होती है परमात्मा की। प्रतीति होती है परमात्मा की माया की। जैसे जल के ऊपर तरंगे उछलती हैं, ऐसे ही प्राप्ति की सत्ता से प्रतीति की तरंगे उछलती हैं। तरंग को कितना भी संभालकर रखो, लेकिन तरंग तो तरंग ही है। ऐसे ही प्रतीति को कितना भी संभालकर रखो, प्रतीति तो प्रतीति ही है।
अब हमें क्या करना चाहिए ?
प्रतीति को जब प्रतीति समझेंगे, तब अनुपम लाभ होगा। प्रतीति को अगर ठीक से प्रतीति मान लिया, प्रतीति जान लिया तो प्राप्ति हो जायेगी अथवा प्राप्ति तत्त्व को ठीक से जान लिया तो प्रतीति का आकर्षण छूट जायेगा। प्राप्ति में टिक गये तो प्रतीति का आकर्षण छूट जायेगा।
प्राप्ति होती है परमात्मा की और प्रतीति होती है माया की। प्रतीति में सत्यबुद्धि होने से उसका आकर्षण रहता है। उसको कहते हैं वासना। वासना पूर्ण करने में कोई बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय लगता है, छोटा आदमी विघ्न डालता है तो क्रोध आता है और बराबरी का आदमी विघ्न डालता है तो ईर्ष्या होती है।
प्रतीति की वासना थोड़ी बहुत पूरी हुई तो 'और मिल जाय' ऐसी आशा बनती है। फिर 'और मिले... और मिले....' ऐसे लोभ बनता है। प्रतीति में सत्यबुद्धि होने से ही आशा, तृष्णा, वासना, भय, क्रोध, ईर्ष्या, उद्वेग आदि सारी मुसीबतें आती हैं। प्रतीति को सत्य मानने में, प्रतीति को प्राप्ति मानने में सारे दोष आते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते है-
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः
सुखेषु
विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः
स्थितधीर्मुनिरूच्यते।।
'दुःखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये है, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है।'
(भगवद् गीताः २.५६)
दुःख आये तो मन को उद्विग्न मत करो। सुख की स्पृहा मत करो।
मुनि माने जो सावधानी से मनन करता है कि प्रतीति में कहीं उलझ तो नहीं रहा हूँ ? जो छूटने वाला है, उसको सच्चा समझकर अछूट से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ ? अछूट में टिका हूँ या छूटने वाले में उलझ रहा हूँ ? इस प्रकार सावधानी से जो मनन करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसकी प्रज्ञा प्राप्ति में प्रतिष्ठित हो जाती है, परमात्मामय बन जाती है।
भक्तमाल में एक कथा आती है।
अमरदास नाम के एक संत हो गये। वे जब तीन साल के थे, तब माँ की गोद में बैठे-बैठे कुछ प्रश्न पूछने लगेः
"माँ ! मैं कौन हूँ ?"
बेटा ! तू मेरा बेटा है ?
"तेरा बेटा कहाँ है?"
माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर, उसके बाल सहलाते हुए कहाः "यह रहा मेरा बेटा।"
"ये तो सिर और बाल है।"
माँ ने दोनों गालों को स्पर्श करते हुए कहाः "यह है मेरा गुलड़ू।"
"ये तो गाल हैं।"
हाथ को छूकर माँ ने कहाः "यह है मेरा बेटा।"
"ये तो हाथ है।"
अमरदास वास्तव में गत जन्म के प्राप्ति की ओर चलने वाले साधक रहे होंगे। इसीलिए तीन साल की उम्र में ऐसा प्रश्न उठा रहे थे। साधक का हृदय तो पावन होता है। जिसका हृदय पावन होता है, वह आदमी अच्छा लगता है। पापी चित्तवाला आदमी आता है, उसको देखकर चित्त उद्विग्न होता है। श्रेष्ठ आत्मा आता है, पुण्यात्मा आता है तो उसको देखकर हृदय पुलकित होता है। इसी बात को तुलसीदासजी ने इस प्रकार कहा हैः
एक
मिलत दारूण
दुःख देवहिं।
दूसर
बिछुड़त
प्राण हरी
लेवहिं।।
क्रूर आदमी आता है तो चित्त में दुःख होने लगता है। सदगुणी, सज्जन जब हमसे बिछुड़ता है, दूर होता है, तब मानो हमारे प्राण लिये जा रहा है। अमरदास ऐसा ही मधुर बालक था। माँ का इतना वात्सल्य और फिर इतना समझदार बेटा ! तीन वर्ष की उम्र में ऐसे-ऐसे प्रश्न करे ! हृदय में पूर्ण निर्दोषता है। निर्दोष बच्चा प्यारा लगता ही है। माँ ने अमरदास को छाती से लगा लिया।
"यह है मेरा बेटा।"
"यह तो शरीर है। यह शरीर कब से तेरे पास है ?"
"यह तो शादी के बाद आया मेरे पास ।"
"तो माँ ! उसके पहले मैं कहाँ था ? शादी के बाद तेरे पास मैं नहीं आया। तुम्हारे शरीर से मेरे शरीर का जन्म हुआ। तुम्हारी शादी के पहले भी कहीं था। इसका अर्थ है कि शरीर मैं नहीं हूँ। यह शरीर नहीं था, तब भी मैं था। शरीर नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूँगा। तो वह मैं कौन हूँ ?"
'मैं कौन हूँ ?' इसकी खोज प्राप्ति में पहुँचा देती है। 'मैं आसाराम हूँ..... मैं गोविन्दभाई हूँ...' यह प्रतीति है। यह शरीर भी प्रतीति है, शरीर के सम्बन्ध भी प्रतीति हैं, शरीर से सम्बन्धित जड़ वस्तु या चेतन व्यक्ति आदि सब प्रतीति मात्र हैं। प्रतीति जिसकी सत्ता से हो रही है वह है प्राप्ति।
शरीर भी प्रतीति, इन्द्रियाँ भी प्रतीति। हाथ भी प्रतीति, आँख भी प्रतीति, कान भी प्रतीति। आँख ठीक से देख रही है कि नहीं देख रही है, कान ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, यह भी प्रतीति हो रही है। मन में शान्ति है कि अशान्ति, इसकी भी प्रतीति हो रही है। बुद्धि में याद रहता है कि नहीं रहता इसकी भी प्रतीति हो रही है।
प्रतीति जिसको होती है, उसको अगर खोजोगे तो प्राप्ति हो जायेगी, बेड़ा पार हो जायेगा।
हम लोग गलती करते हैं कि प्रतीति के साथ अपने को जोड़ देते हैं। प्रतीति होने वाले शरीर को 'मैं' मान लेते हैं। हम क्या हैं ? हम प्राप्ति तत्त्व है, उधर ध्यान नहीं जाता।
मंदिर वाले मंदिर में जा-जाकर आखिर यमपुरी पहुँच जाते हैं, स्वर्गादि में पहुँच जाते हैं। मस्जिदवाले भी अपने ढंग से कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं। अपने-आप में, आत्मा-परमात्मा में कोई विरले ही आते हैं। जो प्राप्ति में डट जाता है वह परमात्मा में आता है और बाकी के लोग लोक-लोकान्तर में और जन्म-मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। धन्य तो वे हैं जो अपने आप में आये, परमात्मा में आये। वे तो धन्य होते ही हैं, उनकी मीठी दृष्टि झेलने वाले भी धनभागी हो जाते हैं।
दैत्यगुरू शुक्राचार्य राजा वृषपर्वा के गुरू थे। वे उसी के नगर में रहते थे। शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। उसकी सहेली थी वृषपर्वा राजा की पुत्री शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा कुछ अपने स्वभाव की थी, प्रतीति में उलझी हुई लड़की थी। शरीर के रूप लावण्य, टिप-टाप आदि में रूचि रखने वाली थी।
एक बार दोनों सहेलियाँ स्नान करने गई। शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिये। देवयानी भी गुरू की पुत्री थी, वह भी कुछ कम नही थी। उसने शर्मिष्ठा को सुना दियाः
"इतनी भी अक्ल नहीं है ? राजकुमारी हुई है और दूसरो के कपड़े पहन लेती है ? भूल जाती है ?"
शर्मिष्ठा ने गुस्से में देवयानी को उठाकर कुएँ में डाल दिया और चली गई। देवयानी दैत्यगुरू की पुत्री थी। दैवयोग से कुएँ में पानी ज्यादा नहीं था। वहाँ से गुजरते हुए राजा ययाति ने देवयानी की रूदन-पुकार सुनी और उसे बाहर निकलवाया।
शुक्राचार्य ने सोचाः जिस राजा की पुत्री अपनी गुरू पुत्री को कुएँ में डाल देती है ऐसे पापी राजा के राज्य ने हम नहीं रहेंगे। वे राज्य छोड़कर जाने लगे। राजा को पता चला की शुक्राचार्य कुपित होकर जा रहे हैं और यह राज्य के लिए शुभ नहीं है। अतः कैसे भी करके उनको रोकना चाहिए। राजा पहुँचा शुक्राचार्य के चरणों में और माफी माँगने लगा। उन्होंने कहाः
"मुझसे माफी क्या माँगते हो ? गुरूपुत्री का अपमान हुआ है तो उसी को राजी करो।"
राजा देवयानी के पास गया।
"आज्ञा करो देवी ! आप कैसे सन्तुष्ट होंगी ?"
"मैं शादी करके जहाँ जाऊँ, वहाँ तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा मेरी दासी होकर चले। तुम अपनी बेटी मुझे दहेज में दे दो, वह मेरी दासी होकर रहेगी।"
राजा के लिए यह था तो कठिन लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं था। अतः राजा को यह शर्त कबूल करना पड़ा। ययाति राजा के साथ देवयानी की शादी हो गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देवयानी के साथ भेजा गया। शर्मिष्ठा तो सुन्दर थी। उस दासी के साथ राजा ययाति पत्नी का व्यवहार न करे, इसलिए शुक्राचार्य ने ययाति को वचनबद्ध कर लिया। फिर भी विषय-विकार के तूफान में ययाति का मन फिसल गया। वह अपने वचन पर टिका नहीं। शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने राजा ययाति को वृद्ध हो जाने का शाप दे दिया। युवान राजा ययाति तत्काल वृद्ध हो गया। शर्मिष्ठा को तो दुःख हुआ, लेकिन ययाति को उससे भी ज्यादा दुःख हुआ। 'त्राहिमाम्' पुकारते हुए राजा ययाति ने गिड़गिड़ाकर शुक्राचार्य से प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने द्रवीभूत होकर कहाः
"तुम्हारा कोई युवान पुत्र अगर तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले और अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो तुम संसार के भोग भोग सकते हो।"
राजा ययाति ने अपने पुत्रों से पूछा। सबसे छोटा पुत्र पुरूरवा राजी हो गया। पिता की मनोवांछना पूर्ण करने के लिए। उसका यौवन लेकर राजा ययाति ने हजार वर्ष तक भोग भोगे। फिर भी उसके चित्त में शान्ति नहीं हुई।
प्रतीति से कभी भी पूर्ण शांति मिल ही नहीं सकती। अगर प्रतीति का उपभोग करने से शान्ति मिली होती तो जिनके पास राजवैभव था, धन था, भोग-विलास था, वे अशान्त और दुःखी होकर क्यों मरे ? किसी सत्तावान को, धनवान को सत्ता और धन से, पुत्र-परिवार मिलने से मोक्ष मिल गया हो, ऐसा हमने नहीं सुना। जिसको ज्यादा विषय-विकार भोगने को मिले, वे बीमार रहे, दुःखी रहे, अशान्त रहे, आत्महत्या करके मरे ऐसा आपने और हमने देखा सुना है। वे नर्कों में गये, मुक्त तो नहीं हुए। जिसको विषय विकार और संसार की चीजें ज्यादा मिलीं और ज्यादा भोगी उसकी मुक्ति हो गयी, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा और सुनोगे भी नहीं। रामतीर्थ बोलते थेः छाया चाहे बड़े पर्वत की हो, लेकिन छाया तो छायामात्र है।
ऐसे ही प्रतीति चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्रतीति तो केवल प्रतीति ही है।
आखिर राजा ययाति को लगा किः
न जातु
कामः कामानां
उपभोगेन
शाम्यति।
हविषा
कृष्णवर्त्मेव
भूय
एवाभिवर्धते।।
अग्नि में घी डालने से आग और भड़कती है ऐसे ही काम-विकार और संसार के भोग भोगने से तृष्णा, वासना, आशा, स्पृहा ये सब उद्वेग बढ़ाने वाले विकार अधिक भड़कते हैं।
राजा ययाति प्रतीति को प्रतीति समझकर, उसे तुच्छ जानकर ईश्वर की ओर लगने के लिए जंगल में चला गया, तप करने लगा।
तपःसु
सर्वेषु एकाग्रता
परं तपः।
‘सब तपों में एकाग्रता परम तप है।’
एकाग्रता और अनासक्ति ये – दो हथियार जिसके पास आ जायें, वह अनपढ़ हो चाहे साक्षर हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, सुप्रसिद्ध हो चाहे कुप्रसिद्ध हो, वह प्राप्ति में टिक सकता है। प्राप्ति तो ब्रह्म-परमात्मा की होती है। ब्रह्म-परमात्मा से बड़ा कौन हो सकता है ?
राजा-महाराजा रूठ जाये, तो क्या कर डालेगा ? उसका जोर स्थूल शरीर पर चलेगा और देवी देवता का जोर सूक्ष्म शरीर तक चलेगा। माया नाराज हो जाय तो उसका जोर कहाँ तक चलेगा ? कारण शरीर तक। प्राप्ति तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीनों शरीरों से परे जो परमात्मा तत्त्व है उसकी होती है। स्थूल शरीर को अधिक से अधिक शूली पर चढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर को माया नर्कों में भेज सकती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तीनों प्रतीति मात्र हैं। प्रतीति को जो जानता है, वह प्रतीति का दृष्टा प्राप्ति-तत्त्व में जाग जाता है, परब्रह्म परमात्मस्वरूप हो जाता है।
'मैं चैतन्य हूँ..... मैं शुद्ध हूँ... जो सदा प्राप्त आत्मा है, वह मैं हूँ। प्रतीत होने वाली देह मैं नहीं हूँ।' सारी पृथ्वी के लोग केवल पाँच मिनट के लिए ऐसा चिन्तन करें तो दूसरी पाँच मिनट में सारी पृथ्वी स्वर्ग के रूप में बदली हुई मिलेगी, ऐसा विवेकानन्द कहा करते थे।
"हे मनुष्यों ! तुम चैतन्य हो..... परमात्मा हो.... हे पक्षी ! तुम भी चैतन्य हो... तुम सब चैतन्य हो... ब्रह्म हो.... मैं भी चैतन्य हूँ.... प्राप्त स्वरूप हूँ..... तुम भी प्राप्त स्वरूप हो.... मैं आनन्द स्वरूप हूँ.... तुम भी वही हो। मरने जन्मने वाला शरीर तुम नहीं हो.... सुखी-दुःखी होने वाला मन तुम नहीं हो.... निर्णय बदलने वाली बुद्धि तुम नहीं हो... रंग बदलने वाला चमड़ा तुम नहीं हो.... भूख और प्यास लगाने वाले प्राणों की धौंकनी तुम नहीं हो। ये सब प्रतीति है। इन सबको जो देख रहा है, वह प्राप्तिस्वरूप चैतन्य तुम हो। तुम अमर आत्मा हो।"
इस प्रकार का चिन्तन गुरू करवाएँ और शिष्य सच्चाई से करने लग जाएँ तो उसी समय वातावरण सुखद हो जाय। परब्रह्म परमात्मा सदा प्राप्त है। उस परमात्मा का चिन्तन करने से गौहत्या जैसे, ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब दुःख दूर हो जाते हैं।
प्रतीति में अगर सत्यबुद्धि है तो कितनी भी सुविधा होगी फिर भी दुःख दूर नहीं होगा। प्रतीति में जब प्रतीतिबुद्धि हो जाय और प्राप्ति में जब सत्यबुद्धि हो जाय तो कितने भी दुःख आ जाएँ तो इतना उद्विग्न नहीं करेंगे। जैसे जलती हुई भट्ठी में ईंधन डाल दिया जाय तो आग अधिक भड़क उठेगी लेकिन ईंधन को फ्रीज में रख दिया जाए तो ? आग तो क्या पैदा होगी, ईंधन ही ठण्डा हो जायगा।
ऐसे ही साधारण आदमी को इच्छा-वासनारूपी ईंधन जितनी ज्यादा होगी, उसका अंतःकरण उतना ज्यादा तपता रहेगा है। ज्ञान के चित्त में वे ईंधन उतनी अशांति की आग नहीं बना सकते।
ईंधन को गोदाम में रखो, फ्रीज में रखो और भट्ठी में डालो, इसमें फर्क होता है। दीये में तेल डालना बन्द कर दो तो दीया बुझ जाता है, निर्वाण हो जाता है। ऐसे ही प्रतीति में सत्यबुद्धि छोड़ दो तो वासना धीरे-धीरे निवृत्त होने लगती है।
निर्मानमोहा
जितसंगदोषा
अध्यात्मनित्या
विनिवृत्तकामाः
।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः
सुखदुःखसंज्ञै-
र्गच्छन्त्यमूढाः
पदमव्ययं तत् ।।
"जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, परमात्मा के स्वरूप में जिनकी नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख-दुःख नामक द्वन्द्वों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते हैं।"
(भगवद् गीताः१५.५)
बड़ी तकलीफ यह होती है कि जो शरीर और संसार दिख रहा है, जो प्रतीति हो रही है, उसको सत्य मानकर जीनेवाले लोगों के बीच हम पैदा हुए, उन्हीं के साथ हम पढ़े-लिखे और उन्ही लोगों के बीच रहकर हम इच्छा करने लगे कि, 'मैं पास हो जाऊँ तो सुख मिले..... मुझे यह मिल जाय तो मैं सुखी हो जाऊँ....' प्रतीति को ही प्राप्ति मानकर उलझ गये।
दो वस्तुएँ हैं। एक प्रतीति और दूसरी प्राप्ति। प्राप्ति परमात्मा की होती है और प्रतीति माया की।
प्रतीति के बिना प्राप्ति टिक सकती है लेकिन प्राप्ति के बिना प्रतीति हो ही नहीं सकती। चैतन्य के बिना शरीर चल नहीं सकता, किन्तु शरीर के बिना चैतन्य रह सकता है। ये जो वस्तुएँ दिख रही हैं, वे चैतन्य के बिना रह नहीं सकतीं, लेकिन वस्तुओं के बिना चैतन्य रह सकता है।
एके ते
सब होत है
सबसे एक न
होई।
बल्लभाचार्य का एक बड़ा प्यारा शिष्य था कुंभनदास। आचार्य पधारें, उसके पहले वह आ जाता था। बड़े ध्यान से सत्संग सुनता था। सुनकर चिन्तन करता था कि, 'गुरू महाराज ने क्या कहा ? मोह से कैसे बचें ? ज्ञान कैसे बढ़े ? भक्ति की भावना से हृदयरूपी चमन सुगन्धित कैसे बने ?"
कुंभनदास के सात बेटे थे। वह साधन-सम्पन्न सुखी आदमी था।
एक दिन गुरूजी के समक्ष भक्त शिष्य समुदाय बैठा था। गुरू जी ने कुंभनदास का हाल-अहवाल पूछाः
"कुंभनदास ! कहो, तुम्हारा सब ठीक चल रहा है ?"
"हाँ महाराज जी !"
"क्या धन्धा करते हो ?"
कुंभनदास ने सब बताया।
"अच्छा....। तुम्हारे बेटे कितने हैं ?"
"गुरू महाराज ! मेरे पास डेढ़ बेटा है।"
"डेढ़ बेटा ! यह कैसे ?" गुरू जी को आश्चर्य हुआ।
"गुरूजी ! पुत्रों के पुतले तो सात है, लेकिन पुत्र केवल डेढ़ ही है। एक बेटा है जिसको ज्ञान और सेवा में रूचि है, इस मार्ग में उसकी गति है। मैं आपसे जो सुनकर जाता हूँ, वह उसे सुनाता हूँ। वह बड़े चाव सुनता है, समझता है। कभी-कभी वह मेरे साथ आपके श्रीचरणों में आता है। उसके जीवन में ज्ञान भी है और सेवा भी है। वह मेरा एक पूरा बेटा है। दूसरे लड़के में पिता के लिए भाव है, भगवन के लिए भक्ति है और सेवाभाव भी है लेकिन भगवान और पिता में एक ही अद्वितीय तत्त्व है, यह उस मूर्ख को ज्ञान नहीं है। इसलिए वह बेटा मेरा आधा बेटा है आधा। पिता को पिता समझकर पूजता है, भगवान की मूर्ति को भगवान समझकर पूजता है लेकिन भगवान का तत्त्व और पिता का तत्त्व अलग नहीं है... भगवान को छोड़कर पिता हो नहीं सकता और पिता को छोड़कर भगवान रह नहीं सकता। भगवान तत्त्व पिता के सहित है, ऐसा अखण्ड ज्ञान उसको नहीं है, इसलिए वह आधा है।"
अखण्ड ज्ञान होता है प्राप्ति में स्थिर होने से। खण्ड-खण्ड का ज्ञान तो बहुत है। कोई आँख का विशेषज्ञ है तो कोई कान का विशेषज्ञ है, कोई हृदय का विशेषज्ञ है तो कोई मस्तिष्क का विशेषज्ञ है। एक शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होते है। फिर भी किसी विशेष में पूर्ण ज्ञान अभी तक हाथ नहीं लगा है क्योंकि यह सब प्रतीति है। प्रतीति कल्पनाओं का जगत होता है। पूर्ण परमात्मा तत्त्व को कोई जान लेगा तो बस, वह भी पूर्ण हो जायेगा। बाकी की माया तो माया ही होती है।
तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पूर्ण है। तुम वास्तव में पूर्ण आत्मा हो। शरीर पूर्ण नहीं हो सकता, शरीर के पूर्जे पूर्ण नहीं हो सकते। शरीर प्रतीति है। शरीर, मन, बुद्धि क्षण क्षण में बदल रहे हैं। जो बदलता है, उसमें सत्यबुद्धि न करें। जो अबदल है, उसमें सत्यबुद्धि करके चिन्तन करें किः
"सत्यस्वरूप मेरा आत्मा है। यह संसार स्वप्न है, प्रतीति मात्र है। इसमें सुख मिला तो क्या ? सुख तो आता है और जाता है। दुःख भी आता है और जाता है। मैं सुख-दुःख से परे, शरीर और संसार की तमाम प्रतीतियों से परे उनके अधिष्ठान रूप आत्मा हूँ... प्राप्तिस्वरूप हूँ।"
"सुख आता है तो जाता है कि नहीं जाता ?"
"जाता है।"
"सुख जाता है तो क्या दे जाता है ?"
"दुःख।"
"दुःख जाता है तो पीछे क्या बचता है ?"
"सुख।"
सुख जाता है तो दुःख दे जाता है। दुःख जाता है तो सुख दे जाता है। जो सुख दे जाता है उसको देखकर घबराते हैं और जो दुःख दे जाता है, उसको देखकर चिपकते हैं क्योंकि प्रतीति में सत्यबुद्धि है। भगवान अर्जुन से कहते हैं-
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः
सुखेषु
विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः
स्थितधीर्मुनिरूच्यते
।।
सुख में स्पृहा मत रखो। दुःख में उद्विग्न मत बनो। ये बादल आये हैं, चले जायेंगे। हो-होकर क्या होगा ? जो प्रतीति मात्र है, उस शरीर के ऊपर ही कुछ होगा। एक दिन तो उस पर सब कुछ होगा। अमरपटा तो उसका है नहीं !
तुम लाये थे तो क्या लाये थे ? तुमने जो कुछ पाया, यहीं से पाया। प्रतीति में सब प्रतीत हो रहा है। आखिर सब स्वप्न हो जायेगा। स्वप्न की चीजों को देखकर जो उलझता है, वह अधूरा है।
पूरा शिष्य तो वही होता है, जिसमें गुरूभक्ति भी होती है और गुरूतत्त्व का ज्ञान भी होता है।
जितना-जितना परमात्म-तत्त्व का ज्ञान बढ़ता है, परमात्म-तत्त्व को पाये हुए महापुरूषों के प्रति भक्ति बढ़ती है उतना-उतना चित्त प्राप्ति के नजदीक होता है, परमात्मा के नजदीक होता है। जितना-जितना परमात्मा के नजदीक होता है, उतना-उतना वह निश्चिन्त होता है, उत्साहित होता है, आनन्दित होता है।
निष्काम कर्मयोग का सिद्धान्त हैः साधक का मन ऐसा होना चाहिए कि दुःखों की प्राप्ति में वह उद्विग्न न हो और सुखों की प्राप्ति के लिए लालायति न हो। जो साधक ऐसा निस्पृह है, तत्पर है, उसका राग चला जाता है, भय चला जाता है, क्रोध चला जाता है।
वीतरागभयक्रोधः
मुनिर्मोक्षपरायणः।।
जिसका भय, राग और क्रोध गया वह मोक्ष के परायण है।
जो प्रतीत होता है, उसमें सत्यबुद्धि होने से राग होता है। जिसमें राग होता है, उसको पाने में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध आता है, भय होता है, ईर्ष्या होती है, चिन्ता होती है। इन सबका मूल है प्रतीति में सत्यबुद्धि। भगवान कहते है कि यह प्रतीति मात्र है इसलिए इसमें राग, भय और क्रोध करने की जरूरत नहीं है। सब बीत जायगा। दुःख से उद्विग्न मत हो। सुख की स्पृहा मत करो। राग, भय और क्रोध चला जायगा तो बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जायगी।
जीव सोचता है कि अपनी वासना पूरी करके सुखी होऊँ। अरे सुखी तो ययाति भी नहीं हुआ, तू कहाँ से होगा ? संसार की चीजें पाकर कोई सुखी हो जाय यह संभव नहीं।
राजा सुषेण अपनी रानी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक तेजस्वी युवान बड़ी मस्ती बैठा था। बाईस साल तक जिसका ब्रह्मचर्य अखण्ड रहता है, वह तेजस्वी होता ही है। राजा सुषेण ने सोचा कि इसको बेचारे को अपने यौवन का सुख लेने का कोई पता ही नहीं है ऐसा लगता है। उन्होंने युवक से कहाः
"आप इतने तेजस्वी जवान ! इधर बैठे हैं ? चलिये, मेरे साथ रथ में बैठिये। मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ, आइये।"
युवक राजा के साथ गया। मीठी बात हो गई तो वह राजी हो गया। था कोई सत्संगी आत्मा गत जन्म का। अभी उसे कोई सदगुरू नहीं मिले थे, ईश्वर का मार्ग नहीं मिला था। फिर भी 'दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः' – ऐसे संस्कार गत जन्म में पाये हुए थे। आध्यात्मिक संस्कार नष्ट नहीं होते।
राजा ने उसे अपना राजमहल दिखाते हुए कहाः
"देखो, संसार का सुख भोगने के लिए यौवन मिला है। तुम्हारी शादी मैं करा देता हूँ। जरा संसार का अनुभव करो।"
युवक ने कहाः "शादी करूँ तो पत्नी आयेगी। उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। क्या पता पत्नी कैसी आ जाय ?"
"नहीं, पत्नी बढ़िया आएगी। देखो, यह मेरी रानी है न, उसकी बहन है। उसी के साथ तुम्हारी शादी करा दूँगा।"
"शादी तो हो जायेगी राजन ! लेकिन आपके पास तो राजपाट है। पत्नी का पालन करने के लिए मुझे तो मजदूरी करनी पड़ेगी। अभी तो जंगल में मस्ती से रहता हूँ।"
"नहीं, नही, मैं तुम्हें रहने के लिए महल दे दूँगा, पाँच गाँव दे दूँगा। कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहोगे तो आधा राज्य भी दे दूँगा। तुम मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो। तुम जैसा पति मिल जाय तो रानी की बहन की जिन्दगी धन्य हो जाय।"
"महाराज ! आप अपनी साली दे सकते हैं, आधा राज्य भी दे सकते हैं, फिर बाल-बच्चे होंगे तो ?"
"आधा राज्य होगा तो बाल-बच्चे भी खाएँगे-पियेंगे, क्या कमी रहेगी ?"
"कमी तो नहीं रहेगी.... लेकिन बच्चे में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लड़की अगर बदचलन हुई तो उसका दुःख आपको होगा कि मुझे होगा ? लड़का अगर पैदा होकर मर गया तो उसका दुःख आपको होगा कि मुझे होगा ?"
राजा ने कहाः "मुझसे ज्यादा दुःख तुमको होगा।"
युवक ने खिलखिलाते हुए कहाः "ऐसा दुःख मैं क्यों मोल लूँ ? ऐसा सुख क्या करना जो दुःख ही दुःख दे ?" युवक उठकर चल दिया। राजा सुषेण सोचने लगेः
"धन्य है जवान ! हम तो राजा है, पर तुम तो महाराजा हो महाराजा ! हम तो संसार के भँवर में आये हैं। निकलेंगे तब निकलेंगे, लेकिन तुम तो भँवर में आते ही नहीं।"
दुःख का मूल है प्रतीति में सत्यबुद्धि। इससे ययाति जैसे राजा भी बेचारे दुःखी हुए। अरे, राजा रामचन्द्रजी के बाप.... भगवान श्रीराम के बाप दशरथ राजा भी संसार से संतुष्ट होकर नहीं गये, सुखी होकर नहीं गये। कावे-दावे करके प्रतीति में सुख खोजने वाला दुर्योधन भी सुखी होकर नहीं गया। चाहे कितना भी कपट करो, कितना भी खुशामद करो, कितनी भी मेहनत मजदूरी करो लेकिन जो प्रतीति है, उससे पूर्ण सुख या संतोष आज तक किसी को हुआ नहीं, हो नहीं रहा और होगा भी नहीं। पूर्ण सुख तो होगा परमात्मा की प्राप्ति से।
प्राप्ति को हम जानते नहीं, इसलिए प्रतीति को प्राप्ति समझते हैं। प्राप्ति होती है परमात्मा की। बाकी होती है प्रतीति। प्रतीति माने धोखा। यह सारा संसार इन्द्रियों का धोखा है। प्राण निकल गये तो कुछ नहीं रहेगा। यह शरीर भी यहीं छूट जायेगा। मिलने की चीज तो आत्म-साक्षात्कार है, मिलने की चीज तो परमात्मा है। बाकी जो भी मिला है, सारा का सारा धोखा है। किसी को छोटा धोखा मिला, किसी को बड़ा धोखा मिला। लोग रो रहे हैं कि हमें बड़ा धोखा नहीं मिला। बड़ी मुसीबत नहीं मिली, इसलिए चिन्ता में है।
"अरे ! क्यों रोते हो।"
"बाबाजी ! चार साल हुए शादी किये। अभी तक गोद नहीं भरी....।"
अरे गोद भरेगी उसके पहले मुसीबत सहना पड़ेगा। बाद में भी क्या पता बेटा आवे, बेटी आवे। मुसीबत नहीं आ रही है, इसलिए मुसीबत हो रही है।
इच्छा करना ही हो तो प्रतीति की नहीं, प्राप्ति की करो। उद्यालक की तरह इच्छा करो। सोलह वर्ष का ब्राह्मण उद्यालक इच्छा करता हैः "मेरे ऐसे दिन कब आएँगे कि मैं संसार को स्वप्न तुल्य समझूंगा ? ऐसे मधुर दिन कब आएंगे कि मेरे राग-द्वेष चले जाएँगे... भय क्रोध शान्त हो जाएँगे। ऐसे दिन कब आएँगे कि मैं सत्ता-समान में स्थित रहूँगा ?
नारायण.... नारायण.... नारायण..... नारायण..... नारायण.....
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
आज तक जो कुछ मैंने देख लिया, भोग लिया, उससे मुझे आनन्द है। सैंकड़ों-सैंकड़ों सुख मैंने भोगे.... देखे.... उससे मुझे आनन्द है। मैं आह्लादित हूँ। हजारों गलतियाँ की होगी, दुःख भोगे होंगे उसका भी मुझे आनन्द है... क्योंकि गलतियों ने मुझे सिखा दिया कि जीवन जीने का यह तरीका ठीक नहीं। दुःखों ने मुझे सिखा दिया कि विकारी सुखों में आसक्त होना ठीक नहीं।
हम घर-बार छोड़कर भाग गये, सब सगे सम्बन्धियों का ठुकराते रहे, अपने शरीर को भी सताते रहे, कष्ट सहते रहे, दुःख भोगते रहे.... यह भी ठीक नहीं। भोग-विलास में लट्टू होकर गिरे रहना भी जीवन जीने का ढंग नहीं।
न भोग ठीक है, न अति त्याग ठीक है। विवेकपूर्ण मध्यम मार्ग ही ठीक है। शरीर को औषधवत खिलाना पिलाना चाहिए। जीवन जीने के साधनों का औषधवत् उपयोग करना चाहिए।
जीवन का पुष्प जीवनदाता के स्वभाव में खिलने के लिए है। मेरा चैतन्य आत्मा जो भीतर है, वही बाहर भी है। जो आज है वही कल भी है और परसों भी है। आज और कल मन की कल्पना है। आज और कल को जानने वाला चिदाकाश चैतन्य.... हर दिल में 'मैं.... मैं....' करता हुआ, मन बुद्धि को सत्ता देता हुआ सत्ताधीश.... मन बुद्धि से परे भी वही चिदाकाश आत्मा मैं हूँ। यह आत्मदृष्टि ही एकमात्र सार है, और सब परिश्रम है।
आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का आदर्श होना चाहिए। जिसके जीवन का कोई आदर्श नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन घोर अन्धकार में भटक जाता है। आत्मज्ञान ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, वह चाहे सैंकड़ों गलतियाँ कर ले, फिर भी वह कभी-न-कभी उस लक्ष्य को पा लेगा। जिसका लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं है, वह हजारों-हजारों गलतियाँ करता रहेगा, हजारों-हजारों जन्मों में भटकता रहेगा।
सर्वत्र ओतप्रोत चैतन्यघन परमात्मा का अनुभव करना जिसके जीवन का लक्ष्य है, वह देर सवेर परमात्मामय हो जाता है।
परमात्मा आनन्दस्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है। कीड़ी में भी ज्ञान है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ रहना और कहाँ से भाग जाना। कीड़ी में चेतना भी है। कीड़ी भी सुख के लिए ही यत्न करती है।
सत्यं
ज्ञानं
अनन्तं
ब्रह्म।
ब्रह्म सत्यस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है, अनन्त है। ब्रह्म स्थूल से भी स्थूल है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कीड़ी मकोड़ा, बैक्टीरिया में भी मेरे परमेश्वर की चेतना है। अर्थात् परमेश्वर ही अनेक रूप होकर बाह्य चेष्टा और आभ्यान्तर प्रेरणा का प्रकाशक है। वही सबका अधिष्ठान है। उसी से इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि चेष्टा करते है। उन्हें खट्टा-मीठा अनुभव होता है। फिर भी उन सब अनुभवों से परे जो मेरा आत्मा है, वही चैतन्य सब अनुभवों का भी आधार है।
बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, चित्त बदलता है, शरीर बदलता है, दरिया बदलता है.... दरिया के किनारे बदलते हैं। यह सब उस चैतन्य की लीला है, चैतन्य की स्फुरणा है। उसी को आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं, माया बोलते हैं। जैसे दूध और दूध की सफेदी अभिन्न है, ऐसे ही मेरा चैतन्य आत्मा और उसकी स्फुरणा शक्ति अभिन्न है।
यह जगत हरिरूप है। हरि ही जगत रूप होकर दिखते है।
स्फुरणा स्फुर-स्फुरकर बदल जाता है, पर स्फुरणा का आधार अस्फुर है। जैसे सागर में तरंग उत्पन्न हो होकर लीन हो जाते है, पर सागर के तल में शांत जल है। विशाल उदधि में कोई बड़ी तरंग है, कोई छोटी तरंग है, कोई शुद्ध तरंग है तो कोई मलिन तरंग है। ये सारी छोटी बड़ी, मलिन-शुद्ध तरंगे उसी सागर में हैं। ऐसे ही मेरे आत्म सागर में कहीं शुद्ध तो कहीं अशुद्ध, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा स्फुरणा दिखता है।
जैसे जल की तरंग सड़क पर नहीं दौड़ती। वह जल में ही पैदा होती है, जल पर ही दौड़ती है और आखिर जल में ही समा जाती है, फिर जल से ही उठती है। ठीक वैसे ही विश्व के तमाम जीव उसी एक ब्रह्म समुद्र की तरंगे हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है, कोई अपना है कोई पराया है। सब उसी विराट-विशाल मुझ चैतन्य सागर की तरंगे हैं। तरंगे उठती हैं, नाचती हैं, आपस में टकराती है, लड़ती-झगड़ती हैं, किल्लोल करती हैं, मिटती हैं। वे कदापि सागर से अलग नहीं हो सकतीं। ऐसे ही संसार में सब चेष्टाएँ करने वाले कोई व्यक्ति परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, अलग हैं नहीं, अलग हो नहीं सकते।
हम उसी परमात्मा में विश्रान्ति पा रहे हैं, उसी में हँस रहे हैं, खेल रहे हैं।
जीवन में होने वाली हजार-हजार गलतियों से हमें सबक सीखने को मिलता है। जब-जब ईश्वर दृष्टि की तब-तब सुख पाया, आनन्द पाया, शान्ति पाई। विचार उन्नत बने। जब-जब अच्छे बुरे की दृष्टि की, अपने और पराये की दृष्टि की, नाम और रूप में आस्था की, तब तब धोखा खाया।
मुझे आनन्द है कि धोखा खाने पर भी हम कुछ सीखे हैं। अनुकूलता-प्रतिकूलता से भी कुछ सीखे हैं। अनुकूलता कहती है कि परमात्मा आनन्दस्वरूप है। धोखा खाने से जो दुःख मिला उसने बताया कि अज्ञान की दृष्टि दुःखदायी है।
हमने जो प्रतिकूलताएँ सही, दुःख सहा या धोखे खाये, उसका भी हमें मजा है। अगर ये गलतियाँ और दुःख, प्रतिकूलताएँ, विघ्न और बाधाएँ न होती तो शायद हम उतने उन्नत भी नही हो पाते। यह हमारे सारे जीवन का अनुभव है कि प्रतिकूलताएँ और दुःख भी हमें कुछ सीख दे जाते हैं। अनुकूलता भी कुछ आनन्द और उल्लास दे जाती है।
अपनी जीवन की सारी यात्राओं की मीमांसा यह है कि हमारे पास अनुभव का फल है। अनुभव रूपी फल का हम आदर करते हैं।
जब-जब देहभाव से आक्रान्त होकर, जब-जब संसार की चलित तरंगों को ही सार समझकर तरंगों के आधार को भूले हैं, तब-तब दुःख उठाये हैं। जब-जब तरंगों को लीलामात्र समझकर, उनके आधार को सत्य समझकर संसार में विचरे हैं, तब-तब आनन्द, सुख और ईश्वरीय मस्ती का अनुभव हुआ है।
सारे धर्म उसी सुखस्वरूप ईश्वर की ओर ले जाने की चेष्टा करते हैं। उनकी भाषा अपनी-अपनी है। जहाँ दृष्टि सीमित हो जाती है, इन्द्रियगत सुख में आबद्ध हो जाते हैं, विकारी सुख में फिसलते हैं, तब प्रकृति थप्पड़ मारती है.... तरंगें टकराती हैं। जब गहन शांत जल में तरंगें विलीन होती हैं, तो कोई कोलाहल नहीं रहता।
दरिया के किनारे पर खड़ा आदमी उछलती-कूदती तरंगों को देखकर यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनका आधार शांत उदधि है। उसके तले में बिल्कुल शांत स्थिर जल है। उसी के अचल सहारे यह चल दिख रहा है। तरंगित होना वाला जल बहुत थोड़ा है.... उसकी गहराई में शांत जल अगाध है, अमाप है।
ऐसे ही तरंगायमान होनेवाला माया का हिस्सा तो बहुत थोड़ा है..... मेरा शान्त ब्रह्म ही अमाप है।
ऐसी कोई बूँद नहीं जो जल से भिन्न हो। ऐसा कोई जीव नहीं जो परमात्मा से भिन्न हो। ऐसी कोई तरंग नहीं जो बिना पानी के रह सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो चैतन्य परमात्मा के बिना रह सके। जिन्दा है तब भी उसमें चैतन्य परमात्मा है और मृत्यु के बाद भी सुषुप्तघन अवस्था में परमात्मा तत्त्व मौजूद रहता है।
प्राण रहित शव जला दिया जाता है, तब उसका जल वाष्पीभूत होकर विराट जल तत्त्व में मिल जाता है। शव का आकाश विराट महाकाश में मिल जाता है। उसका श्वास विराट वायुतत्त्व में मिल जाता है। उसका पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी तत्त्व में मिल जाता है। उसका तेज अग्नितत्त्व में मिल जाता है।
जैसे सागर की तरंगे जल से उत्पन्न होकर फिर सागर जल में ही लीन होती हैं ऐसे ही हम लोग भी ईश्वर से ही उत्पन्न होकर ईश्वर में ही खेलते हैं और फिर ईश्वर में ही मिल जाते हैं। हम दुःख तब उठाते हैं कि जब उसको ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर नहीं जानते, नहीं समझते। हममें ईश्वरतत्त्व का भाव नहीं जागता। मेरे तेरे का भाव ही हमें दुःख देता है, परेशान करता है। इस भाव को बदला तो बेड़ा पार हो जायेगा।
जिसके पास खूब विचार है, तर्क है, तगड़ी खोपड़ी है किन्तु हृदय नहीं है तो उसका जीवन रूखा है। ऐसे जीवन में अशांति, उद्वेग, तर्क-वितर्क, कुतर्क होते हैं। रूखे मस्तिष्क से जीने का मजा नहीं। जीवन में हृदय की नितान्त अनिवार्यता है। जिसके पास विशाल हृदय है, विशाल सहानुभूति है, विशाल प्रेम है, वह परम प्रेमास्पद की विशालता का अनुभव करके आनन्दित रहता है, सुखी रहता है।
केवल हृदय की भावना से भी काम नहीं चलता। अज्ञानता के कारण भावना-भावना में बहुत दुःख उठाने पड़ते हैं। केवल भावना भी उपयुक्त नहीं। भावना के साथ विशाल ज्ञाननिधि भी चाहिए।
तो क्या थोड़ा हिस्सा भावनात्मक हृदय का और थोड़ा हिस्सा ज्ञानात्मक मस्तिष्क का हो ?
नहीं....। हृदय की पूर्ण विशालता हो और मस्तिष्क में ज्ञानमय विशाल समझ हो।
यस्य
ज्ञानमयं
तपः।
आप लोगों के साथ जो कुछ करें, अपने साथ करें। आप ही उन सब के रूप में खेल रहे हो, यह जानते हुए सब करें। आप एक परिच्छिन्न शरीर नहीं हैं। आप जो कुछ देख रहे हैं, अपने आपको ही देख रहे हैं, जिससे देख रहे हैं वह भी आप हैं और जिसको देख रहे हैं वह भी आप ही हैं। जिसके लिए देख रहे हैं वह भी आप हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वह भी आप हैं। ऐसा विशाल ज्ञान.... ! ऐसा विशाल प्रेम... ! इन दोनों का जब प्राकट्य होता है, तब आदमी अनन्त महासागर में सुखानुभूतियाँ करता है। संसार दुःखदायी नहीं। दुःखदायी अज्ञान है। संसार सुखदायी भी नहीं। सुखदायी भी अपनी मान्यताएँ हैं। संसार तो ईश्वरमय है। सुख दुःख तो मन की तरंगें हैं। संसार में सुख नहीं, सुख अपनी वासना के कारण है। वह सुखाभास होता है, वास्तविक सुख नहीं होता है। संसार में दुःख नहीं, दुःख अपनी मलिन वासनाओं के कारण है, अपनी बेवकूफी के कारण है। अपनी बेवकूफी मिटी तो न सुख है न दुःख है। सब परिपूर्ण परमात्मा है, आनन्द का भी आनन्द है। फिर हर हाल में खुश, हर में खुश, हर देश में खुश।
कुसंग से बचें। कुसंग माने संकीर्ण और कुवासना को पोसने में उलझे हुए लोगों का संग। ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव से बचकर सुसंग में रहें। श्रीकृष्ण ने एकान्त और अज्ञातवास में तेरह वर्ष बिताये थे अपने व्यापक स्वरूप में रमण करते हुए। 70 वर्ष की उम्र से लेकर 83 वर्ष की उम्र तक वे घोर अंगीरस ऋषि के आश्रम में अपने आत्मस्वरूप में मस्त रहे।
युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पड़ी तो उस पूर्णता में रमण करने वाले श्रीकृष्ण ने वह भी कर दिया। दुर्योधन की संकीर्ण दृष्टि तोड़नी थी, उसके निमित्त विश्व को सबक सिखाना था तो श्रीकृष्ण ने यह भी मजे से किया। दुर्योधन को ठीक कर दिया और उसके पक्षवालों को भी ठिकाने लगा दिया। फिर भी श्रीकृष्ण कहते हैं-
"युद्ध के मैदान में आने के पहले, संधिदूत होकर गया था तब से लेकर अभी तक मेरे हृदय में पाण्डवों के प्रति राग न रहा हो तो और कौरवों के प्रति मेरे चित्त में द्वेष न रहा हो तो इस समता की परीक्षा के निमित्त यह मृतक बालक (अभिमन्यु का नवजात पुत्र) जिन्दा हो जाय।" वह बालक जिन्दा हो गया। समता की परीक्षा के फलस्वरूप वह जिन्दा हुआ, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा।
आपके जीवन में समता आ जाय, ज्ञान आ जाय। राग से प्रेरित होकर नहीं, द्वेष से प्रेरित होकर नहीं..... सहज स्वभाव जीवन का क्रिया-कलाप चले।
सहजं
कर्म कौन्तेय
सदोषमपि न
त्यजेत्।
ज्ञानवान सदा सहज कर्म करते हैं। उनकी दृष्टि में दोषयुक्त या गुणयुक्त होना बच्चों का खिलवाड़ मात्र है। जैसे जल की तरंग कभी स्वच्छ तो कभी मलिन, कभी छोटी तो कभी मोटी होती है। यह जल की लीला मात्र है। ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप में बैठकर आपकी जो चेष्टा होगी, वह परम चैतन्य की आह्लादिनी लीला है। वह चैतन्य का विवर्त मात्र है। ऐसा समझकर ज्ञानी, जीवन्मुक्त पुरूष संसार में सुख से विचरते हैं।
सः
तृप्तो भवति
अमृतो भवति....।
सः
तरति लोकान्
तारयति....।।
'वे तृप्त होते है, अमृतमय होते हैं। वे तरते है, औरों को तारते हैं।'
ॐ
आनन्द....! ॐ
शान्ति.....!! सचमुच
परमानन्द....!!!
अन्दर बाहर वही का वही सुखस्वरूप मेरा परमात्मा है। अन्दर-बाहर, आगे-पीछे, अधः-ऊर्ध्व वही सारा का सारा भरा है। जैसे मछली के आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, अगल-बगल जल ही जलभरा है, मछली के पेट में भी जल है। इसी प्रकार आपके आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, अन्दर-बाहर वही चिदाकाश परम चैतन्य परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा विशाल भाव, ज्ञान और व्यापक दृष्टि, इनकी एकता होती है तो अनेक में एक और एक में अनेक का साक्षात्कार हो जाता है।
परमात्मा सदा साक्षात् है। वह कभी दूर नहीं, कभी पराया नहीं। संकीर्णता और अज्ञान के कारण उसे हम दूर मान लेते हैं, पराया मान लेते हैं और अपने को अनाथ मान लेते हैं। तुम अनाथ नहीं हो। सर्वनियन्ता नाथ, विश्वेश्वर तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है। विश्वनियन्ता नाथ ही तुम्हारे आगे अनेक रूप होकर बैठा है। विश्वनियन्ता परमात्मा ही तुम्हारे आगे सुख और दुःख के स्वांग करके तुम्हें अपनी असलियत को जतलाने का यत्न कर रहा है।
अतः जो प्रतिकूलता आ रही है उसे धन्यवाद दो और कहो कि यार ! तू मुझे धोखा नहीं दे सकता।
दूसरे विश्वयुद्ध के दौर में सन् 1942 की एक घटना है।
किसी जीवन्मुक्त महापुरूष ने संकल्प कर लिया कि सब तू ही है तो अब बोलेंगे नहीं। जीवन के अंतिन श्वास के क्षण कुछ बोल लेंगे तो बोल लेंगे।
दूसरे विश्वयुद्ध में सैनिकों के द्वारा जासूसी के शक में वे पकड़े गये। पूछने पर कुछ बोले नहीं तो और सन्देह हुआ। ले गये अपने मेजर के पास। डाँट-डपटकर उनसे पूछा गयाः "तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ?" आदि आदि। जबरदस्ती करने के कई तरीके आजमाये गये लेकिन इन महापुरूष ने संकल्प कर रखा था। जीवन्मुक्त को भय कहाँ ? वे जानते थे किः "डाँटने वालों में भी मेरी ही चेतना है। शरीर का जैसा प्रारब्ध होगा वैसा ही होकर रहेगा। भयभीत क्यों होना ? उनके प्रति उद्विग्न क्यों होना ?"
महात्मा ज्यों के त्यों खड़े रहे। पूछने वाले पूछ-पूछकर थक गये। आखिर सूचना दी गई कि अगर नहीं बोलोगे तो गले में भाला भोंक देंगे... सदा के लिए चुप कर देंगे।
फिर भी महात्मा शांत....। उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। उन मूर्ख लोगों ने उठाया भाला। महात्मा के कण्ठकूप में भाले की नोंक रखी। फिर भी जीवन्मुक्त पुरूष को भय नहीं लगा। वे जानते थे कि सब परमात्मा की आह्लादिनी लीला है। जैसे सागर में तरंगे होती हैं, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा में सब लीलाएँ हो रही हैं।
आखिर उस क्रूर मेजर ने सैनिकों को आदेश दे दिया। भाला गले में भोंक दिया गया। रक्त की धार बही। तब वे महात्मा अमृतवचन बोलेः
"यार ! तू सैनिक बनकर आयेगा, भाला बनकर आयेगा, तो भी अब मुझे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं पहचानता हूँ कि उसमें भी तू ही तू है। शरीर का अन्त जिस निमित्त से होने वाला है, वह होगा लेकिन अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता।"
चैतन्यरूपी सागर की सब तरंगे हैं। ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, ना कोई अपना ना कोई पराया। सब परमेश्वर ही परमेश्वर है.... नारायण ही नारायण है। मेरा चैतन्य आत्मा-परमात्मा ही सब कुछ बना बैठा है। ॐ....ॐ....ॐ..... नारायण.... नारायण..... नारायण... तू ही तू.... तू ही तू....।
ऐसे विशाल ज्ञान और विशाल हृदय वाले ज्ञानवान को मृत्यु भी दिखती है तो समझते हैं कि : मृत्यु भी तू ही है। यमदूत भी तू ही है और पार्षद भी तू ही है। वैकुण्ठ भी तुझ ही में है, स्वर्ग भी तुझ ही में है और नर्क भी तुझ ही में है।
जिसके लिये स्वर्ग और नर्क अपना आपा हो गया, उसके लिए स्वर्ग का आकर्षण कहाँ और नर्क का भय कहाँ ? उसके लिये परमात्मा ही परमात्मा है।
"ॐ....ॐ....ॐ.... आनन्द.... खूब आनन्द.... विशाल हृदय, विशाल ज्ञान... दिव्य ज्ञान... विशाल प्रेम.... ॐ....ॐ..... सर्वोऽहम्... सुखस्वरूपोऽहम्। मैं सर्व हूँ.... मैं सुख स्वरूप हूँ.... मैं आनन्दस्वरूप हूँ... मैं चैतन्यरूप हूँ... ।"
सेवा इस आत्मज्ञान को व्यवहार में ले आती है। भावना इस आत्मज्ञान को भावशुद्धि में ले आती है। वेदान्त इस जीवन को व्यापक स्वरूप से अभिन्न बना देता है।
इस विशाल अनुभव से चाहे हजार बार फिसल जाओ, डरो नहीं। चलते रहो इसी ज्ञानपथ पर। एक दिन जरूर सनातन सत्य का साक्षात्कार हो जायेगा। दृष्टि जितनी विशाल रहेगी, मन जितना विशाल रहेगा, बुद्धि जितनी विशाल रहेगी, उतना ही विशाल चैतन्य का प्रसाद प्राप्त होता है। उस प्रसाद से सारे दुःख दूर हो जाते हैं।
जगत में जो भी दुःख हैं, सारे अज्ञानजनित हैं, संकीर्णताजनित हैं, बेवकूफीजनित हैं। वास्तव में दुःख का कोई अस्तित्व नहीं और सुख कोई सार चीज नहीं। परमात्मा तो परमानन्द हैं, परम सुखस्वरूप हैं। जहाँ सुख और दुःख दोनों तुच्छ दिखते है, ऐसा शांत चैतन्य आत्मा अपना स्वरूप है।
हवा चलती है तभी भी हवा है और स्थिर है तभी भी हवा है। ऐसे ही परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति से जगत बनते हैं और मिटते हैं। जगत की स्थिति में भी वही आनन्दघन परमात्मा है और जगत के प्रलय में भी वही परमात्मा। प्रवृत्ति में भी वही है और शान्त भाव में भी वही है।
ऐसा जो जानता है, वह वास्तविक में जानता है। ऐसा जो देखता है, वह वास्तविक में देखता है। ऐसा जो सोचता है, वह वास्तविक में सोचता है। ऐसा जो समझता है, वही वास्तविक में समझदार है। बाकी सब नासमझों का खिलवाड़ है।
ॐ.....ॐ.....ॐ......
खूब आनन्द....! मधुर आनन्द.....!! परमानन्द....!!!
शांति ही शांति...... ! आनन्द ही आनन्द.......... !!
निश्चिन्त नारायण स्वभाव.......! ॐ....ॐ.....ॐ....।
जो लोग बाहर की चीजों में, मेरे तेरे में उलझे हैं, उनके लिए शास्त्र विधान करते हैं कि इतने इतने सत्कर्म करो तो भविष्य में स्वर्ग मिलेगा। कुकर्म करोगे तो नर्क मिलेगा।
जिनको ज्ञान में रूचि है, ईश्वरत्व के प्रकाश में जो जीते हैं, उनको कुछ करके स्वर्ग में जाकर सुख लेने की इच्छा नहीं। नर्क के दुःख के भय से पीड़ित होकर कुछ करना नहीं। वे तो समझते हैं कि सब मेरे ही अंग है। दायाँ हाथ बायें की सेवा कर ले तो क्या अभिमान करे और बायाँ हाथ दाहिने हाथ की सेवा कर ले तो क्या बदला चाहेगा ? पैर चलकर शरीर को कहीं पहुँचा दे तो क्या अभिमान करेंगे और मस्तिष्क सारे शरीर के लिए अच्छा निर्णय ले तो क्या अपेक्षा करेगा ? सब अंग भिन्न भिन्न दिखते हैं फिर भी हैं तो सभी एक शरीर के ही।
ऐसे ही सब जातियाँ, सब समाज, सब देश भिन्न-भिन्न दिखते हैं, वे सत्य नहीं हैं। जातिवाद सत्य नहीं है। स्त्री और पुरूष सत्य नहीं है। बाप और बेटा सत्य नहीं है। बेटा और बाप, पुरूष और स्त्री, जाति और उपजाति तो केवल तरंगें हैं। सत्य तो उनमें चैतन्यस्वरूप जलराशि ही है।
ॐ....ॐ...ॐ.... नारायण... नारायण....नारायण....
नारायण का मतलब है पूर्ण चैतन्य ही चैतन्य.....राम ही राम...आनन्द ही आनन्द....।
तुझमें
राम मुझमें
राम सबमें राम
समाया है ।
कर लो
सभी से प्यार
जगत में कोई
नहीं पराया है
।।
ॐ....ॐ....ॐ....
हे दुःख देने वाले लोग और हे दुःख के प्रसंग ! हे सुख देने वाले लोग और सुख के प्रसंग ! तुम दोनों की खूब कृपा हुई। दोनों ने मुझे यह ज्ञानरूपी फल दे दिया कि सुख भी सच्चा नहीं और दुःख भी सच्चा नहीं। सुख देने वाला भी सच्चा नहीं और दुःख देनेवाला भी सच्चा नहीं। सुख और दुःख देने वालों के मन की तरंगें ही थीं। मन की तरंगों का आधार मेरा चैतन्य आत्मदेव वहाँ भी पूर्ण का पूर्ण था। ॐ....ॐ.....ॐ..... नारायण.... नारायण.... नारायण....।
दिव्य आनन्द.....। मधुर आनन्द.... ! परमानन्द.... ! निर्विकारी आनन्द....! निरन्जन आनन्द...! ॐ.....ॐ.....ॐ....
नर-नारी में बसा हुआ... सुखी-दुःखी में बसा हुआ... अपने पराये में छुपा हुआ परमात्मा में छुपा हुआ भी है, जाहिर भी है.... अन्नत है... निर्विकार है.... निरंजन है....।
ऐसी
भूल दुनियाँ
के अन्दर
साबूत करणी
करता तू ।
ऐसो
खेल रच्यो
मेरे दाता
ज्यों देखूँ
वा तू को तू ।।
कीड़ी
में नानो बन
बैठो हाथी में
तू मोटो क्यूँ
?
बन
महावत ने माथे
बेठो हांकणवालो
तू को तू ।।
दाता
में दाता बन
बैठो भिखारी
के भेळो तू
।
ले
झोळी ने मागण
लागो
देवावाळो
दाता तू ।।
चोरों
में तू चोर बन
बेठो बदमाशों
के भेळो तू
।
कर
चोरी ने भागण
लागो पकड़ने
वाळो तू को तू ।।
नर
नारी में एक
विराजे
दुनियाँ में
दो दिखे क्यूँ ।
बन
बालक ने रोवा
लागो
राखणवाळो तू
को तू ।।
जल थल
में तू ही
विराजे जंत
भूत के भेळो
तू ।
कहत
कबीर सुनो भाई
साधो गुरू भी
बन के बेठो तू ।।
विशाल उदधि की जलराशि में भँवर भी तू ही है और तरंग भी तू ही है। बुलबुले भी तू ही है और जल के टकराने से बनने वाली फेन भी तू ही है। जल में पैदा होने वाली शैवाल भी तू ही है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
नास्तिक लोगों ने भगवान को नहीं देखा, नहीं जाना, इसलिए वे भगवान को नहीं मानते। आस्तिक लोग भगवान को मानते तो हैं, लेकिन वे भी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का आदर नहीं करते। रामतीर्थ कहा करते थेः "ये लोग भगवान को, खुदाताला को सातवें आसमान में स्थित मानते हैं। कम-से-कम खुदाताला पर इतनी तो दया करो कि सातवें आसमान में उसको कहीं ठण्ड न लग जाय !
भगवान केवल गौलोक में, साकेत में, वैकुण्ठ में या शिवलोक में ही नहीं है, अपितु वे तो सर्वत्र ओतप्रोत अनंत-अनंत ब्रह्माण्डों में फैले हैं। वे ही भगवान तुम्हारा आत्मा होकर बैठे हैं।
कल्पना करो कि हिमालय जैसा शक्कर का एक बड़ा पहाड़ है। शक्कर के इस पूरे हिमालय को एक चींटी जानना चाहे तो घूमते घूमते युग बीत जाय। अगर युक्ति आ जाय, वह पहाड़ पह जहाँ खड़ी है, वहीं शक्कर को चख ले तो उसी समय वहीं पर उसको शक्कर के सारे हिमालय का साक्षात्कार हो जाय।
हमारी वृत्ति ऐहिक जगत में सुख खोजती है। वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में, वैकुण्ठ में या शिवलोक में जाकर सुखी होने की कल्पना में उलझती है। इस उलझन से हटकर वृत्ति जहाँ से उठती है, वहीं अपने अधिष्ठान को जान ले तो स्वयं सुखस्वरूप हो जाय। जहाँ वह खड़ी है, वहीं उसकी यात्रा पूरी हो जाय। 'वहाँ जाऊँ... यह पा लूँ.... वह कर लूँ.... तो सुखी हो जाऊँ....' यह जो मन में कल्पना घुसी है, अज्ञान घुसा है, इस अज्ञान को आत्मज्ञान से मिटाकर जीव जब अपने-आप में जाग जाता है तो पूर्ण सुख का और पूर्ण निर्भयता का अनुभव हो जाता है। निर्भीक विचार करने से ही निर्भीकता का अनुभव हो जाता है। मुक्ति का विचार करने से ही अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव होता है। दुःख बन्धन और भय के विचार करने से अपनी हानि होती है।
हमारे मन में अदभुत शक्ति है। मन की कल्पनाओं से ही हम संसार में उलझते हैं। जीव सदा चिन्तित-भयभीत रहता है कि मेरा यह हो जायगा तो क्या होगा... वह हो जायगा तो क्या होगा....? ऐसी कल्पना करके दुःखी क्यों होना ? सदा निश्चिन्त रहना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता।
आदमी जैसा भीतर सोचता है, वैसी ही आभा उसके शरीर के इर्द-गिर्द बनती है, फैलती है। बाह्य वातावरण से ही सजातीय संस्कारों को भी आकर्षित करती है। आप मुक्ति के विचार करते हो तो मुक्ति का आन्दोलन और आभा बनती है। मुक्त पुरूषों के विचार आपको सहयोग करते हैं। आप भय और बन्धन के विचार करते हो तो आपकी आभा वैसी ही बनती है। अगर आप घृणा के विचार करते हो, चोरी और डकैती के विचार करते हो ‘कि कहीं चोरी न हो जाए....डाका न डाला जाए…..!’ तो आपकी वही आभा चोरों और डकैतों को चोरी डकैती के लिए आमंत्रित करती है। आपकी आभा सुन्दर और सुहावनी है तो उसी प्रकार की आभा और विचार आपकी ओर खिंच जाते हैं।
मेरे पास एक जेबकतरा आया। अपनी ब्लेड तोड़कर मेरे पैरों में रख दी और हाथ जोड़कर बोलाः "स्वामी जी ! आप आशीर्वाद दो कि मुझे रिक्शा मिल जाय और मैं अच्छा धन्धा करूँ। आपके सत्संग में आया तब से निश्चय किया कि अब पाप का धन्धा नहीं करूँगा।"
"क्या धन्धा करता था ?"
"जेबकतरा था।"
"अब तो छोड़ दिया है न ?"
"हाँ स्वामी जी !"
"अच्छा... अब सच बताओ कि तुमको कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं ?"
"स्वामी जी ! यह तो सीधी सी बात है। जिनके पास पैसे होते हैं, उनका हाथ बार-बार जेब पर जाता है। वे भयभीत रहते हैं कि जेब कहीं कट न जाय... कट न जाय...। हमे इससे आमंत्रण मिल जाता है कि यहीं ब्लेड घुमाना चाहिए।"
दूसरा एक लड़का आता था पालनपुर से। अहमदावाद आश्रम में आने के लिए उसने ट्रेन का पास निकलवाया था। उसने मुझसे कहा किः "स्वामी जी ! मैं हमेशा अहमदावाद आता जाता हूँ, कभी मेरी टिकट चेक नहीं होता। लेकिन जिस दिन मैं पास घर पर भूल आता हूँ या पास की अवधि पूरी हो जाती है, तभी टी.टी.ई. मेरा चेकिंग करते हैं और मैं फँस जाता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग योग, ध्यान आदि तो कुछ करते नहीं, सिगरेट पीते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि आज मेरे पास 'पास' नहीं है या उसकी तारीख खत्म हो चुकी है ?"
मैंने उसे समझायाः "टी.टी.ई. को तो पता नहीं चलता है लेकिन तेरे को पता होता है कि 'आज मैं पास भूल गया हूँ।' तेरे चित्त में डर रहता है कि, 'वह कहीं पूछ न लें.... पकड़ न लें।' तेरे इन विचारो की आभा तेरे इर्दगिर्द बनती है और टी.टी.ई. को आमंत्रित करती है कि इसकी तलाशी लो।"
तुम्हारे विचारों का ऐसा चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। तुम जब आत्मिक विचार करते हो, तब सर्वव्यापक ईश्वरतत्त्व में, गुरूतत्त्व में जो आत्मा की मुक्तता है, वह तुम्हें सहाय करती है। तुम जब दुःख, भय, बन्धन के विचार करते हो, तब वातावरण में जो हल्के विचार फैले हुए हैं, वे तुम्हें घेर लेते हैं और तुम अधिकाधिक गिरते ही चले जाते हो।
'मैं विश्वात्मा हूँ.... मेरा जन्म नहीं.... मेरी मृत्यु नहीं...' इस प्रकार का जो चिन्तन करता है, वह अपने शुद्ध 'मैं' में जाग जाता है। तुम्हारा मन एक कल्पवृक्ष है। बन्धन के विचार करने से अन्तःकरण बन्ध जाता है। अगर तुम अपने को बन्धनवाला मानते हो तो तुम किस बात से बँधे हो ? रूपयों से बँधे हो ? रूपये तो कई आये और चले गये। तुम अगर रूपयों से बँधे होते तो तुम भी चले जाते। मित्रों से बँधे हो ? कई मित्र बचपन में आये, किशोरावस्था में आये और जवानी में आये, बीत गये। आज वे नहीं हैं। कोई नहीं... कोई नहीं... सब बिखर गये। कपड़ों से बँधे हो ? बचपन से लेकर आज तक तुमने कई कपड़े बदल दिये। घर से बँधे हो ? नहीं। वास्तव में तुम किसी चीज से बँधे नहीं हो। अपनी महिमा तुम नहीं जानते, अपनी मुक्तता को तुम नहीं जानते, इसलिए चित्त के फुरने के साथ तुम जुड़ जाते हो और बँध जाते हो।
किसी राजा ने संत कबीर जी से प्रार्थना की किः "आप कृपा करके मुझे संसार बन्धन से छुड़ाओ।"
कबीर जी ने कहाः "आप तो धार्मिक हो... हर रोज पंडित से कथा करवाते हो, सुनते हो..."
"हाँ महाराज ! कथा तो पंडित जी सुनाते हैं, विधि-विधान बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं... अपनी मुक्तता का अनुभव नहीं हुआ। आप कृपा करें।"
"अच्छा मैं कथा के वक्त आ जाऊँगा।"
समय पाकर कबीर जी वहाँ पहुँच गये, जहाँ राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे कबीर जी से कुछ लेना थ। कबीर जी का भी अपना आध्यात्मिक प्रभाव था। वे बोलेः
"राजन ! अगर कुछ पाना है तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।"
"हाँ महाराज !"
"मैं आपके ेतख्त पर बैठूँगा। वजीर को बोल दो कि मेरी आज्ञा का पालन करे।"
राजा ने वजीर को सूचना दे दी कि अभी ये कबीर जी राजा है। वे जैसा कहें, वैसा करना।
कबीर जी कहा कि एक खम्भे के साथ राजा को बाँधो और दूसरे खम्भे के साथ पंडित जी को बाँधो। राजा ने समझ लिया कि इसमें अवश्य कोई रहस्य होगा। वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खम्भों से बाँध दिया गया। कबीर जी पंडित से कहने लगेः
"देखो, राजा साहब तुम्हारे श्रोता हैं। वे बँधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो।"
"महाराज ! मैं स्वयं बँधा हुआ हूँ। उन्हें कैसे खोलूँ ?"
कबीर जी ने राजा से कहाः "ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं। वे बँधे हुए हैं। उन्हें खोल दो।"
"महाराज ! मैं स्वयं बँधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोलूँ ?"
कबीर जी ने समझायाः
बँधे
को बँधा मिले
छूटे कौन उपाय ।
सेवा
कर निर्बन्ध
की पल में दे
छुड़ाय ।।
'जो पंडित खुद स्थूल 'मैं' में बँधा है, सूक्ष्म 'मैं' में बँधा है, उसको बोलते हो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो ? स्थूल और सूक्ष्म अहं से जो छूटे हैं, ऐसे निर्बन्ध ब्रह्मवेत्ता की सेवा करके उन्हें रिझा दो तो बेड़ा पार हो जाय। वे तुम्हें उपदेश देकर पल में छुड़ा देंगे।"
मानो, कोई भगवान आ भी जाय तुम्हारे सामने, लेकिन जब तक आत्मज्ञानी गुरू का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक सब बंधन नहीं कटेंगे। आनन्द आयेगा, पुण्य बढ़ेंगे, पर आत्मज्ञान की कुंजी के बिना जीव निर्बन्ध नहीं होगा।
दुर्योधन और शकुनि ने श्रीकृष्ण के दर्शन किये थे। ईश्वर प्राप्ति की लगन न होने के कारण उन्होंने फायदा नहीं उठाया। महावीर को कई लोगों ने देखा था, मुहम्मद के साथ कई लोग रहते थे। जीसस जब क्रॉस पर चढ़ाये जा रहे थे तब तालियॉं बजाने वाले, मजा लेने वाले एक लाख लोग उपस्थित थे। जीसस के हाथों पर कीलें ठोंके जा रहे थे और लोग देख रहे थे।
संत भगवंत के दर्शन और सान्निध्य का पूरा लाभ तब होगा जब उनका आत्मज्ञान -परक उपदेश सुनकर आप निर्भय तत्त्व में अपने ‘मैं’ की स्थिति करेंगे। इसके लिए चाहिए उत्कण्ठा.. इसके लिए जिज्ञासा... इसके लिये चाहिए सदगुरूओं का कृपा प्रसाद, प्राप्त हो ऐसा आचरण और व्यवहार।
गुरूओं का ज्ञान यह है कि तुम निर्भीकता के विचार करो। निर्भीकता वह नहीं, जो दूसरों का शोषण करे। जो दूसरों का शोषण करता है, दूसरों को डराता है, वह स्वयं भयभीत रहता है। न आप भयभीत हो और न दूसरों को भयभीत करो। आप निर्भय रहो और दूसरों को निर्भय बनाओ। आप निर्द्वन्द्व बनो और दूसरों को निर्द्वन्द्व तत्त्व में ले जाओ। आप जो बाँटोगे, वह वापस मिलेगा। आप निर्भयता के विचार करो। अपने निर्भयस्वरूप की ओर निगाह रखो।
सुनी है एक कहानी। एक ब्रह्मवेत्ता सूफी फकीर अपने प्यारे शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में बढ़िया माहौल देखा... खुला आकाश.... शांत वातावरण.... निर्जन वन का एकांत स्थान.... बैठ गये ध्यान में। कुछ समय बीता। पास के भयानक जंगल में शेर दहाड़ने लगा। बाबाजी तो समाधि में थे, लेकिन चेला जी तो थर-थर काँपने लगे। शेर की आवाज नजदीक आने लगी।
चेला जी चढ़ गये पेड़ पर। शेर आकर गुरूजी के अंगों को सूँघता हुआ आगे चला गया। कुछ समय बीता। गुरूजी ध्यान से जागे। चेला भी नीचे उतरा। काँप रहा था। अभी भी। गुरूजी बोलेः
"क्या हुआ ?"
"गुरूजी ! शेर आया था। आपको सूँघकर चला गया।"
अब दोनों आगे चलने लगे। इतने में गुरूजी को मच्छर ने काटा। गुरूजी ने 'आहा...' करके मच्छर को उड़ाया। चेला बोलाः
"जब शेर आया तो आप चुपचाप बैठे रहे और मच्छर ने काटा तो...."
गुरूजी ने कहाः "जब शेर आया तब मैं अपने शुद्ध "मैं" में था। अब मेरी वृत्ति इस हाड़-मांस के देह में आ गई है, इसलिए मच्छर ने काटा तो भी आह निकल रही है।"
एक बाबाजी कथा कर रहे थे। जोरों का आँधी-तूफान चलने लगा। श्रोता लोग भाग खड़े हुए क्योंकि छपड़े के टिन खड़खड़ा रहे थे, कहीं गिर न जायें ! जहाँ पक्का शेड था, वहाँ सब लोग चले गये। थोड़ी देर के बाद तूफान रूक गया। सब वापस आये। बाबाजी अपने आसन पर निश्चल विराजमान थे।
"बाबाजी ! हम तो भाग गये।आपको डर नही लगा कि यह छपडा गिर जाएगा ? टिन तूफान में खड़खड़ा रहे थे...।आ क्यों नही भागे गुरूजी ?” गुरूजी ने कहा : “तुम भी भागे, हम भी भागे। तुम तो आर.सी.सी. के शेड के नीचे भागे और मैं अपने शुद्ध 'मैं' में भागा, इसलिए निर्भय हो गया।"
अतः जब जब डर लगे, तब अपने शुद्ध 'मैं' की ओर भाग जाओ। हो-होकर क्या होगा ? मैं निर्भीक हूँ। ॐ....ॐ.....ॐ..... मैं अमर आत्मा हूँ....हरि.... ॐ....ॐ....ॐ....।
मौत के समय हाय-हाय करके डरोगे तो गड़बड़ हो जायगी... मौत बिगड़ जायगी। मौत को भी सुधरना है। मौत तो आयेगी ही। चाहे कितनी भी सुरक्षाएँ कर लो। मौत आये तब सोचो... समझो मैं निर्भीक हूँ। मौत मेरी नहीं होगी, शरीर की होगी। शरीर की मौत को देखना है। जैसे शरीर के कोट, पेन्ट, शर्ट को देखते हैं, ऐसे शरीर की मौत को भी देख सकते हैं। जो मौत के समय सावधान हो जाय, निर्भीक हो जाये, उसकी दुबारा कभी मौत नहीं होती। वह अमर आत्मा में जाग जाता है। यह काम तो अवश्य करना है। दूसरा काम हो चाहे न हो, चल जायगा।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
जब-जब दुःख हो, परेशानी हो, भय हो, तब समझ लेना कि यह अज्ञान की उपज है। कहीं न कहीं नासमझी को पकड़ा है, इसलिए दुःख होता है। विकार उठे तो समझ लो कि नासमझी है, इसलिए बह गये हो विकार में। फिर बहते ही न रहो, सावधान हो जाओ। विकारों ने सबक सिखा दिया कि इसमें कोई सार नहीं। परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं है।क्रोध ने सिखा दिया कि इसमें हानि के सिवाय और कुछ नहीं है। मोह ने सिखा दिया कि इसमें मुसीबत के सिवाय और कुछ नहीं है।
काम शाश्वत नहीं है, राम शाश्वत है। काम आया और गया, लेकिन राम तो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। अपने राम स्वभाव को जानो.... अपने शांत स्वभाव को जानो... अपने अमर स्वभाव को जानो, अपने चिदघन चैतन्य राम को जानो। उस राम को जाननेवाला राम से अलग नहीं रहता। वह राममय हो जाता है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
संगदोष जैसी बुरी चीज संसार में और कोई नहीं है। भीड़-भाड़ में, विकारी लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं। एकान्त में रहना चाहिए या भगवान की मस्ती में मस्त रहने वाले उच्च कोटि के साधकों के बीच रहना चाहिए। वे साधक महसूस करते हैं कि अब इन्द्रियों के प्रदेश में ज्यादा घूमना, जीना अच्छा नहीं लगता। इन्द्रियातीत आत्मभाव में ही सच्चा सुख है। जान लिया कि संसार के कीचड़ में कोई सार नहीं, जान लिया कि तरंग बनकर किनारों से टकराने में कोई सार नहीं... अब तो मुझे जलराशि में ही, आत्मानन्द के महासागर में ही अच्छा लगता है। अब तो ऐसा लगता है किः
"मिल
जाय कोई पीर
फकीर पहुँचा
दे भव पार....।"
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
अनुभवी आदमी प्रकृति की एकाध थप्पड़ से चेत जाता है और नहीं चेतेगा तो दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी। संसार में थप्पड़ मार-मरकर प्रकृति तुम्हें परमात्मा में पहुँचाना चाहती है। समझकर पहुँचना है तो तुम्हें हँसते-खेलते हुए पहुँचा देने के लिए वह प्रकृति देवी तैयार है। अगर नहीं मानते हो, संसार में मोह ममता करते हो तो मोह-ममता की चीजें छीनकर, थप्पड़ें मारकर भी तुम्हें जगाने के लिए वह प्रकृति देवी सक्रिय है। वह है तो आखिर परमात्मा की ही आह्लादिनी शक्ति। वह तुम्हारी शत्रु नहीं है, शुभचिन्तक है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
तर्क्यताम्....
मा
कुतर्क्याताम्
आजकल के किसी सुधारक नास्तिक की पढ़ी-लिखी लड़की किसी सत्संग के घर शादी करके गई। सास ने कहाः "बहू ! चलो मंदिर में देवदर्शन करें।"
"हाँ हाँ....कभी चलेंगे। आज तो मुझे पिक्चर देखने जाना है।"
"बेटी ! देवदर्शन करो तो जीवन का कल्याण होवे। पिक्चरों से तो आँखों की शक्ति क्षीण होती है। बन्द थियेटरों में ऐसे वैसे लोगों के श्वासोच्छावास, अपानवायु, बदबू की अशुद्धि प्रचुर मात्रा में होती है। अशांति और विलास के वायब्रेशन अपना अंतःकरण मलिन करते हैं।"
"माता जी ! आप चिन्ता मत करो। हमें तो मजा आता है। आप मंदिर में जाओ। मैं परसों-तरसों आपके साथ चलूँगी। आज तो....।"
इस प्रकार सास जी को टालते-टालते आखिर उस सुधारक के परिवार से आयी हुई आधुनिक लड़की ने एक दिन सासजी के साथ मंदिर जाना कबूल किया। उसने अपने नाज नखरों से पति को वश कर लिया था और सास को बेवकूफ मानती थी।
भगवान ने अक्ल तो दी है लेकिन भक्तों को बेवकूफ माननेवाली जो अक्ल है, वह देर सवेर नष्ट हो जाती है। तर्क ठीक है, लेकिन कुतर्क करके भक्त की श्रद्धा तोड़ना अथवा कुतर्क करके अपने विषय विकारों को पोसना, भक्ति और सदाचार के मार्ग को छोड़ देना, यह तो पूरे बिगाड़ की निशानी है।
नास्तिक सुधारक के घर में पनपी हुई वह फैशनेबल लड़की हार-शृंगार से देह को सजाकर मंदिर में गई। मंदिर का द्वार आते ही वह चीखी।
"मैं मर गई रे... मुझे बचाओ.... बचाओ... बड़ा डर लगता है !"
सास ने पूछाः "आखिर क्या हुआ ?"
"मुझे बहुत डर लगता है। मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे घर ले चलो। मेरा दिल धड़कता है... मेरा तन काँपता है।"
"अरे ! बोल तो सही, है क्या ?"
"वह देखो, मंदिर के द्वार पर दो-दो शेर मुँह फाड़कर खड़े हैं। मैं कैसे अंदर जाऊँगी ?"
सास ने कहाः "बेटी ! ये दो शेर हैं, लेकिन पत्थर के हैं। ये काटेंगे नहीं... कुछ नहीं करेंगे।"
वह लड़की अकड़कर बोलीः "जब पत्थर के शेर कुछ नहीं करेंगे तो मंदिर में तुम्हारा पत्थर का भगवान भी क्या करेगा ?"
उस पढ़ी लिखी मूर्ख स्त्री ने तर्क तो दे दिया और भोले-भाले लोगों को लगेगा कि बात तो सच्ची है। पत्थर के सिंह काटते नहीं, कुछ करते नहीं तो पत्थर के भगवान क्या देंगे ? जब ये मारेंगे नहीं तो वे भगवान सँवारेंगे भी नहीं। उस कुतर्क करने वाली लड़की को पता नहीं कि पत्थर के सिंह बिठाने की और भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा जिन ऋषियों ने दी है, वे ऋषि-महर्षि-मनीषियों की दृष्टि कितनी महान और वैज्ञानिक थी ! पत्थर की प्रतिमा में हम भगवद् भाव करते हैं तो हमारा चित्त भगवदाकार होता है। पत्थर की प्रतिमा में भगवद भाव हमारे चित्त का निर्माण करता है, चैतन्य के प्रसाद में जागने का रास्ता बनाता है।
मूर्तिपूजा करते-करते, परमात्मा के गीत गाते-गाते मीरा परम चैतन्य में जाग गई थी। आखिर उस मूर्ति में समा गई थी। गौरांग समा गये थे जगन्नाथजी के श्रीविग्रह में। एक किसान की लड़की नरो श्रीनाथ जी के आगे दूध धरती थी। श्रीनाथ जी उसके हाथ से दूध लेकर पीते थे। थी तो वह भी मूर्ति।
तुम्हारे अन्तःकरण में कितनी शक्ति छिपी हुई है ! मूर्ति भी तुमसे बोल सकती है। इतनी तो तुम्हारे चित्त में शक्ति है और चित्त के अधिष्ठान में तो अनंत-अनंत ब्रह्माण्ड विलसित हो रहे हैं। यह ज्ञान जगाने के लिए मंदिर का देवदर्शन प्रारंभिक कक्षा है। भले बाल मंदिर है, फिर भी अच्छा ही है।
उस मूर्ख लड़की से कहना चाहिएः "जब तू चलचित्र देखकर हँसती है, नाचती है, रोती है, हालाँकि प्लास्टिक की पट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है, फिर भी ‘आहा..... अदभुत...’ कहकर तू उछलती रहती है। परदे पर तो कुछ नहीं, सचमुच में गुन्डा नहीं, पुलिस नहीं... पुलिस के कपड़े पहन कर अभिनय किया है। रिवोल्वर भी सच्ची नहीं होती। फिर भी गोली मारते हैं, किसी को हथकड़ियाँ लगती हैं, डाकू डाका डालकर भागता है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ती हैं। ड्रायवर स्टीयरिंग घुमाते हैं..... ॐऽऽऽऽ.....ॐ, तब तुम सीट पर बैठे-बैठे घूमते हो कि नहीं घूमते हो ? जबकि पर्दे पर प्रकाश के चित्रों के अलावा कुछ नहीं है।
ऐसा झूठा चलचित्र का माहौल भी तुम्हारे दिल को और बदन को घुमा देता है तो ऋषियों के ज्ञान और उनके द्वारा प्रचलित मूर्तिपूजा भक्तों के हृदयों को भाव से, प्रार्थना से, परमात्म-प्रेम से भर इसमें क्या आश्चर्य है ?
ब्रह्मवेत्ता ऋषि-महर्षियों द्वारा रचित शास्त्रों के अनुसार मंत्रानुष्ठान पूर्वक विधि सहित मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर वेदोक्त-शास्त्रोक्त विधि के अनुसार प्राण-प्रतिष्ठा होती है। वहाँ साधु-संत-महात्मा आते जाते हैं। मूर्ति में भगवदभाव के संकल्प को दुहराते हैं। हजारों-हजारों भक्त अपनी भक्ति-भावना का अभिषेक उस देव मूर्ति में करते हैं ।ऐसी मूर्ति से भाविक भक्तों को अमूर्त तत्त्व का आनन्द मिल जाय, तो इसमें क्या सन्देह है ?
बड़े बड़े मकानों में रहने वाले सभी लोग सही माने में बड़े नहीं होते। बड़ी-बड़ी कब्रों के अन्दर सड़ा गला मांस और बदबू होती है, बिच्छू और बैक्टीरिया ही होते हैं। बड़ी गाड़ियों में घूमने आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ी कुर्सी पर पहुँचने से भी वह बड़ा नहीं होता। अगर बड़े से बड़े परमात्मा के नाते वह सेवा करता है, उसके नाते ही अगर बंगले में प्रारब्ध वेग से रहता है तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन चीजों के द्वारा जो परमेश्वर का घात करके अपने अहं को पोसता है, वह बड़ा नहीं कहा जाता।
एक ऐसा ही बड़ा कम्युनिस्ट आदमी था। वह मानता था कि भगवान आदि कुछ नहीं होते। वह अपने-आपको कुछ विशेष व्यक्ति मानता था। उसके पास तर्कशक्ति थी, जिसका उपयोग करके वह श्रद्धालु भक्तों की श्रद्धा तोड़ने की हरकतें बेखटके किया करता था। परन्तु बड़े-से-बड़े विश्वनियन्ता विश्वेश्वर की लीला अनूठी है। किस आदमी को कैसे मोड़ना, वह जानता है।
उस कम्युनिस्ट का एक लड़का था। वह अच्छे संग में रहता था। उसका मित्र उसे किसी महात्मा के सत्संग में ले गया। बचपन से ही उसके चित्त में अच्छे सात्त्विक संस्कार पड़ चुके थे। उसे भक्ति, सत्संग, कीर्तन, देवदर्शन में रस आता था। बेटा पूरा आस्तिक था और बाप पूरा नास्तिक। धीरे-धीरे वह सदभागी बेटा बड़ा हुआ।
एक दिन बाप ने उसे डाँटाः "सत्संग, मंदिर आदि में जाकर तू समय क्यों खराब करता है ? भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। यह तो साधु, महाराज, मुल्ला, मौलवी और पादरियों ने अपना धन्धा चलाने के लिए एक प्रकार की धूम मचा दी है, बाकी भगवान है नहीं।"
पुत्र ने कहाः "पिताजी ! कोई चीज बनी हुई होती है तो जरूर उसका कोई बनाने वाला भी होता है। ऐसे ही इतनी बड़ी दुनिया है तो जरूर उसका कोई बनाने वाला भी होगा।"
पिता ने कहाः "जा, पागल कहीं का। गर्मी और गति से यह सारा विश्व बन जाता है। जैसे गर्मी से पानी वाष्पीभूत हुआ, बादलों में गति हुई और फिर कहीं जाकर बरसे।
हिमालय में बर्फ थी। उसे सूर्य की गर्मी मिली। बर्फ पिघली। फिर उसमें गति आई। वही पानी गंगा होकर समुद्र में जा मिला। इस प्रकार गर्मी और गति से यह सारी दुनिया बनी है।
जैसे घड़ी के अलग-अलग पुर्जे मिला दिये। उसको सेल से जोड़ दिया। गर्मी मिली। उसके काँटों में गति आई। घड़ी समय बताने लगी। घंटी भी बजने लगी। खुद घूमती भी है, बोलती भी है और समय बिताकर लोगों को दौड़ाती भी है। कौन सा भगवान है इस दुनियाँ में ? छोड़ो यह सारा पागलपन। गर्मी और गति से ही यह संसार बन गया और चल रहा है।"
समय होने पर लड़का स्कूल में गया। जो साधक होता है, वह करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहता है। उसके स्वभाव में यह स्वाभाविक ही आ जाता है। इस प्रकार जिसका चित्त दक्ष और सात्त्विक श्रद्धा से युक्त रहता है, उसमें शान्ति और दिशासूचकता सहज ही आ जाती है।
लड़के ने एक कागज लिया। उस पर सुन्दर सुहावना चित्र बनाया और स्कूल से आकर पिता के कमरे में वह चित्र रख दिया। पिताजी दफ्तर से लौटे तो चित्र देखकर उनकी विचित्र खोपड़ी में भी आनन्द और आश्चर्य के भाव उभरने लगे। पूछाः
"मेरे कमरे में यह चित्र किसने रखा है ?"
"पिता जी ! मैंने रखा है।" बेटे ने कहा।
"किसने बनाया है ?"
"यह बनाया किसी ने भी नहीं है।"
"तो यह बना कैसे ?"
"पिता जी ! स्कूल में कागज का रिम (जिस्ता) पड़ा था। उसमें से एक कागज गति शक्ति से उड़कर मेज पर आ गया। स्याही मेज पर पड़ी थी जो गर्मी शक्ति से कागज पर ढुल गयी। इस प्रकार गर्मी और गति शक्ति दोनों मिल गई तो हो गया चित्र तैयार।"
पिता गरज उठाः "तू मुझे मूर्ख बनाता है ? गति शक्ति से रिम में से कागज मेज पर आ जाय, गर्मी शक्ति से स्याही दवात में से कागज पर ढुल पड़े और ऐसा सुन्दर चित्र अपने-आप बन जाय, यह असंभव है। तूने, तेरे दोस्त ने या तेरे मास्टर ने, किसी ने तो यह चित्र बनाया ही होगा।"
"नहीं नहीं पिता जी ! इस चित्र को बनाने वाला कोई नहीं है।
यह सब बेवकूफों की बात है। गर्मी और गति से ही यह बना है। रिम में से कागज आ गया और दवात से स्याही आ गई मेज पर। गर्मी और गति की मुलाकात होते ही चित्र बन गया।"
"यह असंभव है।" पिता घुर्राकर बोला।
"जब एक चार पैसे का चित्र अपने आप बनना असंभव है तो यह चित्र-विचित्र ब्रह्माण्ड भगवान के बनाने के सिवाय कैसे संभव हो सकता है ?
जो लोग कहते हैं कि ‘ईश्वर नहीं है’ उनको धन्यवाद दे दो उनकी फालतू खोजबीन के परिश्रम के लिए। वे विशेष प्रकार के मूर्ख हैं। ‘ईश्वर नहीं है’ ऐसा वही आदमी कह सकता है जिसने ईश्वर की खोज के लिए चौदह भुवन छान मारे हों, पृथ्वी के कण-कण की, अणु-परमाणु की जाँच कर ली हो, अतल, वितल, तलातल, रसातल,पाताल आदि सब लोक-लोकान्तर जाँच लिये हों, जो सृष्टि के आदि में हो और सृष्टि के अंत के बाद भी रहा हो। इस प्रकार सर्व काल और सर्व देश में जाँच करके ही कोई निर्णय कर सकता है कि ईश्वर है या नहीं। सृष्टि की आदि में माने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसका होना संभव नहीं, सृष्टि का अंत उसने देखा नहीं, देखेगा भी नहीं क्योंकि सृष्टि के अंत के पहले ही उसका अंत हो जायगा। पचास-पचहत्तर वर्ष की उम्रवाला ऐसा आदमी कह दे कि 'ईश्वर नहीं है' तो यह कहाँ की बुद्धिमानी है ?
'गर्मी और गति से सब बन गया है' यह आपकी मान्यता भूल भूलैया में भटकी हुई है। यह घड़ी जो चल रही है उसके पुर्जे भी किसी ने बनाये हैं, सेल भी किसी ने बनाया है। पुर्जों को जोड़ने वाला और सेल लगाने वाला भी तो कोई अवश्य है। उसको भी सत्ता देने वाला ईश्वर है, परमात्मा है।"
एक अच्छा चित्रकार प्रभातकाल में घूमने गया। प्राकृतिक सौन्दर्य का बड़ा चहेता था। प्रकृति के सुन्दर मनोरम्य दृश्यों को अपनी चित्रकला में उतरता था।
सूर्योदय हो रहा था... विशाल मैदान में हरियाली छाई हुई थी। दूर-सुदूर सुहावनी पहाड़ी दिख रही थी। कल-कल, छल-छल आवाज करती नदी बह रही थी। प्रकृति-प्रेमी कलाकार की कला जाग उठी। उस मनभावन दृश्य का सुंदर चित्र बना दिया। फिर सोचाः
'इस सन्नाटे में प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखने वाला तो मैं यहाँ हूँ लेकिन इस चित्र में दृश्य देखने वाला कोई नहीं है। दृश्य का दृष्टा तो होना ही चाहिए।' उसने दूसरा चित्र बनाया, जिसमें दृश्य को देखने वाला दृष्टा भी चित्रित किया। फिर सोचाः 'सुंदर दृश्य को देखता हुआ दृष्टा तो चित्र में आ गया लेकिन इस दृश्य और दृष्टा के चित्र को देखने वाला मैं रह गया। इस चित्र का भी दृष्टा होना चाहिए। अतः उसने तीसरा चित्र बनाया जिसमें दृश्य को देखने वाला दृष्टा और उन दोनों को देखने वाला दूसरा दृष्टा भी था। फिर सोचा कि इन तीनों को देखने वाला जो है, वह इस चित्र में नहीं है। उसे भी चित्रित करना चाहिए।
अब उसके विचारों में गड़बड़ बढ़ गई। दूसरे दृष्टा को देखने वाला तीसरा, तीसरे को देखने वाला चौथा, चौथे को देखने वाला पाँचवाँ... इस प्रकार हजारों-हजारों दृष्टा के चित्र बनेंगे, उनको भी देखने वाला दृष्टा बाकी रह जायेगा।
जिससे सब दिखता है वह दृष्टा, साक्षी तो असंग का असंग ही रह जाता है। चाँद-सितारे, दरिया, दरिया के किनारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि सब दृश्यों को, दृश्य देखने वाली इन्द्रियों को, मन को, मन के संकल्प-विकल्पों को, बुद्धि को, सुख-दुःख को देखने वाला कौन है ? मैं हूँ। इस 'मैं' का वास्तिक स्वरूप खोज लिया जाय, 'मैं' की वास्तविक पहचान हो जाय तो योगी का योग सिद्ध हो जाय, तपस्वी का तप सफल हो जाय, ज्ञानी का अपना स्वरूप प्रकट हो जाय।
यह भी
देख वह भी देख....
देखत
देखत ऐसा देख.
मिट
जाय धोखा रह
जाय एक।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
आस्तिक और नास्तिक में फर्क यह है कि आस्तिक एक ईश्वर की शरण लेता है और अपनी आवश्यकता पूरी करता है जबकि नास्तिक अनेक पदार्थों की आवश्यकता महसूस करता है। अपनी इच्छाएँ पूरी करते-करते कई जन्म बीत जाते हैं, सदियाँ समाप्त हो जाती हैं।
आवश्यकता तो आवश्यक तत्त्व की है और इच्छाएँ मन की दासता से पैदा होती हैं। आस्तिक एक परमात्मा की शरण लेता है और नास्तिक हजार-हजार वस्तुओं की शरण लेता है।
निःसहाय की सहाय है भगवद् शरण, भोगी का योग है भगवद् शरण, दुर्बल का बल है भगवद् शरण, निराधार का आधार है भगवदशरण। द्वन्द्वी का द्वन्द्वातीत जीवन है भगवद् शरण ! चिंतित की चिंता का निवारण है भगवद् शरण। बुद्धिशून्य की बुद्धि का प्रकाश है भगवद् शरण। बुद्धिमानों की बुद्धि का अहंकार उतारने वाला मंत्र है भगवद् शरण।
ज्ञानी के ज्ञान में निष्ठा उस भगवत्तत्त्व में होती है। उस तत्त्व में जब निष्ठा होती है तब योगी का योग फलता है, तपस्वी का तप फलता है, जपी का जप सार्थक होता है।
जीव जितना-जितना ईमानदारी से, सच्चाई से उस भगवत् शरण को ग्रहण करता है, उतना-उतना वह सफल होता जाता है। भगवद् शरण जितना-जितना छूटता जाता है, उतना-उतना उसके चित्त में बोझा बढ़ता जाता है।
असंख्य चित्त जिस चैतन्य से फुरफुरा रहे हैं, उस चैतन्य वपु परमात्मा के शरणागत कोई जीव किसी भी भाव से शरणागत होता है तो वह जीव आत्मप्रेरणा से, आत्मप्रकाश से और आत्मसहाय से कटीले मार्गों से, बीहड़ जंगलों से सफल यात्रा करके अपना जीवन धन्य कर लेता है। जिसके जीवन में भगवदशरण नहीं है, वह अपने बाहुबल से, अपने तपोबल से, अपने चित्तबल से, अपनी चापलूसी से या अपने और कोई तुच्छ बलों से सुखी रहने का यत्न तो करता है बेचारा प्राणी लेकिन उसे सुख चार कदम दूर ही भासता है। इच्छापूर्ति का क्षणिक हर्ष उसे आ जाता है, फिर इच्छाएँ भी अधिकाधिक भड़कती जाती हैं। इच्छा पूर्ति करते करते जीवन पूरे होते चले जाते हैं उस प्राणी के।
आस्तिक की आवश्यकताएँ होती हैं और नास्तिक की इच्छाएँ होती हैं। आवश्यकता एक होती है नित्य जीवन की, नित्य तृप्ति की, नित्य ज्ञान की, नित्य तत्त्व की। यह मनुष्य की आवश्यकता है और इच्छा मन का विलासहै।
हम लोग मन के विलास को जितना पोसते रहते हैं, उतना हम भीतर से खोखले हो जाते है। अपना व्यक्तिगत खर्च बढ़ाने से अहं की पुष्टि होती है। व्यक्तिगत खर्च घटाने से आत्मबल की पुष्टि होती है। अपनी व्यक्तिगत सेवा अपने आप करने से आत्मिक शक्ति का विकास होता है। दूसरों से व्यक्तिगत सेवा लेने से अहंगत सुख की भ्रांती होती है
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
सुख अगर अपने में फँसाता है तो वह दुःख भी खतरनाक है। दुःख अगर उद्वेग और आवेश देकर बहिर्मुख बनाता है, गलत प्रवृत्ति में घसीटता है तो वह पाप का फल है। दुःख अगर सत्संग में ले जाता है तो वह दुःख पुण्य का फल है। वह पुण्यमिश्रित पुण्य है।
जिसका शुद्ध पुण्य होता है, वह शुद्ध सुख में आता है। जिसका शुद्ध पुण्य होता है, उसको दुःख भी परम सुख के द्वार पर ले जाता है। पुण्य अगर पाप मिश्रित है तो सुख भी विकारी खड्डों में गिरता है और दुःख भी आवेश की गहरी खाइयों में गिराता है।
पुण्यात्मा सुख से भी फायदा उठाते हैं और दुःख से भी फायदा उठाते हैं। पापात्मा दुःख से ज्यादा दुःखी होते हैं और सुख में भी भविष्य के लिए बड़ा दुःख बनाने की कुचेष्टा करते हैं।
इसलिए परमात्मा को प्यार करते हुए पुण्यात्मा होते जाओ। परमात्मा के नाते कर्म करते हुए पुण्यात्मा होते जाओ। परमात्मा अपना आपा है, ऐसा ज्ञान बढ़ाते हुए महात्मा होते जाओ।
वस्त्र गेरूए बनाकर महात्मा होने को मैं नहीं कहता। एक आदमी अपने आपको विषय-विलास या विकार में, शरीर के सुखों में खर्च रहा है। वह गलत राह पर है। उसका भविष्य दुःखद और अन्धकार होगा। दूसरा आदमी सब कुछ छोड़कर निर्जन जंगल में रहता है, अपने शरीर को सुखाता है, मन को तपाता है। 'संसार में खराब है, मायाजाल है.... यह ऐसा है... वह ऐसा है.... इनसे बचो....' ऐसा करके जो बिल्कुल त्याग करता है... त्याग... त्याग... त्याग.. ज्ञान सहित त्याग नहीं बल्कि एक धारा में बहता चला जाता है, वह भी गलत रास्ते की यात्रा करता है।
बुद्धिमान तो वह है जो सब में सब होकर बैठा है उस पर निगाह डाले, मोह-ममता का त्याग करे, संकीर्णता का त्याग करे, अहंकार का त्याग करे, उद्वेग और आवेश का त्याग करे, विषय विकारों का त्याग करे। ऐसा त्याग तब सिद्ध होगा, जब आत्मज्ञान की निगाहों से देखोगे, ब्रह्मज्ञान की निगाहों से देखोगे।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
अनन्य
योग साधो
ऐसी कोई बूँद नहीं जो जल से भिन्न हो। ऐसा कोई जीव नहीं जो परमात्मा से भिन्न हो। ऐसी कोई तरंग नहीं जो बिना पानी के रह सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो चैतन्य परमात्मा के बिना रह सके।
सब घट
मेरा साँईया
खाली घट न कोय ।
बलिहारी
वा घट की जा घट
परगट होय ।।
छुपे हुए तुम्हारे परमात्मा को अनन्य भाव से, अनन्य योग से प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाओ। चालू व्यवहार में सावधान हो जाओ कि अज्ञान की पर्तें कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं ! अज्ञान की पर्तों को हटाते जाओ..... हटाते जाओ। सजगतापूर्वक... अन्य अन्य में जो अनन्य दिख रहा है उसमें प्रतिष्ठित होते जाओ।
अनन्याश्चिन्तयन्तो
मां ये जनाः
पर्युपासते ।
तेषां
नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं
वहाम्यहम् ।।
'जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझ परमेश्वर को निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा भावपूर्ण चिन्तन करने वाले पुरूषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ।'
(भगवद् गीताः९.२२ )
(पूज्य बापू के सत्संग प्रवचन से)
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ